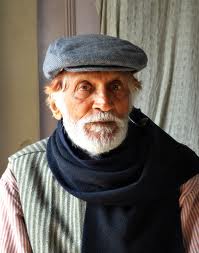|
कहानी संग्रह |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
अकर्मक क्रिया
कहानी संग्रह जन्म 10 जुलाई 1932, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
भूमिका
यों तो आम तौर पर मैं अपने कथा-संग्रह की भूमिका नहीं लिखता - महज पहला संग्रह
'दूसरे चेहरे', जो सन बहत्तर में 'नीलाभ प्रकाशन', इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ
था, उसमें मैंने भूमिका दी थी। वह भूमिका क्या थी, बस अश्क जी के एक पत्र का
उत्तर था जिसमें उन्होंने मेरी कहानियों का उल्लेख करते हुए मेरे समकालीनों
की प्रवृत्तियों का विवरण दिया था। ये वे दिन थे जब कहानी-लेखकों पर विदेशी
लेखकों का अंधा प्रभाव हावी था। कुछ लोग 'ऐंटी हीरो' तो कुछ लोग 'ऐंटी स्टोरी'
का राग अलाप रहे थे। अजीब-सी आपाधापी मची थी और बतौर फैशन हिंदी के नए कथाकार
कुछ बहुत ही दूर की कौड़ी लाने के फेर में थे। अश्क जी ने इस सतही धरातल पर
चोट करते हुए मेरे सहज लेखन का स्वरूप स्पष्ट किया था और मेरे समकालीनों की
उस कुंठा का उल्लेख भी किया था जो उन्होंने मेरे लेखन को ले कर व्यक्त की
थी। अश्क जी का पत्र लंबा था और इसमें कई विवादास्पद स्थितियों की ओर संकेत
किए गए थे इसलिए मैंने 'एक पत्र के संदर्भ में' शीर्षक से अपना उत्तर अश्क जी
को लिख भेजा था, जिसे उन्होंने मेरे संग्रह में भूमिका के रूप में इस्तेमाल
कर लिया था। अब कितने ही वर्ष निकल चुके हैं और 'अकर्मक क्रिया' मेरा आठवाँ
कथा-संग्रह है। इस दौरान मैं लगभग दो सौ कहानियाँ लिख चुका हूँ। आज मैं यह
अनुभव करता हूँ कि अब उस तेजी से लिखना संभव नहीं है, जो प्रारंभ में बहुत सहज
थी - आज परिवेशगत परिदृश्य के संदर्भों को तौल कर देखना आवश्यक हो गया है -
अभिव्यक्ति की तीव्रता ही पर्याप्त नहीं रह गई है, वरन सामाजिक यथार्थ को
सार्थकता के आयामों तक ले जाना भी अपरिहार्य हो गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि अपने पचास वर्षों के लेखन में मैंने पाठकों को कितना
कुछ सार्थक दिया है - हाँ, यह कहने में मुझे कोई दुविधा नहीं है कि उनकी
जागरूकता और जीवन-विषयक समझ ने मुझे स्पष्ट तौर पर यह सुझा दिया है कि लेखक
को क्या नहीं लिखना चाहिए। यों तो मेरे अंतरतम में मेरा अपना आलोचक ही इतना
सख्त और कटु है कि मेरे लेखन और रचना-प्रक्रिया को दुश्मन की नजर से देखता है
कि कहाँ उसका दाँव लगे और वह मुझे पछाड़ दे, पर शायद यही वह बिंदु है जहाँ मैं
पूरी तरह चौकस रहने का प्रयास करता हूँ। हर सजग लेखक जानता है कि उसने कहाँ
निष्ठा और परिश्रम से काम लिया है और कहाँ वह तरह दे कर निकल गया है। अपने इस नवीनतम कथा-संग्रह 'अकर्मक क्रिया' में संगृहीत कहानियों में मैंने
मौजूदा जीवन के तनावों और कुंठाओं को ही नहीं उभारा है बल्कि व्यवस्था और
प्रशासन की उस अमूर्त मारकता का भी भरपूर उल्लेख किया है, जो आदमी के जीवन में
हर पल जहर घोलती रहती है। मैंने केवल इतने को ही अलम नहीं समझा इसलिए अपनी
कहानियों में मनुष्य के सनातन जुझारू स्वभाव का उल्लेख करते हुए यह संकेत भी
दिया है कि स्तर-स्तर व्याप्त पाखंड को वह अपनी जिजीविषा से काट कर विफल कर
दे। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ अकर्मण्यता के विरुद्ध
एक वक्तव्य हैं। इस प्रयास में मैं किंचित भी कृतकार्य हो सका तो मैं समझूँगा
कि लेखन सामाजिक मूल्यों का मूर्त करने का दिशान्वेषी है।
से.रा.
यात्री
डायरेक्टर के दफ्तर से निकल कर मैंने रिक्शा लेने की सोची, मगर घड़ी में अभी
पाँच भी नहीं बजे थे। बस-स्टैंड की दूरी कुछेक मिनटों में ही मजे से नापी जा
सकती थी, इसलिए मैं खरामा-खरामा बस स्टैंड की दिशा में बढ़ लिया। कचहरी से जरा
आगे निकलते ही मुझे दफ्तरों से छूटते हुए बाबुओं का रेला दिखाई पड़ा, तो मैं
सड़क की तरफ मुड़ने के बजाय नाले के किनारे एक पतली-सी सड़क पर चलने लगा। डायरेक्टर के कार्यालय में मैं पिछले पाँच दिनों से लगातार चक्कर काट रहा
था। मेरे एक बिल पर 'ऑब्जेक्शन' लगा कर किसी बाबू ने चिड़िया बिठा दी थी और
मैं तीस मील से रोजाना और सौ काम छोड़ कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चकफेरी
लगा रहा था। मैं चाहे जितनी जल्दी दफ्तर में पहुँचूँ, किसी बाबू को मुझसे
सहानुभूति नहीं थी। इसके अलावा उनकी नजर में यह बिल वाला मामला इतना मामूली था
कि 'रूटीन' में ही सामान्य ढंग से हो जाने वाला था; हाँ, यह बात दीगर थी कि
इसमें अभी और भी साल-दो साल खिंच सकते थे। हम सभी जानते हैं कि यह रूटीन 'डे ऑव
जजमेंट' तक फैला हुआ है और फिर भी अटका हुआ कागज सरकारी सड़क का अडियल टट्टू हो
जाता है। मैं जितनी देर दफ्तर में रहता था, कई बाबुओं के कृपा-कटाक्ष प्राप्त करने
के लिए उन्हें चाय-पानी पिलाता था; सिगरेट की एक पूरी डिब्बी ले कर उनकी
कुर्सियों की बीच धँसता था। जब किसी एक बाबू को सिगरेट पेश करता था, तो एक-एक
करके सारे बाबू अपनी कुर्सियों से उठ कर वहीं आ जाते थे और पूरी डिब्बी साफ
होने में चंद मिनट भी नहीं लगते थे। इसके अलावा उनका एक खास तरीका यह भी था कि
वे मुझे एक-दूसरे की मेज पर टरकाते रहते थे। वे मेरी दृष्टि में प्रत्येक को
महत्वपूर्ण सिद्ध करके 'दफ्तरी समाजवाद' कायम रखना चाहते थे। खैर, जो भी हो,
जब दफ्तर बंद होने का वक्त होने लगता था और मेरे सिर में बराबर हथौड़े चलने
लगते थे, तो मायूस हो कर 'अच्छा, तो मैं चलूँ?' कहता दफ्तर से मरे-मरे कदमों
बाहर निकलने लगता था। मेरी हालत पर झूठा या सच्चा तरस खा कर कोई-कोई बाबू मुझे
सुना देता था, 'यारों, क्या बात है! गरीब कई दिनों से झख मार रहा है, इसका काम
क्यों नहीं करा देते?' एक गुमनाम-सा खूसट चेहरा ऊपर उठता और वीतरागी स्वर में बड़बड़ाता, 'अब
डायरेक्टर के कूल्हे कुर्सी पर लगें तो कुछ हो! उसे टूर से कौन निकाले? साले
महीने में तीन सौ पैसठ दिन गुलछर्रे उड़ाते हैं! बाबुओं को मुफ्त में डंडा
चढ़ाया जाता है!' उनकी आपसी चखचख से मुझे क्या मयस्सर - यही सोचता मैं, अपमानबोध से पीड़ित,
गलियारा पार कर जाता। दफ्तर की कटु स्मृतियों को मस्तिष्क से बाहर धकेलते-धकियाते मैं पुल बेगम
तक जा निकला। अपनी उधेड़बुन में गर्क ज्यों ही मैं पुल से एक तरफ को मुड़ा,
मेरा एक पुराना सहपाठी डी.सी. मेरे कंधे पर धौल जमा कर बोला, 'देखो इस मरदूद
को! चला जा रहा है सिर घुटनों में दिए! गोया किसी को फूँक कर लौटा हो। तुम्हें
पता है कि नहीं, तेरा बाप यहाँ चार साल से मर रहा है?' डी.सी. की इस जीवंत
फिकरेबाजी और मस्त मुखमुद्रा का सामना करने लायक पूरे दिन में मेरे पास कुछ
बाकी नहीं बचा था। मैं महज एक मरियल-सी मुस्कराहट बमुश्किल-तमाम अपने
नाक-नक्श पर चिपकाने की चेष्टाएँ करने लगा। डी.सी. थोड़ा गंभीर हो कर बोला,
'कहाँ से आ रहा है?' एक वाक्य में अपनी विपदा रखने का कौशल भी उस वक्त मेरे
पास नहीं रह गया था और ब्यौरे में जाने का उत्साह तो सौ-सौ कोस तक नहीं रह
गया था। मैंने बात का बिस्तर लपेटते हुए महज इतना कहा, 'डायरेक्टर के दफ्तर
में काम था। अब लौट रहा हूँ।' लेकिन मेरी आवाज इतनी कमजोर निकली कि बात का
आखिरी हिस्सा 'यूँ ही रोज-ब-रोज...' मेरे तालू से चिपक-कर रह गया। । डी.सी. ने मेरे कंधे से अपना हाथ नहीं हटाया। उसके स्पर्श ने मेरी थकन-टूटन
को काफी गहराई तक टटोल लिया था शायद। वह फैसला-सा देता हुए बोला, 'चल, मेफेयर
में 'ब्लू एंजिल' लगी है। छोटी-सी फिल्म है। देख कर चले जाना।' मैं भीतर तक
उधड़ा हुआ था ही। पिछले कुछ दिनों से सारा दिमाग बदजायका हो गया था। मैं डी.सी
का आमंत्रण नहीं ठुकरा सका; उसके साथ लग लिया। मुझे डी.सी. का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे एक घटिया-सी साजिश के
प्रति मर जाने की सीमा तक चिंतित होने से उबार लिया और मैं भी एक भिन्न
मनःस्थिति में जीने योग्य हो गया। इसके बाद उसने एक बढ़िया रेस्तराँ में खाना
खिलाया और बोला, 'वाइफ तो इन दिनों यहाँ है नहीं। चलो, मेरे साथ ही लोट लगाओ।
कल सुबह चले जाना।' और वह मन की आँखों से बहुत दूर देखते हुए बुदबुदाया, 'यार,
कितना वक्त हो गया हम लोगों को मिल बैठे हुए! अब कुछ हो जाना चाहिए...' जैसा कि आम होता है, आप दोस्तों से इतना कट जाते हैं कि बीच में कोई भूमिका
आने लगती है और फिर उनसे बहुत सहजता से जुड़ना तत्काल संभव नहीं हो पाता है।
वही यहाँ हुआ। मैंने डी.सी. को एक खूबसूरत भरम के हवाले करते हुए कहा, 'हाँ
यार, मुद्दत हुई है यार को मेहमाँ किए हुए। अब हमें इस लानत को तोड़ना चाहिए।
मैं जल्दी ही किसी दिन तेरे पास ठहरूँगा और जम कर बैठेंगे।....' डी.सी. ने फिर कोई आग्रह नहीं दिखाया। शायद वह भी अब उतना अनुरोधपरायण नहीं
रह गया था। 'ओ.के.' कह कर उसने हाथ हिलाया और चौराहे से एक सड़क पर मुड़ गया।
मैं भी बस-स्टैंड जाने वाली सड़क पर हो लिया। पिछले तीन-चार घंटों में मुझे
वक्त का कोई एहसास नहीं हो पाया था। डायरेक्टर के दफ्तर में छह-सात घंटे जिस
साँसत में गुजरे थे, उसके मुकाबिले पिछले कुछ घंटे चुटकी बजाते बीत गए थे।
नतीजा सामने था; आखिरी बस छूट चुकी थी और अब लौटने के लिए महज टैक्सियाँ रह गई
थीं। जेब में हाथ डाल कर देखा तो पाया कि टैक्सी का पूरा भाड़ा भी मेरी जेब
में नहीं है! आसन्न संकट में घिर कर मैं कोई रास्ता निकालने की जुगत सोचने लगा। अभी कुल
जमा आधा मार्च बीता था। रात को ग्यारह के बाद खुले में पड़े रहना भी मुमकिन
नहीं था और मैंने अपने अहमकपने में डी.सी. से उसके घर का पता भी नहीं पूछा था।
काफी देर तक मैं बस-स्टैंड की सीमेंट वाली बेंच पर बैठा सोचता रहा। बहुत देर
बाद मुझे यकायक ब्रेन-वेव आई - मेरा एक पुराना दोस्त, शरत, अरसे से इसी शहर
में था; बल्कि शायद उसने तो अब तक अपना मकान भी बनवा लिया हो! कई बरस पहले एक
बार मिला था, तो जबरदस्ती मुझे अपने साथ पकड़ ले गया था। उस समय तक मकान का
सिर्फ एक कमरा ही बना था, बाकी ईंट-सीमेंट, चूने वगैरह के ढेर से यह लगा कि
मकान महीने-डेढ़ महीने में तैयार हो जाएगा। उसके मकान का भी बिल्कुल सही
पता-ठिकाना मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं अनुमान के सहारे भटक-भटका कर वहाँ
पहुँच जरूर सकता था। सड़कों पर आवाजाही में भीड़-भड़क्का काफी कम हो चला था। अलबत्ता पनवाड़ियों
की दुकानों पर अच्छी-खासी रौनक थी! जिस सड़क पर मैं चल रहा था, वहाँ बहुत-से
निठल्ले और मनचले अजीब-अजीब मुद्राओं में इधर-उधर दो-दो, तीन-तीन की टोलियों
में ठट्ट लगाए खड़े थे। मैंने एक पान खाने की सोची। जेब से पैसे खरच करके
अय्याशी किए बहुत देर हो गई थी। पनवाड़ी की ओर बढ़ते हुए आँखें ऊपर एक छज्जे
की तरफ उठ गई। एक औरत दोनों हाथों से मुझे ऊपर आने का आमंत्रण दे रही थी। मेरा
दिमाग बिल्कुल ठस्स हो गया था। क्या जाने क्या बात थी कि मैं बगैर कुछ
सोचे-समझे पनवाड़ी की दुकान से लगे जीने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी पर
पहुँच कर मैंने देखा कि काफी पुराने, घिसे किवाड़ों की संधि से हलकी-सी रोशनी
की लकीरें मेरे टखनों पर पड़ रही हैं। मुझे जरा भी इंतजार नहीं करना पड़ा। साँकल खड़की और दरवाजा खुल गया। उस
कोठरीनुमा दड़बें में महज एक औरत नजर आ रही थी। धुआँ देती ढिबरी की रोशनी में
मैंने देखा, कालौंछ में लिथड़े अल्यूमीनियम के चंद बर्तन दीवार से लगे बेतरतीब
पड़े हैं। इन भांडों में ऊपर तक पानी भरा था और तालाब के पानी पर जमी काई की
मानिंद कुछ मटमैला-सा पानी तैर रहा था; शायद खिचड़ी जैसी कोई चीज पका और खा कर
बर्तनों में पानी भर दिया गया था। एक झिंगली चारपाई पर एक गूदड़ पड़ा था, पायताने एक चीकट चादर थी और चट्टान
जैसा सख्त तकिया सिरहाने से खिसकते हुए अजीब कोण धारण करता चारपाई के
बीचों-बीच पहुँच रहा था। चारपाई के सिरहाने को छूता हुआ एक बहुत पुरानी साड़ी
का इतना गलीज पर्दा टँगा था, जैसे उसे टाँगने के बाद कभी भी पानी से छुलाने की
जहमत न उठाई गई हो। एक कोने में 'फोल्ड' की हुई चटाई खड़ी थी, जो जगह-जगह से
उधड़ चुकी थी, मगर उसे स्थायित्व प्रदान करने की नजर से कोनों पर चितकबरे
कपड़े की गोट सिली हुई थी। अगर यह कोठरी सौ साल पुरानी थी, तो मैं दावे से कह
सकता हूँ कि पचास सालों से इसकी दीवारों पर पुताई नहीं हुई थी। उस भुतही, भयानक ढंग से भभकती ढिबरी के धुएँ से कमरा पूरी तरह दमघोंट हो गया
था। मैंने उस औरत की तरफ हिम्मत करके देखा। उसने जवाब में बीभत्स ढंग से
मुसकराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे झिंगली चारपाई पर लगभग धकेलते हुए कहा,
'खड़े क्यों हैं! बैठिए तो सही!' उसके शब्दों के साथ 'अहमद अली दिलदार अली'
के जर्दे का एक असह्य भभका मेरे नथुनों से ले कर दिमाग तक चढ़ गया। मैंने खड़े
होने की कोशिश करते हुए इधर-उधर टोह ली। शायद पर्दे के उस तरफ कोई हो। कम से कम
अपने लिए तो किसी को उल्लू बना कर फाँसना इस झोझरे बर्तन के बूते की बात नहीं
है। लेकिन जब पर्दा हटा कर कोई आता दिखाई नहीं पड़ा, तो मैं अवसन्न पड़ने लगा।
मेंहदी से रँगे मूँज-बालों की एक पचास-पचपन-साला खूसट अपने सारे गलीजपन और
बदसूरती के साथ मेरी बगल में मैदे की बोरी जैसी लुढ़क पड़ी थी। हे भगवान! इतना
घिनौनापन बरदाश्त करना किसी भी उम्र के आदमी के लिए अकल्पनीय यातना है, मेरी
उम्र ही क्या है? चलो, उम्र को भी छोड़ो... वह कितनी भी सही, लेकिन जो आपके
बगल में फूटा ढोल पड़ा है, उसका आप क्या करेंगे? मैं त्रस्त हो कर खड़ा हो गया और वहाँ से तत्काल भाग निकलने का उपाय सोचने
लगा। इतनी भयावह वास्तविकता के रूबरू खड़े होने की बात मेरे लेखे असंभव थी।
हालाँकि अब मैं अपने पाँवों पर खड़ा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे किसी
कालकोठरी में दानवीय यंत्रणा देने के लिए पटक दिया गया है और वहाँ से भाग
निकलने का अब कोई मार्ग नहीं है। मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ते देख कर वह ढलके बदन की थुलथुल मौत मेरी ओर लपकी और
मुझे कंधे से दबोचते हुए फुसफुसाई, 'क्या मैं अच्छी नहीं लगी अपने बलमा को?'
आज सोचते हुए भी घबराहट होती है। पर उस पल अपनी रुद्ध होती चेतना के बावजूद
मैंने उसके चेहरे पर एक नजर डाली थी; जैसे किसी दरार-खाई स्लेट पर अनेक
चितकबरे धब्बों के बीच किसी अनाड़ी ने आड़ी-तिरछी बेमतलब लकीरें खूब रगड़ कर
खींच डाली हों। हो सकता है, किसी विशिष्ट कालखंड में वह चेहरा देखने लायक रहा
हो लेकिन मेरे प्रत्यक्ष ज्ञान और आँखों ने मुझे यह एक क्षण के लिए भी
स्वीकार नहीं करने दिया। पका हुआ फल उपभोग से वंचित हो कर जिस तरह सड़-गल जाता
है, लगभग वही स्थिति मेरे सामने मूर्तिमान खड़ी थी। उसकी करख्त आवाज और भौंडे संबोधन से हौलदिल होते हुए मैंने पूछा, 'कितने
रुपए चाहिए?' उसने रुपयों की बात घुमा दी, 'अजी, रुपयों की ऐसी भी क्या उतावली। दे देना
बाद में। पहले तो...' उसने चारपाई पर पड़े तकिए को एक अश्लील स्थिति में जमाते हुए मुझे न्यौता
दिया, 'अब आ भी जाओ।' एकाएक वह उठ कर पर्दे के पीछे गई और पानी की छप-छप सुनाई पड़ने लगी। उसने
लौट कर मुझे सूचित किया, 'अब कोई डर नहीं है। मैंने डुटोल से सफाई कर ली...
वैसे भी मैं रुंडे-मुंडे ग्राहक नहीं घुसने देती।' उसके ग्राहकों की श्रेष्ठता का स्तर जानने की जिंदादिली मेरा साथ सिरे से
छोड़ चुकी थी। इस वक्त मेरे हाथ पतलून की जेब में फँसे हुए थे और कोई फैसला कर
रहे थे। मेरी जेब में जितने रुपए थे, उनकी गिनती मेरी उँगलियों में मौजूद थी।
मुझे अपनी टेट में पचास रुपए न होने पर एकाएक बहुत अफसोस हुआ; अगर वे होते, तो
मैं इस वक्त आराम से अपने बिस्तर में लेटा होता। इन थोड़े-से रुपयों के अभाव
ने ही मुझे इस दोजख में ढकेला था। मैंने पतलून की जेब में से हाथ निकाला और एक
बीस रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया और पता नहीं किस अनाम भावना के तहत मेरे
दोनों हाथ उस भयावनी आकृति के सामने जुड़ गए। आज विश्लेषण करना कठिन है कि हाथ
जोड़ते समय मेरी मुक्ति का प्रश्न प्रमुख था या उस औरत की उम्र के प्रति मेरे
सारे व्यक्तित्व में केवल इसी व्यवहार की गुंजाइश थी। इसके तत्काल बाद
मैंने आगे बढ़ कर साँकल खोली और देहरी लाँघ कर जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ लाँघने
लगा। सड़क पर उतर कर मैंने झिझकते हुए इधर-उधर देखा। सड़क और सुनसान हो चली थी।
दो-दो, तीन-तीन की टोलियों में लोग झूमते-झामते यहाँ-वहाँ रेंग रहे थे।
अजीब-अजीब शक्लों और हुलियों के उन लोगों से नजरें बचाते हुए मैं तेज गति से
चलने लगा। बाजार की सारी दुकानें लगभग बंद थीं। हाँ, ऊपर बारजों पर रँगी-पुती
औरतें काफी तादाद में नजर आ रहीं थी। तबले और हारमोनियम की मिली-जुली ठनक के
बीच दारू से बोझिल करख्त स्वर फिजाओं में टूट-फूट कर बिखर रहे थे। एक-दो बार
उचटती-सी निगाहें ऊपर उठीं लेकिन नंगे बुलावों के दौरान अपनी खुश्क हालत के
अहसास ने मेरी नजरें जमीन में गाड़ दीं। मेरे लिए जितनी तेजी से वह सड़क पार
करना मुमकिन था, मैं करने लगा। उस सड़क के अंत पर पहुँच कर मैंने एक राहगीर से अपने मित्र शरत के मोहल्ले
की जानकारी ली। उसने बताया कि मैं गलत जगह पर हूँ; मुझे उसी सड़क पर लौट कर
चौराहे से उत्तर की तरफ लौटना पड़ेगा। चौराहे तक पहुँचने के लिए उसी सड़क पर लौटने की यंत्रणा से मेरे पैर बोझिल
हो गए। लेकिन कोई दूसरा रास्ता न देख कर मैं लौट लिया और अपनी उपस्थिति को
भरसक विदेह बनाने की कोशिश करने लगा। अभी मैं चौराहे के इधर ही था कि बीभत्स गाली-गलौज का रेला मेरे कानों से
टकराने लगा मैं यह देख कर दंग रह गया कि फोश गालियों का शोर उसी कोठरी से उभर
रहा था, जिसमें आधा घंटा पहले मेरी साँस उखड़ रही थी। अजीब-से कौतूहलवश मेरे
पाँव ठहर गए। मैंने उन्हें पनवाड़ी की दुकान तक ठेला और उत्सुकतावश मर्द-औरत
की वजनी और नंगी गालियाँ सुनने लगा। संयोग से पनवाड़ी खाली था। मैंने दबे स्वर
में उससे पूछा, 'क्या किस्सा हो गया?' पनवाड़ी ने खास उत्सुकता नहीं दिखाई। उकताए-से स्वर में तोतली भाषा बोलने
लगा, 'अदी तित्ता ता होता!... वोई लोज ता धगला अ। लंदीथाना तो अई। इती लंदी ता
बेता अ। थाला पीते लौता है और बुलिया तू तंद तल्ला अ। तमाता तो देथो दिन्ने
दना अ उती ते मूं ताला तलै अ हलामी! (अजी किस्सा क्या होता! वही रोज का झगड़ा
है। रंडीखाना तो है ही! इसी रंडी का बेटा है। साला पी के लौटा है और बुढ़िया को
तंग कर रहा है! तमाशा तो देखो, जिसने जना है, उसीसे मुँह काला करे है, हरामी!) मैं पनवाड़ी की तोतली, बगैर उतार-चढ़ाव की ठंडी भाषा सुनते हुए थर्रा उठा।
शायद इस बात को कहने के लिए कोई भाषा या जुबान लड़खड़ाने से नहीं बच सकती थी।
अब मुझे लगा कि सहज उत्सुकता प्रदर्शित करके मैं एक अवांछित प्रसंग की सुरंग
में धँस गया हूँ। मेरे बगैर कहे ही पनवाड़ी ने एक सादा पान लगा दिया था जिसे ले
कर मैंने पैसे चुकाए और दुकान से हट कर चौराहे की दिशा में चल पड़ा। पनवाड़ी के विवरण को अपने जेहन से मैं जितना ही हटाने की कोशिश करता था, वह
उतनी ही शिद्दत से मुझ पर हावी होता जा रहा था। मुझे इस समय किसी घनिष्ठ
व्यक्ति से मिलने की गहरी तलब थी, जिसके नजदीक पहुँच कर मैं विश्वास के साथ
यह महसूस करना चाहता था कि लोगों के आपसी रिश्ते अभी सहज और साधारण है।
विभीषिकाओं के लंबे सिलसिले से बचने के लिए अंततः यह आश्वासन जरूरी था। लंबी भटकन के बाद जब मैं शरत के मकान के सामने पहुँचा, तो मैंने देखा कि वह
मकान एक मुद्दत पहले ही मुकम्मिल तौर पर बन चुका होगा। बाहर रंग-रोगन से लैस
लकड़ी का एक फाटक था, जिस पर शरत के नाम की तख्ती लटक रही थी। मुख्य इमारत तक
पहुँचने से पहले एक छोटा-सा लॉन पार करने को था, जिसमें कई किस्म के फूलों के
पौधे, लतरें और अमरूद-पपीते वगैरह के पेड़ थे। मैंने धीरे से फाटक का कुंडा
हटाया और अंदर लॉन में दाखिल हो गया। शुरू में रात की खामोशी की आहट लेते हुए
संकोच में डूबा रहा। और फिर कोई दूसरा सहारा न देख कर शरत का नाम पुकारने लगा।
पता नहीं, शरत मकान में था या कहीं बाहर गया था। बहरहाल आठ-दस दमदार आवाजों के
बाद भी जब भीतर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाना मेरे लिए
लज्जास्पद हो गया। 'अब क्या किया जाए?' के असमंजस में मैं शरत के द्वार पर कुछ मिनट खड़ा रहा।
फिर मैंने तय किया कि मैं वहीं लान में पड़ रहूँगा। मैंने अपनी चप्पलें एक तरफ
निकाल दीं और घास पर बैठ गया। फिर मैंने जेब से मुड़ी-तुड़ी सिगरेट की डिबिया
निकाली और दबी-भिंची सिगरेटों को निकाल कर उनकी गिनती करने लगा। अब आगे जितनी
भी रात बाकी थी, उसका एक मात्र आसरा ये कुछ सिगरेटें ही थीं। सारे दिन और रात की दु:स्वप्न सरीखी घटनाओं को सामान्य कर लेने की गरज से
मैंने एक सिगरेट जला ली और चप्पलों को एक-दूसरी के ऊपर-नीचे रख कर सिर के लिए
ढासना तैयार कर लिया। सिगरेट के कश खींचते हुए मैं चप्पलों पर सिर टिका कर लेट
गया। ऊपर निरभ्र आकाश में टिमटिमाते तारे ऐसे लगे, गोया उनसे जिंदगी में पहली
बार मुलाकात हुई हो। दूर तहसील में बजते हर घंटे की गूँज दिमाग पर नक्श होती रही। उन थोड़े-से
लम्हों में ही मुझे लगने लगा कि मैं सत्ताइस-अट्ठाइस बरस इस जमीन पर रहने के
बावजूद इस दुनिया-जहान के लिए कितना बाहरी और अपरिचित हूँ। मेरे सिरहाने की
दीवार के उस तरफ शरत और उसके बीबी-बच्चे सोए पड़े हैं; यहाँ से तीसेक मील दूर
तहसीली कस्बे में मेरे नाम पर एक सरकारी क्वार्टर अलाट है, जिसका किराया जमा
करते वक्त मय वल्दियत मेरा नाम-पेशा और दीगर ब्यौरा दर्ज किया जाता है। यही
नहीं, एक देश की सरकार बनाने में गाहे-बगाहे मेरा वजूद साग्रह इस्तेमाल होता
है। लेकिन... मैंने एक सिगरेट और सुलगाई और करवट ले कर लेट गया। करवट के नीचे पतलून में
पड़ी रेजगारी कूल्हों में चुभने लगी। इसी पल मुझे सहसा ख्याल आया कि मेरे पास
अब महज चंद सिक्के रेजगारी की शक्ल में हैं। कल दफ्तर के बाबुओं को
सिगरेट-चाय पिलाने का जुगाड़ भी नहीं हो पाएगा। इसी संदर्भ में उस हवन्नक को
दिए गए पाँच रुपए की नोट की याद आ गई और साथ ही पनवाड़ी के तटस्थता से कहे गए
तुतलाहट-भरे वाक्य भी स्थितिचित्र बन कर उभरने लगे : 'तमाता तो देथो...
दिन्ने दना है, उती ते मूं ताला तलै अ हलामी!' पता नहीं कितने रूपों में ये
शब्द और इनके पीछे मँडराती जुगुप्साएँ किरचों की तरह लगातार मस्तिष्क में
चुभती रहीं। मैंने पाँच का घंटा सुना तो उठ कर बैठ गया। सुबह के साथ उगते ठोस
यथार्थ ने मुझे उस हया का अहसास करा दिया जो चप्पलों पर सिर टिका कर
आवारागर्दी की घोषणा कर रही थी। मानो शरत की पत्नी अभी उठ कर बाहर चली आए और
मुझे इस हकीर-फकीर हालत में पड़े देखे, तो मेरे बारे में क्या-क्या नहीं
सोचेगी! मुझे तो खैर छोड़ ही दो, उन लोगों को क्या कम शर्म आएगी कि उनका
घनिष्ठ यतीम-आवारा की शक्ल में धूल-मिट्टी में लिथड़ा पड़ा है। मैंने सावधानी से चप्पलें पहनीं और बगैर कोई आहट किए दरवाजे का खटका खोल कर
बाहर सड़क पर आ गया। सड़क पर चलते हुए मैंने अपने हाथ-पैरों और कपड़ों को बेदर्दी से झाड़ा और
कमेटी के नल पर मुँह-हाथ धोने लगा। स्वयं को एक काम का आदमी बनाने के लिए बीते
कल की स्थिति में लौटना आवश्यक था। इसके अलावा कम से कम किसी से सौ रुपया भी
लेना जरूरी था - वरना दफ्तर के भुक्खड़ बाबुओं को सारे दिन लपेटे रखने का सवाल
ही नहीं उठता था। मैली सड़कों पर एक-दो घंटे चक्कर काटते-काटते सारा शरीर टूटने लगा, तो
मैंने एक खोखे पर खड़े हो कर दो रुपए की चाय पी और फिर शरत के ही दरवाजे जा
लगा। इस बार मैंने शरत के गेट की कुंडी काफी शोर मचा कर खोली, जिसकी धमक भीतर
तक पहुँच गई। शरत चाय का मग हाथ में थामे बाहर निकल आया। उसे तहमद और बनियान
में देख कर मुझे राहत हुई। वह पूरी तरह पकड़े जाने की हालत में था। मुझे
अलस्सुबह सामने देख कर वह अचंभे से बोला, 'बे तू! कहाँ से टपक पड़ा पौ फटते
ही?' मैंन जांबाजी दिखाते हुए अट्टहास किया, 'सब बताऊँगा। पहले भीतर तो घुस! शाम
की बस रास्ते में बिगड़ गई। मनहूसियत में सारी रात काली हो गई यार!' शरत ने चश्मे के पीछे से आँखें चमकाईं। 'जहाँ जाएगी ऊका वहीं पड़ेगा
सूखा।... तुझ मनहूस की वजह से ही बस खराब हुई होगी!' उसके साथ घर में घुसने से पहले एकाएक मेरी निगाह उस तरफ चली गई जहाँ अभी
घंटे-डेढ़ पहले मैं एक लावारिस की तरह पसरा पड़ा था। अयाचित संदर्भों के खानों
में विभाजित होते आदमी को अपने से दूर झटक कर मैं शरत के साथ कमरे में घुसा और
शरत की पत्नी को संबोधित करते हुए अधिकार के स्वर में बोला, 'भाभी, इधर आप
बहुत सुंदर और सेहतमंद लग रही हैं।' शरत गुर्राया, 'देखा, साले ने आते ही चापलूसी का लेप चढ़ाना शुरू कर दिया।' भाभी भी भरपूर मुस्कराईं। मुझे गहरा संतोष हुआ, क्योंकि शरत की पत्नी का
मूड ठीक होना मेरे पूरे दिन जीवित रहने की पहली शर्त थी। शरत से मैं सौ रुपए
झटकने की कोई कारगर युक्ति सोचने लगा। उसके रंग-ढंग से मुझे साफ लग रहा था कि
वह मेरी माँग की पूर्ति भाभी के माध्यम से ही करने वाला था। पता नहीं क्यों,
ठीक इसी समय मुझे उस औरत की तरफ बढ़ाए हुए बीस रुपए याद आ गए, और साथ ही अपनी
जुड़ी हुई हथेलियाँ भी। प्रभाकर ने पलँग पर जरा उचक कर स्विचबोर्ड को टटोला और लाइट जला दी। वह फिर
से रजाई लपेट कर पलँग पर लेट गया। मैं पलँग से सटी चौकी पर बैठा सिगरेट पी कर
जाड़ा भगाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर की मंजिल में प्रभाकर के बच्चे उछल-कूद
मचा रहे थे जिसकी धमक से कड़ियों की मिट्टी सिर पर गिर रही थी। इस उदास माहौल से निकलने के लिए मैंने प्रभाकर से कहा, भले आदमी, यह बिस्तर
में घुसे रहने का वक्त नहीं है। आ, चल कर कहीं बैठेंगे और कुछ तफरी करेंगे।
प्रभाकर ने रजाई अपने इर्द-गिर्द और कस कर लपेट ली और अपने बड़े लड़के का नाम ले
कर जोर-जोर से पुकारने लगा। लड़के ने उसकी आवाज नहीं सुनी तो मसहरी के सहारे कई
तकिए लगा कर बोला, कोई हमारी नहीं सुनेगा! सब साले अपनी-अपनी खाल में मस्त
हैं... मैं चाहता था, ऐसे में दो प्याले गरम चाय मिल जाती तो थोड़ा जाड़ा भाग
जाता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो मुस्कुरा कर बोला, कुछ कहो यार, अब वह
पुराने वाला नक्शा कुछ जमता नहीं है। पौरख थक गए साले, वरना कोई बात थी!...
मैंने इस मनहूसियत-भरे माहौल से चिढ़ कर कहा, अबे दोजखी, पौरख नहीं थकेंगे तो
क्या होंगे? सरेशाम बिस्तर में लंबा हो कर आज तक कोई जवान रहा है! मेरे
चिढ़ने से प्रभाकर ठठा कर हँस पड़ा और बोला, अब जो तेरे जी में आए बक! जनवरी के
पाले में मैं तो इस वक्त बाहर निकलने से रहा। मैं प्रभाकर की रजाई खींचने की सोच ही रहा था कि बाहर सड़क से कोई आदमी
दरवाजे में धँसता दिखाई पड़ा। आधे मिनट बाद सहन और बरामदा पार करके जो आदमी
डगमगाते हुए कमरे में घुसा, वह याज्ञिक था। उसके चेहरे पर वही हमेशा की नहूसत
फैली थी। प्रभाकर और मैंने उसे गौर से देखा और गंभीर हो गए। याज्ञिक के आने पर
हमेशा यही होता था। उसे देख कर हम लोग भीतर ही भीतर बिफर उठते थे। उसकी चमड़े
की स्ट्रेप वाली घिसी-पिटी चप्पलों और टखनों पर धूल ही धूल चढ़ी थी।
लंबे-चौड़े पायंचों वाली खाकी पैंट सनातन ढंग से फड़-फड़ कर रही थी। उसके
पिलपिले शरीर पर चढ़े हुए बीसों साल पुराने कोट की जेबों से चिमड़ी खाल की
उँगलियाँ झाँक रही थीं। कानों और सिर पर लिपटे मफलर से ज्यादा सुखे हुए तंबाकू
के पत्ते का गुमान होता था। कभी-कभी यह सोच कर हैरत भी होती थी कि यह
छछूंदरनुमा आदमी हम लोगों के साथ कहाँ से लग गया? मैं और प्रभाकर कुछ दिनों से
उसकी परछाईं तक से बचने लगे थे। हालाँकि याज्ञिक सी.डी.ए. में जूनियर क्लर्क
था, फिर भी उसके चेहरे को देख कर यही लगता था कि जैसे पुश्तैनी यतीम हो। उसे
देखते ही मेरे मन में आक्रोश की 'हुं-हुं' उठने लगती थी और मैं खाक हो कर कहता
था, इतने पर भी रईस कविता करेगा! अबे कमीने, कोयला बीन! याज्ञिक ने मुझे और प्रभाकर को बारी-बारी से देखा और अपनी जेब से बीड़ी का
बंडल निकाल कर अपने हाथ में ले लिया। एक मिनट इधर-उधर करके उसने बंडल के ऊपर
वाला कागज फाड़ा और चौकी के नीचे फेंक दिया। दोनों हथेलियों के बीच में बंडल को
मसल कर एक बीड़ी निकाली और दाँतों के बीच में लगा ली। बीड़ी जलाते हुए तीली की
लौ से उसके चेहरे पर कई दिन की बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी चमक उठी। याज्ञिक ने बीड़ी
के कई लंबे कश खींचे और खाँसने लगा। दरअसल मैं और प्रभाकर उसके आ जाने से चिढ़ गए थे, लेकिन भीतरी तनाव को प्रकट
करने का कोई सीधा-सा रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था। याज्ञिक से सहज हो जाने के
मानी थे कि हम लोग उसे भी अपनी बातों में शामिल कर लें। बातें शुरू होते ही
सबसे पहले यह होने वाला था कि वह दो या चार मिनट बाद चाय की माँग सामने रख
देता। इस शख्स से प्रभाकर की बीबी इतनी कुढ़ी हुई थी कि उसे चाय पिलाना तो
दूर, घर में देखते ही भौंहें चढ़ा लेती थी। इसका बहुत साफ कारण था कि
पचास-पचास, सौ-सौ रुपया करके यह आदमी प्रभाकर से जाने कितने रुपए उधार ले चुका
था। होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे सौ-दो सौ रुपया कर्ज ले तो वह पैसा
लौटने की उम्मीद पर किसी दूसरे तक से माँग कर दे सकते हैं, या फिर पत्नी से
इस समझौते पर ले कर मित्र को उधार दे देते हैं कि उसकी जरूरत सच्ची है और वह
सुविधा होते ही रुपया वापस लौटा देगा। लेकिन जब कोई मित्र प्रत्येक विजिट पर
रुपया-धेली लेता है तो पत्नी इस सच्चाई से परिचित हो जाती है, तो उस आदमी की
आबरू पत्नी की नजर में बिल्कुल नहीं रहती। अपनी बात तो मैं कहता हूँ। मुझे इस उधार वाले प्रकरण को ले कर याज्ञिक से
इतनी नफरत हो चुकी थी कि एक दिन मैंने सब दोस्तों की उपस्थिति में बहुत तैश
में कहा था, यार, याज्ञिक की यह बीमारी इतनी असाध्य हो चुकी है कि कोई आ कर
मुझसे कहे कि याज्ञिक मर गया है, उसके कफन का इंतजाम करना है तो मैं जेब में
रुपया होने पर भी साफ झूठ बोल जाऊँगा कि मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है।
मित्र मेरे चेहरे का तनाव देख कर ठठा कर हँस पड़े। एक दोस्त ने याज्ञिक को
कोंच कर कहा भी था, क्यों याज्ञिक जी, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? यह बात
सुन कर याज्ञिक का चेहरा इतना सूख गया था कि मुँह से बात नहीं निकली थी। उसने
हँसने की कोशिश में दयनीयता से कंधे सिकोड़ कर अपने पान-तंबाकू रचे दाँत दिखा
दिए थे और आँखों से चश्मा उतार कर हाथों में ले लिया था। बाद में अपनी नीचता
पर मुझे बड़ी गैरत हुई थी और मैंने सोचा था कि याज्ञिक अब कभी मेरे पास नहीं
आएगा। कुछ भी हो, आदमी में थोड़ा स्वाभिमान भी होता है। पर वैसा कुछ नहीं हुआ।
याज्ञिक बराबर मेरे पास आता रहा। उसने मेरी बात का कभी उल्लेख तक नहीं किया। अपमान भी क्या सबका होता है? कुछ स्थितियाँ होती हैं जो आदमी को मान-अपमान
के बीच एक चीज साफ तौर पर चुनने ही नहीं देतीं। याज्ञिक दोस्तों के पास न आता
तो कहाँ जाता? सी.डी.ए. की नौकरी और कविता से तो जिंदगी नहीं चलती। वह अनेक
वर्षों से धर्मशाला में एक कमरा ले कर रह रहा था। उसी घुचकुली जैसे कमरे में
छठी संतान जन्म ले चुकी थी। इस संतति प्रसार को ले कर जब भी याज्ञिक की
भर्त्सना की जाती, वह इतना बेचारा और 'दूसरा आदमी' हो उठता कि यह बिल्कुल
नहीं लगता था, उसी आदमी के द्वारा यह योजना-विहीन कार्य चल रहा है। दस बरसों
में छह बच्चे सैकड़ों-हजारों आदमियों के यहाँ पैदा होते हैं, लेकिन इस बात को
ले कर हर आदमी की आलोचना यहाँ नहीं की जा सकती। फजीहत महज उसी शख्स की होती है
जो जूनियर क्लर्क हो कर धर्मशाला में डेरा डाले हुए होता है। याज्ञिक के बीबी-बच्चे के बारे में ज्यादा कुछ कहना बेकार है। आज की
स्थितियों में महज तीन हजार रुपए माहवार पाने वाले आदमी के परिवार की क्या
हालत होगी, और खासकर उस स्थिति में, जब इतने अपर्याप्त संबल पर आठ जिंदगियाँ
साँस लेती हों। हम लोगों को याज्ञिक के यहाँ जाने का अवसर कम ही मिलता। जब कोई
नया बच्चा धर्मशाला के माहौल में चीख-पुकार करके अपने अवतरित होने की सूचना
देता है, तो मित्र-मंडली किसी गंभीर दायित्व के तहत वहाँ पहुँच जाती है। पता
नहीं, क्या ऊँच-नीच गुजरे! लेकिन यह प्रतिक्रिया इतनी हताश करने वाली सिद्ध
हुई है कि अब छठे छमाही भी शायद ही कोई याज्ञिक की रूग्णा भार्या और किलबिल
करते आधा दर्जन बच्चों की खैर-खबर पूछने जाता हो। गत वर्ष याज्ञिक इतना बीमार
और तंगदस्त रहा कि उसे देख कर बीभत्स कंकाल की कल्पना साकार होने लगती थी।
पर दोस्तों ने उससे लगभग रिश्ता ही तोड़ लिया था। जब वह मौत के मुँह से निकल
कर हम लोगों के बीच में आ खड़ा हुआ था और अपने बच जाने की चर्चा करते हुए उसने
उत्साह में 'वह तो खैर हुई' वाला वाक्य बोला था तो हममें से किसी को भी खास
खुशी नहीं हुई थी। मन ही मन एक-दो ने जरूर गाली दे कर कहा होगा, 'तेरे मर जाने
से कौन दुनिया सूनी हुई जा रही थी?'... कुछ हो, याज्ञिक अपनी जिजीविषा के बल पर
अपनी गृहस्थी और बजट को धक्का दिए जा रहा था। तीन-चार सुट्टे ले कर याज्ञिक ने बीड़ी खत्म कर दी और अपनी बाँहों को छाती
से कस लिया। कई मिनट की चुप्पी के बाद प्रभाकर ने कहा, कहो याज्ञिक, कहाँ थे?
कई दिन बाद दिखाई दिए! कौन-कौन-से कवि-सम्मेलन मार आए? याज्ञिक ने अपनी आदत के
खिलाफ गंभीरता कायम रखते हुए कहा, कवि-सम्मेलन! नहीं-नहीं, मुझे कई महीने से
निमंत्रण नहीं मिला। प्रभाकर की इस बेवक्त की पूछताछ से मैं और भी झुँझला उठा।
अब अगर याज्ञिक शुरू हो गया तो इतने अरसे में घसीटी हुई अपनी बकवास सुनाना चालू
कर देगा और होते-होते बरसों पुरानी तुकें बताने लगेगा। मैंने अपनी आँखें
प्रभाकर और याज्ञिक की तरफ से हटा कर दीवार पर लगे कैलेंडर पर केंद्रित कर लीं।
प्रभाकर भी शायद याज्ञिक से पिंड छुड़ाने की सोच रहा था। मेरा नाम ले कर बोला,
यार, ऐसा जाड़ा कब तक पड़ेगा? साले जमे जा रहे हैं। मैंने उसके शब्दों की
ध्वनि पकड़ते हुए सोचा कि संभवत: प्रभाकर यह कहना चाहता है कि याज्ञिक ऐसे
जाड़े में क्यों मरता फिरता है! अपने दड़बे से यहाँ आने की इस वक्त क्या खास
जरूरत थी? मैंने कुछ कहने की गरज से जमुहाई लेते हुए कहा, प्रभाकर, तुम्हारी
जनरल नॉलेज बहुत पूअर है। बत्तीस-चौतीस बरस से देख रहे हो कि जनवरी में शीत
लहर आती है, लेकिन यह बात हर साल भूल जाते हो। याज्ञिक ने पहलू बदला और एक पैर
दूसरे घुटने पर चढ़ा कर आराम से बैठ गया। प्रभाकर ने भी जमुहाई ली और अपना खुला
हुआ मुँह हथेली से थपथपा कर बोला, कुछ कहो, यह मौसम है पीने-पिलाने का। लेकिन
ससुरी हिम्मत नहीं कि जाड़े में घर से निकला जाए। घर में वह... चिड़ी कि...
पीने नहीं दे सकती, वरना...। मैंने प्रभाकर का चेहरा ध्यान से देखा। यह कहने
का आखिर क्या मकसद हो सकता है? मैंने तो उससे बाहर चलने का इसरार तक किया था।
वह याज्ञिक के सामने किस मतलब से यह बात कह रहा है? याज्ञिक का चेहरा बेहद
गंभीर हो गया और उसने अपने बंडल से चौथी बीड़ी खींच कर सुलगा ली। ज्यों ही घर जाने के लिए मैं उठ कर खड़ा हुआ याज्ञिक ने मेरा हाथ पकड़ कर
मुझे जबरन बिठा लिया। उसने अपने कोट के भीतर वाली जेब में हाथ डाल कर सौ रुपए
का नोट निकाला और लापरवाही से प्रभाकर के ऊपर पलँग की दिशा में उछाल दिया।
प्रभाकर रजाई एक तरफ फेंक कर तेजी से उठ बैठा और नोट उठा कर इस तरह देखने लगा
गोया वह विश्वास न कर पा रहा हो कि यह भारतीय करेंसी का असली नोट है। प्रभाकर
के चेहरे पर उल्लास उभर आया। उसका सारा जाड़ा हवा हो गया। याज्ञिक का चेहरा
पहले जैसा ही गंभीर रहा। वह तटस्थता से कुछ भिनभिनाया, जिसे पूरी तरह से समझने
की कोई कोशिश ही नहीं की गई। प्रभाकर उल्लसित हो कर बोला, चलो हो जाए। आज
याज्ञिक का ही तर्पण सही! लेकिन उसे डर भी लगा, कहीं अगले मिनट याज्ञिक अपना
नोट न माँग ले, इसलिए आश्वस्त होने के लिए कहने लगा, याज्ञिक, यह मजाक वाला
मामला तो नहीं? हालाँकि इससे कुछ होगा तो नहीं। पर चलो तुम्हारी खुशी के लिए
देशी मँगाए लेते हैं। अपनी सफाई में प्रभाकर ने इतना और जोड़ दिया, चलो, इस
बहाने थोड़ी देर बैठना हो जाएगा। बर्फ भी तो सरक रही है। इस किस्से का सिर-पैर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया, पिछले दस वर्षों से
मैंने याज्ञिक को न कभी इतना गंभीर देखा था न उदार। जो आदमी थोड़ी देर बातें
करने के बाद उठते हुए बीस-दस रुपए उधार माँग लेता हो, वह आज एक साथ सौ रुपए किस
खुशी में फूँक रहा है? मैंने दूर तक सोचा पर बात साफ नहीं हुई। हो सकता है,
एकमुश्त सौ रुपए भकुए को रिश्वत में मिले हों! इस सारे प्रकरण में मेरे करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए याज्ञिक की उदारता
को बेवकूफी करार दे कर स्वयं को समझाने लगा, मरने दो हरामी को! पैदाइशी
भुक्खड़ और बदनसीब आदमी है। आज हाकिम बना है। दो घंटे बाद पैदल चल कर
मरता-खपता घर पहुँचेगा और जोरू के हाथों मार खाएगा तो सारी उदारता धरी रह
जाएगी। दादा-दिली देखो मरकट की! मैं सोचता ही रह गया। प्रभाकर पलँग से उतरा और
पैंट डाल कर बाहर निकल गया। बाहर चौराहे पर खड़े रिक्शे वाले को भेज कर उसने
देशी शराब की एक बोतल और नमकीन मँगवा ली। चौकी के नीचे बोतल रख कर प्रभाकर दबे
पाँव सहन में गया और ऊपर जाने वाले जीने का दरवाजा बंद कर आया। इसके बाद एक
अलमारी खोल कर उसने काँच के दो गिलास निकाले और हमें दे कर बोला, गिलास तो दो
ही है। चलो, दो से ही काम चलाएँगे। क्यों याज्ञिक साहब?' याज्ञिक ने जिंदगी
में पहली बार मित्र के मुँह से निकला आदरसूचक संबोधन शायद बिल्कुल नहीं सुना।
वह कंधे झुकाए बैठा था और उसके चेहरे पर संजीदगी कलौंछ की तरह बढ़ गई थी। उसने
एक बार सिर ऊपर उठाया और फिर खुद में गर्क हो गया। गुसलखाने के नल से प्रभाकर एक लोटा पानी भर लाया। चौकी के नीचे से उसने
बेताबी से बोतल निकाली और उसकी सील उमेठने लगा। यकायक उसे ध्यान आया कि बाहर
का दरवाजा चौपट खुला है। वह लपक कर गया और साँकल बंद कर आया। ऊपर-नीचे से पूर्ण
निरापद हो कर प्रभाकर ने गिलासों में शराब डाली और गिलासों को आपस में टकरा कर
याज्ञिक के हाथ में गिलास देते हुए बोला, फॉर योर फेयर लेडी, चीयरो याज्ञिक...
गो स्ट्रांग विद इट! अपना गिलास लेते हुए मुझे कुछ झिझक हुई। शायद इसलिए कि दस
बरसों में याज्ञिक की तरफ से यही पहली बार हो रहा था। याज्ञिक मुझे और प्रभाकर
को पिला रहा था - वही याज्ञिक जो पीने के लिए हम दोनों के पीछे निठल्ले की तरह
लगा रहता था। न जाने क्यों मुझे बराबर यह लग रहा था कि इस शराब का नशा मुझे
नहीं होगा, लेकिन प्रभाकर जश्न मनाने के मूड में आ चुका था। प्रभाकर की त्वरा
और उत्साह के पीछे शायद यह भावना काम कर रही थी कि याज्ञिक ने उसे खूब चूसा
है, चलो, आज इसी बहाने थोड़ा-सा तो वसूल कर ही लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रभाकर ने उछलते हुए नई गवेषणा की घोषणा की, अबे! सालों,
यहाँ एक प्याला भी तो होना चाहिए। यह कह कर वह उठा और गुसलखाने से हजामत बनाने
का एक हैंडिल-टूटा प्याला उठा लाया। याज्ञिक अपनी गिलास खाली कर चुका था। अब
वह उतना गंभीर नहीं था, बल्कि मुखर होने की चेष्टा कर रहा था। प्रभाकर ने भी
अपना प्याला उठाया और हलक भींच कर एक घूँट में ही खाली कर गया। याज्ञिक हम लोगों की दृष्टि में अब एक परोपजीवी आदमी नहीं था। हमेशा से जोंक
ख्याल किया जाने वाला एक फुसफुस इंसान एक जिम्मेदार आदमी नजर आने लगा। उसके
गाली देने में इस वक्त अधिकार बहुत साफ झलकता था। पहले वह गाली बहुत कम देता
था और अगर दे भी जाता था तो भी दीनता और झिझक उसके सारे व्यक्तित्व पर छाई
रहती थी। प्रभाकर और मैं भूल गए कि याज्ञिक एक मजलूम इंसान है, कि उसकी हरेक
मुद्रा हम लोगों के लिए एकदम बोसीदा और उबाऊ है। एक बोतल दारू का इंतजाम करते
ही वह दूसरी चीज हो गया। आधी बोतल होते-होते प्रभाकर अपनी पत्नी की तरफ से
इतना नि:शंक हो गया कि बाहर का दरवाजा भड़ाक से खोल कर सड़क पर निकल गया और
सिगरेट का पैकेट खरीद लाया। थोड़ी देर बाद सिगरेट और बीड़ी के धुएँ से प्रभाकर का कमरा पूरी तरह
फ्लिम्जी हो गया और काफी जोश-खरोश की बातें होने लगीं। प्रभाकर और याज्ञिक की
आँखों में पहले लाल डोरे उभरे और फिर दोनों का चेहरा दहकते हुए अंगारों की
मानिंद हो गया। याज्ञिक जब इस घर में घुसा था, तो बहुत खोया और गमगीन-सा था,
लेकिन अब उँगलियों में सिगरेट फँसा कर इतमीनान से धुआँ छोड़ रहा था। एक घंटे
पहले वाले वदहवास याज्ञिक की जगह अब अधिकारपूर्वक बतियाने वाला व्यक्ति बैठा
था, हालाँकि उसके कपड़े वही के वही थे और उसकी आर्थिक अवस्था भी अपनी जगह
ज्यों की त्यों थी। प्रभाकर जो दो घंटे पहले रजाई में घुसा बैठा था और अपने
पौरख थकने की याद दिला रहा था, अब अपने दफ्तर की नई रिसेप्शनिस्ट की सुंदरता
का बखान कर रहा था। थोड़ी-सी शराब आदमी को क्या से क्या कर देती है! मैं
दार्शनिक मूड में आ कर बहुत-सी बेतरतीब बातें सोच रहा था। खाली बोतल से दो-चार
बची-खुची बूँदें अपने प्याले में उँड़ेल कर प्रभाकर ने दियासलाई की जलती तीली
बोतल में छोड़ दी। तीली एक क्षण के लिए भक्क करके जली और फिर बुझ गई। प्रभाकर
के चेहरे पर संतोष उभर आया था। खाली शराब थी बेटा, इसमें पानी की एक बूँद नहीं!
कह कर प्रभाकर ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगा, अब खाने का क्या जुगाड़ करें?
वैसे मेरा खाना तो तैयार है और अब ऊपर से पुकार होने वाली है, लेकिन तुम दोनों
के लिए क्या किया जाए! मेरे कुछ कहने से पहले ही उसे रास्ता सूझ गया, 'मैं यह
न करूँ कि लौंडे को बुला कर अपना खाना नीचे ही मँगा लूँ। जो भी होगा,
थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे। प्रभाकर के प्रस्ताव पर याज्ञिक ने बलबला कर कुछ कहा और
दालमोठ की मुट्ठी भर कर मुँह की तरफ ले गया। दालमोठ मुँह में भरते ही उसे बहुत
जोर से खाँसी आई और अड्ड करके बहुत भयंकर उलटी हो गई। प्रभाकर इस स्थिति के लिए
जरा भी तैयार नहीं था। वह व्यस्तता से उठा और याज्ञिक के कंधे पर हाथ रख कर
बोला, याज्ञिक, पहले तुम उठ कर कुल्ला करो और मेरे भाई, अब तुम घर जाने की
फिक्र करो। भाभी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी। घर जाने की बात सुन कर याज्ञिक के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसका चेहरा
किसी विचित्र भय से ऐंठ गया और वह अपनी कुर्सी से उठ कर खड़ा हो गया। अपने कोट
की आस्तीन से मुँह रगड़ते हुए वह बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला, घर? अब मैं
घर कभी नहीं जाऊँगा। प्रभाकर ने आसन्न संकट सिर पर देख कर कहा, नहीं, नहीं,
याज्ञिक, घर में कहा-सुनी सबके यहाँ होती है। घर जाओ, वरना भाभी इधर-उधर दौड़ना
शुरू कर देंगी। कैसी गैर-जिम्मेदारी की बातें करते हो। चलो, मैं तुम्हें
रिक्शे पर बैठाता हूँ। प्रभाकर के बयान से जैसे याज्ञिक को कोई भूली बात याद आ
गई। उसने जोर से सुबकी ली और हाय भर कर बोला, प्रभाकर भैया, मैं घर नहीं
जाऊँगा। शाम से घर में डब्बू मरा पड़ा है... याज्ञिक के शब्द सुन कर मुझे काठ मार गया और प्रभाकर इस तरह विचलित हो कर
उछला, गोया उसका पैर साँप के फन पर पड़ गया हो। डब्बू याज्ञिक का सबसे बड़ा
लड़का था। उम्र यही होगी आठ-नौ साल की। याज्ञिक कह रहा है, उसकी मौत हो गई।
कहीं यह दीवाना तो नहीं हो गया? बेटे की लाश घर में छोड़ कर यों कोई शराब पीता
है? मेरा और प्रभाकर का नशा एक क्षण में काफूर हो गया। हम दोनों के खड़े होते
ही याज्ञिक फुक्का मार कर रोने लगा। रोते-रोते ही उसने बीड़ी सुलगाई और आँसू
पोंछता हुआ बोला, कहाँ जाऊँ?... वह न रो पा रहा था, न बीड़ी पी पा रहा था और न
कुछ तय कर पा रहा था... एक क्षण बाद ही वह फिर गहरी-गहरी साँसें ले कर जोर से
रो पड़ा। प्रभाकर के घर में कोहराम मचने के डर से मैं घबरा उठा। बिना कुछ
निश्चित किए मैं याज्ञिक को जबरदस्ती खींचते हुए बाहर सड़क पर ले आया और
दरवाजे से खींच कर बोला, प्रभाकर, भाभी से कह कर तू आ। मैं इसे ले कर चल रहा
हूँ। आप निराश न हों, ऐसी बीहड़ परिस्थितियाँ जीवन में अनेक बार आती हैं। आखिर हम
किस दिन के लिए हैं। आप निःसंकोच हो कर बतलाइए कि आपका काम कितने में चल सकता
है। खन्ना जी ने चेहरे पर बड़प्पन का भाव लाते हुए कहा। उनकी दिलासा से वह
इतना कृतज्ञ हो आया कि उसके कंधे झुक गए और चेहरे की माँसपेशियाँ आवेश में
काँपने लगीं। सांत्वना और सहानुभूति से आदमी कितना दब जाता है! वह खन्ना जी के बच्चों को कई महीनों से ट्यूशन पढ़ा रहा था। खन्ना साहब को
उसकी परिस्थितियों का आंशिक ज्ञान था। दो मास पहले उसके पिता की मौत शिवाले के
आँगन में हुई थी। मरने से कोई महीने-भर पहले उन्होंने घर की देहरी छोड़ दी थी
और अंत में पुत्र की अनुपस्थिति में ही प्राण त्याग दिए थे। गंगाजल, तुलसीदल
और किसी सगे सुबंधु की अनुपस्थिति में यह संसार छोड़ने में उन्हें जितना कष्ट
हुआ होगा, यह केवल वही जानता था। बाद में मित्रों की सहायता से उसने उनका
क्रिया-कर्म किया था। उसका मुंड़ा सिर देख कर ही खन्ना साहब को पिता के मरने का
ज्ञान हुआ था। छोटी बहन का रिश्ता पिता के सामने ही पक्का हो चुका था, लेकिन
बाद में वह पक्ष कुछ ढीला नजर आने लगा था। इस स्थिति से उबारने का वादा खन्ना
जी ने उसे भरसक सांत्वना दे कर किया था। शायद वह अपनी व्यथा-कथा खन्ना जी से न कहता, क्योंकि उसे उनके यहाँ से
सत्तर रुपए प्रतिमास मिल ही जाते थे, और फिर उसकी कोई ऐसी साख भी नहीं थी कि
कोई उसे एकमुश्त हजार-दो हजार रुपए का कर्ज दे देता। लेकिन खन्ना जी कई बार
आत्मीयता से बातचीत करके उसकी घरेलू परिस्थितियाँ जान गए थे। उनकी
शिक्षा-दीक्षा अमेरिका में हुई थी और विचारों में वह उदारचेता थे। शायद वह
मानवता को कुंठित नहीं देखना चाहते थे। एक दिन बहुत भावुक हो कर कहा भी था,
शायद आप नहीं जानते कि मुझे कितनी गंदगी और संकीर्णता से लड़ना पड़ा है। स्वयं
को स्थापित करने में मुझे कितनी अपने पिता से भी टक्कर लेनी पड़ी थी। मैं
बी.एस-सी. में हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और मेरे पिता एक लखपती थे,
लेकिन उन्होंने मुझे एक बार महीने का खर्च कभी नहीं दिया। कभी पचास तो कभी साठ
तो कभी बीस रुपए भेज देते थे। वह खन्ना जी के पिता के आचरण को एकदम नहीं समझ पाया और हैरानी से उनका
चेहरा देखता रहा। खन्ना जी ने किंचित मुस्करा कर कहा, आप ही क्या, भाई, इस
कमीनेपन को तो कोई नहीं समझ सकता। शायद इसकी वजह यह थी कि एकसाथ सौ-दो सौ रुपए
देते उनकी जान निकलती थी। आप जरा कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसके पास लाखों की
संपत्ति हो और वह अपने इकलौते बेटे को महीने का पूरा खर्च भी एक बार में न दे।
पाँच-सात हजार रुपए माहवार तो मेरे पिता सूद से ही पीट लेते थे। अपनी बात यहीं पर रोक कर खन्ना जी ने नौकर को आवाज दी और चाय के लिए कह कर
फिर अपनी रामकहानी का तार जोड़ा, तो मिश्रा जी, मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही
छोड़नी पड़ी और पानी के जहाज पर खलासी का काम करते हुए मैं अमेरिका जा पहुँचा।
वहाँ रह कर मैंने सात वर्षों में नौकरी करते ही मेकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री
ली। आप मुझसे कसम ले लीजिए जो इस पूरे अर्से में मैंने उनसे दमड़ी भी ली हो।
उन्होंने मुझे सैकड़ों खत लिखे, पर मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। उनकी मौत
के सालों बाद यहाँ लौटा तो अपने बल-बूते पर यह कारोबार खड़ा कर लिया और आपकी
दया से आज अपने पैरों पर खड़ा हो कर रोटी खा रहा हूँ। कुछ ठहर कर खन्ना साहब
ने यह भी बतला दिया था कि आखिर पिता की सारी संपत्ति भी उन्हीं को मिली थी। ये सारी तफसीलें बतलाते हुए खन्ना जी की आँखें आत्मविश्वास के दर्प से
दीप्त हो उठी और उसके अहसास में उनकी सारी देह फैल-सी गई। आपकी दया से रोटी खा
रहा हूँ, यह अंतिम वाक्य उनकी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल विपरीत लगा था। साथ
ही इतने घरेलू और आत्मीय वातावरण में एक लखपती की संघर्ष-कथा सुन कर उसने
स्वयं में भारी स्फूर्ति अनुभव की थी। खन्ना जी उससे नाटकों और कविता पर भी बहस करते थे। कभी-कभी वे उसे पढ़ने को
क्लासिक्स देते थे और यह कहना कभी नहीं भूलते थे कि स्वयं निर्मित व्यक्ति
ही ढंग से जीता है। वे कई बार यह भी कह चुके थे, मैं अपनी जीवनी लिखने बैठूँ तो
समझिए कि आपको सैकड़ों एडवेंचर और जोखिम उसमें अनायास मिल जाएँगे। सच तो यह है
कि ढोल न पीट कर जीने वाले आदमी की जिंदगी में ही खरापन मिलता है। अगर आप असली
आदमियत को परखना चाहते हैं तो वह मामूली कहे जाने वाले आदमियों में ही मिलेगी। ऐसे कितने ही खन्ना जी के लंबे-लंबे प्रवचन वह मुग्ध-सा पी लेता था। अपनी
विपन्नता भी अब उसे इतनी बुरी नहीं लगती थी। ऐसे लोग अब उसे सरासर मूर्ख लगते
थे, जो किसी को संपन्न और दुनियावी स्तर पर सफल देख कर नाक-भौं सिकोड़ने लगते
हैं। उसे यह विचार भी सारहीन लगता था कि कोई भी पैसे वाला, आदमी के दुख-दर्द से
नहीं जुड़ा होता। हालाँकि उसे कम से कम एक हजार रुपए की जरूरत थी, पर वह खन्ना जी की कृपा से
इतना अधिक अभिभूत हो उठा कि उसने सिर्फ पाँच सौ रुपए ही माँगे। खन्ना जी ने
अपने चेहरे पर दानशीलता कायम रखते हुए कहा, बस्स! पाँच सौ रुपए का चेक खन्ना जी के हाथ से लेते हुए उसका हाथ काँपा और आँखें
नम हुईं। गदगद हो कर वह मन ही मन बोला, 'दुनिया में अभी हमदर्द लोगों की कमी
नहीं है। कोई लिखा-पढ़ी नहीं की कि रुपयों को कब और कैसे लौटाना है।' उसने
कृतज्ञ भाव से खन्ना जी को मन ही मन प्रणाम किया। उस समय उसका चेहरा ताजे फूल
जैसा खिल उठा था। रुपए लिए हुए पूरे दो साल गुजर गए। इस दौरान वह खन्ना जी के यहाँ बराबर
आता-जाता रहा। यहाँ तक कि खन्ना जी का पुत्र और पुत्री उसे भाई साहब कहने लगे।
खन्ना जी की पत्नी भी उसके सामने आने लगी। वह उनकी ओर से पूर्ण आश्वस्त हो
गया था। लेकिन खन्ना जी के दोनों बच्चों के इम्तिहान खत्म हो जाने के बाद
ट्यूशन खत्म हो गया। उसकी परिस्थितियाँ सुधरने की बजाय और भी बिगड़ती गईं। वह बहन की शादी कर
चुका था, किंतु बहनोई उसकी बहन और एक बच्चे को छोड़ कर चुपचाप कहीं भाग गया था।
अब बहन और बच्चे का बोझ तो उसके सिर आ ही पड़ा था, बहनोई के भाग जाने की चिंता
अलग से सिर पर सवार थी। बहन हर समय रोती-चीखती रहती थी यद्यपि वह उसके पति को
खोजने का अथक प्रयास करता रहता था, अपनी नौकरी के बावजूद। कभी-कभी मिलते रहने से धीरे-धीरे इस परिस्थिति की जानकारी खन्ना जी को हुई
तो उन्होंने उसे डटे रहने का उपदेश भी दिया। विशेषत: अपनी दानशीलता और
निस्पृहता के किस्से सुना कर और साथ ही अपने सूदखोर दिवंगत पिता पर लानतें
भेज कर खन्ना जी अपनी बातें पूरी करते। जिस समय वह खन्ना जी को अपने संसार का सबसे अधिक सही और दानशील मनुष्य
स्वीकार करने जा रहा था, ठीक उसी समय उसकी मान्यताओं पर भयंकर कुठाराघात हुआ।
हुआ यह कि एक दिन डाकिया उसकी देहरी पर एक लिफाफा डाल गया। उसने उसे खोल कर
धड़कते दिल से पढ़ा और सन्न रह गया। यह एक टंकित इबारत थी, जिसमें खन्ना जी ने
उसे दुनिया-भर का ऊँच-नीच समझाते हुए अपने पाँच सौ रुपए की याद दिलाई थी।
उन्होंने शिष्ट भाषा में यह संकेत भी दिया था, रुपए तो आखिर लौटाने ही हैं,
और अब यों भी ढाई साल निकल चुके हैं। रुपयों की खन्ना साहब को उतनी फिक्र नहीं
थी, जितनी की इस उसूल की कि हर इज्जतदार आदमी कर्जा लौटाता है। हालाँकि खन्ना जी हिंदी बोल और लिख लेते थे लेकिन यह टंकित पत्र अंग्रेजी
में था। शायद सौजन्य-भरे तकाजे के लिए खन्ना साहब को अंग्रेजी ही ज्यादा ठीक
लगी। सहसा अपरिचय, सख्ती और ठंडे लहजे को इस भाषा में बखूबी निभाने की आदत थी
उन्हें शायद। खन्ना जी का पत्र हाथ में ले कर वह विचारों में डूब गया। उसने सपने में भी
न सोचा था कि वे किसी दिन इतने औचक ढंग से अपने रुपयों का तकाजा करेंगे। चंद
दिन पहले ही तो वह खन्ना जी से मिला था, लेकिन अपने रुपयों का उन्होंने कोई
संकेत नहीं किया था। तत्काल रुपए लौटाने की बात उसके मन में थी भी नहीं। वह
सोचता था कि थोड़ी सुविधा होते हो ही वह इस दिशा में कोई उपाय करेगा, लेकिन इस
पत्र को पढ़ कर वह गहरी चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, पाँच सौ की तो क्या
बात, वह फिलहाल पचास रुपए भी नहीं जुटा सकेगा। उसने कर्जा दबाने की बात कभी
नहीं सोची थी, परंतु उसका दीर्घघोषित तर्क यही था कि इन रुपयों को वापस करने की
अभी कोई जल्दी नहीं है। जब होंगे वह चुपचाप खन्ना जी के पैरों में रख आएगा।
यहाँ तक कि उस क्षण वह एक शब्द भी नहीं बोल सकेगा। शब्दों में आखिर रखा भी
क्या है, शब्द तो सारा अहसास भी नहीं ढो पाते हैं। उस रात वह ठीक से सो नहीं सका। उसने दूर-दूर तक सोचा, पर कोई रास्ता नहीं
दिखा। कई दिन तक भाग-दौड़ करने पर भी जब कोई बात नहीं बनी तो उसे सिर्फ एक राह
सूझी : प्राविडेंट फंड से पाँच सौ रुपए कर्ज ले लूँ। उसने तत्काल कोशिश की और
दफ्तर के बाबुओं ने भी पचास झटक लिए। उसके पास नए कर्ज में से कुल जमा चार सौ
पचास बचे। ज्यों-त्यों करके उसने पचास रुपए और जुटाए और खन्ना जी के घर दे आया।
जान-बूझ कर ऐसा वक्त चुना था कि जब खन्ना जी घर पर नहीं थे। रुपए लिफाफे में
बंद कर वह खन्ना जी की पत्नी को दे आया था। उन्होंने लिफाफा हाथ में ले कर
पूछा भी, यह क्या है भाई साहब? वह हँस कर टाल गया, बस, इतना ही कह सका, एक
गुप्त दस्तावेज है, आप खन्ना जी को दे दीजिएगा। पाँच सौ रुपया लौटाने के तीन माह बाद उसे पुन: एक टंकित पत्र मिला। अपने
दफ्तर के पत्र-पैड पर खन्ना जी ने यह पत्र इस प्रकार लिख भेजा था, आपने रुपया
पूरा नहीं भेजा है। बैंक की न्यूनतम ब्याज दर के हिसाब से ढाई वर्ष में दो सौ
रुपए से ऊपर ब्याज निकलता है। कृपया इस पत्र को पाते ही शेष धन भिजवाने का
कष्ट करें। यद्यपि दिसंबर का महीना था, तथापि उसके माथे पर पसीना चुहचुहा आया।
ऐसी अंतर्विरोधी बातें तो उसने किताबों में भी नहीं पढ़ी थीं। बाप की कंजूसी और
सूदखोरी को भला-बुरा कहने वाला कोई स्वनिर्मित संघर्षरत धनी व्यक्ति उसके
जैसी परिस्थितियों में फँसे आदमी को भला सूद से भी छूट न दें! इस बेरहम तकाजे से वह हीरे की तरह सख्त हो गया। उसने खन्ना साहब के घर
जाना तो दूर उस घर के रास्ते तक से निकलना छोड़ दिया। एक दिन उसके घर खन्ना जी का पुत्र नरेंद्र आया और कहने लगा, आप पापा को आगे
से एक पैसा भी न दें। इस बात पर मेरी उनसे काफी तू-तू, मैं-मैं हो चुकी है।
मम्मी और नीरा (छोटी बहन) भी इस बात पर बहुत नाराज हैं। पापा हमारे बाबा जी के
लिए गाली निकालते हैं और खुद उनसे भी गए-बीते हैं, उनके लिए 'ह्यूमन रिलेशन'
(मानवीय संबंध) सिर्फ मजाक की चीज है। अब उन्हें और एक कौड़ी भी न दें। मैं
देख लूँगा, वह आपसे सूद किस तरह वसूल करते हैं। वह नरेंद्र के व्यवहार से द्रवित हो उठा और आकुल हो कर बोला, नहीं, नहीं,
नरेंद्र ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारे पिता जी नेक आदमी हैं। उन्होंने मुझे
जिस आड़े वक्त पर सहायता दी थी, उसको देखते हुए ब्याज वगैरह बहुत मामूली चीज
है। हम किसी का रुपया तो लौटा सकते हैं लेकिन सहायता से मिली सांत्वना की
भरपाई तो नहीं कर सकते। फिर वह नरेंद्र की पीठ पर प्यार से हाथ रख कर बोला,
तुम इन फिजूल की बातों में न पड़ो, तुम लोगों से मेरे जो संबंध हैं, वे मेरे
खाते में एक बड़ी नियामत हैं। दिन निकलते चले गए, वह खन्ना जी को सूद की रकम नहीं भेज पाया। 'कल देखेंगे'
वाली स्थगन प्रक्रिया में अनजाने में ही कई माह निकल गए। और एक दिन आखिर
खन्ना जी उसे अपने दफ्तर में घुसते दीखे। वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और
उनके साथ चुपचाप दफ्तर से बाहर निकल आया। साथ-साथ चलते हुए यकायक उसे उन्हें
निहारने की इच्छा हुई। उसने देखा कि पस्तकद का चुँधी-चुँधी आँखों वाला यह
गंजा आदमी मानवीयता का एक नमूना है। चश्मे के भीतर से खन्ना जी की आँखें उसे
बिज्जू की आँखें जैसी लगीं। उसने तैश में कुछ बातें कहनी चाहीं, लेकिन फिर वह
ढीला पड़ गया। दफ्तर के बाहर एक खाली जगह पर पहुँच कर खन्ना जी बोले, मिश्रा
जी, आपकी तरफ दो सौ रुपए और निकलते हैं। मैंने आपसे कोई लिखा-पढ़ी भी नहीं की
थी। चूँकि यह इंसानियत का सवाल था। आज मेरी पावनादारी की मियाद खत्म हो रही है
और मैंने आपसे एक रुक्का भी नहीं लिखवाया। वह इस 'इंसानियत' शब्द से यकायक भड़क उठा और धैर्य छोड़ कर बोला, खन्ना जी,
फिलहाल उतने रुपए तो मेरे पास हैं नहीं, जब होंगे तब आप जो कहेंगे, दे दूँगा,
चाहें तो आप लिखवा लें। आपकी जैसी मर्जी, कहते हुए खन्ना जी ने सड़क से गुजरते रिक्शे वाले को
आवाज दी और उससे बोले, आइए, रिक्शे में आ जाइए, अभी पंद्रह मिनट में वापस चले
आइएगा। वह बिना कुछ समझे-बूझे उनकी बगल में बैठ गया। रिक्शा चालक से खन्ना जी
ने कहा, जरा जल्दी से कचहरी चलो। रिक्शा सड़क पर दौड़ने लगा। वह सब तरफ से बेखबर हो कर सड़क पर यत्र-तत्र
छितराई भीड़ देखने में डूब गया। सारी चीजों के प्रति उसका भाव एकदम तटस्थ
दर्शक जैसा हो गया। वह एकदम भूल गया कि दफ्तर से बिना किसी से कुछ कहे ही
खन्ना जी के चंगुल में फँस आया है। कचहरी के गेट के सामने पहुँच कर खन्ना
साहब ने रिक्शावाले को पैसे चुकाए और एक झोपड़ी की तरफ बढ़ लिए। वह भी
अनजाने-सा उनके पीछे चलता रहा। खन्ना जी ने झोपड़ी में घुसने से पहले उसकी ओर मुड़ कर देखा और बोले, आ
जाइए। वह भी झोपड़ी में घुस गया। वहाँ एक चौकी और दो-तीन मरी-मरी सी कुर्सियाँ
पड़ी थीं। चौकी पर एक टीन का संदूक रखा था और अधेड़ उम्र का मरगिल्ला-सा
व्यक्ति स्टांप पेपर पर कोई इबारत लिख रहा था। खन्ना जी को देख कर वह बोला,
आइए बैठिए, एक मिनट में फारिग हो कर आपका काम करता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है, जरा जल्दी है, लंबा काम हो तो उसे फिर निबटा लेना। कह कर
खन्ना जी ने अपने बैग से एक स्टांप पेपर निकाल मुंशी के हाथ में थमाया। मुंशी
ने हाथ का काम छोड़ कर स्टांप पेपर अपने सामने संदूक पर रखा और यह लिखने लगा,
'मैंने 250 रुपए मुबलिग जिसका आधा एक सौ पचीस रुपए आज दिनांक... को विहारीलाल
खन्ना वल्द हीरालाल से कर्ज लिया, जिसका बैंक दर से सूद मय मूलधन देने की
देनदारी मेरे सिर पर है। इतना लिखने के बाद उसने सिर उठा कर खन्ना साहब से
व्यस्तता दिखलाते हुए पूछा, मगर वह आदमी कहाँ है, जनाब?' 'मगर वह आदमी कहाँ है, जनाब' उसके सिर में इस तरह बजा जैसे किसी ने घंटे पर
हथौड़े की चोट की हो। वह सहसा आगे बढ़ कर बोला, अगर आप मुझे आदमी मान सकें तो
वह बदनसीब मैं ही हूँ! उसके इतना कहते ही खन्ना जी और मुंशी एकदम सकपका गए।
खन्ना जी के स्वर में खासा उखड़ापन था, आदमी नहीं, मुंशी जी, आप ही हैं वह
मिश्रा जी। 'अच्छा, अच्छा, कहते हुए मुंशी बिलकुल सिटपिटा गया। शायद यह उसकी कल्पना
में भी नहीं था कि सिर्फ ढाई सौ रुपया कर्ज ले कर स्टांप लिखने वाला आदमी ऐसा
भी होता है, जिसे अमूर्त करके अनदेखा नहीं किया जा सकता। वह अपनी कई दिनों की
बढ़ी हुई दाढ़ी खुजलाते हुए बोला, माफ करना बाबू साहब, आप जरा इधर दस्तखत बना
दीजिए। उसने मुंशी के लगाए हुए निशान पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद मुंशी ने उसकी
तरफ निगाह भी नहीं उठाई। वह खन्ना और उसे विस्मृत करके पहले वाली तहरीर में
उलझ गया। असमंजस में वह एक मिनट तक गुमसुम हो कर खड़ा रहा और फिर खन्ना जी और मुंशी
जी को उसी झोपड़ी में छोड़ कर कचहरी के गेट से तेजी से बाहर निकल आया। अपने दफ्तर की ओर कदम नापते हुए उसके दिलो-दिमाग की शिराओं में 'मगर वह आदमी
कहाँ है' बार-बार तेजी से गूँज रहा था। 'तुम्हें मालूम है, हम लोग लड़ाई में भी साथ-साथ रहे थे।' मैं एक छोटे-से रूमाल से गर्दन और बाँहों पर बहते पसीने को पोंछ-पोंछ कर
परेशान हो रहा था। यों मेरी अटैची में एक छोटा तौलिया रखा था, जो इस पसीना
सुखाने वाली क्रिया के लिए ज्यादा उपयुक्त था पर अटैची खोल कर तौलिया निकालना
मुझे एकदम अप्रासंगिक लगा। उनकी बात को बहुत ध्यान दे कर एकाग्रता से सुनने का भाव चेहरे पर ला कर
मैंने कहा, 'अच्छा! लेकिन कब? 'सेकेंड वर्ल्ड वार' में?' वह 'सेकेंड वर्ल्ड वार' का नाम सुन कर बड़े जोर से हँस पड़ीं। कोई डेढ़-दो
मिनट तक खुल कर हँसने के बाद बोलीं, 'बाबा रे बाबा! 'सेकेंड वर्ल्ड वार' का तो
बस मुझे नाम भर मालूम है। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी!' और सहसा वह मुझसे
पूछ बैंठी, 'तुम्हें मेरी उम्र कितनी मालूम पड़ती है?' मैं उनकी जिज्ञासा सुन कर उलझन में पड़ गया। इस घर में आए अभी पाँच-सात मिनट
मुश्किल से हुए होंगे। अपना परिचय देने के लिए मैंने बड़े भैया का पत्र उनके
हवाले कर दिया था। यह पत्र इस घर के मालिक प्रकाश के लिए था जो अभी तक दफ्तर से
नहीं लौटे थे। घर में बच्चे भी नहीं थे, शायद वे स्कूल में रहे हों या फिर
हों ही नहीं और वह मुझसे अपनी उम्र के बारे में पूछ रही थीं उनकी उत्सुकता-भरी
आँखों को मैं दरगुजर नहीं कर सका। लगभग सत्रह-अठारह वर्ष पहले मेरे भाई-भाभी और ये लोग साथ रहे थे। अलग हो
जाने के बाद इन लोगों का एक-दूसरे से मिलना-जुलना भी नहीं हो पाया था। अब इतने
वर्षों के अंतराल पर मैं इस शहर में एक इंटरव्यू देने आया था। और मुझे कम से कम
दो रातें यहीं ठहरना था। बड़े भैया का पत्र पढ़ कर घर की मालकिन ने मुझे बैठने
के लिए कुर्सी और पीने को पानी का गिलास दे दिया था। छत का पंखा भी खोल दिया था
और अब वह अपनी उम्र जानने की उत्कंठा चेहरे पर लिए मेरी तरफ ताके जा रही थीं। मेरी चेतना में उनके दो वाक्य बराबर चकरघिन्नी की तरह चक्कर काट रहे थे,
'हम लोग लड़ाई में भी साथ-साथ रहे थे।' 'तुम्हें मेरी उम्र कितनी मालूम पड़ती है?' मेरी इच्छा हुई कि मैं उनकी उम्र के बारे में कुछ अनुमान लगाने की कोशिश
करूँ, शायद थोड़ी-बहुत सफलता हाथ लग जाए। लेकिन यह काम दुखदायी और जोखिम-भरा
था। औरतें (और अब आदमी भी) अपनी उम्र के दस-बीस बरस एक ही बार में जिस तरह उड़ा
देते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। जिसे आप पच्चीस वर्ष का कहने की सोच रहें हैं,
हो सकता है वह पैंतालीस को ठेंगा दिखा चुका हो। कहीं आपने भूल से उसे पच्चीस
का कह दिया तो वह आपको सिरे से बुद्धू घोषित करके अपनी जन्मपत्री ला कर दिखा
देगा, और बतला कर रहेगा कि वह बाईस बरस पहले पच्चीस साल की उम्र को पीछे छोड़
आया है। बहुत सिर मारने के बाद मुझे एक सूत्र हाथ आया तो मैं गदगद हो उठा। मुझे अपनी
भाभी की उम्र याद आ गई। बस, समस्या हल हो गई। अब मैं चाहूँ तो इन्हें भाभी की
उम्र से दो-चार साल पीछे धकेल कर अनुमानत: सही उम्र बतला सकता हूँ। पर अगले ही
पल मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया, क्योंकि भाभी की उम्र अड़तीस पार कर चुकी थी।
भला किसी महिला की उम्र चौंतीस-पैंतीस बरस बतलाई जा सकती है? खैर, मैंने इस
जानलेवा सिलसिले को एक तरफ ठेल कर दिमाग के बाहर कर दिया और 'लड़ाई' की दिशा
में लौट आया, 'आप लड़ाई में साथ-साथ रहने के बारे में कुछ बतला रही थीं!
'इंडो-चाइना वार' में आप लोग साथ रहे होंगे।' अपनी तरफ से निष्कर्ष निकालने के पहले मैंने दिमागी तौर पर बहुत दूर तक
सर्वे किया था, क्योंकि उस दौरान दादा के ये मित्र और दादा नवविवाहितों की
गिनती में थे। हो सकता है, इन दोनों परिवारों ने युद्ध का आतंक साथ रह कर झेला
हो। लेकिन मेरे अनुमान पर इस दफा तो वह एकदम बेलाग हो कर हँसने लगीं। वायु से
बेतरह फूली उनकी देह कुर्सी में फँसे-फँसे यों हिलने लगी, गोया मोटर के ट्यूब
में हवा भरने का कार्यक्रम चल रहा हो। लाचारी में हँसते चले जाने पर जब उनकी साँस फूल गई तब उन्हें अपनी भद-भद
हँसी पर काबू करना पड़ा और मुझे दिलचस्पी से देखते हुए बोलीं, 'सचमुच क्या
आशा ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बतलाया?' 'किस संबंध में?' मैंने बगैर सोचे-समझे अपना सवाल उछाल दिया। उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए असमंजस उभरा, लेकिन फिर वह अपने अंतर्द्वंद्व
पर काबू पा कर बोलीं, 'तुम्हें मालूम है मेरी और आशा की शादी एक ही महीने में
हुई थी और हम लोग नैनीताल में 'हनीमून' मनाने गए थे?' 'हनीमून मनाने गए थे' उन्होंने जिस शेखी से कहा उसका उदाहरण मिलना कठिन हैं
बाईस-तेईस बरस के लड़के को 'हनीमून' मनाने के चर्चे में शामिल कर लेने में शायद
उन्हें कहीं कोई कठिनाई नजर नहीं आती थी। बस, गनीमत यही हुई कि वह इस 'हनीमून'
मनाने से आगे भी बढ़ गईं। 'तो वहाँ नैनीताल में सारे बड़े होटल घिर गए थे। काफी दूर जा कर एक मकाननुमा
होटल में चालीस रुपए रोज पर एक-दूसरे से जुड़ी हुई दो कोठरियाँ मिलीं, जिनका
पाँच रोज का एडवांस पहले भरना पड़ा। मैंने और आशा ने तय किया कि जो भी खर्च
करना हो, आधा-आधा साझे में करेंगे। सौ मैंने और सौ आशा ने दिए तो मकान का
किराया जमा हो गया। अपनी बात बीच में ही रोक कर वह हँसने लगीं और आधे मिनट बाद हँसी को सहसा
'ब्रेक' दे कर बोलीं, 'एक बात मैं कहूँगी...।' एक बार मेरी ओर सहायता के लिए
देखा तो मैं तत्काल समझ गया कि वह मेरा नाम जानने को व्याकुल हैं। मैंने कहा,
'जी, मुझे उमेश कहते हैं।' 'अच्छा, तो हाँ भैया उमेश, एक बात मैं कहूँगी। आशा में चालाकी शुरू से ही
है।' उन्होंने मेरी ओर ऐसी आँखों से देखा, जैसे मेरे मुँह से ही तसदीक कराना
चाहती हों कि आशा भाभी वाकई चालाक हैं। 'तुम तो उसके सगे देवर हो, इतने दिनों से साथ रहते हो, उसकी यह बात तो जान
ही गए होगे?' उनकी बातों से मुझे भीतर ही भीतर बेचैनी होने लगी। कैसी औरत के पास भेज दिया
मुझे? अब मैं इससे इस बात पर बहस शुरू करूँ कि आशा भाभी चालाक हैं या नहीं! मुझे कुछ भी न कहते देख कर उन्होंने स्वयं ही निष्कर्ष निकाला, 'लड़के हो
अभी, तुम्हें पता नहीं चलता होगा। फिर बुरे आदमी के साथ रहते-रहते उसकी बुराई
पर नजर भी नहीं जाती। मैंने तो पहले दिन ही परख लिया था कि आशा बहुत तेज है।'
वह फिर से हँसने-मुस्कराने लगीं, जैसे बच्चा मुँह में मीठी गोली डाल कर मुदित
भाव से चूस रहा हो। 'तुम्हारे भाई साहब नरेश बाबू भी उसके जादू में बँध गए थे। आशा जिधर चाहती,
नकेल पकड़ कर सुरेश को उधर ही घुमा देती थी। थी भी तो बहुत सुंदर! आदमी बेचारा
करे भी तो क्या करे! सुंदरता तो चीज ही ऐसी है। उसके आगे तो अच्छे-अच्छों को
पानी भरना पड़ता है।' पता नहीं कौन-कौन से विचित्र रहस्य उनके मन में दफन थे। वह बोल रही थीं और
मैं चुपचाप सुन रहा था, 'हम लोगों ने तय किया था कि खाना-पीना अपने हाथों तैयार
करेंगें। एक दिन तो उसने मेरे साथ लग कर मन से खाना तैयार करवाया और अगले दिन
वह अपना घुटना पकड़ कर पलँग पर लेट गई। नरेश बिचारा भी परेशान! आशा के आगे-पीछे
चक्कर काटता फिरे। कभी मालिश की दवा की शीशी हाथ में तो कभी 'हाट-वाटर बॉटल'।
आखिर हार-थक कर मैं और प्रकाश होटल से बाहर चले गए।' हालाँकि वह अपनी दास्तान कहते-कहते हाँफने लगी थीं, लेकिन इस चर्चा को आगे
बढ़ाने के लिए उनमें अदम्य उत्साह नजर आता था। उन्होंने अपनी कहानी आगे बढ़ाई, 'तुमको यकीन नहीं आएगा उमेश, कि मैंने और
प्रकाश ने उसी शाम आशा और नरेश को पहाड़ी रिक्शे पर बैठ कर एक दुकान के सामने
'कोल्ड ड्रिंक्स' पीते देखा। पर मैंने यह बात उन दोनों को कभी नहीं बतलाई। भई,
फिजूल में लड़ाई-झगड़ा, कहा-सुनी मुझे पसंद नहीं है और फिर फायदा भी क्या है,
जो आदमी जान-बूझ कर बीमार बन जाए, उसे कौन ठीक कर सकता है?' मुझे बहुत तेज प्यास महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे अपने भाई और भाभी के बारे
में अलिफ-लैला के किस्से सुनने पड़ रहे थे। यों हमारे अपने घर में एक या दो
मेहमान हमेशा ही ठहरे रहते थे और आशा भाभी को ही घर का सारा काम सँभालना पड़ता
था। लेकिन इस किस्म की बनावटी बीमारी का परिचय उन्होंने कभी नहीं दिया था।
खैर, मुझे उनकी बतलाई हुई बातें सुननी ही पड़ती सो मैं सुन रहा था। अपनी ही
बातें बीच में रोक कर वह सहसा पूछ बैठीं, 'क्या आशा अभी वैसी ही इकहरी, छरहरी
और सुंदर है?' मैंने अनजाने में ही झट से गर्दन हिला कर आशा भाभी की सुंदरता की ताईद कर
दी। उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, 'कितने बच्चे हो गए आशा के?' इस बार उत्तर देने में मैंने और भी जल्दी दिखाई, 'चार बच्चे हैं। बड़ा
लड़का पंद्रह का है; हाईस्कूल पास कर गया है, कॉलेज में पढ़ रहा है।' शायद
उनकी बात से मैं भीतर ही भीतर चिढ़ गया था और उन्हें कष्ट देने की गरज से आशा
भाभी को चार बच्चों की माँ हो जाने के बावजूद सुंदर सिद्ध करना चाहता था। 'हरे राम!' उनके मुँह से यों निकला, जैसे उन पर अचानक वज्रपात हो गया हो। वह
लंबी साँस खींच कर बोलीं, 'मुझे तो पहले बच्चे ने ही दमे की बीमारी दे दी।
सारा बदन फूल गया है। चला-फिरा तक नहीं जाता।' और वह इस तरह काँखने लगीं, जैसे
बस दमे का भीषण आक्रमण होने ही वाला हों। अपनी अन्य जिज्ञासाओं की तरह उन्होंने आशा भाभी की सुंदरता को भी जहाँ का
तहाँ छोड़ दिया और पूछने लगीं, 'नरेश की तनखा तो अब काफी हो गई होगी?' मैंने फौरन कहा, 'हाँ, हजारेक मिलते हैं।' 'बस्स?' उन्होंने मुँह बिचका कर कहा, 'हजार अब क्या होते हैं? इन दिनों
तो पाँच हजार भी कुछ नहीं है। प्रकाश को तीन हजार मिलते हैं, तब भी किच-किच मची
रहती है। आशा तो बिचारी इतने थोड़े रुपयों से बहुत दुखी रहती होगी। चच्च!
कितनी गुड़िया-सी सुंदर थी जब ब्याह कर आई थी! नरेश ने कोई मोटर साइकिल वगैरा
ली?' 'कहाँ? वह तो उसी सड़ियल-सी साइकिल पर दफ्तर जाते हैं।' मैंने उन्हें सूचित
किया। उन्होंने मेरी बात पर टिप्पणी जड़ दी, 'नरेश ने भी तो हद्द ही कर डाली! इस
जमाने में चार-चार बच्चे! आशा कितनी नाजुक थी! भला चार-चार जाए उसके बिरते में
थे? नरेश में गँवारपन शुरू से ही है। आशा की शादी तो किसी अफसर से होनी चाहिए
थी।' फिर उन्होंने कड़वा-सा मुँह बना कर पूछा, 'कै लड़कियाँ हैं?' मैंने इस बार ससंकोच कहा, 'तीन!' 'लो भई, हद्द ही कर दी उस भले मानस ने! जब पहलौठी में ही बेटा हो गया था तो
लड़कियों की लंगर लगाने का क्या शौक पड़ गया था? यहाँ तो पहलौठी लड़का हो जाता
है तो दुबारा...!' उन्होंने अपनी बात बीच में ऐसी जगह तोड़ दी, जहाँ से उसके
खाली स्थान को भरना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था। जिस ढंग पर वह हमारे सारे परिवार के परखचे उड़ाने पर अमादा थीं, वह मेरे लिए
अकल्पनीय था। मैंने विषयांतर करने की चेष्टा की, 'आप कुछ लड़ाई की बाबत बतला
रही थीं!' 'अरे वो! तुम भी बड़े भोले बच्चे लगते हो! कौन-सी क्लास का इम्तिहान दिया
है? आशा अभी से तुम्हें नौकरी में क्यों धकेल रही है? उसके मालिक ने तो
छब्बीस साल की उम्र में नौकरी शुरू की थी।' 'मैं भी तेईस का हो गया हूँ। एम.एस-सी. पास किए भी एक साल से ऊपर हो गया
है।' मैंने उनका अज्ञान दूर करना चाहा। 'अच्छा? लगते तो तुम बचकू हो! नरेश तो एकदम ताड़-सा लंबा है, तुम छुटकू
कैसे रह गए?' उन्होंने मेरी पूरी देह की देख-भाल की और निष्कर्ष निकालते हुए
बोलीं, 'क्या शुरू से ही आशा के पास रह कर पढ़े हो? तब तो वह बड़ी डींग हाँका
करती थी कि घर में 'वनस्पति' नाम को भी नहीं आता। देसी घी पर उसका बड़ा जोर था।
अब पाँच बच्चों के लिए देसी घी कहाँ से आता होगा? मैंने उनकी भूल सुधारने की गरज से कहा, 'पाँच नहीं, चार ही बच्चे तो हैं!' उन्होंने लापरवाही से हवा में हाथ घुमाया और लगभग झिड़की-सी देते हुए कहने
लगीं, 'अरे, चार ही सही! चार में भी बाजा बज जाता है। फिर पाँचवाँ होते क्या
देर लगती है? अभी क्या आशा की उमर बीत गई?' जैसे बिगड़ैल टट्टू रास्ता छोड़ कर बगटुट भाग निकलता है, उसी तरह वह बार-बार
अपने असली मुद्दे से इधर-उधर भाग रही थीं। आशा भाभी को ले कर उनके आक्रोश की
कोई सीमा नहीं थी और दिलचस्प बात यह थी कि पिछले पंद्रह-सोलह बरसों में
उन्होंने न आशा भाभी को देखा था और न उनका कोई समाचार जानने की कोशिश की थी।
यही नहीं, आशा भाभी ने भी कभी उनके संबंध में मुझे कुछ नहीं बतलाया था। इन
पति-पत्नी की (शादी के समय की) एक फोटो उनके एलबम में जरूर थी, जिससे इतनी-सी
सूचना मिलती थी कि दोनों परिवार कभी न कभी और कहीं न कहीं साथ रहे हैं। मुझे
इंटरव्यू देने इस दूर-दराज महानगर में न आना होता तो शायद ही कभी मैं इस भली
महिला के दर्शन कर पाता ओर यह तो कभी जान ही न पाता कि हमारे परिवार को ले कर
वह अपने दिल में कितने गहरे जख्म सँजोए बैठी हैं। अब मुझे उनके हमलों में कुछ अजीब ढंग का रस आने लगा था। मैंने उन्हें फिर
छेड़ा, 'वह लड़ाई वाली बात...!' 'अरे भई, ओफ्फोह! तुम भी कमाल के लड़के हो!' उन्होंने प्रसंग बदल कर पूछा,
'फिर कभी नैनीताल गई आशा?' 'सात-आठ साल पहले गई थीं।' मैंने उन्हें सूचित किया। 'अकेली गई होगी!' 'नहीं, सभी लोग गए थे।' मैंने उनके अनुमान पर चोट की। 'घूमने-फिरने गई होगी - दो-चार दिन के वास्ते।' 'नहीं, हम लोग नैनीताल पूरे जून-भर रहे।' मैंने उनके मंतव्य की गहराई में
घुसे बिना कहा। उनकी आँखें फटी रह गईं। उतावली-से उन्होंने सवाल किया, 'पूरे महीने होटल
में रहे तुम लोग?' 'नहीं, दादा के एक दोस्त के मकान में ठहरे थे; उनका परिवार भी गया था।' 'वही तो मैं कहूँ।' उन्होंने संतोष की लंबी साँस ली और सहसा दुःख में डूब
गईं, 'मैं तो अब पहाड़ पर जा ही नहीं पाती। दमे का जोर होने लगता है। एक बार
'आबू' गई थी। चार-छह दिन बाद ही तबियत बिगड़ गई। लाचार हो कर लौटना पड़ा।' मैंने प्यास की शिद्दत से होठों पर जीभ फेरी, पर मेरी इच्छा पानी का गिलास
माँगने की नहीं हुई। वह भी मेरी प्यास के बारे में कुछ नहीं जान पाईं और परम
आत्मीयता से पूछने लगीं, 'जब तीन-तीन लड़कियाँ हैं तो नरेश ने कुछ रुपया-पैसा
तो जमा किया होगा?' मैंने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया, 'पता नहीं।' 'तुम्हें पता हो या न हो; क्या जमा करेगा वह? आशा लाख चालाक सही, रुपया
जोड़ना उसके भी बस का नहीं है। फिर हजार-बारह सौ में होता ही क्या है इस जमाने
में?' रुपए की बाबत बोलते-बोलते सहसा उन्हें वह बात याद आ गई जो उन्होंने मेरे
आते ही शुरू की थी, 'हम लोग नैनीताल में उस दफा सिर्फ पाँच ही दिन ठहरे। उतने
ही दिनों में मैंने देख लिया कि हम दोनों में से कोई खुश नहीं रहा। चौके का
पूरा सामान खरीद लिया गया था। मिट्टी का तेल, तवा, चिमटा ओर परात भी बाजार से
ही ली गई थीं। पर जब आशा ने चौके का काम एक दिन भी कायदे से नहीं कराया तो हमने
सोचा बेकार बदमजगी बढ़ाने से क्या फायदा! मैंने और प्रकाश ने कुछ दिन लखनऊ
रहने की सोची।' 'लेकिन जून के महीने में तो लखनऊ भट्ठी हो जाता है! नैनीताल से लखनऊ जाने की
सोची आपने?' मैंने अपनी शंका व्यक्त की। 'अब क्या किया जाए? हालाँकि मेरे 'हसबैंड' प्रकाश ने कहा भी कि आशा उम्र
में छोटी है, उसमें बचपना है। उसकी बात पर मत जाओ। लेकिन मैंने कहा, यह भी कोई
बात हुई। आशा अगर छोटी है तो क्या मैं बूढ़ी हो गई?' वह बूढ़ी थीं या नहीं मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल था, क्योंकि बाल सफेद
हो जाना और खाल पर सैकड़ों सिलवटें पड़ जाना ही अगर बुढ़ापे के लक्षण हैं तो वह
कतई बूढ़ी नहीं थी। मगर उनके चेहरे की कुदरती रौनक उन्हें न जाने कब की धोखा
दे गई थी। वह एक कीमती साड़ी पहने थीं, आभूषण भी धारण किए थीं, माँग में गहरी
सिंदूरी रेखा भी चमक रही थी। पर चेहरे पर इस सबके बावजूद गहरा विकर्षण मौजूद
था। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, 'उस होटल से भी हम लोग अनोखे ढंग से निकले।
दरवाजे पर लगे ताले की दो चाबियाँ तो थीं ही जब आशा ओर नरेश कहीं घूमने गए, तो
मैंने और प्रकाश ने तय किया कि अब चल निकलें! लेकिन नहीं, मैंने फिर सोचा ऐसे
जाना ठीक नहीं होगा। एक बोतल मिट्टी का तेल रखा था, उसे मैंने आशा के स्टोव
में डाल दिया। झाड़ू अपने बिस्तर में बाँध ली, परात भी अपने ही बिस्तर में
डाल ली और बाकी सारे बर्तन आशा के लिए वहीं छोड़ दिए। प्रकाश को मैंने बाजार भेज
कर एक पीतल की थाली भी मँगवा ली, जिसे मैंने आशा के लिए छोड़ दिया, कहीं उसे यह
न लगे कि मैंने ज्यादा सामान अपने लिए रख छोड़ा है।' वह परम उत्साह में बर्तन-भांडों के बँटवारे की तफसील सुनाती रहीं और मैं
आश्चर्यविमूढ़ हो कर सुनता रहा। 'और फिर मैं और प्रकाश घूमने निकल गए। हम लोगों ने उस दोपहर खाना भी बाहर
होटल में खाया। अब दो-ढाई बजे मैं और प्रकाश लौट कर आए तो देखा कि आशा और नरेश
भी अपना बिस्तर बाँधे बैठे थे। दो कुली बुलवाए गए और हम साथ-साथ बस-स्टैंड
पहुँचे। नैनीताल से हम लोग एक ही बस में वापस लौटे।' वह लौटते समय कितनी सहज और
तनाव-मुक्त थीं, इसका उदाहरण उन्होंने हँसते हुए पेश किया, 'मैं और आशा एक
सीट पर बैठे और प्रकाश-नरेश एक साथ।' सोलह-सत्रह वर्ष पुरानी इस विचित्र पहाड़ की वापसी का मैं सिर-पैर कुछ नहीं
समझ पाया। क्यों तो ये लोग पहाड़ गए थे और क्यों झख मार कर महज पाँच ही दिन
में वापस लौट आए। जिस 'हनीमून' का शुरू में इस महिला ने बड़े जोश-खरोश से
उल्लेख किया था, उसका क्या बना, यह भी मुझे अंत तक मालूम नहीं हो पाया। ठीक इसी समय 'डिंग-डांग' करती दरवाजे की घंटी बज उठी। वह बड़े आलस्य से उठते
हुए बोलीं, 'लो, प्रकाश आ गए।' एक बहुत ही नाटे कद का गोल-मटोल व्यक्ति, गर्दन पर बहते पसीने को रूमाल से
रगड़ते हुए अंदर आ गया। उसने मेरी तरफ सरसरी दृष्टि से देखा। शायद गहरी और
दिलचस्पी की नजर से देखने की शक्ति उसमें इस क्षण बाकी रह भी नहीं गई थी।
उन्होंने उसे बतलाया, 'नरेश का भाई है। बैंक में इंटरव्यू देने आया है। नरेश
का खत भी लाया है।' कई क्षण तो वह लस्त-पस्त आदमी शायद यही समझने की कोशिश करता रहा कि यह
'नरेश' कौन है। फिर उसने पूछा, 'चिट्ठी कहाँ है?' 'चिट्ठी बाद में देखना,' उन्होंने बेसब्री से कहा, 'तुमने खिड़की के काँच
के लिए बोला किसी को? अब बारिश शुरू हो गई है। बौछारें सीधी कमरे में आती हैं
और टेलीविजन पर गिरती हैं।' उस भले आदमी ने चिचचिपे बदन से बुश्शर्ट खींच कर उतारी और डाइनिंग टेबिल के
इर्द-गिर्द पड़ी कुर्सियों पर फेंकते हुए परम धैर्य से कहा, 'हाँ, मैंने शीशे
के लिए बोल दिया है। वह नाप लेने आता ही होगा।' 'अच्छा! गाड़ी का क्या बना? अब कितने दिनों तक यों ही गाड़ी वर्कशाप में
पड़ी रहेगी?' वह शख्स बहुत धीमे, मगर नपे-तुले शब्दों में बोला, 'कल सुबह फिरोज साहब
इधर हो कर ही निकलेंगे। मैं उनकी गाड़ी में ही वर्कशाप चला जाऊँगा। मगर अभी एक
हफ्ता तो लग ही जाएगा...' उन्होंने अपने पति महोदय को बात पूरी करने का अवसर नहीं दिया। बीच में ही
कूद पड़ी, 'लिफ्ट आज फिर काम नहीं कर रही है! भला सात-सात मंजिल कौन सीढ़ियाँ
चढ़ेगा!' प्रकाश बाबू चेहरे पर पूर्ववत गंभीरता रख कर मिनमिनाए, 'हाँ, बड़ी मुश्किल
है। सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते मेरा तो दम फूल गया। एकाध बार और चढ़ना पड़ गया तो
'एक्यूट टाइप' का ब्लड प्रेशर हो जाएगा।' प्रकाश साहब अपनी बात खत्म करके टेलीफोन की तिपाई के पास दीवाल पर जा कर
बैठ गए और बोले, 'जरा एक गिलास पानी देना।' उनकी पत्नी अपनी कुर्सी से दम लगा कर उठीं और बोलीं, 'हाँ, आज फ्रिज भी
बेकार हो गया, दोपहर से।' फिर मेरी ओर संकेत करके प्रकाश जी को बतलाने लगीं,
'इन्हें भी टेप का वाटर दिया हैं।' प्रकाश ने उनकी सूचना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और वह टेलीफोन का डायल
घुमाने लगे तो उन्हें सहसा कुछ याद आ गया और वह जल्दी-जल्दी बोलने लगीं,
'टी.वी. में पिक्चर ठीक से 'फोकस' नहीं हो पा रही है। जरा उधर भी फोन कर
देना।' इसके बाद वह मेरी ओर मुखतिब हो कर बोलीं, 'फ्रिज की वजह से तुम्हें भी
ठंडा पानी नहीं मिल पाया और 'लिफ्ट' खराब होने से पैदल ऊपर आना पड़ा।' उन्होंने प्रकाश जी को एक गिलास पानी ला कर दिया तो उन्होंने उसे एक तरफ
रख दिया। शायद वह बेहद प्यासे भी थे, लेकिन सात मंजिल तक सीढ़ियाँ फलाँगने के
बाद भी उन्हें घर की महत्वपूर्ण, मगर बिगड़ैल उपलब्धियों ने इतना चैन नहीं
लेने दिया था कि वह शांति के साथ पानी पी सकें। शायद वह फोन में उलझ कर यह भूल गए कि उन्हें पानी का गिलास दिया जा चुका
है। वह बोले, 'बीनू, जरा पानी तो देना।' वह मेरी तरफ देख कर मुस्कुराईं और बोलीं, 'देखा! प्रकाश एकदम फिलासफर हो गए
हैं। इन्होंने अपने हाथ से पानी का गिलास नीचे फर्श पर रखा है और अब फिर से
पानी माँगे जा रहे हैं।' लेकिन उन्हें एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि उनके
पति की शक्ति इस कदर क्षीण भी हो सकती है कि वह झुक कर फर्श से पानी का गिलास
ही न उठा पाएँ। पत्नी की बात सुन कर प्रकाश जी के मस्तक पर हल्की-सी सिलवटें आईं, लेकिन
तत्काल गायब भी हो गईं। उन्होंने पति के निकट जा कर पूछा, 'चाय अभी लोगे, या
कुछ देर बाद?' प्रकाश बाबू अभी कोई उत्तर नहीं दे पाए थे कि दरवाजे की घंटी
फिर से बज उठी। प्रकाश बाबू ने उठ कर द्वार खोला तो एक अधेड़ उम्र के आदमी ने
भीतर घुस कर सलाम किया और पूछने लगा, 'किस खिड़की का काँच टूटा है मेम साब?' वह शख्स मिस्त्री था। उसने अपनी जेब से इंच-टेप निकाली ओर आँखों पर ऐनक
चढ़ा कर जेब से एक छोटी-सी मटमैली जिल्दवाली डायरी निकाल ली। वह व्यस्तता से
डायरी में कुछ नोट करने लगा। उसने डायरी एक तरफ रख कर इंच-टेप से खिड़की का नाप
वगैरह लिया और उसे डायरी में टीप लिया। अभी वह अपने नाप-जोख से फारिग भी नहीं
हो पाया था कि उससे ताबड़तोड़ सवाल किए जाने लगे, 'कितना काँच लगेगा?' '......' 'आज कल शीशे का क्या भाव चल रहा है?' '......' 'पहले तो पूरी खिड़की का शीशा सोलह रुपए में आ जाता था?' '......' 'पता नहीं, आजकल कैसा काँच आने लगा है; हर छह महीने में 'क्रेक' हो जाता है।
पहले तो...!' मिस्त्री पति-पत्नी के हड़बोग-भरे संवादों से पूरी तरह बेखबर हो कर कुछ
हिसाब जोड़ता रहा और मैं उस घर में एक फालतू जिंस बना कुर्सी से चिपका बैठा
रहा। मेरे सौभाग्य से एकाएक एक अच्छा संयोग उपस्थित हुआ। वे दोनों मिस्त्री को
घेर कर अंदर बेडरूम की तरफ ले गए, शायद उधर भी किसी खिड़की-जंगले का काँच टूटा
था या टूटने ही वाला था। उन लोगों के जाते ही मैंने अपनी अटैची बहुत सफाई से
उठाई और लंबे-लंबे डगों से फर्श नापता दरवाजा लाँघ गया। उस समय मुझे यह भी नहीं
सूझा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ! इतने बड़े महासागर जैसे फैले महानगर में एक भी
व्यक्ति और एक भी स्थान से परिचय न होने की दशा में सात मंजिलों की सीढ़ियाँ
उतर कर मैं बाहर सड़क पर आ गया। मेरा धुँधला-सा परिचय केवल उस स्टेशन से था, जहाँ मैं दोपहर को गाड़ी से
उतरा था। अब मेरे लिए मात्र ठिकाना उसी स्टेशन का मुसाफिर-खाना रह गया था।
लेकिन मेरी नजर में उस सतमंजिला स्टोर से जहाँ सिर्फ कंडम सामान और द्वेषी
स्मृतियों के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा था, वह वेटिंग रूम ज्यादा राहत देने
वाला था। शुक्ल जी अपनी बात स्पष्ट करने के लिए हथेली में उँगली गड़ाते हुए बोले,
भाई साहेब, जनतंत्र, में अखबार की शक्ति आप नहीं जानते! आपने 'चाँद' का 'फाँसी
अंक' शायद नहीं देखा! ओ एक ही अंक ऐसा रहा कि अंगरेज बहादुर का छक्का छूट
गया!' शुक्ल जी लगभग बीस वर्ष कलकता में रहे थे। वैसे बनारस के रहनेवाले हैं।
पत्नी बंगाली है। घर में हिंदी-बंगला दोनों बोली जाती हैं। इसलिए वार्तालाप
करते समय बंगला के शब्द और क्रियाएँ स्वत: ही आ जाती हैं। मैंने शुक्ल जी की
बात बहुत धैर्य से सुनी और झिझकते हुए बोला, 'पर शुक्ल जी, इस छोटे-से नगर में
अखबार क्या चल पाएगा और इसके अलावा अखबार के लिए पैसा चहिए, प्रेस और दूसरे
साधन भी।' हवा में अपना पंजा नचाते हुए शुक्ल जी ने अपना भाषण शुरू कर दिया, 'भाई
साहेब, आप सिर्फ संका करना जानता। हम आपसे बोला था कारज को हाथ लगाइए। सहारा
देनेवालों का दल आपसे-आप आ जुटेगा। थोड़ी प्रोशंसा से सब काम सध जाता है। मानुष
छोड़ भगवान खुश हो जाता। हम आपसे पूछता हूँ 'गीता सहस्त्रनाम', 'दुर्गा
सप्तशाती', 'शिवमहिमा स्तोत्र' एऽ सब क्या है? आखिर
तुम्हारा इतना महान पोएट तुलसीदास 'विनाय पोत्रिका' में क्या लिखा है? आप एक
मानुष का नाम बोलें जो तारीफ से खुश नहीं होता!' शुक्ल जी ने मेरी आँखों में
झाँक-कर देखा और लंबे-चौड़े नथुने फुला कर 'सु-ऊं' की आवाज निकालने लगे। मेरी
ओर से कोई विरोध न देख कर आगे बोलने लगे, 'हम पूछता है, आपको प्रोशंसा से क्या
एतराज है? मेरे बाई बेजा न करेगा, किसी की उचित प्रोशंसा तो करेगा! हम योजना
दूँगा। काम आप करेगा। तोम चमक न उठा तो यम.पी. शुक्ला का नाम न लेना! ए
दारिद्र लादे घुमता है! माना लक्ष्मी-सोरस्वती का परंपरागत दुश्मनी ठहरा
परंतु रास्ता पकड़नेवाला आदमी दोनों को साध लेता है।' शुक्ल जी धाराप्रवाह बोले चले जा रहे थे। मेरी नजर कभी उनके मुँह पर चली
जाती थी और कभी मैं उनके सुंदर कालीन में धँसी अपनी गर्द-भरी चप्पलें देखने
लगता था। अपने फटीचर होने का अहसास मुझे बहुत गहराई से हो रहा था। 'मेरा काम ही
ऐसा है' यह सोच कर जिन मैले-मलगजे कपड़ों को मैं लापरवाही से लटकाए घूमता हूँ,
इस वक्त उनसे मुझे बेचैनी हो रही थी। मेरी पतलून पर पीछे की ओर कई थेगलियाँ
थीं, जो बंद गले के लबादे जैसे कोट के पीछे छिपने की नाकाम कोशिश कर रही
थीं।... और पतलून? वह घुटनों पर लोटे के पेंदे की शक्ल में उभर रही थी। टखनों
से ऊपर की ओर खिंचती मोहरियों पर दृष्टि गई तो देखा उधड़ कर झालरों की मानिंद
झूल रही थी! शुक्ल जी निरंतर एक से एक अच्छी बात कह रहे थे और मैं हुँकारी भर कर
बीच-बीच में उनकी बहुमूल्य बातों का अनुमोदन करना चाहता था, पर मुझे कुछ
अच्छे शब्द याद नहीं आ रहे थे। मैं केवल 'हाँ तो', 'जी हाँ', 'आप ठीक फरमाते
हैं' आदि कुछ टुचियल और अहमकपने से भरे हुए फिकरे बोल सकता था। अच्छी बातों को
समर्थन करने के लिए जिस शिष्ट भाषा की जरूरत थी वह मेरे पास सिरे से ही नहीं
थी। उत्साहित करने वाला प्रवचन सुनने के बावजूद मेरी दृष्टि रह-रह कर दीवार पर
लगे क्लाक से टकरा रही थी और सेकंड की अनवरत घूमती हुई सुई मेरे दिल में हौल
पैदा कर रही थी। ग्यारह बज रहे थे। मैं पत्नी से ग्यारह बजे तक लौटने की
बात कह कर आया था। इस समय मैं तय नहीं कर पा रहा था कि अपनी बात कैसे शुरू
करूँ। सहसा मेरे सोचने में व्याघात उपस्थित हुआ। शुक्ल जी ने अपने नौकर को जोर
से पुकार कर कहा, 'कोथाय मातादीन! ऐ मातादीन! ऐ सब क्या गोलमाल किया भाय! आज
हमको एक प्याली चा भी नहीं देगा रे!' मातादीन के उत्तर न देने पर उन्होंने
अपने गाउन की जेबें थपथपाई और सिगरेट-केस निकाल कर मेरे सामने रख दिया, 'तब तक
सिगरेट ही पीया जाए!' मैंने अपनी जेब से माचिस निकाल ली। मेरी जेब में केवल माचिस थी। मुझे
'नाइट-शिफ्ट' से लौटते हुए कभी-कभी आधी रात गुजर जाती है। घर बस्ती से दूर
जंगल में है। घोर अंधकार में माचिस की तीली जला कर उजाला कर लेता हूँ। एक दिन
तो घुप्प अँधेरे में एक कुएँ में गिरते-गिरते बचा था। बस, तभी से हर वक्त जेब
में दियासलाई रखता हूँ और यहाँ शुक्ल जी के घर में दिन के समय भी मरकरी राड जल
रहा है। मैंने शुक्ल जी की दी हुई सिगरेट जला ली और दूधिया उजाले में टेलीफोन
के चमकते चोंगे और हॉल की दीगर चीजों को देखने लगा। सारा हॉल बहुत करीने से सजा
था। पालिश से चमकती हुई खूबसूरत कुरसियों पर डनलप की गद्दियाँ पड़ी थीं और
अलमारियों में सीप और काँच से सुंदर खिलौने सजे हुए थे। शुक्ल जी ने गाउन की जेबों में हाथ डाल कर कमर को एक हलका-सा झटका दिया और
उबासी रोकते हूए बोले, 'हम आपसे सच बोलता है। जिन लोगों की चाकरी में बाहर से
कोई आमदनी का सिलसिला नहीं है, महीना में खाली पगार हाथ पर आता है, उनका काम आज
एकदम नहीं चलने का। आप महंगाई देखता? सिर के ऊपर से गुजर रहा है! हम आपके बारे
में सोचता है तो दिल पर तकलीफ गुजरता। आप जैसा चौरित्रवान भालामानुस क्यों
कष्ट सहता ए? हम एक बार आपका मनीजर बजाज साहेब से बोला। ओ बोला, बेशी स्कोप
इधर नहीं।... खैर, प्लान आप फैलाइए, लाइन हम दूँगा। कैसे क्या होगा नहीं
जानता, ऐ सब आपका सिरदर्दी। कोई राजनैतिक मासिक वा पाक्षिक छापो -
रैजिस्ट्रेशन हम करा दूँगा। एक गारंटी हमारा, विज्यापैन का कमी नहीं। इतना ठो
कोलकत्ता का धनाढ्य पार्लामेंट बैठा ए तोमकू सहायता करेगा। एक अखबार का निमित्त
से तोम देखेगा कि प्रेस और निवास हो जाने का।' बोलते-बोलते शुक्ल जी उठ कर खड़े हो गए। मैं नहीं समझ पाया कि आवेश के इन
घनीभूत क्षणों में वे क्या करनेवाले हैं! आगे बढ़ कर उन्होंने फोन का रिसीवर
उठाया और कोई नंबर डायल करने लगे। मैं भी उठा और उत्सुकता से उनके पास पड़ी एक
खाली कुरसी पर जा कर बैठ गया। शुक्ल जी ने डायरेक्टरी मेरे हाथ में दे कर
जल्दी-जल्दी कुछ नाम बतलाए और नंबर खोजने का आदेश दिया। रिसीवर कान से चिपकाए
बोले, 'एक बहुत बड़े आदमी को रिंग किया हूँ। अब आप सुकुल का कमाल देखेगा!' इस पत्र-प्रकाशन की योजना में शुक्ल जी मुझे लगभग उसी प्रकार धकेल रहे थे
जैसे लोककथा में राजा की अरथी के सामने आ जाने वाले घसियारे को मंत्रियों ने
राजा के खाली सिंहासन पर धकियाकर बिठा दिया था। मेरे मन की बेचैनी मेरे हाथों
में आ गई थी। हाथ लगातार जेबों में आ-जा रहे थे और बार-बार हाथ डालने से जेबों
का मुँह लटके हुए जबड़े जैसा फैल गया था। शुक्ल जी बराबर डायल घुमा रहे थे और
बीच-बीच में सिर भी झटकते जाते थे। टेलीफोन डायल करने की तमाम टेक्नीकों के
बावजूद किसी 'बहुत बड़े आदमी' से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था। मैंने
अत्यंत व्यस्तता दिखाते हुए डायरेक्टरी के पन्ने उल्टे-पलटे और शुक्ल जी
द्वारा बताए गए नामों के नंबर उन्हें बता दिए। लगभग बीस मिनट बाद इस संपर्क-स्थापना की लंबी यंत्रणा का अंत हुआ। मेरा
महादुर्भाग्य! एक भी व्यक्ति से बातचीत न हो सकी! हार कर शुक्ल जी ने रिसीवर
रख दिया और मेरी ओर ऐसे घूरने लगे जैसे मदारी तमाशा खत्म करके मजमे की तरफ
घूरता है। इस बीच मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी बात बहुत स्पष्ट शब्दों में उनके
सामने रख दूँ। अब मैं अधिक देर नहीं रुक सकता था। साढ़े ग्यारह बज रहे थे और
एक बजे गाड़ी जाती थी। मुझे अभी घर पहुँचना था और कई तरह के झंझट मेरी जान को
लग रहे थे। घर पर पत्नी अलग परेशान हो रही होगी! मैं किस झंझट में फँस गया!
मुझे अपनी बात फौरन कहनी चाहिए थी। नंगी स्थितियों में जीवित रहने वाले आदमी को
शिष्टता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आभिजात्य उस तंग जूते की तरह होता
है जो नया, चमकीला ओर कीमती दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर ही भीतर पाँव का भुरकुस
निकाल देता है!... यहाँ इंतजाम न होता तो किसी और से कहता। मेरी हालत यहाँ आ कर
उस व्यक्ति जैसी हुई जो आपके पास कोई खास काम ले कर आए और देर तक संकोच में
पड़ा रहे। मैंने बेसब्री से अपनी बात शुरू की, 'ऐसा है...' लेकिन तभी मातादीन चाय ले
कर आ गया। मेरी बात शुक्ल जी तक नहीं पहुँच पाई। शुक्ल जी ने मेरी ओर आँखें
उठाई। गिलास की तली जैसे मोटे लेस के पीछे से झाँकती आँखें बहुत बड़ी और असह्य
दिखाई पड़ती थीं। कुछ देर तक गंभीर रह कर वे सोचते रहे और फिर सजग होते हुए
बोले, 'आइए, चाय पिया जाए! हम लंच टाइम पर आपके कारज हेतु सबको खड़-खड़ाऊँगा।
आप रहिए, हम इस कारज को पूरा करके ही रहूँगा!' मातादीन ने दो प्याले तैयार
करके हम दोनों के हाथ में थमा दिए और झाड़न उठा कर डाइनिंग टेबल साफ करने लगा। मैंने जल्दी-जल्दी चाय गटकी और खाली प्याला मेज पर रख कर हथेली से अपना
मुँह पोंछने लगा। चाय पीते-पीते शुक्ल जी बोले 'आलमीरा से जरा ओ ऽ
अलबम उठाना जीऽ... आपको तसवीरें दिखाई जाएँ!' अब मैं एक मिनट
भी गँवाने को तैयार न था। जेबों में हाथ डाल कर व्यग्रतापूर्वक उनकी सींवन
उधेड़ने लगा। मेरे पैर बार-बार उठना चाहते थे। मुद्रा बिलकुल उठ भागने की ही
थी, लेकिन शुक्ल जी ने मेरा अधैर्य नहीं देखा। उन्होंने इतमीनान से अलबम खोला
और मुझे एक तस्वीर दिखाने लगे। इस तस्वीर में वे कुछ लोगों से घिरे खड़े थे
और एक विदेशी महिला उनसे मुस्करा कर बातें कर रही थी। शुक्ल जी ने गदगद भाव
से हँस कर मेरी ओर देखा और पहेली बुझाने के अंदाज से बोले, 'पहचाना?' मेरे
नकारात्मक ढंग से सिर हिलाने पर बोले, 'अंबैसी की प्रथम सचिव हैं!' मैं इस समय शुक्ल जी की बात काटने या उनसे विवाद करने के विषय में सोच भी
नहीं सकता था। जिस समय उन्होंने एक बड़े नेता से हाथ मिलाने के अवसर का अपना एक
फोटो मुझे दिखाया, मैंने फोटो के विषय में कतई आश्चर्य व्यक्त किया और
तड़ाक से बोला, 'शुक्ल जी क्षमा कीजिए, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी गंभीर बात
कहनी है। मेरी पत्नी के पिता लखनऊ में बहुत बीमार हैं... वे शायद ही बचें!'
इतना सुनते ही शुक्ल जी गहरा दुख व्यक्त करते बोले, 'ओफ! कब से? यह तो दुख
का खबर रहा!' उन्होंने महसूस किया कि मुझे उनसे शायद और भी कुछ कहना है। बोले,
'आच्छा! बोलो हम क्या सेवा कर सकता हूँ?' मैंने अकारण खों-खों की, 'मुझे इस क्षण एक हजार रुपए की सख्त जरूरत है।
मुझे तत्काल जाना है। पत्नी जाएगी तो बच्चे भी जाएँगे।' मैं बहूत फूहड़ ढंग
से अपनी आवश्यकता और आकस्मिक दुख उनके सामने रख रहा था। मेरे शब्दों में वह
तीव्रता न थी जो किसीको अहसास करा सके कि मेरी जरूरत वास्तविक और अपरिहार्य
है। जेबों में हाथ डाल कर मैंने शुक्ल जी को दिखाने के लिए वह तार निकालना
चाहा जो मुझे आज नौ बजे मिला था। तार तो मेरे हाथ में नहीं आया, हाँ, वह बिल
जेब से अवश्य बाहर आ गया जो मैंने एक सरकारी सेमिनार में सम्मिलित होने पर
सरकार को भेजा था। वह बिल बिना अकाउंट्स अफसर के पास किए लौट आया था और इसे फिर
वापस भेजना था। झगड़े-झंझट के बाद चार या छह महीने तक शायद इसका रुपया
मिलनेवाला था, लेकिन वह अवधि अभी दूर थी। शुक्ल जी मेरी बात सुन कर गंभीर हो गए। मैंने पंद्रह सौ दस रुपए, सत्तानवे
पैसे का बिल उनके सामने फैला दिया। शायद मैं उनको प्रभावित करना चाहता था कि
मुझे जल्दी ही एक रकम मिलने वाली है और जो भी वह मुझे देंगे उसका भुगतान करने
में मुझे कठिनाई नहीं होगी। आपका कोई कितना ही अपना हो, अपने रुपए को डावाँडोल
स्थिति में नहीं फँसाना चाहता। किंतु शुक्ल जी ने बिल की ओर आँख उठा कर भी
नहीं देखा। बोले, 'आपका जरूरत हम मान गया मगर आज का दिन... अच्छा खैर, देखता
हूँ।' शुक्ल जी उठ कर खड़े हो गए। मैं भी उनके साथ उठ गया। शुक्ल जी अंदर चले
गए और मैं बेताबी से गैलरी में पीठ पर हाथ बाँधे चक्कर काटने लगा। ज्योंही शुक्ल जी लौट कर आए मैं धुकधुकाते हृदय से उनकी ओर लपका।
उन्होंने एक भी शब्द बोले बिना मेरे हाथ पर पाँच-पाँच के बीस नोट रख दिए। मैं
सहसा कुछ न समझ पाया। एक हजार की बात कही थी, और केवल सौ रुपए दे रहे थे!
शुक्ल जी संभवत: मेरे मन की बात भाँप गए। वे बहुत निरीह स्वर में बोले, 'बंधु
आपके कष्ट का अपन को बहुत विचार है, नहीं तो अपने पास कौड़ी भी नहीं।' इतना कह
कर फ्रिज की ओर संकेत किया और उदासी के स्वर में बोले, 'इसे चार मास पहले
लिया। सारी किस्त देना है। पंद्रह तारीख की पहला किस्त देने को बोला। जितनी
जल्दी हो, रुपया लौटाने की परम चेष्टा कीजिएगा।' संकोच और झिझक के कारण जिस बात को मैं अपने फटीचर होने के बावजूद नहीं कह
पाया था, वह शुक्ल जी ने बेलौस कह दी, 'आप शायद नहीं जानते, हम कितना गरीब
हुँ! गाड़ी रखनी पड़ती है। सब टीम-टाम जुटानी होती है, इंश्योरेंस का हैवी
प्रीमियम क्लब का मेंबरशिप। सामान की किस्त और इनकटैक्स - देह में रत्ती-भर
खून नहीं छोड़ता! ऊँचा तबका मजदूर से बेसी तंग है। आपको मालूम है, हमको कुल जमा
कितना तनखा मिलता? कट-वट कर केवल पचास हजार माहीना! आप मानेगा नहीं, वर्मा
साहेब, हम सच कहता हूँ। माहीना का आखिर कड़की में होता है। महँगाई ने...' हैरत से मैंने शुक्ल जी का गंभीर चेहरा देखा। मुझे लगा कि वे अपना माथा पकड़
कर विलाप कर रहे हैं। मैं उनकी गरीबी का पूरा आख्यान सुनने में दिलचस्पी रखता
था, लेकिन तभी दीवार पर लगे क्लाक ने बारह बजने की सूचना दे दी। मैंने बदहवासी
में उनसे हाथ मिलाया और भाग खड़ा हुआ। वही पुराना ढोंढ़ का मकान था। सरकंडों वाले मोढ़े सहन में जर्जर जटायु के
पंखों की मानिंद बिखरे पड़े थे, टीन की कुर्सियों के पेंदे भी गल चुके थे। एक
नजर उसने पूरे ढूह पर डाली और आगे बढ़ गया। उस विराट फालतूपन से वह भीतर ही भीतर उखड़ गया। सामने के ओसारे से पिताजी
टायर के सोलवाली चप्पलें घसीटते आ रहे थे। उसने आगे बढ़ कर उनके पैर छू लिए।
उन्होंने जल्दी से नीचे झुक कर उसे बाँहों में ले लिया। पिता का चेहरा उसने
देखा, जिस पर कई रोज की बढ़ी दाढ़ी के बावजूद सघन झुर्रियाँ दिखाई पड़ रही थीं।
ऐनक ढीली पड़ गई थी और एक तरफ की कमानी धोखा दे गई थी, जिसमें उन्होंने जनेऊ
के सूत की डोरी बाँध ली थी। धोती भी खासी मैली लग रही थी। रुई का सलूका भी कम
से कम आठ-दस साल पुराना होगा ही। वह जोर लगा कर बलगमी आवाज में बोले, 'धीरेंद्र की माँ, देखो कौन आया है?' उसके पीछे उसकी पत्नी और बच्चे नि:शब्द आ कर खड़े हो गए थे। पत्नी ने
सिर का आँचल जरा आगे की तरफ खींच लिया था। पिता ने उसकी छोटी बच्ची को, जो माँ
की गोद में ऊँघ रही थी, आगे बढ़ कर अपनी गोद में खींच लिया। दोनों बड़े बच्चे अब
भी सहमे-से एक ओर खड़े थे। एक के हाथ में प्लास्टिक की कंडिया थी और दूसरा
हाथ में अटैची उठाए इधर-उधर की टोह ले रहा था। इसी समय रिक्शा-चालक एक हाथ में सूटकेस और दूसरे में बिस्तर लटकाए सहन में
घुसा। उसकी पत्नी और बच्चे कमरे की दिशा में बढ़ गए और वह पीछे मुड़ कर
रिक्शावाले को किराया चुकाने लगा। रिक्शावाले को विदा करके वह भी कमरे की
देहरी पर जा कर खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ की कराहट सुनी - शायद वह चारपाई पर
बैठने की कोशिश में कराह रही थी। भीतर जा कर उसने देखा, कमरे की अवस्था भी अच्छी नहीं थी। दोनों तरफ की
खिड़कियाँ बंद थीं। माँ अँधेरे में ढीली-सी चारपाई पर लेटी हुई थी और छोटी बहन
रेखा माँ की सूखी पिंडलियों पर तेल की मालिश कर रही थी। इस कमरे में भी घर का
टूटा-फूटा और अंगड़-खंगड़ वह सामान पड़ा था, जिसे अब तक घूरे पर पहुँच जाना
चाहिए था। कुल मिला कर पूरे माहौल में एक अजीब-सी उदासी और विपन्नता फैली हुई थी। घर
में माँ-बाप और जवान बहन की उपस्थिति के बावजूद सब तरफ मौत का सन्नाटा छाया
हुआ था। सहसा उसे याद आया कि इस घर में कई पीढ़ियों से अच्छी-खासी भीड़-भाड़ चली आ
रही थी, लेकिन अब पुराने दरों-दीवारों के साथ घर के आदमी भी जंग खा रहे थे। उसने रजाई का किनारा हल्के से सरका कर माँ के पाँव छुए और उनके पास ही बहुत
आहिस्ता से अदवाइन पर बैठ गया। माँ के चेहरे पर आते-जाते भावों का उसे कोई
अनुमान नहीं हो पा रहा था। माँ का चेहरा उस टूटे-फूटे दर्पण जैसा था, जिसका
पानी कई स्थानों से गायब हो गया हो और उसमें कोई आकृति, चाहे वह कैसी भी हो,
सिवाय विद्रूप के कुछ और नजर न आए। माँ ने अपने पाँव सिकोड़ कर उठने की कोशिश की। शायद वह उठ कर उसके सिर पर
हाथ फेरना चाहती थीं लेकिन उसने उनके पाँव दबा कर उन्हें उठने से रोक दिया और
उनकी वह आवाज सुनी, जिसे अपने कानों और चेतना में वह आसानी से नहीं झेल सकता
था। वह अपने कंठ की चीख बरबस दबा कर रो रही थीं। वह चीत्कार उस बीमार बच्चे
का रुदन जैसा था, जिसकी रो सकने की शक्ति भी जवाब दे गई हो। उसने दाएँ-बाएँ देखा, शायद पिता माँ के आर्तनाद को ले कर कुछ कहें, लेकिन
उसने पाया कि वह आसपास कहीं भी नहीं हैं। उसकी बहन ने संभवत: उसकी आँखों की खोज
को पढ़ लिया। वह तेल की कटोरी जंगले में टिका कर उठते हुए बोली, 'बप्पा दूध
लेने गए हैं। मैं चाय बना कर लाती हूँ।' वह फुर्ती से उठी और रसोई के दरवाजे पर
पहुँच कर बोली, 'माई आपको कई दिन से पूछ रही थीं।' उसे बहन के शब्दों से ऐसा आभास मिला, मानो वह माँ की दिशा में झपटती किसी
अव्यक्त गति की ओर संकेत कर रही हो। वह एकाएक सिहर उठा और उनके सिरहाने पहुँच
कर उनके सिर पर हाथ फेरने लगा। माँ के सिर पर मुट्ठी-भर बाल भी मुश्किल से रह
गए होंगे। यही माँ कभी अच्छी-खासी लंबी-तड़ंगी थी, जब वह चोटी करती थी, तब
इतने बाल तो टूट कर कंघी में ही अटके रह जाते थे। वह माँ के सिर पर हाथ फेरता रहा और उनकी आँखों से ढर-ढर पानी बहता रहा। उसके
पास सांत्वना देने के लिए जो शब्द थे, उन्हें एक साथ इतने रास्तों से ग्रहण
लग गया कि वह केवल एक दीर्घ आह खींच कर रह गया। रो कर जब माँ का मन कुछ हल्का
हो गया तब उन्होंने कष्ट से करवट बदली और धोती के पल्ले से नाक पोंछ ली।
उन्हें खाँसी का दौरा-सा पड़ गया। वह बेचैन हो कर उठने लगीं तो वह उनका आशय
समझ गया। उन्हें कंधों से सहारा दे कर उसने पाटी के नजदीक किया और चारपाई के
नीचे से मिट्टी का कसोरा उठा कर उनके मुँह से सटा दिया। वह सोचने लगा, अपनी पारिवारिक व्यस्तताओं में मैं इतना गर्क रहता हूँ कि
मुझे अपने इस टूटते-ढहते घर का कभी ख्याल नहीं आता। बहन शादी के लिए तैयार
बैठी है, माँ अपाहिज हो चली है, पिता मिडिल स्कूल की हेडमास्टरी से रिटायर हो
चले हैं, जिन्हें अब सिर्फ अट्ठाइस रुपए माहवार की पेंशन मिलती है। माना कि
दादाओं का बनवाया हुआ, बराएनाम यह घर उनके पास है, लेकिन अब तो यह भी सदियों
पुराना लगने लगा है। मरम्मत की बेहद जरूरत है। इसमें सब तरफ मनहूसियत
व्याप्त हो चली है। हालत यही रही तो दो-चार बरस में दीवारें और छतें अपनी जगह
टिकी नहीं रहेंगी। दोपहर को रेखा ने जो खाना उसे परसा, वह देखने में सद्गृहस्थ का ठीक-ठाक
सामान्य भोजन था, लेकिन घर की नाव को जिन डाँवाडोल परिस्थतियों में डगमगाते
देख रहा था, वह उसे परसे हुए भोजन के प्रति स्वस्ति प्रदान नहीं कर पा रही थी।
वह पिता को कुछ ऐसा नहीं दे पाता था जिसे गनीमत कहा जा सके। फिर यह भी कि
नियमित तो वह कभी कुछ दे ही नहीं पाता था। आज के जमाने में सत्तर-पचास का मतलब
क्या होता है और वह भी महने-दो-दो महीने के अंतराल पर! उसे भोजन की थाली के
सामने बैठ कर अपने उस घमंड को ले कर गैरत महसूस हुई जो वह पिता को मनीआर्डर
भेजने के बाद किया करता था। यह कितनी हया की बात है कि उसके द्वारा भेजी गई
राशि से पूरे महीने की एक जिन्स भी पूरी मिकदार में नहीं खरीदी जा सकती। वह खाने से निवृत्त हो कर उस लंबे-से कोठे में जा कर लेट गया, जहाँ वह
विद्यार्थी-जीवन में रहा करता था। दीर्घकाल तक उन दीवारों और छत का साक्षी रहने
के कारण वह तब और अब के अंतर को एक क्षण में जान गया। फर्श में जगह-जगह से चूना
उखड़ गया था और छत चिटक कर दरार-दरार हो गई थी। छत के बीचों-बीच लोहे के कुंडे
में जो रस्सी गाँठ-दर-गाँठ बँधी थी, वह उसके उस बचपन की साक्षी थी। जब वह झूले
के लिए मचल उठता था। रस्सी झुरझुरी हो चली थी, लेकिन किसी ने उसे यहाँ से
निकाला नहीं था, गोया अव्यक्त ढंग से उस कोठे में ऐसा कुछ छोड़ दिया गया था जो
उसकी देह-गंध से खाली नहीं था। उसका ध्यान बच्चों के शोर-शराबे से टूट गया। उसने महसूस किया कि उसके
तीनों बच्चे घर में उन्मुक्त हो कर खेल-कूद रहे हैं और सारे सहन में किलकारी
मारते घूम रहे हैं। उसका अपना फ्लैट अच्छा और आकर्षक है। शहर में आज दिन इतना
बड़ा फ्लैट कोई हँसी-खेल नहीं है। मगर इस लंबे-चौड़े मकान के मुकाबिले वह क्या
है? कहने को उसके पास पूरे दो कमरे हैं, मगर उनमें चार चारपाइयों की समाई भी
नहीं है। अगर बाहर से दो मेहमान आएँ तो एक मुसीबत-सी खड़ी हो जाती है। उसे हजार
रुपए से ऊपर तनखाह मिलती है, पर महीने की पंद्रह तारीख से ही काटा किल-किल शुरू
हो जाती है। वह लोगों के सामने इस तरह रोता है, जैसे वह लंबे वक्त से बेरोजगार
हो। वह जानता है, लोग आधे माह के बाद रुपए को इस हसरत से याद करते हैं, गोया
कोई बहुत नजदीकी उम्र से पहले ही गुजर गया हो। और इस घर में आने वाली मात्र
अट्ठाइस रुपए की पेंशन! इसे तीस-इकतीस दिनों में बाँटने वाला गणितज्ञ अभी शायद
पैदा ही नहीं हुआ। इस घर में तीन प्राणी हैं और उनकी सीमाएँ ही सीमाएँ हैं;
सामर्थ्य नाम की कोई चीज उनके पास नहीं है। कोई अर्थशास्त्री भी अट्ठाइस रुपए
और तीन आदमी की पहेली नहीं सुलझा सकता। खाने से निवृत्त हो कर पिता अपना हुक्का ले कर उसके पास आ बैठे और गंभीर
चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करके बोले, 'सो जा लल्ला!' उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, चारपाई पर उठ कर बैठ गया। वह भी कुछ नहीं
बोले, बस चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। कुछ देर बाद उसे लगने लगा कि वह उससे
भीतर ही भीतर वार्तालाप कर रहे हैं। उनकी चुप्पी अनायास नहीं लगती थी। उसने
बातचीत के लिए कोई मुद्दा सोचने का प्रयास किया, पर उसे हर विषय बहुत नाजुक
लगा। पिता के लिए घर-परिवार की चिंताओं के अतिरिक्त अन्य कोई विषय
महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी चेतना में रेखा की शादी को ले कर गहरा द्वंद्व है।
एकमुश्त रुपया एकत्र कर पाने की स्थितियों में वह कभी नहीं रहे और आज रुपया ही
एकमात्र उपायकरण है। उसने कनखियों से उनकी ओर देखा - माथे पर सलवटें ही सलवटें
थीं और चेहरा सघन झुर्रियों से रेखागणित बन कर रह गया था। तीन दिन निकल गए। उसे दिनों के बीतने का कोई खास अहसास नहीं हुआ। वह इस
दौरान घंटों माँ के पास बैठता रहा। पिता भी उसके पास आ कर बैठ जाते थे और शहर
के फैलते चले जाने पर चिंता प्रकट करने लगते थे। महँगाई बढ़ने का कारण उनकी नजर
में शहरों की बढ़ती आबादी थी वह कई बार कहते थे, 'गाँव शहर हो गए अब तो! पता
नहीं इतनी खलकत कहाँ से अर्रा पड़ी! यही हाल रहा तो पता नहीं दुनिया कहाँ
समाएगी!' इन तीन दिनों में वह बहुत कम वक्त के लिए ही बाहर निकला। साथ पढ़नेवाले और
बचपन के संगी-साथी उसी की तरह शहर को छोड़ कर इधर-उधर जा चुके थे। जो सामान्य
ढंग से परिचित थे, उनसे कोई अंतरंग वार्तालाप संभव नहीं था, महज औपचारिक-सी
बातें हो कर रह जाती थीं। मसलन किस नौकरी में हो? क्या पड़ जाता है वगैरह!
उसकी तनख्वाह को ले कर कोई-कोई अचरज भी प्रकट करता। कस्बे में इतनी तनख्वाह
मिलती भी किसे थी? इन तीन दिनों में बच्चे गलियों में रम गए। रेखा उसकी पत्नी
को ले कर कई घरों में घूम आई। औरतों की भी आवाजाही लगी रही और उसे पहली बार इस
घर में रहते यह अहसास हुआ कि वह मशीनी दिनचर्या से मुक्त है। जब चौथे दिन वह घर से जाने लगा तब माँ ने उसके तीनों बच्चों को अपने पास
बुलाया। उन सबके सिर सूँघ कर प्यार किया और अपने गूदड़ तकिए के नीचे से एक
चिथड़ा निकाला। वह काँपते हाथों से देर तक गाँठें खोलती रहीं। उसने देखा कि माँ
ने मुड़े-तुड़े मगर साफ नोट बच्चों को दिए। वह सोच भी नहीं सकता कि इन बीहड़
परिस्थितियों में कोई किसी को कुछ दे सकता है। वह तीन दिन से लगातार सोचता चला
आ रहा था कि लौटने का किराया बचा कर वह घर से जाते वक्त सारे रुपए माँ को दे
देगा लेकिन अब माँ द्वारा बच्चों को रुपए दिए जाने के बाद उसे यह काम मुश्किल
लगने लगा। उसने तय किया कि घर से बाहर निकल कर वह रुपया किसी को दे देगा - पिता
तो बाहर द्वार पर होंगे ही। जिस समय उसका सामान रिक्शे पर लद रहा था उसने देखा, बच्चों के साथ पिता और
रेखा भी बाहर आ गए हैं। रेखा उसकी छोटी बच्ची को गोद में उठाए हुए थी। उसने
रेखा के नजदीक जा कर बहुत नामालूम ढंग से रुपए उसे पकड़ाते हुए फुसफुसाहट में
कहा, 'माँ की किसी अच्छे डॉक्टर से दवा कराना। मैं पहुँच कर रुपए तुरंत
भेजूँगा।' रेखा ने रुपयों की ओर देखा तक नहीं। उन्हें मुट्ठी में दाबे बोली,
'रास्ते में जरूरत पड़ेगी। कमी न पड़ जाए। फिर भेज देते।' उसने रेखा की बात का
उत्तर नहीं दिया, व्यस्तता से अपनी पत्नी मालती को पुकारने लगा। उसकी पत्नी सास के पैर छू कर लौटी तो उसे लगा उसके चेहरे पर उदासी है। उसने
पिता के पाँव छुए और रिक्शे की तरफ बढ़ लिया। रेखा ने बच्ची को मालती की गोद
में दे दिया और बच्चे पीछे हुड पर चिपक कर बैठ गए। रिक्शा जब गली पार कर गया
तब मालती भरे कंठ से बोली, 'अम्मा की हालत अच्छी नहीं है। आप साथ ले चलते और
वहीं इलाज कराते तो शायद ठीक हो जातीं।' 'सोचता तो कई बार मैं भी यही हूँ, पर वहाँ इनके लिए भागदौड़ बहुत करनी
पड़ेगी। यह अकेले आदमी का काम नहीं है। फिर एक बात यह भी है कि वह हमारे साथ
चलने को राजी नहीं होंगी।' 'सब हो जाएँगी राजी, आप कहते तो... हमारा फर्ज तो है उनके लिए।' उसने मालती से सहमति जतलाई, 'चलो, कोई बात नहीं। वहाँ जा कर पिता जी को लिख
दूँगा। कुछ दिनों के लिए सभी लोगों को अपने पास बुला लेंगे।' 'ऐसा ही करना,' कह कर मालती चिंतामुक्त हो गई, किंतु वह गंभीरता से सोचने
लगा कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि सारे लोगों को अपने पास बुला ले और
मरणासन्न माँ का भरोसे का इलाज करा ले जाए? सोचते-सोचते रिक्शा स्टेशन पर जा पहुँचा, किंतु वह तय नहीं कर पाया कि उसे
माँ का ढंग से इलाज कहाँ और कब कराना चाहिए। स्टेशन की गहमागहमी ने उसकी सोच
को अवरूद्ध कर दिया। रिक्शा चालक ने सामान उतार कर स्टेशन की सीढ़ियों पर रख दिया। उसने जेब में
हाथ डाल कर पर्स निकाला तो उसने देखा, उसमें एक रुपए का कोई नोट नहीं है। उसने
रिक्शेवाले की ओर पाँच रुपए का नोट बढ़ा दिया। वह बोला, 'बाबू जी, मेरे पास
छुट्टा नहीं है। आप एक रुपए का नोट दे देओ।' पत्नी के पर्स में भी छुट्टे के
नाम पर महज एक अठन्नी ही निकली। वह अभी पाँच का नोट तुड़ाने की सोच ही रहा था कि उसका बड़ा बच्चा समीर बोला,
'मेरे पास दादी अम्मा का दिया हुआ जो रुपया है, उसे दे दूँ?' और यह कहने के
साथ ही उसने अपनी जेब से चार तह में मुड़ा हुआ नोट निकाल कर रिक्शेवाले की तरफ
बढ़ा दिया। बेटे की सहज अभिव्यक्ति 'दादी अम्मा का दिया हुआ रुपया' उसके कानों में
गूँजते हुए सर्वांग में एक लहर की माफिक दौड़ गई। एक विचित्र-सी सिहरन अनुभव
करते हुए उसने रिक्शेवाले के हाथ से नोट वापस ले लिया और पत्नी, बच्चों और
रिक्शा-चालक को वहीं छोड़ कर कहीं लपक गया। बच्चों के लिए बिस्कुट का पैकेट खरीद कर उसने पाँच रुपए का नोट तुड़वा
लिया और समीरवाले एक रुपए के नोट को पर्स की भीतरी जेब में डालते हुए वह
बच्चों की तरफ लौट आया। रिक्शा चालक को किराया चुकाने के बाद उसने धातु का एक
रुपया समीर की ओर बढ़ाया, 'लो दादी अम्मा के रुपए के बदले तुम यह चाँदी का
रुपया ले लो।' 'पर दादी का रुपया कहाँ गया पापा?' समीर ने जिज्ञासु भाव से पूछा। किंतु
उसने बेटे की बात को कोई उत्तर नहीं दिया। व्यस्तता से कुली को आवाज लगाने
लगा। गाड़ी प्लेटफार्म पर लग चुकी थी। उसने अफरा-तफरी में बच्चों और सामान को
ट्रेन के अंदर पहुँचाया और कुली को पैसे चुकाने के लिए जेब से पर्स खींच लिया।
समीर के दिए हुए नोट को सर्तकता से बचाते हुए उसने कुली को भाड़ा चुकाया और
हथेली से माथे का पसीना पोंछने लगा। सब तरफ से निश्चिंत होने के बाद उसे फिर उस
रुपए का ध्यान आया जो उसकी माँ ने उसके बेटे समीर को आशीर्वाद स्वरूप दिया
था। पता नहीं उसके मन-मस्तिष्क में क्या बवंडर-सा उठा कि उसने जेब से पर्स
निकाल कर पर्स से वह तुड़ा-मुड़ा नोट खींच लिया और पत्नी की ओर बढ़ाते हुए
धीरे से फुसफुसाया, 'इसे खर्चना मत, पूजा की थाली में रख देना है।' पत्नी उसका चेहरा हैरत से देखने लगी। उस बेचारी की समझ में कुछ नहीं आया।
वह उस चार तहों में मुड़े हुए नोट को मूढ़ भाव से देखती रही। वह पत्नी के
प्रश्नों से बचने की गरज से खिड़की के सामने से खिसक कर आगे बढ़ गया। इस समय
उसकी संपूर्ण चेतना उस कोठे में केंद्रित हो गई, जहाँ उसकी रूग्ण माँ
निरीह-निशब्द लेटी केवल मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपने भीतर
उमड़ती एक विवश रुलाई को बरबस दबा लिया और पत्नी-बच्चों की तरफ लौट गया। 'आपको गायत्री का कोई मंत्र याद है?' किसी महिला का स्वर सुन कर उसने तिरछे हो कर अपनी दाईं तरफ देखा। कई
स्त्री-पुरुष मुँह लटकाए सामने की ओर देख रहे थे। उसने सिर हिला कर श्लोक याद
न होने की विवशता जाहिर कर दी। मंत्र की बात करनेवाली औरत ने एक लंबी साँस खींची और होंठों में 'ओम् नमः
शिवाय' का पाठ आरंभ कर दिया। मरीज के दाएँ-बाएँ लोहे के दो स्टैंड खड़े थे। एक
पर खून की बोलत उलटी करके टँगी थी और काँच की नली से बूँद-बूँद करके रक्त एक
रबर की नली में गिर रहा था। दूसरी ओर से इसी प्रकार ग्लूकोज की बूँदें गिर रही
थीं। मरीज की आँखें टँग गई थीं और नाक में ऑक्सीजन की नली होने के बावजूद
कठिनाई से साँसें खिंच रही थी। मरीज एक बुढ़िया थी। जिसे चारों ओर से उसके दो बेटों, पाँच बेटियों ओर दो-तीन
दामादों ने घेर रखा था। बुढ़िया की बहुओं को भी इस भीड़ में शामिल कर लिया जाए,
तो गरीब एक दर्जन मर्द-औरत वहाँ मौजूद थे। सभी के चेहरों पर मौत का भय उभर रहा
था और लग रहा था कि दवाओं, इंजेक्शनों और खून-ग्लूकोज के बावजूद वृद्धा की
मृत्यु हो जाएगी। एक महिला, बुढ़िया के मुँह से कभी-कभी निकलनेवाले अस्फुट
शब्द सुन कर उसके चेहरे पर झुकती थी और उनका अर्थ जानने की चेष्टा करती थी,
पर शब्द पकड़ में नहीं आते थे। कई डॉक्टर बारी-बारी से आते थे और बहुत
तत्परता से बुढ़िया की नब्ज टटोलते थे। बीच-बीच में ब्लड प्रेशर भी जाँच लेते
थे। यंत्र के गिरते हुए पारे को देख कर उनकी भौंहों में बल पड़ जाते थे।
भाग-दौड़ करते डॉक्टरों-नर्सों को गंभीर देख कर बुढ़िया के संबंधियों के मुँह
से बेसाख्ता लंबी और हताश साँसें छूटने लगती थीं। इतने बड़े समूह के रूप में खड़े आदमियों के मुँह से कोई बात नहीं निकल रही
थी। हाँ, एक बेटी ने अत्यंत कायरता से एक बार स्वगत भाषण के तौर पर यह अवश्य
कहा, था, 'इससे तो यही अच्छा है कि इसकी साँस घर में ही निकले। इसे और क्यों
कटवाते हो! घर में होगी, तो बच्चे आखिरी बार शकल तो देख लेंगे।' मगर उसके
सुझाव पर किसी ने कोई खास तवज्जह नहीं दी। वे सब जड़ता और अवशता की उस स्थिति
को पहुँच गए थे जहाँ कोई भी परिवर्तन सुविधाजनक दिखाई नहीं देता। ज्यादा से
ज्यादा वे लोग यह करते थे कि चुपके से सबकी हाजिरी आखों-आँखों में ले लेते थे
और पहले से भी ज्यादा गंभीर हो जाते थे। गो कि वे लोग मृत्यु के विषय में कुछ न कुछ कहने को बेचैन थे, मगर उन्हें
अपने उद्गार प्रकट करने का क्षण अभी कुछ दूर दीख पड़ता था। जो महिला मरीज के
ऊपर झुक कर कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी, अब एक स्टूल पर टिक कर होंठों में
कुछ बुदबुदा रही थी। शायद वह मंत्र वगैरह के चक्कर में न पड़ कर सीधे-सादे ढंग
से ईश्वर का नाम ले रही थी। तभी वार्ड में एक साथ तीन डॉक्टर दाखिल हुए और उनके पीछे हाथ में सिरींज
पकड़े हुए एक छोटे कद की गुड़िया जैसी खूबसूरत नर्स भी आई। उसने आते ही वृद्धा
की नाक में नली डाल कर उसमें सिरींज अटका कर पानी खींचना शुरू कर दिया। नर्स
कुछ देर तक अपना कार्य बहुत तत्परता से करती रही। जब रक्त मिश्रित पानी से
चिलमची भर गई, तो जमादार को उठाने के लिए पुकारती वह वार्ड के बाहर चली गई। बुढ़िया दर्द से कराह उठी। उसके छटपटाने पर उसकी बेटियों ने अपनी प्रतिक्रिया
आहें भरकर व्यक्त की। अब डॉक्टरों ने मरीज की जाँच आरंभ की। एक डॉक्टर ने,
जो डॉक्टर से अधिक अभिनेता लगता था और जिसके सुनहरे रूखे बाल माथे पर छितराए
हुए थे, खून की बोतल पर ढके कपड़े को हटा कर देखा और बोतल को यथावत ढक दिया।
परीक्षण करके जब तीनों डॉक्टर मस्तक पर सलवटें डाल कर बाहर जाने लगे, तो
उन्होंने बुढ़िया के बड़े बेटे छविनाथ को अपने साथ आने का संकेत किया। बड़े लड़के
के साथ बुढ़िया का छोटा बेटा हरिनाथ और दामाद इस आशा में बाहर की ओर लपके कि
शायद डॉक्टर मरीज के संबंध में कोई विशेष बात बतलाने जा रहे हैं। दो डॉक्टर वार्ड के बाहर जा कर ड्यूटी-रूम में घुस गए और एक दुबला-सा
डॉक्टर, जिसकी चुँधी आँखें चश्मे के मोटे लैंस से आवृत्त, बड़ी भयंकर दिखलाई
पड़ती थीं, अपने अधगंजे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, '...देखिए! ऐसा है कि एक
बोतल खून का आप लोग फौरन इंतजाम कीजिए। जो खून बोतल में बाकी है ज्यादा से
ज्यादा दो घंटे में पास हो जाएगा।' सब लोग साँस रोक कर डॉक्टर की बात सुनते रहे। डॉक्टर ने गले में पड़े हुए
स्टैथकोप को निकाल कर हाथ में ले लिया और अपने सफेद लंबे कोट को हिलाता हुआ
आगे बढ़ गया। सब लोगों को हतवाक्य देख कर वह एक पल रुका और आश्वासन-सा देते
हुए बोला, 'मैं लिख देता हूँ, आप फौरन 'ब्लड बैंक' जाइए और एक बोतल खून ले
आइए। इस टाइम 'वेन' पकड़ में है, खून चढ़ाने में कतई दिक्कत नहीं होगी।' डॉक्टर की यह तजवीज सुन कर बड़े बेटे छविनाथ के चेहरे पर दुविधा दिखाई दी।
वह गला खँखार कर बोला, 'डॉक्टर, क्या उनकी हालत बहुत नाजुक है?' डॉक्टर ने छविनाथ के चेहरे पर आँखें केंद्रित करके कुछ तीखेपन से कहा, 'यह
कौन कहता है? वह निश्चय ही ठीक होने लगी है। हम बढ़िया इलाज कर रहे हैं उसका।
पहले से वह काफी अच्छी है।' और आशा की किरण चमका कर डॉक्टर चिक हटाते हुए
ड्यूटी-रूम में घुस गया। बाहर खड़े पाँचों आदमी कुछ देर तक चुपचाप एक-दूसरे को देखते रहे। शायद वे
लोग खून लाने की व्यवस्था पर विचार कर रहे थे। सब लोगों को सन्नाटे में देख
कर छविनाथ बोला, 'सुबह एक बोतल खून भी मुश्किल से मिला था। ऐसी आसानी से यहाँ
खून मिलता कहाँ है? घंटों डॉक्टर खोसला के आगे-पीछे घूमा हूँ। तब कहीं यह
इंतजाम हो पाया था।' छविनाथ की आवाज में झींकने का भाव देख कर उसके बड़े बहनोई हीरालाल बोले, छवि,
देर का काम नहीं है। जैसे भी हो, खून का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा।' दूसरे बहनोई ने सुझाव दिया, 'मेरे ख्याल से डॉक्टर की सिफारिश ले चलो।' छविनाथ पर दोनों बहनोइयों के सुझावों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वह रोने
के स्वर में बोला, 'जीजा जी, आपको मालूम नहीं, मैं आज सुबह पाँच बजे खोसला
साहब के यहाँ गया था। तब जा कर कहीं बारह बजे खून का इंतजाम हो पाया था, और
जानते हैं, उन्होंने क्या कहा था? वह कह रहे थे, 'आप लोग खून 'डोनेट' क्यों
नहीं करते; हमारे पास इतना खून कहाँ से आएगा?' हीरालाल ने छविनाथ के टूटते धैर्य को सहारा देने की गरज से कहा, 'चलो-चलो,
दूसरी मंजिल पर चलते हैं। कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा ही।' ठीक इसी समय यूनिवर्सिटी में पढ़नेवाला एक स्टूडेंट आ गया जो हीरालाल की दो
बेटियों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाता था। वह समस्या का उत्साहवर्धक निदान देते
हुए बोला, 'मैं इंतजाम करा दूँगा। और अगर कुछ भी न हो सका, तो मैं अपना खून दे
दूँगा। मेरा और नानी जी का ग्रुप एक ही है।' कहा नहीं जा सकता कि उसकी बात में सच्चाई थी या वह महज हीरालाल की नजरों
में चढ़ने के लिए यह दिलेरी दिखला रहा था। जब से सारा घर उठ कर अस्पताल में आ
गया था, वही लड़का, घर की खोज-खबर रखता था। उसका आश्वासन सुन कर सबके चेहरे पर
आशा दपदपा उठी। एक बाहरी आदमी, जिसका बुढ़िया से कोई खून का रिश्ता नहीं था, जब
इतना कुछ करने को तैयार था, तो सब लोगों को लगा कि वह अपने कर्तव्य से मुँह
मोड़ रहे हैं। लिहाजा उन्हें भी तो कुछ करना ही चाहिए। सब लोग सहसा कुछ न कुछ
बोलने लगे। वे सब दूसरी मंजिल पर रक्त-परीक्षण अधिकारी के कमरे में चले गए। जो युवक
अपना खून देने का दिलासा दे कर सबको यहाँ लाया था, रक्त-परीक्षक से बोला,
'मेरा खून ग्रुप 'ए' का है। मेरा खून ले लीजिए।' रक्त-परीक्षक ने उस सूखे पतले लड़के का मुँह देखा और कहा, 'ऐसे खून नहीं
लिया जाता, जनाब। जब भी ब्लड लिया जाएगा, तभी नए सिरे से खून जाँचा जाएगा।' रक्त-परीक्षक कुछ क्षण सोचता रहा और फिर सामने खड़ी भीड़ को संबोधित करते
हुए बोला, 'आपमें से कौन-कौन ब्लड देना चाहते हैं? मेहरबानी करके वे आगे आएँ।' उसके शब्द सुन कर एक मिनट के लिए सन्नाटा छा गया और फिर धुकधुकी भरी
आवाजें गूँज उठीं, 'हमारा खून जाँच लीजिए। हमारा खून ले लीजिए।' रक्त-परीक्षक ने काँच के टुकड़ों पर छह आदमियों का अलग-अलग खून लिया और
कहा, 'बराए-मेहरबानी, आप लोग बाहर बैठें। अभी कुछ वक्त बाद आप लोगों के ग्रुप
बतला दिए जाएँगे।' सारी भीड़ कमरे से बाहर निकल आई। वे सभी परस्पर वार्तालाप करने लगे। दो ने
सिगरेट सुलगा ली और कक्ष के द्वार से सटी बेंच पर पसर गए। वे सब वास्तव में
बहुत थके हुए और शिथिल थे। उनमें से शायद ही कोई अस्पताल छोड़ कर घर गया हो। वे
सब पूरे हफ्ते से अस्पताल में थे और अपनी दैनिक क्रियाओं से भी जैसे-तैसे
अस्पताल में ही फारिग हो लेते थे। घर से कोई लड़का या लड़कियों को ट्यूशन
पढ़ानेवाला लड़का खाना ले आता था तो मरे मन से पेट में डाल लेते थे। वार्ड के
बाहर बेंच पर दो या तीन कंबल-गद्दे पड़े थे जिन्हें वे लोग रात के समय वार्ड
के बाहर गैलरी में डाल कर पड़े रहे थे। हालाँकि वे लोग संख्या में इतने ज्यादा थे कि रात को बारी-बारी से सो या
आराम कर सकते थे, मगर यह कभी संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि हर आधे-पौने घंटे
बाद कोई औरत वार्ड से बाहर निकलती थी और बुढ़िया के अंतिम साँस निकलने की विकट
सूचना देती थी। इसपर वे सब झपट कर खाँसते हुए उठ पड़ते थे और अपनी नींद से
बोझिल आँखें झपकाते हुए बुढ़िया के बिस्तर के पास जा खड़े होते थे। उनमें से
कोई भी घर जाते हुए घबराता था कि कहीं इसे लापरवाही खयाल न किया जाए। लगभग हर
समय मरीज के निकट बनी रहने वाली सात औरतें और पाँच-छह पुरुष रूग्ण हो चले थे।
उनके चेहरों पर कष्ट, निराशा और थकान के स्थायी चिन्ह अंकित हो गए थे। यों तो बुढ़िया की हालत कई दिनों से गंभीर थी, पर आज लग रहा था कि वह कुछ ही
क्षणों की ही मेहमान है। इसलिए उसके हाथों से 'गोदान' के नाम पर कुछ 'पुन्न'
भी करा दिया गया था। यही नहीं, पिछले एक घंटे से डॉक्टरों की नजर बचा कर
बीच-बीच में एक-दो बूँद गंगाजल उसके मुँह में छोड़ा जा रहा था। बुढ़िया को इतने
लोगों से घिरा देख कर कोई-कोई डॉक्टर झुँझला भी उठता था। पर बुढ़िया की सेवा
करनेवाले अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते थे। एक मरीज के पास इतने अधिक तीमारदार देख कर वार्ड के मरीजों को हैरानी भी
होती थी। किसी बीमार के पास रात को शायद ही कोई रिश्तेदार ठहरता हो। खैर, आध घंटे के बाद रक्त-परीक्षक ने अपने कक्ष से निकल कर बेंच पर ऊँघते
लोगों को बतलाया कि बुढ़िया के रक्त से सिर्फ छविनाथ और हरिनाथ का ही खून मिलता
है। हीरालाल ने फैसलाकुन स्वर में कहा, 'ठीक है, हरि खून दे देगा। छवि और उसकी
बीवी रूक्मणी ने तो पिछले महीने अस्पताल जा कर खैरात में एक-एक बोतल खून दिया
था। ऐसा पता होता, तो...।' उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उनका कहने का मतलब
यह था कि अगर यह पता होता कि छविनाथ को किसी दिन घर में ही खून देना पड़ सकता
है, तो वह व्यर्थ में अपना खून अस्पतालवालों को क्यों दे कर आता? हालाँकि हीरालाल ने एक तरह से आखिरी फैसला दे दिया था, लेकिन फिर भी हर आदमी
अपनी कैफियत सुनाने लगा। नंबर दो के दामाद ने कहा, 'विद्या के तो पाँव भारी
हैं।' विद्या उनकी सहधर्मिणी थी। सबसे छोटे दामाद ने कहा, 'प्रभा को तो आप सब
जानते ही हैं, वह 'एनेमिक' है।' अपनी-अपनी पत्नियों का सबने बचाव कर लिया। हालाँकि रक्त-परीक्षक की रिपोर्ट से सबकी स्थिति पूर्ण सुरक्षित हो चुकी
थी, मगर फिर भी, सब अपनी तत्परता और कर्तव्यपरायणता की दुहाई देने में लगे
रहे। अब वृद्धा के लिए खून देने वालों में सिर्फ दो पुत्र बाकी रह गए थे। हीरालाल
की लड़कियों को पढ़ानेवाला लड़का रक्त-परीक्षक से दोस्ताना लहजे में बोला,
'डॉक्टर साहब, कुछ इंतजाम तो होना ही चाहिए।' उसने छविनाथ के लटके हुए चेहरे को लक्ष्य किया और चापलूसी दिखाने लगा,
'मामा जी तो बेचारे इतने भले हैं कि पहले ही ब्लड बैंक को मुफ्त में खून दे
चुके हैं। इनका खून इतनी जल्दी कैसे लिया जा सकता है?' रक्त-परीक्षक इतने लोगों की झों-झों से तंग आ चुका था परंतु फिर भी सभ्यता
से बोला, 'हाँ, यह तो सही है। मगर अब तो अस्पताल में शायद ही कोई 'डोनेटर' मिल
पाएगा।' सहसा उसे अपने उस काम का ध्यान आ गया जो इन लोगों के कारण बीच में ही
छूट गया था। वह किंचित झल्ला कर बोला, 'जाइए, जाइए, आप फौरन 'ब्लड बैंक' जा
कर कुछ कीजिए। यहाँ वक्त खराब करने से क्या हासिल?' उन सबके चेहरे बुझ गए। रक्त-परीक्षक की झिड़की से वे दीन-हीन हो उठे। वे
वहाँ से उठ-उठ कर चल पड़े और मन ही मन एक-दूसरे को तौलने लगे। शायद वह फिर भूल
गए थे कि उनमें से खून किसी को नहीं देना है। सिवाय बुढ़िया के बेटों को छोड़ कर
बाकी सबके ब्लड ग्रुप भिन्न हैं। हीरालाल ने खून की बात शुरू की और छविनाथ के कंधे पर हाथ रख कर कहा, 'चलो अब
इमरजेंसी में तो हम लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा।' एकाएक सबने इधर-उधर कुछ टटोला। उन लोगों के बीच में बुढ़िया का छोटा बेटा
हरिनाथ नहीं था। हीरालाल ट्यूटर से बोले, 'मास्साब! आप जरा हरि को तो बुलाइए।
मेरा खयाल है, वह ऊपर वार्ड में ही बेंच पर रह गया है।' मास्टर लपकते हुए ऊपर मंजिल में गया और वार्ड के दरवाजे पर अपनी पत्नी से
खुसुर-पुसुर करते हरिनाथ को बुला कर नीचे ले गया। मास्टर के साथ हरिनाथ को आते
देख हीरालाल बोले, 'देखो, ऐसी बात है, भैया, कि 'ब्लड' तुम अपना ही दे दो।
डॉक्टर कहता है कि छविनाथ का खून इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता। वह तो अभी
पिछली बार खून दे भी चुका है।' हरिनाथ के चेहरे पर भय का भाव उभर आया, लेकिन वह हौसला दिखलाते हुए बोला,
'हाँ, हाँ, चलो, इसमें ऐसी क्या बात है? जब खून कहीं से मिल ही नहीं रहा तो हम
ही दे देंगे। क्या महतारी के लिए इतना भी नहीं करेंगे?' सब लोग हरिनाथ के कथन से आश्वस्त हो गए। हीरालाल छविनाथ और हरिनाथ को ले
कर आगे बढ़ गए और बाकी लोग पीछे लौट कर बुढ़िया के पास वार्ड में चले गए। कोई आधे घंटे बाद बुढ़िया के बड़े दामाद हीरालाल खून की बोतल हाथ में पकड़े
हाँफते हुए वार्ड के द्वार पर पहुँचे। वे लिफ्ट से नहीं आए थे, इसलिए तीन मंजिल
तक सीढ़ियाँ पार करने में उनकी हँफनी छूट रही थी। वार्ड के दरवाजे पर बैठे जो
लोग इधर-उधर की चर्चा में मगन थे, उन्हें देखते ही एक साथ उठ कर खड़े हो गए और
समवेत स्वर में बोले, 'खून मिल गया?' हीरालाल तैश में बोले, 'मिल क्या ऐसे ही गया! खून आज फिर छविनाथ ने ही
दिया। हरि का तो कहीं पता ही नहीं चला। गया तो हमारे साथ ही था पर बीच में कहाँ
उड़ गया कुछ मालूम ही नहीं हो पाया। मैंने और छवि ने भीतर इंतजार करा, जब वह
नहीं पहुँचा, तो बेचारे छवि को ही खून देना पड़ा।' निष्कर्ष देते हुए वह अंत
में बोले, 'कुछ नहीं जी। धोखेबाजी कर गया।' सबने छवि की ओर देखा। वह हीरालाल के पीछे आ कर खड़ा हो गया था। हालाँकि वह
शांत और संयत था, लेकिन सब उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने लगे। दो-एक
लोगों ने उसे पकड़ कर जबरदस्ती बेंच पर लिटा दिया। उन सबको वहीं छोड़ कर हीरालाल खून की बोतल हाथ में लिए वार्ड में घुस गए।
हालाँकि खून की बोतल ड्यूटी रूम में बैठे डॉक्टर को देनी थी, पर हीरालाल
बुढ़िया के बेड के पास जा पहुँचे और औरतों की ओर मुँह करके हाँफते हुए बोले,
'देखी कमीनी हरकत हरि की? जाने कहाँ भाग गया। खून बेचारे छवि को ही देना पड़ा।' औरतें, जो बुढ़िया से संबंधित कोई न कोई कार्य कर रही थीं, अपनी
व्यस्तताओं से उबरकर एकदम सर्तक हो गईं। प्राय: सभी बहनें आश्चर्य के स्वर
में बोलीं, 'अयं! छवि भैया ने खून दिया? कहाँ है छवि?' और सहसा उनकी अपने बड़े भ्राता के लिए ममता और सहानुभूति उमड़ पड़ी। हीरालाल
ने उँगली से संकेत करके बतलाया, 'होता कहाँ, बाहर बेंच पर पड़ा है।' इसके बाद हीरालाल ने विस्तार से सारी बात समझाते हुए कहा, 'हम सबके साथ
उसने अपने खून की जाँच तो करवा ली, मगर ऐन वक्त पर धोखा दे गया।' बुढ़िया के
छोटे बेटे की बहू नीचे झुक कर बेड के नीचे पड़े कपड़े उठा रही थी। उसके चेहरे
पर हीरालाल की बात सुन कर ऐसा भाव आया मानो कोई बहुत अनहोनी घटना सहसा टल गई।
छविनाथ की पत्नी रूक्मणी सास के मुँह पर भिनभिनाती मक्खियों को यकायक भूल गई।
हीरालाल की बात सुन कर उसने सिर पर दोहत्थड़ मारा और चीत्कार के स्वर में
बोली, 'हाय, मर गई मैं तो, लोगों। देखूँ तो कहाँ पड़े हैं - होश भी है
उन्हें?' छवि की पत्नी के हाय खाने से सारी बहनें और हरिनाथ की पत्नी सहम गईं। उन
सबने बुढ़िया की तरफ देखा। उसकी आँखें थोड़ी-थोड़ी देर बाद खुल रही थी। और
पोपले मुँह से कभी-कभी 'फुरर्र' की ध्वनि भी निकल रही थी। यदा-कदा आँखें
मुलमुला कर वह कुछ अस्फुट स्वरों में बड़बड़ाती भी थी लेकिन उसकी अस्पष्ट
ध्वनि का अर्थ खोजने का उत्साह इस क्षण किसी में दिखाई नहीं पड़ रहा था। बहनों में से किसी ने कहा, 'छवि तो अपना सरवन कुमार निकला।' कई कंठों ने इस
संज्ञा को सही समझ कर ताईद की। डॉक्टर ने जिस समय खून की बोतल बदली, तो कई मर्द-औरतों ने उस बोतल की ओर
देखा जैसे इंतजार की घड़ियाँ इस बार अनिश्चित काल के लिए खिंच गई हो। माँ के
सिरहाने बैठ कर मंत्र पढ़ने वाली बेटी माँ को भूल कर अपने बड़े भाई की हालत
देखने वार्ड के बाहर चली गई। मनीष ने अपनी खटारा साइकिल बहुत नामालूम ढंग से दीवार के सहारे टिका दी और
कमरे में पड़ी एकमात्र कुर्सी पर जा कर धम्म से बैठ गया। हलकी-फुलकी टीन की
कुर्सी उसके बोझ से बुरी तरह डगमगा गई पर चलो खैर हुई, कुर्सी उलटी नहीं। दूसरे
कमरे में बच्चे चीख-चीख कर अंग्रेजी की राइम रट रहे थे, 'हम्टी-डम्टी सेट आन
ए वाल...' हालाँकि आसानी से वह अपना संतुलन नहीं खोता; आड़े वक्त पर कई बार
किताबों की पढ़ाई और उनसे टपकती हुई दार्शनिकता उसे सँभाल ले जाती है। बाज
मौकों पर बच्चों की चीख-पुकार से उसके थके हुए मस्तिष्क की शिराएँ झनझना उठती
हैं, पर वह तर्क से स्वयं को समझाता है, 'बच्चे चीखें-चिल्लाएँगे नहीं तो
क्या बुड्ढों की तरह सिर दाब कर बैठेंगे!' लेकिन आज उसकी तबियत हुई कि जोर से
बच्चों का डाँट दे या उनके कान पकड़ कर उन्हें जमीन से ऊपर उठा ले। जब देखो
कंबख्त घर को मछली-बाजार बनाए रहते हैं और उसकी आँखों में खामख्वाह वह दृश्य
कौंध गया जब लोग अपने बच्चों की जबरदस्ती प्रशंसा करवाने के लिए घर आए
मेहमानों को यह ऊल-जलूल राइम सुनवाते हैं और उन्हें उकसाते हैं, 'हैं-हैं-हैं,
अच्छे बच्चे अंकल को नमस्ते करते हैं, पोइम सुनाते हैं, हैं-हैं-हैं, सुनाओ
बिट्टू, शर्माओ मत... हम्टी डम्टी सेट..' मनीष का सिर भन्ना गया, उसने अपनी
कनपटियों को कस कर दबाया। तात्कालिक दबावों से आदमी की प्रखरता कितनी जल्दी टें बोल जाती है इसे
मनीष अपनी 'आनर्स' की पढ़ाई से नहीं जान पाया था। पिछले कुछ बरसों में नई
साइकिल को खड़खडिया बनते देख कर वह बखूबी इस किस्म का फलसफा समझ गया है। यही
वजह थी कि 'अभावों और असंतोष के खटरागों' को वह बरसों से रोमांटिक बनाता आ रहा
था मगर आज उसे लगा कि उसकी कमर बुरी तरह टूट गई है। शाम को साइकिल बाहर निकालता
था, उसका जैसे आज अंत हो गया है। तीन महीने पहले उसने एक कुर्ता-पायजामा सिलवाने की बात सोची थी और उससे भी
तीन मास पहले एक पाँच-सात रुपए वाली सस्ती-सी चप्पल लेने की बात। वह बात
सोचते-सोचते अब इतनी निर्जीव हो गई थी कि चप्पल खरीदने का उत्साह बिलकुल खतम
हो चुका था, उसी तरह जैसे उछाह से किसी से मिलने जाओ, और पहुँचते-पहुँचते
रास्ते में ही इतने तंग हो जाओ कि मिलने की आतुरता ही दम तोड़ बैठे। संयोग से
उसके मित्र आनंद ने पच्चीस रुपए का एक जूता खरीदा था लेकिन पता नहीं उसके पैर
में जूता कैसे छोटा पड़ गया। एक दिन मनीष को अपने घर से उसने वह जूता जबरदस्ती
पहना कर भेज दिया। मनीष ने ऊपर से काफी संकोच दिखाया था, उसे डर था कि कहीं
आनंद की पत्नी उसे बहुत हीन खयाल न करे... भला जूता भी कोई दोस्तों को दी
जाने वाली चीज है! पर आनंद की पत्नी ने उसका संकोच निवारण करते हुए कहा था,
'आपके पैर में तो एकदम फिट बैठा है।' मनीष से जब कोई उत्तर नहीं बन पड़ा था तो
जबरदस्त ठहाका लगा कर बोला था, 'भाभी, यह इस साले का षड्यंत्र है, दरअसल यह
पिछले जन्म का मोची है इसलिए जबरदस्ती जूता भेंट करने पर तुला है,' और जूता
पैरों से उतारते हुए बोला था, 'चल हरामी, मैं नहीं लेता तेरा यह दान।' आनंद ने आँखें तरेर कर कहा था, 'तो फिर समझ तेरे सिर और इस जूते का रिश्ता
बहुत दिनों तक बना रहेगा - रोज आए सौ जूते खा गए। और न हो तो पैसे दे देना,
मरता क्यों है बे, बहरहाल इस जूते का लौटाना अब मुमकिन नहीं है; दान तो फिर
दान ही ठहरा। कहा भी है किसी ने चर्म दानम् महादानम्।' मनीष आनंद की बात सुन
सकपका गया, कहीं साला आगे की बात भी न बक जाए; भाभी सामने बैठी हैं। मनीष और
आनंद जब अकेले में बैठ कर फोहश मजाक करते थे तो कहते '...बेटा...दानम्।' लेकिन
आनंद की पत्नी को इस पृष्ठभूमि का कोई स्पष्ट संदर्भ ज्ञात नहीं था, इसलिए
उसने कोई नोटिस नहीं लिया। लेकिन अब? अब जाड़ा बीत चुका था; वसंत का मौसम चल रहा था। जाड़े के दिनों
में मनीष गरम कपड़ों - गरम कपड़े भी क्या झग्गर-झोला किस्म की पुरानी पतलून
और कोट - के साथ आनंद के जूतों को चढ़ाता रहा था, लेकिन कुर्ते-पायजामे के साथ
अब यह जूते बिलकुल भी नहीं घिसट पा रहे थे। मनीष ने मजाक में दोस्तों से कई
बार कहा, 'एक कुरते-पायजामे का सवाल है बाबा, एक सस्ती-सी चप्पल का सवाल है
बाबा।' सब लोग उसकी बातों पर हँस देते थे लेकिन असलियत किसी-को मालूम नहीं थी
कि मनीष जो कुर्ता-पाजामा पहन कर दफ्तर आता है और जो हमेशा झकाझक दिखाई पड़ता
है उसे वह रोज रात को धो लेता है और सुबह इस्तरी करके पहन आता है।... खद्दर के
कपड़े पहनने का शौक उस हालत में शौक नहीं मातम हो जाता है जब किसी आदमी के पास
उनकी गिनती महज एक अदद तक जाती हो। दफ्तर की तनख्वाह के अलावा कहीं से एक पैसे की आमदनी नहीं। ढाई सौ मिलते थे
मगर हालत यह थी कि सौ में से पचास चीजें अगले महीने (जन्म) के लिए टाल दी जाती
थीं और यह टालने का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू हुआ था कि इसके अंत का कहीं सूत्र
ही दिखलाई नहीं पड़ता था। बच्चों के कपड़े अगले महीने, सिनेमा अगले महीने,
किसी दोस्त या संबंधी के यहाँ जाना अगले महीने, एक चप्पल अगले महीने... एक
कुर्ते-पाजामे का सवाल है बाबा... अगले महीने, अगले महीने। 'अगले महीने' मनीष
के दिमाग में अब इस तरह बजने लगा था जैसे आपसे कोई भिखारी कुछ माँगे और आप बिना
एक क्षण भी सोचे कहें, 'आगे देखो बाबा।' निशा उससे हर बार कहती, 'नौ साल मुझे इस घर में आए हो गए, अपने हाथ में पैसा
रखने की मैंने कभी जिद नहीं की लेकिन भले आदमी, तुम खाली एक महीने की तनख्वाह
मेरे हाथ पर ला कर रख दो; एक कुर्ता-पाजामा और चप्पलें तो तुम्हें दिलवा ही
दूँगी कम से कम।' वह परम आस्तिक भाव से निशा की बात सुनता। उसके चेहरे पर बात
मान जाने वाले बच्चे का भाव आ जाता और वह स्वीकार की मुद्रा में गर्दन हिला
कर कहता, 'बिलकुल सही कहती हो, मेरा भी खयाल है। देख लेना अगले महीने मैं यही
करने वाला हूँ।' लेकिन अगले मास जब वह दफ्तर से लौटता तो दफ्तर के बंधुओं का
उधार चुकाने के बाद उसके पास कठिनाई से इतने रुपए बचते कि दूध, बच्चों की फीस
और मकान का किराया चुकाया जा सके। मकान मालिक एक ही हरामी था; पहली की शाम को
छाती पर आ खड़ा होता था और मकान का किराया 'अग्रिम में झटक ले जाता था; यह बात
शायद कतई महत्व नहीं रखती थी कि मनीष पिछले चार साल से उसी मकान में 'बैठा'
हुआ था। पिछले कुछ दिनों से मिलने-जुलने वालों का आना भी मनीष को रास नहीं आ रहा था।
गो कि वह चाहता था लोग खूब आएँ-जाएँ; हँसी-मजाक चले, गप्प-गोष्ठियाँ जमें
लेकिन मामूली-से चाय-नाश्ते में जो दो रुपए टूट जाते थे उनकी कसक भी कम नहीं
होती थी। उसे अब पुराने रीति-रिवाज अच्छे लगने लगे थे। जब लोग महज दो वक्त
खाना खाते थे। कोई खाने के वक्त आ गया तो ठीक वरना बेवक्त आनेवाले को पानी के
गिलास या शरबत से ही टरका दिया जाता था। बहुत हुआ हुक्का सामने ला कर रख
दिया। एक चिलम-तंबाकू पाँच आदमी मजे में पी सकते थे - कितने अच्छे थे
किफायतसारी के वे दिन! और अब? अब मुसीबत यह है कि जाड़े में चाय पिलाओ और कुछ
खाने को भी दो। गर्मियों में उससे भी बड़ी मौत; घर का बना शर्बत-शिकंजी कोई
प्रसन्नता से पीता नहीं; बाजार से कोकाकोला मँगाओ तो चार रुपए की चपत मामूली
बात है। आनेवालों को मुस्कराते हुए पेश करो और भीतर से कुढ़ते हुए उनके साथ
खुद भी पीओ। मनीष दफ्तर से लौट कर चाय खतम करते ही निशा से कहता, 'अब घर से जलदी-जल्दी
निकलने की तैयारी करो। मैं बच्चों को कपड़े पहनाता हूँ, तुम भी धोती बदलो;
कहीं कोई आ न मरे।' निशा कहती, 'अभी थोड़ी देर में दूधवाला आएगा; दूध का कैसे
होगा?' 'दूध-फूध छोड़ो, चौधरी साहब से कह देंगे।' और इस तरह चौधरी, वर्मा और खन्ना सभी पड़ोसी मनीष का दूध लेते-देते तंग हो
चुके थे। अब वह उन लोगों से दूध लेने के लिए कहता तो जवाब मिलता, 'भाई, अब आपका
दूध कब तब रखें; आपका कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी रात नौ बजे तो कभी दस बजे
लौटते हैं।' और इतनी लबड़ धों-धों करते-करते कभी तो कोई ठीक उस वक्त द्वार
खटखटाया जब मनीष बच्चों को कपड़े पहना चुका होता और निशा महज ब्लाउज और
पेटीकोट पहने जूड़े, आँखों के काजल या होंठों की लाली में उलझी होती। द्वार पर
होनेवाली खटखट से मनीष का दिमाग खराब हो जाता, वह निशा पर खौखिया उठता, 'लो और
लगाओ छह घंटे सिंगार-पटार में, अब आ मरा कोई साला, दो घंटे से पहले हिलने का
नाम नहीं लेगा।' ऐसे अक्सर पर निशा बेचारी एक लंबी साँस ले कर रह जाती और अभी दो मिनट पहले
उतारी हुई मैली धोती फिर से लपेटने लगती । निशा बाहर निकलने से पहले जब मनीष से पूछती कि कौन-सी साड़ी पहनूँ तो मनीष
की झुँझलाहट का कोई ठिकाना न रहता। वह झुँझला कर कहता, 'कोई भी पहन लो भागवान,
बेकार की बातों में सिर मत खपाओ।' वह मनीष की ओर बड़ी-बड़ी आँखों से चुपचाप
देखती। उन आँखों में घिरी निरीहता जैसे पुकार-पुकार कर कहती, 'पहले तो तुम ऐसे
नहीं थे; शादी के बाद शुरू में न जाने कितने दिनों तक 'आप-आप' करके बोलते थे।
इन बालों में अपना चेहरा छुपा लेते थे। अब इन बालों में कंघी करने की छूट देना
भी तुम्हें बरदाश्त नहीं है। यहाँ तक कि अपनी पसंद की साड़ी भी नहीं बता
सकते!' वह वेधक दृष्टि मनीष अदेखी कर जाता लेकिन जब मनीष रात को बिस्तर पर
लेटता और उसकी बाँह पर सिर टिकाए निशा आराम से सो जाती तो उसे पूरी फिजा में
निशा की वही दो बड़ी-बड़ी कातर आँखें तैरती दिखाई पड़तीं। मनीष देर तक जागता
पड़ा रहता, वह करवट भी न बदलता, कहीं निशा की नींद न टूट जाए। निशा का शांत,
सलोना चेहरा उसके मन में पश्चाताप जगाता, 'मैं इसे कितनी बेरहमी से डाँट देता
हूँ। बेचारी!' पानी सिर के ऊपर से हो कर गुजरने लगा तो मनीष बराबर इसी उधेड़बुन में लग गया
कि अब क्या हो; दिन कैसे कटे? लोग उपदेश तो देते हैं कि जो आमदनी हो आदमी को
उसी में खर्च चला कर आड़े वक्त के लिए दो पैसे बचाने चहिए, मगर यह कोई नहीं
बताता कि आदमी आखिर आधा बन कर कब तक जिए। और चलो आदमी खुद को दूसरा समझ कर अपने
साथ निर्ममता का व्यवहार कर सकता है लेकिन बीवी-बच्चों को यह कैसे समझा सकता
है कि भई, तुम लोग स्वयं को कुछ और खयाल करके अपने साथ दुश्मनों जैसा
व्यवहार करो। चाह और राह के सिद्धांत को ले कर आमदनी यानी ऊपरी आमदनी का एक सिलसिला निकल
ही आया। एक परिचित धनी सज्जन मल्होत्रा साहब की लड़की इंटर की परीक्षा दे रही
थी। परीक्षा का एक-डेढ़ महीना बाकी था। मनीष ने साहित्यरत्न पास कर रखा है और
यह उसने अपने दरवाजे की तख्ती पर भी जड़ रखा है, 'मनीषचंद्र बी. ए. आनर्स,
साहित्यरत्न।' पड़ोस के लोग इसी साहित्यरत्न के चक्कर में उसे शास्त्री
जी कहने लगे थे। मल्होत्रा साहब एक दिन सब्जी वाले की दुकान पर मिल गए तो
कहने लगे, 'बच्ची इंटर का एक्जाम दे रही है; हमें भी आपके ज्ञान का लाभ मिल
जाए। थोड़ी देर उसे देख लिया करें तो क्या कहना।' अपनी सारी अकर्मण्यता झाड़
कर मनीष बोला, 'हाँ, हाँ, क्यों नहीं; जरूर! मैं कल ही आऊँगा।' और इस तरह अतिरिक्त आय का साधन निकल आया। मनीष ने निशा और बच्चों को
घुमाना छोड़ दिया। दफ्तर से लौटते ही चाय पीता और एक सिगरेट पीते हुए साइकिल
निकालता। निशा कहती भी, 'एक फर्लांग दूर उनका घर है पैदल ही क्यों नहीं चले
जाते; घूमना भी हो जाएगा?' वह क्लर्कों की दार्शनिकता बघारता, 'क्लर्क के पास
अपनी दो ही चीज तो होती हैं - एक घरवाली, दूसरी साइकिल; दो में से एक हमेशा साथ
रहनी चाहिए।' महीना जिस दिन पूरा हुआ मल्होत्रा साहब ने सत्तर रुपए लिफाफे में रख कर
दिए। वह बोला, 'अभी ऐसी क्या जल्दी थी, आ जाते,' लेकिन उसने रुपए जल्दी से
जेब के हवाले किए और इस तेजी से घर लौटा गोया जीवन में अपने परिश्रम की कमाई आज
पहली बार उसके हाथ आई हो। मनीष ने लिफाफा निशा के हाथ में दिया तो वह
प्रश्नसूचक दृष्टि से उसे देखने लगी। वह गदगद स्वर में बोला, 'पहले महीने की
कमाई है।' निशा ने लिफाफा खोले बगैर ही पूछा, 'कितने हैं ?' 'मैंने गिने नहीं। ' निशा ने अत्यंत निस्पृह भाव से लिफाफा खोल कर रुपए गिने और बोली, 'सत्तर
हैं।' सब्जी की टोकरी लिए हुए निशा व्यस्तता से कमरे में घुसी। और मनीष को
कुर्सी पर माथा थामे देख कर घबरा गई, क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हो, बड़ी
जल्दी लौट आए आज?' मनीष ने जरा-सी आँखे खोलीं और पहलू बदल कर बैठ गया। निशा ने उसके पास पहुँच
कर उसकी कलाई छू कर देखी, कहीं बुखार तो नहीं हो गया? मनीष ने उसका हाथ धीरे से
हटा दिया और बोला, 'कुछ नहीं हुआ है, एक गिलास पानी भेजो, आज छुट्टी हो गई।' पहली बार तो निशा की समझ में नहीं आई कि 'छुट्टी हो गई' का क्या मतलब है।
वह पूरी बात सुनने के लिए खड़ी रही लेकिन मनीष जब फिर आँखे बंद करके बैठ गया तो
वह पानी लेने चली गई। मनीष के हाथ में पानी का गिलास ला कर दिया तो वह बोला,
'शीला इम्तिहान नहीं दे रही है। मैंने आज जा कर पूछा, पर्चा कैसा हुआ', तो वह
बोली, 'मास्टर साहब, मैं इस साल प्रविष्ट नहीं हो रही हूँ।' मैं सोचता रहा
शायद कोई वजह बताए लेकिन जब उसने कोई साफ कारण नहीं बताया तो मैं उठ कर चला
आया। वहाँ बैठ कर अब क्या करता?' इतने पर भी निशा की समझ में कुछ नहीं आया। शीला इम्तिहान नहीं दे रही है तो
न दे, बड़े आदमी की लड़की है। लेकिन मनीष के सिर में दर्द क्यों है? वह मनीष से
बोली, 'मैं तो डर गई थी, न जाने क्या बात है जो आप माथा पकड़े बैठे हैं, चलिए
कपड़े बदल डालिए।' मनीष ने हाथ में पकड़े हुए गिलास का पानी एक साँस में खतम कर दिया और दुखी
से स्वर में बोला, 'तुम नहीं जानतीं निशा - इससे मौत हमारी ही हुई, उन लोगों
को कोई परवाह नहीं है लेकिन हम तो सत्तर रुपए से मारे गए।' निशा की प्रश्नात्मक मुद्रा देख कर मनीष ने बात साफ की, 'शीला परीक्षा
देती तो अभी अठारह-बीस दिन और पढ़ती कि नहीं? अब वह कुल ग्यारह दिन पढ़ी है।
मल्होत्रा साहब पिछले माह का हिसाब चुकता कर चुके हैं, ग्यारह दिन के ज्यादा
से ज्यादा पच्चीस रुपए बनते हैं और अब तो उन पच्चीस को भी माँगने जाने का
बहाना खतम हो गया।' बजाय दुखी होने के निशा के चेहरे पर मुस्काराहट आ गई। वह ठहाका लगा कर
बोली, 'ओ हो !पच्चीस रुपए के गम में माथा पकड़े बैठे हैं। आपकी हालत हमारे
मोहल्ले के बरकत चाचा जैसी है। बरकत चाचा मुर्गे-मुर्गियाँ पालते थे। एक दिन
एक कुत्ता बरकत चाचा का एक चूजा मुँह में दबा कर भाग खड़ा हुआ। चाचा डंडा ले
कर गालियाँ बकते हुए उसके पीछे दौड़े। दूर जा कर कुत्ता पकड़ में आया तो
उन्होंने उसकी पीठ पर कई डंडे पटका दिए। तब कहीं जा कर चूजा कुत्ते के मुँह
से बाहर आया। लेकिन चूजा अधमरा तो हो ही चुका था। ओह, देखने लायक था वो सीन!
उन्होंने दबे-कुचले चूजे को उठा कर उसके सिर पर कई चपत मारे और रो कर उसे छाती
से लगा लिया। जब वह घर लौट रहे थे तो उनकी दाढ़ी आँसुओं से तरबतर थी और बरकत
चाचा चूजे को ऐसी-ऐसी गालियाँ दे रहे थे कि क्या बताऊँ! बोल हरामी, फिर
निकलेगा दड़बे से बाहर, बोल हरामी...।' हाँ, यह बात दूसरी है कि उन्हीं बरकत
चाचा के घर पूरा मुर्गा किसी भी दिन भून लिया जाता था; घर का मुर्गा दाल बराबर
जो ठहरा।' निशा ने मनीष का लटका हुआ चेहरा देखा और उसे गुदगुदा कर बोली, 'सच बताओ,
ट्यूशन छूट जाने का दुःख है या असली दु:ख उस लड़की से संपर्क टूट जाने का है?
कहीं उसके प्यार में तो नहीं पड़ गए? यह मास्टर कौम इसीलिए बुरी होती है;
लड़की का साथ मिला और भावुक हो कर आत्मा का संबंध जोड़ बैठे।' निशा दुष्टता
से मुस्कराते हुए उठी और दूसरे कमरे की ओर जाते हुए बोली, 'मैं अभी आती हूँ,
इतने में मेरी बात पर 'गहन विचार' कीजिए।' दस मिनट बाद लौटी तो चाय का प्याला और पाँच रुपए का एक नोट हाथ में पकड़े
हुए थी। चाय का प्याला मनीष के हाथ में दे कर वह उसकी आँखों के करीब नोट जा कर
खड़खड़ाने लेगी। मनीष ने उसकी इस क्रिया को बहुत नासमझ अंदाज में देखना शुरू कर
दिया। वह हँसते हुए बोली, 'पच्चीस तो नहीं, हाँ, पाँच रुपए मैं आपको दे सकती
हूँ क्योंकि इस महीने के ट्यूशन से आपको एक चप्पल की कामना थी। लीजिए यह नया
नोट और चप्पल खरीद लाइए।' मनीष ने मुक्त रूप से हँसती हुई निशा का चेहरा देखा और उसे पहली बार अनुभव
हुआ कि जिंदगी के जिन दबावों को वह जीवन-मरण का प्रश्न बनाए हुए है और सहसा
शुरू हुए किसी ट्यूशन के यकायक छूट जाने पर माथा पकड़े बैठा है, वह निशा के लिए
कोई विचारणीय मुद्दा नहीं हैं। छोटे-छोटे बोझ सिर पर लादते चले जाने से आदमी का
यही हश्र होता है। मनीष के मन में गहरा पैठा हुआ विषाद एक क्षण में तिरोहित हो गया। दूसरे कमरे
में शोर मचाते बच्चों की आवाज अब उसे उतनी कर्कश नहीं लगी। निशा की यह बेबाकी
उसे भीतर तक हल्का कर गई। उसने देखा, निशा अभी सुंदर है। जिंदगी के अभाव बहुत
कटु हैं लेकिन अभाव शायद कभी खतम नहीं होंगे पर निशा का सौंदर्य हमेशा ऐसा नहीं
रहेगा। किसी अनोखी प्रेरणा के वशीभूत हो कर वह सहसा उठा और निशा को प्रगाढ़
आलिंगन में बाँध लिया। दहलीज के बाहर दो चमरौधे जूते पड़े देख कर मैं आगंतुक के विषय में कोई
स्पष्ट अनुमान नहीं लगा पाया। मैंने दूर तक सोचा, पर मेरी स्मृति में कोई
ऐसा व्यक्ति नहीं उभरा जो ऐसे अनगढ़ जूते पहनता हो। मैंने समझा, कोई देहात का
रिश्तेदार सरे राह इधर आ निकला है। उत्सुकतावश मैं कमरे में चला गया। पीतल की कमानी का चश्मा लगाए एक
वयोवृद्ध सज्जन सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। पिंडलियों से ऊपर तक एक मोटी
चादर बतौर धोती लपेटे हुए थे और लंबे चोगे जैसा गाढ़े का कुर्ता पहने हुए थे।
इतने मोटे-झोटे लिबास के बावजूद उनका शरीर बहुत दुर्बल लग रहा था। पूरी देह में
सिर्फ मस्तक देखने से ऐसा लगता था कि कभी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। मुझे सामने देख कर वह व्यस्तता से उठे और मुझे अपने आलिंगन में ले लिया।
अपने स्नेह-पाश से मुक्त करने के बाद भी देर तक वह मेरी हथेलियों को स्नेह
से दबाए रहे। उनकी आँखों में एक दर्दमंद और निश्छल मुस्कराहट उभर उठी। कई क्षण
निस्तब्धता में बीत गए। फिर वह स्वयं ही बोले, 'पहचाना नहीं?' उस आवाज में दिल पर दस्तक देने वाली खरज इतनी उम्र बीत जाने पर भी समाप्त
नहीं हुई थी। मेरे मुँह से अनायास निकला, 'महाशय जी?'.... 'हाँ, भाई!' कह कर वह गहरी आत्मीयता से मुस्कुराते रहे। लगभग तीस-बत्तीस
वर्ष बीत चुके थे। उन्हें युगों बाद सामने देख कर मैं आश्चर्यचकित था। मैंने
अपना अचरज दबाते हुए कहा, 'आपको पहचानना वाकई मुश्किल काम है। बदल भी तो कितना
गए हैं इस बीच।' मेरे शब्दों पर उन्होंने सहज भाव से कहा, 'बहुत कुछ बदल चुका है भाई! न
जाने कितना कुछ तो अब ऐसा है, जिसकी शायद शिनाख्त ही नहीं हो सकती।' उनके शब्दों से जैसे एक बहुत दूर छूटी हुई पहचान ताजा हो रही थी। मेरी
दृष्टि सफेद बालों से भरे उनके हाथों और जीर्ण कलाइयों पर अटकी हुई थी। ओह!
वास्तव में चीजें अपनी पहचान खोती चली जा रही हैं। हालाँकि शब्दों से मैंने यही व्यक्त किया था कि महाशय जी बहुत बदल गए
हैं, पर सच्चाई का एक दूसरा पक्ष भी था, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था।
उनके शरीर और आकार में चाहे जो परिवर्तन दीख पड़ता हो, उनके लिबास और व्यवहार
में रत्ती-भर भी बदलाव नहीं आया था। वहीं गाँव के जुलाहे की बुनी हुई चादर
धोती का काम दे रही थी। वही ढीला-ढाला मोटे गाढ़े का कुर्ता था। कोने में खड़ी
गाँठदार लाठी भी शायद कई दशक पुरानी थी। चेहरा बहुत कोशिश पर ही पकड़ में आता
था, तथापि मुस्कराहट आज भी बेलौस और रहमदिल थी। दाँत घिस कर छोटे पड़ गए थे,
लेकिन उन्होंने महाशय जी का साथ नहीं छोड़ा था। प्रशस्त ललाट पर पड़ी रेखाएँ
एक लंबा इतिहास सँजोए हुए थीं। महाशय जी का सही परिचय देने के लिए मुझे सन बयालीस के तूफानी दौर में जाना
पड़ेगा। मैं तब कुल जमा दसेक बरस का बच्चा था। उन दिनों हम लोग गाँव में ही
रहते थे। मेरे बड़े भाई नहरवाई में मुलाजिम थे। हमारा लंबा-चौड़ा परिवार एक
किसान के मकान में आधा हिस्सा ले कर रहता था। महाशय जी स्वराजी थे और किसानों
को मालगुजारी तथा आबपाशी का महसूल जमा करने से रोकते थे। फलस्वरूप गाँव के
गलियारों में बीहड़ दृश्य उपस्थित रहता था। मालगुजारी जमा न करने वाले किसानों
के बर्तन-भांडे, बैल और दीगर सामान कुर्क अमीन के सिपाही मकान के बाहर ला-ला कर
बेरहमी से इधर-उधर पटकते थे। महाशय जी का प्रभाव उन अनपढ़ देहातियों पर कुछ कम
नहीं था। वह लुट जाना बरदाश्त कर जाते थे, मगर महाशय जी की बात नहीं टालते थे। किसानों की औरतें गलियों में बिखरी अपनी दुनिया को देख कर छातियाँ पीट कर
पछाड़ खाती थीं। बच्चे सहमे और धीरज खो कर बिलखते नजर आते थे, पर किसान कुर्क
अमीन या उसके मातहत सिपाहियों की चिरौरी नहीं करते थे। ठीक इसी क्षण पता नहीं कहाँ से महाशय जी प्रकट हो जाते थे। वह किसानों, उनकी
औरतों और बच्चों को अभय करते हुए कहते थे, 'श्रीमान अमीन साहेब! इंसाफ का कम
से कम इतनी बेदर्दी से तो खून मत कीजिए। जब इन लोगों को आपके आका जानवरों की
तरह मेहनत-मशक्कत करा कर भी सूखी रोटी मुहैया नहीं कर सकते, तो उन्हें लगान
वसूल करने का हक कहाँ बनता है? पहले आप अपनी सरकार से इन्हें रोटी, कपड़ा
दिलवाइए और फिर मालगुजारी का जिक्र कीजिए।' भाई के सरकारी नौकर होने के कारण हमारे दरवाजे पर गाँव के चौकीदार और मुखिया
से ले कर उस क्षेत्र के थाना-इंचार्ज तक की आवाजाही बनी रहती थी।
अगस्त-क्रांति के उन तूफानी दिनों में अंग्रेज बहादुर के ताबेदार बराबर कुछ न
कुछ सूँघते चले आते थे। आसपास के सारे गाँवों में महाशय जी घूम-घूम कर आंदोलन
की आग को भरपूर हवा दे रहे थे। किसानों को सरकार के विरूद्ध बहुत सफलता से
उकसाया जा रहा था। किसी न किसी चौकी और थाने पर हर सुबह तिरंगा फहरता दिखाई दे
जाता था, और विचित्र बात यह थी कि महाशय जी पुलिस की पूरी सर्तकता के बावजूद
पकड़ में नहीं आ रहे थे। कई दफे उनके घर पर रात को छापा पड़ा। खुफिया पुलिस के
लोग भी गाँवों में घूमते पाए गए, पर महाशय जी शासन के चौकन्नेपन को भेद कर
अपना प्रचार बदस्तूर करते रहे। महाशय जी के बार-बार बच निकलने के पीछे एक रहस्य था। महाशय जी की धर-पकड़
करने वाले पुलिस कर्मचारी सबसे पहले हमारे घर ही आते थे। उन्हें मेरे बड़े भाई
साहब की सहायता पर पूरा विश्वास था। उनका अनुमान था कि सरकार के खैरख्वाह
मेरे भाई महाशय जी की गतिविधियों पर गहरी नजर रखते होंगे और किसी दिन (वाहवाही
लूटने के ख्याल से) उन्हें जरूर गिरफ्तार करवा देंगे। घर में सयाना बच्चा
होने के कारण भाई ने मुझसे कह रखा था कि जैसे ही पुलिस हमारे दरवाजे पर दिखाई
पड़े, छतों पर से होते हुए महाशय जी के घर में जा कर इत्तिला दे दिया करो और घर
लौट आया करो। यह सिलसिला दिसंबर महीने तक सफलतापूर्वक चलता रहा। महाशय जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। एक राजपूत परिवार में जन्म
लेने के कारण वह श्रेष्ठ और कुलीन माने जाते थे। दहकते तांबें के रंग की
लंबी-चौड़ी देह थी। कंधे बहुत मजबूत थे और खुला हुआ प्रशस्त ललाट देखने वाले
को हठात अपनी ओर आकर्षित करता था। आँखों में बाँधने वाली चुंबकीय शक्ति थी,
लेकिन अपनी जाति की श्रेष्ठता से वह कभी अभिभूत नहीं होते थे, बल्कि जो कुछ वह
करते थे, उससे उनकी बिरादरी को सख्त तकलीफ होती थी। हरिजन, जिन्हें गाँव के सीमांत पर रहने के लिए मजबूर किया गया था, महाशय जी
के परम स्नेही थे। उनकी ऊबड़-खाबड़ गलियों में वह उनके साथ लग कर सफाई करते
थे। रात को हाथ में जलती लालटेन लटकाए वह गलियों से गुजरते दिखाई पड़ते थे और
चमरटोली में जा कर रात्रि पाठशाला चलाते थे। ठाकुरों और हरिजनों में जब भी कोई
तकरार होती थी, महाशय जी आगे आ कर सिर फुटौवल के अवसर बचा जाते थे। महाशय जी के माता-पिता उन्हें बहुत छोटा छोड़ कर मर गए थे। वह अपने एकमात्र
चाचा के साथ रहते थे। उस जमाने में चाचा के बच्चे नाबालिग थे, इसलिए चाचा
महाशय जी से उम्मीद करते थे कि उन्हें खेत के काम में भी थोड़ा हाथ बँटाना
चाहिए। दुनिया-भर के दुख-दर्द में डूब जाने से अपनी क्या भलाई होगी! महाशय जी
के चाचा बड़बड़ाते रहते थे, लेकिन वह अपने भतीजे को प्यार भी बहुत करते थे।
जाति-बिरादरी वालों की आलोचना पर भी कभी कान नहीं देते थे। महाशय जी को
सामाजिक-राजनीतिक काम करने की उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। यह महाशय जी का ही प्रताप था कि उनकी प्रेरणा से गाँव के छोटे-छोटे बच्चे
तक हाथों में रंग-बिरंगी झंडियों और सरकंडों पर लिपटे पोस्टर ले कर गाँव की
गलियों में 'इंकिलास जिंदाबाग' के नारे लगाते बेखौफ घूमते थे। गाँव के मुखिया
और चौकीदार का डराना-धमकाना भी कोई काम नहीं आता था। बयालिस के दिसंबर के आखिरी दिन थे कि गाँव की गलियों में एक सुबह शोर मच
गया, 'महाशय जी पकड़े गए, महाशय जी पकड़े गए!' उनकी गिरफ्तारी से सारे वातावरण
में सनसनी फैल गई। जिस समय पुलिस की गाड़ी उन्हें ले कर जानेवाली थी, सैकड़ों
ग्रामीण उन्हें घेर कर खड़े हो गए। आँखें मलते हुए शीत में सिसियाते बच्चे तक
'पुलिस जीप' के आसपास मँडराने लगे। वह दृश्य मेरी आँखों में आज फिर से उभर
उठा, जब महाशय जी पुलिस अधिकारियों के बीच में खड़े हो कर मुस्करा कर बातें कर
रहे थे। भय तो उनके आस-पास फटक ही नहीं सकता था। उन्हें देख कर ऐसा लग रहा था,
जैसे वह किसी शानदार दावत में जा रहे हों। पैरों में लंबे-चौड़े चमरौधे थे और
कंधों पर खादी आश्रम का मोटा खुरदरा कंबल पड़ा था। महाशय जी पुलिस की गाड़ी में सवार होने को थे कि तभी उनके अधेड़ चाचा रस्सी
में जकड़ा हुआ बिस्तर और खादी का एक झोला लिए आते दिखाई पड़े। झोले में महाशय
जी के चाचा संभवत: कुछ खाने का सामान लाए थे। महाशय जी ने अपने चाचा जी के पैर
छुए और पुलिस की गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी के पीछे खड़ी भीड़ को उन्होंने
दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार किया और 'इंकिलाब' का नारा लगाया। इसी समय पुलिस
की गाड़ी रजबाहे की पटरी पर धूल उड़ाती चल दी। इस घटना के बाद महाशय जी के जेल से छूटने और उसके बाद के राजनीतिक जीवन का
इतिहास मुझे मालूम नहीं। बड़े भाई का तबादला कहीं और हो गया और मैं भी इधर-उधर
पढ़ता रहा। उनका वास्तविक नाम वैसे कुछ और ही था। इसलिए स्वतंत्र भारत की
राजनीति से जुड़े नामों में भी उनकी तलाश संभव नहीं थी। उन्हीं महाशय जी को इतने वर्षों के अंतराल पर अपने कमरे में देख कर मैं
स्तब्ध रह गया। मुझे बहुत-सी बातें एकसाथ जानने की उत्सुकता हुई। सबसे पहले
मैंने उनके घर-परिवार के संबंध में पूछा। वे बतलाने लगे, 'चाचा को मरे हुए बहुत
वक्त बीत गया। उनके लड़के खेती-बाड़ी में लग गए हैं। मेरे हिस्से में जो जमीन
थी, उसमें से मैंने बीस बीघा ले ली थी। दस बीघा भूदान में दे दी और बाकी में एक
प्राइमरी स्कूल खोल कर अध्यापकों की रिहायश कर दी है। थोड़ी जमीन पर
साग-सब्जी हो जाती है, उसी में बच्चों के लिए एक छोटा-सा मैदान भी निकल आया
है।' मैंने अपने मन में छिपी हुई जिज्ञासा बहुत मजाकिया लहजे में व्यक्त की,
'महाशय जी! आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं? आपकी उपयोगिता तो किसी व्यापक
क्षेत्र में थी। आप देश की किसी बड़ी योजना में क्यों नहीं लगे? इतने लंबे
वक्त तक राजनीति में सक्रिय रहने के बाद आपको किसी देशव्यापी काम में लगना
चाहिए था।' महाशय जी के चेहरे पर क्षीण मुस्कान उभरी। उन्होंने व्यंग्य की शक्ल
में व्यक्त की गई मेरी जिज्ञासा को अपनी सहजता से काट दिया, 'भैया!
गाँव-देहात में भी काम की कमी तो है नहीं। कोरी, लुहार, बढ़ई और दूसरे कारीगरों
के धंधे मरते जा रहे हैं। जिसे देखो, शहरों की तरफ भागा चला जा रहा है। मैंने
ऐसा इंतजाम किया है कि स्कूल में ही तेरह-चौदह साल की उमर तक बच्चे कुछ हाथ
का काम सीख जाएँ। मैं आए दिन देखता हूँ कि किसानों के लड़के ऊँची डिग्रियाँ ले
कर गाँव में जाने से कतराते हैं और उन्हें शहर में हजार धक्के खा कर भी कोई
ढंग की नौकरी नहीं मिलती। इन हालात में असंतोष बराबर बढ़ रहा है। पढ़ाई तो वही
अच्छी है, जो साथ ही साथ रोजगार में बदल जाए। यह क्या दीक्षा हुई जो
अच्छे-खासे जवान-जहान आदमी को अपाहिज बना दे।' मुझे महाशय जी के विचार बहुत स्पष्ट और दूरगामी लगे। मुझे एहसास हुआ कि वह
राजनीति के मारक द्वंद्वों और सत्ता से बहुत दूर हैं। पद और प्रभुता का
उन्हें गुमान तक नहीं है। महाशय जी उठ कर खड़े हो गए और मेरा कंधा थपथपा कर बोले, 'अच्छा भाई! अब मैं
चलता हूँ। एक अखबार में तुम्हारा नाम और पता देखा था। बहुत दिनों से मिलने की
इच्छा थी, सो चला आया। लिख-पढ़ रहे हो यह बड़ा पुनीत कार्य है। गाँव के लोगों
के लिए भी तो कुछ लिखना चाहिए। उन सबको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। कभी जल्दी ही
अवसर निकाल कर गाँव के लोगों से मिलने आना। क्या अपना बचपन तुम्हें कभी हम
लोगों की याद नहीं दिलाता?' उनके मुँह से एक ऐसी मनुहार-भरी प्रतीक्षा की बात सुन कर मैं एकाएक संकुचित
हो उठा। मुझे हया की अनुभूति हुई कि मैंने इतने लंबे अर्से में महाशय जी के
बारे में कुछ जानने की कोशिश क्यों नहीं की! महाशय जी आज भी अपने वातावरण और
भूमि से कितने सार्थक ढंग से जुड़े हुए हैं! मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हँसते हुए बोले, 'मिलना था
सो हो गया। तुम्हें देख कर मन को बड़ा सुख मिला। अब चलता हूँ। तुम सपरिवार गाँव
आना और कुछ दिन ठहरना।' महाशय जी जाने लगे तो मैंने उनके दुर्बल शरीर को ध्यान से देखा। एक वक्त
था जब उनकी देह बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन हाँ, उनके कंधे आज भी सीधे और मजबूत
थे। गर्दन उठी हुई थी। उन्नत ललाट पर जो भी रेखाएँ थी, उनमें पूरे युग का
इतिहास अंकित था। सहसा मुझे उन अँधेरी रातों की याद आ गई, जब वीरान गलियों में महाशय जी जलती
लालटेन हाथ में उठाए निरक्षर किसानों और भूमिहीन मजदूरों को अक्षर ज्ञान देने
जाया करते थे। मुझे लगा कि महाशय जी निर्जन टापू पर अकेले हैं, लेकिन उस वीराने
को आबाद करने का संकल्प अभी भी उनके साथ है। बेहतर लड़का तलाश करते-करते बहन पच्चीस पार कर गई, तो मैंने गाँव-जवार की
तरफ जाना ही छोड़ दिया। पिता जी ने कस्बे के एक परिचित व्यक्ति के माध्यम से
आढ़त पर काम करने वाले एक दुहेजू मुनीम को वर के रूप में तलाश कर लिया और मुझे
कई बार खत लिखा कि मैं 'लड़के' को एक बार देख जरूर लूँ। मगर मेरे लिए यह एक
दुखदायी स्थिति थी। मैं स्वयं एम.ए. पास था; बहन भी थोड़ा-बहुत पढ़ चुकी थी,
लेकिन वह मुनीम मुंडी हिंदी की मामूली समझ से अपनी गाड़ी घसीट रहा था। उस आदमी
को अपने बहनोई के रूप में देखना मेरे लिए मरण स्वीकार करने के समान था। मैंने इस संबंध में दूर तक सोचा और बहन के लिए कोई अच्छा वर खोजने के बारे
में विचार करने लगा। मुझे 'अपनी आवाज' साप्ताहिक में काम करते हुए लगभग दो माह
हो चुके थे, मगर अपने साथ काम करने वाले सहसंपादकों-उपसंपादकों के बारे में
मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उन चार-छह लोगों में अवस्थी ही कुछ कम उम्र का
लगता था जो शायद अविवाहित है। बाकी तो सब उम्रदराज और खुर्राट मालूम पड़ते थे। अगले दिन दफ्तर पहुँच कर मैंने अवस्थी को परोक्ष में टटोला, 'अवस्थी जी,
क्या आप यहीं के रहनेवाले हैं?' उसने मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। वह दार्शनिक लहजे में बोला, 'अब
तो मैं कहीं का रहनेवाला नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस देश का
रहनेवाला है। अपने 'स्वाइल' (जमीन) से यहाँ जुड़ा ही कौन है? बेवजह जब कोई फलसफा बघारने लगता है, तो मैं घबरा उठता हूँ। वह आदमी मुझे
पागलपन के निकट पहुँचा हुआ लगने लगता है। मैंने अपना मंतव्य दूसरे ढंग से
प्रकट किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो महज यह जानना था कि वह कुँवारा है अथवा
विवाहित । मैंने कहा, 'भाई-जान, आप सोचते बहुत हैं। घर बसा कर आराम से रहोगे,
तो यह बड़े-बड़े सवाल आपके दिमाग को खराब नहीं करेंगे। शादीशुदा आदमी के पास
फजूल की खुराफात पंख भी नहीं फड़फड़ा सकती।' अवस्थी मेरी सलाह पर ठठा कर हँस पड़ा। उसने मुझसे ही उल्टे पूछ लिया,
'अच्छा यह बात है? तब तो आप बड़े सुखी होगे, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी हुए?
आपको इतना संयत देख कर तो यही लगता है कि आप बाल-बच्चेदार और खासे दुनियादार
सयाने हैं।' मैंने बात को खत्म करने के इरादे से कहा, 'भाई, मुझे इस दिशा में सोचने का
अभी अवसर ही नहीं मिला।' मेरा उत्तर सुन कर वह बेनियाजी से हँसा, 'अरे यह तो गजब हो जाएगा, शर्मा जी!
तब तो दुनिया जहान के बड़े-बड़े सवाल आपके दिमाग को किसी काम का नहीं छोड़ेंगे।
मेरी शुभकामना लीजिए और आप यह मांगलिक कार्य तत्काल संपन्न कर डालिए। और कुछ
न सही, बैठे-ठाले शादी ही सही।' चूँकि सही स्थिति का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैंने मजाक का लहजा
पैदा किया, 'यार अवस्थी, कुछ क्रांति तो होनी ही चाहिए। हम लोग और कोई बड़ा काम
नहीं कर सकते, तो क्या विवाह भी नहीं कर सकते?' 'जरूर कर सकते हैं। मगर अपना नहीं, आपका। मैं तो इस तोंक में अपनी गर्दन
पहले ही फँसा चुका हूँ।' अवस्थी की इस सूचना ने मेरी आशा को एक ही झटके में
तोड़ डाला। मैंने उस बात को झटकते हुए कहा, 'मगर कमाल यह है कि एक शादीशुदा आदमी हो कर
भी तुम महीन बातें करते हो, दाल-रोटी के चक्कर ने अभी तुम्हें गुमराह नहीं
किया है शायद?' मेरी बात सुन कर वह यकायक गंभीर हो गया और उसकी आँखें कहीं दूर चली गई। उसने
कहना आरंभ किया, 'तुमने कभी यह भी सोचा है कि सोचना कितना अजीब रोग है? मेरा
सारा तखमीना ही गलत हो गया। मैं इस सड़ी-गली लाश की मानिंद जिंदगी को बगैर
जरूरत ढोता घूम रहा हूँ। आपको शायद मालूम नहीं, मैं बहुत दिनों से कविता लिखता
चला आ रहा हूँ। मैंने हमेशा यही चाहा कि समर्पित हो कर लिखूँ, मगर होता हमेशा
उल्टा है। यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है कि आप कुछ करने के लिए गंभीर हों,
पर आपको करने के लिए जो काम मिले, उसकी सिर्फ 'नेगेटिव वैल्यू' हो। इस 'डबल
रोल' में आदमी मारा जाता है। इसमें न तो वह साधारण दुनियादार बन कर सामान्य
जीवन में लिप्त हो पाता है और न वह स्वयं में इतनी महानता ला पाता है कि शिखर
पर पहुँच जाए। मेरे दोस्त! शायद तुम नहीं जानते, दोनों तरफ से निर्वासित होना
कितना भयानक है। इसीको मोटे शब्दों में कहा जाता है 'न खुदा ही मिला ना विसाले
सनम।' मैं अवस्थी के घोर आत्मालाप से सिहर उठा। वह धाराप्रवाह बोले चला जा रहा
था, 'जिस आपाधापी में दिन कट रहे हैं, उसमें मुझे अपनी पत्नी और बच्चा परम
शत्रु दिखलाई पड़ते हैं। मैं इतनी कम उम्र में भी सिर उठा कर नहीं चल सकता।
स्वामी रामतीर्थ के इस कथन पर भी कभी-कभी मुझे संदेह होता है कि बचपन और जवानी
पार किए बिना किसी को बुढ़ापा नहीं आ सकता। मुझे देखो। रामतीर्थ मेरे सामने
होते, तो मैं उनसे पूछता, 'मेरा बचपन कहाँ गया? मैं जवान कब हुआ? मैं तो चिर
बूढ़ा ही इस संसार में आया हूँ, स्वामी जी महाराज ।' मैं ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। मुझ पर जादू का-सा असर होने लगा था।
वह कहे जा रहा था, 'इतनी थोड़ी उम्र में मैं सिर उठा कर नहीं चल सकता। इस संसार
में सुख-समृद्धि और लाखों नियामतें हैं। लेकिन वे मेरे-तुम्हारे लिए नहीं हैं।
पता नहीं यह कैसा षड्यंत्र है कि आदमी अपने-आपसे ही बेगाना होता चला जाता है।'
सहसा अवस्थी ने मुझसे सवाल किया, 'क्या आप बतला सकते हैं कि मैं जीवित क्यों
हूँ?' उसके सवाल से मैं भीतर तक दहल गया। मुझसे कोई उत्तर देते न बन पड़ा। मैंने
अवस्थी को प्राय: शांत और संयत देखा था, पर आज उसके सारे व्यक्तित्व पर
विचित्र आक्रोश छाया था। वह सरगोशी में बुदबुदाने लगा, 'यहाँ कुछ नहीं हो सकता।
यह वह पिंजड़ा है, जिसमें घुट कर मर जाने के सिवा कुछ नहीं होगा।' थोड़ी देर बाद उसकी बड़बड़ाहट खामोशी में बदल गई और उसका सिर मेज पर झुक
गया। शायद वह अखबार के लिए कोई लेख लिखने में जुट गया था। अवस्थी फिर उस दिन गंभीर ही बना रहा। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। अक्सर
मैं पाँच बजते ही दफ्तर छोड़ कर चला जाता था, लेकिन उस दिन मैं अँधेरा घिर आने
पर भी बैठा रहा। जब अवस्थी अपने कागज समेट कर मेज की दराज में डाल कर उठा और
खूँटी से किरमिच का बैग उतार कर कमरे से बाहर जाने लगा, तो मैं भी उसके साथ लग
लिया। बस स्टाप पर पहुँच कर मैंने उससे कहा, 'अगर तुम्हें एतराज न हो तो मैं
तुम्हारे घर चलूँ। मैं शहर में अकेला रहता हूँ। पता नहीं, आज घर की मुझे
क्यों याद आ रही। तुम्हारे घर एक प्याला चाय पी कर लौट आऊँगा।' अवस्थी ने ध्यान से मेरा चेहरा देखा और बोला, 'आपको अपने साथ ले जाने में
मुझे संकोच नहीं है, लेकिन मैं किसी अच्छी बस्ती में नहीं रहता। वहाँ का
माहौल इतना गलीज और सड़ांध-भरा है कि आपको कोई खुशी मयस्सर नहीं होगी। और सीमा
यही नहीं है। विडंबना यह भी है कि मेरे पास रहने की अपनी कोई जगह नहीं है। मैं
अपने एक 'पेंटर' दोस्त के साथ रहता हूँ। उसके पास 'अनआथराइज्ड' कालोनी में एक
टूटा-फूटा कमरा और लकड़ी का खोखा है। वह हमेशा बीमार रहता हैं, लेकिन दिल का
बहुत नेक है। अगर आप इतने पर भी चलना चाहें, तो आपका हार्दिक स्वागत है।' थोड़ी देर बाद उस इलाके की तरफ जाने वाली बस आई और मैं भीड़-भड़क्के के
रेले में बस के भीतर पहुँच गया। अवस्थी और मैं बमुश्किल एक पैर पर ही
खड़े-खड़े गंतव्य तक पहुँचे। शहर के गुंजान इलाके से निकल कर बस एक लंबे पुल को पार करके कहीं ठहर गई।
अवस्थी ने मुझसे उतरने को कहा और आगे बढ़ गया। एक नाला पार करके हम लोग एक बीहड़-सी बस्ती में पहुँच गए। उस तरफ ज्यादातर
मेहनत-मजदूरी करनेवाले लोग ही रहते थे। कुछ मिस्कीन किस्म के बाबू टाइप भी
इधर-उधर आते-जाते नजर आ रहे थे। नाले के समानांतर यह बस्ती काफी आगे तक फैली
हुई थी। वहाँ गंदगी और फूहड़पन की कोई सीमा नहीं थी। झोंपड़ीनुमा कच्चे मकान
एक-दूसरे से सटे हुए थे। गलियों में गंदा पानी बह रहा था और जगह-ब-जगह कचरे के
ढेर लगे हुए थे। मुझे यह देख कर अजहद तकलीफ हुई कि अवस्थी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ
इतनी गंदगी में रहता था। गहरा अँधेरा घिर आया था। गलियों में प्रकाश की कोई
व्यवस्था नहीं थी। कहीं कहीं ढिबरी या लालटेन जलती नजर आ जाती थी और
इक्का-दुक्का आदमी गली में ही आग जलाए बैठे बतिया रहे थे। गलियों में
नंग-धड़ंग बच्चे गोल बाँधे ऊधम मचा रहे थे। मैंने अवस्थी से पूछा, 'ये बच्चे
स्कूल नहीं जाते?' अवस्थी मेरे अज्ञान पर विद्रूप से मुस्कराया होगा। अँधेरे में उसका चेहरा
मुझे नहीं दिखा, लेकिन उसके स्वर में गहरा उपहास था। यह बोला, 'शर्मा साहेब!
आप समझते हैं, ये बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएँगे? इनमें से कुछ जेबकतरे बनेंगे।
कुछ जूतों पर पालिश करेंगे। और जिन्हें हम जोर-जबरदस्ती धकिया कर स्कूल
भेजेंगे, बहुत होगा, तो एक-दो किसी दफ्तर में चपरासी लग जाएँगे।' बातें करते-करते मैं और अवस्थी एक तंग-सी गली में पहुँच गए। गली के अंत में
लोहे की जंग खाई चादरें, लकड़ी के फट्टे और पुराने सड़े-गले टाट को जोड़ कर एक
खोखा खड़ा किया गया था - जिसमें से धुएँ का गुबार फूट कर बाहर निकल रहा था।
सारे माहौल में धुआँ, प्याज-लहसुन और जलते तेल की गंध भरी थी। इधर-उधर से
तरह-तरह की आवाजें उठ कर कानों से टकरा रही थीं। अवस्थी उस खोखे के सामने जा कर एक क्षण के लिए ठिठक कर खड़ा रहा और फिर
बोला 'शर्मा भाई, यही है अपना आशियाना।' अपना वाक्य समाप्त करके उसने लकड़ी
का दरवाजा हल्के से हिलाया जो तत्काल खुल गया। अंदर घुसते हुए अवस्थी बोला,
'अब आ ही गए हो, तो अंदर भी आ जाओ।' मैं चुपचाप अवस्थी के पीछे हो लिया। उस खोखे में इधर-उधर अंगड़-खंगड़ सामान
बिखरा पड़ा था। लकड़ी के चौकोर फ्रेमों पर टाट और मारकीन जड़ा हुआ था। दो-तीन
जंग खाई तामचीनी की प्लेटें और ब्रुश इधर-उधर पड़े थे। रंगों के डिब्बे यों
ही अलट-पलट पड़े थे। पूरी दीवारों को क्रास करती हुई सन की रस्सियाँ बँधी हुई
थीं, जिनपर मैले-कुचैले तहमद और बनियान वगैरह झूल रहे थे। अवस्थी उस स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं ठहरा। वह आगे बढ़ गया। आगे जा कर
एक तंग-सा सहन था, जिसमें पत्थर के कोयलों की अँगीठी धुआँ दे रही थी और एक
महिला जमीन तक झुक कर उसे दहकाने की कोशिश कर रही थी। मेरी और अवस्थी की पदचाप सुन कर वह महिला उठ खड़ी हुई। मैंने अँगीठी से
उठते प्रकाश में देखा, एक निहायत पतली-दुबली गोरे रंग और तीखे नाक-नक्श वाली
लड़की मैली चीकट धोती में लिपटी खड़ी है। कभी उसका रंग खूब गोरा रहा होगा,
लेकिन लाल रोशनी के बावजूद उसका चेहरा खून की कमी से सफेद नजर आ रहा था। जो
कष्ट उसे इस माहौल में मिले थे, सारे उसके व्यक्तित्व पर नक्श हुए लगते थे।
दुबलेपन के कारण वह अपनी उम्र से कहीं छोटी, महज एक बच्ची जैसी दिखाई पड़ रही
थी। अवस्थी के साथ मुझे देख कर वह संकोच में पड़ गई। अगर उस मकान में किसी
अन्य मार्ग से पहुँचना संभव हुआ होता, तो शायद अवस्थी मुझे सहन में लाता ही
नहीं, पर दुर्भाग्य से कहीं टिक सकने के स्थान पर हम अभी तक भी नहीं पहुँचे
थे। अवस्थी ने उसके संकोच को अनदेखा करके कहा, 'मेरे साथ दफ्तर में काम करते
हैं। शर्मा जी हैं। यहीं खाना खाएँगे। अँगीठी बाद में जलती रहेगी। तुम
बत्तीवाला स्टोव जला कर पहले दो प्याली चाय बना डालो।' और सहसा जैसे उसे कुछ
याद आ गया, 'माइकेल अंकल किधर है?' 'अंकल बीरू को साथ ले कर सब्जी लेने गए हैं। बस, आते होंगे।' 'ठीक है, तब चाय बनाओ,' कह कर अवस्थी दूसरी तरफ एक कोठरी में चला गया। शायद
यही वह कोठरी थी जिसका एक भाग टूटा हुआ था और सहन में लकड़ी के दो खंभों पर
'टिनशेड' डाल कर सोने की व्यवस्था की गई थी। अपना किरमिच वाला थैला कोठरी में रख कर अवस्थी मेरे पास लौट आया और दीवार
के सहारे खड़ी चारपाई को बिछाते हुए बोला, 'चलो, आपकी यहाँ आने की तमन्ना पूरी
हो गई। जिस जगह आप आए हैं यह बस्ती बड़े शहर का कोढ़ है। जितने नाजायज धंधे हो
सकते हैं, वे सब यहाँ मौजूद हैं। दुनिया का कोई भी श्रेष्ठ उद्देश्य यहाँ
रहनेवालों के लिए नहीं बना। कोई भी उच्च प्रेरणा यहाँ निष्फल है। गांधी जी
गरीब हरिजनों की बस्ती में जा कर रहे, लेकिन क्या इन बस्तियों का वास्तव में
कभी सुधार हो पाया? यहाँ रहनेवालों की जिंदगी जानवरों से भी गई-बीती है।' अपनी
बात कहते-कहते अवस्थी ठहर गया ओर घृणापूर्वक हँस कर बोला, 'और मजे की बात यह
है कि मुझे यहीं ठिकाना मिला है। मैं पत्रकारिता करता हूँ। भाड़े पर तीन कौड़ी
के सड़े हुए राजनीतिक लेख लिखता हूँ।' अवस्थी का आवेश सहसा दुख में बदल गया और
उसके चेहरे को एक निरीह विवशता ने घेर लिया। अवस्थी की पत्नी चाय तैयार करके ले आई और स्टूल डाल कर चाय के प्याले हम
दोनों के सामने रख दिए। हैंडिल उखड़े प्याले ही उठा कर अवस्थी बोला, 'शर्मा
जी, मैं अपने साथ दफ्तर के किसी आदमी को आज तक यहाँ ले कर नहीं आया। आप पहले
व्यक्ति हैं जिसके आग्रह को मैं टाल नहीं पाया।' मैंने लापरवाही दिखाते हुए कहा, 'जो भी हालात हैं, उनसे मुँह चुराने का सवाल
ही नहीं उठता। हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। आप मुझे अपने से बेहतर न समझें।
मैं जिस जगह रहता हूँ, वह भी कोई खास अच्छी नहीं है।' इसी समय खोखे का दरवाजा खड़खड़ाया और एक अधेड़ आदमी ढाई-तीन साल के बच्चे
को गोद में उठाए सहन में दाखिल हुआ। काले रंग का वह आदमी चारखाने का तहमद लपेटे
था और बदन पर उसका ढीला बनियान काफी नीचे तक लटक रहा था। उसे देखते ही अवस्थी
बोला, 'मैं आज अपने दोस्त शर्मा साहब को आपसे मिलाने लाया हूँ।' बच्चे को सँभाले वह शख्स मेरी तरफ बढ़ आया और सब्जी के थैले को जमीन पर
टिका कर वोला, 'गुड ईवनिंग सर! हमारी खुशकिस्मती है जनाब, कि आप तशरीफ लाए।' मैं चारपाई छोड़ कर उठ खड़ा हुआ। मैंने माइकेल से हाथ मिला कर प्रसन्नता
अनुभव की और बोला, 'अवस्थी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं।' माइकेल बोला, 'मैं किस काबिल हूँ साहब।' इसके बाद वह अवस्थी से बोला,
'डाक्टर बोलता है, बाबा के गले में गिल्टियाँ उभर रही हैं। इन्जेक्शन भी
लगेंगे और खाने की दवाइयाँ भी देनी पड़ेंगी।' अब मैंने बच्चे की तरफ गौर किया। माइकेल ने उसे गोद से उतार-कर जमीन पर
खड़ा कर दिया था। वह अजहद सूखा हुआ लंबा-लंबा नजर आ रहा था। उसकी शक्ल-सूरत
अच्छी-खासी थी, मगर चेहरे पर सिर्फ आँखें ही आँखें दिखलाई पड़ती थीं। माइकेल की इस सूचना पर कहीं कोई सिहरन नहीं उभरी। अवस्थी की पत्नी सिर
झुकाए थैले से सब्जी निकालती रही। अवस्थी भी चुपचाप चाय पीता रहा। मुझे लगा,
इस घर के प्राणी शायद बुरी से बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हैं। अब तक अँगीठी दहक उठी थी। उसकी लपटें दीवारों पर अजीबो-गरीब परछाइयाँ बना
रही थीं। माइकेल ने उस तंग से सहन में इधर-उधर घूमना शुरू कर दिया। उस घर में
इस समय पाँच जीवित प्राणी मौजूद थे, लेकिन कोई भी किसी से बातें नहीं कर रहा
था। जीवन की शिराओं में बजने वाला मादक संगीत इस घर की आत्मा से निकल गई थी।
गुनगुनाने की उम्र उदासी में कट रही थी। पता नहीं, हम किसके लिए जी रहे थे;
हमारा संघर्ष किसके लिए था? माइकेल ने जिस बच्चे को अभी थोड़ी देर पहले सीने
से लगा रखा था, वह उसका खून नहीं था, लेकिन अवस्थी के बच्चे की बीमारी उसके
भीतर तक उतर गई थी। लगता था उतावली में इधर-उधर चक्कर काटता माइकेल बच्चे के
बारे में सोच रहा था। शायद हम सब लोग परस्पर बातें कर रहे थे, पर वह भाषा
किताबी ज्ञान से एकदम अलग थी। उस मर्म को समझना और समझाना कठिन था। इसी समय मैंने नोट किया, माइकेल टहलते हुए ठहर गया था और बच्चे के सीने के
सामने उँगलियों से क्रास का संकेत कर रहा था। मुझे अजीब-सी बेचैनी ने घेर लिया था। सहसा मैं चारपाई से उठ कर खड़ा हो गया
और बोला, 'अवस्थी भाई! अब मैं चलूँगा। आपका ठिकाना तो मैंने देख ही लिया है।
जल्दी ही फिर कभी आऊँगा।' मेरी बात से अवस्थी की तंद्रा भंग हो गई। बोला, 'कहाँ जा रहे हो? खाना खा
कर जाना।' 'नहीं, आज नहीं। फिर कभी छुट्टी के दिन आऊँगा। तभी खाना खाऊँगा।' मैंने
जल्दबाजी में कहा। इसके बाद अवस्थी ने विशेष आग्रह नहीं किया। मैं तेजी से मकान के बाहर निकल
कर गली में पहुँच गया। गली में आगे जा कर लालटेन की रोशनी नजर आई। एक औरत कर्कश
स्वर में चीख रही थी, 'मैं दाढ़ीजार से पहले ही कहती थी... को...कोठरी किराए
पर मत दे। यहाँ किसी का धर्म-ईमान नहीं है। छोरा के सहारे बुढ़ापा कट जाता। पर
तू कहाँ माने था। ले गई अब तेरे सुग्गा को उड़ा के - बैठा बंसरी बजा।' भीड़ में से कोई चटखारा ले कर बोला, 'अरे ठगनी नार का क्या भरोसा। चार दिन
में तेरे छोरा कू भी धक्का दे जाएगी, क्यूँ परेसान हौवे है?' मैंने गली से बाहर निकलते हुए घरघराते कंठ वाले एक बुड्ढे की मरियल-सी आवाज
सुनी, जो अपनी पत्नी और भीड़ को सफाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि कोई औरत
बुड्ढे-बुढ़िया के बेटे को ले कर चंपत हो गई थी और वह आपस में एक-दूसरे को इसके
लिए अपराधी घोषित कर रहे थे। मैं चीख-पुकार-भरे उस वातावरण से बाहर आया, तो मुझे अवस्थी और उसके परिवार
की दुर्दशा याद आने लगी। एक शाम किसी के साथ अच्छे ढंग से बिताने आया था,
लेकिन हुआ उसका एकदम उल्टा। मन सहसा इतना भारी हो गया कि पैरों में गहरी थकान
महसूस होने लगी। पुल पार करके मैं एक चाय की दुकान पर बैठ गया, कोई बस आए तो आगे बढ़ूँ। मैं भ्रांत हो कर इधर-उधर घूमता रहा हूँ। जिस किसी से मिलता हूँ, वह बहुत
मीठा व्यवहार करता है। सौंदर्यकला, साहित्य पर देर तक बौद्धिक चर्चा करता है
और चाय-सिगरेट से खातिर करता है। मगर यह सौहार्द कुछ घंटों तक ही सीमित होता
है। जब मैं ऐसे किसी बड़े भारी विद्वान, दिग्गज पुरुष के पास से उठ कर बाहर आता
हूँ तो सोचने लगता हूँ कि उसमें कितनी नफासत है, वह कितने अच्छे ढंग से रहता
है, वह कितना अध्ययन करता है और... हाँ, उसका ड्राइंगरूम कितना सुसज्जित है।
उसकी लाइब्रेरी भी तो कीमती किताबों से भरी हुई है। ओह! कितना सुरुचि-संपन्न
है! उसकी खुशी से चमकती हुई आँखें, उसकी सुजनता मिलनेवालों पर अमिट छाप छोड़ती
है। बँगले, कोठी या आलीशान अंग्रेजी नामधारी 'विला' से बाहर निकल कर सड़क पर मैं
बदहवास हो कर ऊँची-ऊँची दुकानों को देखता सड़क की भीड़ में खोया चलता हूँ और यो
ही न जाने कब तक चलता रहता हूँ और फिर एकाएक मेरे मस्तिष्क में एक फूहड़ विचार
बिजली की तरह कौंधता है - मैं अपने से पूछने लगता हूँ कि ये उपलब्धियाँ आखिर
कैसे संभव हुई? मैंने इतना पढ़ा-लिखा और मेरे सोचने और बातें करने का ढंग भी
वही है जो मेरे आधे घंटे के पहले मेजबान का था, मगर संसार में बिल्कुल नि:संग
और अनपेक्षित हूँ। मैं एक कोठरी तक नहीं जुटा पाया। विशाल बँगले और कोठी की
बातों का तो कहना ही क्या... मेरे कमरे में शायद एक मोमबत्ती या लालटेन भी
तभी होती है जब मैं किसी दूसरे के कमरे का साझीदार हो कर रहता हूँ (कहना न होगा
कि उस कमरे का मालिक वही दूसरा साझीदार होता है और वह दयावश या मेरे मित्र होने
के प्रायश्चितस्वरूप मुझे अपने साथ रहने देता है।) फिर मेरे दिमाग में उन महानुभावों की तस्वीरें उभर उठती है जो कल्पना के
लोक में डूबते-उतराते 'यूटोपिया' बघारते है, गर्म बहसों में मशगूल होते हैं और
मझे बिल्कुल भूल जाते हैं उनमें से किसी नए व्यक्ति से यदि संयोग से कोई
मेरा परिचय कराता है तो वह अपने चश्मे से घूर कर एक क्षण देखते रहते हैं और
चेहरे पर भरसक बनावटी मुस्कान ला कर कहते हैं, 'हें-हें-हें, आप हैं... मैंने
आपका नाम कहीं देखा तो था... (मैं जानता हूँ कि वह सरासर झूठ बोलते हैं,
क्योंकि मेरा नाम अखबारों में तभी छपा था जब मैंने एक के बाद एक कई परीक्षाएँ
पास की थीं)। इतना कहने से उनका दायित्व समाप्त हो जाता है। मुझे उनके चेहरे
से लगता है कि उन्हें मुझसे परिचय करके ग्लानि हुई है। उन्होंने शायद
अनधिकृत व्यक्तित्व को पहचानने का सुमेरु-भार उठाया है। शायद इसीलिए वह अपने
ऊपर से उस अप्रिय परिचित भार को उतार फेंकने के लिए फौरन सिगरेट-केस निकाल कर
सिगरेट सुलगा लेते हैं और फिर उन्हें कुछ शायद याद आता है तो सिगरेट-केस बढ़ा
कर पूछ लेते हैं, 'आप सिगरेट तो पीते ही होंगे?' फिर उनके स्वर से ही एक
स्वचालित क्रिया मुझमें होती है। अभी तो उनके स्वर के संयम और काठिन्य का
अनुभव करके मैं संकुचित हो कर हाथ जोड़ देता हूँ और कभी बहुत लज्जित-सा हो कर,
गर्दन झुका कर सिगरेट-केस से काँपते हाथों से एक सिगरेट निकाल लेता हूँ। ऐसी
अवज्ञा पर मुझे बड़ी आत्म-ग्लानि होती है और मैं सोचता हूँ, काश, मैं, यहाँ न
होता। फिर मैं अपनी दोनों हथेलियों को फैला कर देखता हूँ, मानो अपनी
भाग्यरेखाओं की परीक्षा कर रहा हूँ। मेरे हाथ बुरी तरह पसीजे हुए होते हैं।
मैं लोगों की चर्चा में योगदान देना चाहता हूँ मगर मेरा गला फँस-सा जाता है और
मुझे अपना स्वर बड़ा असंयत और अस्वाभाविक-सा लगता है। जब मैं बिल्कुल मूक
रहता हूँ तो लोग मुझसे भी पूछ लेते हैं कि मेरा क्या विचार है (यद्यपि ऐसा कम
ही होता है)। मैं जो कुछ कहता हूँ (मैं आज तक नहीं जान पाया कि ऐसे अवसर पर मैं
क्या कहता हूँ) वह इतना प्रभावहीन और व्यर्थ होता है कि सब लोग शालीनता के
कारण सुनते तो जरूर रहते हैं किन्तु अंत में एक-दूसरे की ओर इस दृष्टि से देखते
हैं कि आखिर कहा क्या गया है? हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मैं सड़क पर चलता होता हूँ तो बहुत ही चकित हो
कर कुछ सोचता और विस्फारित आँखों से देखता हूँ कि लंबी-चौड़ी सड़क के दोनों ओर
ये कई-कई मंजिलों के विशाल भवन कैसे बन गए है? मीलों तक चले गए इन भवनों का
निर्माण क्या कोई दानव एकाएक किसी रात में सबकी दृष्टि बचा कर जादुई प्रताप से
कर गया है और इन दुकानों में भरा हुआ विपुल सामान और इतना आडंबर और समारोह
किसके लिए हो रहा है? मैं सोचता हूँ... सच तो यह है कि मैं कुछ नहीं सोचता, मैं
केवल प्रिमिटिव होता जा रहा हूँ और सभ्यता के गतिचक्र को उल्टा घुमाना चाहता
हूँ। ट्रांजिस्टरों और माइक्रोफोन की कानफोड़ आवाजों से सारी फिजा भर जाती है।
ऐसे शोर में मन थोड़ी देर के लिए भीतर के कोलाहल से मुक्त हो जाता है और आँखें
चकित हो कर चारों ओर फैले अपरिचित लोक को देखती रहती हैं। विचित्र-विचित्र
प्रसाधनों और परिवेशों से लैस हो कर बूढ़े-बच्चे, युवक और युवतियाँ जाने कितनी
बातें उच्छ्वसित और उमंग में तरंगायित हो कर कहते चले जाते हैं। मगर मेरी समझ
में यह व्यापार जरा भी नहीं आता। मैं तमाशवीन हो कर मूढ़ की भाँति देखता रहता
हूँ। और जब मुझे अपना ध्यान होता है तो मैं आबादी से बिल्कुल बाहर पहुँच गया
होता हूँ, किन्तु असंख्य चेहरे, भीमाकार इमारतें और अस्फुट ध्वनियाँ अब
मुझे चारों ओर से दिखाई और सुनाई पड़ती रहती हैं। कहीं वीराने में या किसी पार्क की खाली बेंच या लान पर बैठ कर मैं सोचने
लगता हूँ कि इस समस्त व्यापार में मैं कहाँ हूँ। मैं प्रत्येक देश के विचारक
और लेखक के गहरे से गहरे मजाक और गहरी से गहरी संवेदना को अनायास ही समझ लेता
हूँ मगर यह चारों ओर फैला व्यापार - जिसमें शायद सोचने-समझने को बहुत अधिक
नहीं है - मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पाता। कितने ही वर्ष हो गए जब मैं करोड़ों
और लाखों रुपयों के हिसाब कक्षा में बैठ कर लगाया करता था; साझेदारी के वे सवाल
मैं बात की बात में हल कर दिया करता था। मगर आज तक अपने समस्त प्रयत्नों के
बावजूद कभी दस रुपए एकत्रित करके जेब में नहीं रख पाया। उधार माँग कर किताबें
पढ़ता हूँ, मित्रों की कलम से लिखता-पढ़ता हूँ और जब डाक का खर्च न जुटा सकने
के कारण किसी कहानी या उपन्यास की पांडुलिपि किसी प्रकाशक के पास ले कर
पहुँचता हूँ तो वह उसको देखने कि कौन कहे, देर तक तो वह मेरी ओर भी आँखें नहीं
उठाता और मेज पर फैले कागजों में अत्यधिक व्यस्त होने का नाटक रचता है। आखिर
कभी तो मेरी ओर देखना ही पड़ता है। ऐसे अवसर पर वह अत्यंत व्यावहरिक और
'पेटेंट' वाक्य दुहराता है, 'कहिए! आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बंधु?' मैं
बहुत ही क्षीण स्वर में उससे अपनी बात कहता हूँ। अपनी बात कहते-कहते मुझे
पसीना आ जाता है और ऐसी दुर्बलता महसूस होती है कि मैं मेज या कुर्सी का सहारा
ले लेता हूँ और जैसे-तैसे अस्फुट स्वरों में अपनी बात पूरी करता हूँ।(एक बार
तो ऐसे ही एक प्रकाशक महोदय की गोल मेज मेरी कँपकँपी से उलटते-उलटते रह गई।)
खैर, वह ध्यान से मेरी बातें सुनता है और फिर मेज पर बिखरे कागजों पर झुक जाता
है। न जाने क्या सोच कर फिर सिर ऊपर उठाता है और दीवार पर टँगे कैलेंडर पर यों
ही कहीं शून्य में दृष्टि केंद्रित कर लेता है। एक हाथ में खुला कलम ले कर तथा
दूसरे हाथ के नाखून को दाँतों से कुतरता हुआ कहता है, 'हम नए लेखकों की रचनाएँ
नहीं छापते।' बड़े-बड़े दो-चार नाम गिना कर कहता है, 'बुरा न मानना, आजकल तो हर
तीसरे आदमी ने लिखने का धंधा पकड़ लिया है...' लेक्चर यहीं खत्म नहीं होता,
मगर इससे अधिक मैं कुछ नहीं सुन पाता। मैं दूर कहीं खो जाता हूँ और अनायास
कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। एकाध टूटा फिकरा सुनाई पड़ जाता है, मसलन, 'लिखे जाओ,
लिखे जाओ...' या 'नए लेखकों का कोई गिल्ड होना चाहिए।' इतना कहते-कहते शायद उसकी अंतरात्मा करवट बदलती है और वह अपने खद्दर के खूब
श्वेत लिबास की ओर देख कर सोचता है कि उसने हिंसा कर दी है; वह चाहे शब्दों
द्वारा ही क्यों न हुई हो। वह पश्चाताप के स्वर में कहता है,
'स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करना मित्र! मेरी बात को अन्यथा न लेना। आप शायद
समझते नहीं होंगे, प्रकाशन का काम कितने रिस्क और जिम्मेदारी का है।' और शायद
यह काफी होता है। आगे इसलिए वह मुझ पर दृष्टि डालना जरूरी नहीं समझता। मेज पर
फैली फाइलों को पढ़ने में जुट जाता है या किसी को आवाज दे कर व्यस्तता से
बुलाने लगता है। इसका स्पष्ट ही यह अर्थ होता है - दूसरा दरवाजा देखो।
कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ है कि पुराने प्रकाशकों से एकदम निराश हो कर मैं कुछ नए
प्रकाशकों के पास पांडुलिपियाँ ले कर गया हूँ। मगर उन्होंने वर्ष-छह मास
उन्हें अपने पास पड़े रहने दे कर अंत में सधन्यवाद वापस कर दिया है। जाहिर है
कि उन्होंने पांडुलिपि को देखा तक नहीं होगा, क्योंकि पांडुलिपि वापस करने के
लिए भी उन्होंने मुझे कई-कई दिनों तक हैरान किया है। वह यह तक भूल गए होते हैं
कि वह पांडुलिपि कहाँ रख दी गई है और एक प्रकाशक ने तो यहाँ तक सदाशयता बरती कि
अनेक बार अपने यहाँ चक्कर कटवाए लेकिन मेरी 'बकवास' का कोई पता-ठिकाना नहीं
मिला और अंत में निराश हो कर मैंने उनके यहाँ जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि इस
बार-बार के अयाचित प्रवेश से वह तंग आ गए थे और उन्होंने अपने चढ़े हुए मुँह
पर यह 'नोटिस' लगा दिया था, 'ऐसी कौन-सी अमर रचना थी जिसके खो जाने से
विश्व-साहित्य किसी अमूल्य कृतित्व से वंचित रह जाएगा। अरे साहब! ऐसा
'कूड़ा' हमारे पास हर रोज ढेर-सी तादाद में आता है। हम उसे कहाँ तक साज-सँभाल
कर रखें। एक कहावत है - सच्चे को इतनी दफा झूठा कहो कि अंत में वह स्वयं को झूठा ही
समझने लगे। इसमें कुछ सच्चाई हो या न हो मगर अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है
कि वास्तव में मैं व्यर्थ ही प्रयास करता हूँ। कोई न कोई धोखा आदमी अपने साथ
निरंतर रचता ही रहता है तभी तो मैं भी स्वयं को किसी न किसी धोखे से बहला ही
देता हूँ। मैं कहता हूँ, मुझमें जरूर कुछ है वर्ना ऐसा कई बार क्यों होता है
कि महानतम विचारकों, कवियों और साहित्यकारों से मेरे विचार आश्चर्यजनक रूप से
सादृश्यमूलक होते हैं। मसलन मैंने कोई विश्लेषण या चित्रण आज किया है - उसी
चित्रण को किसी नए उपन्यास में देखता हूँ तो मेरे मन में सहसा एक हूक-सी उठती
है और साथ ही एक आशा भी करवट लेती है और मैं अपने-आपसे कहने लगता हूँ, यदि मुझे
अवसर मिलता तो क्या मैं इस बहुविज्ञापित रचना से पहले ही प्रकट न हो गया होता। अभी उस दिन कई प्रबुद्धचेता बातें कर रहे थे। एक अत्यंत थुलथुल सज्जन,
दुग्धश्वेत वस्त्र पहने, मुँह में पान के दो बीड़े कचरते और निर्द्वंद्व हो
कर सिगरेट का धुआँ फेंकते हुए बोले, 'आह! असफलताओं का इतिहास भी कितना
मर्मस्पर्शी होता है। विश्व में सफलता प्राप्त करने वालों के मुकाबिले में
मुझे हमेशा वही लोग न जाने क्यों अच्छे लगते हैं जो सारी योग्यता और जीनियस
के बावजूद ठोकर खाते मर गए हैं।' मेरा अंतर्मन एक अव्यक्त पीड़ा से झनझना
उठा। मैंने चाहा कि इस मिथ्यावादी के मुँह पर कस कर चपत जड़ दूँ। यह स्थूलदेह
और स्थूल बुद्धिवाला व्यक्ति जो पाँच व्यक्तियों के बराबर अकेला खाता है,
इसे असफल लोगों से दिली हमदर्दी है? लगता है, हमदर्दी की बातें करना भी इन
दिनों फैशन की बात हो गई है। सुंदर वेशभूषा और व्यवस्थित आर्थिक मर्यादाओं से
सुरक्षित रह कर टूटेपन, बेचारेपन और असफलताओं के प्रति हमदर्दी जाहिर करना किसे
अच्छा नहीं लगेगा? करुणाजनक दृश्यों के प्रति विलगित होना बड़ा 'रोमांटिक'
मालूम पड़ता है बशर्ते कि किसी आदमी को जीवन की पूरी-पूरी सुविधाएँ उपलब्ध
हों। लगता है कि मैं धीरे-धीरे जड़ होता जा रहा हूँ। ऐसा जड़ जो प्रत्येक बात की
समीक्षा करता है। प्रत्येक क्षण के प्रति सजग रहता है। जिसकी चेतना एक क्षण के
लिए भी मूर्छित नहीं होती। किंतु जो चिर दिन के लिए बेचारा बन कर रह जाता है।
और अपने फैशन की भूख शांत करने के लिए लोग जिसके प्रति सहानुभूति का व्यवहार
करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं कटु हो गया हूँ। लोग कौन? यह दूसरा कोई नहीं है
- भला लोगों को मेरे से क्या लेना? यह कहनेवाला मेरा वही साथी होता है जिसके
कमरे में मैं मुफ्त का साझीदार होता हूँ और अपनी ही दृष्टि में 'पैरासाइट'
(परोपजीवी) बन जाता हूँ। यह भी सोचता हूँ कि क्या यह संभव नहीं हो सकता था कि मैं किसी प्रकार से यह
'गुर' सीख लेता कि चार पैसे कैसे कमाए जाते हैं? इस समस्त बौद्धिक चर्चा और
भाव-संपदा से क्या मिला? अपने भविष्य के बारे में अधिक सोचना और मंथन करना
कितने क्लेश की बात है? इसे मैं किसी प्रकार समझा भी तो नहीं सकता। एकाध
ट्यूशन कभी मिला भी है तो मेरे 'शेबी' होने के कारण छूट गया है। मेरे जैसे ही
गरीब मित्र बारी-बारी से मुझे अपने पास रख कर जीवित रख रहे हैं। पता नहीं वह
ऐसा क्यों करते हैं? मैं हृदय से चाहता हूँ कि अपने पूर्व इतिहास,
महत्वाकांक्षाओं और स्वप्नों को निर्ममता से तोड़ कर अलग हट जाऊँ और कुछ न
हो सकूँ तो अपने इन मित्रों जैसा तो हो ही जाऊँ ताकि सुख की साँस ले कर एक बार
तो कह सकूँ - यह मेरा प्राप्य है। मैं इसके बल पर जीवित हूँ। मेरे पौरुष का भी
कोई अंश मेरे जीवन में है। परंतु लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। दो-चार रुपए
हाथ में होने पर उन्हें मैं एकदम से खर्च कर देता हूँ यानि एक प्रकार से फेंक
ही देता हूँ और फिर खाली हाथ होने पर बड़े आश्चर्य से सोचता रह जाता हूँ कि कोई
ऐसा भी तरीका है जिससे मैं एक पैसा भी कमा सकूँ। इस क्रियाशील संसार में मुझे
एक भी उपाय ऐसा नहीं दिख पड़ता जिससे मैं चार पैसे अर्जित करके अपनी उपलब्धि,
अपने अस्तित्व को सिद्ध कर सकूँ। मेरे मित्र-परिचित मेरी सीमाओं को शायद खूब
समझते हैं, इसीलिए तो मुख पर कभी भी शैथिल्य या उपेक्षा का भाव नहीं लाते और
मेरे लटके-सूखे चेहरे को देख कर कहते हैं, 'अरे यार... दूसरों के सामने
तुम्हारा नाम ले कर तो हम अपना मुख उजला कर लेते हैं। तुमसे और कमाने-खाने से
क्या मतलब? मुझे वे एकदम खाट पर नहीं गिर जाने देते, जबरदस्ती मुँह धुलवाते
हैं, चाय पिलाते हैं और उन बातों को बचा कर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं जो
मेरी दुखती रगें हैं। मगर उनकी प्रत्येक बात से मेरा मन कातर हो जाता है और
मुझे संसार का समस्त व्यापार फीका लगने लगता है। कभी-कभी मेरे पाँव अनायास ही मुझे सारे कोलाहल से दूर ले जाते हैं और मैं
ऐसे स्थान पर पहुँच जाता हूँ जो सुंदर नगर के लिए श्राप या दुर्वचन-सा लगता
है। अर्ध अँधेरी बस्ती सोई-सी पड़ी रहती है। दूर तक छोटी-छोटी कच्ची कोठरियाँ
बनी हैं, उनके सामने टीनें पड़ी हुई हैं। कहीं-कहीं बकरी और उनके मेमने बँधे
हुए दिखाई देते हैं। उमस इस कदर होती है कि लोग टीन की छतों से बाहर - फुटपाथ
पर खाटें निकाल लेते हैं। इतनी शिद्दत की गर्मी में भी कोठरियों या टीन की छतों
के नीचे चूल्हे सुलगे होते हैं। सारी कोठरियाँ धुएँ से एकदम काली हो गई हैं,
उनकी छतों में धूल और मकड़ियों के जाले तने हुए हैं। एक आले में मरणासन्न, बुरी
तरह धुआँती ढिबरी टिमटिमाती रहती है और गृहिणी चीख-चीख कर बच्चों को पीटती या
कोसती हुई रोटियाँ थपथपाती रहती है और सड़क की बत्ती कभी ईद-बकरीद जल उठती है।
ये लोग इस जीवन के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इन्हें आक्रोश का इसमें कोई
कारण ही खोजे नहीं मिलता। वे इन सारी कटुताओं को सहज रूप में सहन करते चले जाते
हैं और भाग्य के नाम दो-चार सुंदर अश्रव्य शब्दों का प्रयोग करके कभी हँस भी
लेते हैं, कभी रोष भी व्यक्त कर लेते हैं - 'धत्तेरे की साली फूटी हुई तकदीर
की।' मगर फिर भी दिन कटते चले जाते हैं। किसी-किसी की रात ऐसे ही किसी चपरासी
या तीस-चालीस रुपए पानेवाले प्राइमरी के मुदर्रिस मित्र के यहाँ फुटपाथ में खाट
पर पड़ा मैं दूर-दूर तक निरभ्र आकाश पर फैले तारे देखता रहता हूँ जो मैंने आज,
इस क्षण तक व्यतीत किया है। उस जीवन के विषय में भी सोचता हूँ जिसका मैंने
बहुत दिनों तक स्वप्न देखा था और समझा था कि मजबूरियाँ और परिस्थितियाँ कुछ
नहीं होतीं, व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मगर वह वलवले और उत्साह आज
दम तोड़ चुके हैं। मैं और भी मूक हो कर एक दीर्घ आह भरता हूँ और आकाश के तारों
के व्यर्थ प्रयास हो कर गिनने की कोशिश करने लगता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मेरे जाननेवाले यही चपरासी और प्राइमरी स्कूल के मास्टर
हैं; मेरे जानने वाले, जाननेवाले ही क्यों बचपन से ले कर ऊँची डिग्रियाँ लेने
तक साथ रहने वाले कई ऊँचे अफसर और लेखक-कवि भी हैं। मगर उनकी हार्दिकता से भी
मुझे अब भय लगने लगा है। उनके साथ हो कर तो मैं उनके ठंडे लहजे और अतिशय
विनम्रता और मर्यादा की रक्षा में उन्हें व्यस्त देख कर इतना संकुचित हो
उठता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं नग्न ही हो उठा हूँ। उनके संपर्क में मुझे
इतनी घबराहट होती है कि मैं उनकी 'कंपनी' से हट कर दूर किन्हीं ऐसे आदमियों के
बीच चले जाना चाहता हूँ जो मुझे बिल्कुल न समझते हों। वे मुझे पागल भी समझेंगे
तो क्या है - कम से कम मेरी असफलताओं की इतनी निर्ममता और विद्रूप से खिल्ली
तो न उड़ाएँगे। मैं इन सिविलियन मित्रों से कितना डरने लगा हूँ जो लच्छेदार
भाषा के सहारे अत्यंत निष्करुण हो कर अपनी हँसी को जबरन दबा कर पूछते हैं,
'कहिए कैसे हैं? हाँ भई, बड़े आदमी हो... यार, हमें मत भूल जाना, हम तो
तुम्हारे कितने अंतरंग हैं...' इस काठिन्य की यही सीमा नहीं होती। वह ठहाके
लगा कर यह भी कहने से बाज नहीं आते, 'अरे भाई, और कुछ नहीं तो हमें अपना
प्राइवेट सेक्रेटरी ही बना लेना... इस टुच्ची नौकरी में भला क्या रखा है,
मौलिकता तो यहाँ मर ही जाती है। कुछ भी हो यार, हम तो तुम पर फख्र करते हैं।' मैं इन सब चाबुकों को अत्यंत सहिष्णु हो कर सहन कर लेता हूँ और रोने से भी
बदतर हँसी हँस कर एक ओर को चल देता हूँ और अचेतन में ही नगर की कोढ़ जैसी इस
उजाड़ बस्ती में पहुँच जाता हूँ। यहाँ बहुत थोड़े पढ़े-लिखे, बहुत मामूली लोग
मुझे बैठा लेते हैं और बहुत-सी बातें करते हैं। वे राजनीति की सतही बातें करते
हैं, सिनेमा या किसी बड़े लीडर की चर्चा होती है और मेरे किसी भी वाक्य को वह
बड़े ध्यान से सुन कर कहते हैं, 'इसीलिए तो पढ़े-लिखे आदमी की कद्र होती है।
हम लोग तो पशु हैं... कैसी लाजवाब बात कही है बाबू ने, भई वाह!' और ऐसे समय कोई
भी व्यक्ति - यह भूल कर कि मैं बीड़ी नहीं पीता - मेरी ओर एक बीड़ी बढ़ा देता
है और बिना जली बीड़ी को हाथ में ले कर मैं बेसाख्ता यह सोचने लगता हूँ कि
क्या मैं कहीं भी समझा जा सका हूँ? जिन लोगों ने बगैर पढ़े मेरी पांडुलिपियाँ
वापस की हैं, उन्होंने भी मेरे मर्म को समझने की चेष्टा नहीं की और मेरे ये
अपढ़ और अर्ध शिक्षित दोस्त मेरे अत्यंत ऊपरी और जबरदस्ती ग्रहण किए हुए
स्तर को वास्तविकता समझ कर मेरी सराहना करते हैं। शायद व्यक्ति से यह बात
देर तक छिपी नहीं रहती कि उसको न समझा जाना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है - सबसे
कठोर निर्वासन! |