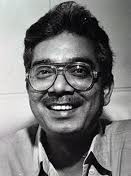|
कहानी |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
दुक्खम शरणम गच्छामि
कहानी 25 दिसंबर 1956, मेरठ, उत्तर प्रदेश ई-मेल dhirendraasthana@yahoo.com
अँधेरा पूरा था और सन्नाटा संगदिल। उस विशाल कैफे के ठंडे हॉल में मेरे कदम इस तरह पड़े जैसे आश्चर्य लोक में एलिस। हॉल सिरे से खाली था और मैं निपट अकेला।
उढ़के हुए शानदार दरवाजे को खोल कर भीतर आने पर सबसे पहला सामना काउंटर के ऊपर वाली दीवार पर टँगी घड़ी से हुआ। सुबह के चार बज कर बीस मिनट हो रहे थे। घड़ी
के ठीक ऊपर एक मर्करी बल्ब जल रहा था, सिर्फ घड़ी के लिए। लगभग बर्फ हो चुकी उँगलियों को एक-दूसरे से लगातार भिड़ा कर उन्हें गर्म करने के निष्फल प्रयत्न के
दौरान मैं एक विशाल दर्पण के सामने आ गया। वहाँ मैं था जैकेट और कनटोप के साथ अपनी उँगलियाँ रगड़ता। जैकेट के साथ लगे सिर के कनटोप को मैंने पीठ पर गिरा
दिया और दोनों हथेलियों को कस कर रगड़ने के बाद चेहरे पर जोर-जोर से फिराने लगा। दर्पण में मेरा प्रतिरूप मेरे साथ-साथ था एक ठिठुरते और धुँधलाते अक्स की
तरह।
तभी बाहर कहीं किसी निर्जन सड़क पर कोई ट्रक गुजरा। मैंने सुना एकदम साफ कि ट्रक की आवाज में एक कर्मठ व्यक्तित्व और मर्दाना लय जैसा कुछ था। किसी ट्रक के
गुजरने को मैंने इससे पहले इस तरह नहीं सुना था। शहरों, खास कर बड़े शहरों में तो एक अराजक शोर भर होता है। और मुंबई में तो किसी वाहन की अपनी कोई निजी आवाज
ही नहीं होती।
कैफे में जागरण का कोई चिह्न नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था मानो किसी भयावह आपदा की खबर पा कर लोग बाग बरसों पहले इस कैफे को छोड़ कर जा चुके हों। भविष्य
लोक से आती किसी भूली भटकी प्रार्थना की आहट तक वहाँ नहीं थी। हर कुर्सी और मेज पर एक अवाक निस्तब्धता सशरीर उपस्थित थी। लगभग चालीस-बयालीस मेजों और
डेढ़-पौने दो सौ कुर्सियोंवाले इतने बड़े तन्हा कैफै में उपस्थित रहने का यह मेरा पहला और मौलिक अनुभव था। मैं घूम-घम कर कैफे को टटोलने लगा तो लगा कि कहीं
कोई आवाज है। मैं रुक गया। आवाज अनुपस्थित हो गई। मैं काउंटर की तरफ बढ़ा। आवाज फिर उभरी। ओहो! मैंने अपने अचरज को विश्राम दिया। यह मेरे अपने चलने की आवाज
थी।
मैंने कैफे को उसके अभिशाप के हवाले छोड़ दिया। बाहर पार्क था। एकदम आक्रामक। वह दूर-दूर जलती उदास रोशनी के बीच ठंड के चाकू ले कर तना हुआ था। कनटोप को
वापस कान पर साधते हुए मैंने सुना कहीं से टप-टप की आवाज आ रही थी। मैं आवाज का पीछा करता चला गया। एक नल था, जो थोड़ा खुला रह गया था। उस नल की गर्दन ऐंठ
कर मुझे लगा जैसे बरसों-बरस बाद मैंने कोई काम संपन्न किया हो। मैं संभवतः समयातीत समय में चल रहा था। यह एलिस का आश्चर्य लोक नहीं मेरा वर्तमान था, मेरी
स्मृतियों, मेरी आदतों और मेरे अभ्यासों के हाथ लगातार पिटता हुआ। मैंने सुना अब एक बड़े जेनरेटर की आवाज गूँज रही थी, किसी अग्रज की तरह आश्वस्त करती कि
मैं हूँ न! जेनरेटर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए पार्क में रात भर बेखौफ टहला जा सकता था। मैं इस तरह टहल रहा था जैसे यह इतना बड़ा पार्क नितांत मेरा है।
मैं सहसा गर्वोन्नत हो उठा। मुंबई का वह दुख यकायक जाता रहा जिससे मैं अपने घर की बाल्कनी में कुछ गमले, कुछ फूल, कुछ घास देखने की आस में सतत तड़पा करता
था। वहाँ बाल्कनी ही नहीं थी। कहाँ से होते फूल, गमले, घास।
और फिर दो घोंसलों से टकरा गया मैं। वे एक पेड़ पर थे - कपड़े के घोंसले। यह आश्वस्ति देते हुए कि वे तोड़े नहीं जाएँगे। जिस भी पक्षी का मन चाहे वह इनमें
अपना घर बसा ले। मुझे अचानक लगा कि हमारे शहर के तो पक्षी तक भी 'स्ट्रगलर' होते हैं। पता है कि घोंसला टूटेगा फिर भी घर बनाते हैं।
घर बेतरह याद आया। घर में बीवी थी। चिड़चिड़ाती और पस्त होती हुई। दो बेटे थे - तेज-तेज कदमों से जवानी की तरफ जाते हुए - अपने-अपने सपनों, जिदों और सूचनाओं
के साथ। उन सपनों, जिदों और सूचनाओं में माँ के गठिया का दर्द और पिता की हताशा तथा वेदना और एकाकीपन के लिए कोई जगह नहीं थी। वहाँ लड़कियाँ थीं, फोन थे,
कंप्यूटर था। फन था और गति थी।
मैं थके कदमों से फिर कैफे में लौट आया। मेरा दिमाग बहुत सारे आँय-बाँय विचारों और न खत्म होने वाले हादसों की मर्मांतक चीखों से लदा-फँदा था। कैफे की घड़ी
पाँच दस बजा रही थी। मुंबई में सुबह की लोकल ट्रनों में लोग लद चुके थे। दादर का फूल बाजार सज चुका था। रात एक पाँच की आखिरी लोकल छोड़ चुके शराबी
कवि-कथाकार-पत्रकार सुबह चार दस की पहली ट्रेन पकड़ अपने-अपने घर पहुँच चुके थे या पहुँचने की प्रक्रिया में थे। नीलम, मेरी बीवी जाग रही थी। अलार्म घड़ी की
अलार्म को तेज गुस्से से बंद किया होगा उसने।
'कोई है?' एक कुर्सी पर बैठ कर मैं चिल्लाया। कैफे की छत बहुत ऊँची थी। मेरी 'कोई है' की अनगिनत प्रतिध्वनियाँ विभिन्न कुर्सी-मेजों तक हो आईं। इसके बाद फिर
वही ठंडा और सख्त सन्नाटा। मैं मुक्तिबोध की पानी और अंधकार में डूबी चक्करदार सीढ़ियाँ उतरने को था कि बदन पर नीली कमीज डाले एक जवान लड़के ने काउंटर के
पीछे बने दरवाजे के उस पार से झाँक कर देखा और शालीनता से बुदबुदाया - 'पहला नींबू शर्बत सुबह छह बजे मिलेगा। तब तक आप पार्क में टहल लीजिए।'
नींबू शर्बत? इस पत्थर-तोड़ ठंड में? मैंने सोचा भर था और इस सोचने के अवकाश का लाभ उठा कर लड़का वापस किचन में गुम हो गया था - अगली सदी के आगमन तक!
कम-से-कम मुझे ऐसा ही लगा था। एक पूरी सदी थी - ठंड-से-ठंड की तरफ जाती हुई। यहाँ के हर अनुभव का आरंभ उस भीषण ठंड की कँपकँपाहट से ही हो रहा था।
सुबह पौने तीन बजे इस गाँव के एक डिग्री वाले टेंपरेचर में मैंने प्रवेश लिया था। रिसेप्शन पर इस अस्पताल की औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद मैं तीन बजे कमरे
में घुसा था और हीटर ऑन करके रजाई में घुस गया था। काफी देर, शायद एकाध घंटे, करवटें बदलने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ था और ठंड के साजो-सामान से लैस हो कर इस
कैफे में चला आया था - यह सोच कर कि यह भी मुंबई की तरह रात भर जागता होगा। पर मुंबई यहाँ इस तरह नदारद थी जैसे चोर के पाँव।
मैं अत्यंत मायूस हो कर उठा और चोर के पाँवों की तरह चलता हुआ 'योगा हॉल' की तरफ बढ़ने लगा। हॉल के बाहर कुछ जोड़ी जूते-चप्पल रखे हुए थे और भीतर से
प्रार्थना के स्वर आ रहे थे -
आरोग्यम शरणम गच्छामि! निसर्गम शरणम गच्छामि! कुछ देर मैं उन दिव्य से लगते प्रार्थना के स्वरों को सुनता रहा। वे सभी स्त्री-पुरुष प्रकृति और स्वास्थ्य की
शरण में जाना चाहते थे। मैं पलट गया।
अस्पताल का लंबा कारीडोर सूना पड़ा था और उस कारीडोर में प्रार्थना के समवेत स्वर अपनी पूरी तन्मयता और लय के साथ तैर रहे थे। मुझे लगा वे परलोक से आती
प्रार्थनाओं की तरह हैं जो इहलोक में आते ही दुर्घटनाओं में बदल जाते रहे हैं। अपनी सपाट हथेली को मैंने सूनी और सिकुड़ती आँखों से देखा, वहाँ बहत्तर साल तक
जीते चले जाने की बद्दुआ दर्ज थी। मैं बीते समय के पायदान उतरने लगा। वहाँ एक अंधा भविष्यवक्ता था - मेरा दोस्त! शहर के बड़े-बड़े आँख, कान और दिमाग वाले
लोग उससे अपाइंटमेंट ले कर मिला करते थे। मेरा रेखाओं और अंकशास्त्र में बिल्कुल भी यकीन नहीं था लेकिन मेरे उस अंधे भविष्यवक्ता दोस्त ने मेरी हथेलियों को
छू-छू कर यह बता दिया था कि बहत्तर साल से पहले मुझे कोई छू भी नहीं सकता है। बहुत बरस पहले जब मैं अपने पुराने शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी खो कर दूसरी
प्रतिष्ठित नौकरी पाने के प्रयत्नों में अपमानित और उदास होता जा रहा था उस दोस्त ने भविष्यवाणी की थी : समुद्र वाले एक सबसे बड़े शहर में, जहाँ लोग अंधों
की तरह दौड़ते भागते हैं, एक सम्मानित नौकरी मेरा इंतजार कर रही है। इस भविष्यवाणी के चंद रोज बाद मैं मुंबई आ गया था और भविष्यवक्ता पुराने शहर में छूटा रह
गया था।
तो, अगर बहत्तर साल की उम्र तक मुझे कोई छू नहीं सकता है... मैंने सोचा तो इस वीराने में मुझे कौन-से डर खींच लाए हैं? सहसा कहीं एक बाँसुरी बजी। मैं कैफे
से बाहर आ गया - तीखी ठंड और मुसलसल टपकती ओस के बीचों-बीच। सुबह-साढ़े पाँच बजे वह जनवरी के जयपुर का एक गाँव था जहाँ अपनी अदम्य जिजीविषा से कोई बाँसुरी
पर अपनी अद्वितीयता सिद्ध कर रहा था। योगा हॉल के भीतर से अब भी वे मंत्र निरंतर बाहर निकल रहे थे जिनका अर्थ था - हमें प्रकृति की शरण में जाना है... हमें
रोगों से दूर ले चलो। मैं फिर पार्क में उतर गया। वहाँ कुछ मोर चले आए थे। मैं उनके निकट चला गया। मुझे देख कर वे भागे नहीं। दुनिया देख चुके बूढ़ों की तरह
वे पूरी शांति से मेरे साथ-साथ टहलते रहे। उनमें शहर के मनुष्य का भय नहीं था।
भय मुझमें भी नहीं था। मरने से नहीं डरता था मैं। मेरी निर्भयता को देख मुंबई का मेरा एक डॉक्टर दोस्त वाघमारे मेरा इलाज छोड़ कर भाग गया था। हुआ यूँ कि एक
शाम वह बिना पूर्व सूचना के मेरे दफ्तर चला आया। मैं उस वक्त सिगरेट पी रहा था। डॉक्टर नाराज हो गया। गुस्से से बोला - 'डॉक्टर से झूठ बोलते हो। तुम्हें
शर्म आनी चाहिए। तुम तो फोन पर हमेशा कहते हो कि सिगरेट छोड़ दी है। तो यह सब क्या है?'
'डॉ. वाघमारे।' मैंने गंभीरता से कहा - 'आपने आज के अखबार पढ़े हैं?'
'नहीं।' डॉक्टर अपने ज्ञान को ले कर चिंतित हो गया। उसे लगा अमेरिका में किसी सिगरेट समर्थक ने कोई खोज तो नहीं कर ली है।
'यह लीजिए।' मैंने अखबार उसके सामने रख दिया। डॉक्टर ने बोल-बोल कर पढ़ा - चीन में भूकंप से चार हजार मारे गए।
'तो?' डॉक्टर ने अपनी उत्सुक आँखें मुझसे मिलाईं।
'तो यह डॉक्टर, कि इन चार हजार मरनेवालों में से आधे से ज्यादा लोग सिगरेट नहीं पीते होंगे, यह मैं शर्त लगा सकता हूँ।' मैंने कहा।
'तुम...' डॉक्टर गुस्से से काँपने लगा... 'तुम एक नंबर के हरामी हो... तुम्हारा इलाज बंद।' डॉक्टर उठा और गुड बाय बोल कर चला गया। शहर के एक योग्य डॉक्टर और
बेहतरीन दोस्त को मैंने इस तरह अकारण खो दिया था।
तो यहाँ क्या पाने आया था मैं? मैंने सोचा - मिस्टर देव सिन्हा, आपका दिमाग क्या उस वक्त जलावतन पर था जब आप मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के इस
निर्जन गाँव में आ कर इलाज कराने का निर्णय ले रहे थे? मेरी घड़ी में पौने छह हो गए थे। मैं पार्क से निकल कर रिसेप्शन की तरफ चला आया। रिसेप्शन के दरवाजे
के पास पहुँच कर एक पल के लिए मैं रुका। दरवाजे के शीशे के पीछे झाँकने पर मैंने पाया - रात की ड्यूटी वाले शर्मा जी काउंटर पर सिर रखे सो रहे थे। ऐसी एक
बेफिक्र और बेझिझक नींद के लिए कितने बरसों से तड़प रहा था मैं। थके और उदास कदमों से मैं अपने कमरे का ताला खोल कर भीतर घुसा और लिहाफ के भीतर दुबक कर
सिगरेट पीने लगा। मुझे छह बजने का इंतजार था।
कैफे जीवित हो रहा था।
छह बज कर दस मिनट पर जब मैं जैकेट उतार, शाल ओढ़ कर वापस कैफे में घुसा तो तीन-चार मेजों पर बैठे कुछ लोग नींबू-शहद का शर्बत पीने में व्यस्त थे। मुझे सहसा
यकीन नहीं हुआ कि नींबू के पानी को भी इतने उत्साह और तन्मयता के साथ पिया जा सकता है। उनमें से कुछ ने मुझे एक उड़ती नजर से देखा और फिर से नींबू पानी में
व्यस्त हो गए। एक-दो लोगों के गिलासों को भेदिए की दृष्टि से देखता हुआ मैं काउंटर पर चला गया।
मेरे कुछ माँगने से पहले ही नीली कमीजवाले लड़के ने मेरे सामने नींबू पानी का गिलास रख दिया। मैंने गिलास को देर तक घूरा फिर लड़के की आँखों में देखते हुए
बोला - 'मुझे एक कप चाय की जरूरत है।'
लड़का हो-हो करके हँसा फिर शालीनता से बोला - 'यहाँ चाय किसी को नहीं मिलती।'
नींबू पानी के गिलास को ठुकरा कर मैं वापस मुड़ा। दरवाजा खोल कर मैं बाहर आया और रिसेप्शन वाले कमरे में घुसा। पौन घंटा पहले काउंटर पर सिर झुका कर सो रहे
शर्मा जी चाक चौबंद खड़े थे।
'यस सर!' उन्होंने अतिशय विनम्रता से पूछा।
'आज के अखबार आ गए क्या?' मैंने पूछा फिर घड़ी देखी और तत्काल लग गया कि सवाल गलत वक्त पर पूछा है। केवल साढ़े छह बजे थे। इस समय तक तो मुंबई में भी अखबार
नहीं मिलते। यहाँ कैसे मिलेंगे?
आश्चर्य हर कदम पर मेरे पीछे लगा हुआ था। लग रहा था कि मुझे नींद से जागे हुए एक युग बीत गया है जबकि घड़ी की सुइयाँ केवल साढ़े छह बजा रही थीं।
मैंने अपनी गलती दुरुस्त की और पुनः पूछा - 'मेरा मतलब है, अखबार कितने बजे आते हैं?'
'अखबार तो यहाँ नहीं आते सर!' शर्मा जी ने माफी-सी माँगते हुए कहा, 'अखबारों में कितनी तो मारकाट, चोरी-चकारी, बलात्कार, हत्या होती है। यहाँ के पवित्र
वातावरण पर दूषित प्रभाव न पड़े इसलिए यहाँ अखबार नहीं आते।'
'मतलब?' मेरी आँखें शायद फटने जा रही थीं। मैंने उन्हें मसल कर वापस उनकी जगह किया, 'मिस्टर शर्मा, आपका मतलब यह है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है,
इससे यहाँ के लोगों को कोई वास्ता नहीं है?'
'देश और दुनिया से थक जाने के बाद ही लोग यहाँ आते हैं सर।'
'लेकिन बिना अखबार का जीवन?' मैं किसी दुखी बूढ़े की तरह गर्दन हिलाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, श्रीकांत वर्मा की पंक्तियाँ मेरे पीछे लग गई थीं - 'बंद
करो अखबारों के दफ्तर और रुपयों की टकसाल। मैंने बिताए हैं खबरों और पैसों के बिना कई साल।'
मैंने दो काम एक साथ किए। अपनी कनपटी पर चाँटा मारा। क्या मुझे यहाँ आए हुए कई साल बीत गए हैं। उसके बाद कमरे का दरवाजा खोल दिया। फोन की घंटी बज रही थी।
भीतर कहीं बहुत दूर उल्लास और हर्ष का सोता-सा फूट पड़ा। फोन! मेरे लिए फोन! इस जंगल में। जंगल के बावजूद।
'गुड मार्निंग मिस्टर देव!' उधर कोई स्त्री स्वर था।
'कौन?' मैं अचकचा गया।
'सॉरी मिस्टर देव! पूरन की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। आपका 'डाइट चार्ट' आ गया है। आप दिन में दो बार हर्बल टी ले सकते हैं। प्लीज कम।' स्त्री स्वर कमनीय
था। उसमें लोच और नजाकत थी, नफासत भी।
'लेकिन आप अपना परिचय तो दीजिए।' मैंने हिचकते हुए कहा। शायद मेरे मन के कुछ उजाड़ कोने यह आत्मीय स्वर सुन कर सिंच रहे थे।
'आप आइए तो।' स्त्री स्वर ने आग्रह किया, 'पहले ही दिन रूठ जाएँगे तो कैसे चलेगा। पूरन बच्चा है। अस्पताल के नियमों से बँधा है। लेकिन मैं किचन की मैनेजर
हूँ। कुछ नियम तोड़ सकती हूँ।' स्त्री स्वर खिलखिलाने लगा। 'बहुत जमाने के बाद इस अस्पताल में कोई राइटर आया है... हम भी तो देखें, राइटर कैसे होते हैं?'
'आता हूँ।' मैंने फोन रख दिया। होंठों को गोल कर एक सीटी बजाई। जेब से कंधी निकाल कर बाल ठीक किए। शॉल को कायदे से लपेटा और कमरे से बाहर निकल कर ताला बंद
करने लगा। मुझसे पहले मेरी जानकारियाँ उड़ रही हैं। मैंने सोचा, थोड़ा आश्वस्त भी हुआ कि कोई तो मिलनेवाला है जो अपने को लेखक की हैसियत से जानता है या
जानना चाहता है।
स्त्री स्वर कैफे के दरवाजे पर ही खड़ा था। जींस की पेंट शर्ट, जींस की टोपी, स्पोर्ट्स शूज, गोरा रक्तिम-सा चेहरा, टोपी के बाहर निकल कर सीने पर लटक गई
लंबी चोटी। मासूम आँखें। यह स्त्री नहीं, बमुश्किल 23-24 वर्ष की एकदम युवा, तरोताजा लड़की थी। पुरुषों की हिंसा से गाफिल, पुरुषों के प्रेम में पड़ने को
आतुर।
इस वीराने में, जीवन से थके-टूटे मरीजों के बीच यौवन और उमंग से लबरेज यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? मैंने सोचा और पूछा - 'आप?'
'आइए।' उसने दरवाजे पर जगह बनाते हुए कहा - 'मेरा नाम सोनल है। सोनल खुल्लर! मैं किचन की इंचार्ज हूँ।'
मैंने देखा - यह विशाल कैफे पुनः खाली था, खाली और प्रतीक्षारत।
'पूरन!' लड़की ने आवाज लगाई, 'दो हर्बल टी। गुड़वाली।' लड़की ने मेज पर बैठने का इशारा किया।
'गुड़ क्यों? मुझे चीनी चाहिए।' मैंने हल्का-सा प्रतिवाद किया।
'क्योंकि शुगर को हम लोग ''व्हाइट पॉइजन'' मानते हैं।' लड़की खिलखिलाने लगी। 'मैंने फोन पर डॉक्टर से आपके लिए स्पेशल परमिशन ली है, हर्बल टी के लिए।'
वही नीली कमीजवाला लड़का मेज पर दो कप चाय रख कर चला गया। तो, यह महाशय पूरन हैं। मैं मुस्कराया। काउंटर पर खड़ा पूरन भी मुस्कराया।
'सारे मरीज कहाँ गए?' मैंने कैफे में नजरें दौड़ाते हुए पूछा।
'इलाज कराने।' लड़की फिर हँसी।
'आपको तुम बोल सकता हूँ?' मैंने लड़की की आँखों में देखा।
'मुझे अच्छा लगेगा।' लड़की मुस्कराने लगी, 'आपके ''डाइट चार्ट'' से पता चलता है कि आप मुझसे दुगनी उम्र के हैं।'
'और क्या-क्या पता चलता है ''डाइट चार्ट'' से?' मैंने क्षुब्ध स्वर में कहा।
'पूरा इंटरव्यू आज ही कर लेंगे। अभी तो पहला ही दिन है। आपको दस दिन हमारे साथ रहना है।' लड़की फिर खिलखिलाने लगी। लड़की को खिलखिलाता देख मुझे याद आया कि
मैं कितने सारे फूलों के नाम भी नहीं जानता हूँ।
'तुम्हारे साथ रहना है?' मैं रोमांचित था।
'मेरा मतलब हम सब लोगों के साथ।' लड़की का चेहरा रक्तिम हो आया, 'एक हर्बल टी और लेंगे?'
'क्या यह संभव है?'
'क्यों नहीं?' वह ताजा उत्साह से दमादम थी, 'आफ्टर ऑल आयम मैनेजर! इतना राइट तो है मेरा।' फिर वह रुकी। शरारत से मुस्कराई और बोली, 'अगर आप मैनेजमेंट से
चुगली न करें तो?'
'निश्चिंत रहें। इस उजाड़ की एकमात्र खुशी का वध नहीं करनेवाला मैं।' मैं मुस्कराया।
'थैंक्यू।' वह फिर खिलखिलाने लगी, 'आप लेखक लोग लोगों का दिल रखना खूब जानते हैं।' जुमला बोल कर वह लपकती हुई किचन के भीतर चली गई। मेज पर उसकी हँसी बिखरी
रह गई थी। मैं उस हँसी की पँखुड़ियों को चुनते हुए सोच रहा था कि इतनी ढेर सारी हँसी वह कहाँ से बटोर लाई है। रास्तों, प्लेटफार्मों, सीढ़ियों, पुलों और
ट्रेनों में लद कर जाती मुंबई की लड़कियाँ आगे-पीछे से उत्तेजक जरूर लगती हैं लेकिन उनकी हँसी कोई छीन कर ले गया रहता है। इस सुनसान गाँव के निविड़ एकांत
में बैठी सोनल खुल्लर की मासूम मादकता को ऐश्वर्या राय देख भर ले तो विश्व सुंदरी का ताज उतार फेंके। सोनल के गालों की तुलना गुलाब से करने के छायावादी
उपक्रम में था मैं कि वह लौट आई। उसके हाथ में दो कप चाय थी।
'पूरन और महेश मरीजों का नाश्ता तैयार कर रहे हैं। मैंने सोचा खुद ही बना लेती हूँ। चख कर देखिए, ठीक तो है।'
'तुमने बनाई है तो उम्दा ही होगी।' मैंने जवाब दिया। यह जवाब देते हुए मैं शोख और चंचल बनना चाहता था लेकिन मैंने पाया कि मैं उदास हूँ। बहुत-बहुत उदास। पता
नहीं क्यों?
'इतनी खूबसूरत जगह में भी आप दुखी हैं?' सोनल की नुकीली नाक की कोर से बूँद-बूँद अचरज टपक रहा था। 'अच्छा यह बताइए कि आप लेखक लोग कहीं भी सुखी नहीं रह पाते
क्या?'
जिस समय उसने यह प्रश्न किया, मैं अपना प्याला उठा रहा था। उसका प्रश्न शायद सीधे प्याले पर जा कर लगा था या फिर मेरे अतीत के किसी हरे जख्म को उसने छू लिया
था। मैंने आश्चर्यों के बोझ से गिरी जा रही पलकों को बमुश्किल ऊपर उठा कर उसे देखा और उसकी आँखों के तेइस-चौबीस वर्षीय अबोध कौतूहल से टकरा गया।
मेरे हाथ का प्याला मेज पर गिर पड़ा था।
लड़की चौंक कर खड़ी हो गई थी।
मरीजों ने आना शुरू कर दिया था।
000
उस पाला मारती ठंड में शाम होते-होते मेरे दुख गर्म हो गए। डॉ. नीरज ने मेरे बदन में उच्च रक्तचाप, लीवर की सूजन और कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा को खोज
लिया था। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी थी और सिगरेट का धुँआ पेप्टिक अल्सर का निर्माण करने में व्यस्त था।
वह एक युवा डॉक्टर था। इतने युवा व्यक्ति को प्रकृति की शरण में जाते हुए मैं पहली बार देख रहा था। प्रकृति, अध्यात्म और मुक्ति वगैरह के पचड़ों में अपने
देश के लोग अमूमन पैंतालिस-पचास के बाद पड़ते हैं और यह तो मुश्किल से चालीस का भी नहीं था। अगर मेरा अनुमान सही है तो डॉक्टर उम्र में मुझसे तीन-चार साल
छोटा था। ताजा कटे अनन्नास जैसा चेहरा था उसका। मेरी मेडिकल रिपोर्टों के बीच वह तन कर बैठा हुआ था। मर्माहत कर देने वाली सर्द आवाज में उसने अपना निर्णय
सुनाया - आकाश, जल, वायु, मिट्टी और अग्नि इन पाँच तत्वों से यह शरीर बना है। इन्हीं में विलीन भी हो जानेवाला है। अंत तो सबका सुनिश्चत है लेकिन समय से
पहले क्यों? मुंबई के मेरे दोस्त ने बताया कि आप लेखक हैं। मैं भी पढूँगा आपकी किताबें, तो लेखक होने के कारण आपके जीवन पर केवल आपका अधिकार नहीं है। उस पर
समाज का हक है...
डॉक्टर बोलता जा रहा था और मैं कहना चाह रहा था कि कौन-से समाज की बात कर रहे हो डॉक्टर? उस समाज की जो मुझे आप तक पहुँचने के लिए अपने उद्योगपति मित्र की
सहायता प्राप्त करने को मजबूर करता है। मैं तो फिर भी भाग्यशाली हूँ कि चार मित्र ऐसे हैं लेकिन पूरे दिन में दो बड़ा पाव खा कर जीवन गुजारनेवाले कैसे
पहुँचेंगे आप तक? उनको तो बिना इलाज के ही पाँच तत्वों में विलीन होना है।
कुछ नहीं कह सका मैं। क्या कह सकता था? दोपहर तक पता चल गया था कि जहाँ मैं हूँ, वह एक पाँच सितारा चिकित्सालय है। एक हजार रोज वहाँ का खर्च था। मेरे दस दिन
का मतलब था दस हजार इलाज के और दस हजार बजरिए विमान यहाँ आने-जाने के यानी पूरे बीस हजार का एहसान ले कर मैं यहाँ आ पाया था।
अचानक मैंने खुद को बहुत फँसा हुआ अनुभव किया, दरअसल मैं एक गंदी और शर्मनाक बीमारी की चपेट में आ गया था। मुझे बवासीर हो गई थी और सभी तरह के इलाज कराने के
बावजूद डटी हुई थी। बदहवासी के उसी दौर में मुंबई के एक उद्योगपति दोस्त ने मुझे यहाँ का पता और आने-जाने का टिकट पकड़ा दिया और मैं मूर्खों की तरह यहाँ आ
कर डॉ. नीरज के सामने बैठ गया था जिन्होंने बवासीर के अलावा भी पता नहीं क्या-क्या खोज लिया था।
'कल सुबह से आपका इलाज शुरू होगा।' डॉक्टर नीरज ने मुस्कराते हुए कहा, 'कहिए, ओराग्यम शरणम गच्छामि।'
'क्या आप कभी अखबार नहीं पढ़ते डॉक्टर?' मैंने एक बेतुका-सा सवाल किया।
'कभी-कभी देख लेता हूँ, जब बाहर जाता हूँ।'
'और टीवी?'
'टीवी नहीं है मेरे पास। कई साल पहले अपनी पत्नी के साथ 'मेरा नाम जोकर' देखी थी। डॉक्टर उत्साह-उत्साह में मित्रता जैसी नर्म और आत्मीय सीढ़ियाँ उतरने लगा।
'बहुत अच्छी फिल्म थी। अब शायद अच्छी फिल्में बनने का चलन नहीं रहा। क्यों आप बहुत फिल्में देखते हैं क्या?'
'नहीं, फिल्में तो मैं भी कभी-कभार ही देखता हूँ मगर एक अखबार तो आपको मँगाना ही चाहिए। नहीं?'
'मिस्टर देव' डॉक्टर की आवाज सहसा बहुत खुश्क हो गई। 'लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं। यहाँ की जो दिनचर्या है उसमें अखबार के लिए न तो समय है, न ही
जरूरत। आप खुद देखिएगा। अब आप जा सकते हैं। मुझे राउंड पर जाना है।' डॉक्टर उठ खड़ा हुआ। मैं भी।
डॉक्टर के चेंबर से निकल कर मैं सिगरेट लेने के लिए परिसर से बाहर निकला। गेट पर सुरक्षा अधिकारी अड़ गए। 'यहाँ सब बड़े लोग ही आते हैं। बड़प्पन का रौब तो
मारिए मत। हमारे लिए सब मरीज हैं। बाहर जा कर आपने चाय सिगरेट पी ली तो हमारी तो नौकरी गई न! अपराध करें बड़े लोग, दंड भरें छोटे लोग। यह तो न्याय नहीं हुआ
न? आप डॉ. नीरज से लिखवा लाइए, हम आपको जाने देंगे।'
मेरा मूड उखड़ गया। मेरे पैकेट में केवल तीन सिगरेट बाकी थीं। सुरक्षा अधिकारियों से झिड़की खा कर मैं कमरे में आ गया। मैंने तय किया कि अपनी यह दस दिवसीय
यात्रा ठीक इसी बिंदु पर पहुँच कर समाप्त कर देना ज्यादा उचित होगा। इतनी सारी वर्जनाओं, इतने घनघोर अकेलेपन, इस कदर दुनिया से कटे रह कर केवल कुछ मरीजों और
एक डेढ़ दर्जन स्टाफ के बीच तो मेरा दम ही घुट जाएगा।
क्या नीलम को याद नहीं रहा, मैंने बची हुई तीन सिगरेटों में से एक को बड़ी शिद्दत से सुलगाते हुए सोचा, कि भीड़ और शोर और निरंतर साथ मेरे जीवन में आरंभ से
ही अनिवार्यता की तरह लगे हुए हैं तो फिर नीलम ने सोचा भी कैसे कि मैं उसके बिना पूरे दस दिन ऐसी जगह रहूँगा जहाँ जीवन से हताश कुछेक मरीजों के सिवा कोई
नहीं होगा। आखिर क्या सोच कर उसने मुझे ठेल-ठाल कर इस यात्रा के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मजबूर किया था।
यहाँ यह मेरी पहली शाम थी और दूसरी शाम यहाँ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। न मिले मुंबई की फ्लाइट। मैं घोड़ा, ताँगा, टैक्सी, ट्रेन कुछ भी ले कर यहाँ से
निकलने का मन बना चुका था।
ठीक ऐसे त्रस्त मन के बीच मुझे गुटरगूँ गुटरगूँ सुनाई दी। कमरे की छत पर शायद ढेर सारे कबूतर चले आए थे।
आह! मैंने सिगरेट फेंकते हुए सोचा - कितने बरस के बाद मैं कबूतरों को सुन रहा था। बची हुई दो सिगरेटों को बड़े प्यार और जतन से छूते हुए मैंने घड़़ी देखी।
शाम के साढ़े सात बजे थे। मुंबई में इस समय मैं अपने दफ्तर में होता था। लेकिन यहाँ रात के खाने का समय आधा घंटा पार कर चुका था।
उसी वक्त किसी भूली-बिसरी याद की तरह फोन की घंटी बजने लगी।
उस तरफ सोनल थी।
000
सात चालीस पर मैंने कैफे में प्रवेश लिया तो सोनल दरवाजे पर ही खड़ी थी।
'खाने का समय छह से सात के बीच का है राइटर।' सोनल एअर इंडिया के महाराज की तरह अदब से झुकते हुए बोली। मैंने क्षण के दसवें हिस्से में ताड़ लिया कि 'राइटर'
कहते समय उसकी मंशा उपहास उड़ाने की नहीं है। मैं सहज हो गया। मुस्कराया और बोला, 'मैं जैन साधु नहीं हूँ मैडम कि सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लूँ।'
'सूर्यास्त से पहले खाना खा लेने के पीछे धर्म नहीं विज्ञान है। खाने की भी एक वैज्ञानिक थ्योरी है।' सोनल गंभीर हो गई।
'वैज्ञानिक थ्योरी तुम अपने पास रखो।' मैंने लापरवाही से कहा, 'तुमने खाना खा लिया?'
'मैंने?' सोनल पानी में डूबी चक्करदार अँधेरी सीढ़ियाँ उतरने लगी, 'मैं तो जयपुर के फार्म हाउस में रहती थी। वहाँ कोई पूछता ही नहीं था। पापा फौज में थे।
मम्मी सोशल वर्कर। अकेले रहते-रहते बड़ी हो गई तो पेशे के लिए एक 'रिमोट एरिया' चुन लिया। यहाँ भी कोई नहीं पूछता मेरे खाने के बारे में। आपके मन में मेरे
खाने की याद कहाँ से चली आई?' सोनल की आँखें पानी-पानी थीं। उस पानी पर रपटते हुए मैं अपने शायर दोस्त निदा फाजली के घर चला गया, जहाँ टेप पर उनकी गजल बज
रही थी -
दिया तो बहुत
जिंदगी ने मुझे
मगर जो दिया वो दिया देर से...
'अंतिम पेशेंट को खिला देने के बाद ही मुझे खाना चाहिए, नहीं?' सोनल पूछ रही थी।
'क्या खिला रही हो?' मैं हँसा। हँसने के पीछे कोई तर्क होता है क्या? मैंने सोचा।
'आज छूट है, कुछ भी खाइए। कल सुबह से आपका इलाज चलेगा। रोज का जो ''डाइट चार्ट'' डॉ. नीरज की तरफ से आएगा, वही खाना होगा।'
'क्या-क्या है तुम्हारे किचन में?' मैंने पूछा, 'तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं खाती हो? अकेले खाना मुझे भाता नहीं है।' मैं सफेद झूठ बोल गया। मुंबई में मैं
दोनों वक्त अकेला ही खाता था। दोपहर को दफ्तर में, रात को बारह-एक बजे, सबके खा-पी लेने के बाद। बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए नीलम को सुबह पाँच बजे उठना
पड़ता था इसलिए वह रात को बच्चों के साथ नौ-दस बजे तक खा लेती थी।
'अरे बाप रे! आप तो मरवा देंगे।' सोनल चौंक गई, 'एक मरीज में इतनी दिलचस्पी लूँगी तो मैनेजमेंट तो मेरी छुट्टी ही कर देगा। चलिए टेबल पर बैठिए, मैं आपके
सामने खड़ी रहूँगी।' सोनल बोली और किचन की तरफ मुँह करके चिल्लाई - 'पूरन, पालक सूप ले आओ।'
खाली कैफे की उस रात होती शाम में सोनल की आवाज मधुर तरीके से गूँज उठी। मुझे लगा इस आवाज के सहारे रहा जा सकता है दस दिन।
'तुम्हारे पेशेंट कहाँ गए?' मैंने यूँ ही पूछा।
'सब गए। पार्क में टहल रहे होंगे या अपने-अपने कमरों में होंगे।' सोनल ने जानकारी दी। पूरन पालक सूप रख गया। सूप का पहला चम्मच पीते ही मुझे कुछ खाली-खाली
सा, कुछ छूट गया सा लगा। याद आया मुंबई में यह समय शराब पीने का होता था या होने वाला होता था।
सूप समाप्त होते ही मेज पर सलाद की प्लेट, छोटी-सी मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुड़ और दही आ गया। पत्ता गोभी और करेले की भाजी भी थी।
'अरे वाह।' मैं सचमुच प्रसन्न हो गया। 'तुमको कैसे पता चला कि मुझे मक्के की रोटी, सरसों का साग और करेले की सब्जी पसंद है?' मैंने आश्चर्य से पूछा।
'डाइट चार्ट के साथ लगी आपकी मेडिकल और फिजीकल रिपोर्ट से।' सोनल सहज थी लेकिन मैं असहज और लज्जित सा हो गया। इसका मतलब यह जान चुकी है कि मुझे बवासीर है,
मैंने सोचा और तत्काल ही मेरा चेहरा लाल हो गया।
'सहज हो जाइए।' सोनल खिलखिलाई, 'यहाँ स्वस्थ लोग नहीं आते। हर पेशेंट की हर तकलीफ के बारे में जानना ही होता है वरना देखभाल कैसे कर पाएँगे?'
लेकिन बवासीर? एक अनजान जवान लड़की की जानकारी में। मेरी चेतना में एक नामालूम-सी शर्म दिप-दिप करने लगी।
मैं चुप खाना खाता रहा। रोटी खत्म करके मैंने सोनल की तरफ देखा। वह शायद मुझे चाव से खाना खाते ही देख रही थी। उसकी आँखों से मेरी आँखें टकरा गईं। वह शरारात
से मुस्कराई, 'बस, और खाना नहीं मिलेगा।'
'केवल एक रोटी?' मैं चकित रह गया।
'यह भी बहुत हेवी हो गया है।' सोनल ने हिदायत दी, 'अब आप एक घंटा टहल लें। चाबी यहाँ छोड़ जाएँ। पूरन सोते समय खाने के लिए आपके कमरे में खजूर रख आएगा।'
'लेकिन मैं खजूर नहीं खाता।' मैंने प्रतिवाद किया।
'क्यों? जितनी भी अच्छी चीजें हैं, उन सबसे बैर है क्या?'
'तुमसे कहाँ बैर है?' मैं पता नहीं क्यों और कैसे बोल गया। आम तौर पर ऐसे नायाब जुमले मुझे शराब पीने के बाद ही सूझते थे।
'अब जाइए। टहल कर आइए और सो जाइए। मैं भी खाना खा कर सोने जाऊँगी। सुबह चार बजे उठना होता है।'
'लेकिन!' मैंने घड़ी देखी, आठ बज कर पाँच मिनट हुए थे, 'इतनी जल्दी कैसे सो जाऊँ?'
'साढ़े नौ बजे लाइटें बंद हो जाएँगी।' सोनल ने नई जानकारी दी। मुझे याद आया, सुबह पौने तीन बजे जब मैं इस अस्पताल में आया था, तो कमरे में लाइट नहीं थी।
मुझे कमरे में रखी मोमबत्ती जलानी पड़ी थी।
'यह तो ज्यादती है।' मैं बुझे मन से उठा, 'पानी तो पिलवाओ।'
'पानी खाना खाने के एक घंटे बाद अपने कमरे में पीजिएगा।'
'इसमें भी कोई विज्ञान है?' मैं चिढ़ सा गया।
'हाँ,' सोनल खिलखिलाने लगी, 'आएगा, बहुत मजा आएगा। आपके साथ बड़ा मजा आएगा।'
'गुड नाइट।' मैं चिढ़ा-चिढ़ा मुड़ गया।
'कमरे की चाबी?' सोनल हँस कर बोली।
'मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे खजूर।' मैंने चिढ़े-चिढ़े ही जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। कमरे में जा कर पहले एक सिगरेट पीनी थी।
कमरे में आ कर सिगरेट पीते हुए मैंने सोचा, नीलम को फोन करूँ क्या? उसे बताऊँ कि मैंने खाना खा लिया है और सोने जा रहा हूँ। घर में किसी को भी यकीन नहीं
होगा। छोटा बेटा पढ़ रहा होगा। बड़ा बेटा कॉलेज से लौटा नहीं होगा। इस वक्त ट्रेन या बस में होगा। नीलम खाना बना रही होगी। निशा मेरे लिए शामी कबाब ले कर आई
होगी और यह सुन कर सिर धुन रही होगी कि उसके अंकल मुंबई में नहीं हैं...
निशा मेरे एक मुस्लिम दोस्त की बेटी थी। उसका पिता शराब नहीं पीता था इसलिए वह अक्सर मेरे लिए शामी कबाब तल कर ले आती थी। ठीक शराब पीने के समय या खाना खाने
के चंद क्षणों पहले। निशा बी.कॉम. में पढ़ती थी, इसके बावजूद उसके हाथों के बने शामी कबाब अविस्मरणीय ढंग से लजीज होते थे। उन कबाबों के कुरकुरेपन में एक
बेटी के अप्रतिम प्यार की सोंधी खुशबू घुली-मिली होती थी।
रिसेप्शन पर आ कर मैंने फोन किया। फोन छोटे बेटे राहुल ने उठाया और आवाज पहचान कर जोर से बोला, 'पापाऽऽऽ मेरे लिए राजस्थान की कठपुतली लाना।'
'मम्मी को दे।' मैंने अधीरता से कहा।
'मम्मी सब्जी लेने मार्केट गई है।'
'खाना खाया?'
'अभी नहीं।'
'लो कर लो बात।' मैंने सोचा और बोला, 'अच्छा मम्मी को बोलना पापा ठीक से हैं।'
'ओके पापा, आपने टीवी देखा?'
'टीवी यहाँ नहीं है बेटा।' मैं दुखी-सा हो गया।
'ओह शिट। पापा, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारा प्लेन हाईजैक कर लिया।'
'अरे?' मैं चौंक उठा।
'हाँ, पापा।' राहुल उत्तेजित था। 'उन्होंने हमारे एक यात्री... को तो मार भी दिया। जहाज में डेढ़ सौ इंडियन हैं।'
'क्या बोल रहा है?'
'हाँ पापा। आप अखबार तो पढ़ो?'
'ओके बेटा बाय! मैं सुबह फोन करूँगा?' मैंने कहा और फोन रख दिया। मेरी बेचैनी मेरे सिर चढ़ कर बोल रही थी। मैं पार्क में घूमने निकल पड़ा।
पार्क एकदम खाली था। खाली और निस्तब्ध। अचानक ऐसा लगा मानो इतनी बड़ी पृथ्वी पर मैं अकेला ही बचा रह गया हूँ। एक राउंड भी पूरा नहीं कर पाया था कि ठंड के
कारण बदन कँपकँपाने लगा। प्यास भी खूब तेज लगने लगने लगी थी। मैं तेज कदमों से पार्क का चक्कर लगा कर वापस कमरे पर आ गया। घड़ी में पौने नौ बजे थे।
बत्तियाँ गुल होने में पूरे पैंतालीस मिनट बाकी थे।
मुझे याद आया। मुंबई में जब किसी कारणवश जल्दी घर आना होता था तो मैं नौ अट्ठावन की ट्रेन पकड़ा करता था। यूँ आमतौर पर मैं रात ग्यारह उनतालिस की आखिरी
फास्ट ट्रेन पकड़ कर जाया करता था।
स्मृतियों पर अवसाद झर रहा था। न सिर्फ स्मृतियों पर वरन पूरी चेतना ही पक्षाघात के जबड़े में जाने को आतुर थी। अपने देश का एक पूरा विमान हाईजैक हो गया था
और यहाँ एक पाँच सितारा चिकित्सालय में खा-खा कर बीमार हुए लोग अपने-अपने कमरों में सो रहे थे।
'मैं उल्लू का पट्ठा हूँ क्या?' मैं जोर से चिल्लाया।
पट्ठा, पट्ठा पट्ठा... शब्द मुझ तक लौट आए।
अस्पताल की बत्तियाँ बुझ गईं। मतलब साढ़े नौ बज चुके थे।
मेरे पास सिर्फ एक सिगरेट बची थी। मुंबई में बच्चे विमान अपहरण का लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे। मैंने सोचा और बिस्तर में घुस कर लिहाफ ओढ़ लिया जैसे
शुतुरमुर्ग रेत में मुँह गड़ा कर सो जाता है।
000
सुबह पाँच बज कर पाँच मिनट पर फोन आ गया। वह तब तक बजता रहा जब तक मैंने फोन को उठा नहीं लिया।
'जय श्री राम।' उधर से आवाज आई। 'सुबह हो गई है। उठिए, फ्रेश हो कर आधा घंटा पार्क में टहलने जाइए। उसके बाद योगा हॉल में आइए, प्रार्थना करेंगे। नमस्कार।'
और फोन कट गया।
बिस्तर में घुसने से पहले मैंने बाथरूम की लाइट बंद नहीं की थी और दरवाजे को भी खुला छोड़ रखा था। फोन बजने पर मैंने रजाई से मुँह निकाला तो बाथरूम में
उजाला था और उसकी लाइट से कमरा भी थोड़ा-थोड़ा रोशन था।
बहुत चिढ़ कर मैं उठा। बिना शराब पिए पूरी रात नींद नहीं आई थी। शायद सुबह के चार सवा चार पर पलकें झपकी थीं। मैं उठा। अंतिम सिगरेट जला कर बाथरूम में घुस
गया। फ्रेश हो कर वापस बिस्तर पर आया। बगल की तिपाही पर रखे कागज को देखा - वह दिनचर्या चार्ट था। यह चार्ट कल दिन में नहीं था। शायद शाम को कोई रख गया
होगा।
चार्ट में दर्ज था - 'सुबह पाँच बजे उठना। साढ़े पाँच बजे तक पार्क में टहलना। छह बजे तक योगा हॉल में प्रार्थना, पौने सात तक हेल्थ क्लब में जा कर नेति,
कुंजल और एनिमा का इलाज लेना, सात बजे कैफे में जा कर नींबू-पानी-शहद पीना। आठ बजे तक वापस योगा हॉल में जा कर योगासन करना। वहीं पर नौ बजे तक डॉ. नीरज का
प्रवचन। नौ से साढ़े ग्यारह तक हेल्थ क्लब में जा कर मिट्टी पट्टी, मालिश, ठंडा-गर्म स्नान, भाप स्नान, पिरामिड चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा आदि लेना। साढ़े
बारह तक कैफे में आ कर खा लेना। दो बजे तक पार्क में घूमना। आराम करना या पुस्तकालय में बैठ कर स्वास्थ्य संबंधी किताबें पढ़ना। ढ़ाई बजे वापस कैफे में जा
कर जूस पीना और पुनः हेल्थ कल्ब में चल देना। साढ़े पाँच बजे इलाज से लौट कर कैफे में फल खाना। साढ़े छह तक पार्क में टहलना। साढ़े सात तक हर हाल में खाना
खा लेना। साढ़े आठ तक पुनः इलाज लेना। नौ बजे कमरे में आना और साढ़े नौ तक सो जाना।'
अचरज की चक्करघिन्नी में गोल-गोल घूम कर मेरे दिमाग की नसें तड़कने लगीं। इस दिनचर्या में रोटी की मशक्कत, भाग-दौड़, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण की बुरी
सूचनाएँ, माधुरी दीक्षित की धक-धक, बिजली गुल होने की समस्या, ट्रैफिक जाम में फँस जाने की पीड़ा, बेटे के देर रात तक घर न लौटने पर नीलम का चिड़चिड़ापन और
चिंता कुछ नहीं था, कहीं नहीं था। यहाँ सिर्फ डॉ. नीरज थे और था उनका प्राकृतिक इलाज।
मैं कमरे से बाहर आ गया - गर्म कपड़ों से लदा हुआ। बाहर, परिसर में इस सिरे से उस सिरे तक एक पागल ठंड हा-हा हू-हू करती दौड़ रही थी। ठंड के कारण मेरे दाँत
बजने लगे थे।
पार्क में परिचित सन्नाटा था। परिसर के विशाल गेट पर सुरक्षा अधिकारी तक नहीं थे। मैंने गेट की छोटी खिड़की से मुँह बाहर निकाल कर देखा - ठीक सामने एक
छोटी-सी गुमटी जैसी बंद दुकान थी। एक टूटी-फूटी कच्ची सड़क दाएँ-बाएँ दूर तक चली गई थी। पता नहीं सामनेवाली दुकान में सिगरेट मिलती है या नहीं? बाहर जाने की
स्पेशल परमिशन तो डॉ. नीरज से लेनी ही होगी।
मैं पलट कर पार्क में आ गया। पार्क के बीचों-बीच सोफे के आकार के जो छह सात झूले खड़े थे, वे संभवतः दोपहर की धूप में आराम करने के लिए रहे होंगे। तभी एक
हल्का-सा झोंका आया और मुझे लगा पार्क में पत्तों की पाजेब बजी है।
अब तक मैं आधे पार्क का चक्कर लगा चुका था। थोड़ा-थोड़ा उजास झरने लगा था। पार्क की बत्तियाँ क्रमशः बुझ रही थीं। हेल्थ क्लब की बत्तियाँ एकाएक जलने लगीं।
मैं एक छोटे से बाँस के घर के सामने रुक गया। उसके भीतर प्यारे-प्यारे खरगोश टहल रहे थे। जीवन में पहली बार मैंने खरगोशों से बातें कीं और उस दिन को नफरत की
तरह याद किया जब मैंने पहली बार खरगोश का माँस खाया था।
उसी समय कबूतरों का एक झुंड वहाँ पर उतरा और पार्क की ओस में भीगी, मखमली घास पर बिखर गया। मैंने तत्काल चप्पलें उतारीं और कबूतरों की तरह उस गीली घास पर
देर तक चलता रहा। शुरूआती ठंड के बाद हरी-गीली-नरम घास पर नंगे पाँव चलना एक सुखद आश्चर्य जैसा लगा, मैं देर तक नंगे पाँव टहलता रहा और सोचता रहा कि
मुंबई-दिल्ली-कलकत्ता के मेरे तमाम दोस्त इस समय निश्चित रूप से सो रहे होंगे। जबकि उनसे अधिक देर तक सोनेवाला मैं यहाँ, नंगे पाँव सूर्य के स्वागत में खड़ा
था।
मेरी चिढ़ का क्या हुआ। क्या सचमुच मेरा भी कायाकल्प हो रहा है। मैं सृष्टि और उसके चमत्कार से मित्रता करने की दिशा में फिसल रहा था क्या? यह एक अपूर्व
अनुभव था - ठीक वैसा, जैसा निर्मल वर्मा की कहानियों और उपन्यासों में मिलता है - धुंध, धुएँ, आलोक में तिरता रहस्यमय मगर चमकीला-सा, वर्षों के कठोर दुखों
को अनवरत सहते रहने के बाद सहसा सामने आ खड़े मायावी सुख-सा, एक चिड़चिड़ी, थका देने वाली जद्दोजहद के बाद की उनींदी नींद के बाद अर्जित हुआ विरल अनुभव।
घड़ी देखी-साढ़े पाँच बज गए थे। अब आधे घंटे की प्रार्थना में जाना था। मैं योगा हॉल में जाने के बजाय रिसेप्शन पर चला गया। मुझे मालूम था कि मुंबई में नीलम
उठ चुकी होगी।
फोन मिलाया। नीलम ही थी।
'मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह तुम हो?' नीलम ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा, 'इतनी सुबह।'
'मार्निंग वॉक से लौट रहा हूँ।' मैंने रौब मार दिया।
'देव, मैं रियली बहुत खुश हूँ... सतुम खुश हो न?' नीलम ने आशंकित हो कर पूछा।
'मैं अपनी अंतिम सिगरेट पी चुका हूँ और कल रात शराब भी नहीं मिली।'
नीलम को खुश होना चाहिए था लेकिन उसके मुँह से अफसोस में डूबा 'बेचारे' शब्द निकल गया। मुझे खुशी हुई कि वह मेरी यातना को समझ पा रही है।
'और क्या समाचार है?' मैंने पूछा।
'सबसे बड़ा समाचार विमान अपहरण का ही है। तुमने नहीं पढ़ा?' नीलम चकित थी।
'यहाँ टीवी और अखबार कुछ नहीं है।' मैंने कुढ़ कर कहा।
'ओह!' नीलम बोली, 'मैं तुम्हें फोन करती रहूँगी।'
'नहीं! तुम फोन मत करना। आज से मैं पेशेंट हूँ। पता नहीं कब कहाँ रहूँगा। मैं ही तुम्हें फोन करूँगा। बाय!' मैंने फोन काट दिया। फोन का बिल अपने खाते में
जमा करने का निर्देश शर्मा जी को दे कर मैं बाहर निकला तो थोड़ा प्रफुल्लित था। यह नीलम से बात हो जाने की प्रसन्नता थी शायद। हालाँकि मन में कहीं यह कसक भी
थी कि विमान में बंधक यात्रियों का थोड़ा विस्तृत समाचार मिल जाता तो अच्छा था। योगा हॉल में जा कर प्रार्थना में शामिल होने का मन नहीं बन रहा था इसलिए छह
बजे तक मैं रिसेप्शन के बाहर बने लंबे कारीडोर में टहलता रहा।
ठीक छह बजे मैं इलाज के लिए 'हेल्थ क्लब' की दिशा में निकल पड़ा।
शायद प्रार्थना ठीक छह बजे समाप्त नहीं हुई थी। इलाज के लिए पहुँचने वालों में मैं सबसे पहला शख्स था।
एक दाढ़ी वाले वर्मा जी ने मुझे एक जग गुनगुना पानी दिया और बोले, 'पूरा पानी पी जाएँ और उसके बाद मुँह में उँगली डाल कर उल्टी कर दें।'
उल्टी के साथ पीला-पीला पित्त और बलगम भी बाहर आ गया। मुझे अच्छा लगा। इसे 'कुंजल' कहते थे। इसके बाद वर्मा जी ने स्टील के एक नली वाले लोटे को पकड़ा कर
बताया, 'दाईं नाक से पानी ले कर बाईं नाक से निकालें, फिर बाईं नाक से पानी ले कर दाईं नाक से निकाल दें।' यह 'नेति' थी। फिर वर्मा जी ने मुझे 'एनिमा' वाले
कमरे में पहुँचा दिया। नीम के पानी का 'एनिमा' ले कर मैं 'कमोड' पर बैठा तो लगा पूरा पेट एक बार में ही खाली हो गया है।
बाथरूम से निकला तो देखा बाकी मरीज आने शुरू हो गए थे। स्त्रियों और पुरुषों की अलग-अलग व्यवस्था थी। स्त्रियों के लिए स्त्री परिचारिकाएँ थीं।
ठंड से कुड़कुड़ाते हुए मैं कैफे में पहुँचा और पूरन से 'हर्बल' टी की माँग की।
'नहीं साब!' पूरन मेरा डाइट चार्ट देख कर बोला, 'आज से नींबू-पानी-शहद ही मिलेगा।'
मैं नींबू-शहद का गिलास ले कर एक कोने में बैठ गया और कैफे में क्रमशः प्रवेश करते मरीजों को देखने लगा। कोई बहुत मोटा था, कोई बहुत पतला। कोई लँगड़ा कर चल
रहा था, किसी की कमर झुकी हुई थी। ज्यादातर अधेड़ स्त्री-पुरुष थे, लेकिन सबके सब निश्चित रूप से संपन्न रहे होंगे।
सात से आठ वाली योगासन की कक्षा मैंने छोड़ दी लेकिन आठ बजने में पाँच मिनट पर मैं 'योगा हॉल' के भीतर था - डॉ. नीरज के प्रवचन के लिए। चिकित्सालय के 'योगा
हॉल' के भीतर था - डॉ. नीरज के प्रवचन के लिए। चिकित्सालय के 'योगा हॉल' से यह मेरा पहला साक्षात्कार था।
वह एक विशाल हॉल था। जिसमें सामने की दीवार पर बहुत बड़े आकार का ताँबे का 'ऊँ' लगा हुआ था। उसके सामने डॉ. नीरज का सफेद आसन था और आसन के सामने पूरे हॉल
में कीमती दरियाँ बिछी हुई थीं। योगासन की कक्षा समाप्त हो गई थी और सभी मरीज डॉ. नीरज के इंतजार में थे।
ठीक आठ बजे चीते जैसी फुर्ती के साथ डॉ. नीरज ने प्रवेश लिया और मुझे गेट पर खड़ा देख प्रसन्न हो गए।
'आइए', डॉ. नीरज ने कहा और अपने आसन पर जा कर बैठ गए। बाकी मरीजों से थोड़ा हट कर मैं भी एक तरफ बैठ गया।
'पहले आप सबका अपने नए सदस्य से परिचय कराते हैं।' डॉ. नीरज ने मेरी तरफ इशारा कर सभा को संबोधित किया। मैंने खड़े होकर सबको नमस्कार कर दिया। प्रत्युत्तर
में बाकी लोगों ने भी हाथ जोड़ दिए।
'यह श्री देव सिन्हा हैं। लेखक और पत्रकार। मुंबई से आए हैं। मेरा श्री देव से आग्रह है कि जब उनके जैसा व्यक्ति यहाँ आ ही गया है तो हमारे इस चेतना के
जागरण के विज्ञान का खुद भी लाभ ले और यहाँ से जा कर दूसरे लोगों को भी जागृत करे। मैं फिर कहता हूँ कि लिखने-पढ़नेवालों का जीवन केवल उनका अपना नहीं होता।
आप यहाँ से एक बड़े समाज के लिए जनहित का संदेश ले कर जाएँगे तो हमारे यह प्रयत्न सार्थक होंगे। चलिए अब मेरे पीछे-पीछे बोलिए -
निसर्गम शरणम गच्छामि!
योगम शरणम गच्छामि!
आरोग्यम शरणम गच्छामि!!
आनंदम शरणम गच्छामि!!
'हाँ तो मित्रो!' डॉ. नीरज शुरू हो गए, 'जैसा कि आप जानते हैं कि दवा से रोग दबा दिया जाता है। दबा हुआ रोग बार-बार उभरता है। हम रोग को दबाने में नहीं, जड़
से मिटाने में यकीन रखते हैं। हमारे केंद्र की एक बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ रोगी न केवल स्वस्थ होता है वरन खुद एक चिकित्सक बन कर जीवन में लौटता है। हम
मानते हैं कि सारे रोग एक हैं और रोग की दवा भी एक ही है। आहार को ले कर हमारा अज्ञान ही समस्त रोगों की जड़ है इसलिए दूषित, जहरीले भोजन से 'कचराघर' बन
चुका पेट यहाँ सबसे पहले स्वच्छ किया जाता है। आज हमारी इंदौरवासी महिला मरीज श्रीमती कुसुम व्यास हमसे विदा ले रही हैं, हमारे केंद्र में आईं तो इनका वजन
पिच्चासी किलो था। अब यह बासठ किलो की हैं। क्यों बहन जी, कोई संदेश?'
श्रीमती व्यास उठ कर खड़ी हो गईं और लजाते हुए बोलीं - 'मुझे तो इतना ही कहना है जी कि मैं यहाँ स्ट्रेचर पर लाई गई थी और अपने पाँवों से चल कर जा रही हूँ।'
सभागार तालियों से गूँज उठा।
'कोई प्रश्न?' डॉक्टर ने पूछा।
मेरा मन नहीं माना। मैंने हाथ उठा दिया।
'पूछिए!' डॉ० नीरज बोले।
'बाहर जो दुख है, शोक है, दैन्य है, रोजी-रोटी की मशक्कत है, भूख है, संताप है, अपहरण, बलात्कार, हत्याएँ, तालाबंदी, हड़तालें और लाठी चार्ज हैं, चौबीस
घंटों की भागदौड़ और तनाव है, झुग्गी-झोपड़ियों का नरक और जीवन का विराट तथा अनवरत संग्राम है और जिसके कारण ही बड़े-बड़े रोग हैं, निधन है, लाचारियाँ हैं,
आत्महत्याएँ है...'
'बस बस! मिस्टर देव! मैं आपका प्रश्न समझ गया!' डॉ. नीरज ने मुझे टोक दिया, 'लेकिन इस शाश्वत प्रश्न का जवाब मुंबई हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल या 'एम्स' का
कोई डॉक्टर दे सकता है?' अंत तक आते-आते डॉ. नीरज का चेहरा तमतमाने लगा था। 'आप चाहें तो इस विषय पर हम अलग से बैठक कर सकते हैं मिस्टर देव, वैसे आपकी सूचना
के लिए बता दूँ कि चिकित्सक होने से पहले मैं कवि और उससे भी पहले मार्क्सवाद का विद्यार्थी था। और इन दोनों कारणों से ही मैं प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ
आया। जिस बाइपास सर्जरी का खर्च मुंबई अस्पताल में डेढ़ दो लाख रुपए आता है उसी रोगी हृदय को हमारे यहाँ बीस दिन और बीस हजार रुपए में ठीक कर देते हैं।'
'थैंक्यू डॉक्टर। मेरी मंशा आपको चोट पहुँचाने की नहीं थी। एक लेखक होने के कारण मेरी जिज्ञासाएँ जरा दूसरी तरह की हैं।' मैंने जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ
क्योंकि स्वयं डॉ. नीरज भी खड़े हो चुके थे। घड़ी में ठीक नौ बज रहे थे। मरीजों को इलाज के लिए हेल्थ क्लब जाना था।
000
रात बारह बजे आने वाले फोन ने जगा दिया।
इस समय? मैंने लिहाफ में से मुँह निकाल कर सोचा और टेबल लैंप जला कर घड़ी देखी - सचमुच बारह ही बजे थे। असल में दिन भर के इलाज ने शरीर को भरपूर राहत देने
के साथ-साथ बेतरह थका भी दिया था। आखिरी, गर्म पानी में पैरों का स्नान और नाभि में गाय के दूध से बना शुद्ध घी लगवा कर जब मैं कमरे पर लौटा तो रात ग्यारह
बजते-बजते ही बड़ी सुहानी नींद में चला गया था।
फोन पर शर्मा जी थे।
'कीचड़ स्नान के लिए जाना है क्या?' मैं चिढ़ कर पूछा।
'नहीं सर! डायरेक्ट लाइन पर आपका फोन है मुंबई से।' शर्मा जी संयत थे।
'आया।' मैंने कहा और बिस्तर से निकल कर शॉल ढूँढने लगा। इस समय फोन क्यों किया होगा नीलम ने? मैंने सोचा। हालाँकि मुंबई के लिहाज से यह कोई ज्यादा समय नहीं
था। इस समय तक तो मैंने रात का खाना भी नहीं खाया होता था।
'देव बुरी खबर है।' नीलम हाँफ-सी रही थी। 'आज दोपहर निशा ने 'रैटौल' खा कर आत्महत्या कर ली। अभी-अभी अस्पताल से उसकी बॉडी ले कर आए हैं। बाहर पूरी कॉलोनी
जमा है। मैं उसे देखने अस्पताल गई थी। वह अंत समय तक बड़बड़ा रही थी कि देव अंकल होते तो मैं बताती मेरे साथ क्या हुआ?'
'ओह!' मेरे मुँह से निकला। फिर मैंने फोन रख दिया। शरीर का एक-एक रोम खड़ा हो गया था।
फिर रात भर नींद नहीं आई। ऐसा क्या हुआ होगा कि चार्टर्ड एकांउटेंट बनने का स्वप्न देखने वाली एक युवा लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा?
सिगरेट होती तो मैं शायद रात भर चहलकदमी करता। बिस्तर में पड़े-पड़े सुबह पाँच बजे आने वाले फोन का इंतजार करता रहा। भूख भी बहुत कस कर लग रही थी क्योंकि
डॉ. नीरज ने मुझे तीन दिन के उपवास पर रख दिया था - सिर्फ नींबू-पानी-शहद पीने की छूट थी।
000
मैंने तुम्हें एक नया नाम दिया है। सुबह सात बजे मैं सोनल को बता रहा था। सात से आठ वाली 'योगा क्लास' से डॉ. नीरज ने मुझे मुक्ति दिला दी थी। इसलिए यह पूरा
एक घंटा मेरा स्थायी रूप से कैफे में बीतता था - सोनल के साथ। यह मेरी पाँचवीं सुबह थी।
'क्या नाम दिया है सुनें तों!' सोनल किचन के उस पार से मेरे लिए खुद नींबू-पानी-शहद ले कर आ गई थी।
'रिमोट एरिया की महारानी।' मैं बुदबुदाया।
सोनल ने सुना और खिलखिलाने लगी लेकिन खिलखिलाते-खिलखिलाते वह दूर चली गई। काउंटर के उस पार जा कर वह चीखी, 'तुम्हारा आज का चार्ट आ गया है राइटर! आज तुमको
दोपहर के खाने में एक प्लेट सलाद, सोयाबीन का दही और आधा प्लेट उबला हुआ पालक मिलने वाला है।'
मैं विस्मित रह गया। उसी विस्मय में थरथराता मैं काउंटर तक गया और बोला - 'तुमको मालूम है, तुम मुझे तुम कह रही हो।'
'क्या? नहीं!!' काउंटर के उस पार सोनल थिर थी।
फिर वह धीरे-धीरे पीछे हटी, एकाएक झटके से घूमी और भीतर किचन में कहीं गायब हो गई।
कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने काउंटर पर ठक-ठक की तो पूरन बाहर निकला।
'सोनल कहाँ है?' मैंने पूछा।
'मेम साब अपने कमरे पर चली गई हैं।' पूरन ने बताया और मुझे अवाक छोड़ किचन के भीतर चला गया।
कैफे की एक मेज पर मेरा नींबू-पानी-शहद लावारिस पड़ा था।
000
दोपहर का भोजन वही था जो सोनल ने बताया था लेकिन खुद सोनल वहाँ नहीं थी। वह रात के खाने पर भी नहीं दिखी। पूरन ने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह कमरे पर
हैं। बहुत डरते-डरते पूरन ने सोनल के कमरे का फोन नंबर दिया।
रात नौ बजे मैंने सोनल का फोन नंबर घुमा दिया। सोनल ही थी।
सोनल मैं देव!'
'जी।' उधर से दबा भिंचा स्वर आया।
'बीमार हो?'
'हाँ।'
'तुम लोग भी बीमार पड़ते हो?' मैंने परिहास किया, 'खाना खाया?'
'नहीं।'
'क्यों?'
'क्यों इतना पूछते हैं?' सोनल बिदक गई।
'आखिर तुम्हें हुआ क्या है?' मैं झल्ला ही तो पड़ा।
'मैं कमजोर पड़ गई हूँ राइटर। मुझे बख्श दो प्लीज।' सोनल बाकायदा सिसक रही थी, 'जैसा भी था मेरा एक जीवन था, जो सिर्फ मेरा अपना था, उसमें किसी की पूछताछ
नहीं थी, उपेक्षा नहीं थी, अपेक्षा भी नहीं थी। तुमने ये सब चीजें मुझमें जगा दीं राइटर। और मैं नहीं चाहती कि ये सब चीजें मुझमें जाग जाएँ। प्लीज... गुड
नाइट।' सोनल ने फोन काट दिया, एकाएक।
मैं सन्न रह गया। अनजाने ही मैंने एक क्रूर काम कर दिया था। हम लेखक लोग अंततः क्रूर ही होते हैं। उम्मीदें जगा कर फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं।
सचमुच सोनल को मेरे बीत चुके और आने वाले जीवन के बारे में क्या पता था? यह सच है कि चार-पाँच रोज बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे चले जाने के बाद सोनल का
जो जीवन होगा उसमें क्या कोई उससे पूछने वाला होगा कि तू इतनी उदास क्यों है सोनल।
मैंने फिर फोन नंबर घुमाया। फोन एंगेज था। शायद सोनल ने फोन उठा कर रख दिया था।
तभी कमरे की बत्ती चली गई।
अरे? साढ़े नौ बज गए? मैंने सोचा और दोनों हाथों से माथा पकड़ कर बिस्तर पर बैठ गया।
अगले रोज दोपहर मेरे जीवन में एक नया दुख लग गया। पूरन ने मुझे एक नीले रंग का खूबसूरत कागज दिया। उस पर लिखा था - 'राइटर! मैं यह चिकित्सालय छोड़ कर जा रही
हूँ। हममें से किसी एक को इस तरह जाना ही था। तुम तो संवेदनशील हो। सहृदय हो। हो सके तो, इस तरह छोड़ कर जाने के लिए, माफ कर देना। तुम्हारी - रिमोट एरिया
की महारानी।'
'पूरन, मुझे एक हर्बल टी पिला सकते हो?' मैंने पूछा
'नहीं साब।' पूरन ने सपाट-सा जवाब दिया।
'शटअप।' मैं बड़बड़ाया और पार्क में जा कर एक झूले पर लेट गया।
उसी समय मुझे ढूँढ़ते हुए रिसेप्शन वाले शर्मा जी आ गए। 'देव साब, अपने घर पर फोन करें। भाभी जी का फोन था। जरूरी बात करनी है।'
नीलम ने जो बताया उससे मेरे रहे सहे होश भी जाते रहे।
मालिकों ने हमारी पत्रिका अपने फर्नीचर और कर्मचारियों सहित दिल्ली के किसी सेठ को बेच दी थी। कर्मचारी संगठित हो कर लेबर कोर्ट में जा रहे थे और चाहते थे
कि इस लड़ाई में मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊँ। मुझे तत्काल बुलाया गया था।
000
शाम को मैं डॉक्टर से विदा ले रहा था। डॉक्टर ने जयपुर तक के लिए अपनी गाड़ी का इंतजाम कर दिया था। जयपुर में मेरा एक दोस्त रात की किसी फ्लाइट का टिकट ले
कर प्रतीक्षारत था।
'मैं तो जा ही रहा था सोनल।' मैंने सोचा, 'तुम क्यों चली गईं?'
'सचमुच बहुत सुख मिला यहाँ।' मैंने डॉक्टर से हाथ मिलाया और कार में बैठ गया। सुरक्षा अधिकारियों ने चिकित्सालय का विशाल द्वार खोल दिया।
बाहर दुख था।
|