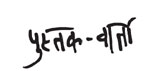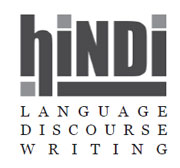|
फाल्गुनी पूर्णिमा का चन्द्र
गंगा के शुभ्र वक्ष पर आलोक-धारा का सृजन कर रहा था। एक छोटा-सा बजरा
वसन्त-पवन में आन्दोलित होता हुआ धीरे-धीरे बह रहा था। नगर का
आनन्द-कोलाहल सैकड़ों गलियों को पार करके गंगा के मुक्त वातावरण में
सुनाई पड़ रहा था। मनोहरदास हाथ-मुँह धोकर तकिये के सहारे बैठ चुके
थे। गोपाल ने ब्यालू करके उठते हुए पूछा-
बाबूजी, सितार ले आऊँ?
आज और कल, दो दिन नहीं। -मनोहरदास ने कहा।
वाह! बाबूजी, आज सितार न बजा तो फिर बात क्या रही!
नहीं गोपाल, मैं होली के इन दो दिनों में न तो सितार ही बजाता हूँ और
न तो नगर में ही जाता हूँ।
तो क्या आप चलेंगे भी नहीं, त्योहार के दिन नाव पर ही बीतेंगे, यह तो
बड़ी बुरी बात है।
यद्यपि गोपाल बरस-बरस का
त्योहार मनाने के लिए साधारणत: युवकों की तरह उत्कण्ठित था; परन्तु
सत्तर बरस के बूढ़े मनोहरदास को स्वयं बूढ़ा कहने का साहस नहीं रखता।
मनोहरदास का भरा हुआ मुँह, दृढ़ अवयव और बलिष्ठ अंग-विन्यास गोपाल के
यौवन से अधिक पूर्ण था। मनोहरदास ने कहा-
गोपाल! मैं गन्दी गालियों या रंग से भगता हूँ। इतनी ही बात नहीं,
इसमें और भी कुछ है। होली इसी तरह बिताते मुझे पचास बरस हो गये।
गोपाल ने नगर में जाकर उत्सव देखने का कुतूहल दबाते हुए पूछा-ऐसा
क्यों बाबूजी?
ऊँचे तकिये पर चित्त लेकर
लम्बी साँस लेते हुए मनोहरदास ने कहना आरम्भ किया-
हम और तुम्हारे बड़े भाई गिरिधरदास साथ-ही-साथ जवाहिरात का व्यवसाय
करते थे। इस साझे का हाल तुम जानते ही हो। हाँ, तब बम्बई की दूकान न
थी और न तो आज-जैसी रेलगाड़ियों का जाल भारत में बिछा था; इसलिए रथों
और इक्कों पर भी लोग लम्बी-लम्बी यात्रायें करते। विशाल सफेद अजगर-सी
पड़ी हुई उत्तरीय भारत की वह सड़क, जो बंगाल से काबुल तक पहुँचती है
सदैव पथिकों से भरी रहती थी। कहीं-कहीं बीच में दो-चार कोस की
निर्जनता मिलती, अन्यथा प्याऊ, बनिये की दूकानें, पड़ाव और सरायों से
भरी हुई इस सड़क पर बड़ी चहल-पहल रहती। यात्रा के लिए प्रत्येक स्थान
में घण्टे में दस कोस जानेवाले इक्के तो बहुतायत से मिलते। बनारस
इसमें विख्यात था।
हम और गिरिधरदास होलिकादाह का उत्सव देखकर दस बजे लौटे थे कि प्रयाग
के एक व्यापारी का पत्र मिला। इसमें लाखों के माल बिक जाने की आशा थी
और कल तक ही वह व्यापारी प्रयाग में ठहरेगा। उसी समय इक्केवान को
बुलाकर सहेज दिया और हम लोग ग्यारह बजे सो गये। सूर्य की किरणें अभी
न निकली थी; दक्षिण पवन से पत्तियाँ अभी जैसे झूम रही थीं, परन्तु हम
लोग इक्के पर बैठकर नगर को कई कोस पीछे छोड़ चुके थे। इक्का बड़े वेग
में जा रहा था। सड़क के दोनो ओर लगे हुए आम की मञ्जरियों की सुगन्ध
तीव्रता से नाक में घुस कर मादकता उत्पन्न कर रही थी। इक्केवान की
बगल में बैठे हुए रघुनाथ महाराज ने कहा-सरकार बड़ी ठण्ड है।
कहना न होगा कि रघुनाथ महाराज बनारस के एक नामी लठैत थे। उन दिनों
ऐसी यात्राओं में ऐसे मनुष्यों का रखना आवश्यक समझा जाता था।
सूर्य बहुत ऊपर आ चुके थे, मुझे प्यास लगी थी। तुम तो जानते ही हो,
मैं दोनो बेला बूटी छानता हूँ। आमों की छाया में एक छोटा-सा कुँआ
दिखाई पड़ा, जिसके ऊपर मुरेरेदार पक्की छत थी और नीचे चारों ओर
दालाने थीं। मैंने इक्का रोक देने को कहा। पूरब वाली दालान में एक
बनिये की दूकान थी, जिसपर गुड़, चना, नमक, सत्तू आदि बिकते थे। मेरे
झोले में सब आवश्यक सामान थे। सीढिय़ों से चढ़ कर हम लोग ऊपर पहुँचे।
सराय यहाँ से दो कोस और गाँव कोस भर पर था। इस रमणीय स्थान को देखकर
विश्राम करने की इच्छा होती थी। अनेक पक्षियों की मधुर बोलियों से
मिलकर पवन जैसे सुरीला हो उठा। ठण्डई बनने लगी। पास ही एक नीबू का
वृक्ष खूब फूला हुआ था। रघुनाथ ने बनिये से हांड़ी लेकर कुछ फूलों को
भिगो दिया। ठण्डई तैयार होते-होते उसकी महक से मन मस्त हो गया। चाँदी
के गिलास झोली से बाहर निकाले गये; पर रघुनाथ ने कहा-सरकार, इसकी
बहार तो पुरवे में है। बनिये को पुकारा। वह तो था नहीं, एक धीमा स्वर
सुनाई पड़ा-क्या चाहिए?
पुरवे दे जाओ!
थोड़ी ही देर में एक चौदह वर्ष की लडक़ी सीढिय़ों से ऊपर आती हुई नजर
पड़ी। सचमुच वह सालू की छींट पहने एक देहाती लडक़ी थी, कल उसकी भाभी
ने उसके साथ खूब गुलाल खेला था, वह जगी भी मालूम पड़ती
थी-मदिरा-मन्दिर के द्वार-सी खुली हुई आँखों में गुलाल की गरद उड़
रही थी। पलकों के छज्जे और बरौनियों की चिकों पर भी गुलाल की बहार
थी। सरके हुए घूँघट से जितनी अलकें दिखलाई पड़तीं, वे सब रँगी थीं।
भीतर से भी उस सरला को कोई रंगीन बनाने लगा था। न जाने क्यों, इस
छोटी अवस्था में ही वह चेतना से ओत-प्रोत थी। ऐसा मालूम होता था कि
स्पर्श का मनोविकारमय अनुभव उसे सचेष्ट बनाये रहता, तब भी उसकी आँखे
धोखा खाने ही पर ऊपर उठतीं। पुरवा रखने ही भर में उसने अपने कपड़ों
को दो-तीन बार ठीक किया, फिर पूछा-और कुछ चाहिए? मैं मुस्करा कर रह
गया। उस वसन्त के प्रभाव में सब लोग वह सुस्वादु और सुगन्धित ठण्डई
धीरे-धीरे पी रहे थे और मैं साथ-ही-साथ अपनी आँखों से उस बालिका के
यौवनोन्माद की माधुरी भी पी रहा था। चारों ओर से नीबू के फूल और आमों
की मञ्जरियों की सुगन्ध आ रही थी। नगरों से दूर देहातों से अलग कुँए
की वह छत संसार में जैसे सबसे ऊँचा स्थान था। क्षण भर के लिए जैसे उस
स्वप्न-लोक में एक अप्सरा आ गई हो। सड़क पर एक बैलगाड़ी वाला बन्डलों
से टिका हुआ आँखे बन्द किये हुए बिरहा गाता था। बैलों के हाँकने की
जरूरत नहीं थी। वह अपनी राह पहचानते थे। उसके गाने में उपालम्भ था,
आवेदन था। बालिका कमर पर हाथ रक्खे हुए बड़े ध्यान से उसे सुन रही
थी। गिरिधरदास और रघुनाथ महाराज हाथ-मुँह धो आये; पर मैं वैसे ही
बैठा रहा। रघुनाथ महाराज उजड्ड तो थे ही; उन्होंने हँसते हुए पूछा-
क्या दाम नहीं मिला?
गिरधरदास भी हँस पड़े। गुलाब से रंगी हुई उस बालिका की कनपटी और भी
लाल हो गई। वह जैस सचेत-सी होकर धीरे-धीरे सीढ़ी से उतरने लगी। मैं
भी जैसे तन्द्रा से चौंक उठा और सावधान होकर पान की गिलौरी मुँह में
रखता हुआ इक्के पर आ बैठा। घोड़ा अपनी चाल से चला। घण्टे-डेढ़ घण्टे
में हम लोग प्रयाग पहुँच गये। दूसरे दिन जब हम लोग लौटे, तो देखा कि
उस कुएँ की दालान में बनिये की दूकान नहीं है। एक मनुष्य पानी पी रहा
था, उससे पूछने पर मालूम हुआ कि गाँव में एक भारी दुर्घटना हो गयी
है। दोपहर को धुरहट्टा खेलने के समय नशे में रहने के कारण कुछ लोगों
में दंगा हो गया। वह बनिया भी उन्हीं में था। रात को उसी के मकान पर
डाका पड़ा। वह तो मार ही डाला गया, पर उसकी लडक़ी का भी पता नहीं।
रघुनाथ ने अक्खड़पन से कहा-अरे, वह महालक्ष्मी ऐसी ही रहीं। उनके लिए
जो कुछ न हो जाय, थोड़ा है।
रघुनाथ की यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। मेरी आँखों के सामने चारों ओर
जैसे होली जलने लगी। ठीक साल भर बाद वही व्यापारी प्रयाग आया और मुझे
फिर उसी प्रकार जाना पड़ा। होली बीत चुकी थी, जब मैं प्रयाग से लौट
रहा था, उसी कुएँ पर ठहरना पड़ा। देखा तो एक विकलांग दरिद्र युवती
उसी दालान में पड़ी थी। उसका चलना-फिरना असम्भव था। जब मैं कुएँ पर
चढऩे लगा, तो उसने दाँत निकालकर हाथ फैला दिया। मैं पहचान गया-साल भर
की घटना सामने आ गयी। न जाने उस दिन मैं प्रतिज्ञा कर बैठा कि आज से
होली न खेलूँगा।
वह पचास बरस की बीती हुई घटना आज भी प्रत्येक होली में नई होकर सामने
आती है। तुम्हारे बड़े भाई गिरिधर ने मुझे कई बार होली मनाने का
अनुरोध किया, पर मैं उनसे सहमत न हो सका और मैं अपने हृदय के इस
निर्बल पक्ष पर अभी तक दृढ़ हूँ। समझा न, गोपाल! इसलिए मैं ये दो दिन
बनारस के कोलाहल से अलग नाव पर ही बिताता हूँ।
-- |