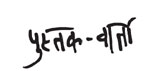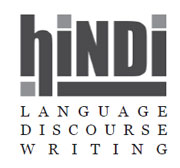|
कहानी |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
उस धूसर सन्नाटे में
कहानी 25 दिसंबर 1956, मेरठ, उत्तर प्रदेश ई-मेल dhirendraasthana@yahoo.com फोन करनेवाले ने जब आर्द्र स्वर में सूचना दी कि ब्रजेंद्र बहादुर सिंह
थोड़ी देर पहले गुजर गए तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उनका मरना तो उसी रात तय हो गया था, जब आसमान पर मटमैले बादल छाए हुए थे और
सड़कों पर धूल−भरी आँधी मचल रही थी। अखबारों में मौसम की भविष्यवाणी सुबह ही की
जा चुकी थी। अफवाह थी कि लोकल ट्रेनें बंद होनेवाली हैं। गोराई की खाड़ी के
आसपास मूसलाधार बारिश के भी समाचार थे। कोलाबा हालाँकि अभी शांत था लेकिन आजाद
मैदान धूल के बवंडरों के बीच सूखे पत्ते सा खड़खड़ा रहा था। यह रात के ग्यारह बजे का समय था। क्लब में उदासीनता और थकान एक साथ तारी हो
चुकी थीं। लास्ट ड्रिंक की घंटी साढ़े दस बजे बज गई थी - नियमानुसार, हालाँकि
आज उसकी जरूरत नहीं थी। क्लब की चहल-पहल के सामने, ऐन उसकी छाती पर, मौसम उस
रात शायद पहली बार प्रेत-बाधा सा बन कर अड़ गया था। इसलिए क्लब शुरू से ही
वीरान और बेरौनक नजर आ रहा था। उस दिन मुंबई के दफ्तर शाम से पहले ही सूने हो गए थे। हर कोई लोकल के बंद हो
जाने से पहले ही अपने घर के भीतर पहुँच कर सुरक्षित हो जाने की हड़बड़ी में था।
भारी बारिश और लोकल जाम - यह मुंबईवासियों की आदिम दहशत का सर्वाधिक असुरक्षित
और भयाक्रांत कोना था, जिसमें एक पल भी ठहरना चाकुओं के बीच उतर जाने जैसा था।
और ऐसे मौसम में भी ब्रजेंद्र बहादुर सिंह शाम सात बजे ही क्लब चले गए थे।
क्लब उनके जीवन में धमनियों की तरह था - सतत जाग्रत, सतत सक्रिय। क्लब के वेटर
बताते थे कि ब्रजेंद्र बहादुर सिंह पश्चिम रेलवे के ट्रैक पर बने मुंबई के सबसे
अंतिम स्टेशन दहिसर में बने अपने दो कमरोंवाले फ्लैट से निकल कर इतवार की शाम
को भी आजाद मैदान के पास बने इस क्लब में चले आते थे। सो, उस शाम विपरीत मौसम
के बावजूद, ब्रजेंद्र बहादुर सिंह क्लब में जिद की तरह मौजूद थे। करीब ग्यारह बजे उन्होंने खिड़की का पर्दा सरका कर आजाद मैदान के आसमान की
तरफ ताका था। नहीं, उस ताकने में कोई दुश्चिंता नहीं छिपी थी। वह ताकना लगभग
उसी तरह का था जैसे कोई काम न होने पर हम अपनी उँगलियाँ चटकाने लगते हैं लेकिन
सुखी इस तरह हो जाते हैं जैसे बहुत देर से छूटा हुआ कोई काम निपटा लिया गया हो।
आसमान पर एक धूसर किस्म का सन्नाटा पसरा हुआ था और आजाद मैदान निपट खाली था
- वर्षों से उजाड़ पड़ी किसी हवेली के अराजक और रहस्यमय कंपाउंड सा। विषाद जैसा
कुछ ब्रजेंद्र बहादुर सिंह की आँखों में उतरा और उन्होंने हाथ में पकड़े गिलास
से रम का एक छोटा घूँट भरा फिर वह उसी गिलास में एक लार्ज पेग और डलवा कर टीवी
के सामने आ बैठ गए - रात ग्यारह के अंतिम समाचार सुनने। ब्रजेंद्र बहादुर सिंह क्लब के नियमों से ऊपर थे। उन्हें साढ़े दस बजे के
बाद भी शराब मिल जाती थी, चुपके−चुपके, फिर आज तो क्लब वैसे भी सिर्फ उन्हीं से
गुलजार था। छह वेटर और ग्राहक दो, एक ब्रजेंद्र बहादुर सिंह और दूसरा मैं। मैं दफ्तर में उनका सहयोगी था और उनके फ्लैट से एक स्टेशन पहले बोरीवली में
किराए के एक कमरे में रहता था। उतरते वह भी बोरीवली में ही थे और वहाँ से ऑटो
पकड़ कर अपने फ्लैट तक चले जाते थे। मैं उनका दोस्त तो था ही, एक सुविधा भी था।
सुबह ग्यारह बजे से रात ग्यारह, बारह और कभी−कभी एक बजे तक उनके संग-साथ और
निर्भरता की सुविधा। हाँ, निर्भरता भी क्योंकि कभी-कभी जब वह बांद्रा आने तक ही
सो जाते थे तो मैं ही उन्हें बोरीवली में जगा कर दहिसर के ऑटो में बिठाया करता
था। मेरे परिचितों में जहाँ बाकी लोग नशा चढ़ने पर गाली-गलौज करने लगते थे या
वेटरों से उलझ पड़ते थे वहीं ब्रजेंद्र बहादुर सिंह चुपचाप सो जाते थे। कई बार
वह क्लब में ही सो जाते थे और जगाने पर 'लास्ट फॉर द रोड' बोल कर एक पेग और
मँगा कर पी लेते थे। कई बार तो मैंने यह भी पाया था कि अगर वह लास्ट पेग माँगना
भूल कर लड़खड़ाते-से चल पड़ते थे, तो क्लब के बाहरी गेट की सीढ़ियों पर कोई
वेटर भूली हुई मुहब्बत-सा प्रकट हो जाता था - हाथ में उनका लास्ट पेग लिए। ऐसे क्षणों में ब्रजेंद्र सिंह भावुक हो जाते थे, बोलते वह बहुत कम थे,
धन्यवाद भी नहीं देते थे। सिर्फ कृतज्ञ हो उठते थे। उनके प्रति वेटरों के इस
लगाव को देख बहुत से लोग खफा रहते थे। लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता था कि
क्लब के हर वेटर के घर में उनके द्वारा दिया गया कोई न कोई उपहार अवश्य मौजूद
था - बॉल पेन से ले कर कर कमीज तक और पेंट से ले कर घड़ी तक। नहीं, ब्रजेंद्र बहादुर सिंह रईस नहीं थे। जिस कंपनी में वह परचेज ऑफीसर थे,
वहाँ उपहारों का आना मामूली बात थी। यही उपहार वह अपने शुभचिंतकों को बाँट देते
थे। फिर वह शुभचिंतक चाहे क्लब का वेटर हो या उस बिल्डिंग का दरबान, जिसमें
उनका छोटा सा, दो कमरोंवाला फ्लैट था। फिलीपींस में असेंबल हुई एक कीमती
रिस्टवाच उस वक्त मेरी कलाई में भी दमक रही थी जब ब्रजेंद्र बहादुर सिंह आजाद
मैदान के आसमान में टँगे उस सन्नाटे से टकरा कर टीवी के सामने आ बैठ गए थे -
अंतिम समाचार सुनने। कुछ अरसा पहले एक गिफ्ट मे कर उन्हें यह घड़ी दे गया था। जिस क्षण वह
खूबसूरत रैपर को उतार कर उस घड़ी को उलट-पुलट रहे थे, ठीक उसी क्षण मेरी नजर
उनकी तरफ चली गई थी। मुझसे आँख मिलते ही वह तपाक से बोले थे - 'तुम ले लो। मेरे
पास तो है।' यह दया नहीं थी। यह उनकी आदत थी। उनका कहना था कि ऐसा करके वह अपने बचपन के
बुरे दिनों से बदला लेते हैं। सिर्फ उपहार में प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से ही
नहीं, अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित धन को भी वह इसी तरह नष्ट करते थे। एक सीमित,
बँधी तनख्वाह के बावजूद टैक्सी और ऑटो में चलने के पीछे भी उनका यही तर्क काम
कर रहा होता था। सुनते हैं कि अपने बचपन में ब्रजेंद्र बहादुर सिंह अपने घर से अपने स्कूल की
सात किलोमीटर की दूरी पैदल नापा करते थे क्योंकि तब उनके पास बस का किराया दो
आना नहीं होता था। टीवी के सामने बैठे ब्रजेंद्र बहादुर सिंह अपना लास्ट पेग ले रहे थे और मैं
टॉयलेट गया हुआ था। लौटा तो क्लब का मरघटी सन्नाटा एक अविश्वसनीय शोरगुल और
अचरज के बीच खड़ा काँप रहा था, पता चला ब्रजेंद्र बहादुर सिंह ने अपने सबसे
चहेते वेटर हनीफ को चाँटा मार दिया था। जिंदगी के निचले पायदानों पर लटके-अटके हुए लोग, क्रांति की भाषा में उनके
पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अगर प्रतिक्रियास्वरूप सारे वेटर एक हो जाएँ और
उस सुनसान रात में एक चाँटा भी ब्रजेंद्र बहादुर सिंह को जड़ दें तो उसकी आवाज
पूरे शहर में कोलाहल की तरह गूँज सकती थी और मीमो बन कर ब्रजेंद्र बहादुर सिंह
के बेदाग कैरियर में पैबंद की तरह चिपक सकती थी। ऐसा कैसे संभव है? मैं पूरी तरह बौराया हुआ था और अविश्वसनीय नजरों से
उन्हें घूर रहा था। अब तक अपना चेहरा उन्होंने अपने दोनों हाथों में छुपा लिया
था। क्या हुआ? मैंने उन्हें छुआ। यह मेरा एक सहमा हुआ-सा प्रयत्न था। लेकिन वह
उलझी हुई गाँठ की तरह खुल गए। उस निर्जन और तूफानी रात के नशीले एकांत में मैंने देखा अपने जीवन का सबसे
बड़ा चमत्कार। वह चमत्कार था या रहस्य। रहस्य था या दर्द। वह जो भी था इतना
निष्पाप और सघन था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ब्रजेंद्र बहादुर सिंह के अधेड़ और अनुभवी चेहरे पर दो गोल, पारदर्शी आँसू
ठहरे हुए थे और उनकी गहरी, भूरी आँखें इस तरह निस्संग थीं, मानों आँसू लुढ़का
कर निर्वाण पा चुकी हों। दोनों घुटनों पर अपने दोनों हाथों का बोझ डाल कर वह
उठे। जेब से क्लब का सदस्यता कार्ड निकाला। उसके चार टुकड़े कर हवा में उछाले
और कहीं दूर किसी चट्टान से टकरा कर क्षत-विक्षत हो चुकी भर्राई आवाज में बोले
-'चलो, अब हम यहाँ कभी नहीं आएँगे।' 'लेकिन हुआ क्या?' मैं उनके पीछे-पीछे हैरान-परेशान स्थिति में लगभग घिसटता
सा क्लब की सीढ़ियों पर पहुँचा। बाहर बारिश होने लगी थी। वह उसी बारिश में भीगते हुए स्थिर कदमों से क्लब का
कंपाउड पार कर मुख्य दरवाजे पर आ खड़े हुए थे। अब बाहर धूल के बवंडर नहीं,
लगातार बरसती बारिश थी और ब्रजेंद्र सिंह उस बारिश में किसी प्रतिमा की तरह
निर्विकार खड़े थे। निर्विकार और अविचलित। यह रात का ग्यारह बीस का समय था और
सड़क पर एक भी टैक्सी उपलब्ध नहीं थी। मुख्य द्वार के कोने पर स्थित पानवाले की
गुमटी भी बंद थी और बारिश धारासार हो चली थी। 'मुझे भी नहीं बताएँगे?' मैंने उत्सुक लेकिन भर्राई आवाज में पूछा। बारिश की
सीधी मार से बचने के लिए मैंने अपने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की फाइल को सिर पर
तान लिया था और उनकी बगल में आ गया था, जहाँ दुख का अँधेरा बहुत गाढ़ा और
चिपचिपा हो चला था। 'वो साला हनीफ बोलता है कि सुदर्शन सक्सेना मर गया तो क्या हुआ? रोज कोई न
कोई मरता है। सुदर्शन 'कोई' था?' ब्रजेंद्र बहादुर सिंह अभी तक थरथरा रहे थे। उनकी आँखें भी बह रही थीं - पता
नहीं वे आँसू थे या बारिश? 'क्या?' मैं लगभग चिल्लाया था शायद, क्योंकि ठीक उसी क्षण सड़क से गुजरती एक
टैक्सी ने च्चीं च्चीं कर ब्रेक लगाया था और पल भर को हमें देख आगे रपट गई थी।
'सुदर्शन मर गया? कब?' मैंने उन्हें लगभग झिंझोड़ दिया। 'अभी, अंतिम समाचारों में एक क्षण की खबर आई थी - प्रख्यात कहानीकार सुदर्शन
सक्सेना का नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद देहांत।'
ब्रजेंद्र बहादुर सिंह समाचार पढ़ने की तरह बुदबुदा रहे थे, 'तुम देखना, कल के
किसी अखबार में यह खबर नहीं छपेगी। उनमें बलात्कार छप सकता है, मंत्री का जुकाम
छप सकता है, किसी जोकर कवि के अभिनंदन समारोह का चित्र छप सकता है लेकिन
सुदर्शन सक्सेना का निधन नहीं छप सकता। छपेगा भी तो तीन लाइन में... मानो सड़क
पर पड़ा कोई भिखारी मर गया हो,' ब्रजेंद्र बहादुर सिंह क्रमशः उत्तेजित होते जा
रहे थे। आज शराब का अंतिम पेग उनकी आँखों में नींद के बजाय गुस्सा उपस्थित किए
दे रहा था। लेकिन यह गुस्सा बहुत ही कातर और नख-दंतविहीन था, जिसे मुंबई के उस
उजाड़ मौसम ने और भी अधिक अकेला और बेचारा कर दिया था। 'और वो हनीफ...' सहसा उनकी आवाज बहुत आहत हो गई, 'तुम टॉयलेट में थे, जब
समाचार आया। हनीफ सोडा रखने आया था... तुम जानते ही हो कि मैंने कितना कुछ किया
है हनीफ के लिए... पहली तारीख को सेलरी ले कर यहाँ आया था जब हनीफ ने बताया था
कि उसकी बीवी अस्पताल में मौत से जूझ रही है...पूरे पाँच सौ रुपए दे दिए थे
मैंने जो आज तक वापस नहीं माँगे... और उसी हनीफ से जब मैंने अपना सदमा शेयर
करना चाहा तो बोलता है आप शराब पियो, रोज कोई न कोई मरता है... गिरीश के केस
में भी यही हुआ था। दिल्ली से खत आया था विकास का कि गिरीश की अंत्येष्टि में
उस समेत हिंदी के कुल तीन लेखक थे। केवल 'वर्तमान' ने उसकी मौत पर आधे पन्ने का
लेख कंपोज करवाया था लेकिन साला वह भी नहीं छप पाया था क्योंकि ऐन वक्त पर ठीक
उसी जगह के लिए लक्स साबुन का विज्ञापन आ गया था... यू नो, हम कहाँ जा रहे
हैं?' सहसा मैं घबरा गया, क्योंकि अधेड़ उम्र का वह अनुभवी, परचेज ऑफीसर, क्लब का
नियमित ग्राहक, बुलंद ठहाकों से माहौल को जीवंत रखनेवाला ब्रजेंद्र बहादुर सिंह
बाकायदा सिसकने लगा था। हमें सिर से पाँव तक पूरी तरह तरबतर कर देने के बाद बारिश थम गई थी, और
ब्रजेंद्र बहादुर सिंह को शायद एक लंबी, गरम नींद की जरूरत थी। ऐसी नींद,
जिसमें वह मनहूस हाहाकार न हो जिसके बीच इस समय ब्रजेंद्र बहादुर सिंह घायल
हिरनी की तरह तड़प रहे थे। तभी एक अजाने वरदान की तरह सामने एक टैक्सी आ कर रुकी और टैक्सी चालक ने
किसी देवदूत की तरह चर्च गेट ले चलना भी मंजूर कर लिया। हम टैक्सी में लद गए।
बारिश फिर होने लगी थी। ब्रजेंद्र बहादुर सिंह टैक्सी की सीट से सिर टिका कर
सो गए थे। उनके थके-थके आहत चेहरे पर एक साबुत वेदना अपने पंख फैला रही थी। ००० फिर करीब छह महीने तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वह दफ्तर से लंबी छुट्टी पर
थे। तीन चार बार मैं अलग-अलग समय पर उनके फ्लैट में गया लेकिन हर बार वहाँ ताला
लटकता पाया। इस बीच देश और दुनिया, समाज और राजनीति, अपराध और संस्कृति के बीच काफी कुछ
हुआ। छोटी बच्चियों से बलात्कार हुए, निरपराधों की हत्याएँ हुईं, कुछ नामी
गुंडे गिरफ्तार हुए, कुछ छूट गए, टैक्सी और ऑटो के किराए बढ़ गए। घर-घर में
स्टार, जी और एमटीवी आ गए। पूजा बेदी कंडोम बेचने लगी और पूजा भट्ट बीयर।
फिल्मों में लव स्टोरी की जगह गैंगवार ने ले ली। कुछ पत्रिकाएँ बंद हो गईं और
कुछ नए शराबघर खुल गए। और हाँ, इसी बीच कलकत्ता में एक, दिल्ली में दो, मुंबई
में तीन और पटना में एक लेखक का कैंसर, हार्ट फेल, किडनी फेल्योर या ब्रेन
ट्यूमर से देहांत हो गया! गाजियाबाद में एक लेखक को गोली मार दी गई और
मुरादाबाद में एक कवि ने आत्महत्या कर ली। ऐसी हर सूचना पर मुझे ब्रजेंद्र बहादुर सिंह बेतरह याद आए। लेकिन वह पता
नहीं कहाँ गायब हो गए थे। क्लब उनके बिना सूली पर चढ़े ईसा-सा नजर आता था! फिर तीन महीने बाद अप्रैल की एक सुबह ब्रजेंद्र बहादुर सिंह दफ्तर में अपनी
सीट पर बैठे नजर आए। दफ्तर के हॉल में घुसने पर जैसे ही मेरी नजर उनकी सीट पर
पड़ी और वे उस पर बैठे दिखाई दिए तो अचरज और खुशी के आधिक्य से मेरा तन−मन लरज
उठा। मैं तो इस बीच उनको लगभग खो देने की पीड़ा के हवाले हो चुका था। लेकिन वह
थे, साक्षात। 'बैठो!' मुझे अपने सामने पा कर उन्होंने अत्यंत संयत और सधे हुए लहजे में
कहा। वे किसी फाइल में नत्थी ढेर सारे कागजों पर दस्तखत करने में तल्लीन थे और
मेरी उत्सुकता थी कि पसीने की मानिंद गर्दन से फिसल कर रीढ़ के सबसे अंतिम
बिंदु पर पहुँच रही थी। मैं चुपचाप, अपनी उत्सुकता में बर्फ-सा गलता हुआ अपने
उस चहेते, अधेड़ दोस्त को अनुभव कर रहा था जो नौ महीने पहले मुंबई की एक मनहूस,
बरसाती रात में मुझसे बिछुड़ गया था और आज, अचानक, बिना पूर्व सूचना के अपनी उस
चिर परिचित सीट पर आ बैठा था जो इन नौ महीनों में निरंतर घटती अनेक घटनाओं के
बावजूद एक जिद्दी प्रतीक्षा में थिर थी। ब्रजेंद्र बहादुर सिंह दुबले हो गए थे। उनकी आँखों के नीचे स्याह थैलियाँ-
सी लटक आई थीं। कनपटियों पर के मेंहदी से भूरे बने बाल झक्क सफेद थे। आँखों पर
नजर का चश्मा था जिसे वह रह-रह कर सीधे हाथ की पहली उँगली से ऊपर सरकाते थे। और
हाँ, दस्तखत करने के दौरान या बीच−बीच में पानी का गिलास उठाते समय उनके हाथ
काँपते थे। उनकी आँखों में एक शाश्वत किस्म की ऐसी निस्संगता थी जो जीवन के
कठिनतम यथार्थ के बीच आकार ग्रहण करती है। नौ महीने बाद लौटे अपने उस पुराने
मित्र को इन नई स्थितियों और अजाने रहस्यों सहित झेलने का माद्दा मेरे भीतर
बहुत देर तक टिका नहीं रह सका। फिर, मुझे भी अपनी सीट पर जा कर अपने कामकाज
देखने थे। 'मिलते हैं।' कह कर मैंने उनके सामने से उठने की कोशिश की तो वे एक अत्यंत
तटस्थ सी 'अच्छा' थमा कर फिर से फाइल के बीच गुम हो गए। मैं अवाक रह गया। उत्सुकता को कब का पाला मार चुका था। फिर सारे दिन दर्द की
ऐंठन से घबरा कर जब-जब मैंने उनकी सीट की तरफ ताका, वह किसी फंतासी की तरह
यथार्थ के बीचोंबीच झूलते से मिले। छत्तीस साल गुजारे थे मैंने इस दुनिया में। उन छत्तीस वर्षों के अपने बेहद
मौलिक किस्म के दुख-दर्द, हर्ष-विषाद, अपमान और सुख थे मेरे खाते में।
नाते-रिश्तेदारों और एकदम करीबी मित्रों के छल-कपट भी थे। प्यार की गर्मी और
ताकत थी तथा बेवफाई के संगदिल और अनगढ़ टुकड़े भी थे। नशीली रातें, बीमार दिन,
सूनी दुपहरियाँ, अश्लील नीली फिल्में और धूल चाटता उत्साह - क्या कुछ तो दर्ज
नहीं हुआ था इन छत्तीस सालों में लेकिन इन छत्तीस कठिन और लंबे वर्षों में मैं
एक पल के लिए भी उतना आंतकित और उदास नहीं हुआ था जितना इस एक छोटे-से लम्हे
में ब्रजेंद्र बहादुर सिंह की वीतरागी उपस्थिति ने मुझे बना डाला था। क्या वह
दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बाहर चले गए हैं? दुनिया देख लेना और दुनिया
से बाहर चले जाना क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या इनका कोई अलग−अलग मतलब
है? नौ महीने बाद वापस लौटे ब्रजेंद्र बहादुर सिंह के पास ऐसे कौन-से रहस्य हैं
जिन्होंने उन्हें इतना रूक्ष और ठंडा बना दिया है? माँ के गर्भ में नौ महीने
बितानेवाला शिशु भी क्या कुछ ऐसे रहस्यों के बीच विचरण करता है जो आज तक अनावृत
नहीं हुए। आखिर किस गर्भ में नौ महीने बिता कर लौटे हैं ब्रजेंद्र बहादुर सिंह।
पूरा एक दिन मेरा सवालों के साथ लड़ते-झगड़ते बीत गया। दो सेरीडॉन सटकने के
बावजूद दर्द माथे पर जोंक-सा चिपटा हुआ था और उधर ब्रजेंद्र बहादुर सिंह की
सदा-बहार-खुशगवार सीट पर जैसे एक दर्जन मुर्दों का मातम कोहरे सा बरस रहा था।
आखिर वह उठे। शाम के सात बजे। दफ्तर साढ़े पाँच बजे खाली हो चुका था। अब तीन
लोग थे - मैं, वे और चपरासी दीनदयाल। मैं रूठा-सा बैठा रहा, उनके उठने के
बावजूद। वे धीरे-धीरे चलते हुए मेरी सीट तक आए। मैंने उन्हें देखा, उन्होंने
मुझे। उनकी आँखों में रोशनी नहीं, राख थी। मैं पल भर के लिए सिहर गया। 'उठो दोस्त!' वे बोले, उनकी आवाज कई सदियों को पार कर आती-सी लग रही थी।
मैंने देखा, वह ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। कभी दाएँ झूल जाते थे, कभी
बाएँ, मानो किसी बाँस पर कोई कुर्ता हवा में अकेला टँगा हो। ००० बिना वार्तालाप का तीसरा पेग चल रहा था और मैं भावुकता के कगार पर आ पहुँचा
था। हम उनके दहिसरवाले फ्लैट में थे - नौ महीने के स्पर्श और संवादहीन अंतराल
के बाद। कमरे में रोशन तीन मोमबत्तियों की लौ एक नंबर पर चलते पंखे की
हल्की−हल्की हवा के बीच पीलिया के मरीज-सी काँप रही थीं। फ्लैट में घुसते ही
उन्होंने बता दिया था कि अब उन्हें अपनी रातें कम से कम रोशनी के बीच ही सुख कर
लगती हैं और पूरा अँधेरा तो उन्हें बुखार में बर्फ की पट्टी-सा अनुभव होता है।
चीजों, रहस्यों और सत्यों को अँधेरे में टटोल−टटोल कर पाने का सुख ही कुछ और
है। आखिर एक घंटे की मुसलसल खामोशी के सामने मेरा धैर्य तड़क गया। शब्दों में
तरलता उँडेलते हुए मैंने धीमे−धीमे कहना शुरू किया, 'आपको मालूम है, आपके सबसे
प्रिय नौजवान कवि ने कुछ समय पहले पंखे से लटक कर जान दे दी।' 'हाँ, यह समाचार मैंने दार्जिलिंग में पढ़ा था।' उन्होंने आहिस्ता से कहा और
चुप हो गए। मैं चकित रह गया। यह वे ब्रजेंद्र बहादुर सिंह नहीं थे जिन्होंने नौ महीने
पहले क्लब में अपने चहेते वेटर हनीफ को चाँटा मार दिया था। 'और... और आपके बचपन के दोस्त, हमप्याला-हमनिवाला शायर विलास देशमुख भी जाते
रहे...' एक सच्चे दुख के ताप के बीच खड़ा मैं पिघल रहा था... 'बहुत कारुणिक अंत
हुआ उनका। घटिया-से अस्पताल में बिना इलाज के मर गए... यहाँ की हिंदी और उर्दू
अकादमियों ने कुछ नहीं किया। वे अंत समय तक यही तय नहीं कर पाईं कि एक
महाराष्ट्रियन व्यक्ति को उर्दू का शायर माना जाए या हिन्दी का गजलगो।' मैंने
क्षुब्ध स्वर में उन्हें जानकारी देनी चाही। ब्रजेंद्र बहादुर सिंह ने गहरी खामोशी के साथ अपने गिलास से रम का एक बड़ा
घूँट भरा और बिना किसी उतार-चढ़ाव के पहले जैसी शांत-स्थिर आवाज में बोले -
'हाँ, उन दिनों मैं देहरादून में था अपनी एक दूर की भतीजी के पास, मुझे कोई
अजीब-सी स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। चालीस दिन तक लगातार सहस्रधारा के गंधकवाले
सोते में नहाता रहा। इस विवाद के बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा था।' अखबार... समाचार... खबर... हर मृत्यु पर वे क्लब के वेटर हनीफ की तरह बोल
रहे थे - क्रूरता की हद तक पहुँची निस्संगता के शिखर पर खड़े हो कर। नहीं, वे
मेरे दोस्त ब्रजेंद्र सिंह तो कतई-कतई नहीं थे। मेरे उस दोस्त की काया में कोई
संवेदनहीन, निर्लज्ज और पथरीला दैत्य प्रवेश पा चुका था। चौथा पेग खत्म करते−करते मेरा जी उचट गया। एक क्षण भी वहाँ बैठना भारी पड़ने
लगा मुझे। मुँह का स्वाद कसैला हो गया था और शब्द मन के भीतर पारे की तरह
थरथराने लगे थे। और फिर मैं उठा। लड़खड़ाते कदमों से बिजली के स्विच बोर्ड के पास जा कर
मैंने सारे बटन दबा दिए। कमरा कई तरह के बल्बों और ट्यूबलाइट की मिली-जुली
रोशनी में नहाता हुआ विचित्र-सी स्थिति में तन गया। साथ ही तन गईं, अब तक किसी
संत की तरह बैठे ब्रजेंद्र सिंह के माथे की नसें। 'ऑफ... लाइट ऑफ!' वे दहाड़ पड़े। यह दहाड़ इतनी भयंकर थी कि डर के मारे
मैंने फौरन ही कमरे को फिर अँधेरे के हवाले कर दिया। 'सर, ब्रजेंद्र बहादुर सिंह, आप तो ऐसे नहीं थे?' मैंने आहत हो कर कहा था और
स्विच बोर्डवाली दीवार से टिक कर जमीन पर पसर गया था, 'जीवन की उस करुणा को
कहाँ फेंक आए आप जो...' 'यंग मैन!' मोमबत्तियों के उस अपाहिज उजाले में ब्रजेंद्र बहादुर सिंह का
भर्राया और गीला स्वर गूँजा - 'किस करुणा की बात कर रहे हो तुम, करुणा की जरूरत
किसे है आज? नौ महीने इस शहर में नहीं था मैं... क्या मेरे बिना इस दुनिया का
काम नहीं चला?' 'वो तो ठीक है सर...' अब तक मेरा स्वर भी आर्द्र हो चुका था। 'कुछ ठीक नहीं है यंगमैन।' उनकी थकी-थकी आवाज उभरी, 'तुम जानते हो कि मेरा
अपना कोई परिवार नहीं है। क्लब में घटी उस घटना के बाद मैं अपनी सारी जमा पूंजी
ले कर यात्रा पर निकल गया था। इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई उम्मीद नजर आए
लेकिन गलत... एकदम गलत... मेरे प्यारे नौजवान दोस्त! संवेदनशील लोगों की जरूरत
किसी को नहीं है और कहीं नहीं है। मुझे समझ में आ गया है कि उस रात हनीफ ने
कितने बड़े सच को मेरे सामने खड़ा किया था। रोज कोई न कोई मरता है... क्या फर्क
पड़ता है कि किसी कवि ने आत्महत्या की या कोई कारीगर रेल से कटा। कवि का मरना
अब कोई घटना नहीं है। वह भी सिर्फ एक खबर है।' 'तो?' मैंने तनिक व्यंग्य के साथ प्रश्न किया। 'तो कुछ नहीं। फिनिश। इसके बाद भी कुछ बचता है क्या?' वे मुझसे ही पूछने लगे
थे। फिर से वही मुर्दा राख उनकी आँखों में उड़ने लगी थी, जिससे मैं डरा हुआ था।
यह मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। नशे में थरथराती उस दार्शनिक सी लगती रात के
दो महीने बाद तक वह फिर दफ्तर नहीं आए थे। कुछ व्यस्तता के कारण और कुछ उनको
बर्दाश्त न कर पाने की कमजोरी के कारण मैं स्वयं भी उनकी तरफ नहीं जा सका था।
और अब यह सूचना कि ब्रजेंद्र बहादुर सिंह चल बसे। मैंने बताया न, मुझे
आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि उनका मरना तो उसी रात तय हो गया था जब आजाद मैदान के
आसमान पर वह धूसर सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस रात उन्होंने क्लब के वेटर हनीफ के
गाल पर चाँटा मारा था। उसी रात जब रात के अंतिम समाचारों की अंतिम पंक्ति में
दूरदर्शन वालों ने सुदर्शन सक्सेना के देहाँत की खबर दी थी और सर ब्रजेंद्र
बहादुर सिंह निपट अकेले थे। नहीं, सर ब्रजेंद्र बहादुर सिंह लेखक या कवि या कलाकार नहीं थे। वह तो एक
व्यावसायिक कम्पनी में परचेज ऑफीसर थे। लेकिन उनका दुर्भाग्य कि वह उन किताबों के साथ बड़े हुए थे जिनकी अब इस
दुनिया में कोई जरूरत नहीं रही।
|