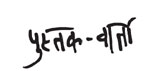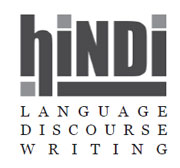|
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रंथावली -1
मलिक मुहम्मद जायसी
प्रथम संस्करण का वक्तव्य
'पद्मावत' हिन्दी के सर्वोत्तम प्रबन्धकाव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के
माधुर्य और भावों की गम्भीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। पर खेद के
साथ कहना पड़ता है कि इसके पठनपाठन का मार्ग कठिनाइयों के कारण अब तक बन्द
सा रहा। एक तो इसकी भाषा पुरानी और ठेठ अवधी, दूसरे भाव भी गूढ़, अत: किसी
शुद्ध अच्छे संस्करण के बिना इसके अध्यनयन का प्रयास कोई कर भी कैसे सकता
था? पर इसका अध्यायन हिन्दी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है, यह
इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढाँचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी
तुलसीदासजी ने अपने लोकप्रसिद्ध ग्रन्थ 'रामचरितमानस' की रचना की। यही अवधी
भाषा और चौपाई दोहे का क्रम दोनों में है, जो आख्यानकाव्यों के लिए हिन्दी
में संभवत: पहले से चला आता रहा हो। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी
और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी के भाषा के स्वरूप को
पूर्णतया समझने के लिये जायसी की भाषा का अध्यायन आवश्यक है।
इस ग्रन्थ के चार संस्करण मेरे देखने में आए हैं -एक नवलकिशोर प्रेस का,
दूसरा पं. रामजसन मिश्र सम्पादित काशी के चन्द्रप्रभा प्रेस का, तीसरा
कानपुर के किसी पुराने प्रेस का फारसी अक्षरों में और म. प. पं. सुधाकर
द्विवेदी और डॉक्टर ग्रियर्सन सम्पादित एशियाटिक सोसाइटी का जो पूरा नहीं,
तृतीयांश मात्र है।
इनमें से प्रथम दो संस्करण तो किसी काम के नहीं। एक चौपाई का भी पाठ शुद्ध
नहीं, शब्द बिना इस विचार के रखे हुए हैं कि उनका कुछ अर्थ भी हो सकता है
या नहीं। कानपुरवाले उर्दू संस्करण को कुछ लोगों ने अच्छा बताया। पर देखने
पर वह भी इसी श्रेणी का निकला। उसमें विशेषता केवल इतनी ही है कि चौपाइयों
के नीचे अर्थ भी दिया हुआ दिखाई पड़ता है। यह अर्थ भी अटकलपच्चू है किसी
मुंशी या मौलवी साहब ने प्रसंग के अनुसार अंदाज से ही लगाया है, शब्दार्थ
की ओर ध्यामन देकर नहीं। कुछ नमूने देखिए-
1. 'जाएउ नागमती नगसेनहि। ऊँच भाग, ऊँचै दिन रैनहि।'
इसका साफ अर्थ यह है कि नागमती ने नागसेन को उत्पन्न किया; उसका भाग्य ऊँचा
था और दिन रात ऊँचा ही होता गया। इसके स्थान पर यह विलक्षण अर्थ किया गया
है-
'फिर नागमती अपनी सहेलियों को हमराह लेकर बहुत बलंद मकान में बलंदीए बख्त
से रहने लगी'। इसी प्रकार 'कवलसेन पदमावती जाएउ' का अर्थ लिखा गया है ''और
पदमावत मिस्ल कवल के थी, अपने मकान में गई''। बस दो नमूने और देखिए-
2. 'फेरत नैन चेरि सौ छूटी। भइ कूटन कुटनी तस कूटी'।
इसका ठीक अर्थ यह है कि पद्मावती के दृष्टि फेरते ही सौ दासियाँ छूटी और उस
कुटनी को खूब मारा। पर 'चेरि' को 'चीर' समझकर इसका यह अर्थ किया गया है-
'अगर वह ऑंखें फेर के देखे तो तेरा लहँगा खुल पड़े और जैसी कुटनी है, वैसा
ही तुझको कूटे'।
3. 'गढ़ सौंपा बादल, कहँ, गए टिकठि बसि देव'।
ठीक अर्थ-चित्तौरगढ़ बादल को सौंपा और टिकठी या अरथी पर बसकर राजा (परलोक)
गए।
कानपुर की प्रति में इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है-'किलअ बादल को सौंपा
गया और बासदेव सिधारे''। बस इन्हीं नमूनों से अर्थ का और अर्थ करनेवाले का
अन्दाज कर लीजिए।
अब रहा चौथा, सुधाकरजी और डॉक्टर ग्रियर्सन साहब वाला भड़कीला संस्करण।
इसमें सुधाकरजी की बड़ी लम्बी चौड़ी टीका टिप्पणी लगी हुई है; पर दुर्भाग्य
से या सौभाग्य से 'पद्मावत' के तृतीयांश तक ही यह संस्करण् पहुँचा। इसकी
तड़क भड़क का तो कहना ही क्या है। शब्दार्थ, टीका और इधर उधर के किस्सों और
कहानियों से इसका डीलडौल बहुत बड़ा हो गया है। पर टिप्पणियाँ अधिकतर अशुद्ध
और टीका स्थान स्थान पर भ्रमपूर्ण है। सुधाकरजी में एक गुण यह सुना जाता है
कि यदि कोई उनके पास कोई कविता अर्थ पूछने के लिए ले जाता तो वह विमुख नहीं
लौटता था। वे खींच तानकर कुछ न कुछ अर्थ लगा ही देते थे। बस, इसी गुण से इस
टीका में भी काम लिया गया है। शब्दार्थ में कहीं यह नहीं स्वीकार किया गया
है कि इस शब्द से टीकाकार परिचित नहीं। सब शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ मौजूद
है, चाहे वह अर्थ ठीक हो या न हो। शब्दार्थ के कुछ नमूने देखिए-
1. ताईं = तिन्हें (कीन्ह खंभ दुइ जग के ताईं)। 2. आछहि =अच्छा (बिरिछ जो
आछहि चंदन पासा)। 3. ऍंबरउर =आम्रराज, अच्छे जाति का आम या अमरावती। 4.
सारउ =सास, दूर्वा, दूब (सारिउ सुआ जो रहचह करहीं)। 5. खड़वानी =गडुवा,
झारी। 6. अहूठ = अनुत्थ, न उठने योग्य। 7. कनक कचोरी =कनिक या आटे की
कचौड़ी। 8. करसी = कर्षित की, खिंचवाई (सिर करवत, तन करसी बहुत सीझ तेहि
आस)।
कहीं कहीं अर्थ ठीक बैठाने के लिए पाठ भी विकृत कर दिया गया है, जैसे,
'कतहु चिरहटा पंखिन्ह लावा' का 'कतहु छरहठा पेखन्ह लावा' कर दिया गया है और
'छरहटा' का अर्थ किया गया है 'क्षार लगानेवाले' 'नकल करनेवाले'। जहाँ 'गथ'
शब्द आया है (जिसे हिन्दी कविता का साधारण ज्ञान रखनेवाले भी जानते हैं)
वहाँ 'गंठि' कर दिया गया है। इसी प्रकार 'अरकाना' (अटकाने दौलत अर्थात्
सरदार या उमरा) 'अरगाना' करके 'अलग होना' अर्थ किया गया है।
स्थान स्थान पर शब्दों की व्युत्पत्ति भी दी हुई मिलती है जिसका न दिया
जाना ही अच्छा था। उदाहरण के लिए दो शब्द ही काफी है-
पउनारि-पयोनाली, कमल की डंडी।
अहुठ-अनुत्थ, न उठने योग्य।
'पौनार' शब्द की ठीक व्युत्पत्ति इस प्रकार है-सं. पि+नाल = प्रा.पउम्+नाल=
हिं., पउनाड़ या पौनार। इसी प्रकार अहुठ =सं. अर्धाचतुर्थ'1
प्रा. अज्हुट्ठ, अहवे =हिं. अहुठ (साढ़े तीन, 'हूँठा' शब्द इसी से बना है)।
शब्दार्थों से ही टीका का अनुमान भी किया जा सकता है, फिर भी मनोरंजन के
लिए कुछ पद्यों की टीका नीचे दी जाती है-
1. अहुठ हाथ तन सरवर, हिया कवल तेहि माँझ।
सुधाकरी अर्थ-राजा कहता है कि (मेरा) हाथ तो अहुठ अर्थात् शक्ति के लग जाने
से सामर्थ्यहीन होकर बेकाम हो गया और (मेरा) तनु सरोवर है जिसके हृदय मध्य
अर्थात् बीच में कमल अर्थात् पद्मावती बसी हुई है।
ठीक अर्थ-साढ़े तीन हाथ का शरीररूपी सरोवर है जिसके मध्यस में हृदय रूपी कमल
है।
2. हिया थार कुच कंचन लारू। कनक कचोरि उठे जनु चारू।
सुधाकरी अर्थ-हृदय थार में कुच कंचन का लड्डू है। (अथवा) जानों बल करके
कनिक (आटे) की कचौरी उठती है अर्थात् फूल रही है (चक्राकार उठते हुए स्तन
कराही में फूलती हुई बदामी रंग की, कचौरी से जान पड़ते हैं)।
ठीक अर्थ-मानो सोने के सुन्दर कटोरे उठे हुए (औंधे) हैं।
1. एक शब्द 'अध्युसष्ट ' भी मिलता है पर वह केवल प्राकृत 'अवझुट्ठ' की
व्युत्पत्ति के लिए गढ़ा हुआ जान पड़ता है।
3. धानुक आप, बेझ जग कीन्हा।
'बेझ का अर्थ ज्ञात न होने के कारण आपने 'बोझ' पाठ कर दिया और इस प्रकार
टीका कर दी-
सुधाकरी अर्थ-आप धानुक अर्थात् अहेरी होकर जग (के प्राणी) के बोझ कर लिया
अर्थात् जगत् के प्राणियों को भ्रूधनु और कटाक्षबाण से मारकर उन प्राणियों
का बोझा अर्थात् ढेर कर दिया।
ठीक अर्थ-आप धनुर्धर हैं और सारे जगत् को वेध्यब सा लक्ष्य किया है।
4. नैहर चाह न पाउब जहाँ।
सुधाकरी अर्थ-जहाँ हम लोग नैहर (जाने) की इच्छा (तक) न करने पावेंगी।
('पाउब' के स्थान पर 'पाउबि' पाठ रखा गया है, शायद स्त्रीलिंग के विचार से।
पर अवधी में उत्तमपुरुष बहुवचन में स्त्री. पुं. दोनों में एक ही रूप रहता
है)।
ठीक अर्थ-जहाँ नैहर (मायके) के खबर तक हम न पाएँगी।
5. चलौं पउनि सब गोहने फूल डार लेइ हाथ।
सुधाकरी अर्थ-सब हवा ऐसी या पवित्र हाथ में फूलों की डालियाँ ले लेकर चलीं।
ठीक अर्थ-सब पौनी (इनाम आदि पानेवाली) प्रजा-नाइन, बारिन आदि-फूलों की
डालियाँ लेकर साथ चलीं।
इसी प्रकार की भूलों से टीका भरी हुई है। टीका का नाम रखा गया है
'सुधाकर-चन्द्रिका'। पर यह चन्द्रिका है कि घोर अन्धकार? अच्छा हुआ कि
एशियाटिक सोसाइटी ने थोड़ा-सा निकालकर ही छोड़ दिया।
सारांश यह कि इस प्राचीन मनोहर ग्रन्थ का कोई अच्छा संस्करण अब तक न था और
हिन्दी प्रेमियों की रुचि अपने साहित्य के सम्यक् अध्यरयन की ओर दिन- दिन
बढ़ रही थी। आठ नौ वर्ष हुए, काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी 'मनोरंजन
पुस्तकमाला' के लिए मुझसे 'पद्मावत' का एक संक्षिप्त संस्करण शब्दार्थ और
टिप्पणी सहित तैयार करने के लिए कहा था। मैंने आधे के लगभग ग्रन्थ तैयार भी
किया था। पर पीछे यह निश्चय हुआ कि जायसी के दोनों ग्रन्थ पूरे निकाले
जायँ। अत: 'पद्मावत' की वह अधूरी तैयार की हुई कापी बहुत दिनों तक पड़ी रही।
इधर जब विश्वविद्यालयों में हिन्दी का प्रवेश हुआ और हिन्दू विश्वविद्यालय
में हिन्दी साहित्य भी परीक्षा के वैकल्पिक विषयों में रखा गया, तब तो
जायसी का एक शुद्ध उत्तम संस्करण निकालना अनिवार्य हो गया क्योंकि बी.ए. और
एम.ए. दोनों की परीक्षाओं में पद्मावत रखी गई। पढ़ाई प्रारम्भ हो चुकी थी और
पुस्तक के बिना हर्ज हो रहा था; इससे यह निश्चय किया गया कि समग्र ग्रन्थ
एकबारगी निकालने में देर होगी; अत: उसके छह छह फार्म के खंड करके निकाले
जायँ जिससे छात्रों का काम भी चलता रहे। कार्तिक संवत् 1980 से इन खंडों का
निकलना प्रारम्भ हो गया। चार खण्डों में 'पद्मावत' और 'अखरावट' दोनों
पुस्तकें समाप्त हुईं।
'पद्मावत' की चार छपी प्रतियों के अतिरिक्त मेरे पास कैथी लिपि में लिखी एक
हस्तलिखित प्रति भी थी जिससे पाठ के निश्चय करने में कुछ सहायता मिली। पाठ
के सम्बलन्धभ में यह कह देना आवश्यक है कि वह अवधी व्याकरण् और उच्चारण तथा
भाषाविकास के अनुसार रखा गया है। एशियाटिक सोसाइटी की प्रति में 'ए' और 'औ'
इन अक्षरों का व्यवहार नहीं हुआ है: इनके स्थान पर 'अइ' और 'अउ' प्रयुक्त
हुए हैं। इस विधान में प्राकृत की पुरानी पद्धति का अनुसरण चाहे हो, पर
उच्चारण की उस आगे बढ़ी हुई अवस्था का पता नहीं लगता जिसे हमारी भाषा, जायसी
और तुलसी के समय में प्राप्त कर चुकी थी। उस समय चलती भाषा में 'अइ' और
'अउ' के 'अ' और 'इ' तथा 'अ' और 'उ' पृथक्-पृथक् स्फुट उच्चारण नहीं रह गए
थे, दोनों स्वर मिलकर 'ए' और 'औ' के समान उच्चरित होने लगे थे। प्राकृत के
'दैत्यादिष्वइ' और 'पौरादिष्वउ' सब दिन के लिए स्थायी नहीं हो सकते थे।
प्राकृत और अपभ्रंश अवस्था पार करने पर उलटी गंगा बही। प्राकृत के 'अइ' और
'अउ' के स्थान पर 'ए' और 'औ' उच्चारण में आए-जैसे प्राकृत और अपभ्रंश रूप
'चलइ', 'पइट्ठ', 'कइसे', 'चउक्कोण' इत्यादि हमारी भाषा में आकर 'चलै', पैठ,
'कैसे', 'चौकोन' इस प्रकार बोले जाने लगे। यदि कहिए कि इनका उच्चारण आजकल
तो ऐसा होता है पर जायसी बहुत पुराने हैं, सम्भवत: उस समय इनका उच्चारण
प्राकृत के अनुसार ही होता रहा हो, तो इसका उत्तर यह है कि अभी तुलसीदासजी
के थोड़े ही दिनों पीछे की लिखी 'मानस' की कुछ पुरानी प्रतियाँ मौजूद हैं
जिनमें बराबर 'कैसे', 'जैसे', 'तैसे', 'कै', 'करै', 'चौथे', 'करौं', 'आवौं'
इत्यादि अवधी की चलती भाषा के रूप पाए जाते हैं। जायसी और तुलसी ने चलती
भाषा में रचना की है, प्राकृत के समान व्याकरण के अनुसार गढ़ी हुई भाषा में
नहीं। यह दूसरी बात है कि प्राचीन रूपों का व्यवहार परम्परा के विचार से
उन्होंने बहुत जगह किया है, पर भाषा उनकी प्रचलित भाषा ही है।
डॉक्टर ग्रियर्सन ने 'करइ', 'चलइ', आदि रूपों को ही कविप्रयुक्त सिद्ध करने
के लिए 'करई', 'धावई' आदि चरण के अन्त में आने वाले रूपों का प्रमाण दिया
है। पर 'चलै', 'गनै' आदि रूप भी चरण के अन्त में बराबर आए हैं जैसे-
क. इहै बहुत जो बोहित पावौं। -जायसी।
ख. रघुबीर बल गर्वित वीभीषनु घाल नहिं ताकहँ गनै। -तुलसी।
चरणांत में ही नहीं, वर्णवृत्तों के बीच में भी ये चलते रूप बराबर दिखाए जा
सकते हैं जैसे-
एक एक की न सँभार। करै तात भ्रात पुकार -तुलसी
जब एक ही कवि की रचना में नए और पुराने दोनों रूपों का प्रयोग मिलता है, तब
यह निश्चित है कि नए रूप का प्रचार कवि के समय में हो गया था और पुराने रूप
का प्रयोग या तो उसने छन्द की आवश्यकतावश किया है अथवा परम्परापालन के लिए।
हाँ, 'ए' और 'औ' के सम्बलन्ध में ध्याजन रखने की बात यह है कि इनके 'पूरबी'
और 'पच्छिमी' दो प्रकार के उच्चारण होते हैं। पूरबी उच्चारण संस्कृत के
समान 'अइ' और 'अउ' से मिलता-जुलता और पच्छिमी उच्चारण 'अय' और 'अव' से
मिलता जुलता होता है। अवधी भाषा में शब्द के आदि के 'ए' और 'औ' का अधिकतर
पूरबी तथा अन्त में पड़नेवाले 'ए' 'औ' का उच्चारण पच्छिमी ढंग पर होता है।
'हि' विभक्ति का प्रयोग प्राचीन पद्धति के अनुसार जायसी में सब कारकों के
लिए मिलेगा। पर कर्ता कारक में केवल सकर्मक भूतकालिक क्रिया के सर्वनाम
कर्ता के तथा अकारान्त संज्ञा कर्ता में मिलता है। इन दोनों स्थलों में
मैंने प्राय: वैकल्पिक रूप 'इ' (जो 'हि' का ही विकार है) रखा है, जैसे केइ,
जेइ, तेइ, राजै, सूए, गौरे, (किसने, जिसने, उसने, राजा ने, सूए ने, गौरा
ने)। इसी 'हि' विभक्ति का ही दूसरा रूप 'ह' है जो सर्वनामों के अन्तिम वर्ण
के साथ संयुक्त होकर प्राय: सब कारकों में आया है। अत: जहाँ कहीं 'हम्ह'
'तुम्ह', 'तिन्ह' या 'उन्ह' हो वहाँ यह समझना चाहिए कि यह सर्वनाम कर्ता के
अतिरिक्त किसी और कारक में है-जैसे हम्म हमको, हमसे, हमारा, हममें, हमपर।
सम्बिन्धकवाचक सर्वनाम के लिए 'जो' रखा गया है तथा यदि या जब के अर्थ में
अव्यय रूप 'जौ'।
प्रत्येक पृष्ठ में असाधारण या कठिन शब्दों, वाक्यों और कहीं चरणों में
अर्थ फुटनोट में बराबर दिए गए हैं जिससे पाठकों को बहुत सुबीता होगा। इसके
अतिरिक्त 'मलिक मुहम्मद जायसी' पर एक विस्तृत निबन्ध भी ग्रन्थारम्भ के
पहले लगा दिया गया है जिसमें कवि की विशेषताओं के अन्वेषण और गुणदोषों के
विवेचन का प्रयत्न अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार किया है।
अपने वक्तव्य में 'पद्मावत' के संस्करणों का मैंने जो उल्लेख किया है, वह
केवल कार्य की कठिनता का अनुमान कराने के लिए। कभी कभी किसी चौपाई का पाठ
और अर्थ निश्चित करने में कई दिनों का समय लग गया है। झंझट का एक बड़ा कारण
यह भी था कि जायसी के ग्रन्थ बहुतों ने फारसी लिपि में उतारे। फिर उन्हें
सामने रखकर बहुत सी प्रतियाँ हिन्दी अक्षरों में तैयार हुईं। इससे एक ही
शब्द को किसी ने एक रूप में पढ़ा, किसी ने दूसरे रूप में। अत: मुझे बहुत
स्थलों पर इस प्रक्रिया से काम लेना पड़ा है कि अमुक शब्द फारसी अक्षरों में
लिख जाने पर कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है। काव्य भाषा के प्राचीन स्वरूप
पर भी पूरा ध्याेन रखना पड़ा है। जायसी की रचना में भिन्न भिन्न
तत्त्वसिद्धान्तों के आभास को समझने के लिए दूर तक दृष्टि दौड़ाने की
आवश्यकता थी। इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बिना धोखा खाए पार करना मेरे ऐसे
अल्पज्ञ और आलसी के लिए असम्भव ही समझिए। अत: न जाने कितनी भूलें मुझसे इस
कार्य में हुई होंगी, जिनके सम्बड़न्धस में सिवाय इसके कि मैं क्षमा माँगू
और उदार पाठक क्षमा करें, और हो ही क्या सकता है?
कृष्ण जन्माष्टमी - रामचन्द्र शुक्ल
संवत् 1981
द्वितीय संस्करण का वक्तव्य
प्रथम संस्करण में इधर उधर जो कुछ अशुद्धियाँ या भूलें रह गई थीं वे इस
संस्करण में जहाँ तक हो सका है, दूर कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जायसी के
'मत और सिद्धान्त' तथा 'रहस्यवाद' के अन्तर्गत भी कुछ बातें बढ़ाई गई हैं
जिनसे आशा है, सूफी भक्तिमार्ग और भारतीय भक्तिमार्ग का स्वरूपभेद समझने
में कुछ अधिक सहायता पहुँचेगी। इधर मेरे प्रिय शिष्य पं. चंद्रबली पांडेय
एम. ए. जो हिन्दी के सूफी कवियों के सम्बरन्ध में अनुसंधान कर रहे हैं,
जायस गए और मलिक मुहम्मद जायसी की कुछ बातों का पता लगा लाए। उनकी खोज के
अनुसार 'जायसी का जीवनवृत्त' भी नए रूप में दिया गया है जिसके लिए उनके
प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मैं आवश्यक समझता हूँ।
इस ग्रन्थावली के प्रथम संस्करण में जायसी के दो ग्रन्थ-'पदमावत' और
'अखरावट'-संगृहीत थे। उनका एक ग्रन्थ 'आखिरी कलाम' फारसी लिपि में बहुत
पुराना छपा हुआ हाल में मिला। यह ग्रन्थ भी इस संस्करण में सम्मिलित कर
लिया गया है। कोई और दूसरी प्रति न मिलने के कारण इसका ठीक ठीक पाठ निश्चित
करने में कड़ी कठिनता पड़ी है। एक तो इसकी भाषा 'पदमावत' और 'अखरावट' की
अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधी, दूसरे फारसी अक्षरों में लिखी हुई।
बड़ी परिश्रम से किसी प्रकार मैंने इसका पाठ ठीक किया है, फिर भी इधर उधर
कुछ भूलें रह जाने की आशंका से मैं मुक्त नहीं हूँ।
जायसी के और दो ग्रन्थों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है।
इसमें इसलाम की मजहवी किताबों के अनुसार कयामत के दिनों का लम्बा चौड़ा
वर्णन है। किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को
तपाएगा, सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे, ईश्वर न्याय
करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थरथर काँपेंगे, इन्हीं सब
बातों का ब्योरा इस छोटी सी पुस्तक में है। जायसी ने दिखाया है कि ईसा,
मूसा आदि और सब पैगम्बरों को तो आप आपकी पड़ी रहेगी, वे अपने अपने आसनों पर
रक्षित स्थान में चुपचाप बैठे रहेंगे; पर परम दयालु हजरत मुहम्मद साहब अपने
अनुयायियों के उद्धार के लिए उस शरीर को जलानेवाली धूप में इधर उधर व्याकुल
घूमते दिखाई देंगे, एक क्षण के लिए भी कहीं छाया में न बैठेंगे। सबसे अधिक
ध्यायन देने की बात इमाम हसन हुसैन के प्रति जायसी की सहानुभूति है।
उन्होंने लिखा है कि जब तक हसन हुसैन को अन्यायपूर्वक मारनेवाले और कष्ट
देनेवाले घोर यंत्रणापूर्ण नरक में डाल न दिए जाएँगे, तब तक अल्लाह का कोप
शांत न होगा। अन्त में मुहम्मद साहब और उनके अनुयायी किस प्रकार स्वर्ग की
अप्सराओं से विवाह करके नाना प्रकार के सुख भोगेंगे, यही दिखाकर पुस्तक
समाप्त की गई है।
चैत्र पूर्णिमा - रामचन्द्र शुक्ल
संवत् 1992
मलिक मुहम्मद जायसी
सौ वर्ष पूर्व कबीरदास हिन्दू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके
थे। पण्डितों और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते पर साधारण जनता 'राम और रहीम'
की एकता मान चुकी थी। साधुओं और फकीरों को दोनों दीन के लोग आदर और मान की
दृष्टि से देखते थे। साधु या फकीर भी सर्वप्रिय वे ही हो सकते थे जो भेदभाव
से परे दिखाई पड़ते थे। बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते हिन्दू और मुसलमान
एक-दूसरे के सामने अपना-अपना हृदय खोलने लग गए थे, जिससे मनुष्यता के
सामान्य भावों के प्रवाह में मग्न होने और मग्न करने का समय आ गया था। जनता
की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर हो चली थी। मुसलमान हिन्दुओं की राम कहानी
सुनने को तैयार हो गए थे और हिन्दू मुसलमान का दास्तानहमजा। नल और दमयन्ती
की कथा मुसलमान जानने लगे थे और लैला मजनूँ की हिन्दू। ईश्वर तक पहुँचने
वाला मार्ग ढूँढ़ने की सलाह भी दोनों कभी कभी साथ बैठकर करने लगे थे। इधर
भक्तिमार्ग के आचार्य और महात्मा भगवत्प्रेम को सर्वोपरि ठहरा चुके थे और
उधर सूफी महात्मा मुसलमानों को 'इश्क हकीकी' का सबक पढ़ाते आ रहे थे।
चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और रामानन्द के प्रभाव से प्रेमप्रधान वैष्णव
धर्म का जो प्रवाह बंग देश से गुजरात तक रहा, उसका सबसे अधिक विरोध शाक्त
मत और वाममार्ग के साथ दिखाई पड़ा। शाक्तमतविहित पशुहिंसा, मन्त्रा, तन्त्रत
तथा यक्षिणी आदि की पूजा वेदविरुद्ध अनाचार के रूप में समझी जाने लगी।
हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के बीच 'साधुता' का सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित
हो गया था। बहुत से मुसलमान फकीर भी अहिंसा का सिद्धान्त स्वीकार करके
मांसभक्षण को बुरा कहने लगे।
ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान 'प्रेम की पीर' की कहानियाँ लेकर साहित्य
क्षेत्र में उतरे। ये कहानियाँ हिन्दुओं के ही घर की थीं। इनकी मधुरता और
कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य
मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूपरंग
के भेदों की ओर से ध्याृन हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है।
अमीर खुसरो ने मुसलमानी राजत्वकाल के आरम्भ में ही हिन्दू जनता के प्रेम और
विनोद में योग देकर भावों के परस्पर आदान-प्रदान का सूत्रपात किया था, पर
अलाउद्दीन के कट्टरपन और अत्याचार के कारण जो दोनों जातियाँ एक दूसरे से
खिंची- सी रहीं, उनका हृदय मिल न सका। कबीर की अटपटी वाणी से भी दोनों के
दिल साफ न हुए। मनुष्य मनुष्य के बीच रागात्मक सम्ब न्धी है, यह उसके
द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के व्यवहार में जिस हृदयसाम्य का अनुभव
मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। जिस प्रकार दूसरी
जाति या मत वाले के हृदय हैं उसी प्रकार हमारे भी हैं, जिस प्रकार दूसरे के
हृदय में प्रेम की तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी, प्रिय
का वियोग जैसे दूसरे को व्याकुल करता है वैसे ही हमें भी, माता का जो हृदय
दूसरे के यहाँ है वही हमारे यहाँ भी, जिन बातों से दूसरों को सुख-दु:ख होता
है उन्हीं बातों से हमें भी, इस तथ्य का प्रत्यक्षीकरण कुतबन, जायसी आदि
प्रेमकहानी के कवियों द्वारा हुआ। अपनी कहानियों द्वारा इन्होंने प्रेम का
शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवनदशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य
मात्र के हृदय पर एक प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिन्दू हृदय और मुसलमान हृदय
आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा।
इन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुओं की कहानियाँ हिन्दुओं की ही बोली में पूरी
सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार
हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई
परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य
सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। वह जायसी द्वारा पूरी हुई।
प्रेमगाथा की परम्परा
इस नवीन शैली की प्रेमगाथा का आविर्भाव इस बात के प्रमाणों में से है कि
इतिहास में किसी राजा के कार्य सदा लोकप्रवृत्ति के प्रतिबिम्ब नहीं हुआ
करते। इसी को ध्यान में रखकर कुछ नवीन पद्धति के इतिहासकार प्रकरणों का
विभाग राजाओं के राजत्वकाल के अनुसार न कर लोक की प्रवृत्ति के अनुसार करना
चाहते हैं। एक ओर तो कट्टर और अन्यायी सिकन्दर लोदी मथुरा के मन्दिरों को
गिराकर मसजिदें खड़ी कर रहा था और हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर
रहा था, दूसरी ओर पूरब में बंगाल के शासक हुसैनशाह के अनुरोध से, जिसने
'सत्य पीर' की कथा चलाई थी, कुतबन मियाँ एक ऐसी कहानी लेकर जनता के सामने
आए जिसके द्वारा उन्होंने मुसलमान होते हुए भी अपने मनुष्य होने का परिचय
दिया। इसी मनुष्यत्व को ऊपर करने से हिन्दूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि के उस
स्वरूप का प्रतिरोध होता है जो विरोध की ओर ले जाता है। हिन्दुओं और
मुसलमानों को एक साथ रहते अब इतने दिन हो गए थे कि दोनों का ध्यान
मनुष्यता के सामान्य स्वरूप की ओर स्वभावत: जाय।
कुतबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। उन्होंने 'मृगावती' नाम का एक
काव्य सन् 909 हिजरी में लिखा। इसमें चन्द्रनगर के राजा गणपतिदेव के
राजकुमार और कंचननगर के राजा रूपमुरार की कन्या मृगावती के प्रेम की कथा
है।
जायसी ने प्रेमियों के दृष्टान्त देते हुए अपने पूर्व की लिखी कुछ
प्रेमकहानियों का उल्लेख किया है-
विक्रम धँसा प्रेम के बारह । सपनावति कहँ गएउ पतारा॥
मधूपाछ मुगुधावति लागी । गगनपूर होइगा बैरागी॥
राजकुँवर कंचनपुर गयऊ । मिरगावति कहँ जोगी भयऊ॥
साधु कुँवर खंडावत जोगू । मधूमालति कर कीन्ह वियोगू॥
प्रेमावति कहँ सुरसरि साधा । ऊषा लगि अनिरुधा बर बाध॥
विक्रमादित्य और ऊषा अनिरुद्ध की प्रसिद्ध कथाओं को छोड़ देने से चार
प्रेमकहानियाँ जायसी के पूर्व लिखी हुई पाई जाती हैं। इनमें से 'मृगावती'
की एक खण्डित प्रति का पता तो नागरीप्रचारिणी सभा को लग चुका है।
'मधुमालती' की भी फारसी अक्षरों में लिखी हुई एक प्रति मैंने किसी सज्जन के
पास देखी थी पर किसके पास, यह स्मरण नहीं। चतुर्भुजदास कृत 'मधुमालती कथा'
नागरीप्रचारिणी सभा को मिली है जिसका निर्माणकाल ज्ञात नहीं और जो अत्यन्त
भ्रष्ट गद्य में है। 'मुग्धावती' और 'प्रेमावती' का पता अभी तक नहीं लगा
है। जायसी के पीछे भी 'प्रेमगाथा' की यह परम्परा कुछ दिनों तक चलती रही।
गाजीपुर निवासी शेख हुसेन के पुत्र उसमान (मान) ने संवत् 1670 के लगभग
चित्रवली लिखी जिसमें नेपाल के राजा धरनीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर के
राजा चित्रसेन की कन्या चित्रवली की प्रेमकहानी है। भाषा इसकी अवधी होने पर
भी कुछ भोजपुरी लिए है। यह नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुकी है।
दूसरी पुस्तक नूरमुहम्मद की 'इन्द्रावत' है जो संवत् 1796 में लिखी गई थी।
इसे भी उक्त सभा प्रकाशित कर चुकी है।
इन प्रेमगाथा काव्यों में पहली बात ध्याीन देने की यह है कि इनकी रचना
बिलकुल भारतीय चरितकाव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों
के ढंग पर हुई है, जिसमें कथा सर्गों या अध्याोयों में विस्तार के हिसाब से
विभक्त नहीं होती, बराबर चली चलती है, केवल स्थान स्थान पर घटनाओं या
प्रसंगों का उल्लेख शीर्षक के रूप में रहता है। मसनवी के लिए साहित्यिक
नियम तो केवल इतना ही समझा जाता है कि सारा काव्य एक ही मसनवी छन्द में हो
पर परम्परा के अनुसार उसमें कथारम्भ के पहले ईश्वरस्तुति, पैगम्बर की
वन्दना और उस समय के राजा (शाहे वक्त) की प्रशंसा होनी चाहिए। ये बातें
पद्मावत, इन्द्रावत, मृगावती इत्यादि सबमें पाई जाती हैं।
दूसरी बात ध्यादन देने की यह है कि ये सब प्रेमकहानियाँ पूरबी हिन्दी
अर्थात् अवधी भाषा में एक नियमक्रम के साथ केवल चौपाई, दोहे में लिखी गई
हैं। जायसी ने सात चौपाइयों (अधार्लियों) के बाद एक एक दोहे का क्रम रखा
है। जायसी के पीछे गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने 'रामचरितमानस' के लिए यही
दोहे चौपाई का क्रम ग्रहण किया। चौपाई और बरवै मानो अवधी भाषा के अपने छन्द
हैं, इनमें अवधी भाषा जिस सौष्ठव के साथ ढली है उस सौष्ठव के साथ व्रजभाषा
नहीं। उदाहरण के लिए लाल कवि के 'छत्रप्रकाश', पद्माकर के 'रामरसायन' और
व्रजवासीदास के 'ब्रजविलास' को लीजिए। 'बरवै', तो व्रजभाषा में कहा ही नहीं
जा सकता। किसी पुराने कवि ने व्रजभाषा में बरवै लिखने का प्रयास भी नहीं
किया।
तीसरी बात ध्यांन देने की यह है कि इस शैली की प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के
ही द्वारा लिखी गईं। इन भावुक और उदार मुसलमानों ने इनके द्वारा मानो
हिन्दू जीवन के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की। यदि मुसलमान हिन्दी और हिन्दू
साहित्य से दूर न भागते, इनके अध्यकयन का क्रम जारी रखते, तो उनमें
हिन्दुओं के प्रति सद्भाव की वह कमी न रह जाती जो कभी कभी दिखाई पड़ती है।
हिन्दुओं ने फारसी और उर्दू के अभ्यास द्वारा मुसलमानों की जीवनकथाओं के
प्रति अपने हृदय का सामंजस्य पूर्ण रूप से स्थापित किया, पर खेद है कि
मुसलमानों ने इसका सिलसिला बन्द कर दिया। किसी जाति की जीवनकथाओं को बार
बार सामने लाना उस जाति के प्रति और सहानुभूति प्राप्त करने का स्वाभाविक
साधान है। 'पद्मावत' की हस्तलिखित प्रतियाँ अधिकतर मुसलमानों के ही घर में
पाई गई हैं। इतना मैं अनुभव से कहता हूँ कि जिन मुसलमानों के यहाँ यह पोथी
देखी गई, उन सबको मैंने विरोध से दूर और अत्यन्त उदार पाया।
जायसी का जीवनवृत्त
जायसी की एक छोटी सी पुस्तक 'आखिरी कलाम' के नाम से फारसी अक्षरों में छपी
है। यह सन् 936 हिजरी में (सन् 1528 ई. के लगभग) बाबर के समय में लिखी गई
थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मुहम्मद जायसी ने
अपने जन्म के सम्बन्ध में लिखा है-
भा अवतार मोर नव सदी। तीस बरस ऊपर कवि बदी।
इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। 'नव सदी' ही पाठ मानें तो जन्म
काल 900 हिजरी (सन् 1492 के लगभग) ठहरता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ यही
निकलेगा कि जन्म के 30 वर्ष पीछे जायसी अच्छी कविता करने लगे। जायसी का
सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है पदमावत जिसका निर्माणकाल कवि ने इस प्रकार दिया
है-
सन नव सै सत्ताइस अहा। कथा अरम्भ बैन कवि कहा।
इसका अर्थ होता है पद्मावत की कथा के प्रारम्भिक वचन (अरम्भ बैन) कवि ने
सन् 927 हिजरी (सन् 1520 ई. के लगभग) में कहे थे। पर ग्रन्थारम्भ में कवि
ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार 'शाहे वक्त' शेरशाह की प्रशंसा की है जिसके
शासनकाल का आरम्भ 947 हिजरी अर्थात् सन् 1540 ई. से हुआ था। इस दशा में यही
सम्भव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो 1520 ई. में ही बनाए थे,
पर ग्रन्थ को 21 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। इसी से कवि
ने भूतकालिक क्रिया 'अहा' (= था) और 'कहा' का प्रयोग किया है1A
जान पड़ता है कि 'पद्मावत' की कथा को लेकर थोड़े से पद्य जायसी ने रचे थे।
उसके पीछे वे जायस छोड़कर बहुत दिनों तक इधर उधर रहे। अन्त में जब वे जायस
में आकर रहने लगे तब उन्हों ने इस ग्रन्थ को उठाया और पूरा किया। इस बात का
संकेत इन पंक्तियों में पाया जाता है-
जायस नगर धारम अस्थानू। तहाँ आइ कवि कीन्ह बखानू॥
'तहाँ आइ' से पं. सुधाकर और डॉक्टर ग्रियर्सन ने यह अनुमान किया था कि मलिक
मुहम्मद किसी और जगह से आकर जायस में बसे थे। पर यह ठीक नहीं। जायस वाले
ऐसा नहीं कहते। उनके कथनानुसार मलिक मुहम्मद जायस ही के रहने वाले थे। उनके
घर का स्थान अब तक लोग वहाँ के कंचाने मुहल्ले में बताते हैं। 'पद्मावत'
में कवि ने अपने चार दोस्तों के नाम लिए हैं -यूसुफ मलिक, सालार कादिम,
सलोने मियाँ और बड़े शेख। ये चारों जायस ही के थे। सलोने मियाँ के सम्बफन्ध,
में अब तक जायस में यह जनश्रुति चली आती है कि वे बड़े बलवान थे और एक बार
हाथी से लड़ गए थे। इन चारों में से दो एक के खानदान अब तक हैं। जायसी का
वंश नहीं चला, पर उनके भाई के खानदान में एक साहब मौजूद हैं जिनके पास
वंशवृक्ष भी है। यह वंशवृक्ष कुछ गड़बड़ सा है।
जायसी कुरूप और काने थे। कुछ लोगों के अनुसार वे जन्म से ही ऐसे थे पर
अधिकतर लोगों का कहना है कि शीतला या अर्धांग रोग से उनका शरीर विकृत हो
गया था। अपने काने होने का उल्लेख कवि ने आप ही इस प्रकार किया है-'एक नयन
कवि मुहम्मद गुनी'। उनकी दाहिनी ऑंख फूटी थी या बाईं, इसका उत्तर शायद इस
दोहे से मिले-
मुहमद बाईं दिसि तजा, एक सरवन एक ऑंखि।
इससे अनुमान होता है कि बाएँ कान से भी उन्हें कम सुनाई पड़ता था। जायस में
प्रसिद्ध है कि वे एक बार शेरशाह के दरबार में गए। शेरशाह उनके भद्दे चेहरे
1. पहले संस्करण में दिए हुए सन् को शेरशाह के समय में लाने के लिए, 'नव सै
सैंतालिस' पाठ माना गया था। फारसी लिपि में सत्ताइस और सैंतालिस में भ्रम
हो सकता है। पर 'पद्मावत' का एक पुराना बँगला अनुवाद है, उसमें भी 'नव सै
सत्ताइस' ही पाठ माना गया है-
शेख मुहमद जति जखन रचिल ग्रन्थ संख्या सप्तविंश नवशत।
यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन् 1650 ई. के आस पास आलो
उजाला नामक एक कवि से कराया था।
को देख हँस पड़ा। उन्होंने अत्यन्त शान्त भाव से पूछा-'मोहिका हससि,कि
कोहरहि?' अर्थात् तू मुझ पर हँसा या उस कुम्हार (गढ़नेवाले ईश्वर) पर? इस पर
शेरशाह ने लज्जित होकर क्षमा माँगी। कुछ लोग कहते हैं कि वे शेरशाह के
दरबार में नहीं गए थे, शेरशाह ही उनका नाम सुनकर उनके पास आया था।
मलिक मुहम्मद एक गृहस्थ किसान के रूप में ही जायस में रहते थे। वे आरम्भ से
बड़े ईश्वरभक्त और साधु प्रकृति के थे। उनका नियम था कि जब वे अपने खेतों
में होते तब अपना खाना वहीं मँगा लिया करते थे। खाना वे अकेले कभी न खाते;
जो आसपास दिखाई पड़ता उसके साथ बैठकर खाते थे। एक दिन उन्हें इधर उधर कोई न
दिखाई पड़ा। बहुत देर तक आसरा देखते देखते अन्त में एक कोढ़ी दिखाई पड़ा।
जायसी ने बड़े आग्रह से उसे अपने साथ खाने को बिठाया और एक ही बरतन में उसके
साथ भोजन करने लगे। उसके शरीर से कोढ़ चू रहा था। कुछ थोड़ा सा मवाद भोजन में
भी चू पड़ा। जायसी ने उस अंश को खाने के लिए उठाया पर उस कोढ़ी ने हाथ थाम
लिया और कहा, 'इसे मैं खाऊँगा, आप साफ हिस्सा खाइए' पर जायसी झट से उसे खा
गए। इसके पीछे वह कोढ़ी अदृश्य हो गया। इस घटना के उपरान्त जायसी की
मनोवृत्ति ईश्वर की ओर और भी अधिक हो गई। उक्त घटना की ओर संकेत लोग अखरावट
के इस दोहे में बताते है। -
बुंदहिं समुद्र समान, यह अचरज कासौं कहौं।
जो हेरा सो हेरान, मुहमद आपुहिं आपु महँ॥
कहते हैं कि जायसी के पुत्र थे, पर वे मकान के नीचे दबकर, या ऐसी ही किसी
और दुर्घटना से मर गए। तब से जायसी संसार से और भी अधिक विरक्त हो गए और
कुछ दिनों में घरबार छोड़कर इधर उधर फकीर होकर घूमने लगे। वे अपने समय के एक
सिद्ध फकीर माने जाते थे और चारों ओर उनका बड़ा मान था। अमेठी के राजा
रामसिंह उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। जीवन के अन्तिम दिनों में जायसी अमेठी
से कुछ दूर एक घने जंगल में रहा करते थे। कहते हैं कि उनकी मृत्यु विचित्र
ढंग से हुई। जब उनका अन्तिम समय निकट आया तब उन्होंने अमेठी के राजा से कह
दिया कि मैं किसी शिकारी की गोली खाकर मरूँगा। इस पर अमेठी के राजा ने
आसपास के जंगलों में शिकार की मनाही कर दी। जिस जंगल में जायसी रहते थे,
उसमें एक दिन एक शिकारी को एक बड़ा भारी बाघ दिखाई पड़ा। उसने डरकर उस पर
गोली छोड़ दी। पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी मरे पड़े थे। कहते हैं
कि जायसी कभी कभी योगबल से इस प्रकार के रूप धारण कर लिया करते थे।
काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद
मिली थी, अपनी याददाश्त में मलिक मुहम्मद जायसी का मृत्युकाल रज्जब 949
हिजरी (सन् 1542 ई.) दिया है। यह काल कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता।
इसे ठीक मानने पर जायसी दीर्घायु नहीं ठहरते। उनका परलोकवास 49 वर्ष से भी
कम अवस्था में सिद्ध होता है पर जायसी ने 'पद्मावत' के उपसंहार में
वृद्धावस्था का जो वर्णन किया है वह स्वत: अनुभूत-सा जान पड़ता है।
जायसी की कब्र अमेठी के राजा के वर्तमान कोट से पौन मील के लगभग है। यह
वर्तमान कोट जायसी के मरने के बहुत पीछे बना है। अमेठी के राजाओं का पुराना
कोट जायसी की कब्र से डेढ़ कोस की दूरी पर था। अत: यह प्रवाद कि अमेठी के
राजा को जायसी की दुआ से पुत्र हुआ और उन्होंने अपने कोट के पास उनकी कब्र
बनवाई, निराधार है।
मलिक मुहम्मद, निजामुद्दीन औलिया की शिष्यपरम्परा में थे। इस परम्परा की दो
शाखाएँ हुईं-एक मानिकपुर, कालपी आदि की, दूसरी जायस की। पहली शाखा के पीरों
की परम्परा जायसी ने बहुत दूर तक दी है। पर जायस वाली शाखा की पूरी परम्परा
उन्होंने नहीं दी है; अपने पीर या दीक्षागुरु सैयद अशरफ जहाँगीर तथा उनके
पुत्र पौत्रों का ही उल्लेख किया है। सूफी लोग निजामुद्दीन औलिया की
मानिकपुर कालपीवाली शिष्यपरम्परा इस प्रकार बतलाते है। -
निजामुद्दीन औलिया (मृत्यु सन् 1325 ई.)
|
सिराजुद्दीन
|
शेख अलाउल हक
| (जायस)
| |
शेख कुतुब आलम (पण्डोई के, सन् 1415) ×
| |
शेख हशमुद्दीन (मानिकपुर) ×
| |
सैयद राजे हामिदशाह ×
| |
शेख दानियाल |
| |
सैयद मुहम्मद |
| सैयद अशरफ जहाँगीर
शेख अलहदाद |
| |
शेख बुरहान (कालपी) शेख हाजी
| |
शेख मोहिदी (मुहीउद्दीन) | |
शेख मुहम्मद या शेख कमाल
मुबारक
'पद्मावत' और 'अखरावट' दोनों में जायसी ने मानिकपुर कालपीवाली गुरुपरम्परा
का उल्लेख विस्तार से किया है, इससे डॉक्टर ग्रियर्सन ने शेख मोहिदी को ही
उनका दीक्षागुरु माना है। गुरुवन्दना से इस बात का ठीक ठीक निश्चय नहीं
होता कि वे मानिकपुर के मुहीउद्दीन के मुरीद थे अथवा जायस के सैयद अशरफ के।
पद्मावत में दोनों पीरों का उल्लेख इस प्रकार है-
सैयद असरफ पीर पियारा। जेइ मोहिं पंथ दीन्ह उजियारा॥
गुरु मोहिदी खेवक मैं सेवा। जलै उताइल जेहि कर खेवा॥
अखरावट में इन दोनों की चर्चा इस प्रकार है-
कही सरीअत चिस्ती पीरू। उधारी असरफ और जहँगीरू॥
पा पाएउँ गुरु मोहिदी मीठा। मिला पन्थ सो दरसन दीठा॥
'आखिरी कलाम' में केवल सैयद अशरफ जहाँगीर का ही उल्लेख है। 'पीर' शब्द का
प्रयोग भी जायसी ने सैयद अशरफ के नाम के पहले किया है और अपने को उनके घर
का बन्दा कहा है। इससे हमारा अनुमान है कि उनके दीक्षागुरु तो थे सैयद अशरफ
पर पीछे से उन्होंने मुहीउद्दीन की भी सेवा करके उनसे बहुत कुछ ज्ञानोपदेश
और शिक्षा प्राप्त की। जायसवाले तो सैयद अशरफ के पोते मुबारकशाह बोदले को
उनका पीर बताते हैं, पर यह ठीक नहीं जँचता।
सूफी मुसलमान फकीरों के सिवा कई सम्प्रदायों (जैसे, गोरखपन्थी, रसायनी,
वेदान्ती) के हिन्दू साधुओं से भी उनका बहुत सत्संग रहा, जिनसे उन्होंने
बहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त की। हठयोग, वेदान्त, रसायन आदि की बहुत
सी बातों का सन्निवेश उनकी रचना में मिलता है। हठयोग में मानी हुई इला,
पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों की ही चर्चा उन्होंने नहीं की है बल्कि
सुषुम्ना नाड़ी में मस्तिष्क, नाभिचक्र (कुंडलिनी), हृत्कमल और दशमद्वार
(ब्रह्मरंधा्र) का भी बार-बार उल्लेख किया है। योगी ब्रह्म की अनुभूति के
लिए कुण्डलिनी को जगाकर ब्रह्मद्वार तक पहुँचाने का यत्न करता है। उसकी इस
साधना में अनेक अन्तराय (विघ्न) होते हैं। जायसी ने योग के इस निरूपण में
अपने इस्लाम की कथा का भी विचित्र मिश्रण किया है। अन्तराय के स्थान पर
उन्होंने शैतान को रखा है और उसे 'नारद' नाम दिया है। यही नारद दशमद्वार का
पहरेदार है और काम, क्रोध आदि इसके सिपाही हैं। यही साधाकों को बहकाया करता
है (दे. अखरावट)। कवि ने नारद को झगड़ा लगानेवाला सुनकर ही शायद शैतान बनाया
है। इसी प्रकार 'पद्मावत' में रसायनियों की बहुत सी बातें आई हैं। 'जोड़ा
करना' आदि उनके कुछ पारिभाषिक शब्द भी पाए जाते हैं। गोरखपन्थियों की तो
जायसी ने बहुत-सी बातें रखी हैं। सिंहलद्वीप में पद्मिनी स्त्रियों का होना
और योगियों का सिद्ध होने के लिए वहाँ जाना उन्हीं की कथाओं के अनुसार है।
इन सब बातों से पता चलता है कि जायसी साधारण मुसलमान फकीरों के समान नहीं
थे। वे सच्चे जिज्ञासु थे और हरएक मत के साधु महात्माओं से मिलते जुलते
रहते थे और उनकी बातें सुना करते थे। सूफी तो वे थे ही।
इस उदार सारग्रहिणी प्रवृत्ति के साथ ही साथ उन्हें अपने इस्लाम धर्म और
पैगम्बर पर भी पूरी आस्था थी, यद्यपि कबीरदास के समान उन्होंने भी
उदारतापूर्वक ईश्वर तक पहुँचने के अनेक मार्गों का होना तत्त्वत: स्वीकार
किया है-
विधिना के मारग हैं तेते। सरग नखत, तन रोवाँ जेते॥
पर इन असंख्य मार्गों के होते हुए भी उन्होंने मुहम्मद साहब के मार्ग पर
अपनी श्रद्धा प्रकट की है-
तिन्ह महँ पन्थ कहौं भल गाई। जेहि दूनौं जग छाज बड़ाई॥
सो बड़ पन्थ मुहम्मद केरा। है निरमल कैलास बसेरा॥
जायसी बड़े भावुक भगवद्भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध पहुँचे हुए
फकीर माने जाते थे, पर कबीरदास के समान अपना एक 'निराला पन्थ' निकालने का
हौसला उन्होंने कभी न किया। जिस मिल्लत या समाज में उनका जन्म हुआ उसके
प्रति अपने विशेष कर्तव्योंक के पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्यधर्म के
सच्चे अनुयायी थे। सच्चे भक्त का प्रधान गुण दैन्य उनमें पूरा पूरा था।
कबीरदास के समान उन्होंने अपने को सबसे अधिक पहुँचा हुआ कहीं नहीं कहा है।
कबीर ने तो यहाँ तक कह डाला कि इस चादर को सुर, नर, मुनि सबने ओढ़कर मैली
किया, पर मैंने 'ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया'। इस प्रकार की
गर्वोक्तियों से जायसी बहुत दूर थे। उनके भगवत्प्रेमपूर्ण मानस में अहंकार
के लिए कहीं जगह न थी। उनका औदार्य वह प्रच्छन्न औद्धत्य न था जो किसी धर्म
के चिढ़ाने के काम में आ सके। उनकी वह उदारता ऐसी थी जिससे कट्टरपन को भी
चोट नहीं पहुँच सकती थी। प्रत्येक प्रकार का महत्त्व स्वीकार करने की
क्षमता उनमें थी। वीरता, ऐश्वर्य, रूप, गुण, शील सबके उत्कर्ष पर मुग्ध
होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त था, तभी 'पद्मावत' ऐसा चरितकाव्य लिखने की
उत्कण्ठा उन्हें हुई। अपने को सर्वज्ञ मानकर पण्डितों और विद्वानों की
निन्दा और उपहास करने की प्रवृत्ति उनमें न थी। वे जो कुछ थोड़ा बहुत जानते
थे उसे पण्डितों का प्रसाद मानते थे-
हौं पण्डितन्ह केर पछलगा। किछु कहि चला तबल देइ डगा॥
यद्यपि कबीरदास की और उनकी प्रवृत्ति में बहुत भेद था-कबीर विधिविरोधी थे
और वे विधि पर आस्था रखनेवाले, कबीर लोकव्यवस्था का तिरस्कार करनेवाले थे
और वे सम्मान करने वाले-पर कबीर को वे बड़ा साधक मानते थे, जैसा कि इन
चौपाइयों से प्रकट होता है-
ना-नारद तब रोई पुकारा। एक जोलाहे सौं मैं हारा॥
प्रेम तन्तु निति ताना तनई। जप तप साधि सैकरा भरई॥
जायसी को सिद्ध योगी मानकर बहुत से लोग उनके शिष्य हुए। कहते हैं कि
पद्मावत के कई अंशों को वे गाते फिरते थे और चेले लोग भी साथ साथ गाते चलते
थे। परम्परा से प्रसिद्ध है कि एक चेला अमेठी (अवध) में जाकर उनका नागमती
का बारहमासा गा गाकर घर घर भीख माँगा करता था। एक दिन अमेठी के राजा ने उस
बारहमासे को सुना। उन्हें वह बहुत अच्छा लगा, विशेषत: उसका यह अंश-
कँवल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गयउ सुखाइ।
सूखि बेलि पुनि पलुहै, जो पिय सींचै आइ॥
राजा इस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने फकीर से पूछा, 'शाह जी! यह दोहा किसका
बनाया है?' उस फकीर से मलिक मुहम्मद का नाम सुनकर राजा ने बड़े सम्मान और
विनय के साथ उन्हें अपने यहाँ बुलाया था।
'पद्मावत' को पढ़ने से यह प्रकट हो जाएगा कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और
'प्रेम की पीर' से भरा हुआ था। क्या लोकपक्ष में और क्या भगवत्पक्ष में,
दोनों ओर उसकी गूढ़ता और गम्भीरता विलक्षण दिखाई देती है। जायसी की
'पद्मावत' बहुत प्रसिद्ध हुई। मुसलमानों के भक्त घरानों में इसका बहुत आदर
है। यद्यपि उसको समझनेवाले अब बहुत कम हैं पर उसे गूढ़ पोथी मानकर यत्न से
रखते हैं। जायसी की एक और छोटी सी पुस्तक 'अखरावट' है जो मीरजापुर में एक
वृद्ध मुसलमान के घर मिली थी। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर
सिद्धान्त सम्बीन्धी कुछ बातें कही गई हैं। तीसरी पुस्तक 'आखरी कलाम' के
नाम से फारसी अक्षरों में छपी है। यह भी दोहे-चौपाइयों में है और बहुत छोटी
है। इसमें मरणोपरान्त जीव की दशा और कयामत के अन्तिम न्याय आदि का वर्णन
है। बस ये ही तीन पुस्तकें जायसी की मिली हैं। इनमें से जायसी की कीर्ति का
आधार 'पद्मावत' ही है। यह प्रबन्ध काव्य हिन्दी में अपने ढंग का निराला है।
यह इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका अनुवाद बंगभाषा में सन् 1650 ई. के आसपास
अराकान में हुआ। जायसवाले इन तीन पुस्तकों के अतिरिक्त जायसी की दो और
पुस्तकें बतलाते है। -'पोस्तीनामा' तथा 'नैनावत' नाम की प्रेमकहानी।
'पोस्तीनामा' के सम्बकन्धा में उनका कहना है कि मुबारकशाह बोदले को लक्ष्य
करके लिखी गई थी, जो चण्डू पिया करते थे।
मलिक मुहम्मद जायसी
भाग - 1 //
भाग - 2 //
भाग - 3 //
भाग - 4 //
भाग - 5 //
भाग - 6 //
भाग - 7 //
भाग - 8 //
भाग - 9 //
अनुक्रम
|