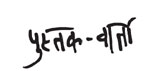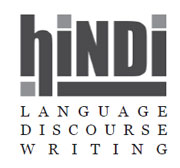|
बहादुर
शाह ज़फ़र
(1775 – 1862)
ग़ज़ल
नहीं
इश्क़ में इसका तो रंज हमें, किशिकेब-ओ-क़रार ज़रा न रहा
ग़मे-इश्क़ तो अपना रफ़ीक़ रहा, कोई और
बला से रहा-न-रहा
दिया अपनी
ख़ुदी को जो
हमने मिटा, वह जो परदा-सा बीच में था न रहा
रहे परदे में अब न वो परदानशीं, कोई दूसरा उसके सिवा न रहा
न थी हाल की जब हमें अपने ख़बर, रहे देखते औरों के ऐबो-हुनर
पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा
हमें साग़रे-बादा के देने में अब, करे देर जो साक़ी तो हाय ग़ज़ब
कि यह अहदे-निशात ये दौरे-तरब, न रहेगा जहाँ में सदा न रहा
उसे चाहा था मैंने कि रोक रखूँ, मेरी जान भी जाये तो जाने न दूँ
किए लाख फ़रेब करोड़ फ़सूँ, न रहा, न रहा, न रहा, न रहा
‘ज़फ़र’
आदमी उसको न जानियेगा, हो वह कैसा ही साहबे, फ़हमो-ज़का
जिसे ऐश में यादे-ख़ुदा न रही, जिसे तैश में ख़ौफ़े खुदा न रहा
बयाने-ग़म
गयी यक
ब यक जो हवा पलट नहीं दिल को मेरे क़रार
करूं इस सितम का मैं क्या बयां, मिरा ग़म से सीना फिग़ार है
यह
रिआया-ए-हिन्द तबाह हुई कहो क्या-क्या इन पे जफ़ा हुई
जिसे देखा हाकिमे-वक्त ने, कहा यह भी क़ाबिले-दार है
यह किसी
ने ज़ुल्म भी है सुना कि दी फांसी लोगों को बेगुनह
वले कल्मागोइयों
की सिम्त से अभी उनके दिल में ग़ुब है
न था
शहर देहली, यह था चमन, कहो किस तरह का था यां अमन
जो ख़िताब था वह मिटा दिया, फ़क़त अब तो उजड़ा दयार है
यही तंग
हाल जो सब का है, यह करिश्मा क़ुदरते रब का है
जो बहार
थी सो ख़िज़ां हुई जो ख़िज़ां थी अब वह बहार है
शबो-रोज़ फूल में जो तुले, कहो ख़ारे-ग़म को वह क्या सहे
मिले
तौक़ क़ैद में जब उन्हें, कहा गुल के बदले यह हार है
सभी जा
वह मातमे-सख़्त
है, कहो कैसी गर्दिशे-बख़्त
है
न वह ताज है न तख़्त है, न वह शाह है न दयार है
न वबाल
तन पे है सर मिरा नहीं जान जाने का डर ज़रा
कटे ग़म
ही निकले जो दम मिरा, मुझे अपनी जिन्दगी बार है
ग़ज़ल
ऐश से गुज़री कि ग़म के साथ अच्छी निभ गयी
निभ गयी जो उस सनम के साथ अच्छी निभ गयी
दोस्ती उस दुश्मने-जाँ ने निबाही तो सही
गो निभी ज़ुल्मो-सितम के साथ अच्छी निभ गयी
ख़ूब गुज़री गरचे औरों की निशातो-ऐश में
अपनी भी रंजो-अलम के साथ अच्छी निभ गयी
बूए-गुल क्या रह के करती, गुल ने रहकर क्या किया !
बस नसीमे-सुबहदम के साथ अच्छी निभ गयी
शुक्र-सद शुक्र अपने मुँह से जो निकाली मैंने बात
ऐ ज़फ़र उसके करम के साथ अच्छी निभ गयी
ग़ज़ल
क्या कहें उनसे बुतों में हमने क्या देखा नहीं
जो यह कहते हैं सुना है, पर ख़ुदा देखा नहीं
ख़ौफ़ है रोज़े-क़यामत का तुझे इस वास्ते
तूने ऐ ज़ाहिद! कभी दिन हिज्र का देखा नहीं
तू जो करता है मलामत देखकर मेरा ये हाल
क्या करूँ मैं तूने उसको नासिहा देखा नहीं
हम नहीं वाक़िफ़ कहाँ मसज़िद किधर है बुतकदा
हमने इस घर के सिवा घर दूसरा देखा नहीं
चश्म पोशी दाद-ओ-दानिस्तख: की है ऐ ज़फ़र वरना
उसने अपने दर पर तुमको क्या देखा नहीं |
ग़ज़ल
सूफ़ियों
में हूँ न रिन्दों में, न मयख़्वारों में हूँ,
ऐ बुतो, बन्दा ख़ुदा का हूँ,
गुनहगारों में हूँ!
मेरी
मिल्लत है मुहब्बत, मेरा मज़हब इश्क़ है
ख़्वाह हूँ मैं क़ाफ़िरों में, ख़्वाह दीं-दारों में हूँ
नै
मेरा मूनिस है कोई, और न कोई
ग़म-गुसार
ग़म मेरा ग़मख़्वार है, मैं ग़म के ग़मख़्वारों में हूँ
जो
मुझे लेता है, फिर वह फेर देता है मुझे
मैं अजब इक जिन्स नाकारा ख़रीदारों में हूँ
ऐ
ज़फ़र मैं क्या बताऊँ तुझको, जो कुछ हूँ सो हूँ
लेकिन अपने फ़ख़्रे-दीं के कफ़श
बरदारों में हूँ
ग़ज़ल
न
किसी की आँख का नूर हूँ न किसी के दिल का क़रार हूँ। जो किसी के काम न आ
सके मैं वह एक मुश्तेग़ुबार हूँ
मैं
नहीं हूँ नग़मा ए जाँ फ़िज़ा कोई सुन के मेरी करेगा क्या ?
मैं बड़े ही दर्द की हूँ सदा किसी दिल जले से पुकार हूँ।
मेरा
रंग-रुप बिगड़ गया मेरा हुस्न मुझसे बिछ़ड़ गया
चमन खिजाँ से उजड़ गया मैं उसी की फ़सले-बहार हूँ
कोई
फ़ातिहा पढ़ने
आए क्यों कोई चार फूल चढ़ाए क्यों ?
कोई आ के शम्मा जलाए क्यों कि मैं बेकसी का मज़ार हूँ
न
‘ज़फ़र’
किसी का रक़ीब हूँ न ‘ज़फ़र’
किसी का हबीब हूँ
जो बिगड़ गया वह नसीब हूँ जो उजड़ गया वह दयार हूँ
लगता
नहीं है जी मेरा
लगता
नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में
किस की बनी है
आलम-ए-नापायेदार में
कह दो इन हसरतों से कहीं
और जा बसें
इतनी जगह कहाँ है
दिल-ए-दाग़दार
में
उम्र-ए-दराज़ माँग कर लाये
थे चार दिन
दो आरज़ू में कट गये दो
इन्तज़ार में
कितना है बदनसीब "ज़फ़र"
दफ़्न के लिये
दो गज़ ज़मीन भी न
मिली कू-ए-यार में
हमने
दुनिया में आके क्या देखा
हमने
दुनिया में आके क्या देखा
देखा जो कुछ सो ख़्वाब-सा
देखा
है तो
इन्सान ख़ाक का
पुतला
लेक पानी का बुल-बुला देखा
ख़ूब देखा जहाँ के
ख़ूबाँ को
एक तुझ सा न दूसरा देखा
एक दम पर हवा न बाँध हबाब
दम को
दम भर में याँ हवा
देखा
न हुये तेरी ख़ाक-ए-पा हम
ने
ख़ाक में आप को
मिला देखा
अब न दीजे "ज़फ़र" किसी को
दिल
कि जिसे देखा बेवफ़ा देखा
ग़ज़ल
अगर ग़फ़लत का परदा हम उठाते अपनी आँखों से
तो जो वाँ देखते, याँ देख जाते अपनी आँखों से
बला से आप ही पैग़म्बर
हम अपने हो जाते
कि जाते वाँ और उसको देख आते, अपनी आँखों से
मिलायेंगे नज़र किससे कि वह बेदीद हैं ऐसे
नहीं आईना में आँखें मिलाते, अपनी आँखों से
जो वह आँखों में आया कौन उसको देख सकता था
क़सम आँखों की हम उसको छुपाते अपनी आँखों से
‘ज़फ़र’ गिरिया हमारा कुछ-न-कुछ तासीर रखता है
उन्हें हम देखते हैं, मुसकुराते अपनी आँखों से
बसन्त
हवा है अब्र है और सैर-सब्ज़ा-ज़ारे-बसन्त
शिगुफ़्ता क्योंऔ न हो दिल देखकर बहारे-बसन्त
ख़बर बसन्त की भी कुछ तुझे है ऐ साक़ी !
पियाला भर, कि है फिर आमदे-बहारे-बसन्त
किया बसन्त के मिलने का वादा जो उसने
तमाम साल रहा हमको इन्तज़ारे-बसन्त
समझ न सेहने-चमन में इसे गुले-नरगिस
झुकी हुई है ‘जफ़र’ चश्म- पुर-ख़ुमारे-बसन्त
बहादुर शाह ज़फ़र - भाग 2
|