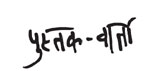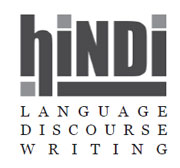| हिंदी का रचना संसार | ||||||||||||||||||||||||||
|
मुखपृष्ठ | उपन्यास | कहानी | कविता | नाटक | आलोचना | विविध | भक्ति काल | हिंदुस्तानी की परंपरा | विभाजन की कहानियाँ | अनुवाद | ई-पुस्तकें | छवि संग्रह | हमारे रचनाकार | हिंदी अभिलेख | खोज | संपर्क |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
स्वामी सहजानन्द सरस्वती रचनावली-4 सम्पादक - राघव शरण शर्मा किसान क्या करें
(4)किसान और जमींदार मगर किसानों की असली हालत और उससे ताल्लुक रखने वाले काश्तकारी कानून (Tenancy act) को जानने के लिए उसमें क्या दोष-गुण हैं, हमें यहाँ की जमीन के बन्दोबस्त (Land tenure) का जान लेना जरूरी है। शिक्षा वगैरह की कमी तो उसी हालत को और भी बदतर कर देती है। बेशक, यदि किसानों के हक के लिए लड़ने और मर मिटने की माद्दा हो, भाव हो तो शिक्षा उन्हें ऐसा बना देती है कि आसानी से ही जल्द से जल्द अपना हक हासिल कर लेते हैं। और अगर यह माद्दा उनमें न हो तो भी शिक्षा के फलस्वरूप धीरे-धीरे उस ओर बढ़ते हैं। इसीलिए हर हालत में शिक्षा निहायत जरूरी है, उनकी प्रगति की जान (essential) है, जैसा कि कहा गया है। मगर झारखंडी किसान तो बड़े ही बहादुर और जमीन के सच्चे प्रेमी हैं यह बात पहले कही जा चुकी है। इनके जमीन सम्बन्धी प्रेम और इनकी बहादुरी के बहुत से दृष्टांत पाए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के नागवंशी राजे, जिनके हाथ में पहले यहाँ का शासन था, इन्हीं के यहाँ के मूल निवासियों के ही वंश के थे। पुरानी पंचायती प्रथा के अनुसार ही इनने उन्हें अपना सरदार और मुखिया चुना, जो समय पाके इनके मालिक बन गए, जैसा कि सामन्तशाही का इतिहास सभी देशों में पाया जाता है और जमींदारी प्रथा की बुनियाद जिससे कायम हुई है। मुगल जमाने तक तो बात ठीक पाई गई बताई जाती है। मगर पीछे दिल्ली दरबार में जाने-आने का सिलसिला खतरनाक साबित हुआ। जब तक इन जंगलों में वे लोग रहे तब तक तो राजसी ठाट-बाट और व्यसन की वैसी बात थी नहीं। मगर वहाँ जाने पर साज-सामान और घोड़े-हाथी वगैरह का शौक देखा-देखी जरूरी था। ऐयाशी भी सूझी। फिर तो इन सामानों और हाथी-घोड़ों को पहुँचाने वाले लोगों का प्रसार यहाँ होना जरूरी था। पश्चिमी प्रान्तों से सिख, पठान और दूसरे कारबारी पहुँचने लगे और दरबारी सामान वगैरह पहुँचा के माल लूटने लगे। जब सामान के बदले रुपए नहीं मिलते तो गाँव के गाँव ठेके पर दे दिए जाते। इस प्रकार बाहरी जमींदारों का यहाँ पदार्पण हो गया। दूसरे तरीकों से भी कुछ लोग पहुँचे ही थे। दोस्ती और लड़ाई के जरिए भी, जैसा कि पहले होता था, बहुतेरे लोग आ गए। मुगलों की खुशामद और अंग्रेजों की सेवा के बल पर भी 1765 के बाद कुछ लोगों का यहाँ पहुँच जाना जरूरी था। अब तो खरीद-बिक्री के जरिए भी कितने ही आ गए हैं। विवाह-शादी और नाते-रिश्ते के चलते भी पहले ही बहुतेरे आए। दुर्भेद्य जंगलों में गढ़ बना के रहने के लिए भी कुछ लोग पहुँची गए। इस प्रकार जब धीरे-धीरे बाहरी शोषक लोग यहाँ जम के किसानों का दोहन और शोषण करने लगे तो ये घबराए और इनकी ऑंखें खुलीं कि यह क्या? मारवाड़ी साहूकारों और दूसरे बनिए महाजनों ने भी इन्हें कम नहीं लूटा। इनके खेती से गाढ़ी कमाई जो भी मिलती सब की सब इन जमींदारों, मारवाड़ियों और सूदखोर बनियों के पेट में चली जाती। यहाँ तक कि इनकी इज्जत-आबरू तक पर आ बनती। नए अंग्रेजी कानूनों की शरण लेके इन भोले-भाले किसानों का रक्त चूसा जाता, जमीनें छीनी जातीं और ये गुलाम बना लिये जाते। जेलों में भी बन्द हो जाने की नौबत बार-बार आती थी। इससे ऊबकर छोटानागपुर के किसानों ने 1820 और 1831-32 में तथा उसके बाद भी जानें कितनी बार बगावतें कीं, लूटपाट कीं। 1855 की 30वीं जून से प्रस्थान करके पहले पहल 7वीं जुलाई को वीरभूम में तीस हजार संथालों के दल ने जो पुलिसवालों पर हमले किए और लूटपाट की वह इसी अत्याचार से ऊब जाने के बाद ही हुई। 1889-90 से लेकर फिर जो गड़बड़ी हुई और 1895 में जो बीरसा आन्दोलन राँची जिले में शुरू होके आग की तरह चारों ओर बात की बात में फैल गया उसके भीतर भी यही बात थी। सबसे आखिर में जो 'तानाभगत' आन्दोलन 1914 के यूरोपीय महासमर के शुरू होने पर जारी होके 1921 के असहयोग के समय तक काफी तेज था वह तो साफ ही किसान आन्दोलन था। ताना लोगों का एक जबर्दस्त दल जमींदारों को लगान देने से साफ इनकार करता, जेल जाता, तबाह होता और जमीनें नीलाम करवाता था। जबकि भारत में रौलटएक्ट और पंजाब के मार्शल लॉ की बातें लेकर तथा खिलाफत के मसले पर भी राजनीतिक आन्दोलन बड़े-बड़े धुरंधर नेता चालू कर रहे थे। उसी समय झारखंड की भोले-भाले, पर बहादुर किसान अपने ही ढंग से ऐसा जबर्दस्त किसान आन्दोलन और लगान बन्दी तथा कर बन्दी की जबर्दस्त लड़ाई चला रहे थे कि देखते ही बनता था। हमारी असली लड़ाई का रूप तो उनने ही खड़ा किया और सारे मुल्क का प्रदर्शन वे लोग जबान से नहीं, अपने कामों से कर रहे थे। वे तो मूक ठहरे। शिक्षा तो उन्हें दी गई न थी। फिर बोलते क्या बोलने का काम तो देश के दूसरे कोने में नेता लोग करी रहे थे। बोलना ज्यादातर उनका काम था और काम करना इनका। असल में तानाभगतों की वह लगानबन्दी हर्गिज नहीं रुकती, यदि 1921 के आश्विन में गांधी जी खुद रांची में आके उन्हें अपनी जबान से नहीं रोकते और पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग घूम-घूम के प्रचार नहीं करते कि जमींदार का लगान जरूर दे दो! यह हमारी राजनीति का नमूना और यह है यहाँ के किसानों की लड़ाई का सच्चा रूप। ये सीधे और भोले किसान तो धर्म में साधु -महात्मा में विश्वास करते थे। ये लोग भगत तो कहे जाते ही थे। बस गाँधी जी को महात्मा समझ इनने उनकी आज्ञा मान कर बन्दी बन्द कर दी। जब इनकी नाकों दम हो जाता है ये सीधे लोग तभी उभड़ते हैं। नहीं तो जहाँ तक हो सकता है जुल्मों को चुपचाप पशु की तरह बर्दाश्त करते जाते हैं। 1820 और 1831-32 के जमाने में ये कैसे सताए गए तब इनने क्या किया इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ हम कैप्टन डालटन के शब्दों में लिखते हैं जो उस समय छोटानागपुर के प्रबन्धक थे। वे लिखते हैं कि 'The oppressions of these men (jagirdars) were however borne with courage, but a far worse class of men had obtained a footing in the country about the year 1820, when the late Maharaja Jagarnath Sahi Deo obtained his ancestral gadi on the death of his father in July of that year. These men were Musalmans, Sikhs and some others who came to the country as horse dealers, and shawl and brocade merchants, fetched enormous offers for their goods from the Nagvanshi Chiefs and obtained farms of villages instead of cash, of which latter the Chiefs were always in want. The foreign farmers having but a temporary interest in the villages squeezed as much as possible from the ryots in the shape of rents, abwabs and salami. But this was not all. They proved their yoke to be galling indeed and rendered true the very name thikadar in Chhotanagpur in farms.* ^The Pathans have taken our hoormat and the Sikhs our sisters, our lives are of no value, and being of one caste let us stand fast to each other and commence to plunder, murder and loot,* thus said they. 'जागीरदारों के जुल्मों को तो इन लोगों ने किसी प्रकार हिम्मत करके बर्दाश्त किया। मगर 1820 की जुलाई में अपने पिता के मरने पर भूतपूर्व महाराजा जगरनाथ शाही देव को जब गद्दी मिली उस समय एक दूसरे ही दल के लोगों को इस प्रदेश में जगह मिल गईं। ये लोग थे मुसलमान, सिख और कुछ दूसरे जो घोड़ों कारचोबी की चीजों और शाल-दुशालों के सौदागर थे। इन्हें अपने माल के लिए इन नागवंशी राजाओं से काफी पैसे मिलते थे। मगर पास में पैसे न होने से ये राजे अपने गाँव इन्हें ठीके में दे दिया करते थे। इन बाहरी ठीकेदारों का गाँवों से और क्या स्वार्थ था सिवाय इसके कि थोड़ी ही मुद्दत में ज्यादा से ज्यादा पैसे किसानों से लगान, अबवाब और सलामी के रूप में जबर्दस्ती चूसें? लेकिन इतना ही न था। सचमुच उनने किसानों को सता-सता के अपना ठीकेदार नाम छोटानागपुर में सार्थक कर दिया!' ऊब कर किसानों ने कहा कि 'पठानों ने हमारी इज्जत (हुर्मत) और सिखों ने हमारी बहनें ले लीं। हमारी जिन्दगी अब बेकार है। हम तो एक ही वर्ग (जाति) के हैं। इसीलिए आइए परस्पर एक-दूसरे से खूब मिल जाएँ और लूटमार, कत्ल और डाका शुरू कर दें।' उनने जो कुछ भी ऊबकर किया यहाँ उसके खंडन-मंडन से हमारा मतलब नहीं है। उनने तो उसका नतीजा खुद भोगा। हमें तो सिर्फ यही दिखाना है कि जब कोई रास्ता यहाँ के किसानों को नहीं सूझता तो हथेली पर जान लेके खड़े हो जाते हैं और लूटमार शुरू करके स्वयं भी तबाह हो जाते हैं। और रास्ता तो अब तक उन्हें मालूम न था। इसीलिए उनने कहा कि हमारा जीना धिक्कार है। यहाँ पर जो उनका यह कहना लिखा है कि हम एक ही जाति या वर्ग के हैं, बड़े ही मार्के का है। इससे पता चलता है कि उनमें वर्गचेतना (class consciousness) बहुत पहले से ही है। यह ठीक है कि वह पुराने ढंग की है और उसे नए साँचे में ढालना होगा। वे संगठन भी बड़ा पक्का करते हैं और लाखों की तादाद में एक ही साथ इसीलिए उठ खड़े होते हैं। यही तो उनका असली बल है। मगर इसका प्रयोग ठीक रास्ते पर तथा उचित नेतृत्व में होना चाहिए। ऐसे समयोपयोगी नेतृत्व का उनमें एकदम अभाव है। इसे पैदा करना हमारा काम है। इसी प्रकार हण्टर ने जो अपनी किताब बंगाल की देहातों के इतिहास (Annuals of Rural Bengal by W.W. Hunter) में संथालों के 1855 वाले विद्रोह के बारे में लिखा है उसकी भी कुछ पंक्तियाँ यहाँ जानकारी के लिए लिख देना जरूरी है। उनसे उन गरीबों की लूट और उन पर होने वाले अत्याचारों का पता चलता है। वहाँ लिखा है कि, 'They cheated the poor Santal in every transaction. The forestor brought his jars of clarified butter for sale, the Hindus measured in vessels for salt, oil, cloth and gunpowder; the Hindu used heavy weights in ascertaining the quantity of grain, light ones in weighing out the articles given in return. If the Santal remonstrated, he was told that salt, being and excisable commodity, had a set of weights and measures peculiar to itself. The fortunes made by trafic in produce were augmented by usury. ‘The Hindu dealer gave them a few shillings worth of rice, and seized the land as soon as they had cleared it and sown the crop. Another family, in a fit of hospitality, feasted away their whole harvest, and then opened an account at the grain dealers, who advanced enough to keep them above starvation during the rest of the year. From the moment the peasant touched the borrowed rice, he and his children were the serfs of the corn merchant. No matter what economy the family practised, no matter what effort they made to extricate themselves, stint as they might, toil as they might, the Hindu claimed this whole crop, and carried on a balance to be paid out of the next harvest. ‘Year after year Santhals sweated for his oppressor. If the victim threatened to run off into the jungle, the userer instituted a suit in the courts, taking care that the Santhal should know nothing of it till the decree had been obtained and execution taken out. Without the slightest warning, the poor husbandsman's buffaloes, cows and little homestead were sold, not omiting the bronze household vessels which formed the sole heirloom of the family. Even the cheap iron ornaments, outward tokens of female respectability among the Santhals, were torn from the wife's wrists.* ये बनिए हर बात में संथालों को ठगते थे। जंगली लोग घड़े भर के शुद्ध घी लाते थे और हिन्दू बनिए उसे नमक, तेल, कपड़ा और बारूद तौलने के बर्तनों से (क्योंकि पहले तराजू की जगह बर्तनों से ही तौल होती थी और आज भी संथाल वगैरह ऐसा ही करते हैं) ही तौलते थे। बनिए अपनी चीजों को हलके बाटों से और संथाल किसानों के गल्ले को वजनी बाटों से तोलते थे। यदि संथाल इस पर कुछ हो हल्ला करते तो चट उन्हें कह देते कि नमक पर तो टैक्स लगता है। इसीलिए उसके तौलने के बाट वगैरह और ही हैं। इस प्रकार चीजों की लेन-देन में जो नफा वे कमाते थे उसे सूदखोरी के जरिए और भी बढ़ाते थे। 'हिन्दू बनिए संथालों को कुछी रुपयों के चावल देकर उनकी सारी जमीनों को फौरन हथिया लेते जिन्हें साफ करके उनमें वे फसल बोते थे। कोई घर ऐसा होता कि खिलाने-पिलाने की उमंग में सारी पैदावार खर्च कर देता और उसके बाद गल्ला बेचने वालों से उधार अन्न खर्च के लिए लेता था। ये गल्ले वाले अन्न देकर साल के बाकी दिनों में उन्हें भूखों मरने से बचा लेते थे सही। मगर ज्योंही किसान ने उनसे चावल वगैरह उधार लिया कि वे और उनके बाल बच्चे बनियों के गुलाम बन गए! फिर चाहे कितनी ही किफायत से खर्च करें और बनिए से पिंड छुड़ाने के लिए हजार कोशिश करें, जितनी भी कंजूसी करें और कलेजा फाड़ के मेहनत करें। मगर बनिया उनकी सारी फसल का दावीदार बनने के साथ ही आगे के लिए कुछ न कुछ बकाया भी रख छोड़ता था। 'प्रति साल इन जालिमों के लिए संथाल खून को पसीना बनाते रहते थे। यदि ऊबकर जंगल में भाग जाना चाहते तो सूदखोर उन पर अदालतों में केस करते थे। मगर यह काम इस चालाकी से किया जाता था कि जब तक डिक्री होके दखल दिहानी जारी न हो जाए तब तक बेचारे संथाल को इसका जरा भी पता चले ही न। फिर तो बिना कहे-सुने ही उस गरीब की भैंसें, गाएँ और घर-बार सभी चीजें नीलाम कर ली जाती थीं, यहाँ तक कि बाप-दादों के वक्त के जो काँसे के बर्तन होते वे भी न बच पाते। गरीब संथाल की औरत की इज्जत की निशानी के रूप में उसकी कलाइयों में लोहे के जेवर होते वे भी जबर्दस्ती छीन लिये जाते थे!'' इसी का नतीजा था वह 1855 के मध्य का संथाल-विद्रोह जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं। हजारीबाग वगैरह के बारे में तो पहले ही कह चुके हैं। गत सर्वे की रिपोर्ट में भी उनके बारे में यही लिखा है कि उनने जो विद्रोह किया था वह इन सूदखोरों और जालिमों से ही बचने के लिए। जैसे 1855 में तीस हजार संथालों ने जमा होके यह काम किया। ठीक उसी तरह 1831 में छोटानागपुर वालों ने भी गिरोह बाँध के यही काम किया था। साफ लिखा है कि, 'They unnaturally became excited by the weakening of the authority and thought the occasion opportune for squaring with the oppressive money lenders and others. Several bands of Santals collected for marauding purposes.' 'जैसा कि आमतौर से नहीं होता वैसी गर्मी उनमें आ गई जबकि शासन सूत्र की कमजोरी का उन्हें अन्दाज लगा। उनने सोचा कि यही मौका है कि जालिम बनियों, सूदखोरों और दूसरों से बदला सधा लिया जाए। फलत: गिरोह के गिरोह संथाल लूटपाट वगैरह के लिए जमा हो गए!' यहाँ तो सरकार की कमजोरी का जिक्र है। मगर संथाल परगना के संथालों के सम्बन्ध में तो लिखा गया है कि वे कलकता जाके लाट साहब को अर्जी देना चाहते थे कि जुल्म होता है और आपकी अदालतें भी हमें सताती हैं। चाहे बात कुछ भी क्यों न हो। मगर जब उनने देखा कि न्याय के नाम पर अंग्रेज, कानून और अदालतें उनका खून कर रही हैं और शोषक मालदारों का ही साथ दे रही हैं तो सरकार के ऊपर उनका गुस्सा जरूरी हो गया। नतीजा यह हुआ कि सरकार को तमाचे लगे और उसने सोचा कि इनके साथ दूसरे ढंग से पेश आना चाहिए। इनकी अपनी रहन-सहन और रीति-रिवाज पर ध्यान देना उसने जरूरी समझा। चाहे वह उनकी यथार्थत: रक्षा भले ही न कर सकी, और उसके लिए यह संभव भी न था। फिर भी उसी तरह की कानूनी व्यवस्था का इन्तजाम उसने करना शुरू कर दिया। एक ओर सभ्यता के शिखर पर बैठी सरकार और दूसरी ओर अवनति के अतल गर्त में गिरे ये किसान! फिर दोनों का मेल हो तो कैसे? चाहे वह हजार कहे कि हमें इन आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था के ही अनुसार चलना है। फिर भी वह भारत में जिस काम के लिए आई वह तो शोषण की बुनियाद पर चल सकता है। इसीलिए घुमा-फिरा के इनका भी शोषण होई जाता है। फिर भी 1897 के छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट, 1879 के छोटानागपुर लैंडलोर्ड टेनेन्ट प्रोसीजर एक्ट, 1879 के छोटानागपुर कम्यूटेशन एक्ट, 1903, 1905 और 1908 के छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट्स वगैरह के जरिए यहाँ का शासन कुछ दूसरे ही ढंग से चलाया जाने लगा ताकि वैसी लूट न हो सके। इसी तरह 1855, 1859, 1872, 1888 आदि के खास ढंग के नियमों और विधानों के ही अनुसार संथाल परगना का शासन होने लगा। संथाल परगना को सब तरह के साधारण विधानों से बाहर (non-regulation) और छोटानागपुर को पिछड़ा हुआ (backward) इलाका भी तभी से घोषित किया गया जो आज तक यह बात किसी न किसी रूप में मौजूद है। लेकिन किसानों के त्याग और बलिदान ने इतना कर तो दिया। इससे आगे का रास्ता भी साफ हो गया। किसानों की समय-समय की बेचैनी और उतेजना को जानने के साथ ही यहाँ की जमीन की बन्दोबस्ती व्यवस्था कैसी है यह भी जानना जरूरी है। उसमें भी किसानों की काश्तकारी जमीनें कितनी तरह की हैं इसका तो आगे स्वतंत्र वर्णन करेंगे। क्योंकि यहाँ की खास बात है और इससे स्थिति का कुछ खास पता चलता है। यहाँ सिर्फ जमींदारी या जमीन की मलिकाई पर ही प्रकाश डालना है। किसानों की असली लड़ाई तो इसी जमींदारी प्रथा से है। अतएव उसके बारे में एवं तत्संबंधी कानूनों के बारे में जो कुछ आगे कहा जाएगा उसे समझने के लिए यहाँ यह जान लेना है कि यहाँ के प्रधान जमींदार कैसे और कौन-कौन से हैं। झारखंड के कुल छह जिलों में तीन तरह के जमींदार पाए जाते हैं। बिहार की भी यही हालत है। मगर यहाँ जो कुछ विशेषता है वह यह है कि सरकार यहाँ सबसे बड़ा जमींदार है। दामिने कोह, संथाल परगना की बात तो पहले ही कही जा चुकी है। घने पर्वतों के बीच के बहुत बड़े भूभाग पर, जिसका क्षेत्र समूचे जिले के क्षेत्रफल का प्राय: एक-चौथाई है और करीब डेढ़ हजार वर्गमील में जो फैला है, सरकारी जमींदारी या खासमहाल है जिसे गवर्नमेंट इस्टेट भी कहते हैं। यह सबसे पिछड़ा इलाका है। इसी में साठ हजार पहड़िया लोग बसते हैं। जिनके एक बच्चे के भी पढ़ने का प्रबन्ध खासमहाल ने अब तक नहीं किया है। यह सरकार दूसरे जमींदारों को क्या कहेगी जब खुद जमींदार बन के कुछ नहीं करती। पहड़िया लोगों की खास तकलीफ तो आगे लिखी जाएगी। सिंहभूम के दलभूम सब-डिविजन का एक बहुत बड़ा भाग भी, जिसे कोल्हान कहते हैं, खासमहल ही है। उसी सब-डिविजन का प्रधान नगर जमशेदपुर या टाटा नगर है। यह कोल्हान भी वैसा ही पिछड़ा हुआ है जैसा कि दामिन का इलाका। यहाँ के किसान भी प्रधान रूप से वही आदिवासी लोग ही हैं जिन्हें जबान मिली ही नहीं है। और अंग्रेजों की तो हालत यह है कि इनने खुद तूफान खड़ा करके ही अपने लिए स्वराज्य हासिल किया है। इसीलिए ये तो वैसे ही आन्दोलन को समझते हैं और उसके सामने सिर झुकाते हैं। यों तो छोटे-मोटे और भी इलाके खासमहाल के हैं। इन्कम्बर्ड इस्टेट्स एक्ट के अनुसार जाने कितनी ही जमींदारियों का इन्तजाम भी खुद सरकार ही अपने कोर्ट ऑफ वाड्र्स नामक विभाग के जरिए करती है। सरकार की यह दूसरी चीज है। सरकार की एक तीसरी चीज और है। यहाँ के बहुत से घने जंगल भी ठेठ सरकार के ही हाथ में हैं और उनका इन्तजाम वह खुद करती है। यों तो जमींदारों के भी अपने जंगल हैं जो सुरक्षित (reserved) हैं और जिनके भीतर कोई आदमी या पशु पाँव तक नहीं दे सकते। मगर सरकारी सुरक्षित जंगल (reserved forest) बहुत ज्यादा हैं। इन सुरक्षित जंगलों के चलते और तकलीफें तो हईं जिन्हें आगे बताएँगे, मगर इनके पास के किसान और उनके पशु खासकर र्गमीयों में पानी के बिना मर जाते हैं। असल में पानी के सोते ऐसे ही जंगलों में होते हैं जो घने, आबाद और सुरक्षित होते हैं। पहाड़ों में कुऑं खोदना भी किसानों के बिसात के बाहर की बात है। जमींदार या सरकार को तो इसकी परवाह होती ही नहीं। अब अगर वे या उनके पशु पानी पीने के लिए रक्षित जंगलों के झरनों पर जाएँ तो कानून के अनुसार फौरन उन पर केस चले। यह तो आम बात है और किसान इसके चलते खून के ऑंसू रोते रहते हैं। इस पर आगे ज्यादा कहेंगे। अब रहे गैर-सरकारी जमींदार। वे भी दो तरह के हैं। एक तो घटवार और दूसरे साधारण जमींदार। ये साधारण या आमतौर के जमींदार तो वही हैं जो बिहार में पाए जाते हैं। उनमें और इनमें, जहाँ तक इनका किसानों से ताल्लुक है, कोई बुनियादी फर्क नहीं है। हाँ, इनके खास अधिकार हैं जो गवर्नमेंट से इन्हें प्राप्त हैं, जैसा कि कर्ज में डूबने पर खासतौर से उसकी जाँच वगैरह करके असल कर्ज का पता लगाना और उसके चुकाने के लिए सरकार के द्वारा जमींदारी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना इत्यादि। इसी तरह की कुछ और भी बातें हैं। मगर यह कोई मौलिक या बुनियादी फर्क है नहीं। इस फर्क से किसानों का कोई मतलब भी नहीं है। मगर घटवार या घटवाल तो निराले ढंग के जमींदार हैं। उन्हें यह जमींदारी तो खास तरह के काम या सेवा के लिए ही दी गई है। इसीलिए अंग्रेजी में 'र्सवस टेन्योर' या 'काम के लिए दी गई जागीर' कहते हैं। जिस प्रकार जमींदार या किसान चौकीदार, नाऊ, पुरोहित आदि को पहले कुछ जमीनें जागीर के रूप में दे देते थे। ठीक उसी तरह की यह चीज है, जागीर है। फर्क इतना ही है कि यह खुद सरकार के द्वारा दी गई है। इसीलिए उसी जागीर की तरह यह भी छिनी जा सकती है यदि घटवाल अपनी डयूटी समय पर अदा न करे। यहाँ के डिप्टी कमिश्नरों की जरा भी नजर बिगड़ी और यह घटवाली गई! झारखंड में घटवार नाम की एक जाति भी है। शायद उस जाति के लोग पहले वही काम करते हों जो पीछे इन घटवारों को दे दिए गए। इसीलिए तो गोड़ाइत नामक एक और भी जाति यहाँ हो गई है। मगर ये जो जमींदार के रूप में घटवाल आज पाए जाते हैं वह दूसरे ही हैं। उनका घटवार जाति से कोई ताल्लुक नहीं है। 30.11.41A यह ठीक है कि वे लोग किसी खास जाति के नहीं हैं ठीक जैसे जमींदारों की कोई एक जाति नहीं है। किन्तु सभी जाति और धर्म के लोग जमींदार हैं। घटवाल भी सभी जाति के हैं। घाटी का नाम तो अकसर पढ़ा सुना जाता है। पहाड़ों में जहाँ उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है और इसीलिए पार करने में दिक्कत होती है उसे ही घाटी कहते हैं। घाट भी उसी का नाम है। पहाड़ी इलाकों में प्रवेश करने और जाने के रास्ते यों तो आमतौर से होते नहीं। जहाँ कहीं नदियों के गुजरने से पहाड़ कटे से मालूम पड़ते हैं वहीं से इधर-उधर आ-जा सकते हैं। आजकल तो डाइनामाइट नाम की बारूद को लगाके तथा और भी वैज्ञानिक ढंगों का प्रयोग करके बड़े से बड़े पहाड़ों को काट के, उड़ा के, फाड़ के उनके बीच से रास्ते बनाए जाते हैं, सुरंगें (tunnels) बनती हैं जिनसे होके रेलें पास करती हैं। मगर पहले तो नदियों के किनारों को पकड़ के ही, या दो पहाड़ों के बीच के भारी चढ़ाव-उतार वाले रास्ते के जरिए ही पहाड़ी प्रदेशों में आना-जाना संभव था। यदि ऐसा न किया जाता तो खूँखार जानवर खा जाते और पहाड़ों के ऊपर चढ़ना गैर-मुमकिन हो जाता। यों भी पहाड़ों पर चढ़ना असंभव ही होता है। इसलिए पहले के जमाने में घाटों या घाटियों के ही जरिए आ जा सकते थे। इसीलिए राजे महाराजाओं और शासकों को इस बात की जरूरत बनी रहती थी कि इन घाटों की निगरानी की जाए, चौकसी और देखभाल बराबर की जाए, पहरेदारी हो। नहीं तो दुश्मनों या हमला करने वालों का गिरोह जाने किस रास्ते कब भीतर घुस जाए और दखल जमा ले। दिन-रात इन घाटों पर पहरा दिये बिना काम नहीं चल सकता था। दूसरा उपाय था भी नहीं। इसीलिए इस बात की जिम्मेवारी जिन लोगों पर रखी जाती थी वे घटवार या घटवाल कहे जाने लगे। पर्वतीय प्रदेश में घाटों की संख्या के ही हिसाब से कम या ज्यादा घटवाल तैनात किए जाते थे। भागलपुर, मुंगेर या गया जिले के भी दक्षिणी पहाड़ी इलाकों में जमींदार के बजाय घटवार ही रहते थे। आज भी कुछ न कुछ पाए जाते हैं। हालाँकि उनके वह काम अब कहीं भी शायद ही पाए जाते हैं। अब तो इस वैज्ञानिक युग में सभी बातें बदलचुकीहैं। मगर घटवार लोग यह काम खुद तो करते न थे। वे इसी काम के लिए काफी तादाद में चौकीदार रखते थे। और जैसे आज चौकीदारों के ऊपर दफादार होते हैं उसी तरह पहले भी रखे जाते थे। ताकि चौकीदारों के काम की देखभाल ठिकाने से होती रहे। इन्हीं सब कामों और उनके खर्च के लिए जो जमीनें घटवारों को दी जाती थीं उन्हें घटवारी या घटवाली कहते हैं। उन्हें इन जमीनों के लिए सरकार को माल या मालगुजारी बहुत ही कम देनी होती थी। एक तो बंगाल और बिहार के जमींदारों की मालगुजारी यों ही कम ठहरी। तिस पर भी तुर्रा यह कि घटवाली जमीनों पर और भी कम लगती थी। यह मालगुजारी घटती-बढ़ती भी न थी। जहाँ कहीं इस्तमरारी बन्दोबस्त नहीं है वहाँ तो मालगुजारी घटती-बढ़ती है और इस सूबे में भी कहीं-कहीं ऐसा पाया जाता है। मगर जब यह इस्तमरारी बन्दोबस्त न था तब भी घटवाली जमीनें इस्तमरारी ही थीं। संथाल परगना की जाँच की रिपोर्ट में घटवालों के बारे में यों लिखा है ^In consideration of their preforming certain duties in support of the police the ghatwals were granted a special status and protcetion. Their tenures were assessed to a low rent fixed in perpetuity and were declared inalienable and impartible. The ghatwals were precluded from granting any lease or creating any charge upon their estates beyond the term of their own life, except in case of leases for mining, irrigation or building, for which the commissioner's consent is required, and for reclamation. The net result is that when a ghatwal dies, his debts are simulataneously extinguished' (page 61). 'पुलिस की मदद के लिए कुछ खास ढंग के कामों के करने के कारण ही घटवालों को विशेष स्थान दिया गया है और उनकी रक्षा का भी खास प्रबन्ध है। उन्हें दी गई जमीनों पर बहुत ही कम लगान या माल देना पड़ता है जो घटता-बढ़ता नहीं। वे जमीनें न तो बिक सकती हैं और न उनका बँटवारा किया जा सकता है। जैसा कि मुश्तरका खानदान में जुदाई होने पर और जमीनों का होता है। घटवालों को अधिकार नहीं है कि अपनी जमीनें आमतौर से पट्टे पर दे दें। वे किसी तरह का ऐसा खर्च या कर्ज भी उन जमीनों पर ले नहीं सकते जो उनकी मौत के बाद कायम रह जाए। हाँ, खानों, सिंचाई के कामों और मकानों के ही लिए पट्टे पर जमीनें दे सकते हैं। मगर इसमें भी कमिश्नर की मंजूरी जरूरी होती है। जंगल, परती आदि गैर-आबाद जमीनों को आबाद करने के लिए पट्टा जरूर दे सकते हैं। इन सब बन्धनों का सम्मिलित परिणाम यह है कि ज्यों ही कोई घटवाल मरा कि उसका कर्ज भी अपने आप खत्म हो गया।' आगे चलके 62वें पृष्ठ में यह भी लिखा है कि 'The ghatwals are charged with the maintenance of chaukidars in their estates and on failure to meet these obligations are liable to the dismissal.' 'घटवालों को अपनी जमींदारी में चौकीदारों को रखना और तनख्वाह देना पड़ता है और ऐसा न करने पर उनकी घटवाली छीन ली जा सकती है।' इसका सीधा अर्थ यही है कि अब पुराने ढंग से न तो उन्हें घाटों की रक्षा करनी पड़ती है और न चौकीदार वगैरह रखने पड़ते हैं। अब तो सिर्फ यही होता है कि जिस घटवाल की जमींदारी के मौजों में जितने चौकीदार हों उनके वेतन के लिए उन गाँव वालों से चौकीदारी टैक्स नहीं वसूला जाकर घटवालों को ही अपने पास से वह वेतन चुकाना पड़ता है। मगर एक बात जरूर हो गई है कि बिहार प्रान्त के सभी पहाड़ी इलाकों में घटवाल या जमींदार जगह-जगह रास्तों के नाकों पर अपने खास नौकर या चौकीदार रखते हैं। ये पुलिस वाले चौकीदार नहीं हो के घटवालों और जमींदारों के निजी नौकर होते हैं। इनका काम यही होता है कि गरीब लोग जब पास के जंगलों में लकड़ी काटने जाते हैं तो उनसे पैसे वसूला करते हैं। इन्हीं पैसों या टैक्सों को अब घाट कहने लगे हैं। हमने यह दृश्य खुद देखा है। जंगली इलाकों के किसानों और गरीबों को अपने घरेलू काम के लिए और अकसर बेचकर जीविका करने के लिए भी जंगल से प्रतिदिन लकड़ी, पत्ता, घास, बाँस, फल, फूल वगैरह लेना जरूरी होता है। मगर जब तक घाट वाला टैक्स पहले ही चुकता न कर लें जंगलों में घुसने वे पाते ही नहीं। यह अत्याचार बहुत ही बढ़ा-चढ़ा है। छोटानागपुर के बाहर भी मुंगेर आदि जिलों के पहाड़ी इलाकों के किसान इससे तबाह हैं। खासमहल और घटवालों के अलावा तीसरे ढंग के जमींदार तो यहाँ वैसे ही हैं जैसे बिहार खंड में। इनमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है जैसा कि कही चुके हैं। इन छहों जिलों में तो यों छोटे-मोटे जमींदार और घटवाल बहुतेरे हैं। मगर बड़े-बड़ों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हम जानकारी के लिए यहाँ कुछ प्रमुख लोगों को ही गिना देना चाहते हैं। मगर ऐसा करने के पूर्व हजारीबाग के 1917 के गजेटियर की एक बात लिखना जरूरी समझते हैं। उसके लेखक हैं ई. लिस्टर, सी.आई.ई., आई.सी.एस.। उसके 165 पृष्ठ में जमींदारों के बारे में जो कुछ लिखा गया है उससे साफ है कि उन्हें बहुत ही नाममात्र के लिए सरकार को माल देना पड़ता है। वे लोग खूब मजा मारते हैं। वहाँ लिखा है'The demand of Rs. 47620 (due in respect of seventy permanently held estates) represents about seven rupees a square mile, and the cash rent alone which landlords receive are twelve lakhs, on which sum the government revenue is less than four percent over and above the cash rent. The landlords have extensive areas in their own cultivation and also collect a considerable produce rent.* 'इस्तमरारी बन्दोबस्त (परमानेण्ट सेटलमेण्ट) वाली सत्तर जमींदारियों से जो कुल 47620 रुपए सरकारी मालगुजारी में मिलते हैं वह प्रति वर्गमील सात रुपए के हिसाब से पड़ते हैं। मगर उनके बदले जमींदार लोग जो सिर्फ नगद लगान किसानों से वसूल करते हैं वह बारह लाख रुपया है। इसके मानी हैं यह कि नगद लगान के 4 प्रतिशत से भी कम वे लोग सरकार को देते हैं! इसके सिवाय उनकी अपनी खेती की भी बहुत ज्यादा जमीनें हैं और बँटाई या भावली लगान भी काफी वसूल करते हैं।' यह तो लूट है। घटवालों को कम माल देना पड़ता है सही। मगर झारखंडी जमींदारों की तो देखिए। यह कोई हजारीबाग जिले की खास बात थोड़े ही है। यही दशा सभी जिलों में है। किसानों से जो नगद वसूली करते हैं उसका चार सैकड़ा भी सरकार को नहीं देते! बँटाई, भावली, जंगल की आमदनी और कोयला, अबरक वगैरह की आय की तो बात ही जाने दीजिए। उसका तो हिसाब ही नहीं कि कितनी हैं। जिरात, कामत और बकाश्त के नाम पर भी बहुत ज्यादा जमीनें पड़ी हैं। सलामी और नजराना का कुछ कहना ही नहीं। अनेक अबवाब और सूद, तावान वगैरह जुदे ही ठहरे। यह लूट नहीं है, तो है क्या? फिर भी जब किसानों की ओर से कोई भी दावा पेश हो तो न सिर्फ जमींदार और घटवाल, बल्कि उनके दोस्त, दलाल और सरकारी आदमी भी हाय-तौबा मचाने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि जमींदार मरे जा रहे हैं! अच्छा तो अब कुछ प्रमुख
जमींदारों को हर जिले के हिसाब से गिना के आगे बढ़ेंगे। संथाल परगनामें ये
हैं (1) पत्संडा इस्टेट (2) मनिहारी इस्टेट (3) बलबड्डा इस्टेट (4) महेशपुर
इस्टेट (5) बभनगाँवा की घटवाली इस्टेट वगैरह। हजारीबाग में, (1) सतगांवा
(चन्द्रधारी सिंह) इस्टेट (2) गरवां (नाबालिग) इस्टेट (3) दोरंडा इस्टेट
(4) पालगंज इस्टेट (5) कुंदा इस्टेट (6) पद्मा इस्टेट (7) धानवार इस्टेट
वगैरह। राँची में, (1) पालकोट (2) रातू (3) मसमानो ठाकुर गाँव (4) बिड़ला
ब्रदर्स की चौरासी गाँव की जमींदारी (5) कैरोगढ़ वगैरह। मानभूम में (1)
पंचकोट (2) बराह बाजार (3) ईचागढ़ (4) पाटकुम (5) बेगम कुदार (6) झालदा (7)
मऊवाजर
(5) किसानों की जमीनें और उनकी तकलीफें हमें आगे बढ़ने के पहले यहाँ के किसानों की जमीनें कितनी तरह की हैं यह बात भी जान लेना जरूरी है। झारखंड के किसानों की यह खास बात है। यों तो बिहार के किसानों की जमीनें कई तरह की होती हैं और वे झारखंड में भी पाई जाती हैं। मगर उनके अलावा कुछ खास ढंग की भी काश्तकारी जमीनें हैं और यही हैं यहाँ के किसानों के प्राण स्वरूप। बेशक जमींदारों की जिरात जमीनों के बारे में भी बिहार की अपेक्षा यहाँ कुछ विशेषता है। इसलिए उसे भी जान लेना जरूरी है। मगर यह बात पीछे कही जाएगी। अभी तो काश्तकारी जमीनों की खास बातों पर ही पहले विचार कर लेना है। बिहार तथा छोटानागपुर के काश्तकारी कानूनों की चौथी धारा में किसानों (tenants) की कई किस्में बताई गई हैं। दोनों कानूनों की चौथी ही धारा में यह बात लिखी है। कुछ किस्में तो दोनों में एक ही हैं। टेन्योर होल्डर या अन्डर टेन्योर होल्डर दोनों ही में आते हैं। टेन्योर होल्डर कहते हैं जमींदार के ठेकेदार को जो आमतौर से लगान की वसूली के लिए जमीन पर किसानों को आबाद करता है। साधारणत: वह खेती नहीं करता। किन्तु लगान किसानों से लेके जमींदार का हिस्से देता है और बाकी खुद लेता है। वह गैर-आबाद जमीन को भी वहाँ किसान बसा के आबाद करवाने का ठेका लेता है। उस ठेकेदार से जो फिर वैसा ही ठेका ले वही मातहत ठेकेदार या अण्डर टेन्योर होल्डर कहा जाता है। मगर जो आदमी किसी से भी जमीन लेता है आमतौर से सिर्फ खेती करने के लिए वही रैयत कहा जाता है। जो उसके मातहत होगा वह अण्डर रैयत या शिकमी कहा जाता है। इस तरह टेन्योर होल्डर और रैयत में अन्तर है। मगर टेनेन्ट (किसान) तो सभी हैं। इस तरह दोनों कानूनों में ये चार तरह के किसान बताए गए हैं। इसी तरह दोनों ही में कायमी (occupancy) और गैर-कायमी (non-occupancy) किसान भी कहे गए हैं। कायमी किसान की जमीन अपनी मानी जाती है और उसे बिहार में अपनी जमीन पर पेड़, बाँस वगैरह लगाने, ईंट, खपड़ा बनाने और कुऑं, तालाब खोदने का हक प्राप्त है। उस पर वह अपने घर-गिरस्ती के लिए पक्के मकान भी बनवा सकता है। इसी प्रकार बिना काश्तकारी कानून की शर्त तोड़े या बाकी लगान की डिक्री में नीलाम कराए वह जमीन से बेदखल भी नहीं किया जा सकता है। मगर गैर-कायमी किसान को ये कोई भी हक प्राप्त नहीं है। उसका लगान भी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। मगर कायमी का लगान बढ़ाना कठिन है दिक्कत से होता है। यह ठीक है कि झारखंड के कायमी किसान को मकान वगैरह बनाने का हक नहीं प्राप्त है और यह भारी अन्याय है। वह बाग भी लगा नहीं सकता और न ईंट, खपड़े बना सकता है। फिर भी ये दोनों ही किस्म के किसान भी दोनों जगह हैं। इसके बाद फर्क चलता है। बिहार में पूर्वोक्त छह तरह के किसानों के अलावे एक सातवें प्रकार का किसान है जिसे 'फिक्स्ड रेट' (Fixed rate) या गुजश्तेदार किसान कहते हैं। उसका लगान इस्तमरारी होता है, जो न कभी बढ़ता है और न घटता है। मगर झारखंड के छोटानागपुर के पाँच जिलों में इस्तमरारी किसान की जगह कई और तरह के किसान पाए जाते हैं। वे तीन तरह के हैं (1) भुंइहर या भुंइहरी जमीन वाले (2) खुंटकट्टीदार या खुटकट्टी जमीन वाले, और (3) मुंडारी खुटकट्टीदार या मुंडारी खुटकट्टी जमीन वाले। इन तीनों का लगान आमतौर से घटता-बढ़ता नहीं है। मगर इनमें कुछ-कुछ खास बातें हैं। इसीलिए ये तीनों ही जुदा जुदा हैं। इसीलिए इनकी ये इस्तमरारी जमीनें भी भुंइहरी, खुटकट्टी और मुंडारी खुटकट्टी के नाम से क्रमश: विख्यात हैं। इस्तमरारी जमीनों में और खुटकट्टी में जो थोड़ा अन्तर है वह आगे मालूम हो जाएगा। झारखंड में एक तरह के और भी किसान होते हैं जो गाँव के मुखिया या जेठ रैयत की किस्म के होते हैं और जिन्हें प्रधान, मांझी और मानकी कहते हैं। कहीं-कहीं ठेकेदार और इजारदार के नाम से भी वे लोग पुकारे जाते हैं। प्रधान तो संथाल परगना, हजारीबाग, राँची में और मांझी हजारीबाग, मानभूम में तथा मानकी मानभूम और सिंहभूम में आमतौर से पाए जाते हैं। यों तो इधार-उधार भी मिल सकते हैं। कहते हैं कि जंगलों में पहले पहल जो किसान आए उनने जगह-जगह खेती वगैरह के लिए जमीनें चुन लीं, ठीक कर लीं और आबाद कर लीं। वही भुंइहर कहाए। यह झारखंड का खास शब्द है। और जगह यह शब्द बोला नहीं जाता। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पहले मुंडा लोग आए और उनके पीछे आए उराँव लोग। इसलिए मुंडा लोगों की पहले ठीक की हुई जमीनें जब उराँव लोगों ने हथिया लीं तो वे बेचारे दूसरी फिक्र में लगे और उनने अपने लिए पीछे जंगल काट के जो जमीनें तैयार कीं वह मुंडारी खुटकट्टी के नाम से विख्यात हुई और उनकी पहली जमीनें भुइंहरी कही गई। चाहे जो भी बात होµया तो यहाँ मुंडा लोगों के साथ ही साथ रहने वाले उरांव लोगों ने जो जमीनें हथियाई वही भुंइहरी हुईं और मुंडावाली मुंडारी खुटकट्टी या मुंडा लोगों से ही छिनी जमीनें भुंइहरी हुईं और उनने पीछे अपने लिए मुंडारी खुटकट्टी तैयार की हर हालत में ये दो तरह की जमीनें पहले बनी थीं। यह ठीक है कि भुंइहरी जमीनें आमतौर से उराँव लोगों के पास ही हैं। एक तीसरी जमीन भी है जिसे खुटकट्टी कहते हैं। वह मुंडारी खुटकट्टी से जुदी है। यहाँ के काश्तकारी कानून के अनुसार जिस किसी गाँव के बसाने वालों ने खूंटी या जंगल काट के जमीनें शुरू में आबाद कीं वही तो खुटकुट्टी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। मगर चाहे गाँव बसाने वाले रहे हों या न रहे हों, फिर भी मुंडा लोगों ने जंगलों को काट के जिन्हें बसाया वही मुंडारी खुटकट्टी कही गई। इस तरह खुटकट्टी जमीनें भी आमतौर से सिर्फ उराँव लोगों के ही हाथ में हैं। यहाँ भुंइहरी जमीन को भुंइहरी पत्थरगड़ी खुटकट्टी को खुटकट्टी पत्थरगड़ी तथा मुंडारी को भी मुंडारी पत्थरगड़ी सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जब पहले-पहले 1869 में या उसके आसपास यहाँ सर्वे हुआ तो इन जमीनों की चौहद्दी में पत्थर गाड़ के इन्हें जुदा-जुदा कर दिया गया। नहीं तो पीछे चल के झमेला और गड़बड़ी हो सकती थी। पहले जमाने में किसानों की जमीनें और भी दो प्रकार की थीं, जो मालूम होता है, पीछे छिन गईं। ये थीं मझिहस और बेठखेता। मझिहस का अर्थ है माझी का अंश, भाग या हिस्सा और माझी कहते हैं मुखिया को। इस तरह यह नाम बताता है कि जैसे आज प्रधान, मानकी या माझी वगैरह की खास जमीनें हैं तैसे बहुत पहले भी थीं। मगर जमींदारों ने पीछे छीन के उन्हें अपनी जिरात जमीन बना लीं। इसी तरह बेठखेता का अर्थ है बेगार के लिए दिया गया खेत। बेठ कहते हैं, बेगार को। मालूम होता है, पहले जिन लोगों से खासतौर से जमींदार लोग बेगार करवाते थे, जैसा कि संथाल परगना के दामिन इलाके में अभी तक सड़क वगैरह बनाने में आमतौर से सभी ग्रामवासियों से बेगार कराई जाती है, उन्हें कुछ जमीनें इसलिए देते थे। दामिन में रोडसेस के बदले यह बेगार करवाई जाती है जिसे जाँच कमिटी ने बन्द करने को कहा है। वही जमीनें बेठखेता कही जाती हैं। मगर अब ये दोनों हीमझिहस और बेठखेता जमींदार की खास या जिरात जमीन में गिनी जाती हैं। यह बात छोटानागपुर के काश्तकारी कानून की 118(ब) धारा में लिखी है। उसी कानून की 124वीं धारा में यह भी लिखा है कि जिस मौजे में बेठखेता या मझिहस जमीन 1869 के सर्वे में दर्ज है वहाँ उसके अलावे दूसरी जमीन जमींदार की खास, जिरात या कामत मानी नहीं जा सकती है। फलत: मझिहस और बेठखेता का ताल्लुक तो अब किसानों से रहा नहीं। किसानों की ओैर भी जमीनें हैं और वे हैं सबसे महत्वपूर्ण। मगर उनका विचार करने के पहले इन पूर्वोक्त तीन खास तरह की जमीनों की कुछ जरूरी खूबियों को भी जान लेना चाहिए। सबसे पहले भुंइहरी को लीजिए। यह ठीक है कि ये जमीनें पहले बनी थीं। अब तो वे घटती-बढ़ती हैं नहीं। ज्यों की त्यों रहती हैं। इसीलिए भुंइहरी भी एक निश्चित परिमाण में ही है। उसका लगान भी बहुत कम होता है। हमें तो यह भी कहा गया है कि प्राय: चार आने बीघे से ज्यादा नहीं होता। लेकिन इस जमीन की जो सबसे बड़ी खूबी है वह यह है कि एक तो वह किसी भी हालत में किसी डिग्री में नीलाम नहीं हो सकती। दूसरे उस जमीन वाले किसान को किसी भी डिग्री में गिरफ्तार करके जेल में रखा नहीं जा सकता। तीसरे यदि वह भुंइहरी जमीन समूची या उसका एक भाग किसी को ठेके में दे दे तो ठेकेदार को उसमें कायमी (occupancy) हक हासिल हो नहीं सकता। चौथे जिस प्रकार पहली गिनाई हुई दोनों सूचियों वाली यहाँ की जातियों को यह हक नहीं है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के हाथ में 15 साल से ज्यादा के लिए, सो भी सिवाय भोगबन्धाक या भुगुतबन्धा (usufructary mortgage) के और किसी भी ढंग से, जमीन दे सकें, और न दूसरों के ही हाथ। इसी तरह सात साल से ज्यादा के लिए, या पाँच साल से ज्यादा के लिए किसी भी हालत में ठेके पर किसी को नहीं दे सकते। ठीक यही हालत भुंइहरी जमीन की भी है। पाँचवीं बात यह है कि जैसे पूर्वोक्त आदिवासी या पिछड़ी जाति वाले अपनी जमीन अपनी ही बिरादरी (दल) वालों के हाथ उसी थाने के अन्दर ही अदला-बदली कर सकते या बेच सकते हैं, या डिप्टी कमिश्नर की राय से अपने सगे सम्बन्धी को दे सकते हैं, ठीक वही बात भुंइहरी जमीन वाले किसानों की उन जमीनों पर लागू है जो भुंइहरी वाले मौजे में भुंइहरी के अलावे भी होती हैं। छठीं बात यह है कि भुंइहरी जमीन के खिलाफ न तो कोई डिग्री ही हो सकती है और न उसमें वह नीलाम ही हो सकती है। सातवीं बात यह है कि यदि भुंइहरी जमीन के लगान के बाकी होने पर उसकी डिग्री हो तो सिर्फ उस जमीन की पैदावार सेही वह सधााई जाएगी, या उस किसान की किसी और भी चल सम्पत्तिा से। छोटानागपुर के काश्तकारी कानून की 47, 48, 48(अ) तथा 184 (अ) धाराओं में यह बातें लिखीहैं। खुटकुट्टी जमीन की खास बातें ये हैं कि एक बार उस जमीन का सर्वे हो जाने पर जितनी जमीन खुटकुट्टी लिखी जा चुकी है, उससे अधिक वह कभी हो नहीं सकती। वह घटती-बढ़ती नहीं है। यह पहली बात है। दूसरे यदि खुटकुट्टी जमीन कायम होने के ही समय लगान बढ़ाने की कोई शर्त तय न पाई हो तो जितनी खुटकुट्टी जमीनें 1908 से पहले के बीस साल के भीतर न बनके उसके पहले बनी थीं उनका लगान कभी बढ़ नहीं सकता। तीसरे, अगर ऐसा न होने पर उस जमीन का लगान बढ़ाया भी जाए क्योंकि 1908 के पूर्व के बीस साल के भीतर ही वैसी जमीन कायम होने पर लगान बढ़ सकता है तो हर हालत में उस जमीन का कुल लगान उस कायमी जमीन के लगान के आधे से ज्यादा हर्गिज नहीं हो सकता है जो उसी मौजे में उसी ढंग की हो और उसे उसी तरह की सभी सहूलियतें प्राप्त हों। उसी कानून की 37 और 134 धाराओं में यह बात लिखी है। आमतौर से जो बन्धान यहाँ के किसानों की जमीनों की खरीद-बिक्री पर है वह तो खुदकट्टी के भी लिए ही। इसी प्रकार मुंडारी खुटकट्टी की भी कुछ विशेषताएँ हैं। पहली यह है कि जो जमीन एक बार सर्वे में मुंडारी खुटकट्टी लिखी जा चुकी तो उसके अलावे और जमीन उसमें आ नहीं सकती। दूसरी यह कि उस जमीन का इजारा भुगुतबन्धा के सिवाय और तरह का हो नहीं सकता। सो भी किसी भी तरह सात साल से ज्यादा के लिए हर्गिज नहीं। तीसरे उस जमीन का ठेका किसी को दिया जा सकता नहीं, सिवा मुंडा रैयत को खेती के लिए गैर आबाद जमीन के ठेके के, या वैसे ही रैयत को गैर-आबाद जमीन के मुकर्ररी ठेके के सिवा, जो इसलिए दिया जाए कि उसमें जितनी हो सके खेती के लिए आबाद करे। चौथे वह जमीन किसी डिग्री में बिक सकती नहीं। पाँचवें बिना डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा के उस जमीन का लगान बढ़ाया जा सकता नहीं। उसमें भी यह बात सिद्ध करना होगा कि जब लगान बढ़ाने की दरखास्त पड़ी उससे पूर्व बीस साल के अन्दर ही वह जमीन मुंडारी खुटकट्टी बनी है। और अगर लगान बढ़ा भी तो ठीक वैसे ही बढ़ेगा जैसा कि खुटकट्टी के बारे में कहा गया है यानी वैसी ही जमीन के आधो से ज्यादा कुल मिलाके बढ़ा हुआ लगान नहीं हो सकता। छठे, उस जमीन का लगान सिर्फ र्सटीफिकेट या जब्ती-कुर्की के द्वारा वसूल होता है। मगर यह बात वहीं होती है जहाँ उस जमीन का सर्वे हो चुका हो। लेकिन सर्वे न होने पर बकाए की नालिश होती है। फिर भी उसकी डिग्री की वसूली या तो उसकी चल सम्पत्ति से होती है, या यदि उसे किसी और से लगान या कर्ज वसूल होने को हो तो उसे ही जब्त करके। अगर यह कोई भी न हो सके तो डिप्टी कमिश्नर उस जमीन को जब्त करके लगान वगैरह की वसूली का प्रबन्ध करता है। वसूली के बाद वह जमीन फिर वापस दे दी जाती है। यह बातें उस कानून की 240, 243, 246, 248 और 256 आदि धाराओं में लिखी हैं। इस प्रकार मुख्य-मुख्य बातें इन तीनों जमीनों के सम्बन्ध की लिखी गई हैं। इनके अलावे और भी बातें हैं। मगर उन्हें जानने के लिए समूचा टेनेन्सी कानून ही पढ़ना उचित है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात झारखंडी किसानों की जमीन के बारे में है और जिस पर ही उनके आराम का दारमदार है उसका लिखा जाना जरूरी है। बात यह है कि इस पहाड़ी इलाके की यह हालत है कि जिस जमीन में खेती होती रहती है वह कुछी दिनों के बाद अकसर बेकार हो जाती है। या तो उसकी उत्पादन शक्ति ही नष्ट हो जाती है, या जंगली जानवरों का उत्पात बढ़ जाने से उसे छोड़ना ही पड़ता है, या आसपास में जो झरना, नदी आदि सिंचाई का सामान था वही खत्म हो जाता है, या पहाड़ी पानी की कभी-कभी बाढ़ आ जाने से वह जमीन बालू कंकड़ के नीचे दब जाती है। इसी प्रकार के अनेक कारणों से किसानों को जमीनें छोड़नी ही पड़ती हैं। यदि जमींदार या उसके अमलों का जुल्म बढ़ गया या जंगल से लकड़ी आदि मिलने का कष्ट हुआ तब भी छोड़ना ही पड़ता है और वे दूसरी जगह जाके नई जमीन आबाद करते हैं। यों भी जमीन की कमी हो जाने पर या उपज की कमी होने पर यदि नई जमीन आबाद न की जाए तो गुजर कैसे हो? जंगल में फिजूल की पैदावार जमीनें तो पड़ी रहती हैं नहीं। हमेशा नई जमीनें ही खोद-खाद और कोड़-काड़ के आबाद की जाती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसान की जमीन के तख्ते (holding) के अन्दर कुछ जमीन धानखर, धानखेत या धानी होती हैं, जिसे दोन भी कहते हैं और कुछ ऊँची, बारी या टांड़ होती है। फलत: मौका लगने पर ऊँची या टांड़ को ही खोदके और चारों ओर आड़ और बाँधा लगाके दोन या धानखेत तैयार करते हैं। टांड़ में तो चाहे कुछ रबी या मूँग वगैरह पैदा होती रहती है, या कुछ भी पैदा नहीं होता। हर हालत में उसे दोन बना लेते हैं। जो जमीन पहले खेती में थी, मगर पीछे गैर आबाद हो गई, उसे भी फिर से आड़-वाड़ देके दोन बनाते हैं। आमतौर से ऐसी जमीन धान के ही लिए बनाई जाती है। इस तरह जो जमीन तैयार की जाती है उसे कोड़कर, अरियट, बाहुबला और जलसासन कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। कोड़ कर ही तो वह तैयार की जाती है। बिना कोड़े-खोदे तो बन सकती नहीं। इसीलिए कोड़कर कही जाती है। उसकी चारों ओर आड़ या बाँधा देके पानी रोकने के कारण उसे अरियट कहते हैं। अपने बाहु के बल से ही वह तैयार की जाती है। इसीलिए उसे बाहुबला भी कहते हैं। जल के भीतर, जल के कब्जे में रहती है। पानी का उस पर बराबर शासन रहता है। धाान की जमीन ही तो ठहरी। इसीलिए उसका नाम जलशासन या जलसासन पड़ा होगा। उसे खंडवत भी कहते हैं। अकसर धान के खेतों में पानी जमा करते हैं और मौके से आड़ काट के बहा भी देते हैं। फिर भर भी लेते हैं। धान की खेती में ऐसा करना पड़ता है। बाँधा या आड़ को पानी बहाने के लिए जहाँ काट देते हैं उसे खांड़ कहते हैं। धानी जमीन इसीलिए खंडवत भी कही जाने लगी होगी। 1.12.41A ऐसी जमीन को पलामू और राँची जिले में उटकर जमीन भी कहते हैं। आमतौर से कोड़कर और उटकर में कोई खास अन्तर नहीं है। लेकिन व्यवहार में साधारणतया यही माना जाता है कि जो जमीन दोन के साथ मिली होती है, या जो किसान के तख्ते के भीतर ही टांड़ जमीन होती है जब उसे कोड़ करके दोन बनाते हैं तो उसे कोड़कर नाम दिया जाता है। मगर जब उसके तख्ते से बाहर या दोन के पास न हो, किन्तु जमींदार की खास गैर-मजरुआ जमीन को खोद-कोड़ के आबाद करें और खेती के लायक बनाएँ तो उसे उटकर कहते हैं। इसीलिए उटकर का ज्यादा प्रचार पलामू जिले में ही है। उटकर में ज्यादातर गोंदली, सावां, मडुवा, कुर्थी, मकई आदि फसलें ही होती हैं। पलामू की तो अधिाकांश जमीन ऐसी ही है। यदि कहीं दोन के पास मौके से जमीन मिल गई तब तो उसे कोड़कर बनाएँगे ही। मगर ऐसा मौका मिलता ही कहाँ है। इसी प्रकार संथाल परगना में एक खास ढंग की जमीन खेती के लिए तैयार की जाती है। इसे दामिन इलाके के पहड़िया लोग तैयार करते हैं। पहड़िया लोग वहाँ के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। संथाल लोग तो संथाल परगना में, कहा जाता है, 1810 में ही पहले पहल पहुँचे। पहड़िया लोग इतने लड़ाकू माने जाते थे कि किसी को घुसने नहीं देते थे। जो ऐसी कोशिश करता था उसे बड़ी बेरहमी से मारते-काटते और भगा देते थे। वह निहायत ही भोली कौम है। उन्हें खेतीबारी का कोई भी दूसरा तरीका नहीं मालूम है। वह हल-बैलों वाली खेती जानते ही नहीं और न अब तक जीविका के लिए कोई दूसरा प्रचलित या सभ्य रास्ता उनने सीख पाया है। इसके लिए सरकार ने कोई खास उपाय किया भी नहीं है। कहा जाता है कि सबसे पहले वारेन हे¯स्टग्स की नजर इन पहड़ियों की ओर गई और उसे उन्हें सभ्य करने की सूझी। कैप्टेन ब्राउन की मातहती में उसने एक फौजी टुकड़ी, वहाँ पहले पहल भेजी। फिर कुछ दिन बाद मिस्टर जेम्स और क्लीवलैंड नामक दो अंग्रेज भेजे गए कि उनकी हालत जानी जाए। क्योंकि फौज से उनका सर होना या सभ्य बनाया जाना कुछ कठिन जान पड़ा। क्लीवलैंड ने, कहा जाता है, तेरह सौ सरदारों को चुन के उनके भीतर काम करने और उन्हें सभ्य बनाने को भेजा जिन्हें मासिक दस रुपए दिए जाते थे। आज भी ये सीरदार या सरदार उन आदिवासियों के इलाके में पाए जाते हैं। क्लीवलैंड ने उनके सुधारने के कुछ रास्ते और भी सुझाए। मगर उन पर सरकार ने अमल किया ही नहीं। पहड़िया लोगों की हालत यह है कि जंगलों में पहाड़ों पर ही ज्यादातर रहते हैं। इसीलिए पहड़िया बोले भी जाते हैं। जंगली फलों, मूलों और पत्ता के सिवाय वे एक तरह की खेती पुराने जमाने से करते आते हैं। यही दशा सभी मुल्कों में पहले, ऐतिहासिक युग के पूर्व, पाई जाती थी जब हल वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था। खेती के बाद जब कुछी दिनों में जमीनें उपजाऊ नहीं रह जाती थीं तो नए स्थान में जंगल वगैरह काट के नए खेत बनाए जाते थे। उनके पुराने पड़ जाने पर फिर दूसरी जमीन तैयार की जाती थी। जमीन में नोकीली लकड़ी से और पीछे औजार बनने पर उसी से छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे गढ़े, छिद्र या कुंड बना के उन्हीं में बीज डालते थे। आज भी दियारे की जमीनों या बालूवालियों पर खरबूज, तरबूज, ककड़ी, करेले आदि खेती ऐसी ही ढंग से की जाती है। वही बीज मिट्टी के नीचे पड़े-पड़े उगते और फलते-फूलते हैं। पहड़िया लोग भी अब तक यही करते चले आ रहे हैं। उसी ढंग के छिद्र, सूराख या कुंड बना के उसमें मकई, ज्वार, अरहर और घघरा आदि अन्नों के बीज डाल देते हैं। जमीन के उन छिद्रों को संस्कृत के पुराने ग्रंथों में कुंड भी कहते हैं। उनमें खेती करने के कारण ही उसे कुंडचास या कुरांवचास कहने लगे। चास तो बंगला में खेती को कहते ही हैं और चासी कहते हैं किसान को। 'कुंड' का ही कुंडवा या कुडांव होके कुरांव हो गया और कुरांवचास कहने लग गए। संथाल परगनाकी जाँच कमिटी की रिपोर्ट में भी उसे कुरवा या कुंडवा (Kurwa) लिखा है। उसे ही झूमचास भी कहते हैं। बंगाल के जंगली इलाकों में झूम जमीन या झूमलैंड (Jhumland) के बारे में हमने पढ़ा है। जंगलों और झाड़ियों को काट या जला के साफ करते हैं। असल में जलाते ही हैं ज्यादातर। बिना जलाए झाड़ियों का साफ होना कठिन होता है। जलाने से जो जमीन पर राख पैदा होती है उससे खाद का काम हो जाता है। इसी तरह की तैयार जमीन को झूमचास या झूमलैंड कहते हैं। पहड़िया लोग भी पहाड़ों पर और उनकी ढाबू जमीनों पर इसी तरह जमीनें तैयार करके खेती करते आ रहे हैं। अब इधार पाँच-सात साल से उसमें बाधा दी जाने लगी है। बात असल यह है कि आज से प्राय: चालीस साल पहले उन सभी जंगलों को संरक्षित घोषित किया गया था। मगर संरक्षित (reserved) होने पर भी जाने किस खयाल से या डर से सरकार ने पहड़िया लोगों को बेमुरव्वती और बेरहमी से शुरू कर दिया है। जंगलों को रिजर्व कर लेना तो सरकार छेड़ा नहीं। अब इधार कुछी साल से उस पर अमल होने लगा है। जमींदार या सरकार ने उन गरीबों के इस सनातन अधिकार पर प्रहार करना बड़ी के हाथ की बात है। उसमें कोई फौजी लड़ाई या लाठी चलाने का सवाल तो है नहीं। मगर आखिर उन गरीब किसानों की जीवन यात्रा भी तो होना जरूरी है। जंगल रिजर्व (संरक्षित) किए जाते हैं लोगों की ही भलाई के नाम पर। मगर लोग ही मर जाए तो भलाई कैसी? तब जंगल से फायदा किसका होगा? क्या उसकी लकड़ी से उन अन्न बिना मरे हुए पहड़िया लोगों का शव दहन होगा? यह तो बंगाल के हिन्दुओं वाला 'हरिबोल' वाला ही किस्सा हुआ कि मरणासन्न मनुष्य को पहले ही हरि बोलने को विवश करते थे और उसकी जबान से ज्योंही 'हरि' निकला कि उसे गंगा या नदी में डाल दिया! समझते थे कि उसका उपकार हो गया और बैकुण्ठ चला गया! भूखों मार के रिजर्व फारेस्ट खड़ा करना तो कुछ अजीब चीज है। वे जिन्दा कैसे रहेंगे? इस तरह बलात् सभ्य बनना तो अजीब बात है! और जब उनके बच्चों में एक को भी सरकार ने अब तक पढ़ाया तक नहीं, तो फिर वे सभ्य कैसे बनाए जाएँगे? जंगलों के काटने से उन्हें रोकना घोर अन्याय और बेदर्दी है। यह तो बेचारे मूक पहड़िया लोगों की बात हुई जिनमें एक भी पढ़ा-लिखा है नहीं। मगर मुंडा, उराँव, संथाल आदि तो पढ़ने-लिखने लगे हैं। उन्हें सभ्य बनाया जा भी रहा है। कम-से-कम मिशन वाले तो यह काम युगों से कर रहे हैं। मगर उनकी कोड़कर और उटकर जमीनों की भी कम फजीती नहीं है। यह हक उनसे प्राय: छीना जा चुका और बचा-बचाया कानूनी दाँवपेंच के जरिए बड़ी निर्दयता से छीना जा रहा है। कोड़कर वगैरह का जो वर्णन पहले किया गया है वह यहाँ के काश्तकारी कानून की 3 (13) धारा में लिखा गया है। लेकिन उसकी 64, 65, 66, 67 और 67 (अ) धाराओं में जो विशेष बातें और शर्त लिखी गई हैं उनमें एक प्रकार से घुमा-फिरा के किसानों के कोड़कर और उटकर के हकों को, जो सनातन काल से चले आ रहे थे और जमींदारों तथा जमींदारी के जन्म से पहले से ही जिन्हें उनने प्राप्त किया था, छीन लिया है। कम से कम छीनने की कोशिश तो भरपूर की है और उसमें सफलता भी मिली है। कानूनी दाँवपेंच ही तो ठहरा। असल में कोड़कर या उटकर के बारे में जमींदार की मंजूरी की जो शर्त 64वीं धारा में लगा दी है उसी ने तो गजब कर दिया है। यों कहने को तो उसमें कहा गया है कि (1) जो ऊँची या टांड़ जमीन किसान की कायमी जमीन की रैयती जमीन में शामिल हो, या (2) जहाँ जिस गाँव में पुराने रिवाज के अनुसार जमींदार की मंजूरी जरूरी नहीं हो उन जमीनों को कोड़कर बनाने में किसान स्वतंत्र हैं और जमींदार की आज्ञा की उन्हें जरूरत नहीं। यह भी कहा गया है जिस मौजे में बेठखेता और मझिहस के सिवाय दूसरी जमीन 1867 वाले सर्वे के कागज में दर्ज है यानी भुंइहरी जमीन है वहाँ भुंइहरी वालों किसानों को, तथा जहाँ मुंडारी खुटकट्टी जमीन लिखी गई हो वहाँ यदि मुंडा लोग जमीन जोतते हों तो उन्हें भी, जमींदार से बिना पूछे ही कोड़कर बनाने की स्वतंत्रता है। (3) उस धारा में तीसरी बात यह भी लिखी गई है कि जहाँ जमींदार का हुक्म जरूरी भी हो वहाँ भी यदि किसान ने उटकर या कोड़कर बनाना शुरू कर दिया और उसके दो साल के भीतर उस जमीन से उसे बेदखल करने के लिए कलक्टर (डिप्टी कमिश्नर क्योंकि झारखंड में कलक्टर को ही डिप्टी कमिश्नर कहते हैं) के पास जमींदार ने दरखास्त न दी तो माना जाएगा कि किसान को जमींदार से हुक्म मिल चुका था। फलत: वह पीछे उस जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो किसी मौजे का रहने वाला (देही) किसान उसी मौजे में कोड़कर बनाए तो बिना डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा के वह उस जमीन से बेदखल हो सकता नहीं और डिप्टी कमिश्नर तो बेदखली की आज्ञा दे सकता नहीं। इसके बाद 65 और 66 धााराओं में लिखा गया है कि जब बेदखली की दरखास्त डिप्टी कमिश्नर के पास दी जाएगी तो वह जाँच करने के बाद यदि ठीक समझेगा तो बेदखली का हुक्म दे देगा। किसान से जमींदार को हर्जाना भी दिला सकता है। इस तरह वह न सिर्फ जमीन से ही हाथ धोएगा। बल्कि घर का आटा भी उसे गीला करना होगा। हाँ, यदि उसने बेदखली की आज्ञा न दी तब तो बात ही दूसरी है। मगर क्या यह मुमकिन है? यह भी लिखा है कि दूसरे की जोत जमीन, घर (बसौढ़ी) की जमीन या बाग-बगीचे की जमीन को कोड़कर बनाया जा सकता नहीं। भला यह कैसे होगा कि दूसरे के जोत पर कोई धावा बोल दे, या उसके बाग को काट के या मकान को गिरा के या जबर्दस्ती करके कोड़कर बना ले? मगर यह गोल-मोल बातें इसीलिए की गई हैं कि इन्हीं के बहाने पर किसान को कोड़कर से बेदखल किया जा सके। जमींदार को झूठी गवाही तो आसानी से मिल सकती है। यहाँ के किसान अदालत में लड़ना क्या जानें? अब जरा इन तीन धाराओं में लिखी शर्तों पर विचार तो करें। आखिरी (67) वाली का तो विचार कर भी चुके कि उसके शब्दावली बड़ी ही गोल-मोल और पेचीदा है जिससे किसान धोखे में पड़ सकता है। मगर शेष दो की भी र्शते कम खतरनाक नहीं हैं। असल में जमींदार से पूछने का सवाल ही गलत है। इसी में धोखा और चालबाजी है। यह कहना, कि जहाँ रस्म-रिवाज हो वहाँ पूछने की जरूरत तो ही नहीं, भी गलत और धोखे का है। कोड़कर तो बनता है तब से जब यहाँ जमींदार थे भी नहीं और जब मुंडा, उराँव वगैरह यहाँ पहले पहल आए थे जब से यहाँ आदमी बसे थे। फिर रिवाज की बात ही क्या है? वह तो समूचे झारखंड के लिए एक-सा है। जब जमींदार थे ही नहीं तो पूछने की बात ही कहाँ उठ सकती थी? फलत: सर्वत्र रिवाज ही था। ऐसी हालत में रिवाज की बात उठाना खामख्वाह जमींदार को लाठी और रुपए के बल से 'दाल-भात में मूसरचन्द' बनने का मौका देना है। वह तो सभी जगह कह बैठेगा कि रिवाज नहीं है और बिना जमींदार के पूछे कोड़कर बनता नहीं। हाँ, केवल भुंइहरी और खुटकुट्टी वाले गाँवों में ही भुंइहार और मुंडारी खुटकट्टीदार के लिए साफ कहा गया है कि जमींदार से पूछना जरूरी नहीं है। सो भी तभी जब मुंडारी के पास कोई दूसरी जमीन हो। न होने के उसे भी पूछना ही होगा। ऐसे गाँवों में भुइंहर और मुंडारी लोगों के बारे में जमींदार को ही सिद्ध करना होगा कि उससे हुक्म लेना जरूरी है। खूबी तो यह है कि यदि जमींदार से आज्ञा लेना जरूरी भी हो तो यह बात जमींदार को ही सर्वत्र सिद्ध करनी होगी, ऐसी शर्त भी नहीं दी गई है। क्योंकि इससे किसानों को आसानी और जमींदार को दिक्कत होती। यहाँ तो ऐसी बेहूदा शर्त है जिससे यह बात सिद्ध होती है कि सर्वत्र जमींदार से पूछना ही होगा, और अगर कहीं न पूछना हो तो यह चीज किसान को ही साबित करनी होगी। इससे सारा भार किसान पर आ गया और यही इन शर्तों का असली जहर है। यही बात जाँच-पड़ताल में भी है। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की जाँच के समय कचहरी की चालबाजियों और खर्चों में गरीब किसान क्या पार पा सकता है? उसे तो कानूनी पेचीदगी मालूम नहीं। इधर सारा मामला चौपट हो जाता है और वह न सिर्फ जमीन से हाथ धोता है उस जमीन से जिसे बाहुबला कहते हैं और जिसे बनाने में उसने अपने खून को पानी कर दिया किन्तु हर्जाना भी देने की नौबत आती है! हर्जाने की बात तो किसान को धमकाने के लिए है। ताकि इसी डर से पहले ही जमींदार का पाँव पूजे और उसकी मुट्ठी गर्म करे। जमींदार की रजामंदी का तो यही अर्थ ही है। वह तो हर्जाने की बात सुनते ही काँप उठेगा। नहीं तो यह बात रखी ही क्यों गई? जो जमीन बेकार थी, जिसे कुत्ता भी पूछता न था उसे ही किसान ने अपने परिवार का खून-पसीना बना के खेती के योग्य कर दी! उसके बेदखल होने पर जमींदार को क्या यही कम फायदा हुआ? अब तो इसी जमीन पर किसी से भी नजराना और लगान पा सकता है, जिसे पहले कोई पूछता न था। जो लोग कानूनी ज्ञान की बदहजमी मिटाते और नाहक वकालत करते फिरते हैं उन्हें पता नहीं कि 64वीं धारा में यह लिखने पर भी, कि कायमी किसान की रैयती जमीन के भीतर वाली टांड़ जमीन को उटकर या कोड़कर बनाने में जमींदार की मंजूरी का सवाल उठता ही नहीं, ज्यों ही किसान ने ऐसा किया कि उस कोड़कर पर अलग लगान लाद दिया जाता है। काश्तकार की रैयती जमीन को तो छोड़िए। ऐसी जमीन तो कई हो¯ल्डगों में हो सकती है। मगर जिस हो¯ल्डग का एक भाग दोन तथा दूसरा टांड़ है उसके उसी टांड़ को दोन बनाने पर भी जमींदार लोग जबर्दस्ती लगान बांध देते हैं और रैयत को देना ही पड़ता है। नहीं देने पर हजार ढंग से उसे तंग किया जाता है। आखिर 'जबर्दस्त की लाठी सर पर' का भी तो कुछ मतलब होता ही है और वह लाठी जितनी झारखंड में चलती है उतनी शायद ही कहीं। यहाँ के किसान निरे अनजान जो ठहरे। अतएव कोड़कर के बारे में लगाई गई सभी शर्त जब तक हटा न ली जाए किसानों की खैरियत नहीं। अब जरा उनके परेशान किए जाने की संक्षिप्त कहानी सुनिए। सबसे पहले तो जमींदार इसी बात पर जोर देता है कि कोड़कर बनाने के पहले ही उससे आज्ञा मानी जाए। और अगर किसान ऐसा करे तो मनमानी सलामी, मनचाहा नजराना उससे तलब किया जाता है इतना ज्यादा कि सुनके तबीयत घबरा जाए। जितना बाहरी लोग सोच भी नहीं सकते उतना नजराना जमींदार माँग बैठता है। यदि इस डर से किसान ने उससे पूछा नहीं, तो जमींदार के यमदूत ये अमले ढूँढ़-ढाँढ़ के पता लगा ही लेते हैं। उनका तो यही काम ही ठहरा। फिर तो पहले वे खुद सौदा करते हैं और कहते हैं कि हमारी पूजा ठीक-ठीक करो, नहीं तो न सिर्फ जमींदार को खबर देंगे, बल्कि तुम्हें यहीं दुरुस्त भी करेंगे। ऐसा प्राय: होता है कि कुछ या काफी घूस न पाने पर अमले मार-पीट बहुत करते और बाँधा-बूँधा कर या घसीट के जमींदार की कचहरी में किसान को ले जाते हैं। फिर तो वहाँ उसे सबकुछ भुगतना पड़ता है। हाँ, यदि अमलों की पूजा हो गई तो मारपीट से जान बचती है। मगर जमींदार तो काफी नजराना लेता ही है और लगान भी मनचाहे ढंग पर बाँध देता है। की-कराई मेहनत बेकार न जाए इसी खयाल से किसान जमींदार को जैसे हो खुश करता ही है। नहीं तो जमीन से ही हाथ धोना पड़ जाए। हाँ, यदि अमलों को खूब पैसे दिए तो कह-सुन के रिआयत करा देते हैं। मगर थोड़ी ही बहुत। यदि किसान ने शायद हिम्मत से काम लिया और कह दिया कि कानून के अनुसार जमींदार को सचमुच ही बोलने का हक नहीं है, तो उसके लिए बला समझिए। कानून-वानून क्या करेगा? यहाँ तो जमींदार की मर्जी ही कानून है। जबर्दस्ती लाठी के बल कोड़कर या उटकर से बेदखल कर दिया जाएगा। यदि वह डँटा, तो सैकड़ों ढंग के जालफरेब और मुकदमे में फँसा के तंग तबाह कर दिया जाता है। इसलिए हर हालत में बिना जमींदार की शरण गए और उसे खुश किए किसान को पनाह नहीं उसकी खैरियत नहीं। कानून यह भी कहता है, जैसा कि 67वीं धारा से स्पष्ट है कि कोड़कर या उटकर जमीन ज्यों ही तैयार हुई उस पर किसान का कायमी हक हो जाता है। आमतौर से बारह साल लगातार जोतने की जरूरत जो और जमीनों पर कायमी हक होने के लिए होती है वह कोड़कर के लिए नहीं है। साथ ही, सेटल रैयत होने की भी शर्त इसमें नहीं है और न 18वीं धारा के अनुसार, जिसमें कि भुंइहर और मुंडारी खुटकट्टीदार को भुंइहर, मुंडारी खुटकट्टी या जमींदार की जिरात के अलावे उस गाँव की बाकी जमीनों के जोतते ही सेटल रैयत का हक मिल जाता है, कोड़कर वाले किसान को भुंइहर वगैरह होने की ही जरूरत है। यह इस जमीन की खूबी है। मगर क्या भरसक जमींदार ऐसा होने देते हैं। रैयत कुछ जानता नहीं और उसकी नादानी से अनुचित लाभ उठाते हैं जमींदार और उसके पापी अमले! 67(अ) धारा में कोड़कर या उटकर के लगान का नियम है। वहाँ लिखा है कि उस जमीन में पहली फसल कट जाने के बाद चार साल तक यानी पूरे पाँच वर्ष तक फसल काटने के बाद ही कोड़कर जमीन पर लगान लग सकता है। उसके पहले हर्गिज नहीं। मगर जिस कानून से किसान को फायदा हो उसे कौन माने? जमींदार की बला उसे मानने जाए। वह क्यों उसकी परवाह करने लगा? वह तो जमीन तैयार होने के पहले से ही किसान का खून चूसने लगता है। तब उसी से पूरे पाँच वर्ष तक खामोशी की उम्मीद? उसी धारा में यह भी लिखा है कि पाँच साल के बाद जब जमींदार उस जमीन पर लगान लगाए तो, आमतौर से उस गाँव में जो धान की तीसरे दर्जे की (यानी सबसे खराब) जमीन हो उसके लगान से ज्यादा लगान उस कोड़कर पर लगा नहीं सकता। मगर अगर मौजे का रिवाज ऐसा हो कि कोड़कर का लगान उतना भी न हो के उसका आधा ही होता हो, तो जमींदार को भी ऐसा ही करना होगा। इसके बाद इसका सारा ब्योरा डिप्टी कमिश्नर के पास वह जमींदार बाकायदा भेजेगा और डिप्टी कमिश्नर जाँच-पड़ताल करके और किसान से भी भरसक पूछताछ करके उस लगान पर मुहर देगा। तभी वह लगान वसूल किया जाएगा। मगर यहाँ तो दूसरी ही गंगा बहती है। हमने तो जवाबदेह किसानों को रोते-चिल्लाते पाया है कि जमींदार मनमाना लगान वसूल करता है। डिप्टी कमिश्नर को कौन पूछे? कानून-फानून की धाराएँ कौन देखे? अब जरा उटकर की विशेष वार्ता सुनिए। कही चुके हैं कि कोड़कर ही का यह भी एक रूप है। मगर इसमें ज्यादातर ऊँची या बारी जमीन ही होती है जिसमें मूँग वगैरह बोते हैं। ज्यादातर पलामू में और कहीं-कहीं रांची में भी यह जमीन पाई जाती है। कुछ उटकर में तो हर साल खेती होती है। बाकियों में दो-तीन साल का बीच देकर ही। मगर जमींदार शुरू से ही मनमाना लगान लेते हैं और रसीद देते ही नहीं। अगर देते हैं तो तभी जब और कायमी जमीन के साथ उटकर का लगान पाते हैं। मगर पूरा-पूरा नहीं। फलत: उटकर की तो रसीद देते हैं और कायमी की नहीं देते। जिससे आगे चलके उसे नीलाम करवा लेते हैं। किसान को पहले क्या मालूम? वह रसीद पढ़ने थोड़े ही जाता है। लगान भी नगदी और भावली दोनों ही होती है। अच्छी जमीन की भावली और खराब की नगदी जमींदार तो गुरू-घंटाल होते ही हैं। खूबी तो यह कि ऐसी जमीनों पर लगे पलास या महुवा के पेड़ों का अलग बन्दोबस्त करते और लगान लेते हैं। महुवा खाते हैं और पलास पर लाह जो होती है। कभी-कभी अच्छी उटकर जमीनों से किसानों को इस्तीफा देने पर भी विवश किया जाता है। यह तो कही चुके हैं कि उटकर बनाने में शुरू में ही या बीच में भी सलामी माँगी जाती है। न देने पर मार-पीट के सिवाय जबर्दस्ती जुर्माना वसूल किया जाता है और झूठा केस चलाने की धमकी भी दी जाती है। कभी-कभी केस भी चल जाते हैं। लगान की दर तो गजब की होती है जिससे हार के किसान जमीन छोड़ के भाग जाते हैं। भावली में जमींदार के हिस्से का गल्ला कभी-कभी इतना ज्यादा ठहराया जाता है जितनी कि खेत की कुल पैदावार भी नहीं होती! सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी जमीनों को लेके यह होती है कि किसानों को कानून का पता तो रहता नहीं। एक बार हाल में ऐसा हुआ कि प्राय: पाँच सौ किसानों ने पलामू में डिप्टी कमिश्नर के पास लगान ठीक करने की दरखास्त दी थी। मगर सबकी सब रद्द कर दी गई। वे बेचारे मुँह ताकते रह गए।
(6)जंगल की तकलीफें यह ठीक है कि कुरांवचास, कोड़कर और उटकर से ताल्लुक रखने वाली तकलीफें किसानों को सबसे ज्यादा अखरती हैं और असह्य हैं। इनसे तो मौत को ही वे ज्यादा पसन्द करते हैं। इसीलिए इन पर सबसे ज्यादा उनका ध्यान जाता है। मगर इनके अलावा उनकी और भी तकलीफें हैं जो कम अखरती नहीं हैं। कोड़कर आदि जमीनों की तकलीफों के ही मुकाबले की दो तकलीफें उन पर और आ पड़ी हैं और इस तरह इन तीन विपदाओं की चट्टानें उन्हें पीस रही हैं। इन दो में एक तो है जंगल के फल, फूल, काठ, बाँस, घास, पत्तो, मूल, जल आदि की। इन्हें पहले भी चाहे और तकलीफें हजार रही हों। लेकिन उन जंगली पदार्थों की तो कोई कमी न थी। जब चाहे जितना लाते और इस्तेमाल करते रहे। कपड़ा तो इनके पास पूरा होता ही नहीं। ज्यादातर तो लँगोटी ही रखते हैं। शेष शरीर नंगा औरतों की भी सारी देह तो कपड़े से ढँकती नहीं। इतने कपड़े इन्हें मिलें भी कहाँ से? इसीलिए जाड़ों में आग जलाके और पुआल घास में घुसके गुजर करते थे। खेत की रखवाली के लिए काँटे और झाड़ियाँ काट लाते और किनारे-किनारे गाड़ के घेरा तैयार कर देते थे। घर के चारों ओर न घेरें तो जंगली जानवरों से कभी न बच सकें। उन्हीं घेरों पर सेम वगैरह की लताएँ भी फैलती और फूलती हैं। पानी खुद पीते, नहाते, पशुओं को पिलाते और खेत सींचने के काम में लाते थे। महुआ, गेंठी, केना वगैरह फल-फूल खाते थे। इधार पलास, कुसुम आदि पेड़ों पर लगी लाह बेच के पैसे कुछ कमा लेते थे। गाड़ी, हल, घर की छाजन के लिए काफी काठ और बाँस उन्हें मिलता था। पतो के पत्ताल बना के बाजारों में बेच लाते, बरसात में पत्तो के सुन्दर छाते बना के भीगने से बचते और लकड़ियाँ बेच के भी गुजर करते थे। मगर सब पर आफत आ गई! ये गरीब ताज्जुब में हैं कि यह क्या हो गया? वे समझी नहीं सकते कि यह हक क्यों छिन गया। सर्वे में खतियान बनी और गुरू-घंटाल जमींदारों और उनके अमलों ने घूस दे के जंगलों पर अपना खास कब्जा लिखवा लिया! ऐसे ही जंगलों में नमूने के लिए पारसनाथ पहाड़ का भी जंगल है। सबकुछ जमींदार का ही लिखा है। सर्वे की खतियान दिखा के उसकी तराई के माझियों (संथालों) को लकड़ी, बाँस, फल, फूल, पत्तो और झरने के पानी लेने तक से रोका जाता है! वे बेचारे खतियान क्या जानने गए? उन्हें क्या मालूम कि यह खतियान कौन सी बला है? वे तो सीधो और अपढ़ ठहरे। खतियान बनने के समय उन्हें पता भी न था कि क्या बन रहा या बिगड़ रहा है। उन्हें सपने में भी खयाल न था कि ये गौरवर्ण, अहिंसाव्रतधारी, जैनी मालदार दिल के ऐसे काले हैं कि उनके जंगली हक भी छीन लेंगे और उन्हें तथा उनके पशुओं को पानी तक पीने न देंगे। यदि ये जानते कि ये दोपाए खूँखार पशु भीतर के काले हैं और ऐसा करने आए हैं तो उसी समय निपट लेते। नतीजा चाहे जो होता। इस अत्याचार से उनके खून में आग लगी है। पीरटांड और डुमरी में जब मैं इनकी मीटिंग में गया तो इनमें इसी अत्याचार की चर्चा थी कि कैसे इसे खत्म करें। सुना है कि उसके बाद पुलिस के लाख मना करने पर भी इनने जंगल पर धावा बोल ही तो दिया। उस कांग्रेसी मंत्रियों का आसन डिग गया। मगर उनसे इतना भी न हो सका कि इनके ये हक साफ-साफ इन्हें दे डालें! यही तो उनकी जन-सेवा और किसान-प्रेम का नमूना है! रिजर्व जंगलों के करते भी यही आफत आती है। इसका जिक्र पहले किया जा चुका है। सर्वे के बाद भी समय-समय पर जंगल रिजर्व होते जाते हैं। इसीलिए पानी, फल, फूल वगैरह की तकलीफें इन किसानों को बढ़ती ही जाती हैं। उन्हें निश्चय ही नहीं कि कब कहाँ क्या बला आएगी और उनके ये अधिकार छिन जाएँगे। कहने के लिए तो बताया जाता है कि घर-गिरस्ती के काम के लिए सब चीजें जंगल से लेने का हक खतियान में है। मगर व्यवहार में क्या होता है। हमें इसी से काम है। न कि लिखे हुए से। हम तो ये किसान तो लिखना नहीं जानते। किन्तु करना जानते हैं और उस करना में गड़बड़ी है। खतियान में लकड़ी के नाम और लम्बाई, चौड़ाई, मौटाई वगैरह की ऐसी बाल की खाल खिंची होती है कि ये बेचारे पार नहीं सकते। पहले ये लोग इंजीनियरिंग पास करें और पास में स्केल, परकाल वगैरह रखें। तब शायद काम चले तो चले। मगर ये तो ठहरे पूरे 'काले अक्षर भैंस बराबर' और 'लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर'। तब कैसे काम चलेगा? और इतना ही तो नहीं है। अभी तो बड़ा घनचक्कर बाकी ही है। यदि ये किसान और गरीब लकड़ी वगैरह ले के चले ही जाए और अपना काम चलाई लें, तो जंगल विभाग के छोटे-बड़े नौकर क्या मक्खी मारेंगे? उनका मजा तो किरकिरा होई जाएगा। वे इन्हीं को सता के तो गुलछर्रे उड़ाते हैं। थोड़ी-थोड़ी तनख्वाह वाले रेंजर, फारेस्टर, पेट्रोल, अर्दली और जाने कौन-कौन से महारथी जंगलों में ताक लगाए खूँखार जानवरों की ही तरह शिकार की ताक में बैठे रहते हैं। यदि इनकी पूजा शुरू में ही, या बीच में ही सही, न कर दी जाए, तो हजार मीनमेख निकाल के गरीबों को तबाह कर छोड़ते हैं। मैंने यह तमाशा खुद देखा है। गावां थाना (हजारीबाग) के एक गाँव में, जो गावां से हजारीबाग आने के समय सकरी नदी पार करने के बाद पड़ता है और जिसका नाम मैं भूलता हूँ, मुझे किसानों ने जो-जो दर्दनाक दास्तानें सुनाईं उनसे मैं खून के ऑंसू रोया। ऐसी बातें जाने कितनी जगह हुईं। मेरा तो खून खौल उठा। मगर लाचार था। जंगल विभाग और उसके नियम-कायदे यहाँ के गरीबों को तिलतिल करके मारते हैं! दूसरों को क्या पता? जिनके सिर गुजरती है वही जानते हैं! मैं तो उनके दिलों में प्रवेश करने की भारी कोशिश करके ही थोड़ा समझ पाता हूँ। बाबू लोग असेम्बलियों और सेक्रेटेरियट की कुर्सयाँ तोड़ते रहें। वे हजार जन्म में भी इन दुखिया लोगों की वेदना आह शायद ही समझ पाएँ। इसके लिए तो दिल चाहिए। सो भी दूसरे ही ढंग का। 2.12.41A एक बात और भी है। दो तरह के जंगल होते हैं अलावे मामूली और उजड़े जंगलों के। एक तो सुरक्षित या प्रोटेक्टेड और दूसरे रक्षित या रिजर्व या यों कहिए कि जिन पर रोक लगी है। सुरक्षित (protected) जंगलों के भीतर तो कोई पाँव दे नहीं सकता और न एक तृण छू सकता है। हाँ, रक्षित या रिजर्व (reserved) जंगलों में से ही समय-समय पर घरेलू काम के लिए मामूली बल्ले वगैरह लिये जा सकते हैं जिनकी लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई वगैरह निश्चित रहती है। साथ ही यह भी तय रहता है कि किन-किन पेड़ों से ये लकड़ियाँ भी नहीं ली जा सकती हैं। यह तो एक तरह का जंगल-पुराण ही समझिये। पत्तो, घास वगैरह तो ले सकते ही नहीं। ये चीजें तो मामूली जंगलों से ही ली जा सकती हैं और रिजर्व से शायद ही बड़ी दिक्कत से। जंगल के हर गाँव की खतियान में लिखा रहता है कि कहाँ तक जंगल में जा सकते हैं। ऐसा फासला चौहद्दी के साथ लिखा रहता है। तिस पर भी तुर्रा यह है कि जमींदार लोग कर लेते हैं जिसे टंग कर या टांगी कर कहते हैं। पलामू पहुंवाडांड थाने के सिवाय सभी जगह यह टंग कर है। इसके लिए बड़ा तूफान हुआ। महुंवाडांड वाले बहुत ही बागी बने थे। तब भी उनका पिंड छूटा नहीं। झमेला चलता ही रहता है। हरेक घरवाले को साल में चार आना देना ही पड़ता है चाहे लकड़ी लें या न लें। मगर वे लोग कुछ लकड़ियाँ काट के बेच भी सकते हैं। दूसरे थाने वाले तो घर-गिरस्ती के ही लिए पा सकते हैं। बेचने के लिए हर्गिज नहीं। बेचने के लिए भी वही मामूली बल्ले, सो भी आदमी अपने सिर पर ही लाद के ला सकता है। राँची वगैरह में सभी जगह जमींदार का यह टंग कर या वन कर बड़ी सख्ती से वसूल होता है। इन जिलों में और मानभूम, हजारीबाग वगैरह में भी टंग कर, वन कर, पत कर, लह कर, चुल्ह कर आदि नामों से ये टैक्स लिये जाते हैं। काटने की टांगी के हिसाब से, जलाने की चूल्हे के हिसाब से या यों ही वसूल होता है। पत्ता लेने पर पत कर, लकड़ी के लिए वन कर। राँची जिले में तो पता चला कि पहले फी घर साल में सिर्फ एक आना देना होता था। सर्वे के समय चार आना हो गया। अब तो सवा रुपया वसूल होता है। इसके सिवाय रसीद देने में चपरासी और मुहखर चार आने लेते हैं। जंगल में जो चपरासी या बरकन्दाज रहते हैं वह भी कुछ न कुछ लेते ही हैं। नहीं तो तरह-तरह से परेशान करते हैं। और जगहों में भी व्यवहार में यह कर बढ़ गया है। चाहे कागज में कम ही क्यों न लिखा हो। किसान देना नहीं चाहते। इसीलिए झमेले होते रहते हैं। पलामू के रांका जमींदारी में पहले चुल कर के नाम से यह कर वसूलते थे जबर्दस्ती। मगर जब सर्वे के समय यही चार आना लिखवाने की कोशिश जमींदार ने बहुत ही छल-फरेब करके की। मगर सर्वे अफसर ने नहीं माना। महुवाडांड में तो जमींदारों ने धीरे से यह चार आना टंग कर सर्वे की खतियान में लिखवाई लिया। मगर बहुत दिनों तक चुप्पी साधो रहे और एक पैसा नहीं वसूला। किसानों को पहले शक हुआ था कि कुछ न कुछ टंग कर लगा है। वे बौखलाए भी थे, जैसा कि कह चुके हैं। मगर जब वसूली नहीं हुई तो उनने समझ लिया कि खत्म हो गया और निश्चिन्त रहे। जब वहाँ की कई जमींदारियाँ कोर्ट आफ वाड्र्स की मातहती में आ गई तब फिर वसूली जारी हुई और किसानों की ऑंखें खुलीं। हलचल भी उनमें काफी हुई। बवंडर शुरू भी हुआ। मगर फिर कुछ-कुछ ठंडे पड़े। आज भीतर ही भीतर असन्तोष की आग धाक्धाक कर रही है। 1939 के दिसम्बर में मैं जब वहाँ गया था तो यह बात साफ मालूम हुई। मगर यह चार या आठ आने का कोई नियम एक तरह का नहीं है। मैंने तो हजारीबाग में और दूसरी जगह किसानों के पास रसीदें देखी हैं जिनसे पता चलता है कि हर तरह की लकड़ियों के लिए, जो सिर्फ घर-गिरस्ती के ही काम आती हैं, जुदे-जुदे कर निध्यानर्रित हैं और बिना दिए बेचारों की गुजर नहीं है। यह भी होता है कि रिजर्व जंगलों में कुछ खास-खास जगहें होती हैं और वहीं से लकड़ी ले सकते हैं। जैसे मन्दिर का फाटक बन्द हो और खुले वैसे ही ये जगहें भी समय-समय पर ही खुलती और बन्द होती हैं। खुलते ही दौड़ मचती है और पैसे देके लकड़ी काटना जरूरी होता है। फिर बन्द होने पर कुछ न हो सकेगा। एक बार खुलके तीन-तीन साल के लिए ये बन्द हो जाते हैं। इसीलिए जल्दी-जल्दी ईंधन लकड़ी वगैरह लेना ही पड़ता है। नहीं तो तीन साल तक मरना ही पड़े। यह तो बर्फानी इलाकों और देशों की बात हुई कि अब सामान जमा कर लो, नहीं तो बर्फ के दिनों में मरना होगा। क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। कभी-कभी तो गाँवों से ये जगहें बहुत दूर होने के कारण किसानों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ता है। पलामू वगैरह में गाय-भैंसों आदि के रखने वालों से खरची के नाम नाजायज कर लिया जाता था, जो पीछे बड़ी दिक्कत से बन्द हुआ था। रांका वगैरह के जमींदार खासतौर से कई ऐसे कर वसूलते थे। मुझे उस नोटिस की बात बखूबी याद है जो मिस्टर गोडबोले ने, जो आज बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, और उस समय पलामू के डिप्टी कमिश्नर थे, उसी हैसियत से चारों ओर बँटवाई थी। उसमें जमींदारों को उनने धमकाया था कि खरची वगैरह नाजायज वसूलियाँ बन्द कर दो। नहीं तो सजा होगी। जहाँ-जहाँ खरची वगैरह लेते थे तहाँ-तहाँ मवेशियाँ बिना यह कर दिए जंगलों में जाने पाती न थीं। रिजर्व जंगलों में और प्रोटेक्टेड फारेस्ट में भी आज भी यही दशा है। वहाँ की घास सूख जाती है। मगर मजाल क्या कि कोई पशु पाँव भी दे दे। ऐसा होने पर या तो फौरन ही काजीहाउस (मवेशीखाना, अड़गड़ा, पौंड) में डाल दिए जाते हैं। नहीं तो जंगल के गार्ड (रक्षक) और चपरासी फारेस्टर कसके जुर्माने के नाम पैसे वसूल लेते हैं। जमींदारों की यह हालत है कि अपने जंगलों को आमतौर से ठेकेदारों को दे देते हैं। फिर तो किसान मजबूर होता है। जमींदार कहता है कि क्या करे, वह तो ठेके पर दे दिया है। किसान बेचारा ठेकेदार से सौदा करता और पैसे दे के लकड़ी वगैरह लेता है। यों सीधो पैसा माँगने और लेने में दिक्कतें होती हैं और गैर-कानूनी बात भी हो जाने का डर है। क्योंकि खतियान में जहाँ ऐसा न हो वहाँ पैसे कैसे लेंगे। यही कारण है कि चालाकी से काम लिया जाताहै। जहाँ किसानों को लकड़ी वगैरह लेने का हक भी है वहाँ भी जमींदार लोग तरह-तरह से उन पर दबाव डालते हैं कि बिना खबर दिए लकड़ी नहीं काट सकते और न जंगल में घुस सकते हो। बेचारे भोले-भाले किसान क्या करें? वे जब जमींदार के पास कहने जाते हैं तो बिना रुपया-पैसा लिये हुक्म मिलता ही नहीं। यदि नहीं जाएँ तो जंगल के चपरासी वगैरह पकड़ के तरह-तरह से सताते हैं। हमने जेल में ऐसे कैदी पाए हैं जो अपने हक के ही अनुसार जंगल से लकड़ी काटने गए थे, फिर भी रोके गए और न मानने पर मारपीट हो जाने से खून तक हो गया। वे बेचारे बेकार फँसाए गए। अदालत ने उनका हक तो कबूल कर लिया। इसीलिए उन्हें फाँसी की सजा न हो सकी। मगर आत्मरक्षा (self defence) की मर्यादा से आगे बढ़ जाने के कारण उन्हें जेल की सजा हो गई और कई साल भुगतने पड़े! ऐसा क्यों हुआ? इसमें शैतानियत तो जमींदार के आदमियों की ही ठहरी। न वे रोकते, न मार-पीट होती और न खून होता। फिर सीमा या मर्यादा लाँघने की बात ही कैसे उठती? जब कांग्रेसी मंत्रियों के जमाने में हजारीबाग के डुमरी और पीरटांड़ थानों के संथाल वगैरह किसानों ने पारसनाथ पहाड़ की तराई में जंगलों से जबर्दस्ती लकड़ी आदि काटना शुरू कर दिया था तो बड़ा तूफान मचा था। हथियारबन्द सिपाही वहाँ भेजे गए थे उन्हें रोकने, पकड़ने और सबक सिखाने के लिए। ऐसी सनसनी और हलचल थी कि कुछ कहिए मत। उसके पहले उन जगहों में किसानों की मीटिंगों में मैं गया था। मेरा दौरा जो हो रहा था। जब किसानों ने कुछ तो अपनी टूटी-फूटी जंगली जबानों से और ज्यादातर भावभंगी से अपने अपार कष्टों का वर्णन किया तो मुझे बड़ा दर्द हुआ। मुझे कहा गया कि और जमींदारों की ही तरह, जिस जैनी सेठ ने उस पहाड़ को खरीदा है वह भी कहता है कि सर्वे में साफ लिखा है कि सोते (झरने) के पानी, जंगल के फल-फूल और काठ-बाँस वगैरह पर किसानों का कोई हक नहीं है। फलत: बिना सेठ की मर्जी के और बिना हर चीज के लिए कर दिए वे लोग कोई चीज छू नहीं सकते! इस पर मैंने साफ सुना दिया कि सर्वे में अगर हवा और सूर्य की रोशनी पर भी जमींदार अपना कब्जा लिखा लें तो क्या गरीब लोग और किसान मर जाएँ और न साँस लें, न सूर्य की रोशनी शरीर पर लगने दें? किसानों को क्या पता कि खतियान में कब, किसने, क्या बला लिख लिखा दी? उन्हें किसने इस बात की नोटिस दी थी कि खतियान में ऐसा लिखा जा रहा है, तुम लोग चलके जो कुछ उज्र करना हो करो? उन्हें उस समय अगर ऐसा कहा गया होता उसी समय वे निपट लेते और चाहे जो भी होता, मगर खतियान को बदलवा के ही छोड़ते। मगर चोरी-चोरी ऐसा लिखवा लेने के बाद अब इन्हें मारना यह शैतानियत है, निहायत वेजा बात है। शरीर और घर-गिरस्ती के लिए काठ, बाँस, फल, फूल, घासपात, जल वगैरह तो इन्हें चाहे जैसे हो मिलना ही चाहिए। यदि इन्हें यों ही घुल के मरना नहीं है तो ये चीजें ये लोग लेके ही रहेंगे। इस पर बड़ी कानाफूसी हुई थी कि मैंने भोले मांझियों को उकसा दिया और वे कानून तोड़ने पर तैयार हो गए! अजीब बात है। वे जिन्दा रहना चाहते थे और चाहते हैं और इसीलिए पानी, काठ, वगैरह चाहते हैं। उन्हें ये चीजें देना नहीं और जबर्दस्ती घुल के मरने देना, फिर भी कहना कि उभाड़ा जाता है! चाहे जहाँ से जैसे हो जरूरी चीजें उन्हें दीजिए, दिलाइए। फिर देखिए कि कानून तोड़ने या उभाड़ने-उभड़ने की बात कहाँ आती है। फिर भी जो लोग ऐसी बातें बोलते ही रहते हैं उन्हें संसार के एतत् सम्बन्धी इतिहास को पढ़के अपनी अक्ल की दवा कर लेना चाहिए। जंगल के इन्हीं हकों को लेके पहले के समय में संसार के किसानों ने क्या-क्या नहीं करडाला? इस बात की थोड़ी सी झाँकी उन्हें कराने के लिए मैं श्री पॉल लाफार्ग (Paul Lafargue) की किताब सम्पत्ति का विकास (Evolution of Property) से एक उद्धरण देना उचित समझता हूँ। वह यों है ^The forests were grabbed up more brutally : eschewing all legal formalities, the landlords adjudged to themselves the ownership of the woods and underwood; they enclose the forests and forbade hunting and abolished the right of estovers; the right of taking wood for fuel and for the repairs of houses, fences, implements, etc. The encroachments of the nobles on the forest lands, which were the Common property of the village, gave rise to terrible revolts of the peasants. The Jac queries, which broke out in the middle of the fourteenth century (1357-58) in the provinces of the north and the centre of France, were in fact, occasioned by the pretentions of the nobles to forbid hunting and to interfere with the right of common in the forerts, and the enjoyment of the rivers. Similar conflicts arose in Germany, such as the famous revolt of the Saxons against the Emperor Henry II, and that of the Suabian peasants, who, in the time of Luther, took up arms against the lords, who debarred them from the enjoyment of the forests. These peasant insurections compelled the lord on several occasions to respect the ancient rights of Common, which consisted in the right—limited only by the peasents' wants—to take wood and brushwood for hedging, firing and repairing his implements (hedge-bote, fire-bote and plough-bote); and in the right of Common pasture, or the right to send his cows, horses, swine and in some cases his goats to graze on the commons throughout the year, the month of May alone excepted. So firmly were rooted these rights that Lapoix de Freminville declared, in 1760, that even in the event of their abuse by the peasants, they could not be taken away from them ‘for the right of usage is perpetual, and being so, in is accorder alike to the actual inhabitants and to those who may come after them; one cannot strip of an acquired right even those who are as yet unborn. But the revolutionary bourgoisie of 1789 felt none of the fedual legists' respect for the peasant's rights, and abolished them for the benefit of the landed proprietors.’ 'अधिक निर्दयता के साथ जंगलों को हथिया लिया गया। कानूनी बातों को ताक पर रखके जमींदारों ने जंगलों और झाड़ियों पर अपना अधिकार जमा लिया। उनने जंगलों को घेर दिया (रिजर्व और प्रोटेक्टेड बना लिया), उनमें औरों का शिकार खेलना रोक दिया और घर-गिरस्ती के लिए काठ-बाँस वगैरह लेना खत्म कर दिया, जिससे ईंधन तथा घर, घेरा, औजारों की मरम्मत वगैरह के लिए कुछ भी जंगल से लिया जा सकता न था। जो जंगल बराबर गाँवों की सार्वजनिक सम्पत्ति थे उन्हें इस तरह जमींदारों के द्वारा हथियाए जाने का नतीजा यह हुआ कि किसानों के भयंकर विद्रोह होने लगे। फ्रांस के मध्य एवं उत्तारी हिस्सों में जो चौदहवीं सदी के मध्य में (1357-58) जैकरी नाम के किसान-विद्रोह होते रहे वे दरअसल इसीलिए हुए कि जमींदारों ने जंगलों में आम लोगों के शिकारों और दूसरे हकों को छीनना शुरू कर दिया था और नाले-नदियों के सम्बन्ध में भी यही किया था। जर्मनी में भी इस तरह के विद्रोह हुए, जैसा कि शहंशाह द्वितीय हेनरी के विरुद्ध सैक्शनों (सैक्शनी प्रान्त के निवासियों) का विख्यात विद्रोह। स्वैव इलाके के किसानों ने भी लूथर के जमाने में इसी तरह उन जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिया, जिनने उनके जंगल सम्बन्धी हकों को छीना था। किसानों की इन बगावतों और विद्रोहों का नतीजा यह हुआ कि जमींदार लोग बहुत मौकों पर आम लोगों के उन अधिकारों को कबूल करने के लिए मजबूर हुए जिनके फलस्वरूप लोग काठ-बाँस और काँटे-कुश, घास-पात वगैरह खेतों आदि के घेरने, जलाने और दूसरी जरूरतों के लिए, जैसा कि घेरने, आग जलाने और हल आदि के लिए, ले सकें। जमींदारों ने सार्वजनिक चरागाहों के हकों को भी माना जिससे किसान लोग अपनी गाएँ, घोड़े, सूअर और कभी भी बकरियाँ भी चरागाहों में साल-भर बराबर चरने को भेजा करें। जंगल के काठ-बाँस वगैरह कितना लिया जाए इसमें किसान की जरूरत ही निर्णायक थी। (न कि कोई शर्त थी कि इतना ही लिया जाए)। केवल मई मास में ही चराई पर रोक थी। ये अधिकार इतना ज्यादा सर्वजनप्रिय थे कि 1760 में फ्रांस में लापोआद फ्रेमिनविल नामक विद्वान ने घोषित किया था कि अगर किसान इन अधिकारों का दुरुपयोग भी करें, तो भी उनसे हक छीने जा सकते नहीं हैं। क्योंकि रस्मोरिवाज के अनुसार जो हक हासिल होते हैं वे सनातन हैं। इसीलिए ये हक न सिर्फ उन्हें प्राप्त होते हैं जो मौजूद हों, किन्तु जो पीछे आएँगे या पैदा होंगे उन्हें भी प्राप्त रहते हैं और जो लोग अभी पैदा हुए ही नहीं उनके हकों को कोई कैसे छीन सकता है? मगर 1789 के क्रान्तिकारी पूंजीवादियों के दिल में सामन्त युग के कानूनी हकों के जानकारों की तरह इन हकों के लिए जरा भी खयाल न था। इसलिए उनने जमीन के मालिकों के फायदे के लिए किसानों के इन हकों को मिटा दिया।' इस उद्धरण पर टीका-टिप्पणी बेकार है। यह इतना साफ है कि सारी बातें आईने की तरह झलक रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि इसका लेखक झारखंड में बैठ के सारी दास्तानें ऑंखों देखने के बाद ही ये पंक्तियाँ लिख रहा है! यहाँ की सारी बातें अक्षरश: इसमें चित्रित की गई हैं, सिवाय एक बात के। फ्रांस, जर्मनी आदि मुल्कों में किसानों ने लगातार विद्रोह करके और जमींदारों का सशस्त्र मुकाबला करके ही उन्हें मजबूर किया था कि अपनी शैतानियत से बाज आएँ और खुले आम किसानों के इन जंगल के हकों को कबूल करें। मगर यहाँ वह बात नहीं हुई। अगर कभी-कभी किसानों ने कुछ किया भी तो शान्ति से थोड़ा आगे बढ़के खुद दब गए, दबा दिए गए। वे अपने बल से जमींदारों को विवश कर न सके, उनके मद को ध्यानवंस कर न सके। नदी-नालों पर रोक की बात तो पारसनाथ पहाड़ के झरनों और सोतों पर जैनियों के द्वारा डाले गए प्रतिबन्ध को ही याद दिलाती है। रिजर्व जंगल में भी जो यह रोक लगी है वह भी एकाएक याद हो आती है। जिस प्रकार 1789 में फ्रांस के धानियों ने किसानों के ये हक जबर्दस्ती छीन के बेरहमी से जमींदार को दे दिए ठीक वैसे ही यहाँ भी काम किया गया है। सनातन हक कलम की एक नोक से पूँजीपतियों की सरकार ने खत्म कर दिया और जमींदारों की पाँचों घी में करदी। यहाँ एक कमी और भी है। फ्रांस में तो एक ऐसा विद्वान कानूनदाँ हो गया जो सामन्त-युग के कानूनी हकों को खूब जानता था। इसलिए उसने 1760 में ही यह घोषित कर दिया था कि 'चाहे किसान इन अधिकारों का दुरुपयोग भी करें। फिर भी उनके ये हक कथापि छिन नहीं सकते। ये हक इतने सर्वजन प्रिय माने जाते हैं और लोगों के दिलों में ये इतने जमे हैं कि जो आगे पैदा होंगे उन्हें भी ये प्राप्त हैं। क्योंकि पुरानी रीति-रिवाजों के ही अनुसार ये हासिल हुए हैं, न कि कानून के जरिए। इसीलिए सदा रहने वाले हैं और इसीलिए जो अभी तक जनमे ही नहीं या आए ही नहीं, किन्तु भविष्य में आने वाले हैं उनके ये हक कैसे छिन सकते हैं? यह बात हो नहीं सकती, आदि।' मगर यहाँ ऐसे कहने-सुनने वाले विद्वान और ईमानदार लोगों का पता नहीं चलता। उनकी लिखी ऐसी बातें यहाँ पाई जाती ही नहीं। कितनी सुन्दर और स्वाभाविक बात है कि जंगल के अधिकार कानून के जरिए न तो मिलते हैं और इसीलिए न छीने जा सकते हैं। ये तो परम्परा प्राप्त है। वंश परम्परा और रीति-रिवाजों के अनुसार ही हासिल हैं। इसलिए कानून का सिर्फ एक काम है और वह यह कि इन पर अमिट मुहर लगा दे और ताम्रपत्र में लिखके घोषणा कर दे कि ये हक आदि औलाद के लिए हमेशा कायम रहेंगे। ये कभी छीने जा सकते नहीं। यदि इसका दुरुपयोग भी किसान करें तो भी उनसे इन्हें कोई छीनने की हिम्मत कभी न करे, खबरदार। आजकल के दिमागदार और देश सेवक कहे जाने वाले कहते हैं कि किसान लोग अधिाकारों का दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए इनका छिना जाना या सीमित किया जाना जरूरी है। ऊपर के वाक्यों में आज से प्राय: दो साल पहले ही एक विद्वान ने इसका मुँहतोड़ उत्तर दे दिया है कि हर्गिज ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। यह तो सरासर जुल्म होगा। छीनना तो छीनना, वह तो कहता है कि इन्हें संकुचित भी नहीं कर सकते। किसान जितनी लकड़ी, जितनी घास, जितने बाँस वगैरह चाहे खुशी से ले सकता है। जब सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था तब यह बात कही गई ठेठ सामन्त युग में। अब तो पूँजीवादी युग माना जाता है जहाँ सभ्यता अपनी टाँगें तोड़के बैठी है और अधिकारों की बड़ी छानबीन होती देखी जाती है। मगर फिर भी यह अन्धेर देखें, कब यहाँ के किसान अपने इस सनातन परम्परा प्राप्त अधिकारों को फिर पहले की ही तरह पूर्णरूप से प्राप्त करते हैं। जंगल के अधिकारों के मुतल्लिक एक जरूरी बात कहके हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पहले कहा गया है, लाह की बात लेके पलास वगैरह के पेड़ों पर किसानों का हक प्राय: छिन गया है। झारखंड के प्राय: सभी जिलों में कमोबेश लाह पैदा होती है। पलास, कुसुम (वनवृक्ष) और बेर के ही पेड़ों में यह होती है। इन्हीं पर लाह के कीड़े लगते हैं, लगाए जाते हैं और उन्हीं से लाह पैदा होती है। हमने पलामू में यह चीज ऑंखों देखी है। किसानों के दुखड़े भी हमारे सामने वहाँ खासतौर से पेश हुए थे। रांका की जमींदारी की बात थी। हम सुन के ताज्जुब में आ गए! मगर बात तो सही थी, सही है। जमींदारी के चलते जो न पाप हो जाए! ऐसा होता है कि खेतों में पलास वगैरह के पेड़ लगे हैं और सर्वे की खतियान में वे खेत किसानों के कब्जे में ही उनके कायमी लिखे गए हैं। मगर ज्यादातर ऐसा किया गया है कि उन्हीं खेतों के भीतर के पलास वगैरह के पेड़ों पर कब्जा लिखा गया है जमींदार का। यह गजब की बात है। चारों ओर किसानों के ही खेत हैं। जमींदार की खास कब्जे की, जिरात या गैर मजरुआ जमीन कहीं एक इंच भी नहीं है। किसान बेचारे बराबर ही उन खेतों में खेती करते और फसल उपजाते हैं, रखवाली करते, सोते-बैठते और मरते-मिटते हैं! जमींदार का या उसके यमदूतों का पाँव भी वहाँ कभी नहीं पड़ता! फिर भी उन्हीं खेतों के बीच खड़े पलास के पेड़ों पर जमींदार का अधिाकार और किसान का नहीं! यह तो महान अन्धेर है! यह भी नहीं कि उन पेड़ों को कभी जमींदारों ने ही लगाया लगवाया हो। वे तो जंगली हैं। यों ही पैदा हुए हैं। अब भी पैदा होते रहते हैं ! फिर भी जमींदारों के! गजब है! एक बार सर्वे खतियान में किसी अक्ल के अन्धो ने लिख दिया! फिर तो जो नए भी पेड़ पैदा होंगे वह जमींदार के ही होंगे! यह तो गजब की अन्धेरपुर नगरी है। कहते हैं, सर्वे के अफसर लोग बड़ी जाँच-पड़ताल करके असलियत का पता लगाते थे! तो क्या यही असलियत है? या कि उस समय संयोगवश शराब पीके वे मतवाले हो गए थे? या कि किसी और तरह की शराब के नशे ने अपना काम कर दिया? यही हालत महुवा के पेड़ों की भी है। पलास वगैरह से तो लाह पैदा होती है और उससे मिलते हैं पैसे, काफी पैसे। मगर महुवा? उससे तो यह बात है नहीं। महुवा के फूल से तो शायद ही चार-आठ आने कभी मिल सकें। हाँ पहाड़ी इलाके के गरीबों का वह प्रधान खाद्य है। बेचारों को चीनी-गुड़ तो पहले मिलते न थे और न दूसरा खाद्य ही। इसलिए मीठे-मीठे महुवा के सूखे फूलों को जमा करके और सुखा के रखते थे, ताकि साल-भर आवश्यकतानुसार काम चलाते रहें। वे मीठे बहुत होते थे। गर्म भी इतने कि कुछ कहिए मत। मगर वे तो उन गरीबों के आधार ठहरे। हंड़िया नाम की उनकी अपनी शराब में भी शायद महुवों से मदद मिलती थी। चावल के भात से ही यह शराब पहड़ी लोग तैयार करते और उसे ही पीते हैं। हमने कलेजे पर पत्थर रख के पहली बार एक किसान को देखा कि गमछे के किनारे एक मुट्ठी महुवा बाँधो बहुत सवेरे जंगल की ओर टांगी लिए चला जा रहा है। रोक के पूछा कि कहाँ जा रहा है? उत्तार मिला कि लकड़ी काटने जंगल में। कब लौटेगा, यह पूछने पर उत्तर मिला कि शाम के ऍंधोरे तक। अगले दिन बाजार में बेचने और उसी पैसे से गुजर करने की बात थी। पास में दिन-भर का खाना? मैंने यह सवाल किया। उसने वही मुट्ठी-भर महुवा दिखा दिया। चार पैसे भी थे। मैंने पूछा, 'और ये पैसे?' उसने कहा कि यह तो घाट पर जमींदार के चौकीदार को देंगे! रोज-रोज यही करते हैं। मुश्किल से दो आने की लकड़ी लाते हैं! उसमें एक आना तो जमींदार का ही हुआ। लकड़ी लाने और बेचने में दो दिन लग जाते हैं। क्योंकि पहला दिन तो लाने में ही जाता है। बाजार दूर है। जाने-आने में दूसरा दिन खत्म! एक आना रोज की कमाई! इतनी मेहनत! फिर भी खाने को सिर्फ मुट्ठी-भर महुवा! एक आने में ही तो दो दिन गुजर करना था। फिर बच्चे और कपड़ा-लत्ता चाहिए। ऐसी दशा में मुट्ठी-भर महुवा से ज्यादा कैसे मिलता? हाँ, जमींदार को तो पूरे एक आने मुफ्त ही मिले! उसकी हड्डियाँ साफ दीखती थीं। गिन सकते थे कि कितनी हैं। मेरी हिम्मत टूट गई। बोल न सका! दिल में आया कि यदि अभी धारती फटे तो शर्म से समा जाऊँ। नहीं तो जमींदारी को और वर्तमान समाज को मिटा के ही छोड़ईँ! यह है संक्षेप में महुवा की दर्दनाक दास्तान! खूबी तो यह है कि महुवा के पेड़ों पर भी जो खेतों में भी होते हैं और बाहर भी, जमींदार का ही कब्जा लिखा रहता है। मगर ये होते हैं काफी फैले। इसलिए एकाधा कट्ठे में फसल होने ही नहीं देते। पलास तो ऐसे होते नहीं। मगर महुवा महाराज तो बड़े ही खतरनाक होते हैं। यह कोई नहीं पूछता कि यदि वे जमींदार के हैं तो खेत की फसल मारने का हर्जाना जमींदार क्यों नहीं देता? नहीं तो कम से कम उतनी जमीन का लगान तो छोड़ दे जितनी की फसल मारी जाती है। मगर यह पूछे कौन? यहाँ तो कुएँ में ही भाँग पड़ी है! म्याऊँ का ठौर कौन पकड़े? सबके सब तो जमींदार के दोस्त-दलाल ही ठहरे। और किसान सभा वालों की सुने कौन? वे तो सरकार तथा जमींदार दोनों के ही बागी ठहरे। सबसे दर्द की बात तो यह है कि उन महुवा, पलास आदि पेड़ों का बन्दोबस्त उस किसान के साथ न करके हमेशा गैरों के साथ ही ये जमींदार भलेमानुस करते हैं? क्यों? इसीलिए कि अपने खेतों में दूसरों को जाने देना किसान चाहेगा नहीं। फलत: मजबूरन औरों से भी ज्यादा पैसे देके खुद बन्दोबस्त लेगा। इसे ही रक्त चूसना कहते हैं। जमींदार किसानों से खून निकालने की बेदर्द कोशिश उसी तरह करते हैं जिस तरह सूखी हड्डी से खून निकालने की कुत्तो करते हैं! किसान हजार चिल्लाए। मगर सुने कौन? सरकार बहरी, उसकी कचहरियाँ बहरी, हाकिम बहरे, पुलिस बहरी, नेता बहरे, साधु-महात्मा बहरे, देवी-देवता बहरे और भगवान भी बहरा! मेरे सामने जब यह दुखड़ा पेश हुआ तो मैंने मीटिंगों में साफ ही कह दिया कि 'यदि ऐसी अन्धेर है और जमींदार नहीं मानते हैं तो उन्हें गैरों के साथ इन पेड़ों का बन्दोबस्त करने दो और चुपचाप रहो। मगर डंके की चोट सुना दो कि बन्दोबस्त लेने वालों को हमारे खेतों से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे खेतों में पाँव देने का उन्हें कोई कानूनी या नैतिक हक नहीं, जब तक हम आज्ञा न दें। और हम तो साफ कहते हैं कि किसी दूसरे का पाँव खेतों में धरने हर्गिज न देंगे। पहले से ही सुना देते हैं। लोग सजग हो जाएँ, बन्दोबस्त और ठेका लेने वाले सँभल जाएँ। हवाई जहाजों से, जादू मंतर से या जैसे हो, ऊपर ही ऊपर उड़ के पेड़ों पर आएँ और बिना जमीन छुए ही ऊपर से ही लाह या महुवे के फूल लेके चले जाएँ। तभी खैरियत है। तब हम कुछ न बोलेंगे। मगर अगर उनने हमारे खेतों में अपने पाँव दिए तो जान लें कि हम उन पाँवों को तोड़ देंगे और इसमें अपराधी वही होंगे। हमारा इसमें कुछ भी दोष न होगा। यह बात तो वे लोग कभी भूलें मत आदि-आदि। बस, तुम्हारी जीत होके ही रहेगी। यही तो सीधा दवा है। मगर है यह अचूक। आज भी मैं यही उपाय उन किसानों को बता सकता हूँ। दूसरा उपाय मेरे पास है नहीं। जालिम लोग आरजू-मिन्नत से या गिड़गिड़ाने से कभी नहीं मानते। बल्कि और ज्यादा हिम्मत से जुल्म करने लग जाते हैं। किसानों में स्वावलम्बन आए और वे अपने पाँवों पर खड़े हों, तो उनका बेड़ा पार हो। वे हक के लिए मरना मिटना सीखें, निर्भय बनें और संगठित हों। क्योंकि एक-दो-चार के ऐसा कहने से भी जमींदार न मानेंगे जब तक सामूहिक रूप से उन्हें इन पेड़ों के बारे में डट के ललकारा न जाए। ज्योंही किसानों ने व्यापक और सामूहिक रूप से मीटिंगें करके और नोटिसें बाँट के ऐसी ललकार शुरू की कि जमींदार और उनके ठेकेदार दोनों ही पस्त हो जाएँगे। 3.12.41A महुवा के सम्बन्ध से हमें एक महत्वपूर्ण घटना याद आ गई। जब पलामू के दौरे के सिलसिले में 1939 के दिसम्बर में हम महुवाडांड़ गए थे तो वहाँ जो कुछ देखा कभी भूलने का नहीं। कई मील से ही वहाँ के आदिवासी किसानों ने बड़े-बड़े झंडों के साथ गाँव से जुलूस में निकल-निकल के हमारा स्वागत किया। हमने तरह-तरह के झंडे पहले-पहले वहीं देखे। किसान स्त्री पुरुष, बच्चे ऐसे सीधे और भोले कि कुछ पूछिए मत। फिर जब हम मीटिंग में गए तो देखा कि डाकबँगले के लम्बे मैदान में ही सोलहों आने स्वदेशी ढंग का मंच बना है। जंगली डाल पात से ही उसे सजाया था। ऊँचा काफी था। चारों ओर दल के दल स्त्री-पुरुष बैठे थे। बहुत बड़ी जमात थी। जाड़े के असली दिन और सबसे ठंडी वह जगह। नेतरहाट का पहाड़ जो सबसे ठंडा माना जाता है, महुवाडांड़ का पड़ोसी है। सभा से ही नजर आता था। फिर भी किसान स्त्री-पुरुषों के पास कपड़े कहाँ? मामूली ही कपड़े थे। वे तो यों भी अधानंगे होते ही हैं। मगर हृष्ट-पुष्ट, काले-काले और देखने में बड़े ही सुन्दर थे। मैं सदा इन लोगों की सुन्दरता और गठीले बदन को देख के मुग्धा हो जाता हूँ। यदि इन्हें घी, दूधा और सुन्दर खाना मिलता, तब ये कैसे होते, यही तो बात सोचने की है। उस अपार भीड़ के बीच मंच
पर जाते ही मैंने जंगली पत्ता की बड़ी-बड़ी पुड़ियों में तीस-पैंतीस ढंग के
फल-फूल वगैरह देखे। पूछने से पता लगा कि इन गरीबों की यही खुराक है। मगर
जमींदारों के करते यह भी मिलने नहीं पाती! इस पर भी कर है! उफ! जंगली जड़ें,
फूल, फल, पत्तो और उन पर भी आफत! कई तो चीजें इनमें ऐसी भी थीं जो बहुत
कड़वी और एक तरह से जहरीली होती हैं। उन्हें बार-बार उबालने और पानी में देर
तक डुबो रखने पर ही गले के नीचे जैसे-तैसे वे लोग भी उतार सकते हैं! आखिर
भूख तो मानती ही नहीं। दृष्टान्त के लिए (1) गेंठी को लीजिए। यह एक जड़ है।
इसे लगातार चार बार उबालने के बाद सारी रात पानी में डाल रखते हैं। तब कहीं
खा सकते हैं। इसी तरह (2) सरई को लीजिए।यहबड़ी ही कड़वी होती है। यह है साखू
के पेड़ों का फल। इसे छह बार पानी में उबालना जरूरी होता है। इन दो के सिवाय
कुछ के नाम ये हैं, (3) तेंद, (4) डिंठोरा, (5)जंगली बेर, सभा में तो मैंने अपना हृदय निकाल के ही रख दिया। वे लोग मंत्रामुग्धा की तरह सुनते रहे। मैं तो ऐसी सीधी भाषा बोलने का आदी हूँ कि जंगल के किसान भी उसे समझ सकते हैं। गुजरात वगैरह में भी मुझे जंगली लोगों से काम पड़ा है। बातें सुनके उनका चेहरा खिल उठा। जब मुझे सभा में ही पता चला कि पास के पुराने रोमन कैथलिक मिशन वालों ने जिन्हें ईसाई बनाया है वे सभा में नहीं आए हैं। वे रोके जाते हैं आदि-आदि, तो मुझे बड़ा गुस्सा हुआ। मैंने साफ सुना दिया कि धर्म-मजहब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो आदमियों से मिलना और बातें करना चाहता हूँ। मुझे तो उन्हें समझाना है। फिर चाहे वह किसी धर्म के हों। इसीलिए मुझे ईसाई धर्म से कोई भी लड़ाई नहीं। मगर जब उनकी यह हरकतें सुनता हूँ तो गुस्सा आता है। क्या वे प्रभु ईसू मसीह की भेड़ें तैयार करना चाहते हैं? यह तो गलत है। मैं समझता था कि ईसाई लोग आदिवासियों को भले ही ईसाई बनाते होंगे। मगर उसी के साथ उन्हें हकों के लिए लड़ना सिखाते होंगे। ऐसा देखा भी गया था कि चमार वगैरह ईसाई होते ही हिन्दू जमींदारों से कहीं-कहीं भिड़ गए थे। मैं यह भी सोचता था कि जब तक ये आदिवासी हिन्दू थे तब तक बेशक इनमें तीन गुण पाए जाते थे और वो थे सच बोलना, व्यभिचार से बचना और निर्भीकता। मगर उनका जीवन पशुवत् था। कम से कम हिन्दुओं ने उन्हें ऐसा ही बना दिया था। इसलिए ईसाई होते ही यद्यपि वे तीनों महान् गुण जाते रहे और यह पक्की बात है कि सभ्यता पिशाची जरूर ही उन तीनों को खा जाती है। उन्हीं की कब्र पर वह फलती-फूलती है। तथापि वे पशु से आदमी जरूर बनते होंगे और मर्द की तरह हक के लिए लड़ते होंगे। मेरा यह भी खयाल था जिन यूरोपीय देशों से ये पादरी यहाँ आए हैं वहाँ के किसानों ने तो क्रान्तियाँ की हैं और शहंशाहों के तख्त उलट दिए हैं। जंगल के हकों के लिए तो जैसा कि पहले कहा है उनने क्या-क्या नहीं कर डाला था। इसीलिए उन्हें यह शिक्षा भी दी जाती होगी। मगर जब मैंने देखा और पास के गाँवों में जाके पूछताछ करके पता भी लगाया कि ईसाइयों को वे लोग मसीह के मेमने के रूप में ही रखते हैं और बाकी किसानों से उनकी निराली ही दुनिया बना छोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द हुआ। इस बात की आशा न थी। पास-पड़ोस के ही अपने भाइयों से ही धर्म बदलते ही, वे लोग बिलकुल ही नाता तोड़ के गूलर के कीड़ों जैसी अपनी अलग दुनिया बना लें यह बात असह्य थी। तब तो मानना होगा कि ये मिशन भारी अनर्थ कर रहे हैं! केवल धर्म के नाम पर ही हिन्दुओं से लड़ा देना कोई अच्छी बात नहीं! यह तो संसार की पुरानी बीमारी है और हमारे अभागे देश में बुरी तरह फैली है। हम तो इससे बचना चाहते हैं और हमें आशा थी कि पश्चिमी देशों वाले ये मिशन इस बात की रोशनी वहाँ से जरूर ही अपने साथ लेके ही पहुँचे होंगे। फलत: रोटी, जमीन और हक के लिए ही ईसाई किसान भी लड़ना सीख गए होंगे। मगर यह न पाके हमें बड़ी निराशा हुई। यह हमारे लिए पहला ही मौका था। और जब हम पास के गाँवों में पूछताछ करने गए और यह देखने कि किसानों की दशा कैसी है तो हमें एक दो अजीब बातें मालूम हुईं। पहली तो यह कि रास्ते में शाम को तीन-चार बच्चियाँ-बच्चे मिशन की तरफ जाते मिले। हमने कौतूहल से जानना चाहा कि इस समय ये कहाँ जा रहे हैं। जब हमारे 'किसान' जाति वाले एक साथी ने उनकी ही भाषा में उनसे पूछा तो उत्तर मिला कि 'पाप स्वीकार करने' के लिए फादर (पादरी गुरु) के पास जा रहे हैं। एक बच्ची ने यह उत्तार दिया और हमने सुना। हम समझी न सके कि यह माजरा क्या है। मरने के समय तो ईसाई पादरी पाप स्वीकार (confession) करवाते हैं ऐसा जाना-सुना था। यह क्या बात है? पीछे जाँच से पता चला कि प्रतिदिन दो-चार दिनों बाद फादर के पास जाके पाप स्वीकार करने का इनमें नियम है और जब घर वाले प्राय: काम के कारण छुट्टी नहीं पाते तो, बच्चे-बच्चियों को ही सब की ओर से कनफेशन करने को भेज देते हैं! यह खूब रहा! प्रतिदिन सारे कुकर्मों के धोने का यह अच्छा साबुन मिला! जैसे हिन्दू संध्यानया गायत्री के जरिए और मुसलिम नमाज के जरिए रोज-रोज पाप धोते हैं वैसे ही ईसाई कनफेशन के जरिए! इतिहास की ठीक ही पुनरावृत्ति हो रही है! दूसरी बात यह मालूम हुई कि हिन्दू गुरुओं और मुसलिम पीरों की ही तरह पादरी गुरु साल में एक बार गाँवों में चेलों के पास जरूर जाते और खा-पी के तथा 'पूजा' के रूप में रुपया, कपड़ा वगैरह लेके लौट आते हैं। हो सका तो कुछ नए चेले भी जरूर बना लेते हैं! यह भी वही गुरुओं की 'रामत' हो गई! सिवाय धार्म के नाम पर पाखंड फैलाने के और कुछ भी सामयिक उपदेश गृहस्थों को वे भी नहीं देते! खुदा खैर करे! अब महुवाडांड़ की सभा की एक ही बात रह जाती है और है वह दिलचस्प। सभा के बाद सभी किसान, जो दूर से चावल, लकड़ी और हांडी साथ लेते आए थे वहीं ठहर के जत्थे-जत्थे खाना पकाने लगे। उनके खाने के पूर्व ही मैं सो गया। मगर अचानक आधी रात में नींद टूटी तो मृदंग वगैरह बाजे की ध्यानवनि के साथ गाने की मधुर तान सुनी। बाहर निकल के देखा तो जगह-जगह स्त्री-पुरुष गिरोह के गिरोह नाच गान कर रहे हैं! कितने ही गिरोहों में एक दल स्त्रिायों का और दूसरा पुरुषों का आमने-सामने खड़ा चक्कर देता और नाचता गाता है। ऐसी सुन्दर चीज कि क्या कहा जाए? नाच गाने के साथ व्यायाम और परिश्रम भी कितना सुन्दर! नजदीक से देखा! स्त्री-पुरुषों की होड़ भी खूब थी! सारी रात यह बात चलती रही! जरा भी विराम नहीं! ठेठ सुबह उजाले में कहीं जाके खत्म हुई! किसी ने पलक भी न मारी! पहले सोचता था कि कपड़े बिना कड़ाके के जाड़े में यहाँ मैदान में इनकी रात कैसे कटेगी। मगर उत्तर मिल गया! व्यायाम भी हुआ, मनोरंजन भी, कला भी कायम रही और जाड़ा भी कट गया! वाह रे दिमाग जिसने एक ही साथ चार सुन्दर काम करने का रास्ता साफ किया! रात-भर आग भी जगह-जगह जलती जरूर रही। मगर उसके नजदीक ज्यादा देर तक तो कोई बैठ न सका! यह स्वर्णीम दृश्य मैं भूल नहीं सकता। गुजरात के जंगली प्रदेशों में भी मैंने ऐसा ही देखा है। दूसरी जगह भी ऐसा ही होता है! अब जंगल के कष्टों से ही ताल्लुक रखने वाली खास बात एक ही रह जाती है और है वह बड़ी ही सख्त। मैंने उसके करते गरीब किसानों को छाती पीटते और हाथ मारके रोते देखा है। उसके चलते वे लुट जाते हैं, तंग तबाह हो जाते हैं, सर्वस्व गँवा देते हैं। वे तो सचमुच लुट जाते हैं और उनकी कमर सीधी हो नहीं पाती। बात असल यह है कि काजीहाउस या अड़गड़े जंगली प्रदेशों में अकसर होते हैं जिनमें पशु घुसा दिए जाते हैं। यों तो अड़गड़े सर्वत्रा ही कसाई खाने का काम करते हैं। उनमें जाने वाले पशु घास और पानी बिना मर जाते हैं। देखने के लिए शायद ही नाममात्रा को जरा मरा चारा उनके सामने फेंक दिया जाता हो। मगर दरअसल पशुओं को वहाँ मार ही डालते हैं! मैंने इसका खूब अनुभव किया है। ये सभ्य कसाई खाने क्यों बने, यह समझने में मैं तो असमर्थ हूँ। मगर जंगलों के अड़गड़े तो गजब के होते हैं! जरा भी जंगल के चपरासी किसानों से रंज हुए या जमींदार के अमले रंज हुए कि ढूँढ़-ढ़ाँढ़ के उनके सभी पशुओं को जबर्दस्ती काजीहाउस में घुसा देते हैं! एक-एक बार पचास-पचास सौ-सौ या उनसे भी ज्यादा! और उन्हें वापस लाने में जुर्माना देना होता है उसके करते किसान का घर-बार और जमीन बिक जाती है। कानून ऐसा है कि रोक सकते नहीं। नहीं तो फौजदारी में जा फँसें! दिन-रात सबका पड़ने के कारण दूधे दही, घी, घूस वगैरह न देने पर अमले और चपरासी खामख्वाह रंज होते ही हैं! किसानों ने हजारों बार खून के ऑंसू बहाके कहा है कि किसी प्रकार ये काजीहाउस तो यहाँ से मिटें! तब तो उन्हें साँस आ जाएगी।
|
|
मुखपृष्ठ | उपन्यास | कहानी | कविता | नाटक | आलोचना | विविध | भक्ति काल | हिंदुस्तानी की परंपरा | विभाजन की कहानियाँ | अनुवाद | ई-पुस्तकें | छवि संग्रह | हमारे रचनाकार | हिंदी अभिलेख | खोज | संपर्क |
| Copyright 2009 Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha. All Rights Reserved. |