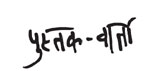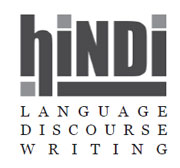पूर्वमीमांसा दर्शन
प्रत्येक
प्राणी के
चित्त
में सर्वदा यह उत्कण्ठा बनी रहती है कि दु:ख मुझे न हो किन्तु सुख ही
सर्वदा बना रहे। अतएव सभी तदनुकूल ही यत्न
क्षेत्र
में पदार्पण भी करते हैं परन्तु पूर्णतया पदार्थज्ञान न होने से उचित
उपायों का अनुसरण न कर अपने अभीष्ट का सम्यक् लाभ नहीं कर सकते,
किन्तु आनन्दकण के ही भागी होते हैं और वह भी
अचिरस्थायी तथा मधुमिश्रित-विषभक्षण-जन्य-सुख
के सदृश होता है। दु:ख-निवृत्ति
का तो नाम भी नहीं,
प्रत्युत
सर्वत्र
उनको दु:खों से ही सामना करना पड़ता है,
फलत: वे अपना मनोरथ नहीं सिध्द कर सकते। हाँ,
केवल मनुष्य में यह शक्ति ईश्वर प्रदत्ता है कि वह जो चाहे सो
प्राप्त कर सकता है और इसीलिए उपरोक्त नियमानुसार वह भी उसी
धुन
में लगता है परन्तु यह वार्ता गुप्त नहीं कि प्रत्येक वस्तु के
प्राप्त करने के उपाय होते हैं जिनसे ही वह वस्तु प्राप्त की जा सकती
है। अतएव मनुष्यता के कारण कार्याकार्यी-विचारक्षम होने से वह भी
उपायान्वेषण में
दत्तचित्त
होता है,
परन्तु स्मरण रहे कि उपदेष्टा के बिना इष्टसिध्दि
के उपाय जाने नहीं जाते। सब का ज्ञानभण्डार उत्पत्ति
के साथ ही फूट नहीं पड़ता किन्तु अन्ततोगत्वा ताले में कुंजी तो लगानी
ही पड़ती है। विश्वविद्यालय के बनाये नियमों के बिना बी. ए. की डिग्री
प्राप्त करना तथा उससे फल प्राप्त करना सम्भव नहीं,
इसके अलावे सदुपदेश न मिलने पर वंचक लोगों को तो
उपदेश मिलेगा ही, जिसका परिणाम यह होगा कि
लक्ष्यसिध्दि तो दूर रही उससे सैकड़ों कोस पड़ जाना होगा। जैसे कोई
बालक शिक्षाकाल में उचित शिक्षा स्थानों में प्राप्त न हो
दुष्टसंसर्ग से भ्रष्टसंस्कार होकर मनुष्यशरीर-साध्य-लक्ष्य
से वंचित रह जाता है और उसका जीवन भविष्य में माता-पिता तथा अन्य
सम्बन्धियों का महान् अनर्थकारी हो जाता है तथा कितने ही भावी सपूतों
की आशा पर उसके संसर्ग से पानी फिर जाता है। ठीक वही दशा मनुष्य की
भी हो सकती है। इसीलिए दयालु महर्षिगणों द्वारा दर्शनों का
प्रादुर्भाव हुआ। जो सदुपदेश तथा असदुपदेश की शाण रूप हैं,
इस बात को आगे प्रसंगवश स्पष्टतया
तत्र यत्र
प्रदर्शन करेंगे। उनका उद्देश्य केवल यही है कि उनसे ज्ञान लाभ कर
पुरुष स्वार्थ तथा परार्थ को यथोचित रीति से सिध्द कर सके। जैसा कि
बालक सभी स्वकीय एवं स्वसम्बन्धियों की इष्टसिध्दि में समर्थ हो सकता
है जब शिक्षालय में प्राप्त होकर उचित शिक्षा क्रम से ग्रहण करे।
कितनों का यह कथन है कि तो फिर दर्शनों का परस्पर
विरोध
क्यों
? एक-दूसरे का खण्डन-मण्डन क्यों करता है
? द्वैत तथा अद्वैत दोनों तो सत्य हो ही नहीं
सकते, पदार्थों की सात और चौबीस या पच्चीस
संख्या तो हो ही नहीं सकती, एक ही बात
सत्य होगी, इससे जाना जाता है कि दर्शनकर्ता
भी पारंगत न थे। किन्तु जिसकी बुध्दि में जैसा आया वैसा ही लिख मारा।
कितने लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे जलवायु प्रभृति ईश्वरीय पदार्थ
सबके लिए समान हैं वैसे ही ईश्वरप्राप्ति का मार्ग भी सबके लिए एक ही
होना चाहिए अर्थात् एक ही
धर्म
व दर्शन चाहिए न कि नाना इत्यादि। इस सब कथनों का तत्तव तथा समाधान
उपरोक्त बालक दृष्टान्त से ठीक-ठीक समझ में आ जायेगा। दर्शन नाम
ज्ञान का तथा जिस द्वारा ज्ञानप्राप्ति होती है उसका है। यद्यपि
ज्ञान प्रद से सभी घट घटादि ज्ञानों का ग्रहण हो सकता है तथापि
शास्त्रीय
संकेत,
प्रकरण और तात्पर्यादि वश से मोक्षोपयोगी
आत्मज्ञान ही यहाँ पर लिया जाता है, अतएव
जिससे उसकी प्राप्ति होगी वह भी उन्हीं पदार्थों का प्रतिपादक होना
चाहिए जो उस ज्ञान के उपयोगी होवें, इस
प्रकार से आत्मज्ञानोपयोगी पदार्थ प्रतिपादक वाक्यसमूह का ही नाम
दर्शनशास्त्र
हुआ। अब विचारना चाहिए कि क्या उस ज्ञानप्राप्ति के अधिकारी सब समान
ही हैं जिससे सबके लिए एक प्रकार का ही उपदेश या दर्शन होना चाहिए
?
क्या स्कूल या कॉलिजों में सब बालकों के लिए एक ही प्रकार के क्लास,
किताबें या उपदेश होते हैं
?
क्या प्राइमरी क्लास के बालकों के लिए बी.
ए.
इत्यादि क्लासों की शिक्षा विरोधिनी नहीं होती जिससे वे हटाकर नीचे
दर्जों में भर्ती किये जाते हैं
?
हाँ पढ़-लिख
लेने पर कोई भी शिक्षा विरोधिनी नहीं हो सकती। ठीक वही दशा दर्शनों
की भी समझनी चाहिए। ये भी बालकवत् अधिकारी के अनुरोध से प्रवृत्ता
हुए हैं और उसी दृष्टि से परस्पर विरुध्द भी प्रतीत होते हैं परन्तु
विचारदृष्टि से नहीं,
इस विषय को आगे प्रत्येक दर्शन में प्रतिपाद्य विषयों के अधिकारी आदि
निरूपण प्रसंग में विस्तार से दिखलावेंगे। इसीलिए इनको
Six schools of Philosophy
कहते हैं। स्कूल पद से उपरोक्त ही तात्पर्य का ग्रहण उचित है। वस्तुत:
तो दर्शनों का परस्पर विरोध है ही नहीं किन्तु विचार बिना ही प्रतीत
होता है इस बात को परस्पर संगति दिखलाते हुए प्रदर्शन करेंगे। अत:
ऋषिगणों की पारंगतता में कोई संशय नहीं है। सबके लिए जल,
वायु आदि समान हैं यह भी कहना असंगत ही है,
प्रत्येक प्रदेशों की भूमि,
जल,
वायु आदि भिन्न-भिन्न
प्रकार के हैं,
किसी की प्रकृति के अनुकूल ही जलादि दूसरे के प्रतिकूल हैं,
शीत,
प्रदेशवासियों के विरुध्द गर्म देश हैं और इनके लिए गर्म देश विरुध्द
हैं,
इत्यादि। और भी देखना चाहिए कि एक ही गृह में पिता पुत्रादि का धर्म
जब समान नहीं होता तो सृष्टि मात्र का कैसे समान हो सकता है। क्या
बड़े राजे-महाराजों
के पास पण्डित,
मूर्ख,
ब्राह्मण और चाण्डाल की बराबर पहुँच हो जाती है और उनकी वहाँ बराबर
ही प्रतिष्ठा होती है
?
इससे स्पष्ट है कि सबके लिए एक धर्म या दर्शन बनाना गोया सब स्कूल या
कॉलिजों में बालकमात्र के लिए एक ही क्लास तथा उपदेशकादि बनाना है।
इसलिए सब लोगों को सामान्यत:
यह बात मान लेनी होगी कि आर्षदर्शनों की प्रवृत्ति के नियमानुकूल
लोगों के बोध होने के लिए ही है। जैसे किसी ऊँचे मकान की छत पर
पहुँचने के लिए सोपान होते हैं वैसे ही परमात्मा जो अति दुर्ज्ञेय
होने के कारण ऊँची छत के तुल्य है उसकी प्राप्ति के लिए दर्शन
सोपानवत् है। जैसे एक सोपान से दूसरे पर जाने से ही सकुशल ऊपर पहुँच
सकता है,
वैसे ही एक दर्शन ज्ञानोत्तर अन्य दर्शन ज्ञान से ही परमात्मा की
प्राप्ति हो सकती है अन्यथा नहीं यह वात्त आगे स्पष्ट की जावेगी।
जो मनुष्य मद्यपान करके विचारहीन हो रहा है उससे किसी ने हँसी में कह
दिया कि तुम्हारे मुख पर कालिमा-पूर्ण बिन्दु विद्यमान है,
उसने विचार में अक्षम होने के कारण स्वयं विचार न करके दूसरों से
पूछा तो किसी ने कहा कि
'नहीं'
और दूसरे हास्यप्रिय ने उत्तर दिया कि
'हाँ'।
बस,
अब क्या था
?
उसका लोगों के कथन पर विश्वास जाता रहा और वह अपने इस क्लेश के
निवारण का यत्न सोचने लगा। इतने ही में किसी वृध्द ने उसे यह सम्मति
दी कि तुम्हारे गृह के अमुक भाग में एक दर्पण है,
उसमें अपने मुख का अवलोकन कर स्वकीय संशय और तज्जन्य दु:ख इन दोनों
को हटा सकते हो। परन्तु स्मरण रहे कि वह दर्पण बाहर नहीं है किन्तु
उसके ऊपर सूक्ष्म वस्त्र का आच्छादन लगा तदनन्तर काष्ठा के ढक्कन से
ढक कर पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया गया है,
इसलिए प्रथम तुम्हें यही उचित है कि उसके ऊपर का मल (मिट्टी) हटाकर
ढक्कन सहित उसे ऊपर करो,
तदुपरान्त काष्ठा का पर्दा भी हटाना होगा और उसके बाद सूक्ष्म वस्त्र
आवरण को दूर कर स्वच्छन्दतापूर्वक स्वमुख निरीक्षण कर सम्पूर्ण
क्लेशों का निवारण कर सकते हो। इस उचित और परमोपयोगी उपदेश को सुनकर
उस पुरुष ने क्रमश: तीनों कार्य करके निर्मल दर्पण को प्रकट किया और
उसमें अपने स्वरूप का प्रतिबिम्ब सुस्पष्ट रूप से अवलोकन कर मुक्त
क्लेश हुआ। यदि प्रथम ही वह मुख ही देखना चाहता और कुछ व्यापार (कर्म
या क्रिया) नहीं करता अथवा वस्त्र रूप आवरण या काष्ठ को ही प्रथम
हटाना चाहता तो क्या कभी भी उसके सफल मनोरथ होने की सम्भावना भी हो
सकती थी या है
?
अथवा क्या कभी भी विचार में यह बात आ सकती है कि जिस पुरुष ने उसे
मुँह देखने के लिए प्रथमत:
'न'
कहकर मल (मिट्टी) हटाने के ही लिए उसे उपदेश दिया उसका तात्पर्य
दर्पण में मुख देखने में नहीं है
?
उसमें मुख को देख लेना तो फल है,
अत: उसके लिए उपदेश करना व्यर्थ है,
साधनों के होने से वह अपने आप ही सिध्द हो सकता है। जो मनुष्य किसी
की बुभुक्षा (भूख) का निवारण करना चाहता है वह उसे
'भोजन
करो'
ऐसी आज्ञा वा उपदेश न देकर
'चावल,
लकड़ी इत्यादि लाओ'
इस प्रकार से भोजन के साधनों का ही उपदेश करता है। यह तो हुई
दृष्टान्त की बात। अब दार्ष्टान्त में आइये। मनुष्य का हृदय सत्य गुण
का कार्य होने के कारण दर्पण से भी निर्मल है इसीलिए वही दर्पण
स्थानापन्न है। जिसमें यह जीव...
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखराशी।
सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा। वारि वीचि इव गावहिं वेदा ॥
इस अपने वास्तव परमात्मस्वरूप का साक्षात्कार करके विविध नामों से
रहित होता है,
जिस जीव के वास्तव स्वरूप के विषय में वेदों की ये घोषणाएँ हैं कि-''अहं
ब्रह्मास्मि,
तत्तवमसि,
अयमात्मा ब्रह्म,
प्रज्ञानं ब्रह्म,
यत्तपरं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्। सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं
नित्यं,
तत्तवमेव त्वमेव तत्॥''
गीता में भगवान् श्रीकृष्णजी ने भी यही कहा है कि
'क्षेत्रज्ञं
चापि मां विध्दि सर्वक्षेत्रोषु भारत'
(गीता
अ.
13)
परन्तु उस अन्त:करण (हृदय) रूप दर्पण् के ऊपर पूर्वोक्त मिट्टी,
काष्ठ और वस्त्र की तरह तीन आवरण (पर्दे) पड़े हैं जिन्हें क्रमश: मल,
विक्षेम और आवरण कहते हैं। इसलिए जब तक ये तीनों पर्दे हटाये न जावें
तब तक अन्त:करण रूप दर्पण में महामोहमदन्मत्ता जीवात्मा अपने वास्तव
पूर्वोक्त स्वरूप को नहीं देखता है और जैसे पूर्वोक्त पुरुष कालिमा
के संशय से दु:खी रहता है उसी प्रकार यह जीव भी भिन्न-भिन्न ग्रन्थों
में भिन्न-भिन्न बातें सुनकर इस सन्देह में मग्न रहता है कि जीवात्मा
ईश्वर से भिन्न है अथवा उसी का स्वरूप और इसी संशय अथवा विपरीत
निश्चय से कि जीव ईश्वर से भिन्न ही हैं,
अपने को दु:खी,
सुखी कर्ता और भोक्ता इत्यादि माना करता है। मनुष्यों के हृदय में जो
राग-द्वेष,
मद,
छल और कपट प्रभृति दुर्गुण भरे रहते हैं उनका ही नाम प्रथम (सबसे
ऊपर) या मल का पर्दा है। और चित्त की प्रबल चंचलता-जिसे गीता में
स्पष्ट ही कह दिया है कि-
चंचलं हि मन: कृष्ण,
प्रमाथि बलवद् दृढम्।
तस्याहं निग्रहं मन्ये,
वायोरिव सुदुष्करम्॥
अर्थात् मन अत्यन्त चंचल है जिसका रोक सकना वायु को रोक रखने के समान
है-का नाम विक्षेम अथवा दूसरा पर्दा है और अपने वास्तव स्वरूप की
अप्रतीति वा अज्ञान तीसरा अथवा आवरण रूप पर्दा है। इन तीनों की
निवृत्ति क्रमश: कर्म,
उपासना और ज्ञान से होती है। क्योंकि यदि किसी के मकान में धूल पड़ी
होवे तो वह क्रिया (झाड़ई देने) से ही हट सकती है न कि किसी का ध्यान
या विचार करने से। इसी प्रकार विक्षेप रूप मन की चंचलता किसी इष्ट
देव या वस्तु के ध्यान रूप उपासना से ही हट सकती है क्योंकि अत्यन्त
चंचल जन्तुओं के रोकने का उपाय यही होता है कि वे एक ही स्थान में
बाँध दिए जाते हैं। तीसरा आवरण या अज्ञान रूप पर्दा ज्ञान से ही
निवृत्ति हो सकता है क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान का नाशक है। इसीलिए
वेदों या गीता में तीन काण्ड पाये जाते हैं,
कर्म,
उपासना और ज्ञान,
जिनके अनुसार ही सभी दर्शन तीन भागों में विभक्त हैं,
या तो कर्म के प्रतिपादक हैं अथवा उपासना या ज्ञान के।
उनमें से पूर्वमीमांसा दर्शन कर्म का ही प्रतिपादक है और उसी में
उसका पर्यवसान है। न्याय,
वैशेषिक और योग इन तीन दर्शनों का प्रधानत: प्रतिपाद्य विषय उपासना
है। यद्यपि उनमें ज्ञान की भी झलक प्रतीत होती है तथापि वह उनका
उद्देश्य या प्रधान विषय नहीं है किन्तु उपासना के अनुगुण होने से
उपासना ही उनका मुख्य उद्देश्य और प्रतिपाद्य विषय है। इसकी सविस्तर
मीमांसा आगे होगी। सांख्य और वेदान्त इन दोनों का मुख्य विषय अथवा
उद्देश्य ज्ञान मात्र ही है। उनमें से भी सांख्य का ज्ञान आंशिक और
वेदान्त का सर्वांगपूर्ण है। इस स्थान पर इतना और हृदयंगम कर लेना
अच्छा होगा कि यद्यपि न्याय और वैशेषिक दर्शनों का पर्यवसान उपासना
में ही है तथापि योगदर्शन उपासना के अतिरिक्त कुछ ज्ञानपक्ष की भी
सहायता करता है और उससे कुछ ही अंशों में अधिक सहायता ज्ञान की
सांख्य दर्शन करता है अतएव उसका मुख्य विषय ज्ञान ही माना गया है।
तात्पर्य यह है कि वेदान्त दर्शन जिस ज्ञान का प्रतिपादन करता है वह
वही है जैसा कि पूर्व कह चुके हैं कि
'सो
तैं ताहि तोहि नहिं भेदा'
इत्यादि। परन्तु उस वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मज्ञान-जीव ब्रह्म से
वास्तव में पृथक् नहीं है। ऐसे ज्ञान में ब्रह्म और जीव के वास्तव
स्वरूपों के जानने की आवश्यकता है क्योंकि तभी यथार्थ ब्रह्मज्ञान हो
सकता है। जब तक हम दो पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को न जानें तब तक
यह क्योंकर जान सकते हैं कि एक पदार्थ दूसरे का स्वरूप ही है अथवा
उससे पृथक् इसीलिए उस ब्रह्म के शुध्द स्वरूपज्ञान में योग दर्शन
साहाय्य प्रदान करता है और जीव के शुध्द स्वरूपज्ञान में सांख्य
दर्शन। इस विषय में जो विशेषता सांख्य दर्शन की योग दर्शन से है वह
आगे विदित होगी। अब इन दोनों की सहायताओं को पा वेदान्त दर्शन उन
द्वारा रही सही त्रुटियों को हटाकर विशुध्द ब्रह्मज्ञान उत्पन्न कर
देता है जिससे परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की सिध्दि हो जाती है। जैसे
न्याय योगादि दर्शन उपासना द्वारा ज्ञान के सहायक होते हैं वैसे ही
पूवमीमांसा दर्शन उपासना की सहायता द्वारा ज्ञान में परम्परया उपयोगी
होता है। सारांश यह है कि मीमांसा या विचार का प्रारम्भ पूर्वमीमांसा
दर्शन से प्रारम्भ होता है। इसलिए इसे पूर्वमीमांसा कहते हैं और
न्याय,
वैशेषिक,
योग और सांख्य दर्शनों द्वारा पुष्टि को प्राप्त होता हुआ वेदान्त
दर्शन में समाप्त हो जाता है इसी से वेदान्त दर्शन को उत्तर मीमांसा
दर्शन भी कहते हैं जिसका अर्थ यही है कि मीमांसा का अन्त या समाप्ति
इस प्रकार सभी आर्ष (ऋषि प्रणीत) दर्शन एक ही विचार रूप सरणि या
मार्ग में शृंखलाबध्द हैं। अब देखना यह है कि पूर्वमीमांसा दर्शन इस
विचारमार्ग में कहाँ तक और क्योंकर उपयोगी है। यह आस्तिक सिध्दान्त
है कि पूर्वमीमांसा दर्शन विचारमार्ग का प्रथम सोपान है। यह बात इस
दर्शन के सूत्रों और भाष्यों की रचना शैली ही प्रमाणित कर रही है।
यद्यपि न्याय दर्शन प्रभृति के भी सूत्र भाष्यादि रचना में विलक्षण
हैं तथापि इतनी सूक्ष्मता और कठिनतापूर्ण विचित्र लेखनशैली किसी में
भी नहीं पायी जाती है। इस तरह ज्यों-ज्यों जो-जो दर्शन सूत्र या उनके
भाष्यों का निर्माण पीछे होता गया त्यों-त्यों वे सरल होते गये हैं,
यहाँ तक कि वेदान्तदर्शन का भाष्य सबके अन्त में रचे जाने के कारण
प्राय: आधुनिक लेखन प्रणाली से ही लिखा गया है और सांख्य दर्शन
सूत्रों का भाष्य तो बहुत हाल में बना है अत: उसकी भाष्यशैली बिलकुल
ही आधुनिक है। इसमें संशय नहीं है कि महर्षि पाणिनि कृत
व्याकरणसूत्रों की अष्टाध्यायी और उसके भाष्य तो मीमांसा दर्शन से भी
प्राचीन हैं इसीलिए उनकी रचनाशैली और भी विचित्र है। प्राचीन लोगों
की यह रीति थी कि लेख को बहुत ही संक्षिप्त करते थे। अतएव पाणिनीय
सूत्रों में बहुत ही संक्षेप पाया जाता है यहाँ तक कि दूसरे-दूसरे
सूत्रों के ही पद अन्य सूत्रों में मिलकर उनके अर्थ में सहायक होते
हैं। इससे बढ़कर संक्षेप क्या हो सकता है। अतएव वैयाकरणों का यह
सिध्दान्त है कि-
''अर्ध्दमात्रलाघवेन
पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणा:''
जिसका अभिप्राय यह है कि यदि सूत्रों के निर्माण में एक रीति को
अवलम्बन करने से आधी मात्र की भी बचत होवे तो वे लोग उतने ही से
पुत्रजन्म के समान आनन्द मानते हैं। यह भी देखा जाता है कि
मीमांसादर्शन भाष्य में बहुत जगह पाणिनीय सूत्रों अथवा उनके अंशों को
ज्यों का त्यों लिखा है। अत: पाणिनिसूत्र और उनका भाष्य सभी दर्शनों
से प्राचीन है,
इसीलिए जैसे व्याकरण महाभाष्य में जिन गावी,
गोणी,
गोता और गोपोतलिका शब्दों का सर्ंकीत्तान है उन्हीं का मीमांसा दर्शन
में भी परन्तु उस भाष्य में इसकी रचना शैली कुछ सुगम अवश्य है,
अत: वह भी इससे प्राचीन ही है। अस्तु,
चूँकि पूर्वमीमांसा दर्शन विचार का प्रथम सोपान या सीढ़ी है,
और मोक्षमार्ग के लिए यत्न करने में सबसे प्रथम कर्मों की ही
आवश्यकता पड़ती है जैसा कि पूर्व में ही कहा जा चुका है,
इसीलिए पूर्वमीमांसा दर्शन ने कर्मों पर ही विशेष रूप से दबाव डाला।
इस दर्शन के कर्ता महर्षि प्रवर जैमिनि जी का यह दृढ़ विचार था कि
मनुष्य को सबसे पहले कर्मवीर होना चाहिए उसके बाद सभी सिध्दियाँ अथवा
सभी वस्तुएँ उसे प्राप्त हो जाती हैं। इसी से उन्होंने कर्मवीर बनाना
ही अपना मुख्यर् कर्तव्य समझा है। ठीक भी है,
क्योंकि हृदयदर्पण के ऊपर जो सबसे मोटा आवरण या पर्दा राग
द्वेषादिरूप मलों का पड़ा हुआ है तो उस दर्पण से दूसरा काम कैसे हो
सकता है
?
उस बुध्दि से दूसरे सूक्ष्म विचार कैसे हो सकते हैं। इसीलिए
पूर्वमीमांसा दर्शन कर्मकाण्ड कहलाता है। परन्तु चूँकि जब तक मनुष्य
को यह न विदित हो जावे कि जो वस्तु हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति के
लिए अमुक (फलाँ) साधन ही ठीक है न कि दूसरे भी उपाय हैं तब तक वह
नि:संशयरूप से उस यत्न में नहीं लगता। क्योंकि उसे यह संशय लगा रहता
है कि हमारा उपाय झूठा तो नहीं है,
दूसरे उपाय हमारे साधन की अपेक्षा सहज तो नहीं हैं
?
अथवा उनसे शीघ्र फल की प्राप्ति तो न हो जायगी
?
और जब तक संशय बना हुआ है तब तक उचित यत्न किसी भी वस्तु की प्राप्ति
के लिए कैसे हो सकता है
?
अतएव भगवान् श्रीकृष्ण जी ने भी यही कहा है :
नायंलोकोऽस्तिन परो,
न सुखं संशयात्मन: (गीता)।
अर्थात् जिसके चित्त में सन्देह को स्थान मिल गया है उसके न तो ऐहिक
ही कार्य सिध्द हो सकते हैं और न परलौकिक ही क्योंकि संशयाक्रान्त हो
जाने से सभी कार्य छूट सकते हैं। और चूँकि सभी विवेकियों को मोक्ष की
ही आन्तरिक अभिलाषा रहती है,
इसलिए जैमिनि भगवान् ने अपने मीमांसा दर्शन में यही दिखलाया कि मोक्ष
के साधन यदि कोई हैं तो वे कर्म ही हैं। इस प्रकार से उन्होंने
कर्मों पर इतना जोर दिया जिसको कह नहीं सकते। इसलिए उन्होंने उपासना
और ज्ञान दोनों की निन्दा की जिसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि लोग
निस्सन्देह कर्मों में प्रवृत्ता हों,
न कि उनका वास्तव में निन्दा में ही तात्पर्य है। अतएव पूर्वमीमांसा
भाष्यकार शंबर स्वामी ने कई जगह लिखा है कि
'नहिं
निन्दा निन्द्यं निन्दयितुं प्र्रवत्ताते,
किन्तु निन्द्यादितरत्प्रशंसयितुम्'
अर्थात् किसी की निन्दा इसलिए नहीं कि जाती या की गयी है कि वास्तव
में वह वस्तु ऐसी ही है,
बल्कि उस निन्दा का अभिप्राय उस निन्दित पदार्थ से भिन्न अपने अभीष्ट
वस्तु की प्रशंसा में ही होता है। उन्होंने यह समझा कि चाहे जैसे हो
अधिकारी पुरुष को कर्म में प्रवृत्ता कर दो। जब कर्मों के करने से
उसका हृदयदर्पण निर्मल हो जायगा तो उसमें उत्तम,
मध्यम,
कनिष्ठ वस्तुएँ आप ही भान होने लगेंगी-उस पुरुष को यह बिना कहे ही
विदित हो जायगा कि मोक्ष क्या वस्तु है और उसके साधन ज्ञान अथवा
उपासना हैं वा नहीं।
चार्वाक आदि नास्तिकों ने देह अथवा इन्द्रियादि को ही आत्मा मानकर
स्मरण को ही मुक्ति,
सांसारिक विषय सुख को ही स्वर्ग,
दु:ख को ही नर्क और राजा को ही ईश्वर माना था,
या अब तक भी वे मानते ही हैं,
अतएव उनके मत में धर्माधर्म कोई वस्तु नहीं है,
क्योंकि उसके फल सुख और दु:खों को स्वर्ग,
यमलोक या जन्मान्तर में भोगनेवाला कोई जीव मरणान्तर रही नहीं जाता,
जिसे उसका भय अथवा उसी की प्राप्ति की अभिलाषा हो। इसी से उन्होंने
ये सिध्दानत निकाला कि-
''यावज्जीवेत्
सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य,
पुनरागमनं कुत:॥''
अर्थात्
''जब
तक शरीर रहे तब तक आनन्द से रहे और ऋण लाकर भी अच्छी तरह घी,
दूध,
खावे,
क्योंकि मरणोत्तार जब शरीरात्मा का दाह हो जायगा तो फिर संसार में
आना थोड़े ही है जिससे सुख-दु:ख का भय हो।''
इसलिए पूर्वमीमांसा दर्शन ने कर्मवाद चलाया और यह युक्तियों से सिध्द
किया कि धर्म का ही फल सुख और अधर्म का फल दु:ख है,
जिसे अवश्य ही परलोक या जन्मान्तर में भोगना पड़ता है। अत:एव शरीरादि
से भिन्न ही आत्मा को मानना पड़ेगा,
नहीं तो इस शरीर से किये गये धर्माधर्म के फलों को पीछे कौन भोगेगा
?
यदि कर्ममूलक यह सृष्टि न मान कर अकस्मात् ही मान ली जावे तो इसकी
विचित्रता भंग हो जावेगी,
क्योंकि बिना विचित्र कारणों के विचित्र कार्य नहीं होते,
यह भी नहीं देखा गया कि केवल रक्त या श्वेत तन्तुओं से चित्र रंग का
वस्त्र तैयार होता है अथवा बिना भोजन किए ही तृप्ति होती है। यदि
पुनर्जन्म न माना जावे तो कृतहानि और अकृताभ्यांगम रूप दोष भी होगा।
तात्पर्य यह है कि इस शरीर से मरणोपर्यंत जो कुछ किया है उसका बिना
भोग के ही नाश,
और बाल्यावस्था से लेकर ही इस शरीर के सुख-दु:खों की प्राप्ति बिना
कुछ किए ही होगी,
क्योंकि भोगने वाला शरीर तो प्रथम था ही नहीं,
तो अच्छे या बुरे कर्म किसने किए
?
परन्तु ऐसा इस संसार में नहीं देखा जाता है कि जो चोरी न करे उसकी
सजा हो और चोर जान बूझकर छोड़ दिया जावे। यदि सोने के बाद जागना और
जागने के बाद सोना यह संसार का अटल नियम है और मृत्यु भी एक प्रकार
की गहरी निद्रा ही है तो उसके बाद फिर पुनर्जन्म रूप जागरण क्यों न
होगा
?
जो बालक थोड़ा पढ़ता है उसका ज्ञान अल्प होता है अधिक पढ़ने वाले का
अधिक। अर्थात् जिसने जितना ही अधिक अर्जन किया है उसका ज्ञान उतना ही
अधिक होता है,
परन्तु जो जन्म के थोड़े दिन बाद ही बिना पढ़े-लिखे ही विशेष ज्ञानवान
होता है उसने इस शरीर से तो ज्ञानार्जन किया है नहीं,
इसलिए मानना ही पड़ेगा कि दूसरे शरीर में ही उसने यह कमाया था। जन्म
के साथ ही मनुष्य बालक जंगल के पशु या कीड़े जो माता के स्तन पीने लग
जाते और यदि उन्हें कोई मारने चले तो भागने लग जाते हैं इत्यादि,
इससे सिध्द है कि वे जीवन अदृष्ट (धर्माधर्म) के प्रभाव से
जन्मान्तरीय स्तनपान के सुख और मारने के दु:ख को स्मरण करके ही ऐसा
करते हैं,
क्योंकि इस जन्म में तो अब तक उनहोंने ऐसे सुख या दु:ख का अनुभव किया
ही नहीं,
और बिना अनुभव के स्मरण हो नहीं सकता,
क्योंकि बिना जानी बात को याद कौन कर सकता है
?
यदि ऐसा कहा जावे कि जिस माता-पिता से बालक की उत्पत्ति हुई है उसी
के हाथ,
पाँव और मुखादि जैसे बालक के भी हाथ,
पाँव आदि जिस तरह होते हैं न कि,
जन्मान्तर जैसे,
उसी तरह माता-पिता के स्तनपान प्रभृति धर्म भी बालक में प्राकृतिक
नियमानुसार आ जाते हैं,
न कि इनके लिए जन्मान्तर की आवश्यकता है,
तो फिर यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर पण्डितों के बच्चे मूर्ख और
मूर्खों के पण्डित क्यों हुआ करते हैं
?
पिता का पाण्डित्य पुत्र में वैसे ही क्यों नहीं चला आता
?
काले पिता के गोरे पुत्र और गोरे के काले क्यों हुआ करते हैं
?
और अन्धों और बहिरों के बच्चे ऑंख और कान वाले क्यों हुआ करते हैं
?
जिन लोगों का यह कहना है कि कोई बुध्दिमान और कोई निर्बुध्दि कोई धनी
और कोई निर्धन,
कोई मनुष्य और कोई पशु इत्यादि सृष्टि की विचित्रता इसलिए नहीं हुई
कि उन्होंने पूर्वजन्म में विचित्र कर्म (धर्माधर्म) किए थे,
किन्तु पृथ्वी,
जल और वायु आदि के परमाणुओं के विलक्षण-विलक्षण रासायनिक संयोग से
विलक्षण-विलक्षण् वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। जो रासायनिक संयोग से
उत्तम या उससे उत्तम वस्तु बनी,
एवं मध्यम से मध्यम इत्यादि। अत: उसके लिए धर्माधर्मों के मानने की
कोई आवश्यकता नहीं। इसी तरह शरीर से पृथक् जीवात्मा भी कोई वस्तु
नहीं है,
किन्तु जैसे कत्था,
पान और सुपारी आदि के मेल या रासायनिक संयोग से रक्तिमा उत्पन्न हो
जाती,
है,
जो प्रत्येक में नहीं होती। अथवा जैसे महुआ और गुड़ के मेल से मादकता
(नशा) कोयला और कबूतर के पर इत्यादि के संयोग से विद्युत (बिजली)
पैदा हो जाती है इत्यादि,
जो प्रत्येक वस्तुओं में नहीं रहती। उसी प्रकार इन्हीं पूर्वोक्त
पृथिवी आदि के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से ही चेतना पैदा हो जाती
है जिसे जीवात्मा कहते हैं और उन्हीं परमाणुओं के उस रासायनिक संयोग
के बिगड़ जाने से चेतनता नष्ट हो जाती है जिसे मृत्यु कहते हैं।
यदि किसी का यह प्रश्न उन नास्तिकों (चार्वाक आदि) के प्रति होवे तो
फिर जिस विलक्षण संयोग (रासायनिक संयोग) से विलक्षण वे पदार्थ बने वह
रासायनिक संयोग विलक्षण-विलक्षण क्यों हुआ
?
सभी संयोग एक ही प्रकार के क्यों न हो गये
?
इससे उसी विलक्षण के लिए अदृष्ट (धर्माधर्म) रूप कोई कारण अवश्य
मानना होगा। तो इस समस्या को वे लोग इस प्रकार हल करने का यत्न करते
हैं कि यह तो स्वभाव
(Nature)
है जिससे सभी रासायनिक संयोग एक प्रकार के नहीं होते,
और इस स्वभाव के विषय में प्रश्न किया जा नहीं सकता,
क्योंकि अग्नि उष्ण क्यों हुई और जल शीतल क्यों हुआ
?
ऐसे प्रश्न हो ही नहीं सकते। इन्हीं बातों को उन्होंने यों कहा है-
अत्रा चत्वारि भूतानि,
भूमि वार्यनलानिता:।
चतर्श्य:
खलु भूतेभ्यश्चैतन्यमुपाजायते॥1॥
किण्वादिभ्य:
समेतेभ्यो,
द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्।
अहं स्थूल:
कृशोऽस्मीति समानाधिकरण्यत:॥2॥
देह:
स्थोल्यादियोगाच्च स एवात्मा नवापर:।
मम देहोऽय मित्युक्ति:
सम्भववेदौपचारिकी॥3॥
नित्यसत्तवा भवन्त्येके,
नित्यसत्तवाश्च केचन।
विचित्र:
केचिदित्यत्रा,
तत्स्वभावो नियामक:॥4॥
अग्निरुष्णो जलं शीतं,
समस्पर्श स्तकाऽनिल:।
केनेदं रचितं तस्मात् स्वभावात्तद्व्यवस्थति:॥5॥
इसका तात्पर्य वही है जैसा कह चुके हैं,
केवल इतना ही अधिक इसमें है कि उन्होंने देह को ही आत्मा मानने से यह
भी युक्ति दिखलाई है कि जब
'हम
स्थूल हैं,
कृश हैं'
ऐसी प्रतीति हो रही है तो देह से भिन्न आत्मा की सत्ता हो कैसे सकती
है
?
क्योंकि स्थूलता प्रभृति तो शरीर के ही धर्म हैं।
'मेरा
शरीर है'
ऐसी प्रतीति जब कहीं भी होती है तो उससे यह न समझ लेना चाहिए कि जैसे
'मेरा
घर है,'
ऐसा कहने वाला घर से पृथक् है,
वैसे ही
'मेरा
शरीर'
कहने वाला जीव शरीर से भिन्न है,
क्योंकि वह तो प्रतीति ऐसी ही है जैसी राहु का सिर यह प्रतीति।
क्योंकि राहु तो सिर का नाम है ही,
फिर उसका कौन सा सिर हो सकता है
?
परन्तु फिर भी ऐसा व्यवहार होता रहता है,
उसी प्रकार आत्मा तो शरीर रूप ही है,
फिर भी
'शरीरात्मा
का शरीर'
यह व्यवहार होता रहता है,
इससे यह स्पष्ट है कि आत्मा शरीर से अलग कोई वस्तु नहीं है,
किन्तु पूर्वोक्त रीति से चेतना उत्पन्न होने पर उसे ही अथवा वह चेतन
शरीर ही जीवात्मा है।
यहाँ पर नास्तिकों से यह पूछना चाहिए कि जिन विलक्षण विलक्षण
रासायनिक संयोगों से वस्तुओं की विचित्रता हुई वे संयोग बिना कारण ही
विचित्र-विचित्र क्यों हो गये
?
यदि इस प्रश्न को वे लोग स्वभाववाद का अवलम्बन कर टालने का यत्न करें,
तो उन्हें यह कह कर रोकना चाहिए कि यदि आपको आगे चल कर निरुत्तार
होने पर स्वभाववाद का ही आश्रयण करना था तो रासायनिक संयोग तक क्यों
गये
?
चेतनता और विचित्रता को ही स्वाभाविकी क्यों न मान लिया
?
यदि इस चेतनता आदि का आप कारण ढूँढ़ते और मानते हैं,
तो फिर इसी प्रकार आपको इसके कारण विलक्षण रासायनिक संयोग का भी कारण
बलात् मानना ही पड़ेगा। यदि प्रथम से ही अथवा आगे चलकर ही आपके इस
स्वभाव रूप समाधान को मानें तो भी उसका तात्पर्य यही हो सकता है कि
आप यथावत् उत्तर नहीं दे सकते। अर्थात्
'हम
नहीं जानते'
इसी बात को
'स्वभाव
से ही'
इस शब्दान्तर से कहते हैं। क्योंकि यदि आपका स्वभाववाद रूप निर्मूल
समाधान (उत्तर) सत्य और उचित मान लिया जावे तो बड़ी-बड़ी लीलाएँ
दृष्टिगोचर होंगी,
क्योंकि जो बात आप कहते हैं उससे विरुध्द पक्ष को ही यदि कोई आस्तिक
सिध्द करना चाहेगा तो कुछ देर तक आपका उत्तर देता रहेगा और जहाँ पर
उसे उत्तर न आवेगा वहीं
'स्वभाव
से ही'
ऐसा कह बैठेगा,
जिससे आपको पराजय मानना ही होगा। साथ ही इस प्रकार का स्वभाववाद लेकर
इस संसार में सभी बातें सत्य ही सिध्द की जा सकती हैं। इसलिए आपको
स्वयं ही अवश्य स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार
'स्वभाव
से ही'
यह उत्तर उचित नहीं है किन्तु इसका तात्पर्य यही है कि
'हम
नहीं जानते।'
जो अग्नि और जल का दृष्टान्त देकर आप स्वभाववाद का अवलम्बन करते हैं
वह भी ठीक नहीं है,
क्योंकि वैसे ही दृष्टान्त आपसे विपरीतवादी को भी मिल सकते हैं।
दूसरी और सत्य बात तो यह है कि स्वभाव उसका नाम है जिसे सभी लोग
प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हों और जिसमें किसी को विवाद न हो,
जैसे जल की शीतता अथवा अग्नि की उष्णता को सभी लोग प्रत्यक्ष ही
जानते हैं और इनमें किसी को भी विवाद नहीं है। अत: ये उष्णता आदि
स्वभाव कहे जाते हैं। परन्तु भूतों या परमाणुओं
(Atoms)
की चेतनता और रासायनिक संयोग की विलक्षणता में तो विवाद भी है और वे
प्रत्यक्ष भी नहीं हैं,
क्योंकि चेतनता
मात्र
का प्रत्यक्ष है न कि वह चेतनता परमाणुओं में ही है,
ऐसा भी प्रत्यक्ष है,
क्योंकि यदि ऐसा होता तो अग्नि की उष्णता की तरह उसमें विवाद ही नहीं
होता। और जैसे सभी अग्नि उष्ण ही देखी जाती है वैसे सब परमाणु चेतन
नहीं देखे जाते, क्योंकि मिट्टी का ढेला
जड़ ही होता है इत्यादि, इसी से उसमें
विवाद है। और रासायनिक संयोग तो बिलकुल ही अप्रत्यक्ष है,
इसीलिए उसके स्वरूप और कारणता दोनों में ही विवाद
है, ऐसी दशा में अग्नि के औष्ण्य की तरह
वहाँ भी स्वभाव मान कर समाधान
नहीं किया जा सकता,
प्रत्युत ऐसा नितान्त भ्रम है।
और जो दृष्टान्त मदिरा की मादकता अथवा पान की रक्तिमा का दिया गया है
वह प्रकृत में असंगत है,
क्योंकि वहाँ तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि रासायनिक संयोग से ही
मादकता उत्पन्न होती है और रक्तिमा भी वैसे ही देखी जाती है। परन्तु
चेतनता भी परमाणु संयोग से ही उत्पन्न होती है यह बात तो कहीं भी
प्रत्यक्ष नहीं है। अत: कहना पड़ेगा कि उसी मदिरादि के दृष्टान्त से
यह अनुमान किया जाता है कि चेतनता भी रासायनिक संयोग से ही उत्पन्न
होती है,
परन्तु यह वार्ता भी असंगत है,
क्योंकि दृष्टान्त मात्र से ही अनुमान नहीं होता,
अन्यथा संसार में सभी वस्तुओं का अनुमान सुगमता से हो सकता है,
क्योंकि दृष्टान्त मात्र सर्वत्र ही सुलभहै।
इसीलिए भगवान् कात्यायन ने न्याय दर्शन भाष्य में कहा है कि-
''नहिं
दृष्टान्तमात्रमप्रतिसंहितंकिञ्चित्करं।
दृष्टान्तवत्प्रतिदृष्टान्तस्यापि संभवात्॥''
अर्थात् बिना किसी विशेष हेतु के कोई वस्तु दृष्टान्त मात्र से सिध्द
नहीं हो सकती,
क्योंकि उस दृष्टानत के विपरीत भी दृष्टान्त मिल सकते हैं जिनसे उस
वस्तु का उलटा भी सिध्द किया जा सकता है। अत: आपको विलक्षण रासायनिक
संयोग से चेतनता की उत्पत्ति सिध्द करने के लिए कोई विशेष हेतु देना
होगा,
जिसमें पूर्वोक्त मदिरा वाली बात दृष्टान्त बनेगी। परन्तु स्मरण रहे
कि अनुमान करने के लिए जो हेतु कहा जाता है उसका और जो वस्तु सिध्द
की जावेगी इन दोनों की व्याप्ति होती है,
जिसे अंग्रेजी वाले नियम
'ला'
(Law)
कहते हैं,
जिसका तात्पर्य यह है कि जब कहीं दूर से केवल
धुएँ
को देखकर वहाँ अग्नि का अनुमान करते हैं तो उस अनुमान से प्रथम ही यह
निर्णात रहता है कि जहाँ
धुऑं
रहता है वहाँ अग्नि भी अवश्य रहती है,
जैसा कि रसोई के घर वगैरह में देखा जाता है। इसी
नियम को व्याप्ति कहते हैं, जिसमें रसोई
का घर दृष्टान्त है; इसीलिए
धुऑं
रूप हेतु उस जगह अग्नि का ठीक-ठीक अनुमान करवा सकता है। इसी तरह
प्रकृत में भी रासायनिक संयोग से होनेवाली चेतनता और उस हेतु की
व्याप्ति होनी चाहिए जिसका प्रयोग उस चेतनता का अनुमान करवाने के लिए
किया जावेगा। परन्तु स्मरण रहे कि यह नियम
(Law)
वा व्याप्ति दो प्रकार की होती है,
जिनमें से किसी के भी रहने से साधनीय
वस्तु की सिध्दि उस हेतु से हो सकती है,
अन्यथा नहीं।
एक तो व्याप्ति ऐसी होती है कि जिस वस्तु को हमें सिध्द करना है उसी
के साथ हेतु की व्याप्ति अन्यत्र निर्णीत हो। जैसे जिस धूम से हमें
कहीं अग्नि सिध्द करनी है उसी अग्नि के साथ उस धूम की व्याप्ति
(Law)
अन्यत्र पाकशाला आदि में निश्चित रहती है। परन्तु इस प्रकार की
व्याप्ति प्रकृत में नहीं हो सकती,
क्योंकि जैसे अग्नि अन्यत्र प्रत्यक्ष ही
निर्विवाद देखी जाती है और वही व्याप्ति का निश्चय होता है,
वैसे विलक्षण रासायनिक संयोग से चेतनता की उत्पत्ति
कहीं भी प्रत्यक्ष देखी नहीं जाती जहाँ हेतु के साथ उसकी व्याप्ति का
निश्चय हो। क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर विवाद ही नहीं होता और सभी
लोग चेतनता को रासायनिक संयोगों से ही उत्पन्न करने लग जाते,
जिससे इस संसार से यमराज या मृत्यु का काम ही उठ
जाता और मृत्युलोक भी देवलोकवत् अमरलोक हो जाता।
दूसरी व्याप्ति यह है कि यद्यपि जिस वस्तु को हमें कहीं सिध्द करना
है उसका प्रत्यक्ष कहीं न भी हुआ हो तथापि उसी ढंग की अन्य वस्तुओं
का प्रत्यक्ष होने से हेतु के साथ व्याप्ति निर्णीत हो जाने पर भी
प्रकृत में उसी हेतु से साध्य पदार्थ की सिध्दि हो जाती है। जैसे
यद्यपि चक्षुरादि इन्द्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण से किसी ने भी नहीं
देखा है,
क्योंकि इन्द्रियों के स्थान (गोलक) ऑंखों दीखते हैं वे तो इन्द्रिय
स्वरूप हैं नहीं,
अन्यथा उनके बने रहने पर भी जो कभी-कभी उन-उन इन्द्रियों से
किसी-किसी मनुष्य को विषयों का ज्ञान नहीं होता है वह क्योंकर हो
सकता है
?
और इन्द्रियों एवं विषय का सम्बोधन होने पर ही ज्ञान होता है,
नहीं तो दीवार के पीछेवाले पदार्थ भी ऑंखों दीखते। परन्तु वे
इन्द्रियों के स्थान वा गोलक तो अपनी जगह से हट सकते नहीं और न दूर
के पदार्थ ही पास में चले आते हैं। अत: यह निर्विवाद सिध्द है कि उन
गोलकों से इन्द्रियाँ भिन्न-भिन्न हैं,
जो सूर्य की किरणों की तरह दूर-दूर के पदार्थों तक भी शीघ्र ही पहुँच
जाती हैं। इसलिए यह बात सत्य है कि इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष प्रमाणों से
देखी नहीं जातीं। तथापि यह देखा जाता है कि जितनी क्रियाएँ होती हैं
वे किसी न किसी कारण से अवश्य ही उत्पन्न होती हैं,
क्योंकि कारण का स्वरूप ही ऐसा है जैसा कि भर्तृहरि जी ने अपनी
व्याकरण महाभाष्य की कारिकाओं में लिखा है कि-
''क्रियाया:
परिनिष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरम्।
विवक्ष्यते यदा यत्रा,
करणं तत्तदा
मतम्॥''
अर्थात् जिस वस्तु के व्यापार के अनन्तर ही क्रिया की उत्पत्ति होती
है उसे ही करण कहते हैं। यह बात छेदन आदि क्रियाओं में प्रत्यक्ष ही
है कि जब तक लोहार अपना बसूला नहीं चलाता,
तब तक छेदन क्रिया नहीं होती,
परन्तु जभी उसका बसूला छूटता है तभी छेदन हो जाता है। इसलिए बसूला
रूप करण से ही छेदन क्रिया की उत्पत्ति होती है,
इसी तरह अन्य क्रियाओं में भी कोई न कोई करण अवश्य ही उनका उत्पादक
रहा करता है। इस प्रकार करण के साथ क्रिया की व्याप्ति निश्चित कर,
चूँकि ज्ञान भी एक प्रकार की क्रिया ही है,
अत: उसके भी करण अवश्य होने चाहिए और चूँकि बसूला वगैरह बाहरी करणों
का तो वहाँ सम्भव नहीं है,
इसलिए आन्तरिक करण ही सिध्द होते हैं,
जिन्हें इन्द्रिय कहा करते हैं। इसी तरह प्रकृत में भी यद्यपि
जहाँ-जहाँ चेतनता उत्पन्न होती वह सभी विलक्षण रासायनिक संयोग से ही
होती है यह व्याप्ति
(Law)
निश्चित नहीं है,
तथापि इस प्रकार की व्याप्ति हो सकती है कि इस
संसार में जितनी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं उनके कारण अवश्य ही हुआ
करते हैं जैसे घट का कारण कुलाल (कुम्हार),
मदिरा की मादकता का रासायनिक संयोग या वृक्ष का
बीज। और चूँकि चेतनता भी उत्पन्न होने वाली वस्तु है,
इसलिए उसका भी कोई कारण अवश्य होगा। परन्तु चूँकि
दूसरे बाहरी तो वहाँ हो नहीं सकते, इसलिए
जैसा मदिरा की मादकता का कारण रासायनिक संयोग है,
वैसा ही प्रकृत में भी चेतनता का कारण रासायनिक
संयोग ही होगा। इस तरह से विलक्षण रासायनिक संयोग सिध्द करने के लिए
अनुमान का स्वरूप खड़ा किया जा सकता है। परन्तु यह भी ठीक नहीं है,
क्योंकि यद्यपि बाहरी
कारणवहाँ
नहीं है तथापि
धर्माधर्म
या अन्य कारणों को जो वहाँ ही विद्यमान हैं,
न मानकर आपके संयोग को ही क्यों कारण मानेंगे
? इसमें कोई विशेषता तो है ही नहीं जिससे अन्यों
का अनादर किया जावे।
दूसरी बात यह है कि जब व्याप्ति वा नियम
(Law)
ठीक रहता है तभी अनुमान भी ठीक होता है। जैसे जहाँ
धुऑं
रहता है वहाँ अग्नि भी अवश्य रहती है यह नियम सत्य है,
इसी से कहीं दूर से भी
धुएँ
को देख अग्नि का अनुमान करना ठीक होता है। परन्तु जहाँ अग्नि रहती है
वहाँ
धुऑं
अवश्य रहता है यह विपरीत नियम ठीक नहीं है,
क्योंकि अंगार में अग्नि रहते हुए भी
धुऑं
नहीं रहता। इसीलिए अग्नि को कहीं देखकर उसमें
धुएँ
का अनुमान करना ठीक नहीं हो सकता। उसी तरह यदि प्रकृत
में
यह नियम होता कि जितने कार्य होते हैं वे रासायनिक संयोग से ही बनते
हैं,
तो चेतनता का कारण भी रासायनिक संयोग ही माना
जाता। परन्तु यह बात तो है नहीं, क्योंकि
घट, पट वगैरह कार्यों की उत्पत्ति
तो रासायनिक संयोग से होती ही नहीं,
ऐसी दशा में आपका नियम कहाँ ठीक ठहरा ?
यदि थोड़ी देर के लिए यह स्वीकार भी कर लें कि
जितने घट, पट आदि कार्य उत्पन्न होते हैं
वे रासायनिक संयोग से ही होते हैं, हाँ वे
संयोग विलक्षण-विलक्षण हैं यह दूसरी बात है। तो हम आपसे पूछते हैं कि
आपको कुछ न कुछ केवल मूल पदार्थ भी तो मानने पड़ेंगे जिनके मेल या
संयोग से रासायनिक पदार्थों की उत्पत्ति,
जैसे जब गुड़ और महुआ मूल पदार्थ हैं तभी तो उनके
मेल से मादकता (नशा) पैदा होती हैं। इसीलिए यद्यपि काले या हरे
इत्यादि रंग रासायनिक संयोग से बनते हैं तथापि उनके कारण स्वरूप लाल
या पीले वगैरह दो एक रंग तो वैज्ञानिकों द्वारा अवश्य ही ऐसे माने
गये हैं जो किसी के मेल या रासायनिक संयोग से न बनकर स्वयमेव अपने
लाल या पीले कारणों से ही बनते हैं। और यदि आप मूल (Original)
पदार्थ कोई मानेंगे ही नहीं तो उसके बिना आपका रसायन भी कैसे सिध्द
होगा। अत: रासायनिक संयोग के कारण स्वरूप पदार्थ तो आपको ऐसे मानने
ही पड़ेंगे जो रासायनिक संयोग से नहीं बनते। ऐसी दशा में आपका यह नियम
व्याप्ति
(Law)
कहाँ रहा कि सभी पदार्थ रासायनिक संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। और
जब नियम ही न रहा तो चेतनता का कारण रासायनिक संयोग सिध्द क्योंकर हो
सकता है
? क्या अग्नि देखकर भी
धुऑं
सिध्द किया जाता है
?
यदि रासायनिक संयोगों से ही पदार्थों की विलक्षणता और चेतनता की
उत्पत्ति होती रहती तो फिर,
जिस तरह पान,
सुपारी और कत्था वगैरह सभी के मेल से जो रक्तिमा उत्पन्न होती है वह
उनमें से किसी एक के भी न रहने से नहीं होती। अथवा महुआ और गुड़ दोनों
में से एक के न रहने से जैसे,
मादकता की उत्पत्ति नहीं होती है,
उसी तरह जिस प्राणी के हाथ-पाँव आदि अंगों में से एक भी टूटे या कट
जाय उसे तत्काल चेतनताहीन अर्थात् मृतक हो जाना चाहिए।
यदि वे लोग इस कठिन समस्या के हल करने का साहस यों करें कि,
यद्यपि रासायनिक वस्तुओं के कारण जितने पदार्थ हैं उनमें से किसी की
भी कमी होने से उस रासायनिक पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती या उसका
नाश हो जाता है,
तथापि उन सभी पदार्थों को रासायनिक रीति से संयुक्त करके उस वस्तु की
उत्पत्ति होने के पश्चात् उन सम्मिलित पदार्थों के कुछ संयुक्त अंश
के हटा देने पर भी जिस प्रकार रासायनिक पदार्थ बना रहता है। क्योंकि
चार बीड़ा पान के साथ सभी चूना और कत्था प्रभृति को मिलाने पर जब
उसमें रक्तिमा पैदा हो जाती है तो पुन: एक बीड़ा पान और उसी के अनुगुण
चूना वगैरह इन सभी मिश्रित पदार्थों यानी सम्पूर्ण पदार्थ के
चतुर्थांश को विभक्त करने पर भी अवशिष्ट तीन अंशों में लालिमा बनी ही
रहती है। वैसे ही यदि किसी प्राणी का कोई अंग कट जाता है तो उससे
रासायनिक संयोग के आधार किसी एक ही वस्तु की कमी न होकर सम्मिलित
द्रव्यों (वस्तुओं) की ही न्यूनता हो जाती है। इसी से चेतनता
पूर्ववत् ही बनी रह जाती है।
तो इस पर उन लोगों से यह कहा जा सकता है कि तो फिर गला वगैरह अंगों
के कट जाने पर मनुष्य को चेतन या जीता ही रहना चाहिए। अथवा जैसे
रासायनिक संयोग के आधार सम्मिलित द्रव्यों का जो अंश पृथक् किया जाता
है उसमें भी रक्तिमा आदि रासायनिक पदार्थ रहते हैं उसी तरह धड़ से अलग
हो जाने वाले हाथ,
पाँव और मस्तक में भी अवश्य ही चेतनता रहनी चाहिए और कटे हुए सिर को
भी बोलना चाहिए।
साथ ही उन लोगों को यह भी विचारना चाहिए कि जब रासायनिक संयोग के
आधार स्वरूप सम्मिलित वस्तुओं में से कुछ अंश विभक्त कर देते हैं तो
सम्पूर्ण मिश्रित द्रव्यों के रहने से जितना परिमाण उस रासायनिक
पदार्थ का रहता है उतना नहीं रह जाता है,
किन्तु यदि चतुर्थांश द्रव्य अलग कर दिया जावेगा तो रासायनिक वस्तु
भी चतुर्थांश जाती रहेगी। इसी तरह आधा निकाल देने से आधी इत्यादि।
यदि चेतनता भी रासायनिक संयोगों से ही बनी रहती तो हाथ,
पाँव आदि दो चार अंगों के कट जाने पर जीवों में वह आधी ही अथवा उसी
हिसाब से ही रह जाती। परन्तु देखा जाता है कि ऐसे-ऐसे पंगु वगैरह हैं
जिनकी दोनों जाँघें वगैरह काट दी गयी हैं,
लेकिन यदि जीते हैं तो उनकी चेतनता प्रथम से कुछ भी न्यून नहीं हुई
है।
एक बात यह भी है कि जिन पदार्थों के सम्मिश्रण से रासायनिक द्रव्यों
की उत्पत्ति होती है वे जब एक दूसरे से बिलकुल ही अलग कर दिये जावें
तभी उस द्रव्य का नाश होता है न कि उनके कुछ अंशों के मिले और कुछ के
अलग रहने से। जैसे आक्सिजन और हाइड्रोजन
(Hydrozon)
स्वरूप जिन दो वायुओं के मेल से जल उत्पन्न होता है उनको सर्वात्मना
एक-दूसरे से पृथक् कर देने पर ही उस जल का नाश हो जाता है न कि उनके
कुछ अंश मिले भी रहते हैं। इसी तरह अन्य रासायनिक वस्तुओं में देखा
जाता है। तद्वत् प्रकृत में मरणकाल में सर्वशरीरव्यापिनी चेतना का
कारण जो सर्वांगवत्तर्ी रासायनिक संयोग है उसका नाशक कौन है
? गला काट लेने या एक वाण के किसी अंग में लग
जाने से जो प्राणी ज्ञानशून्य हो जाता है उसके सम्पूर्ण अंग
प्रत्यंगों से चेतनता का वियोग कराने वाली कौन सी वस्तु है इसको वे
लोग
क्योंकर
बतला सकते हैं
? इत्यादि
सहर्षों
दूषण इस रासायनिक संयोगवाद में दिये जा सकते हैं।
इससे निर्विवाद रूप से यह स्वीकार करना होगा कि रासायनिक संयोग से
चेतनता की उत्पत्ति और वस्तुओं की विलक्षणता नहीं होती या हो सकती है,
किन्तु चेतन जीवात्मा नित्य है और मनुष्य शरीर से धर्माधर्म का अर्जन
करता हुआ ज्ञान आदि का भी संग्रह करता है। जिन धर्माधर्मों के होने
से ही सृष्टि की विचित्रता होती है। अर्थात् कोई निर्धन कोई धनी एवं
सुखी,
दु:खी बुध्दिमान् और मूर्ख हुआ करते हैं।
इसी तरह आर्हत (जैन) मतानुयायियों ने जो सिध्दान्त स्थिर किया है कि
यद्यपि रासायनिक संयोग से जीवात्मा अथवा चेतना की उत्पत्ति नहीं है,
तथापि जैसा मीमांसकों ने जीव को विभु (व्यापक) और भगवान् रामानुज या
बौधायन प्रभृति के अनुयायियों ने परमाणु स्वरूप माना है,
वैसा वह नहीं है,
किन्तु जिस शरीर में वह रहता है उतना ही बड़ा होता है। अर्थात् चींटी
के शरीर में चींटी जैसा और हाथी के शरीर में उसी जैसा। इसी को मध्यम
परिमाण वाला भी कहते हैं। क्योंकि यदि उसे व्यापक मान लेवें तो शरीर
से बाहर भी दीवार वगैरह में सभी जीवों को सुख-दु:ख का अनुभव होना
चाहिए। और देवदत्ता आदि सभी की आत्माएँ व्यापक हैं तो एक ही शरीर में
सबके विद्यमान रहने से एक के दु:ख,
सुखादि को सभी अनुभव क्यों नहीं करते
?
इस दूषण के उध्दार के लिए यदि जीवात्मा को परमाणु स्वरूप मान लेवें
तो फिर शरीर में सिर प्रभृति किसी एक स्थान में चन्दन लगाने या चोट
लगने से सम्पूर्ण शरीर में शैत्य अथवा व्यथा का अनुभव न होना चाहिए,
क्योंकि अनुभव करनेवाला तो शरीर के किसी एक ही कोने में रहेगा। हाँ,
यदि उसे शरीर जितना ही बड़ा मान लेवें तो पूर्वोक्त कोई भी दूषणों का
अवकाश नहीं है। यदि यह कहा जावे कि जब शरीर के बराबर वह है तो फिर
हाथी के मरने पर वह जीव यदि चींटी का शरीर पावे तो उसमें क्योंकर समा
सकता है
?
अथवा चींटी के शरीर से हाथी के शरीर में जाने पर क्योंकर उतना बड़ा हो
सकता है
?
तो वे लोग कहते हैं कि जैसे दीपक छोटे स्थान में रहने से उतनी ही दूर
में प्रकाश करता और बड़े स्थान में फैल जाता है ठीक वही दशा जीवात्मा
की है। वह भी प्रकाशस्वरूप होने से स्थानानुसार संकोच और विकासशील
होती है।
परन्तु उन लोगों का यह सिध्दान्त भी उचित नहीं है। यदि आत्मा को
संकोच और विकासशील अथवा मध्यम परिमाण वाला मानेंगे तो फिर वह विनाशी
हो जायगा। क्योंकि संसार में जितने भी ऐसे पदार्थ दीपक या घट,
पट आदि हैं सभी विनाशशील ही देखे जाते हैं। और जब उसे आप आगमापायी
स्वीकार कर लेंगे तो फिर वही पूर्व वाले कृतहान और अकृताभ्यागम,
एवं सृष्टि वैचित्रय-भंग आदि रूप सहर्षों
दोष होंगे। साथ ही जिसका नाश होता है उसकी उत्पत्ति
भी इस जगत् में देखी जाती है। अत: आपको भी उसकी उत्पत्ति
माननी पड़ेगी। परन्तु उत्पत्ति
मानने में तो पूर्वोक्त रासायनिक संयोगवाद वाले सभी दूषण आपके मत्थे
पड़ेंगे।
यदि आप वह कहें कि हम तो किसी भी वस्तु का अत्यन्त नाश नहीं मानते,
किन्तु संसार के सभी पदार्थ केवल परिणामी हैं। अर्थात् जैसे घड़े का
सर्वात्मना नाश न होकर उसका कपाल या चूर्ण रूप रूपान्तर ही हो जाता
है। एवं कपड़े का तन्तु रूप इत्यादि,
इसी तरह जीवात्मा का भी यदि नाश होगा तो सर्वात्मना (अत्यन्त) न होकर
केवल उसका भी रूपान्तर हो जायगा। एतावता पूर्वोक्त कोई भी दूषण नहीं
लग सकते,
क्योंकि हम यदि उसका अत्यन्त अभाव व नाश मानते तो पुन: उसकी उत्पत्ति
आदि की आवश्यकता होती।
परन्तु यह भी कथन निस्सार है,
क्योंकि रूपान्तर मान लेने से भी आपका काम न चल सकेगा और पूर्वोक्त
दूषण सहò
आपके सिर पड़ेंगे ही। कारण कि जिस कपड़े या घड़े का रूपान्तर हो जाता है
उसी की उत्पत्ति
देखी जाती है,
तो फिर इस तरह आत्मा की उत्पत्ति
को आप क्योंकर हटा सकेंगे
? दूसरी बात यह है कि जब
वस्त्र
या घट का रूपान्तर उसके नाश होने पर हो जाता है तो जो काम उससे प्रथम
पहनना या पानी लाना वगैरह होते थे वे अब नहीं हो सकते। इसीलिए उन
कामों के लिए दूसरे घड़ों वा कपड़ों की आवश्यकता होती है। अथवा उस घट
में जो पदार्थ रहता है उसके फूल जाने या रूपान्तर हो जाने पर वह
उसमें नहीं रह सकता। सारांश यह कि प्रथम के होने वाले कोई भी काम
उससे अब नहीं हो सकते। उसी तरह जब जीवात्मा का नाश या रूपान्तर हो
जावेगा तो फिर वह शरीर वा इन्द्रियों का प्रकाश नहीं कर सकता।
अर्थात् उसके रहने से शरीर में जो चेतनता रहती थी अथवा सुख-दु:खादि
के ज्ञान होते थे वे अब न हो सकेंगे और उनके लिए दूसरे जीवात्मा की
आवश्यकता अनिवार्य होगी। और उसमें जो प्रथम ज्ञानों के संस्कार या
धर्माधर्मादि
थे वे भी न रह सकेंगे और न वे अपने काम ही कर सकेंगे। क्योंकि जब जल
का हाइड्रोजन और ऑक्सिजन स्वरूप रूपान्तर हो जाता है तो उससे कपड़े
गीले नहीं हो सकते। फल इसका यह होगा कि पूर्व देखी,
सुनी वस्तुओं के स्मरण न हो सकेंगे और न सृष्टि की विचित्रता
ही हो सकेगी और पूर्व के कृतहान आदि भी गले में मढ़ दिये जावेंगे।
एक बात और भी विचारने की है कि यदि आप जीवात्मा को दीपक के प्रकाश की
तरह संकोच और विकासशाली मानेंगे तो वहाँ कुछ विपरीत ही बात होगी।
क्योंकि यह देखा जाता है कि यदि दीपक का प्रकाश अधिक स्थान में फैल
जाता है तो वह सम्पूर्ण स्थान में एक सा न होकर कहीं अधिक,
कहीं मन्द प्रतीत होता है। इसी तरह यदि आत्मा भी दीपक के प्रकाश सदृश
ही माना जावे तो यदि वह हाथी के शरीर में रहे तो उसके सर्वांगों में
उतनी चेतनता प्रतीत नहीं होनी चाहिए किन्तु अल्प ही। परन्तु जब वही
चींटी के शरीर में प्रवेश करता है तो उस शरीर में चेतनता वा ज्ञान
हाथी के शरीर की अपेक्षा लाख या करोड़ गुना होने चाहिए। परन्तु यहाँ
तो विपरीत ही देखा जाता है कि चींटी की अपेक्षा हाथी या मनुष्य शरीर
में ही अधिक चेतना ज्ञान वा विवेक होता है।
यह भी स्मरण रहे कि यदि आत्मा को घट घटादि की तरह मध्यम परिणाम वाला
मानेंगे तो उसे बलात् सावयव (अवयव वाला) स्वीकार करना होगा। क्योंकि
जो ही वस्तु मध्यम परिणाम वाली होती है वही सावयव होती है। यदि वे
लोग इसे भी मान लेवें तो फिर यह प्रश्न होगा कि जब वह सावयव है तो
उसके प्रत्येक अवयवों में भिन्न-भिन्न चेतनता होती है अथवा अवयवों के
समुदाय में ही
?
प्रथम पक्ष में जितने अवयव होंगे उतने ही चेतन वा जीवात्माएँ उस शरीर
में होंगी। फल यह होगा कि जब दो एक की सम्मति सर्वदा एक सी नहीं रहती,
किन्तु कभी-कभी झगड़े या विवाद होकर वे मनमाना काम करने लग जाते हैं,
तो फिर सहर्षों
रहेंगे वहाँ कब एक सी सम्मति होने की
? परिणाम यह होगा कि किसी भी कार्य में एक यदि
शरीर को पूर्व की ओर खींचेगा तो दूसरा पश्चिम,
तीसरा
उत्तर
और चौथा दक्षिण की ओर। और जैसे दो पत्नी वाला पति दोनों तरफ खींचा
जाकर बीच में उसी जगह मर जाता है उसी तरह शरीर की भी किसी ओर प्रवृत्ति
न होगी और एक ही जगह उसकी धज्जियाँ उड़ जावेंगी। यदि इस दोष की निवृत्ति
के लिए अवयवों के समुदाय में ही केवल एक ही चेतनता मानी जावे तो फिर
कर चरणादि किसी भी अंग के कट जाने पर उतने दूर के जीव के अवयवों के
नष्ट हो जाने से वह पूर्व वाला अवयव समुदाय न रह गया,
इससे लूले या लंगड़े मनुष्य को मर जाना चाहिए।
क्योंकि जिस समुदाय में चेतनता रह सकती है वह तो समुदाय है ही नहीं।
निराश्रय वस्तु क्योंकर रह सकती है ?
इत्यादि अनेकों दूषण आर्हत (जैन) मतानुयायियों के भी मत में हैं।
अत: निर्भ्रान्त सिध्द हो गया कि जीवात्मा शरीर परिमाण वाला नहीं है,
किन्तु व्यापक ही है। तो भी जिस आत्मा का मन जहाँ रहता है वहीं उसको
सुख-दु:ख का अनुभव होता है और वह मन प्रत्येक जीव के अपने-अपने शरीर
में ही रहता है। इसलिए आत्मा के व्यापक होने पर भी शरीर से बाहर अथवा
अन्य के सुख-दु:खों का अनुभव अन्य को नहीं हो सकता।
इसलिए मीमांसकों ने यही निश्चय किया कि व्यापक और अनादि जीवात्मा ही
धर्माधर्म का आश्रय है और उन्हीं धर्माधर्मों के बल से सृष्टि प्रलय
और विचित्रताएँ हुआ करती हैं और चूँकि वह जीव अनादि है इसलिए उसके
आश्रित होकर रहने वाले धर्माधर्म भी अनादि हैं। इससे यह शंका भी
निर्मूल हो गयी कि यद्यपि जगत् के कारण धर्माधर्म हैं,
तथापि सृष्टि के प्रारम्भ में तो वे थे ही नहीं तो उस समय जैसे
स्वभाव से ही विचित्र सृष्टि हुई,
वैसे ही आजकल भी हो सकती है। क्योंकि जब हम धर्माधर्म के प्रवाह को
और साथ ही सृष्टि प्रवाह को भी अनादि मानते हैं तो किसी भी सृष्टि का
आदि काल कोई हो ही नहीं सकता। जो सृष्टि हुई उसके कारण उससे प्रथम
सृष्टि के धर्माधर्म और उसके भी उससे पूर्व के इत्यादि रूप ही सृष्टि
परम्परा और धर्माधर्म का प्रवाह वैसी ही है जैसी वृक्ष और बीज की
परम्परा या प्रवाह। क्योंकि वहाँ भी यह प्रश्न नहीं हो सकता कि प्रथम
बीज था या वृक्ष,
अथवा सबसे प्रथम वृक्ष कैसे हुआ
?
क्योंकि वहाँ बीज था ही नहीं। इसी बात को भगवान् व्यास जी ने
वेदान्तदर्शन में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि-
''वैषम्य
नैघृण्ये इति चेन्न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति।
न कर्माविभागादिति चेन्नादित्वात्॥शा.211।35-35॥
इन दोनों सूत्रों का तात्पर्य वही है जैसा कि अभी दिखलाया गया है।
हाँ पूर्व सूत्र के अर्थ में कुछ पूर्वोक्त विषय से अधिक भी है,
जिसका मर्म यह है।
जिन ईसाइयों,
मुसलमानों,
या अन्यमतवादियों ने यह माना है कि यह वर्तमान सृष्टि ही सबसे प्रथम
और अन्त की भी है। न तो इससे पूर्व कोई भी सृष्टि थी,
और न आगे (प्रलयानन्तर) दूसरी होगी भी। अकस्मात् ही ईश्वर ने अपने ही
मन से एक बार ऐसी रचना कर दी है जिसमें लोग उसकी पूजा किया करें।
किसी को निर्धन तो किसी को धनसम्पन्न एवं मूर्ख और बुध्दिमान्,
मनुष्य,
पशु,
कुत्तो,
शूकर इत्यादि जीव योनियों को विचित्र विचित्र बनाने में केवल उसकी
इच्छा ही कारण है। वह सर्वशक्तिमान है,
अत: उसने जैसा चाहा बना दिया। साथ ही बिना भिन्न-भिन्न प्रकार की
सृष्टि के उसका काम भी नहीं चल सकता। सभी अमीर हो जावें तो उनकी सेवा
कौन करेगा
?
इत्यादि।
उन लोगों का यह सिध्दान्त अफीमची की पिनक सा है। क्योंकि यह बात
सविस्तार सिध्द की जा चुकी है कि बिना कारण अकस्मात् कोई भी वस्तु बन
नहीं सकती। इसके अतिरिक्त यदि ईश्वर ने अपनी पूजा के ही लिए सृष्टि
रची है,
वह भी अपनी इच्छा के ही अनुसार,
तो कहना होगा कि वह आपका ईश्वर,
ईश्वर नहीं,
किन्तु कोई हम लोगों जैसा साधारण,
लोभी,
प्रमादी,
अन्यायी,
निर्दयी और स्वेच्छाचारी मनुष्य है,
क्योंकि ईश्वर शब्द का वास्तविक और पवित्र अर्थ है आप्तकाम,
न्यायकर्ता और सृष्टि का संरक्षण एवं शासन कर्ता। परन्तु यदि उसे
अपनी ही पूजा की चिन्ता रहती है और देखा करता है कि कौन मेरी पूजा
करता है
?
तो क्या वह स्वार्थी और घूसखोर न हुआ
?
यदि उसने मनमाने किसी को धनी,
किसी को निर्धन और किसी को बकरा और दूसरे को उसका निर्दयी भक्षक
अकारण ही बना दिया तो क्या वह प्रमादी,
स्वेच्छाचारी अन्यायी और निर्दयी इत्यादि विशेषणों से विभूषित नहीं
किया जावेगा
?
यदि हम लोगों की ही तरह उसे भी अपनी पूजा की पड़ी है तो आप्तकाम
क्योंकर कहा जा सकता है
?
हाँ,
ऐसा कह सकते हैं कि वह भी कोई हम लोगों जैसा जीव ही है। अन्तर केवल
इतना ही है कि वह कुछ ऐसे भी काम कर सकता है जिन्हें साधारण जीव नहीं
कर सकते। जैसा कि बड़े-बड़े अविष्कार केवल वैज्ञानिक लोग ही कर सकते
हैं न कि दूसरेभी।
इसीलिए कर्मवादियों ने यही स्थिर किया है कि यह सृष्टिप्रवाह अनादि
है,
साथ ही उसका कर्म प्रवाह भी तदनुसार ही सृष्टि में हुआ करता है और
हुआ करेगा। ईश्वर तो केवल जड़ कर्मों का सृष्टिनिर्माण में सहायक होकर
निमित्त मात्र है। इसी से उसमें निर्दय अथवा अन्याय आदि की शंका भी
नहीं हो सकती और न स्वार्थ ही। क्योंकि कर्मवादियों का यह अटल
सिध्दान्त है कि यह सृष्टि किसी की पूजा आदि विशेष उद्देश्य से न
होकर केवल जीवों का अपने-अपने कर्मों के फल भोगने और संसार से
छुटकारा (मुक्ति) प्राप्ति के ही लिए है। चाहे वह ईश्वर की पूजा के
या किसी दूसरे ही उपाय से क्यों न हो,
यह दूसरी बात है। और इस तरह यदि ईश्वर के नामर् कीत्तान या पूजन
प्रभृति से किसी के पापों का विनाश हो अथवा उसका दण्ड उसे न मिले,
तो ईश्वर इससे स्वार्थी अथवा घूसखोर नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ऐसा
उसका स्वरूप वा स्वभाव है कि इस तरह वह चाहता न कुछ है न करता है।
जैसे अग्नि में तृण। यदि वह भस्मीभूत हो जाता है तो उससे अग्नि में
कुछ लगता या यह सिध्द नहीं किया जा सकता कि वह स्वार्थी है इसी
तात्पर्य को लेकर पूर्वोक्त प्रथम सूत्र की रचना हुई है। कुमारिलं
स्वामी ने भी मीमांसादर्शन वार्तिक के चतुर्थ व्याख्यानावसर में कहा
है जिसका तात्पर्य पूर्वोक्त ही है वह यों है-
नन्वार्थापत्तिरेवं
स्याद् जगद्वैचित्रयदर्शनात्।
सुखिदु:ख्यादिभेदो हि नादृष्टात्कारणादृते॥101॥
दृष्टस्य व्यभिचारित्वात् तदभावेऽपि संभवात्।
सेवाधययनतुल्यत्वे दृष्टा च फलभिन्नता॥102॥
इत्यादि।
अस्तु,
अब यहाँ पर यह विचार उत्पन्न होता है कि इस प्रकार जगत् अथवा उसके
वैचित्रय का कारण स्वरूप अदृष्ट (धर्माधर्म) सामान्यत: यद्यपि सिध्द
हो गया। तथापि उससे क्या
?
इतने मात्र से लोगों की प्रवृत्ति क्योंकर हो सकती है
?
लोग किस वस्तु को धर्म समझकर कर सकते और अधर्म समझ उससे अलग रह सकते
हैं
?
क्योंकि सामान्य ज्ञान तो केवल विशेष ज्ञान में उपयोगी होता है न कि
उससे किसी प्रकार की प्रवृत्ति भी हो सकती है। आम्र भी एक वस्तु या
फल है,
इस इतने ज्ञान से कोई भी उसके तोड़ने में प्रवृत्ता नहीं हो सकता,
जब तक उसे विशेष रूप से यह न बतला दिया जावे कि इसे आम्र कहते हैं।
इसलिए कुमारिल स्वामी ने भी पूर्व प्रसंग में ही कहा है कि-
अधर्मे
धर्मरूपे
वा ह्यविभक्ते फलं प्रति।
किमप्यस्तीतिविज्ञानं नराणां क्वोपयुज्यते॥105॥
इसका अर्थ यही है कि
'अमुक
धर्म का अमुक फल है और अमुक अधर्म का अमुक,
जब तक यह विशेष ज्ञान न हो जावे तब तक धर्माधर्म भी कोई वस्तु है यह
सामान्य ज्ञान किस काम का है
?'
यदि यह कहा जावे कि यज्ञ,
दान और हवन आदि ही विशेष धर्म हैं तो यह कहना पड़ता है कि,
एक तो इस बात के मानने में प्रमाण ही क्या है
?
दूसरे तो फिर बौध्दों के चैत्यवन्दन-(बुध्द भगवान् की अस्थि को ताम्र
आदि के पात्र में रख कर उसके ऊपर कुछ स्तूप या ऊँचे टीले वगैरह बनाये
जाते थे उन्हें ही चैत्य कहते हैं,
क्योंकि उसके नीचे अस्थि का चयन वा चिति होती है,
और उसके ही वन्दन को चैत्यवन्दन कहते हैं)-और ईसाई,
मुसलमानों के बपतिस्मा और सुन्नत एवं बाइबिल तथा कुरान पढ़ने आदि को
भी धर्म क्यों न मानें
?
अथवा विपरीत ही क्यों न हो
?
या हिंसा को ही धर्म और अहिंसा को आर्म मानने में कौन सा बाधक है
?
इस बात को भट्टाचार्य जी ने उसी प्रसंग में कहा है। जैसा कि-
किन्नुयागादितो दु:खं हिंसादे: किं सुखोद्भव:।
स्वर्गपुत्रादिभेदश्च
कीदृशात्कर्मभेदत:॥106॥
इति यावदविज्ञानं तावन्नैव
प्रवर्तते॥इत्यादि॥
इसका समाधान मीमांसक लोग इस तरह करते हैं कि हम यह नहीं कहते कि अमुक
पुरुष की कही बात को सत्य मान कर उसे ही धर्म मानिए,
अन्य को नहीं। क्योंकि बिना शरीरादि के उपेदश होता ही नहीं और यदि
होगा भी तो उसमें यह विश्वास नहीं हो सकता कि किसी अदृश्य व्यक्ति का
उपदेश सत्य है वा मिथ्या अथवा इसका कहनेवाला कोई सज्जन है या प्रतारक
(ठग) बिना शरीर का ही उपदेशक मानने से यह भी कल्पना हो सकती है कि
धर्माधर्म की व्यवस्था मनमानी होगी। क्योंकि जैसी बातें इस संसार में
देखी जावें वैसी बातों की कल्पना ऐसी ही है जैसी कि पानी को देखकर
अग्नि की कल्पना। यदि उपदेष्टा का शरीर मानेंगे तो जो शरीरी होता है
उससे भ्रम या प्रमाद प्रभृति भी हुआ ही करते हैं। अत: उसका ठिकाना ही
क्या है,
क्योंकि यदि उसकी चार बातें सत्य हों तो दो मिथ्या भी हो सकती हैं।
इसीलिए किसी भी पुरुष की बात मानी नहीं जा सकती। किसी पुरुष को
सर्वज्ञ मानकर उसके ही उपदेशों को स्वीकार करना भी मनुष्य की बुध्दि
वा अनुमान से बाहर है। क्योंकि जब आजकल कोई सर्वज्ञ नहीं दीखता तो
कालान्तर में था,
यह अनुमान भी क्योंकर हो सकता या यह बात बुध्दि में आ सकती है
?
इन्हीं बातों को वार्तिककार कुमारिल स्वामी ने भी द्वितीय सूत्र पर
कहा है। जैसा कि-
सर्वज्ञोदृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभि:।
निराकरणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना॥117॥
कुडयादिनिसृतत्वत्रयनाश्वासो देशनासुन:॥348॥
किन्नुबुध्द प्रणीता: स्यु किमुकैश्चिहद्दरात्मभि:॥
भदृश्यैर्विप्रलम्भार्थं पिशाचादिभिरीरिता:॥140॥
एवं यै: केवलं ज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिण:।
सुक्ष्मातीतादिविपयं जीवस्य परिकल्पितम्॥141॥
दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो नृषुकश्चित्प्रवर्तते॥142॥
सर्वदा चापि पुरुषा: प्रायेणानृत वादिन:।
यथाऽद्यत्वे न विस्रम्भस्तथाऽतीतार्थकीर्त्तने॥144॥इत्यादि
इन सब श्लोकों का तात्पर्य वही है जो ऊपर दिखलाया जा चुका है न कि
कुछ दूसरा।
किन्तु प्राकृतिक पदार्थों से जैसे अन्य उपदेश लिए जाते हैं उसी तरह
धर्माधर्म के भी विषय में समझना चाहिए। जिस प्रकार चन्द्र-सूर्यादि
के उदय और अस्त एवं कालादि के परिवर्तन से यह उपदेश मिलता है कि
सांसारिक पदार्थों की एक सी दशा नहीं रह सकती। सभी आगमापायी वा
क्षणभंगुर हैं,
अथवा जैसे न्यूटन को सेब के फल के भूमि पर पतन से आकर्षण शक्ति के
विषय में उपदेश मिला था। उसी तरह के उपदेशों से धर्माधर्म का निश्चय
करना चाहिए न कि बनावटी उपदेशों से। क्योंकि उनके मिथ्या होने का भय
या सम्भावना नहीं है। इस पर जब यह जिज्ञासा हुई कि वह कौन सा
प्राकृतिक पदार्थ अकृत्रिम है जिससे धर्मज्ञान हो सकता है,
तो मीमांसकों ने उत्तर दिया कि
'वेद'
अथवा तन्मूलक स्मृति आदि। इस पर जब प्रश्नोत्तार होने लगे तो
उन्होंने यही सिध्द किया कि वेद किसी का रचा हुआ नहीं है। इसलिए वे
लोग वेद को अपौरुषेय कहते हैं। जिसका अर्थ यह है कि जो किसी पुरुष
द्वारा रचा न गया हो। क्योंकि यदि उसकी रचना पुरुष द्वारा हुई होती
तो महाभारतादि की तरह उसके कर्ता का भी नाम लिखा रहता,
अथवा न भी लिखे रहने पर बराबर लोग कहते चले आते कि अमुक पुरुष का
बनाया हुआ है। मंत्रभाग तो नहीं,
पर ब्राह्मण भाग जो कहीं-कहीं पुरुषों के नाम से प्रतीत होते हैं,
उसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन पुरुषों ने उन भागों की रचना की है।
किन्तु जिसने जिस शाखा का विशेष अध्यापन वा प्रचार किया उसी के नाम
से वह शाखा प्रसिध्द हो गयी। जैसा कि आजकल भी गानविद्या वा
युध्दविद्या के प्राचीन होने पर भी जिसने उसमें विशेष कुशलता दिखलायी,
उसके सम्बन्ध में उसका नाम हो गया अथवा होता है,
जैसा कि तानसेन या मास्टर मदन प्रभृति का। अथवा वे नाम इन उन
शास्त्रों के ही हैं। परन्तु जो उसमें विशेष संलग्न या प्रवीण हुए
उनका भी वही नाम हो गया। जैसी प्रथा आजकल भी है और वेदों में भी
ऐसे-ऐसे आख्यान आते रहते हैं। जैसा कि प्राणों की उपासना करने वाले
एक ब्रह्मचारी का वर्णन छान्दोग्योपनिषद् में है। जो अपने को
प्राणस्वरूप समझता और वैसा ही व्यवहार करता था,
इत्यादि रीति से मीमांसा दर्शन के आख्या प्रवचनात्।1।1।30।
इत्यादि सूत्रों के भाष्य और र्वात्तिकादि ग्रन्थों में यह बात
विस्तार पूर्वक दिखलाई गयी है।
इन पूर्वोक्त बातों का खण्डन-मण्डन करके जिन लोगों का यह आग्रह होता
है कि वेद पौरुषय ही हैं वे लोग मीमांसकों के अभिप्राय को नहीं
समझते। यदि यह वात्त वस्तुत: न भी हो यही बात मान ली जावे तो भी
मीमांसकों के मत का खण्डन नहीं होता। क्योंकि वेद को अपौरुषेय बतलाने
से उनका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि उसमें कहे गये उपदेश
निर्दोष होने के कारण सर्वदा ग्राह्य हैं। यदि ईश्वर ने ही वेदों को
बनाया हो और वे निर्दोष हों तो भी उनका मत सिध्द हो ही जाता है,
क्योंकि उनका अभिप्राय केवल वेदों का निर्दोष मानने में है। अत:
आधुनिक नैयायिकादि मतवादियों का एतद्विषयक दुराग्रह अश्रद्वेय है।
मीमांसकों ने तो वेदकर्ता ईश्वर या अन्य का खण्डन केवल इसीलिए किया
कि ऐसा मानने से बहुत सी कुकल्पनाएँ होने लग जाती हैं,
जैसा कि दिखला चुके हैं। परन्तु उन कुकल्पनाओं के वारण करने में कोई
समर्थ हो तो भले ही ईश्वरनिर्मित या अन्यरचित ही वेदों को मानें।
इसमें उनको कोई आग्रह नहीं है इसीलिए र्वात्तिककार ने भी यही
अभिप्राय झलकाया है जैसा कि-
कर्तमत्तवे
तु वेदस्य सम्यङ्मिथ्यात्व वादिगि:।
कर्ता
गुणाश्च दोषाश्च महाजनपरिग्रह:॥
एवमादि विनायुक्त्या कल्प्यं मीमांसकै: पुन:।
इदानीमिव
सर्वत्र
दृष्टान्नाधिकमिप्यते॥
अर्थात् वेदों का कर्ता मानने पर उनके मानने वाले ईश्वर में मानेंगे
और बुध्दादि में दोष। एवं बौध्द लोग इसके विपरीत। इसी तरह वेदवादी
लोग कहेंगे कि यदि वेदोक्त बातें मिथ्या होतीं तो महाजन वा विवेकी
लोग उनको स्वीकार करते बहुत दिनों से क्यों चले आते
?
यह बात बौध्दादि के धर्मग्रन्थों में नहीं है,
इत्यादि बातें बिना युक्ति या प्रमाण के माननी होंगी और विपरीतवादी
लोग इससे विरुध्द ही मानेंगे। परन्तु मीमांसकों को तो इस समय की तरह
ही कुछ भी कभी भी अधिक कल्पना करनी नहीं पड़ती है। जैसे नेत्रादि
प्रमाण प्राकृतिक हैं वैसे ही वेद को भी वे लोग मानते हैं।
वेदों की अपौरुषेयता के सम्बन्ध में एक यह बात भी ध्यान देने योग्य
है कि यद्यपि उनमें उनके रचयिता का नाम नहीं लिखा है तथा उनका
निर्माणकर्ता कोई पुरुष उसी दशा में माना जा सकता है जब कि उसका उचित
रीति से अनुमान किया जा सके। तात्पर्य यह कि वेदों की लेखशैली और
संस्कृत-वाक्यावली जैसी है उस ढंग का यदि कोई भी ग्रन्थ मनुष्यरचित
कहीं भी समुपलब्धा हो जाता तो उसी आधार पर उनका रचनाकाल और रचयिता
पुरुष दोनों ही विदित हो जाते। पर यह बात आज तक सम्भव न हो सकी,
वेदों की लेखप्रणाली अलौकिक और अद्वितीय ही है। इसीलिए जिन लोगों के
तर्क इस प्रकार के होते हैं कि यदि हम एक पत्र लिखकर अपने घर में
बिना नाम का ही रख देवें और थोड़े या अधिक दिनों बाद कोई भी इसे देख
यह कहने लग जावे कि यह पत्र तो अपौरुषेय है। कारण कि इस पर इसके लेखक
का नाम है ही नहीं। तो क्या उसकी बात मानी जा सकती है
?
बस,
यही हाल वेदों की अपौरुषेयता का है। वे लोग अपौरुषेयतावादी मीमांसकों
के पूर्वोक्त अभिप्राय को न हृदयंगम करके ही ऐसा करते हैं। क्योंकि
पत्र की रचनाशैली से ही सामान्यत: किसी न किसी लेखक का अनुमान किया
जा सकता है। इसी तरह महाभारतादि ग्रन्थों या आधुनिक पुस्तकों के
दृष्टान्तों से भी जो लोग वेदकर्ता पुरुष का अनुमान करते हैं वे लोग
भी लेखशैली वाले अभिप्राय से अनभिज्ञ हैं। अतएव उनके वे अनुमान भी
अकिंचित्कर ही हैं।
अत: अगत्या यही मानना पड़ता है कि जैसे पृथ्वी,
जल,
वृक्ष और पशु प्रभृति पर उनके रचयिता ईश्वर का नाम नहीं लिखा हुआ है
और वे ईश्वरकृत ही माने जाते हैं साथ ही उनकी रचना भी अद्वितीय है,
उसी तरह वेदों को भी पौरुषेय (पुरुष वा मनुष्य कृत) न मानकर ईश्वरकृत
ही मानना उचित और युक्तिसंगत है। यही अपौरुषेयतावादी मीमांसकों का
वास्तविक अभिप्राय है,
न कि वे लोग ईश्वर का सर्वथा ही अपलाप करते हैं। अतएव
मीमांसार्वात्तिककार कुमारिल स्वामी ने श्लोकर्वात्तिक के प्रारम्भ
में ही महर्षि वेदव्यास के श्लोक द्वारा ही मंगलाचरण करते हुए ईश्वर
की सत्ता झलकाई है। वह श्लोक यों है-
''विशुध्दज्ञान
देहायत्रिवेदी दिव्यचक्षुषे।
श्रया:प्राप्ति
निमित्तय
नम: सोमार्धाधारिणे॥''
इसका अर्थ यह है कि विशुध्द ज्ञान स्वरूप,
तीन वेद स्वरूप,
तीन दिव्य नेत्र वाले,
कल्याणप्राप्ति के निमित्त और अर्ध्दचन्द्र (द्वितीया के चन्द्र) को
धारण करनेवाले परमात्मा शिव को नमस्कार है। यही अर्थ इसका लोक उचित
और सर्वविद्वजन
एवं मीमांसा सम्मत है। अतएव केवल कर्म को प्राधान्य
देने वाले-कर्म ही सब कुछ है और वही सुख-दु:खादि का देनेवाला है न कि
दूसरा कोई ऐसा कहनेवाले मीमांसकों का अभिप्राय केवल यही है कि लोग
उसी को
सर्वप्रधान
मान उसके लिए सजग और सन्नध्द हो कर्मवीर वा सच्चे कर्मयोगी बन जावें
और विशेष रूप से उनका ध्यान कर्मों पर ही आकृष्ट हो। इस प्रकार जब
लोग कर्मों को श्रध्दा से करेंगे तो आगे चलकर उनके फलों की प्राप्ति
में कौन सी अड़चन है
? ईश्वर की कृपा से वे मिल ही जावेंगे। न कि
उनका यह तात्पर्य है कि ईश्वर है ही नहीं अस्तु,
जब हम वेदों को अपौरुषेय मानते हैं तो यह हमारा
अभिप्राय कदापि नहीं कि उनके प्रादुर्भाव से मनुष्य का कुछ भी
सम्बन्ध
है ही नहीं,
जैसा कि पृथ्वी, जल
आदि का प्रादुर्भाव बिना मनुष्यों की सहायता के
स्वतन्त्र
रूप से ही हुआ है। क्योंकि पृथ्वी,
जल प्रभृति तो ज्ञान की तरह सर्वदा
परतन्त्रक
स्वरूप नहीं हैं। अतएव वे बिना किसी मनुष्य,
जीव वा शरीर की सहायता के भी हो सकते हैं,
जैसा कि देखा ही जाता है। परन्तु वेद शब्द का
अर्थ है ज्ञान और वास्तव में सबसे प्रथम होने वा कहने वाले ईश्वरीय
ज्ञान स्वरूप ही वेद हैं भी। इससे वे बिना शरीर वा पुरुष के प्रकट हो
सकते नहीं। अतएव इस विषय में आस्तिक सिध्दान्त यही है कि वेदों के
मन्त्र समाधिस्थ
महर्षियों के अन्त:करणों में व्यक्त हुए थे। अतएव लोक में जो यह
व्यवहार है कि अमुक
मन्त्र
का ऋषि अमुक है उसका तात्पर्य यही है कि ईश्वरीय कृपा से
समाधिस्थ
उस ऋषि के अन्त:करण में वह
मन्त्र
प्रथम व्यक्त हुआ था। इसी से लोगों को यह भ्रम होने लगा कि वह
मन्त्र
उसी ऋषि का बनाया हुआ है। इसी तरह अमुक
मन्त्र
का देवता अमुक है,
इसका भी अर्थ यही है कि उसी देवता का प्रतिपादन
वा स्तुति उस
मन्त्र
में है। अस्तु-
इस प्रकार सामान्यत: कर्म की सत्ता सिध्द करने के उपरान्त मीमांसकों
ने उसे भिन्न-भिन्न फलों के लिए भिन्न स्वरूपों में विभक्त किया है।
जैसे स्वर्ग प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र और ज्योतिष्टोमादि यज्ञ,
वृष्टि के लिए कारीरी याग,
पुत्र के लिए पुत्रोष्टि,
पितरों की तुष्टि के लिए पितृयज्ञ (श्राध्द तर्पणादि देवों के लिए
देव यज्ञ बलि वैश्वदेवादि) प्रभृति को समझना चाहिए। इस जगह पर कर्मों
के फल के सम्बन्ध में मीमांसकों का एक निश्चित और अवश्यज्ञेय
सिध्दान्त यह है कि वे यह नहीं मानते कि कर्मों के फल उनके कर्ता को
ही प्राप्त होते हैं। जो यह नियम है कि शास्त्रफलं प्रयोक्तरि
अर्थात् कर्म के फल कर्ता को ही मिलते हैं,
वह सामान्यत: है न कि सभी जगह लगता है। क्योंकि यदि ऐसा मान लिया
जावे तो पूर्व वन्तोऽविधानार्था: है (मी. अ.
1
सू.
17)
इस वैश्वानरेष्टि वा जातेष्टि नामक यज्ञ के प्रकरण में जो यह लिखा
गया है कि वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् पुत्रो जाते...यस्मिन्आत
एतामिष्टिं निर्वपति पूत एव तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियाघो पशुमान् भवति।
अर्थात् पुत्र के उत्पन्न होते ही जातेष्टि वा वैश्वानर यज्ञ पिता
करे। उससे पुत्र तेजस्वी अन्न से सम्पन्न हृष्ट पुष्ट इन्द्रिय वाला
और पशु वाला होता है,
वह मिथ्या...क्योंकि नास्तिक लोग तो पारलौकिक अपने या दूसरे के किये
हुए कर्मों के फलों को मानते ही नहीं। अत: वे तो चाहें कह सकते हैं।
परन्तु आधुनिक वैदिक कहलाने वाले जो कर्मों के पारलौकिक फलों को
मानते हैं,
क्योंकर ऐसा कह सकते हैं
?
अतएव उनका यह कथन केवल पूर्वप्रदर्शित मीमांसासिध्दान्त को न जानकर
ही है। क्योंकि पितादिकों के लिए श्राध्द,
दानादि करने वाले पुत्र प्रभृति तो एक प्रकार ऋत्विक की तरह हैं। अत:
उनका किया हुआ पितादिकों को क्यों न मिलेगा
?
साथ ही वह पितादिकों के ही उद्देश्य से किया भी जाता है।
यदि इस पूर्वोक्त अभिप्राय को हृदयंगम न कर सकने के कारण वे लोग यह
कहने का साहस करें कि पुत्र प्रभृति द्वारा किये गये श्राध्दादि मृत
पितादि को प्राप्त हो जाते हैं इसमें प्रमाण ही क्या है
?
कारण वे अन्यत्र और हम अन्य जगह रहते हैं। जिस प्रकार इस संसार में
विदेशवासी पुरुष के पास उसके सम्बन्धियों के भेजे हुए द्रव्य वगैरह
डाक द्वारा पहुँच जाते हैं उसी प्रकार मृतकों के पास श्राध्दादि की
वस्तुएँ पहुँचाने वाली कौन सी डाक है
?
साथ ही यहाँ तो उसके पास पहुँचने की रसीद मिला करती है,
जिसके न मिलने पर प्रवासी के पास प्रेषित वस्तु के पहुँचने में संशय
रहता है,
अथवा वह नहीं ही पहुँचती है,
पर वहाँ कौन सी रसीद मिलती है जिससे पहुँचना सत्य प्रमाणित हो
?
और रसीद न मिलने की दशा में यह क्यों न कल्पना की जाये कि बीच के ही
बेईमान लोगों ने उस पदार्थ को हड़प लिया,
जैसा कि देखा जाता है कि तीर्थ के पण्डे,
महाब्राह्मण व पुरोहित आदि ही उस पदार्थ को भोगते हैं
?
एक बात और भी ध्यान योग्य है,
वह यह कि मृत्यु के अनन्तर सर्वदा ही सभी लोग किसी पितृदि लोक विशेष
में ही रहा करते हैं यह वात्त तो मानी जा सकती नहीं,
क्योंकि ऐसी दशा में नयी सृष्टि रुक जावेगी और हमारा वैदिक सिध्दान्त
भी ईसाई अथवा मुसलमानों के सिध्दानत सा ही हो जावेगा,
जो युक्तियुक्त नहीं है। अत: यह मानना ही पड़ेगा कि मृत्यु के अनन्तर
पुनर्जन्म भी होता ही है। ऐसा मानने में पुनर्जन्मवाद वाली सभी
युक्तियाँ सहायक होंगी। ऐसी दशा में यदि मृतक पिता प्रभृति पशु,
कीट,
पक्षी अथवा राक्षसादि योनि में उत्पन्न हो गये-क्योंकि वह अमुक योनि
में जन्म लेंगे यह तो निर्धारित है ही नहीं-तो उनके लिए जौ के कच्चे
आटे के पिण्ड या तिल वगैरह किस काम के
?
उनके लिए तो उस उस योनि के सेव्य पदार्थ घास प्रभृति मिलने चाहिए। तो
क्या घास वगैरह के भी पिण्ड दिये जावेंगे
?
यह भी तो देखा जाता है कि हम लोग जितने यहाँ दीखते हैं सभी ने मृत्यु
के बाद ही जन्म लिया है। पर किसी को भी कभी भी पिण्ड वा तिलों की
प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं हो रही है। क्या इससे पूर्व जन्म के
हमारे सम्बन्धी लोग हमारे वास्ते श्राध्द न करते होंगे
?
तो फिर वह क्या हुआ
?
एक बात यह भी विचारणीय है कि जब मृत्यु के बाद तुरन्त ही जन्म का
होना सिध्द है,
जैसा कि भगवद्गीता में भी कहा है कि-
''वासांसि
जीर्णानि यथा विहाय नवानि
गृह्णाति
नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥''
अर्थात् जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ते ही नये वस्त्र को पहन
लेता है,
वैसे ही जीवात्मा पुराने (प्रथम) शरीर को छोड़ते ही नया शरीर धारण
करता है,
तो फिर किसके लिए श्राध्दादि किये जावें
?
एवं वैतरणी प्रभृति यमपुरी के मार्ग में रहनेवाले स्थानों के लिए
गोदान वगैरह कर्म किये जावें
?
क्योंकि यमपुरी या स्वर्गादि में तो जाने का अवकाश जीवों को है ही
नहीं। अतएव यमपुरी और यमदूत आदि एवं विविध नरकों को मानना केवल कमाने
का रास्ता और पॉपलीला मात्र है। इतने पर भी यदि यह दुराग्रह बना ही
रहे कि पुत्रादि द्वारा किये गये श्राध्द प्रभृति मृत पितरों को
मिलते ही हैं,
तो इसकी जाँच इस प्रकार करके सन्तोष करना होगा। अर्थात् प्रथमत:
जीवित पिता को ही कोठे पर बिठा कर उसके नीचे वाले मकान में पिता के
ही निमित्त ब्रह्मभोज वा श्राध्दादि करके यह देख लेना चाहिए कि वे
पदार्थ कोठे पर ही स्थित पिता को मिलते हैं वा नहीं। यदि इतनी ही दूर
रहनेवाले को नहीं मिल सके तो लोकान्तर वा शरीरान्तर में रहनेवाले मृत
जीवों को क्योंकर मिल सकेंगे
?
यह विषय विश्वास से बाहर है। यदि यह बात होती कि जिस किसी के नाम से
जो ही कुछ जहाँ ही कहीं कोई भी दे देवे,
वह उसे,
जहाँ रहेगा वहाँ ही मिल जावेगा,
तो फिर परदेश करनेवाले को चोर वा डाकुओं के भय से बचने के लिए रुपये
वगैरह सामान साथ ले जाने की क्या आवश्यकता है
?
घर पर ही उतनी वस्तुएँ उनके नाम से ब्राह्मण वगैरह को दे दी जानी
चाहिए,
बस इतने ही से प्रवासी लोग जहाँ रहेंगे वहाँ ही से चीजें उन्हें मिल
जाया करेंगी।
यदि विचारदृष्टि से देखा जाय तो सभी कुतर्क और बातें निस्सार विदित
होंगी। कारण,
धार्मिक कारणों में साधारण डाक और रसीद की आवश्यकता ही नहीं है। इस
संसार के ऐहलौकिक कार्यों में रसीद वगैरह की आवश्यकता तो इसलिए पड़ा
करती है कि न तो भेजनेवाला ही सर्वज्ञ और भूत-भविष्य का वेत्ता है और
न सरकार ही,
जिसके प्रबन्ध से विदेश में रुपये आदि भेजे जाते हैं। साथ ही डाक के
कर्मचारी और प्रबन्धकर्ता मनुष्य ही हैं और भेजनेवाला भी वही। ऐसी
दशा में भेजने वाला कर्मचारियों और प्रबन्धकर्ताओं का विश्वास
क्योंकर कर सकता है
?
कारण कि भूल और बेईमानी आदि मनुष्यों के साधारण धर्म हैं। अत: वह
उन्हें भी अपने ही सदृश समझता है चाहे वे सत्पुरुष ही क्यों न हों।
उसकी यह धारणा उचित भी है। क्योंकि जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं और
जो हमारे पूर्ण परिचित हैं जब उनमें भी भूल और बेईमानी देखी जाती है
तो जिनसे हम बिल्कुल ही अपरिचित हैं उनका विश्वास क्योंकर करें
?
परन्तु यह बात ईश्वरीय राज्य और प्रबन्ध में सम्भव नहीं। वह तो
सर्वज्ञ,
दयालु,
न्यायकर्ता एवं भूत-भविष्यादि सभी का जानने वाला है। वह अपने प्रबन्ध
को अपनी ऑंखों देखता रहता है,
कारण वह सर्वत्र ही विद्यमान है। अत: उसकी साक्षिता में-क्योंकि वह
व्यापक है और अग्नि आदि भी उसी के स्वरूप हैं-जो कुछ भी दिया वा किया
जावेगा वह जिसके निमित्त होगा उसी को निस्सन्देह प्राप्त होगा,
चाहे वह कहीं भी हो। अतएव यदि अपने लिए भी किया जायेगा तो अपने आपको
भी,
जहाँ रहेंगे,
अवश्य ही प्राप्त होगा। वहाँ भूल अथवा बेईमानी की जगह कहाँ
?
ऐसी दशा में रसीद की आवश्यकता ही न रह गयी,
वरन् उसके लिए प्रश्न करना ईश्वर की ईश्वरता और न्याशीलता में बट्टा
लगाना और परम नास्तिकता है। इसी से चार्वाकादि नास्तिकों को ही यह मत
मान्य हो सकता है न कि वैदिक नामधारियों को भी और उन्हें भी वही
मार्ग रुचा तो उनको प्रच्छन्न नास्तिक समझना चाहिए।
यदि यह बात न मानी जावे तो अपने लिए जो कुछ भी पारलौकिक कार्य किये
जाते हैं वे भी न किये जा सकेंगे। कारण परलोक अथवा जन्मान्तर में
हमारे कर्मों का फल हम मिलेगा इसमें प्रमाण ही क्या है
?
जो कुछ भी हमने किया है उसकी रसीद हमारे पास है ही क्या जिससे उसके
मिलने का विश्वास करें। इसीलिए कोठे वाला अथवा विदेशयात्रा करने वाले
का दृष्टान्त भी विषम और असंगत है। क्योंकि यदि कोठे के नीचे
रहनेवाले को खिलाया हुआ कोठे पर वाले को न मिलने और यहाँ खिला या दे
देने से परदेश वाले को न मिलने से यह मान लिया जावे कि अन्य का
(पुत्रादि का) किया वा दिया अन्न (मृत पितादि) को नहीं मिलता तो उसी
दृष्टान्त से यह भी मानने को विवश होना होगा कि अपना किया भी
पारलौकिक कर्म अपने को फलदायक नहीं होता। कारण अपने लिए भी खिला वा
देकर कोठे पर अथवा विदेश में उसे नहीं पाते। फिर उसमें भी क्योंकर
विश्वास हो
?
इसलिए यही हार कर कहना और मानना होगा कि मनुष्य कर्म करने में ही
स्वतन्त्र है न कि उसके फल पाने में। जैसा कि भगवान् ने कहा है कि
'कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन गीता
02।47
अतएव चाहे तभी उसके कर्मों का फल उसे नहीं मिल सकता। किन्तु उसका समय
आने पर ही मिलेगा। इसी से यदि कोई आम्र वृक्ष लगाकर शीघ्र ही अथवा
कुछ ही दिन बाद इसका फल खाना चाहे तो नहीं खा सकता है,
किन्तु उसका समय आने पर ही। अत: अपने लिए भी जो कार्य वा कर्म करेंगे
उसका फल हमारी इच्छा के अनुसार ही कोठे पर अथवा परदेश में नहीं मिल
सकता,
वरन् अपने समय पर ही नियम के अनुसार ही मिलेगा,
चाहे कभी मिले। बस,
ठीक-ठीक यही हाल दूसरे (पुत्रादि) के किये हुए को दूसरे (मृत पितादि)
को मिलने के विषय में भी समझ लेना चाहिए। अत: रसीद और कोठे आदि
परीक्षा की कसौटी वालीबात धर्माधर्म के विषय में केवल अनभिज्ञता मूलक
कर्म योग के रहस्य को न जानकरहीहै।
रह गयी डाकवाली बात। सो तो है ही। ईश्वरीय राज्य और प्रबन्ध में तो
ऐसी विलक्षण डाक बनी और लगी हुई है जिसे सभी मानते जानते हैं। उसका
प्रबन्ध ऐसा जँचा जँचाया और पक्का है कि कोई चूँ तक नहीं कर सकता।
चन्द्र और सूर्य का ठीक समय पर ही उदय एवं अस्त होना,
ऋतुओं का अपने-अपने पर ही अवश्य प्रादुर्भाव और उनके फल फूलादि का
अपने-अपने जँचे जँचाये ही समय पर उत्पन्न होना,
बहुत दिनों तक पृथिवी में पड़े हुए बीजों से भी अपने ऋतु वा समय पर ही
अंकुर निकलना तथा उनसे अन्नादि की प्राप्ति और संसार के अन्यान्य
जीवनाधीन कार्यों का उचित समय पर ही होना इत्यादि बातें क्या ईश्वर
के दृढ़ और कभी न विचलने वाले प्रबन्ध की पोषक नहीं हैं
?
यदि किसी को इन बातों से भी सन्तोष न हो तो वह ईश्वर को मानता ही
क्यों है
?
क्योंकि यदि उसे स्वीकार करेगा तो उसे मानना ही पड़ेगा कि कर्मों के
उचित और विभागयुक्त फल प्रदान के अतिरिक्त कोई काम है ही नहीं जिसके
लिए वह माना जावे। क्योंकि सृष्टि स्थिति और प्रलयादि भी तो जीवों के
कर्मों के फल ही हैं। पूर्वोक्त ईश्वरीय नियम अथवा प्रबन्ध को
अस्वीकार करने वालों से यह प्रश्न हो सकता है या होगा कि,
जिस जगह जितने जीव मरते हैं वे उसी जगह तो जन्म लेते हैं नहीं। कारण
उन्हें कर्मानुसार सभी भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेना होता है और
सभी योनियों के जीव एक जगह मिल सकते नहीं। व्याघ्र जंगल में ही रहता
है तो भेड़ बकरियाँ ग्रामों में ही और कस्तूरीमृग बर्फानी जगहों में
ही इत्यादि। साथ ही यदि ऐसा मान लिया जावे तो किसी स्थान को भी
उच्छिन्न हो जाना वा डीह पड़ जाना न चाहिए। ऐसी दशा में सौ दो सौ अथवा
सहर्षों
कोसों पर उन उन योनि वाले स्थानों में मृत्यु के अनन्तर उन जीवों को
पहुँचाने वाली कौन सी डाक,
रेल अथवा तार है ? यदि
थोड़ी देर के लिए स्वीकार भी कर लें कि जो जीव जहाँ मरते वहीं जन्म भी
ग्रहण करते हैं तो भी यह प्रश्न अनिवार्य है कि किस डाक,
रेल व तार ने उन्हें एक शरीर से अलग कर अन्य पिता
के शरीर और माता की देह में पहुँचाया है अथवा कौन पहुँचाया करता है।
क्योंकि यदि पिता और माता के शरीर में भागश: उन्हें पहुँचना अथवा
केवल पिता के ही शरीर में उनको पहुँचना न स्वीकार
करें
तो पिता के संयोग बिना ही
पुत्र
जन्म होना चाहिए। यदि ऐसा भी मानने को कोई निर्लज्ज होकर सन्नध्द हो
तो भी यह प्रश्न नहीं हट सकता। क्योंकि जब माता के गर्भाशय से ही
पुत्रोत्पत्ति
होती है तो उस गर्भाशय में पहुँचाने वाली कोई डाक अथवा अन्य
साधन
मानना ही पड़ेगा। बस,
जो ही डाक वा अन्य
साधन
पहुँचाने के इस कार्य को करते हैं,
वे ही
पुत्रादि
द्वारा किये गये श्राध्दादि कर्मों के फलों को मृत पितादि को जहाँ
कहीं भी वे हों,
पहुँचाते हैं और वे ही हमारे निज के पारलौकिक
कर्मों के फलों को भी हमें, मरणान्तर जहाँ
कहीं भी
सहर्षों
कोसों पर हम जावें पहुँचाते हैं। नहीं तो हमें अपने किये कर्मों के
फल जन्मान्तर में हमें डाक के न होने से न मिलने चाहिए। परन्तु
आस्तिक समाज और वैदिक नामधारी
इसे मानने को तैयार नहीं।
इस डाक या पहुँचाने के ईश्वरीय साधन को हम केवल तर्कों और युक्तियों
से ही सिध्द नहीं कर रहे हैं किन्तु सामवेदीय छान्दोग्योपनिषत् के
पंचम प्रपाठक के द्वितीय से लेकर नवम खण्ड तक के आठ खण्डों अग्नि,
विद्या,
प्रकरण में यही बात दिखलायी गयी है और वहाँ पहले इसी विषय के पाँच
उपस्थित हुए हैं,
जो युक्त द्वितीय ही
'वेत्थ
यदितोऽधि'
इत्यादि वाक्यों द्वारा दिखलाये गये हैं,
यों का सारांश यही है कि इस संसार में लोगों का आवागमन कार होता है,
देवयान और पितृयान मानों द्वारा लोग कैसे देवयान वाले कैसे मुक्त हो
जाते हैं लोगों की माता के गर्भ में यदि क्योंकर होती है और देवयान
एवं पितृयान मार्गों का कैसा है इत्यादि। यही बात बृहदारण्यकोपनिषद्
अष्टम अध्याय ब्राह्मण में भी ज्यों की त्यों लिखी गयी है।
''अग्रौ
प्रास्ताहुति: सन्यगादित्यमुपतिष्टते।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं तत: प्रजा:।''-मनु.
3।73
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव:।
यज्ञाद्भवति पर्जन्य: यज्ञ:कर्म समुद्भव:॥''-गीता
3।14
अर्थात् अग्नि में जो आहुति दी जाती है वह सूर्य के पास जाती है,
वृष्टि से जीवों की उत्पत्ति होती है इत्यादि मनुस्मृति और भगवद्गीता
के वाक्यों से भी यही बात सिध्द होती है।
जब इस प्रकार ईश्वरीय प्रबन्ध या डाक अपने लिए किये गये स्वकीय अथवा
परकीय कर्मों के फलों एवं जीवों की देहान्तर तथा जन्मान्तर में
अविवाद रूप से पहुँचाने के लिए सिध्द हो गयी-सर्वमान्य हो गयी तो घास
इत्यादि के पिण्डवाली शंकाएँ और समस्याएँ आप ही आप हल हो जाती हैं।
कारण देखा जाता है कि इस संसार के एकदेशी छोटे-बड़े राष्ट्र से दूसरे
राष्ट्र में रुपए पैसे आदि पहुँचाने का सुव्यवस्थित नियम बना लिया है
जिसमें कभी भी अन्यथा भाव की सम्भावना नहीं है। तो फिर ऐसा मानने के
लिए कोई भी समुचित कारण प्रतीत नहीं होता कि यही न्याय ईश्वरीय
प्रबन्ध में क्यों न लागू हो और ऐसी ही सुव्यवस्था वहाँ भी क्यों न
मानी जाय। क्योंकि प्रथम कहा जा चुका है और आगे भी प्रसंगवश कहा
जावेगा कि इन्हीं लौकिक छोटे-बड़े राज्यों और उनके प्रबन्धों को देखकर
तदनुरूप ही अलौकिक (अप्रत्यक्ष) ईश्वरीय राज्य और प्रबन्ध का अनुमान
किया जाता है। हम देखते हैं कि किसी का कोई सम्बन्धी एक राज्य से
दूसरे सुदूर वा निकट के राज्य में चला जाता है और वह अपने
सम्बन्धियों को अथवा उसके सम्बन्धी उसकी आवश्यकतानुसार कुछ रुपया आदि
भेजना चाहते हैं। साथ ही उन दोनों या उनके मध्यवर्ती राष्ट्रों के
सिक्के वा रुपये भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इसी दशा में वे
जिस राज्य में रहते हैं उसी के सिक्के भेजने को बाध्य होते हैं,
परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार पानेवाले को वे सिक्के न
मिलकर जिस राज्य में वह रहता है उसी के सिक्के मिला करते हैं।
विचित्र बात है कि जो रुपये मिलें वे न भेजे जायँ और जो न मिल सकें
वे ही भेजे जायँ। एक दूसरा ही भेजने को बाध्य है,
दूसरा ही पाने को। यह मनुष्यकृत अन्तर्राष्ट्रीय सुशृंखला नियम का
प्रभाव है। वास्तव में यदि विवेकबुध्दि से देखा जाये तो पानेवाले को
यदि भेजनेवाले के ही सिक्के ज्यों के त्यों अविकल रूप से मिल जायँ तो
उसके किस काम के
?
पर वे भेजे तो जाते हैं काम के ही लिए अत: ऐसा नियम बना लिया गया है
कि भेजे हुए सिक्के उसको उसी रूप में मिलते हैं जिसकी उस राज्य में
चलन होती है। औरों को वहाँ कोई पूछ ही नहीं सकता। बस इसी दृष्टान्त
और न्याय को सर्वतोभाव से ईश्वरीय प्रबन्ध में लगा लेना चाहिए। मृत
पितर चाहे पितृलोक में हों,
देवलोक में हों नरक में हों अथवा मनुष्य,
पशु,
पक्षी एवं कीट आदि योनियों में हों,
उनके पूर्व जन्मवाले सम्बन्धी लोग जौ के कच्चे आटे,
तिल अथवा तण्डुलादि निश्चित वस्तुओं को ही पिण्ड रूप में प्रदान
करेंगे। तथापि उन पितरों को वे वस्तुएँ अमृत,
अन्न,
वस्त्र व घास आदि उन्हीं वस्तुओं के रूप में मिलेंगी व मिलती हैं
जिनसे उनको उन स्थानों और योनियों में लाभ पहुँच सकता है,
न कि सर्वत्र अविकल रूप से
और के पिण्ड और तिल प्रभृति वे वस्तुएँ ही मिला करती हैं।
यहाँ पर यह प्रश्न भी नहीं किया जा सकता कि तिलादि के ही पिण्ड क्यों
दिये जायँगे और दूसरी वस्तुओं के नहीं। कारण यह नहीं कह सकते कि
पृथ्वी के सभी राष्ट्र एक ही प्रकार के सिक्के क्यों नहीं रखते
?
प्रस्तुत यदन्न:
पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता:
अर्थात् मनुष्य जो खाता है वही अपने देवता पितरों को भी समर्पण करे-इसके
अनुसार फलादि के भी पिण्ड दिये जा सकते हैं। जैसा कि वाल्मीकि
रामायणादि से स्पष्ट है और देखा भी जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के
अनन्तर दशाहादि के समय मृतक के सुख के लिए सभी प्रकार की वस्तुएँ दी
जाती हैं और समय पर सुख की जो वस्तुएँ नहीं मिल सकतीं इनके स्थान पर
द्रव्यादि पदार्थान्तर ही दे दिये जाते हैं। तथापि नित्य के
व्यवहारों में कुछ ऐसे नियम निश्चित रूप से बना देने की आवश्यकता
होती है जिनके अनुसार सभी लोग प्रतिदिन ठीक-ठीक
व्यवहार किया करते हैं और मनमाना घरजाना होकर किसी बात में गड़बड़ नहीं
होने पाता। बस इसी तथा ऐसे ही अन्यान्य विचारों को मन में रखकर
महर्षियों ने कुछ अवसरों के लिए श्राध्दादि की आटा,
तिल एवं तण्डुलादि वस्तुएँ निर्दिष्ट कर दी हैं।
प्रथम जो पूर्वपक्ष में यह कहा गया है कि मृत्यु के अनन्तर ही झटपट
शरीरांतर मिल जाता है। मृतक को स्वर्ग,
नरक,
मृतलोक वा यमपुरी आदि में नहीं जाना पड़ता है और इसी की पुष्टि में
वासांसि जीर्णानि इत्यादि गीता के वाक्य भी दिखलाये गये हैं। इस पर
सिध्दान्त पक्ष का वक्तव्य यह है कि यह कल्पना निराधार व प्राणशून्य
है क्योंकि मरणोत्तार दस महीने तक तो माता के गर्भाशय में अवश्य ही
रहना पड़ता है। साथ ही गर्भाशय में पहुँचाने में जो ईश्वरीय डाक है
उससे स्पष्ट है कि वही पहुँचने से प्रथम किरण,
वायु और मेघादि में क्रमश: प्रवेश द्वारा अन्न में प्रवेश करा देता
है जैसा कि पूर्वोक्त छान्दोग्य और बृहदारण्यक आदि के पंचाग्निविद्या
प्रकरण से स्पष्ट है। इससे क्यों कर कहा जा सकता है कि मरणोपरान्त
तुरन्त ही शरीर मिल जाता है
?
एक बात यह भी विचारणीय है कि जब पारलौकिक व्यवहार अनुमानगम्य है और
पृथ्वी के छोटे-छोटे राज्यों को देखकर तदनुसार ही ईश्वरीय राज्य और
ईश्वर का अनुमान किया जाता है तो उसकी अन्यान्य बातों की कल्पना भी
प्रत्यक्षानुसारिणी ही होनी चाहिए। बस इसी नियम के अनुसार स्वर्ग,
नरक,
यमपुरी,
और यमदूत आदि की कल्पना की गयी है। कारण,
देखा जाता है कि यहाँ के छोटे-छोटे राजे अपने-अपने राज्य में
प्रतिष्ठा की पदवियाँ एवं स्थान सत् कार्यों के लिए रखते हैं। उसी
प्रकार असत् कार्यों,
अपराधों के लिए अप्रतिष्ठा सूचक स्थान कारागारादि रखते व अपराध आदि
के निर्णय के लिए छोटे बड़े न्यायालय क्रमश: बनाने उनमें विभिन्न
पदाधिकारी कार्यानुसार रखते,
दण्डनीय व्यक्तियों के पकड़ने के लिए वैसे कर्मचारी रखते एवं
सत्कार्यों की सूचना के लिए कार्यकर्ता रखते हैं। ठीक इसी तरह
पारलौकिक व्यवहार में सत्कार्यों के लिए स्वर्गादि तथा असत् कार्यों
के लिए नरक,
वैतरणी आदि की कल्पना की गयी है। यमराज को न्यायकर्ता समझना चाहिए
क्योंकि यम का अर्थ है दण्ड देने वाला। इसी तरह यमदूतादिक और
स्वर्गीय दूतों को भी समझना चाहिए। इससे विपरीत जो कोई भी कल्पना
होगी वह प्रत्यक्षानुसारिणी न होने के कारण श्रध्देय नहीं हो सकती।
फिर यह बात कहाँ रह गयी कि यमपुरी आदि में जीव नहीं जाते
?
फिर श्राध्द किनके लिए किया जाय। मरणोपरान्त शीघ्र जन्म के विषय में
जो गीता का वाक्य कहा गया है वह भी इसके भाव को हृदयंगम न कर सकने के
कारण ही। क्योंकि वहाँ कपड़े का दृष्टान्त केवल इसी अंश में दिया गया
है कि एक शरीर से दूसरे में जाने में आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता
है जैसा कि कपड़ा पहिनने वाला एक को छोड़ने व दूसरे को पहिनने में।
दृष्टान्त को सब अंशों में नहीं घटाना चाहिए क्योंकि ऐसा कहीं नहीं
किया जाता। नहीं तो यह भी स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ेगा जैसे
कपड़ा पहनने वाला नये कपड़े पहनकर पश्चात् पुराने को उतारता है वैसे ही
जीव भी नये शरीरों को प्राप्त कर लेने पर पीछे से पुराने शरीर को
छोड़ता है।
यदि यमपुरी आदि को न मानकर भी तुरन्त ही शरीरान्तर का स्वीकार थोड़ी
देर के लिए मान लिया जाय तो भी शरीरान्तर में रहने वाले ही जीव के
लिए श्राध्दादि का किया जाना अपरिहार्य होगा। इस विषय में ध्यान
रखना चाहिए कि यदि श्राध्दादि के विषय में पूर्वोक्त अन्तर्राष्ट्रीय
नियम के सदृश ईश्वरीय प्रबन्ध में नियम न माने जायें तो जन्मान्तर की
अपनी दी या की हुई वस्तुएँ अपने को मिलती हैं इसमें कोई प्रमाण न मिल
सकेगा। कारणयदि हमने पूर्व जन्म में केवल घास में देकर वही वस्तुएँ
अपने लिए दूसरे को दी हों अथवा परोपकारादि दूसरे ही धर्मकार्य किये
हों और मरणोत्तार हमें हंस या पशु का शरीर मिल जाय तो वहाँ केवल मोती
अथवा घास क्योंकर मिल सकेंगे। और अन्य पदार्थ तो मिलते देखे जाते
नहीं। अत: यह नियम नहीं माना जा सकता कि अन्य के अथवा अपने लिए जो ही
पदार्थ दिये अथवा किये जाते हैं शरीरान्त या परलोक में वही अविकल
रूप से मिला करते हैं।
इसी तरह जो लोग यह शंकाएँ किया करते हैं कि यद्यपि जो कर्म
दृष्टार्थक हैं अर्थात् जिनका फल इसी जगह मिलने वाला है,
जैसे वृष्टि के लिए किया गया कारीरी याग,
उनके विषय में सन्देह नहीं हो सकता,
कारण उनके फल प्रत्यक्ष प्रमाण गोचर हैं। तथापि स्वर्गादि अदृष्ट
फलार्थक जो कर्म हैं प्रमाण हैं
?
इत्यादि उनके लिए मीमांसकप्रवरों की यह युक्ति है कि वेदों या
महर्षियों के उपेदशों के एक अंश को प्रामाणिक देखकर परोक्षांश में भी
प्रत्यक्षांशवत् ही सप्रमाणता का अनुमान कर लेना चाहिए। क्योंकि जब
इस बात में कोई भी प्रमाण नहीं है कि वे लोग स्वार्थी अथवा अकारण
परोपकारी थे-कारण,
जंगलों में सर्वसुख-परित्याग पूर्वक तप आदि सत्कर्मों में ही
अद्दोरात्र दत्तचित्त रहा करते थे एवं प्राप्त संपदाओं तथा
प्रतिष्ठाओं की अवहेलना कर कणभक्षण में ही अपने को
कृत्कृत्य
और
वल्कलवस्त्रधारण
से ही सन्तुष्ट समझते थे। हाँ,
उनकी सत्यता में क्या परहितार्थ शरीरत्याग तक कर
डालते थे जिसके शतश: दृष्टान्त महर्षि दधीचि
प्रभृति पड़े हैं-तो फिर क्योंकर कहा जा सकता है कि उन लोगों ने जनता
के प्रतारणार्थ ही यह उपदेशाडम्बर रचा था। यह भी देखा जाता है कि तब
उन्हीं के बनाये हुए आयुर्वेद एवं ज्योतिषशास्त्र
अक्षरश: प्रामाणिक सिध्द हो रहे हैं और तुलसी
पत्र,
गोमूत्र
एवं गोमय तथा निम्ब के वृक्षों की जो महिमा उन्होंने भर पेट गायी है
उसे आधुनिक
वैज्ञानिक मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं तो फिर पारलौकिक कर्मों के
सम्बन्ध
में उनके उपदेश क्योंकर प्रमाण नहीं माने जावेंगे
? इसी तात्पर्य से न्याय दर्शन में कहा गया है कि
मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवद्यतत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात् (2।1।69)
इसका तात्पर्य वही है जो ऊपर दिखलाया जा चुका है।
महर्षिवात्स्यायन ने भी कहा है स ने मन्येत दृष्टार्थ एवाप्तो देश:
प्रमाणमर्थस्यावधरणादिति,
अदृष्टार्थोऽपि प्रमाणमर्थस्यानुमानादिति। (1।1।8)।
अर्थात् ऐसा न समझना चाहिए कि दृष्टार्थक कर्म ही प्रामाणिक हैं,
क्योंकि उनका फल प्रत्यक्ष है वरन् अदृष्टार्थक
कर्मों के भी फलों का इन्हीं द्वारा अनुमान करके उन्हें भी तुल्य रूप
ही प्रामाणिकता मिलनी उचित है।
जिन युक्तियों का ऊपर दिग्दर्शन कराया गया है ऐसी ही दार्शनिक
रीतियों से मीमांसकानुयायी पंडितों ने दृष्टार्थक एवं अदृष्टार्थक
द्विविधा कर्मों की प्रामाणिकता अक्षुण्ण रूप से स्थापित की है।
यद्यपि लोग कहा करते हैं कि पूर्वोक्त यमपुरी आदि की कल्पनाएँ
पौराणिक है क्योंकि दार्शनिक ग्रन्थों में उनका उल्लेख नहीं है।
तथापि यह बात ठीक नहीं है। कारण न्यायर्वात्तिक में इस बात का स्पष्ट
उल्लेख है। ऐसा न भी मानें तो भी इन पौराणिक कल्पनाओं की प्रामाणिकता
बिना पूर्वोक्त मीमांसकों की दार्शनिक युक्तियों को छोड़ अन्यथा सिध्द
नहीं हो सकती है। अतएव इन कल्पनाओं की मीमांसा दर्शन का ही प्रपंच
(विस्तार) मानना युक्तियुक्त और विद्वत्सम्मत है।
न्यायर्वात्तिककार भगवान् उद्योतकराचार्य ने अपने र्वात्तिक में इस
प्रकार स्पष्ट रूप से वैतरणी नदी का वर्णन विज्ञानवादी बौध्द के
मतखण्डन प्रसंग में किया है-
'अथ
मन्यसे यथा तुल्यकर्मविपाकोत्पन्ना: प्रेता: पूयपूर्णां नदीं
पश्यन्ति। न तन्न नद्यस्ति,
न पूयं,
न ह्येकं वस्त्वनेकाकारं भवितुमर्हति। दृष्टाश्च विज्ञानभेद: के
चित्तमेव जलपूर्णां पश्यन्ति,
केचित् रुधिरपूर्णामिति।'
(न्याय.
वा. अ.
4,
अ.2
सू.
34)
यदि विज्ञानवादी की यह शंका हो कि जिस प्रकार मरणोत्तार यमपुरी के
मार्ग में एक ही प्रकार के दुष्कर्म से यातना (शास्ति) शरीर पानेवाले
मृतक पीव आदि से पूर्ण नदी (वैतरणी) का अनुभव करते हैं और वहाँ
वस्तुत: वैसी नदी है। साथ ही दूसरे प्रकार के मृतक (प्रेत) उसी नदी
को जलपूर्ण देखते हैं और यह सम्भव नहीं कि एक ही वस्तु (नदी) अनेक
विरुध्द प्रकारों की हो जावे। इससे मानना होगा कि वहाँ पूय (पीव)
पूर्ण नदी न होने पर भी किसी दोषवश उन्हें प्रतीत होती है। ठीक यही
दशा संसार की भी है। यद्यपि यहाँ भी पदार्थ वस्तुत: नहीं हैं,
तथापि दोष वश ही प्रतीत भर होते हैं। इत्यादि। इससे निर्विवाद सिध्द
है कि यह यमपुरी आदि की कल्पना दार्शनिकों को भी मान्य है।
यहाँ इस बात को भी विस्मृत न होने देना चाहिए कि सामग्री के रहने
परहीकार्य हुआ करता है,
न कि एकाध कारण मात्र के रह जाने से। सकल कारण-कारणसमूह वा साकल्य-को
ही सामग्री कहते हैं। यह कभी नहीं देखा जाता कि केवल अग्नि,
स्थाली वा काष्ठादि अथवा इनमें से दो या तीन के भी होने से पाक
(रसोई) कभी भी निष्पन्न हो जावे। इस कथन का प्रकृत में यह उपयोग है
कि जिसके उद्देश्य से वा जिसके लिए श्राध्दादि किये जाते हैं उसे वे
उसी दशा में प्राप्त हो सकेंगे जबकि उनकी प्राप्ति की सामग्री
विद्यमान हो। उन वस्तुओं को मृत पितादि के पास पहुँचाने के लिए
जिन-जिन कारणों की आवश्यकता होती है उनमें अज्ञान वा सांसारिकता भी
एक है,
तात्पर्य यह कि जब तक वह मृतक मुक्त न हो जावेगा तभी तक वे पदार्थ
उसे मिल सकेंगे। या यों कहिए कि जब तक उसे उनकी आवश्यकता बनी रहे,
योग्यता बनी रहे और उसे उनका इन्कार या उनकी कामना का परित्याग न हो
गया हो। कारण,
मुक्त की सभी वासनाएँ विलीन हो जाती हैं,
और वह मुक्ति से प्रथम ही ब्रह्मलोक पर्यन्त को तृणवत् समझता है। लोक
में भी देखा जाता है कि जिसके पास कोई पदार्थ डाक द्वारा भेजा जावे
पर उसमें किसी प्रकार की अयोग्यता ऐसी आ पड़े जिससे वह न पा सकता हो
तो कभी भी नहीं पाता और इन्कार वा अस्वीकार की भी दशा में वह
प्रेरित पदार्थ प्रेरक को ही प्राप्त हो जाता है। अत: मुक्त पुरुषों
के लिए जो श्राध्दादि होते हैं-क्योंकि करनेवाले को क्या मालूम कि
उसके मृत पितादि मुक्त हो गये हैं-वे न तो मुक्त पुरुष को ही मिलते
और न व्यर्थ ही हो जाते हैं,
वरन् उनका फल कर्ता को ही मिलता है। या यों कहिये कि वे कर्ता के पास
लौट आते हैं और उसे इस जन्म या जन्मान्तर में मिलते हैं,
क्योंकि पारलौकिक पुण्य-पापों के भी फल कभी-कभी पर बहुत ही कम,
इस जन्म में भी प्राप्त हो जाया करते हैं। जैसा कि अभियुक्त पुरुषों
का वचन है कि-
त्रिभिर्वर्षैस्त्रिभिर्मासैस्त्रिभि: पक्षैस्त्रिभिर्दिनै:।
अत्युत्कटै: पुण्यपापैरिहैव फलमश्नुते॥
-अत्यन्त
उत्कट पुण्य-पापों के फल इसी जन्म में उनको योग्यता के अनुसार तीन
वर्षों,
तीन महीनों,
तीन पक्षों वा तीन दिनों में ही मिल जाया करते हैं। इससे दैवात्
मुक्त पितादि पर ध्यान देकर श्राध्दादि के वैयर्थ्य की जो शंका हो
सकती या हुआ करती है वह भी नहीं हो सकती। अतएव अब इस बात के स्वीकार
में आनाकानी नहीं की जा सकती कि जिन कर्मों को हम पौराणिक कह माना
करते हैं और वैदिक नाम से किया करते हैं वे सभी पूर्व मीमांसा दर्शन
के ही विषय हैं। अत: उन्हें केवल पौराणिक नहीं कह सकते। अथवा यदि
किसी को उन्हें ऐसे ही मानने का आग्रह वा अभिनिवेश हो तो भले ही रहे,
तथापि उन्हें प्रामाणिक सिध्द करना मीमांसा दर्शन का ही काम है जैसा
कि प्रथम कहा गया है। इसी बात को भट्ट कुमारिल स्वामी ने अपने
मीमांसार्वात्तिक में एक स्थान पर यों कहा है :
धार्मे प्रमीयमाणे हि येदेन करणात्मना।
कृतिकर्तव्यता भांग जीवांचा पूरयिष्यति॥
-जिस
प्रकार काष्ठच्छेदन क्रिया में परशु करण (साधन) होता है और उसका
उद्यमन निपातन इतर्कर्तव्यता वा क्रियानिष्पादन का प्रकार।
क्योंकि परशु से क्योंकर काष्ठच्छेदन किया जावे ऐसी जिज्ञासा होने
पर यही कहा जाता है कि उसे ऊपर उठा एवं काष्ठ पर गिरा कर। ठीक इसी
प्रकार जब धर्म के स्वरूप अथवा उसकी प्रामाणिकता का निर्णय किया
जाता है तो उस निर्णय क्रिया में वेद (क्योंकि स्मृतियाँ,
पुराणों और सदाचारों को भी वेदमूलक होने से ही मीमांसक लोग धर्म
में प्रमाण माना करते हैं) करण होते हैं और मीमांसा ही
इतर्कर्तव्यता हुआ करती है। अर्थात् जैसे उद्यमन निपातन बिना
काष्ठच्छेदन नहीं हो सकता,
वैसे ही मीमांसा दर्शन की युक्तियों एवं प्रमाणों के बिना धर्म के
स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता। अतएव भगवान् मनु ने कहा है कि-
आर्ष धार्मोपदेशं च वेदशास्त्रविरोधिना।
यस्तर्केणानुसन्धात्रो स धार्मं वेद नेसर:॥ (म. अ.
12,
श्लोक 106)
'जो
वेदों एवं स्मृत्यादि के धर्मोपदेशों का विचार तदगुण मीमांसा दर्शन
की युक्तियों (न्यायों वा तर्कों) द्वारा करता है वही धर्म के
वास्तविक स्वरूप को जानता है न कि अन्य भी।'
पूर्वोक्त कुमारिल स्वामी के र्वात्तिक में केवल धर्म शब्द आया न कि
कोई विशेष शब्द और मीमांसक लोग वेदमूलक होने से पुराणादि को भी उसी
तरह प्रामाणिक मानते हैं,
तथा मनुजी का पूर्वोक्त वाक्य भी इसी बात का पोषक है। ऐसी दशा में
सभी सनातन धर्म स्वरूप प्रासादों को मीमांसा दर्शन की युक्ति स्वरूप
भित्तियों पर अवलम्बित मानना ही युक्तिसंगत है। अस्तु।
जिन युक्ति-प्रमाणों का अबतक दिग्दर्शन कराया गया है,
अथवा यों कहिये कि जिन प्रमाणों के आधार पर मीमांसक लोग धर्माधर्म के
गहन तत्तवों का निर्णय करामलकवत् करते और विरुध्द मतवादियों के मतों
का यौगिक निराकरण करते हैं,
उन्हें उन लोगों ने छ: भागों में विभक्त किया है। उनके नाम प्रत्यक्ष
अनुमान,
आगम (शब्द) उपमान,
अर्थ तथा अनुपलब्धि हैं। यद्यपि धर्म के स्वरूप निर्णय में केवल आगम
(शब्द) प्रमाण ही अपेक्षित है और सच पूछा जावे तो उसी की वहाँ गति है,
जैसा कि प्रथम सविस्तर दिखलाया जा चुका है और महर्षि जैमिनि को भी
अभिमत है। कारण वे खिलते हैं कि-
औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य
ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपलब्धो तत्प्रमाणं बादरायणस्यान
प्रेक्षत्वात्।
(मी. अ.1,
पा.1,
सू.
5)
वेदादिवाक्य रूप आगम ही धर्म में प्रमाण है क्योंकि शब्द और अर्थ का
सम्बन्ध नित्य है और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका कभी भी बाधा
नहीं होता तथा उसे किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। अतएव वह
प्रकारान्तर से अविदित अर्थ का ही बोधक होता है। यह बात
बादरायणाचार्य भी मानते हैं। मीमांसा दर्शन भाष्य में भी इस स्थल पर
ऐसा ही प्रतिपादन किया गया है। तथापि वैदिक धर्म की प्रतिद्वन्द्विनी
जितनी शंकाएँ और उसके विरोधी जितने मतवाद हैं उनका खण्डन सप्रमाण
किये बिना धर्मस्वरूप का निर्णय सर्वथा असम्भव है। साथ ही पूर्वापर
सन्दर्भ-निर्णय बिना प्रत्यक्ष और अनुमानादि के हो सकता नहीं। इसीलिए
शब्द से भिन्न भी पाँच प्रमाणों का अवलम्बन मीमांसा धुरीणों ने किया
है। यद्यपि मीमांसा दर्शन के अनन्तर होनेवाले न्यायदर्शन में चार ही
प्रमाण माने गये हैं और अन्त के दो त्याग दिये गये हैं,
तदुपरान्त वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही माने गये
हैं पुन: सांख्य और योग ने प्रत्यक्ष,
अनुमान एवं शब्द तीन ही माने हैं। तथापि उन लोगों ने उन्हीं से अन्य
प्रमाणों के काम चलाकर उनमें उनका अन्तर्भाव कर दिया है। अत: इस विषय
में विवाद किसी दर्शन को भी नहीं है,
केवल नाम और प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न हैं। क्योंकि ये दर्शन सभी
लोगों को ऊहापोहकुशल बनाते हुए परमात्मा तक पहुँचा देने के ही लिए
प्रवृत्ता हुए हैं। परन्तु मीमांसकों की दृष्टि संकुचित नहीं है।
अतएव कुछ ही प्रमाण नाम के लिए स्वीकार कर उन्हीं से इतर प्रमाणों का
भी काम चलाना उन्होंने गुरुतर तथा क्लेशजनक समझ त्याग दिया है और
व्यापक दृष्टि का अवलम्बन कर उन्होंने छ: प्रमाण स्वीकृत किये हैं।
यह तो हुई पूर्वमीमांसा दर्शन की बात। ठीक यही दशा उत्तरमीमांसा या
वेदान्त दर्शन की भी है। उसने भी छ: ही प्रमाण माने हैं। कारण उसकी
दृष्टि तो और भी व्यापक और उदार है। इस प्रकार प्रमाणों की उतरती और
चढ़ती सीढ़ी छ: प्रमाणों से प्रारम्भ होकर छ: ही पर विश्राम लेती है।
इनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे भी
प्रत्यक्ष ही कहते हैं। एवं अनुमान से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति शब्द
से शाब्दबोध,
उपमान से उपमिति,
अर्थापत्ति से अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान को
अभावनिश्चय कहा करते हैं।
इन्द्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। परन्तु यह धारणा साधारण
है। किसी-किसी के मत में इन्द्रिय तथा विषय का सन्निकर्ष ही
प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। परन्तु इससे भी आगे बढ़कर बहुतेरे लोग
उससे उत्पन्न ज्ञान को ही प्रत्यक्ष माना करते हैं। इसी प्रकार
अनुमिति शब्द प्रभृति के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए। अतएव
भट्टाचार्य ने मीमांसार्वात्तिक में लिखा है कि-
प्रमाणं चापि शब्दो वा तज्ज्ञानं वा निरूप्यते।
पदार्थ
स्तन्मतिर्वास्याद् वाक्यार्थाधिगमोऽथवा॥10॥(अ.1,
पा.1,
सू. 2)
प्रमाण शब्द को भी कहते हैं और उसके ज्ञान,
पदार्थ,
पदार्थज्ञान अथवा वाक्यार्थबोध को भी। शब्द प्रमाण का प्रकरण था,
इससे उन्होंने केवल शब्द प्रमाण के सम्बन्ध में होने वाले ही मतभेदों
का वहाँ उल्लेख किया है। यही बात तुल्य न्याय से अन्य प्रमाणों के
विषय में भी उन्हें इष्ट है। अतएव भाष्यकार शबरस्वामी चतुर्थ सूत्र
के भाष्य में स्पष्ट ही लिखते हैं कि-बुध्दिर्वा,
जन्मवा,
सन्निकर्षो वा नैषां कस्यचिदवधरणार्थं सूत्रम्।
-चतुर्थ
सूत्र इस निर्णय के लिए नहीं बना है कि इन्द्रिय सन्निकर्ष,
बुध्दि,
जन्म अथवा बुध्दि में से किसी अमुक को ही प्रमाण मानना चाहिए। इसी
प्रकार प्रमिति (प्रमा) वा फल के विषय में भी समझ लेना होगा कि
इन्द्रिय अथवा सन्निकर्ष आदि को प्रमाण मानने पर विषयज्ञान वा
वाक्यार्थ बोध ही फल (प्रमा) कहलाता है पर,
जब उसे ही प्रमाण मान लेते हैं तो हानि,
उपादान वा उपेक्षा अथवा प्रवृत्ति,
निवृत्ति या उदासीनता के ही ज्ञान को फल मानते हैं। कारण,
ज्ञानोत्तर इष्ट वस्तु द्रव्यादि की बुध्दि स्वभाविक होती है। एवं
अनिष्ट सर्पादि में निवृत्ति भिन्न मार्ग पतित तृणादि में उपेक्षा
बुध्दि का हो जाना अनिलिये पूर्व प्रसंग में ही र्वात्तिककार ने भी
कहा है कि हेतु प्रमाणत्वे फलताऽन्तस्य गम्यते। दे को प्रमाण मानने
में वाक्यार्थ बोधदि ही फल कहलाते हैं। मिश्र भी यही बात कहते हैं,
शब्दादीनां प्रामाण्ये म: फलं तत्प्रामाण्येहानादि बुध्दि: फलमिति,
इसका अर्थ में प्रवृत्ति करने की बुध्दि स्वाभाविक होती है। एवं
अनिष्ट सपादि में निवृत्ति तथा दोनों से भिन्न मार्ग पतित तृणादि में
उपेक्षा बुध्दि का हो जाना अनिवार्य है। इसीलिए पूर्व प्रसंग में ही
र्वात्तिककार ने भी कहा है कि-
'पूर्वेषांतु
प्रमाणात्वे फलताऽन्तस्य गस्यते।'
शब्दादि को प्रमाण मानने
में वाक्यार्थ बोधादि ही फल कहलाते हैं। श्री पार्थ सारथि मिश्र भी
यही बात वहाँ कहते हैं, शब्दादीनां प्रामाण्ये वाक्यार्थाधिगम: फलं
तत्प्रामाण्येहानादि बुध्दि: फलमिति, इसका अर्थ पूर्वोक्त ही है।
(शीर्ष पर वापस)