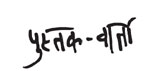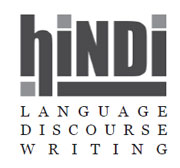पूजा के भेद
गीता
की एक और बात भी बड़े ही मार्के की है। आमतौर से यही समझा जाता है कि
कण्ठी-माला जपना,
चन्दन-अक्षत और पत्र-पुष्प
आदि चढ़ाना तथा घण्टा-घड़ियाल वगैरह बजा के
धूप,
दीप, आरती और भोगराग अर्पण
करना यही भगवान् की पूजा है। तीर्थ-व्रत आदि करने,
भगवान्
के गुणों को वर्णन करने वाले ग्रन्थों का पाठ करने,
स्तुति करने और गीत-भजन ऊँचे स्वर से गाने को भी किसी
कदर पूजा मान लेते
हैं।
ऑंखें बन्द करके
ध्यान
में बैठना तो
भगवान्
की भक्ति जरूर ही है। प्राय: देखा जाता है कि
भगवान्
के प्रेम के नाम पर ऑंखों में नकली ऑंसू भर के कभी-कभी भक्त नामधारी
लोग रोते भी
हैं।
रामलीला के नाम पर नाटक वगैरह का जो प्रपंच फैलाया जाता है उसे भी पूजा के
भीतर ही मानते
हैं।
आजकल तो रसिक सम्प्रदाय और सखीसम्प्रदाय के नाम पर नाचने-गाने के अलावा
जानें क्या-क्या नकलें की जाती
हैं
और
स्त्री
बनने का भी स्वाँग रचा जाता है। इसे भी भगवद्भक्ति ही मानने की बीमारी तेजी
के साथ फैल रही है।
मगर गीता
ने एक निराला ही रास्ता निकाला है और इस तरह ऐसा करने वालों का सौदा ही
फीका कर दिया है। बेशक,
दुनिया को दिखाने के लिए नहीं,
किन्तु भीतरी श्रद्धा के साथ,
जो
कुछ पत्र,
पुष्प आदि भगवान् के नाम पर अर्पण किया जाता है उसे भी नवें अध्याय के
'पत्रां
पुष्पं' (26)
श्लोक में पूजा कहा है। मगर वहाँ
'भक्त्या'
और
'प्रयतात्मन:'
के
साथ ही जो 'भक्त्युपहृतं'
कहा है उससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि सरल स्वभाव और निष्कपट मन से
श्रद्धा और प्रेम के साथ जो कुछ किया जाता है उसे ही भगवान् स्वीकार करते
हैं और वही उनकी पूजा है। श्रद्धा-भक्ति की जरा भी कमी हुई और यह बात चौपट
हुई। तब तो यह कोरा रोजगार हो जाता है। दो बार
'भक्ति'
शब्द एक ही श्लोक में कहने का मतलब ही यही है कि छलछलाते प्रेम और सच्ची
श्रद्धा के साथ ही ऐसा करना पूजा मानी जा सकती है। नरसी मेहता और नामदेव
आदि भक्तों के बारे में ऐसा ही कहा जाता है। शबरी तथा विदुर की ऐसी ही बात
सर्वजन विदित है।
यह तो हुई
एक पूजा। लेकिन यह है बहुत ही संकुचित। इसमें कितने ही बन्धन जो लगे हुए
हैं। पूजा के लिए पत्र,
पुष्प आदि लाना और उसकी खासतौर से तैयारी करना इस बात के लिए जरूरी हो जाता
है। इसलिए यह पूजा निराबाध नहीं चल सकती। इसका दिन-रात चलना भी असम्भव है।
आखिर घर-गिरस्ती सँभालना तो पड़ता ही है। अपने शरीर-सम्बन्धी मल-मूत्र त्याग
आदि की क्रियाएँ तथा खान-पान वगैरह भी तो जरूरी हैं। समय-समय पर लोगों से
बातचीत और सोना-जागना भी आवश्यक है। यदि कोई नौकरी-चाकरी या मजदूरी करते
हैं तो उस समय भी यह काम नहीं हो सकता है। यदि हल चलाते,
खेत खोदते,
विद्यार्थी की दशा में पाठ का अभ्यास करते और सिपाही बन के पहरा देते हैं,
तो
भी यह पूजा नहीं हो सकती। बीमार हो जाने पर भी यह चीज असम्भव है। इस प्रकार
हजार बाधाएँ मौजूद हैं जिनसे यह पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए गीता ने बहुत
ही आसान और सर्वथा सर्वदा सुलभ मार्ग बताया है।
नवें
अध्याय का जो
'पत्रां
पुष्पं'
श्लोक पहले बताया है उसी के बाद के
27
और 28
दो श्लोकों में जो कुछ भी कहा गया है उससे सभी दिक्कतें और बेबसियाँ दूर हो
जाती हैं। हाँ,
अपने मन की दिक्कतें रहती हैं जरूर। मगर इसका तो कोई बाहरी उपाय है नहीं।
यह खुद हटाने की चीज है। मन की शैतानियत तो दूसरा कोई दूर कर सकता नहीं।
हाँ,
तो उन
श्लोकों में पहले यज्ञ,
दान और तप के नाम से तीन कामों को गिना के कहा है कि इन्हें करके भगवदर्पण,
मदर्पण,
मुझे अर्पण करो। मगर फिर इनमें भी वही दिक्कतें और बाधाएँ समझ के आखिर में
कह दिया है कि इन्हें तो नमूने के तौर पर गिना दिया है। असल में जो कुछ भी
करते हो, 'यत्करोषि',
उसे ही भगवान् को अर्पण करो। इसका सीधा मतलब यही है कि जो भी काम करते हो
सभी कुछ भगवदर्पण बुद्धि से,
यह
समझ के कि यह भगवान् की पूजा ही रूपान्तर में हो रही है,
करो। चौबीस घंटे में जो कुछ भी किया जाय-और इसमें सोना,
मल-मूत्र त्याग आदि भी आ ही जाता है-सभी के मुतल्लिक एक ही भावना होनी
चाहिए,
एक
ही खयाल होना उचित है कि यह तो और कुछ नहीं है;
केवल भगवान् की पूजा है। इसी खयाल का अभ्यास होने से ही काम चल जाता है।
फिर तो लोक-परलोक के लिए दूसरी चिन्ता-फिक्र करने की जरूरत ही नहीं होती।
काम का काम हुआ और भगवान् की पूजा भी हो गयी!
'आम
के आम रहे और गुठली का दाम भी मिल गया!'
इसे ही 'एक
पन्थ दुइ काज'
कहते हैं।
गीता में
यह बात किसी न किसी रूप में बार-बार आती गयी है और अन्त में अठारहवें
अध्याय की समाप्ति के पहले भी
45
और 46
श्लोकों में यही बात कही गयी है। वहाँ तो
'स्वकर्मणा
तमभ्यचर्य'-''अपने-अपने
कर्मों से ही उस भगवान् की पूजा अच्छी तरह करके''-ऐसा
साफ ही कह दिया है। यज्ञ,
दान आदि का वहाँ नाम भी नहीं ले के केवल
'स्वकर्म'
को
ही पूजा के रूप में बताया है। खूबी तो यह है कि
'स्वधर्म'
भी
नहीं कह के 'स्वकर्म'
कहा है। धर्म और कर्म गीता की नजरों में तो पर्यायवाची हैं और दोनों का एक
ही अर्थ है। मगर सर्वसाधारण का खयाल तो ऐसा है नहीं। वे तो धर्म कुछ और ही
चीज मानते हैं। साधारण क्रिया को तो वे धर्म मानते नहीं। उनके लिए तो विशेष
प्रकार का कर्म ही धर्म है। इसीलिए यहाँ
'स्वकर्म'
कह
दिया है। ताकि लोग भूलभुलैया में न पड़े रहें और क्रिया मात्र को ही पूजा के
रूप में समझने एवं मानने की कोशिश करें,
ऐसा ही मानें।
श्रीमद्भागवत में भी राजा रहूगण और मस्तराम जड़भरत के संवाद में कहा गया है
कि ''स्वधर्म
आराधानमच्युतस्य यदीहमानो विजहात्यघौघम्''
(5।
10।
23)।
इसका आशय यह है कि
''अपने
कर्तव्यों का पालन करना ही भगवान् की पूजा है,
जिसके चलते पाप का पहाड़ भी खत्म हो जाता और नजदीक नहीं आता है।''
रहूगण ने अपने राज्यकार्य संचालन और शासन आदि को ही लक्ष्य करके ऐसा कहा
है। लोग यह न समझें कि दंड देने का काम तो बीभत्स है,
इसीलिए उनने कह दिया है कि वह तो राजा का कर्तव्य होने के कारण भगवत्पूजा
ही है। बेशक,
यहाँ स्वकर्म न कह के स्वधर्म कहा है। मगर मतलब एक ही है। यदि दंड आदि रूप
सख्त काम और अमल एवं मार-काट तथा युद्ध को पूजा कह सकते हैं,
ये
सभी काम यदि पूजा ही हैं,
तो
लोगों के सभी साधारण कामों का क्या कहना?
वे
तो आसानी से उस पूजा के भीतर आ ही जाते हैं।
यहाँ
'स्वधर्म'
और
गीता में जो
'स्वकर्म'
कहा है इन दोनों में
'स्व'
शब्द देकर यही बताया गया है कि खुद कर्मों के अच्छे-बुरे होने की कोई बात
नहीं। अपने-अपने कर्म ही पूजा बन जाते हैं। उनकी बाहरी बनावट और रूपरेखा
कोई चीज होती नहीं। इसीलिए अपने खराब कामों को छोड़ दूसरों के अच्छों की ओर
झपट पड़ना भी ठीक नहीं।
'अपने'
का
अर्थ है हरेक के लिए जो निर्धारित या तयशुदा
(assigned)
हैं।
पूजा को
ऐसा रूप देने में एक बहुत ही बड़ी खूबी और भी है। सभी चाहते हैं कि हरेक काम
अच्छी तरह पूरा हो और सुन्दरता के साथ किया जाय। हरेक चीज की सबसे बड़ी खूबी
है उसकी पूर्णता। यदि अधूरापन किसी भी काम में रहने न पाये तो संसार मंगलमय
बन के ही रहे। मगर यही बात नहीं हो पाती और लापरवाही,
अन्यमनस्कता आदि कितनी ही चीजें इसकी वजह हैं। लोग अकसर यह भी समझते हैं,
खासकर जब कोई कठिन,
परन्तु अप्रिय,
काम उन्हें सौंपा जाय,
कि
'गले
पड़ी,
बजाये
फुर्सत।'
इसीलिए जैसे-तैसे उसे कर-कराके अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए जरूरत
है इस बात की कि लोगों में काम के लिए अनुराग पैदा किया जाय,
उनमें उसकी धुन लाई जाय और ऐसा किया जाय कि काम के लिए उनमें आग पैदा हो।
यही बात इस पूजा वाली प्रक्रिया से हो जाती है। जब लोग समझने लगते हैं कि
हम जो कुछ भी करते हैं वह भगवान् की पूजा ही है तो खामख्वाह मनोयोगपूर्वक
करना चाहते हैं। दिल में यह खयाल हो आता है कि पूजा में कोई कोर-कसर न रह
जाय। इसलिए धुन और लगन के साथ सच्चे प्रेम से अपने-अपने काम न सिर्फ करते
हैं,
बल्कि
उन्हें पूर्ण बनाने के लिए सिरतोड़ परिश्रम करते हैं। जब आमतौर से किसी भी
बड़े के लिए तैयार की गयी भेंट को सुन्दर से सुन्दर बनाने की कोशिश की जाती
है तो फिर बड़ों के भी बड़े-सबसे बड़े-के लिए होने वाली हमारे कामों की भेंट
क्यों न सर्वात्मनां सुन्दर बनाई जाय?
इसमें बाहरी खर्च-वर्च और परेशानी की भी बात नहीं है। यहाँ तो केवल मनोयोग
का प्रश्न है। इस प्रकार सभी काम पूर्ण होंगे और संसार सुखमय होगा।
(शीर्ष पर वापस)
गीता का योग
योग
शब्द के कितने अर्थ गीता में माने गये
हैं
यह बात तो आगे बताई जायगी। मगर गीता का जो अपना योग है,
जिसका ताल्लुक कर्मयोग से है और जो गीता की अपनी खास
देन है वह जानने की चीज है। यों तो उसका जिक्र कई स्थानों पर आगे भी आया
है। लेकिन दूसरे अध्याय
के 'एषा
तेऽभिहिता' (39) श्लोक से जिस योग की भूमिका
शुरू करके 'कर्मण्येवाधिकारस्ते'
(47) तथा उसके बाद वाले (48वें)
श्लोक में जिस योग का वर्णन है वही गीता का निजी योग है। इन दोनों श्लोकों
को मिलाकर ही उसका रूप पूरा हुआ है। आगे के 50वें
श्लोक में उसी योग का निचोड़ या संक्षिप्त रूप 'योग:
कर्मसुकौशलम्' शब्दों में बताया है। लोग कहीं
ऐसा न समझ बैठें कि पहले बताया गया योग कोई दूसरी ही चीज है,
इसीलिए गीता साफ कहे देती है कि वह और कुछ नहीं है
सिवाय कर्म करने की चातुरी, उसकी कुशलता,
विशेषता
(specialism)
के।
कोई मनुष्य कर्मों के करने में विशेषज्ञ
(specialist)
हो
जाता है उसे ही योगी या कर्मयोगी कहते
हैं।
उसे ऐसी हिकमत मालूम हो जाती है कि कर्मों के करते रहने पर भी
बन्धन
में नहीं फँस सकता और निर्वाणमुक्ति या ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त कर लेता है।
योग शब्द का यों भी युक्ति या उपाय अर्थ माना जाता है और कर्म के
सम्बन्ध
की यह हिकमत भी युक्ति ही तो है।
यह युक्ति,
हिकमत या विशेषज्ञता क्या है और कैसे प्राप्त होती है,
यही बात 47
और 48
श्लोकों में बताई गयी है। अगर कर्म,
क्रिया,
काम या अमल को हम दायरे या वृत्त के रूप में मान लें तो यह बात समझने में
आसानी होगी। तब तो कर्म करने का मतलब होगा मनुष्य का उस वृत्त में घुसना।
गीता की नजरों में कर्म करने वाले के लिए कहा गया है कि
''उसका
हक या अधिकार सिर्फ कर्म तक ही है''-'कर्मण्येवाधिकारस्ते।'
इसका आशय यह है कि हमें उस वृत्त के भीतर ही सीमित या बँधे रहने का ही हक
है-हमें उसके भीतर ही रहना चाहिए। परिधि को डाँकना नहीं चाहिए-परिधि डाँकने
का यत्न हरगिज करना नहीं चाहिए।
'कर्मणि'
के
आगे जो 'एव'
शब्द है वही डाँकने की मनाही करता है,
हमें डाँकने से रोकता है। लेकिन यह तो सूत्र जैसी बात हो जाती है। इसका
स्पष्टीकरण हो जाना जरूरी है। इसीलिए
47वें
श्लोक के शेष तीन चरण (हिस्से) और पूरा
48वाँ-दोनों
ही-यही स्पष्टीकरण करते हैं।
कर्म को
वृत्त करार देने पर मान लें कि करने वाले के आगे वह वृत्त है और उसके तथा
वृत्त के बीच में किसी और चीज की सम्भावना है जिससे उसका वृत्त के साथ
अत्यन्त निकट का सम्बन्ध न हो के बीच में वही चीज आ सकती है-आ जाती है और
इस तरह वृत्त में घुसने में उसे बाधा पहुँचाती है। उसी तरह वृत्त के भीतर
घुसने के बाद वृत्त के बाहर उस आदमी के सामने वृत्त के दूसरे किनारे के उस
पार भी कोई वस्तु है। मतलब यों समझें कि हम पूर्व मुख खड़े हैं और हमारे आगे
एक वृत्त है। मगर वृत्त और हमारे बीच में भी कोई चीज है या हो सकती है जो
हमें वृत्त में जाने से या तो रोकती है,
या
इतना ही होता है कि हम वृत्त में जाने के पहले उस वस्तु से होकर ही गुजरते
हैं और सामने की परिधि पार करके सीधे वृत्त में पूर्व मुख खड़े ही पहुँच
जाते हैं। फिर वृत्त में जाने पर जब परिधि का पिछला भाग न देख के सामने
वाला ही देखते हैं,
तो
उसके आगे-परिधि के पार-पूर्व ओर कोई दूसरी वस्तु भी नजर को आकृष्ट करती है,
कर
सकती है। साथ ही परिधि के भीतर वृत्त में पाँव देने के पहले जो यह कहा गया
है कि किसी और चीज से गुजरने के बाद ही वृत्त में पाँव दे सकते हैं,
वह
चीज एक भी हो सकती है और दो भी। गीता ने शुरू में ज्यादे से ज्यादा दो
चीजों की और पीछे चलकर वृत्त के बाहर आगे की एक चीज की सम्भावना करके
उन्हीं तीनों की रोक लिखी है। कर्म करने वालों को उनमें एक पर भी दृष्टि
नहीं दौड़ाना चाहिए,
एक
का भी खयाल-परवाह-नहीं करना चाहिए,
यही आदेश 40
और 48
श्लोकों के शेष अंशों में दिया है। इन तीनों के सिवाय दायरे (वृत्त) के
भीतर भी वृत्त के अलावा एक चीज है,
एक
खतरा है। उससे भी आगाह कर दिया गया है। जो इन चार खतरों से बच जाता है वही
पक्का योगी या कर्मयोगी होता है,
यही गीता का कहना है।
पहले की
दो चीजों-दो खतरों-में एक है कर्म के फल का खयाल,
उसका चिन्तन,
उसकी इच्छा,
फलेच्छा या फल का संकल्प। मन में फल के स्वरूप की कल्पना करके ही किसी काम
में आमतौर से हाथ बढ़ाते जो हैं। दूसरा है कर्म का त्याग या उसका न करना।
ऐसा होता है कि या तो यों ही कर्म में जी नहीं लगने के कारण उसे करते ही
नहीं;
या यदि फल
की इच्छा या सम्भावना ही न हो तो भी कर्म नहीं करते हैं। इसीलिए कर्म के फल
की इच्छा की ही तरह अकर्म या कर्म का त्याग,
उसे छोड़ देना भी कर्म के पहले ही आ जाता है-यह बात कर्म के दायरे में पाँव
देने के पहले ही आ जाती है। दायरे के बाहर आगे जो चीज दायरे में पाँव देने
पर आती है और जिससे खतरा है वह है उस कर्म का खुद फल ही। कर्म करने के पहले
तो मन में फल का संकल्प मात्र करते हैं। मगर कर्म शुरू कर देने और पूरा
करने तक तो साक्षात् फल पर ही नजर जा पड़ती है। इसीलिए यह भी एक खतरा है।
चौथा खतरा है खुद कर्म से ही-वृत्त या दायरे से ही,
यदि कर्म में आसक्ति,
संग ममता,
अन्धाप्रेम (blind attachment)
हो
जाय। यह कर्म की आसक्ति भी भारी खतरनाक है। यह भी याद रखना चाहिए कि जो
शुरू के दो खतरों में कर्मत्याग को गिनाया है उसका भी मतलब है कर्म के छोड़
देने की आसक्ति या हठ से ही। जैसे कर्म करने की आसक्ति या हठ बुरा है,
ठीक उसी प्रकार उसके न करने का भी हठ खतरनाक है। हठ
किसी ओर नहीं होना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण अभी हुआ जाता है।
हाँ,
तो
अब जरा देखें कि इन चारों खतरों की रोक क्यों कर की गयी है।
47वें
श्लोक के दूसरे हिस्से को हम यों पाते हैं,
''मा
फलेषु कदाचन''-''कर्मों
के फलों में तो हमारा अधिकार कभी नहीं है।''
इस
तरह वृत्त में पाँव देने के बाद जो आगे वाला खतरा है परिधि के बाहर और जिसे
हमने तीसरा कहा है उसे रोक दिया। कर्म के साथ फल का ताल्लुक स्वभावत: होता
ही है। इसलिए कर्म के बाद चटपट उसी से रोकना उचित समझा गया। इसके बाद
47वें
के शेष-उत्तारार्ध्द-में वृत्त के पहले वाले दो खतरों से रोका है
''मा
कर्मफलहेतुभूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि''-''कर्म
के फल के कारण मत बनो,
अर्थात् कर्मफल का खयाल करके काम हर्गिज शुरू न करो।''
फल
के लिए संकल्प और चिन्तन के जरिये ही तो फल तक पहुँचते हैं अब यदि वह
संकल्प या चिन्तन रहा ही नहीं,
फल
का खयाल हुई नहीं तो
'रहा
बाँस न बाजी बाँसुरी'
वाली बात हो गयी और फल से स्वयमेव ताल्लुक बँधा ही नहीं। यही कारण है कि
पहले फल की बात रोक के उसके कारण-स्वरूप फलेच्छा या फल संकल्प की बात पीछे
रोकी गयी है। क्योंकि फल की इच्छा या संकल्प होने पर तो फल तक पहुँचना रुकी
नहीं सकता।
इस पर
सहसा यह कहा जा सकता है कि तो फिर कर्म करेंगे ही क्यों?
जब
न तो फल की परवाह है और फल का संकल्प ही है,
तो
कर्म की बला में नाहक फँसा क्यों जाय?
इसी का उत्तर श्लोक का आखिरी हिस्सा
'मा
ते संगोऽस्त्वकर्मण्0श्निा'
देता है कि खबरदार,
अकर्म (कर्म छोड़ने) में आसक्ति या हठ हर्गिज होने न पाये। कर्म का न किया
जाना एक चीज है और उसमें-न करने या छोड़ने में-हठ बिलकुल दूसरी ही चीज है।
ऐसा हो सकता है कि समय पा के खुद-ब-खुद कर्म छूट जाय। परिस्थिति ऐसी हो जाय
कि हजार चाहने पर भी कर्म छोड़ने के अलावा दूसरा चारा होई न। इसलिए अपने आप
या मजबूरन कर्म छूट जाय। गीता यह बात मानती है और इसका विरोध उसे इष्ट
नहीं। मगर कर्म के छोड़ने का हठ हर्गिज उसे बर्दाश्त नहीं। हम कर्म कभी
करेंगे ही नहीं चाहे जो भी हो जाय,
यही चीज गीता को पसन्द नहीं। कर्म के मार्ग में यही उसकी नजरों में तीसरा
खतरा है और वह लोगों को इसी से सजग करती है।
लेकिन
चौथे खतरे का सामना हो जा सकता है। वृत्त के बाहर परिधि के इधर-उधर के उक्त
तीनों खतरों से बचने पर भी चौथा खतरा उसके भीतर ही-दायरे के अन्दर ही-हो
सकता है। वह है कर्म के करने का हठ या आसक्ति। इसी को कर्म में संग,
कर्म का संग,
कर्मसंग या कर्मासंग भी कहते हैं। जैसे सक्ति और आसक्ति का अर्थ एक ही है
चिपक जाना या सट जाना और जिसे अंग्रेजी में अटैचमेण्ट
(attachment)
कहते
हैं;
ठीक उसी प्रकार संग और आसंग का भी यही अर्थ है। दोनों
शब्दों में 'आ' के
जुट जाने से चिपकने या लिपटने में सिर्फ
अन्धापन
या हठ (जिद्द) जुट जाता है और इसे
'ब्लाइण्ड
अटैचमेण्ट' (blind
attachment)
कह
सकते
हैं।
मगर 'आ'
के न रहने पर भी यही अर्थ होता है। गीता के मत से जैसी
ही बुरी अकर्म (कर्मत्याग) की जिद है वैसी ही कर्म की जिद भी। आसक्ति या हठ
दोनों का ही बुरा है। इसी हठ को 'ऊँट की पकड़'
कहते
हैं।
ऊँट किसी चीज को एक बार पकड़ने पर छोड़ता ही नहीं। बन्दरिया की आसक्ति या
अन्धाप्रीति अपने बच्चे के साथ होती है। फलत: बच्चे के मर जाने पर भी उसे
नहीं छोड़ती। किन्तु छाती से लिपटाये फिरती है जब तक कि वह खुद टुकड़े-टुकड़े
हो के गिर नहीं पड़ता है। यह चीज बुरी है और यही रोकी गयी है। हजार कोशिश और
दृढ़ संकल्प (determination)
के बाद
भी कभी-कभी परिस्थितिवश कर्म का छूट जाना अनिवार्य हो जाता है।
परिस्थितियाँ किसी के वश की जो नहीं होती
हैं।
फिर हठ या जिद क्यों?
न करने की जिद हो और न तो न करने की ही। जिद ही तो बला
है।
दृढ़
संकल्प और आसक्ति या हठ में फर्क है-दोनों दो चीजें हैं। दृढ़ संकल्प का तो
इतना ही मतलब है कि विघ्न-बाधाओं से कदापि विचलित न हो के कर्म करते
रहें-चट्टान की तरह अटल रहें-मगर इतने पर भी कर्म छूट जा सकता है। यह जरूरी
नहीं कि हम उसे करते ही रहें। परिस्थितियाँ हमें मजबूर कर दे सकती हैं।
फलत: दृढ़ संकल्प के होते हुए भी इस तरह कर्म के छूट जाने पर हमें कष्ट न
होगा। क्योंकि हमारा तो यही रास्ता है और होना चाहिए कि
''आओ
विपत्तियाँ तुम,
दु:खों को साथ लाओ। पीटूँगा मैं तुम्हीं को,
तुमसे ही या पिटूँगा।''
मगर यदि कर्म में आसक्ति या करने की जिद रही,
तो
हमें मर्मान्तक वेदना ऐसी दशा में जरूर हो जायगी और सारा मजा ही किरकिरा हो
जायगा। ठीक इसी तरह कर्म के त्याग के हजार हठ करने पर भी उसे करने की
मजबूरी कभी-कभी हो सकती है और हठ होने से हम उस दशा में तिलमिला जा सकते
हैं। यही बात गीता रोकना चाहती है। इसीलिए कर्म के करने या न करने-कर्म या
संन्यास दोनों ही-में आसक्ति,
जिद या हठ को उसने खतरा करार दिया है और कहा है कि कर्म चाहे पूरा हो या
अधूरा ही रह जाय या चाहे हम उसे शुरू ही न कर पायें-हर हालत में हमारे
दिल-दिमाग की समता या गम्भीरता (balance of mind)
बिगड़ना
नहीं चाहिए। हमें दोनों ही हालतों में,
पूरा होने, न होने-कर्म की
सिद्धि
और असिद्धि-में
सम रहना चाहिए-एकरस (unconcerned)
रहना
चाहिए,
जैसा कि जनक ने मिथिलापुरी में आग लगने पर कहा था कि
मिथिला जलती है तो जले, मेरा क्या जलता है?-''मिथिलायां
प्रदग्धायां
न मे कि×चन
दह्यते।''
यही है योग। इसी योग को प्राप्त करके,
काबू में करके-योगस्थ हो के-हमें कर्म करना चाहिए। फल
और उसके संकल्प के त्याग का भी असली प्रयोजन यही है कि दिल-दिमाग की
गम्भीरता और समता-एकरसता (balance)-न
बिगड़े।
इन चारों
खतरों से बचने का निचोड़ इसी सिद्धि,
असिद्धि की समता में ही आ जाता है। इसीलिए इसे ही योग कहा है। फल की तरफ
खयाल होने या फल का संकल्प होने पर कुछ भी गड़बड़ होते ही हायतोबा मचती ही
है। इसीलिए उससे बचना जरूरी है। ऐसा भी होता है कि काम पूरा होने तथा विजय
मिलने पर खुशी के मारे मनुष्य आपे से बाहर हो जाता है और ऐसा न होने या
पराजय होने पर रंज के मारे ही आपे से बाहर या बेसुध हो जाता है। दोनों ही
हालतों में दिल-दिमाग की समता खत्म हो जाती है। फलत: ऐसा करना चाहिए कि
दोनों में एक का भी मौका ही आने न पाये। इसीलिए तो आसक्ति का त्याग जरूरी
बताया गया है। पूरे
48वें
श्लोक में यही बात खूब सफाई के साथ कही गयी है। न रंज के मारे छाती पीटने
का और न खुशी के मारे बेहोश होने का ही मौका इसी के चलते आने पायेगा। यही
योग है।
इसमें
सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब कर्म करनेवाले का मन इधर-उधर कहीं भी जरा भी न
जा के सिर्फ काम में ही लग जायगा-वहीं केन्द्रीभूत
(concentrated)-हो
जायगा,
तो
वह काम होगा भी ठीक-ठीक। किसी भी काम की पूर्णता के लिए दिल और दिमाग का
उसमें लग जाना,
उसी में जा के अड़ जाना और लिपट जाना-उससे बाहर न जाना-बुनियादी और मौलिक
कारण है। फिर तो वह सिद्ध और पूर्ण हो के ही रहेगा। अधूरेपन की गुंजाइश
उसमें रहेगी ही नहीं। दिल और दिमाग में बड़ी ताकत है। जिसे इच्छाशक्ति
(will-power)
कहते
हैं
वह यही चीज है। योगियों और सिध्दों के जो अद्भुत काम कहे गये
हैं
और उनकी सिद्धियों
का जो वर्णन मिलता है उसका रहस्य यही है। और जब मन के-दिल और दिमाग के-कहीं
इधर-उधर
जाने की गुंजाइश रखी ही नहीं गयी है,
तो वह केन्द्रीभूत खामख्वाह होगा ही। फल,
उसका संकल्प, कर्म के करने
का आग्रह और उसके न करने का हठ-यही चार-ही तो ऐसी चीजें
हैं
जिनकी ओर मन कर्म के सिलसिले में भटक सकता है,
भटकता फिरता है। मगर गीता ने इन चारों का दरवाजा बन्द
करके उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है कि भाग सके।
नतीजा यह
होगा कि कर्म की सांगोपांग पूर्ति तो होगी ही। उसी के साथ उसका फल,
परिणाम या नतीजा भी हो के ही रहेगा। उसमें दिक्कत की गुंजाइश रही कहाँ?
गड़बड़ी के सभी रास्ते तो बन्द होई गये। यह भी कितनी मौजूँ और युक्तियुक्त
बात है कि कर्म के फलों को तो कोई सीधे पकड़ सकता नहीं। उन्हें तो कर्म के
द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। इन्सान काम करता है और काम से फल होता है,
चाहे बुरा हो या भला। हम सीधे फल तो पैदा करते ही नहीं। हमारे वश की चीज तो
कर्म या क्रिया ही है। फल तो है नहीं। फिर हम क्रिया की ही फिक्र क्यों न
करें?
फल की ओर
नाहक क्यों दौड़ें?
यह
तो मृगतृष्णा की बात ही ठहरी। जो चीज हमारे वश की नहीं,
अधिकार की नहीं,
उस
पर नाहक क्यों दौड़ें और लट्टू हों
?
फलत: गीता
ने जो कहा है कि सिर्फ कर्म में ही अधिकार है,
वही तो युक्तिसंगत बात है। वह कोई आश्चर्य की चीज तो है नहीं। और कर्म या
अकर्म का हठ तो महज नादानी है,
जैसी कि सभी तरह के हठों की बात है।
इस उपदेश
का फल यह हुआ कि एक तो कर्म का फल जरूर ही मिलेगा-उसका मिलना एक प्रकार से
निश्चित ही समझिये,
यदि कोई दैवी बाधा आ न पहुँचे। मगर यह बात फल की इच्छा,
लालसा और संकल्प के होने पर सम्भव नहीं। क्योंकि
'मन
न होय दस-बीस'
के
अनुसार एक ही मन कभी कर्म की ओर जायगा तो कभी फल की ओर,
कभी उसके त्याग की ओर और कभी उसके करने के हठ की तरफ। कभी उसे कर्म अपनी ओर
खींचेगा तो कभी फलेच्छा अपनी तरफ। इस खींचतान में न तो वह कर्म में जमेगा,
न
वह पूरा उतरेगा और न फल मिलेगा। दूसरी बात-दूसरा लाभ-इससे यह हुआ कि जहाँ
पहले फल मिलने पर या न मिलने पर भी कर्म बन्धन का-जन्म-मरण का-कारण होता था,
तहाँ अब वह बात जाती रही। जैसे भाड़ में डालने पर अन्न में-बीज में-अंकुर
पैदा करने की ताकत जाती रहती है। वैसे ही इस योग के फलस्वरूप कर्मों में
बन्धन की ताकत रही नहीं जाती-वह खतम हो जाती है। दरअसल कर्मों का संस्कार
मानसपटल पर जमने पाता ही नहीं। फिर वह जन्म-मरण में फँसायें तो कैसे?
जन्म-मरण का तो अर्थ ही है कर्मों के करने का सिलसिला जारी रहना। और इस
सिलसिले के लिए उसके संस्कार जरूरी हैं,
जैसे बीज में अंकुरजनन की शक्ति। मगर यहाँ तो योग के चलते हम कर्मों के
करने या न करने या उनके फलों से कतई प्रभावित होते ही नहीं-तटस्थ या उदासीन
रह जाते हैं। तब मानसपटल पर-जो निर्लेप बन गया है-संस्कार कैसे पैदा होगा?
संस्कार के लिए उदासीनता की नहीं,
किन्तु अनुराग,
मैत्री या लालसा की जरूरत होती है। जिन चीजों से हम उदासीन हों उनके
संस्कार मन में पैदा होते ही नहीं। हाँ,
जिनमें मन लगा हो उनके संस्कार जरूर ही पैदा हो जाते हैं। यही कारण है कि
इसी योग को कर्म का कौशल कहा है। यही तो कर्म करने की असली कला है-कर्म
करने का जादू है,
कारीगरी है।
जिस
समत्वरूप योग का वर्णन अभी किया गया है उसके सम्बन्ध में अनेक बातें जानने
की हैं। इसीलिए इस पर बहुत कुछ लिखना बाकी ही है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले
यहीं पर पूर्वोक्त
47वें
श्लोक की एक महत्तवपूर्ण बात और भी जान लेना जरूरी है। कर्म करने और उसके
त्यागने का झमेला कुछ ऐसा है और इधर कुछ गीता के टीकाकारों ने उसे इतना
ज्यादा बढ़ा दिया है कि हमें विवश हो के यह लिखना पड़ रहा है। उस श्लोक के
पहले चरण के तीन शब्दों
'कर्मणि,
एव,
अधिकार:'
में 'एव'
शब्द कुछ विचित्र है। वह
'कर्मणि'
के
आगे आया है।
'अधिकार:'
के
आगे भी आ सकता था और ऐसा होने पर अर्थ में कुछ विशेषता आ जाती। एव शब्द
किसी बात पर जोर (emphasis)
देने
के ही लिए आता है। फलत: जिस पदार्थ के वाचक शब्द के बाद आता है उसी पर जोर
देता है। यहाँ स्वभावत: कर्म पर ही जोर देता है। उसी के बाद आया जो है। यदि
'अधिकार:'
के बाद आता तो अधिकार,
वश या काबू पर ही जोर देता। क्योंकि अधिकार
शब्द इन्हीं का वाचक है। जोर देने का मतलब यही होता है कि जिस पर जोर होता
है उससे अन्य चीजें रोकी जाती
हैं।
अन्य चीजों से मतलब है उन्हीं से जिनकी संभावना होती है-यानी उसकी
विरोधी
या
सम्बन्ध
वाली चीजें।
इसीलिए
यहाँ कर्म-सम्बन्धी फल,
फलेच्छा,
कर्मासक्ति आदि का निषेधा हो जाता है,
इन
पर रोक आ जाती है और दोनों श्लोकों में यही बात आयी भी है। यदि
'अधिकार:'
के
बाद 'एव'
रहता तो हक या अधिकार या वश के विरोधी तथा सम्बन्धी पदार्थों पर रोक हो
जाती। मगर यहाँ वह बात हुई नहीं। फिर भी असली बात जो हमें कहनी है वह तो यह
है कि कर्म एवं अधिकार दो में एक के साथ
'एव'
के
लगने से यहाँ निरालापन आया है। जैसा है वैसी दशा में खामख्वाह कर्म करने
में हठ नहीं हो सकता। लेकिन अधिकार के साथ आ जाने पर यही हठ आ जाता।
क्योंकि तब तो स्पष्ट हो जाता कि हमें कर्म छोड़ने का कोई हक हुई नहीं और
हमें उससे लिपटे रहना होगा। जिस चीज पर आगे रोक लगी है वही चीज तब हो जाती।
जहाँ अब अर्थ होता है कि कर्म के अतिरिक्त फलादि का हक हमें नहीं है,
तहाँ उलट के अर्थ हो जाता कि हक के सिवाय किसी और का सम्बन्ध कर्म के साथ
हुई नहीं।
जिन दो
पदार्थों के बीच में एक पर यह जोर रहता है उन्हीं में दूसरे के साथ एक को
यानी पहले को बाँध देता है और बाकियों को,
जिनकी सम्भावना हो,
रोक देता है। इसे और भी साफ तौर से यों समझें कि कर्म पर ही यहाँ जोर देने
के कारण उसी के अनुकूल या अधीन हक रहता है। कर्म की ही प्रधानता रहती है।
हक उसकी छाती पर बैठ के उसे घसीट नहीं सकता। विपरीत इसके यदि अधिकार या हक
पर जोर होता तो उसी की प्रधानता होती और कर्म की छाती पर बैठ के वह अपने
साथ यानी आदमी के साथ कर्म को घसीटता फिरता। तब कर्म किसी भी दशा में
त्याज्य या त्यागने योग्य नहीं रह सकता। मगर वर्तमान दशा में तो हक ही
त्याज्य नहीं है। कर्म का त्याग तो हो सकता है। जब हम कर्म करते हैं तो यह
कोई नहीं कह सकता कि उस पर हमारा हक नहीं है। इस तरह देखते हैं कि इस
'एव'
शब्द का स्थान बदलने से दोनों श्लोकों के बाकी अंशों के साथ पहले चरण का
कोई मेल होता ही नहीं।
इतना
लिखने का हमारा मतलब दोनों श्लोकों के सभी अंशों में परस्पर मेल या
सामंजस्य लाना नहीं है। यह तो गीता के रचयिता का ही काम था कि बेमेल बात न
बोलें। हम उस कवि के वकील भी नहीं हैं कि जो कुछ त्रुटि मालूम हो उसे
मिटाने की वकालत करें। गीता के कर्ता व्यास को वकील की जरूरत ही न थी। वह
तो खुद इतने योग्य थे कि ऐसी मोटी भूल कर सकते न थे। हमारा मतलब सिर्फ यह
दिखलाने का है कि गीता के अनुसार कर्म की आसक्ति या उससे खामख्वाह लिपटना
ठीक नहीं है। उसने कर्म और धर्म के संन्यास-दोनों ही-के लिए गुंजाइश मानी
है,
दोनों के
लिए पूरा स्थान रखा है। वे दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर ठीक हैं,
उचित हैं,
कर्तव्य हैं। खूबी तो यह है कि जिस योग को ले के कुछ लोगों ने इस बात पर
जोर दिया है कि गीता तो संन्यास की विरोधिनी है;
वह
तो कर्म पर ही जोर देती और उसी का समर्थन करती है,
वही योग कर्म और कर्मत्याग-कर्म के योग और उसके त्याग-दोनों ही का
प्रतिपादक है-उसके भीतर दोनों ही आ जातेहैं!
बेशक,
यह
बात उल्टी-सी लगती है। योग शब्द तो जोड़ने,
जुटने या सम्बन्ध को-संयोग को-ही कहता है,
ऐसा साफ दीखता है। फलत: कर्मयोग का अर्थ है कर्म का संयोग या सम्बन्ध। यही
उचित भी प्रतीत होता है। मगर कर्मयोग का अर्थ ही कर्म का वियोग या त्याग
(संन्यास),
यह
तो निराली चीज है। लेकिन किया क्या जाय?
खुद गीताकार को भी यह चीज सूझी थी-उन्हें इसी तरह का विरोध इस योग में या
योग शब्द के अर्थों में प्रतीत हुआ था। फिर भी उसने उसका समर्थन किया। छठे
अध्याय के
23वें
श्लोक का पूर्वार्ध्द कुछ इसी तरह की पहेली का खयाल करके ही बनाया गया
मालूम होता है। वह है
''तं
विद्याद् दु:खसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्।''
इसका आशय यही है कि
''यद्यपि
उसे योग कहा जाता है,
तथापि वह तो दु:खों के संयोग (सम्बन्ध) का वियोग ही है-अर्थात् दु:खों का
वियोग करने वाला है।''
इस
तरह वियोग को ही योग नाम दिया गया है ऐसा वह मानते हैं। ठीक वही बात यहाँ
भी है। अत: निर्विवाद है कि गीता कर्म करने के हठ की विरोधिनी है।
कर्म से
चिपकने और लिपटने के इसी हठ को,
जो
गुड़ के साथ लिपटे चींटे की तरह अनर्थ और मृत्यु का कारण होता है,
गीता ने दूसरे-दूसरे नामों से भी कह के बुरा ठहराया है। अठारहवें अध्याय
के 24वें
श्लोक में इसी को अहंकार कहा है और
27वें
में राग-वहाँ
'रागी'
शब्द है-कहा है। चौथे अध्याय के
19वें
श्लोक में इसे ही संकल्प नाम दिया गया है। जिस प्रसंग में और जिस ढंग से ये
बातें उन स्थानों में कही गई हैं उससे साफ है कि अहंकार आदि का आशय कर्म का
हठ या आसक्ति ही है। इसीलिए निन्दित अर्थ में ही उनका प्रयोग भी हुआ है।
चौदहवें अध्याय के
22, 23
श्लोकों में द्वेष,
राग और उदासीनता शब्द तथा बारहवें के दसवें में
'मदर्थ'
शब्द भी इसी मानी में हैं। और भी ऐसे ही शब्द आये हैं।
मगर इतना
ही नहीं है। ठेठ दूसरे अध्याय से ही शुरू करके अठारहवें अध्याय तक कम से
कम बीस बार संग,
आसक्ति,
आसक्त आदि आये हैं और सिवाय कर्म में आसक्ति या करने के हठ के त्याग के और
कोई अर्थ इनका हो ही नहीं सकता। ये बीस स्थान तो ऐसे हैं जहाँ निस्सन्देह
कर्मों का हठ बुरा ठहराया गया है। चौथे अध्याय के
21वें
श्लोक में 'केवल'
शब्द लिखके इस हठ के त्याग को बड़ी सफाई के साथ दिखाया है। इसी तरह उसी
अध्याय के
14वें
श्लोक में 'लिम्पन्ति'
शब्द लेप,
लीपने या लिपटने के मानी में लिख के बताया गया है कि कर्मों में हमारा
लिपटना या कर्मों का हममें लिपटना ठीक नहीं है। यह तो स्पष्ट है कि कर्म तो
कोई गुड़,
गोबर या गीली मिट्टी नहीं है जो यों ही लिपटेंगे। वे तो हठ,
राग या आसक्ति के द्वारा ही मन में लिपट जाते हैं।
लोग ऐसा न
समझें कि हमने यों ही बीस जगहों का नाम ले लिया है,
इसीलिए प्रत्येक अध्याय और श्लोकों के अंकों को जान लेना चाहिए ताकि कोई
भी आसानी से यह बात जाँच सके। दूसरे अध्याय के
48वें
श्लोक का तो व्याख्यान हो ही चुका है जहाँ
'संग'
शब्द साफ ही आया है। तीसरे के
7, 9, 19, 25, 28, 29
श्लोकों
में;
चौथे के
10, 23
में;
पाँचवें
के 10, 11
में;
छठे के
4
में नवें
के 9
में और
अठारहवें के
6, 9, 10, 22, 24, 26, 34,
और
49
श्लोकों
में यही बात है। यों ही,
मोटामोटी नजर दौड़ाने पर भी यह स्पष्ट हो जाता है। यदि गौर से विचारा जाय तब
तो कुछ कहना ही नहीं है। सन्दिग्ध श्लोकों का तो हमने जिक्र किया ही नहीं
है। इस प्रकार कर्म संन्यास में कोई भी बाधा गीता की नजरों में हो नहीं
सकती।
परन्तु
गीता ने तो और भी साफ-साफ यह बात कही है। चौथे अध्याय के
'योगसंन्यस्तकर्माणं
ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम्'
(41)
और
पाँचवें अध्याय के
'संन्यासस्तु
महाबाहो दु:खमाप्तुमयोगत:। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति'
(6)-इन
दो-श्लोकों को देखने से ज्ञात होता है कि गीता संन्यास को न सिर्फ कर्तव्य
मानती है,
बल्कि उसका रास्ता और मौका भी बताती है। यदि गौर से दोनों श्लोकों को
मिलायें तो एक तो यह पता चलता है कि संन्यास की बात दोनों ही में है। दूसरे
यह कि संन्यास के पहले कर्म करना जरूरी है। आखिर संन्यास तो कर्मों का
त्याग ही ठहरा और जब तक कर्म करें ही न,
तबतक त्याग कैसा
?
जिनके पास
जो चीज होई न,
वही उसी चीज का त्याग कैसे करेगा?
तब
तो 'वृद्धा
वेश्या तपस्विनी'
वाली बात हो जायगी न?
यह
भी तो पक्की ही बात है कि जब तक वर्णमाला नहीं सीख लें,
तब
तक जब कभी छोटी-बड़ी कोई भी पुस्तक पढ़ना चाहेंगे,
वर्णमाला सामने खड़ी हो जाया करेगी। यदि उससे पिंड छुड़ाना है तो उसे एक बार
पूरा कर लीजिये। दूसरा रास्ता हुई नहीं। ऊपर लिखे दोनों श्लोकों का यही आशय
है।
चौथे
अध्याय वाले
'योगसंन्यस्तकर्माणं'-''कर्मों
(योग) के द्वारा ही कर्मों का त्याग या संन्यास हासिल करने वाले''
का
अभिप्राय हमने अच्छी तरह साफ कर दिया है। उसके
'ज्ञानसंछिन्नसंशयम्'
का
प्रयोजन तो आगे है। वह तो इतना ही कहता है कि
''जिनका
संशय ज्ञान के प्रताप से खत्म हो गया है।''
ज्ञान तो संन्यास के बाद ही होता है। फलत: सभी प्रकार के संशयों तथा
शक-शुभों का खात्मा संन्यास के बाद ही होता है,
ऐसा माना गया है। यह भी सही है कि आत्मा-परमात्मा केयथार्थ एवं समयग्दर्शन
के लिए शक-सन्देहों का निर्मूल हो जाना आवश्यक है। इस प्रकार निर्वाण के
लिए संन्यास जरूरी हो गया है। यही कारण है कि उस श्लोक के शेषआधो
'आत्मवन्तं
न कर्माणि निबधनन्ति धानंजय'
से
साफ पता चलता है कि
''इस
प्रकार आत्मज्ञान या आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर ही कर्मों की बन्धनशक्ति
जाती रहतीहै।''
पाँचवें
अध्याय के उक्त श्लोक का तो साफ ही मतलब है कि
''संन्यास
की प्राप्ति तो कर्म (योग) के बिना अत्यन्त कष्टसाध्य-अर्थात् असम्भव-है।
विपरीत इसके जो मननशील विवेकी कर्म करता है वह शीघ्र ही संन्यास के योग्य
हो के उसे प्राप्त कर लेता है।''
इसमें इस बात की पुष्टि कर दी गयी है कि संन्यास के लिए कर्म करना जरूरी
है। इसीलिए कर्म के बिना वह प्राप्त होता नहीं और कर्म से हो जाता है। कारण
तो उसे ही कहते हैं जिसके बिना चीज होई न और जिसके रहने पर अवश्य हो जाय।
इसी को पुराने लोगों ने अन्वय और व्यतिरेक कहा है। इस श्लोक के चौथे चरण
में संन्यास न लिख के यद्यपि ब्रह्म लिखा है,
तथापि ब्रह्म का अभिप्राय संन्यास ही है। श्लोक के शेष तीन चरणों से यह बात
साफ हो जाती है। इसके पहले जो कई श्लोक आये हैं उन्हें गौर से पढ़ने से भी
यही अभिप्राय निकलता है। इसके सिर्फ दो दृष्टान्त गीता से ही देने से बात
साफ हो जायगी।
(शीर्ष पर वापस)
संन्यास और त्याग
अठारहवें अध्याय
में ''नियतस्य
तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्यते। मोहात्तास्य परित्यागस्तामस: परिकीर्तित:''
(7) और ''अनिष्टमिष्टं
मिश्रं च
त्रिविधां
कर्मण: फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित्''
(12) ये श्लोक आये
हैं।
इन दोनों में ही
'संन्यास'
और 'त्याग'
या 'संन्यासी'
तथा 'त्यागी'
शब्द आये
हैं।
इस अध्याय
के पहले ही श्लोक में जो प्रश्न किया गया है उससे स्पष्ट है कि संन्यास और
त्याग दो चीजें
हैं।
इसीलिए दोनों की हकीकत अलग-अलग जानने के खयाल से ही सवाल किया गया है। फलत:
यह
धारणा
स्वभावत: हो जाती है कि आगे के श्लोकों में जहाँ कहीं ये दोनों शब्द आये
हैं,
अलग-अलग मानी में ही प्रयुक्त हुए
हैं।
मगर है यह बात गलत-यह
धारणा
निराधार
है। यह ठीक है कि अठारहवें अध्याय
में त्याग और संन्यास के स्वरूप अलग-अलग बताये गये
हैं
और हम भी उनके बारे में कुछ न कुछ कहेंगे। फिर भी उसका मतलब शब्दों के अर्थ
से नहीं है। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो अकसर एक ही माना जाता है। और गीता
में एक ही अर्थ में दोनों ही प्राय: बोले गये
हैं।
फर्क तो त्याग और संन्यास नाम की चीजों की भीतरी बातों को लेकर ही माना
जाता है। ऊपर से एक होने पर भी भीतर से इनमें कुछ बारीक भेद है-आमतौर से
पुराने लोगों ने कुछ भेद इनमें किया है। उसी के जानने के लिए शुरू में
प्रश्न किया गया है और जवाब भी दिया गया है।
फलत: यदि
भ्रान्त धारणा को जुदा करके या हटाके हम देखें तो पता लगेगा कि पूर्व लिखे
7वें
और 12वें
श्लोकों में त्याग तथा संन्यास एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं और एक की
जगह दूसरे को बदल देने से अर्थ में कोई फर्क न पड़ के और भी स्पष्टता हो
जायगी। पहले श्लोक का सीधा अर्थ यही है कि
''किसी
के भी लिए जो कर्म निश्चित कर दिये गये हैं उनका संन्यास उचित नहीं है,
और
अगर भूल या धोखे में पड़ के उनका त्याग कर दिया जाय तो वह तामस (तमोगुणी)
त्याग माना जाता है।''
यहाँ पहले वाक्य में जिस मानी में संन्यास शब्द आया है,
दूसरे में उसी मानी में त्याग शब्द है। दूसरा मानी सम्भव नहीं है। इसीलिए
पहले लिखे संन्यास शब्द के ही अनुसार त्याग का भी अर्थ आगे लगता है। विपरीत
इसके 12वें
श्लोक के उत्तारार्ध्द में पहले त्यागी (त्यागिनाम्) लिख के पीछे संन्यासी
(संन्यासिनाम्) लिखा है। श्लोक का अर्थ सिर्फ यही है कि
''बुरे,
भले और मिश्रित-तीन प्रकार के-जो फल कर्मों के होते हैं वह उन्हीं को मिलते
हैं जो त्यागी नहीं हैं,
संन्यासियों को तो ये फल कभी नहीं मिलते।''
यहाँ त्यागी के ही अनुसार संन्यासी का अर्थ भी त्यागी ही माना जाता है। यह
बात बहुत साफ है। ठीक इसी तरह पाँचवें अध्याय के उक्त श्लोक में भी पीछे
के ब्रह्म शब्द का अर्थ पूर्व लिखे संन्यास शब्द के बल से संन्यास ही होना
ठीक है। उपनिषदों में भी
'संन्यासो
हि ब्रह्म'
आदि प्रयोग में ब्रह्म शब्द संन्यास के अर्थ में ही आया है और गीता तो
उपनिषद् हुई।
जैसा कि
अभी-अभी कहा है,
गीता के अठारहवें अध्याय में जो शंका त्याग और संन्यास की हकीकत या असलियत
के बारे में की गयी है,
उससे भी संन्यास की कर्तव्यता सिद्ध हो जाती है। हम तो कही चुके हैं कि इन
दोनों शब्दों के अर्थों में फर्क नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न के बाद भी गीता
में ही दोनों एक ही अर्थ में बोले गये हैं। सवाल तो हकीकत या बारीकी के
बारे में ही है। इसीलिए प्रश्नवाले पहले श्लोक में,
'तत्तवमिच्छामि
वेदितुम्'
लिखा है,
जिसका अर्थ है कि
''इन
दोनों की हकीकत,
असलियत या भीतरी बारीकियाँ जानना चाहता हूँ।''
तत्तव शब्द इसी मानी में बोला ही जाता है। शब्दार्थ को तत्तव नहीं कहते।
किन्तु जब कभी तत्तव कहना होगा तो जिनके तत्तव से अभिप्राय होगा उन चीजों
की परिभाषा कर दी जायगी,
उनका लक्षण कर दिया जायगा। यही बात हमेशा होती आती है। यहाँ भी आमतौर से
दोनों का एक ही अर्थ समझा जाने के कारण ही अर्जुन को पूछना पड़ा कि आया
दोनों की परिभाषा एक ही है या जुदी-जुदी?
दोनों की असलियत एक है या दो?
दोनों में बारीकियाँ कुछ-कुछ हैं या नहीं?
इसी हिसाब से उसे उत्तर भी दिया गया है।
उत्तर की
हालत यह है कि त्याग के बारे में लोगों की चार रायें होने के कारण और कृष्ण
का खुद अपना भी एक स्वतंत्र विचार होने के कारण पहले उसी की हकीकत कहनी पड़ी
है। हालाँकि प्रश्न में पहले संन्यास ही आया है। संन्यास के बारे में मतभेद
या अनेक रायें न होने के कारण ही उसकी बात उनने पीछे उठाई हैं। सो भी बहुत
दूर जा के। असल में त्याग का ब्योरा और विवरण देने के बाद ही संन्यास की
बात समझने में आसानी भी हो जाती है। इसलिए भी त्याग के मुतल्लिक सारी बातें
कहने के बाद ही संन्यास की बात कहना उचित समझा गया है। यही कारण है कि
आरम्भ से लेकर पूरे
48
श्लोकों
में कर्म के सम्बन्ध की ही सारी बातें ब्योरे के साथ कही गयी हैं,
जिनसे त्याग के स्वरूप और उसकी हकीकत पर पूरा प्रकाश पड़ जाता है। फिर
49वें
और 57वें
श्लोकों में संन्यास का जिक्र आया है। मगर
57
वें श्लोक
वाला संन्यास शब्द तो ठीक वैसा ही है जैसा कि तीसरे अध्याय के
''मयि
सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा''
(30)
में आया
है। क्योंकि वहाँ लिखा है कि
''चेतसा
सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर:।''
मालूम होता है कि प्राय: अक्षरश: एक ही श्लोक का यह हिस्सा दोनों जगह लिखा
गया है। तीसरे अध्याय वाले में जो
'अध्यात्म'
शब्द ज्यादा प्रतीत होता है,
उसकी जगह अठारहवें वाले में आगे
'बुद्धियोगमुपाश्रित्य'
लिख दिया है। और भी आगे-पीछे बहुत-सी बातें मिल जाती हैं। फलत: वहाँ भी
संन्यास का वही पुराना सर्वजन विदित अर्थ ही है। जिसे ईश्वरार्पण या मदर्पण
आदि नाम दिया गया है। संन्यास शब्द संन्यास की उस हकीकत को यहाँ नहीं बताता
है जिसके बारे में सवाल हुआ है।
बाकी बचा
49वें
श्लोक का संन्यास। ठीक है यह तो उसी बात को कहता है जिसकी-जिस हकीकत
की-जानकारी के लिए शुरू में ही शंका की जा चुकी है,
प्रश्न हो चुका है। यदि इस समूचे श्लोक को गौर से विचारा जाय तो यह बात साफ
हो जाती है। हम खुद आगे यह विचार करेंगे। मगर इतना तो जान लेना ही होगा कि
यह श्लोक भी उस संन्यास की हकीकत या उसके स्वरूप की ओर सिर्फ इशारा ही करता
है और यही कहता है कि संन्यास के जरिये किस तरह परम नैर्ष्कम्यसिद्धि या
सर्वात्मना कर्मत्याग की तरफ आदमी जा सकता है। लेकिन उस संन्यास का स्पष्ट
रूप तो बिना उस शब्द का उच्चारण किये ही आगे के
'सर्वधार्मान्परित्यज्य'
नामक 66वें
श्लोक में ही बताया गया है। इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे। मगर अभी त्याग की
बात जान लें,
तो
अच्छा हो।
जैसा कि
कहा जा चुका है दूसरे से लेकर
48वें
श्लोक तक त्याग के सम्बन्ध की ही बातें कही गयी हैं। सबसे पहले दो और
तीन-दो-श्लोकों के दो-दो हिस्से करके चारों हिस्सों में त्याग के सम्बन्ध
के चार मत कहे गये हैं जो संसार के विद्वानों में प्रचलित हैं। उसके बाद
चार से लेकर छ: तक के-तीन-श्लोकों में कृष्ण ने त्याग के बारे में अपना
सिद्धान्त निश्चित रूप से कहा है और उसी का स्पष्टीकरण किसी न किसी रूप में
48वें
तक के श्लोकों में किया है। दूसरे श्लोक में
'न्यासं'
और
'संन्यासं'
शब्दों को देख के यह समझने की भूल हर्गिज नहीं की जानी चाहिए कि
पूर्वार्ध्द में
'संन्यास'
का
लक्षण कहा है। न्यास और संन्यास शब्दों का तो एक ही अर्थ है। फलत:
कामनापूर्वक किये गये (काम्य) कर्मों के संन्यास को संन्यास कहते हैं,
इस
कथन का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हम तो यही मानते हैं कि दूसरे के
पूर्वार्ध्द में
'कवयो
विदु:'-'सूक्ष्म
बुद्धिवाले जानते हैं',
उत्तारार्ध्द में
'विचक्षणा:
प्राहु:'-'कुशल
लोग कहते हैं'
तथा तीसरे के पूर्वार्ध्द में
'प्राहुर्मनीषिण:'-'मनीषी
लोग कहते हैं,'
और
उत्तारार्ध्द में
'अपरे
प्राहु:'-'दूसरे
लोग कहते हैं'-ऐसा
कह के चार मतवादों या सिद्धान्तों का कर्मों के त्याग के बारे में वर्णन
किया गया है। साफ ही चारों एक दूसरे से पृथक् मालूम पड़ते हैं। प्रश्न में
भी त्याग के बारे में
'पृथक्'
तत्तव या अलग-अलग हकीकत पूछी गयी है। इसीलिए उत्तर भी उसी ढंग का दिया गया
है। इस प्रकार संक्षेप में पहला मत है केवल काम्य कर्मों के ही त्यागने का,
दूसरा है केवल सभी कर्मों के फलों के ही त्याग का,
न
कि किसी भी कर्म के त्याग का,
तीसरा है सभी कर्मों के ही त्याग का और चौथा है यज्ञ,
दान तथा तप के सिवाय शेष कर्मों के त्याग का। इस प्रकार त्याग के बारे में
चार तरह के सिद्धान्त साफ हो जाते हैं।
आगे के
4
से 6
तक के श्लोकों में कृष्ण ने जो खुद अपना मत बताया है उसमें यह कहा है कि
यज्ञ,
दान तथा
तप को भी कर्मासक्ति एवं फलासक्ति छोड़कर ही,
करना यही त्याग कहा जाता है,
कहा जाना चाहिए। उनने इन तीनों कर्मों की बड़ी बड़ाई की है और कहा है कि
''ये
तो पवित्र करने वाले हैं ऐसा मनीषी लोग भी मानते हैं''-''यज्ञो
दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।''
फलत: इनके छोड़ने का सवाल तो उठी नहीं सकता। हाँ,
यह
किया जाना चाहिए जरूर कि इनमें तथा इनके फलों में आसक्ति रहने न पाये। जहाँ
चौथा पक्ष इन तीनों के करने में कोई विशेष बात नहीं कहता,
तहाँ कृष्ण का मत है कि इन तीनों को भी कर्मासक्ति तथा फलासक्ति छोड़कर ही
करना होगा।
फिर
7
से लेकर 12
तक के श्लोकों में त्याग की सात्तिवक आदि किस्में बताके उसका विवरण दिया
गया है। उसके बाद कर्म के पाँच कारणों का निरूपण करके
13
से 17
तक यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा तो इन पाँचों में है नहीं। वह तो अलग और
निर्लेप है। इसलिए कर्म का साथी उसे मानके सभी कर्मों से बचने की कोशिश
बेकार है,
नादानी है। बाद में
18
से
28
तक यह बात
विचारी गयी है कि आखिर कर्म होता है कैसे और वह रहता है कहाँ,
और
इस तरह प्रतिपादन किया गया है कि आत्मा से उसका ताल्लुक हुई नहीं। वह तो
दूसरी ही चीजें हैं जिनसे कर्म सम्बद्ध है। कर्म के करने में अन्त:करण या
बुद्धि और धृति (हिम्मत,
धारणशक्ति) की जरूरत होती है। ये दोनों न रहें तो कर्म हवा में मिल जाय।
बुद्धि रास्ता बताती है और धृति पस्ती आने न देकर कर्म मार्ग में डँटे रहना
लाती है। इसलिए जरूरी हो गया है कि इन दोनों का भी विश्लेषण किया जाय।
क्योंकि शायद इनमें किसी में कहीं आत्मा आ जाय। मगर
29
से
35
तक के
श्लोकों में इन दोनों को त्रिगुणात्मक बताके आत्मा को अलग ही मान लिया है।
जिस आराम और सुख के लिए कर्म करते हैं उसका निरूपण
36-39
श्लोकों
में करके उनमें सात्तिवक सुख को आत्मानन्द माना है सही;
मगर वह कर्मजन्य हुई नहीं। उसके लिए केवल अपनी बुद्धि की निर्मलता अपेक्षित
है-'आत्म-बुद्धिप्रसादजम्।'
वह
भले ही कर्मजन्य हो सकती है। शेष दो सुख तो आत्मा से लाख कोस दूर हैं। इसके
उपरान्त आमतौर से
40वें
में कह दिया है कि कर्म तो सांसारिक चीजों की सिद्धि के ही लिए किया जाता
है और वह चीजें तो सभी की सभी त्रिगुणात्मक होने के कारण आत्मा से अलग हैं।
प्रसंगवश चारों वर्णों के स्वाभाविक गुणों का
41-44
श्लोकों
में दिग्दर्शन कराके दिखा दिया है कि आत्मा से इनका क्या ताल्लुक?
इस
प्रकार जब कर्मों से ही भय करने की कोई वजह न होने के कारण बन्धन के डर से
उन्हें स्वरूपत: त्याग करने का सवाल आता ही नहीं,
तो
यज्ञ,
दान,
तप
के स्वरूपत: त्याग की बात कहाँ और क्यों आयेगी?
इस
तरह त्याग का सविस्तार निरूपण पूरा हो जाता है। चारों वर्णों के कर्म जब
स्वाभाविक (स्वभावज) ही हैं तो फिर उनके बुरे-भले या छोटे-बड़े होने का
प्रश्न भी कहाँ आता है?
जैसा कि आग का स्वाभाविक काम जलाना और पानी का भिगोना होने के कारण उनमें
भले-बुरे या नीच-ऊँच का सवाल नहीं उठता;
ठीक यही बात यहाँ भी है। इस तरह वर्ण-धर्मों और कर्मों की समानरूपता भी
प्रसंगत: सिद्ध हो जाती है।
विपरीत
इसके 45-48
श्लोकों में स्पष्ट कह दिया है कि स्वकर्म यदि ऊपर से बुरा भी प्रतीत हो तो
भी उसे हर्गिज नहीं छोड़ना चाहिए। वह सहज (स्वाभाविक) जो ठहरा। उसी के
द्वारा भगवान् की पूजा भी तो होती है। कर्म ही तो भगवत्पूजा है। यदि भगवान्
को सन्तुष्ट करना या उसे जानना चाहते हो तो स्वकीय कर्मों को ही ठीक-ठीक
करना चाहिए। इस तरह तो त्याग की जगह कर्मों का करना ही जरूरी हो जाता है।
क्योंकि भगवत्पूजा तो आखिर करनी ही है न?
इसके बाद
49-55
तक संन्यास की उपयोगिता और उसकी दशा को बताके
56-65
तक उसके लिए ही कर्मों की उपयोगिता बताई गयी है। अब रह गयी संन्यास की बात।
सो तो 49
से ही शुरू होती है और
66वें
में उसका स्पष्ट रूप दिखाया गया है।
49वाँ
श्लोक यों है,
'असक्तबुद्धि:
सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह:। नैर्ष्कम्य सिध्दिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति''।
इसका सीधा अर्थ यही है कि
''जिसकी
बुद्धि कहीं लिपटी न हो,
जिसका मन अपने वश में हो और जिसे कोई भी लोभ-लालच रह न गया हो वही संन्यास
के द्वारा कर्मों के त्याग की अन्तिम दशा को प्राप्त हो सकता है।''
मन,
बुद्धि आदि पर अपना अधिकार रखने से कर्मों के त्याग का रास्ता साफ हो जाता
है और बहुतेरे काम छूट भी जाते हैं। फिर भी नियत या स्वाभाविक कर्म तो होते
ही रहते हैं। फलत: जब तक उनका भी त्याग न हो जाय पूरी निष्कर्मता या कर्मों
के त्याग की आखिरी और पूर्ण हालत पर पहुँच नहीं सकते। इसीलिए संन्यास या
कर्मों का स्वरूपत: त्याग तब जरूरी हो जाता है।
कर्मत्याग
की पूर्णता की जरूरत क्या है,
यह
सवाल हो सकता है। मगर इसका उत्तर तो
'आरुरुक्षोर्मुनर्यो'
की
व्याख्या के समय दिया जा चुका है। वही बात यहाँ भी
50
से लेकर 55
तक के श्लोकों में कही गयी है। ये श्लोक समाधि का ही ब्योरेवार निरूपण करते
हैं और कहते हैं कि अगर कुछ भी कर्मों का झमेला रहा तो समाधि हवा में ही
मिल जायगी। फिर तो योगारूढ़ या आत्मदर्शी होना असम्भव हो जायगा। समाधि के
लिए प्राय: बहुत ज्यादा समय लगता है-दीर्घकाल की अपेक्षा है। सो भी जब वह
निरन्तर चालू रहे और बीच में विराम होने न पाये। मन के निरोध को ही तो
समाधि कहते हैं। फलत: उसके निरोध के लिए जो अभ्यास किया जाता है उसके बारे
में योगदर्शन के समाधिपाद में पतंजलि ने साफ ही कह दिया है कि
श्रद्धापूर्वक निरन्तर बहुत दिनों तक करते रहने पर ही वह दृढ़ होता है-''स
तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारसेवितो दृढ़भूमि:''
(14)।
तब इसमें कर्म की जरा भी गुंजाइश कहाँ रह जाती है?
उसकी तो जरूरत तभी तक थी जब तक कि आत्मदर्शन की तरफ मन का झुकाव नहीं हुआ
था। अब वैसा होने पर तो कर्मों का त्याग नितान्त आवश्यक हो जाता है।
हाँ,
आत्मदर्शन हो जाने के बाद भले ही कर्म कर सकते हैं। क्योंकि तब तो खामख्वाह
कर्मों के छोड़ने का सवाल रही नहीं जाता। पुराने संस्कारों के बल से
आत्मज्ञानी लोग दोनों ही तरह के होते हैं,
जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है। कर्मयोगी भी होते हैं,
जैसे जनक आदि और संन्यासी भी,
जैसे शुकदेव आदि। पहले तो भगवदर्पण बुद्धि वगैरह से ही कर्म करते हैं। फिर
ज्ञान के बाद कर्तव्यबुद्धि से या विशुद्ध लोकसंग्रह की ही दृष्टि से। यही
बात 56
से
65
तक के
श्लोकों में कहके और इसी पर जोर देके
66वें
में संन्यास के स्वरूप वाले प्रश्न का उत्तर देते हुए साफ कह दिया है कि
''सभी
धर्मकर्मों को छोड़ के अद्वितीय परमात्मा (आत्मा) की शरण जाओ-आत्मज्ञान
प्राप्त करो। उसी के फलस्वरूप सभी पुण्यपाप रूप बन्धानों से छुटकारा हो
जायगा। फिक्र मत करो-''सर्वधार्मान्परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।''
पहले इसी चीज को भक्ति के भी नाम से
54वें
श्लोक में कहा है और
55वें
में बताया है कि यह भक्ति अद्वैत ब्रह्मज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं है।
सातवें अध्याय के
'चतुर्विधा
भजन्ते मां'
आदि 16-19
श्लोकों में भी अद्वैत ज्ञान को ही सबसे ऊँचे दर्जे की भक्ति कहा है।
इसीलिए जो लोग इस श्लोक में शरणागति और प्रपत्ति आदि के नामों से उपासना,
श्रवण,र्
कीत्तान आदि नामक भक्ति की बात सोचते हैं वह सत्य से बहुत दूर हैं। यदि
पहले के ही कुछ श्लोकों पर अच्छी तरह गौर करें तो भी उन्हें पता लग जायगा
कि यहाँ सर्वकर्म-संन्यासपूर्वक अद्वैतज्ञान से ही मतलब है। उसी के बाद
निर्वाण-मोक्ष के लिए कोई चिन्ता करने की गुंजाइश नहीं रहती। बाकी भक्ति
आदि में तो रहती ही है। फलत: फिक्र मत करो,
कहना गलत हो जायगा। क्योंकि यदि और नहीं तो भगवान् को प्रसन्न करने की ही
चिन्ता रह जाती है।
जिस तरह
कर्म और संन्यास की ही बात को लेके अठारहवें अध्याय का विश्लेषण करना
जरूरी हो गया है,
क्योंकि अन्तिम एवं उपसंहारवाला वही है;
उसी तरह दूसरे अध्याय की भी कुछ बातें विचारणीय हैं। पहला अध्याय पूरा का
पूरा और दूसरे के शुरू के दस श्लोकों को गीतोपदेश की भूमिका मानते हैं,
जिसमें उपदेश के लिए भूमि,
क्षेत्र या प्रसंग तैयार किया गया है। यह बात तो श्लोकों के अर्थ के ही समय
और आगे भी विदित होगी।
11वें
श्लोक 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं'
से
उपदेश शुरू होता है। गीता पर शंकर का भाष्य भी इसी श्लोक से शुरू होता है।
बेशक,
उनने भी
भाष्यारम्भ में एक लम्बी भूमिका लिखी है और उसी से हमने शुरू में
'तत्तवज्ञानिनां
कर्म तु'
आदि एक छोटा-सा अवतरण दिया है। इस अध्याय के कुल
72
श्लोकों
में शुरू के
10
तो यों
ही-चले गये। उनके बाद से लेकर
38वें
तक मुख्यत: आत्मा के स्वरूप आदि का विवेचन करके
39वें
में लिखा है कि
''हमने
अब तक सांख्य (तत्तवज्ञान) की जानकारी तुम्हें बतायी है। अब आगे योग की
जानकारी की बात सुनो''-''एषा
तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु।''
इससे स्पष्ट है कि आगे दूसरी-योग की ही-बात कही गयी है।
(शीर्ष पर वापस)
आत्मा का स्वरूप
यह ठीक
है कि योग या कर्मयोग की बात तो
47वें
श्लोक से ही शुरू होती है और 2 श्लोकों में उसके
स्वरूप को अच्छी तरह बताके उसी का विवेचन आगे किया है। लेकिन 39-46
श्लोकों में उसी योग की महत्तासूचक
स्वतन्त्र
प्रस्तावना दी गयी है। यह समूचे गीतोपदेश की प्रस्तावना न होके सिर्फ उसी
योग की है। इसीलिए हमने इसे
स्वतन्त्र
कहा है। यह भी बड़े काम की चीज है,
खासकर योग-सम्बन्धी
आगे की बातें समझने और पिछली बातों के साथ
सम्बन्ध
जानने के लिए। यह योग तो गीता की खास देन है यह पहले ही कहा जा चुका है।
इसीलिए इस पर ज्यादा प्रकाश डालना जरूरी है। इसी दृष्टि से इसकी
स्वतन्त्र
प्रस्तावना के
8
श्लोकों के साथ ही तत्तवज्ञान सम्बन्धी पहले के
11-38 श्लोकों पर भी एक निगाह डालने की आवश्यकता है।
ऐसा करते ही मालूम हो जाता है कि 11-30 श्लोकों
में तो आत्मा की अजरता, अमरता,
निर्विकारिता और नित्यता का प्रतिपादन बहुत अच्छी तरह
किया गया है। यह ठीक है कि वह प्रतिपादन यहाँ
स्वतन्त्र
नहीं है;
किन्तु स्वधर्म
और स्वकर्म की कर्तव्यता की पुष्टि के ही लिए किया गया है। इसी से यह भी
निर्विवाद हो जाता है कि गीतोपदेश की भित्ति
की बुनियाद
अध्यात्मवाद
से ही बनी है। इसीलिए शुरू में वही बात आई है। मरने-मारने के तथा
हिंसा-अहिंसा के ही खयाल से तो अर्जुन स्वकर्म से विचलित हो रहा था। कृष्ण
ने शुरू में ही उसकी जड़ ही काट दी।
उनने कह
दिया है कि मरने-मारने तथा हिंसा-अहिंसा का खयाल तो महज नादानी है।
भीष्मादि की आत्मा तो मरती नहीं और न दूसरों को मारती है। क्योंकि सभी
आत्माएँ अविनाशी और निर्विकार हैं। फिर हिंसा-अहिंसा की बात ही कहाँ रही?
रह
गयी उनके शरीरों की बात। सो तो आज खत्म हुए,
कल
खत्म हुए जैसे ही हैं। उनका नाश तो कोई भी शक्ति-परमेश्वर भी-रोक सकती
नहीं। वह तो अनिवार्य है अवश्यम्भावी है। यदि युद्ध में नहीं,
तो
ज्वर महामारी आदि से ही वे शरीर एक न एक दिन खत्म होंगे ही। फर्क यही है कि
तब मरना केवल मरना होगा। लेकिन अब मरने में मजा है,
बहादुरी है,
नाम और यश है,
आत्मसम्मान है,
''समर
मरण अरु सुरसरि तीरा। रामकाज क्षणभंग शरीरा''
वाली बात है। फिर चिन्ता कैसी?
आगा-पीछा कैसा?
यही तो फायदे का सौदा है।
19वें
और 21वें
श्लोकों में जो करारी डाँट उन लोगों को बताई है जो आत्मा के बारे में
चिन्ता करते और हिंसा-अहिंसा की बातें करते हैं वह बहुत ही सुन्दर है,
निराली है,
खूब है! साफ ही कह दिया है कि जो इस आत्मा को मारने वाली चीज मानते हैं और
जो इसे मरने वाली समझते हैं,
''वे
दोनों ही कुछ नहीं जानते,
बेवकूफ हैं,
नादान,
हैं,
कोरे हैं''-''उभौ
तौ न विजानीत:''
(19)।
इसी तरह 21वें
में साफ ही कहते हैं कि
''जिसने
इस प्रकार आत्मा को अजन्मा अविकार,
सनातन और अविनाशी जान लिया भला वह किसी को मार-मरवा सकता है!''-''वेदाविनाशिनं
नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथं स पुरुष: पार्थ कं घातयति हन्ति कम्!''
यहाँ 'कथं
स पुरुष:'
और
भी सुन्दर है। वह तो मर्द है,
नामर्द तो है नहीं। तब भला वह कैसे मारने-मरवाने की बात सोचे! यह तो
नामर्दी का रास्ता है,
इससे तो नामर्दी और हिचक को प्रोत्साहन मिलता है और मर्द होके वह ऐसा काम
करेगा! यह सारा का सारा वर्णन इतना सरस और युक्ति-दलीलों से भरा है कि
लोट-पोट हो जाना पड़ता है। तर्क भी इतना जबर्दस्त और सामयिक
(uptodate)
एवं
वैज्ञानिक है कि कुछ कहिये मत। एक नमूना सुनिये।
13वें
श्लोक में आत्मा की अविनाशिता की दलील दी गयी है। कहते हैं कि
''एक
ही जन्म में कुमारावस्था,
युवावस्था तथा वृद्धावस्था से हमें आमतौर से गुजरना होता है''-'देहिनोऽस्मिन्यथादेहे
कौमारं यौवनं जरा।'
यह
याद रखना होगा कि इन तीनों अवस्थाओं का शरीर एक हर्गिज नहीं होता। कम से कम
तीन तो होते ही हैं जो एक दूसरे से सोलहों आने जुदा होते हैं। यों तो एक-एक
अवस्था में भी जानें कितने जुदा-जुदा शरीर हो जाते हैं। जिन अनन्त परमाणुओं
से खून,
मांस,
हड़डी आदि
के जरिये किसी एक अवस्था का शरीर बना होता है दूसरी अवस्था में वह एक भी
पाये नहीं जाते! वे तो जाने कहाँ गायब हो जाते हैं और उनकी जगह बिलकुल ही
नये और निराले परमाणु (atoms)
ले
लेते हैं!
नहीं तो तीनों अवस्थाओं में पार्थक्य क्यों होता?
यों भी कुमारावस्था के शुरू में होने वाली देह के साथ युवावस्था के अन्तिम
परिपाक के समय के शरीर से कोई मिलान हो सकती है क्या?
वे
दोनों तो साफ ही जुदे हैं-जुदे
मालूम होते हैं!
फिर वृद्धावस्था से मिलान का सवाल क्या?
विभिन्न अवस्थाओं के जुदे-जुदे
और परस्पर विरोधी काम ही इस बात के सबूत हैं कि शरीर जुदे-जुदे
हैं। बाल्यावस्था की निपट असमर्थता और जवानी की पूर्ण समर्थता के बाद
बुढ़ापे की निराली असमर्थता ही पुकार-पुकार
के अपने-अपने
शरीरों को अलग बताती हैं।
इसे यों
भी समझ सकते हैं। नया चावल कोठी के भीतर बन्द करके रखते हैं और किसी भी तरफ
से हवा न जा सके इसका पूरा प्रबन्ध करते हैं-कोई जरा भी छिद्र या सूराख
रहने नहीं देते। नहीं तो बाहर से कीड़े घुस जायँ और बरसाती हवा चावल को चौपट
कर दे। फिर भी चार-छ: साल के बाद अगर उन्हीं चावलों को निकालें,
पकायें और खायें तो निराला ही स्वाद,
निराली गन्ध और निराली तृप्ति होती है जो बातें नयों में पायी ही न जाती
थीं। पचने में तब भारी थे अब हलके हो गये;
तब
देर से पकते थे,
अब
फौरन पक जाते हैं,
तब
माँड़ को छोड़ते न थे,
अब
माँड़ से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं ऐसा प्रतीत होता है! यह बात क्यों और
कैसे हो गयी! मोटी बुद्धि में तो यह बात समाती नहीं। मगर यह तो मानना ही
होगा कि हजार कोशिश करने और हवा का प्रवेश रोकने पर भी परमाणुओं की आवाजाही
रोकी जा सकती नहीं! वे तो सर्वशक्तिमान जैसे हैं! उनकी अपार महिमा है! फलत:
चावल के भीतर जितने भी पुराने परमाणु थे,
जिनसे वह बना था,
एक-एक करके सभीभाग निकले,
खिसक गये इन्हीं चार-छ: सालों में,
और
उनकी जगह बिलकुल ही नयों ने ले ली! दूसरी बात होई नहीं सकती! हमें पता ही न
लगा और चावल दूसरे हो गये! पहलेवाले फरार हो गये और उनने अपनी जगह दूसरों
को बिठा दिया-ऐसोंको,
कि
कोई गिरफ्तार करी नहीं सकता,
चाहे लाख यत्न करे! पुराने चम्पत! नये हाजिर!
केवल
अन्दाजी बात नहीं है। अब विज्ञान की महिमा से ऐसी प्रयोगशालाएँ
(Laboratories)
बनी
हैं
कि उनमें घुस के आप यह सृष्टि का करिश्मा ऑंखों देख सकते
हैं।
यों तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। मगर अगर किसी
प्रयोगशाला के वैज्ञानिक
यन्त्रों
के सामने अपना हाथ रख दें,
तो हमें आश्चर्यचकित हो जाना होगा यह देखके,
कि किस तेजी के साथ हमारे अपने हाथ से लक्ष-लक्ष परमाणु
हर सेकण्ड में भागे जा रहे
हैं
और उनकी जगह नये घुस रहे
हैं।
हमें ताज्जुब होगा और अवाक् रह जाना पड़ेगा। मगर इसी के साथ साफ-साफ दिखेगा
कि किस प्रकार पुरानी चीज खत्म होके उसकी जगह एकदम नयी और ताजी चीज तैयारी
हो रही है,
हो जाती है। उसी जगह यह भी मालूम हो जायगा कि जानें
कितने ही शरीर पचास-साठ साल के भीतर बने और बिगड़े। हालाँकि यों देखने से
मालूम पड़ता है कि वही एक ही शरीर बराबर बना है-केवल कुछ मरम्मत हुई है या
मुलम्मा चढ़ा है। यही
बात
वत्तामान साम्यवादी अंग्रेज विद्वान् श्री जौन स्टे्रची ने अपनी पुस्तक
'समाजवाद
का सिद्धान्त
और व्यवहार'
(The Theory and Practice of
Socialism)
के
392
पृष्ठ में लिखते हुए
मार्क्सवाद
के मूल नेता श्री फ्रेडरिख एंगेल्स के
'डयूिÐंग
के विरुद्ध'
(Anti Duhring)
पुस्तक
के एक अंश को ज्यों का त्यों
उध्दृत
कर दिया है। वह इस प्रकार है-
"In the same way Engels observes
that the eating and excreting processes, which everyliving thing must
continually maintain, mean that the actual physical structure of every
man (for example) is continually changing. A man is not compased of the
same cells as he was thirty years ago. Not a single one of the atoms of
matter, which then constituted the man is left. And yet we say without
hesitation that it is the same man. The movement or evolution, through
time, of a living organism, seems to present an analogous contradiction
to the movement of an object through space. Life is, therefore, also a
contradiction, which is present in things and processes themselves and,
which constantly asserts and soves itself; and as soon as the
contradiction ceases, life too comes to an end, and death steps
in—'Anti-Duhring,' page 138."
इसका आशय
यह है, ''उसी
तरह एंगेल्स का यह भी कहना है कि हरेक जानदार के लिए जिस खाने और पखाने का
निरन्तर जारी रहना लाजिमी है उसी का यह मतलब है कि हरेक इन्सान वगैरह के
जिस्म की बनावट निरन्तर बदल रही है। तीस साल पहले जिन सजीव झिल्लियों से
मनुष्य का शरीर बना होता है,
वे
उस मुद्दत के बाद रह नहीं जाती हैं। उस समय जिन परमाणुओं से शरीर बना था
उनमें एक भी रह नहीं जाते। फिर भी बिना हिचक कह देते हैं कि यह वही आदमी
है। किसी जीवित पदार्थ का समय पाके जो विकास होता है या उसमें जो गति हो
जाती है,
उसमें जो परस्पर विरोध होता है वह ठीक वैसा ही है जैसा कि किसी पदार्थ के
एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में।
''इसलिए
जीवन भी विरोधी चीज है और यह विरोध खुद पदार्थों और उनकी क्रियाओं में ही
मौजूद है। यह विरोध अपने आप ऊपर आ जाता है और फिर इसका समाधान भी हो जाता
है। यह विरोध ज्यों ही खत्म हुआ कि जीवनलीला का भी अन्त हुआ और मौत आ
धामकी।''
इस प्रकार
अत्यन्त वैज्ञानिक तर्क दलील के साथ गीता ने भी बहुत समय पहले एंगेल्स की
ही तरह कह दिया था कि यदि इस प्रकार परस्पर विभिन्न शरीरों के होते हुए भी
हम उन्हें एक ही मानते हैं,
और
सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा एक ही रहती है;
उसका परिवर्तन या नाश नहीं होता;
इसीलिए तो बचपन की देखी-सुनी बातों की याद बुढ़ापे में भी हो आती है;
तो
वर्तमान शरीर के मिलने के पूर्व और इसके खत्म होने के बाद जो शरीर थे और जो
मिलेंगे उनमें भी उसी आत्मा की सत्ता मानने में क्या अड़चन है जो इस वर्तमान
शरीर में है?
जिस तरह एक जन्म के ही तीन विभिन्न शरीर बताये गये हैं वैसे ही तो तीन
जन्मों के भी तीन हैं और आगे बढ़के तीस और तीन लाख जन्मों के भी होते हैं।
बात तो सर्वत्र एकसी है। यदि बचपन की सभी बातें बुढ़ापे में याद नहीं आती
हैं और शायद ही एकाध का स्मरण होता है। तो दूसरे जन्म के शरीरों के बारे
में भी ऐसा ही होता है। कोई बच्चा पढ़ने या दूसरे ही कामों में कुन्द कोई
तेज और कोई अत्यन्त विलक्षण होता है। इससे मानना पड़ता है कि पूर्व जन्म के
अभ्यास काम कर रहे हैं,
ठीक जैसे निद्रा के बाद पहले पढ़ी-लिखी बात याद आ जाती है। मौत भी तो आखिर
नींद की बड़ी बहन ही है न?
इसमें तम या ऍंधोरे का पर्दा बहुत ही सख्त होने के कारण स्मृति और भी पतली
पड़ जाती है या शायद ही कभी किसी को होती है। लेकिन हमारा प्रयोजन यहाँ इन
बाहरी दलीलों से नहीं है। हमें तो एक ही युक्ति-तर्क को नमूने के तौर पर
पेश कर देना था।
बीच के
'अथ
चैनं नित्यजातं'
(26)
आदि
श्लोकों में जो आत्मा के मरने या विनाश की बात कही गयी है,
वह
तो केवल स्वधर्म से,
विमुख न होने के ही लिए सहकारी तर्क
(supplementary argument)
के रूप
में ही है। वहाँ तो इतना ही कहना है कि जैसे शरीर का नाश अनिवार्य है,
इसीलिए उसे बचाने के खयाल से भी युद्ध
रूप स्वधर्म
से भागना मूर्खता है,
ठीक उसी तरह यदि आत्मा को भी नश्वर और क्षणभंगुर ही मान
लें, तो भी स्वधर्म
से विमुख होना कभी वाजिब नहीं। क्योंकि जो बिगड़ेगा वह फिर बनेगा और जो
बनेगा,
जरूर ही बिगड़ेगा, यही संसार
का नियम है और यह हमारे काबू की बात है नहीं कि इसे ही रोक दें। यदि हम न
भी लड़ें, तो आत्मा का नाश तो होगा ही,
यदि हमने उसे अनित्य मान लिया। बस,
इसका इतना ही मतलब है। ऐसा समझने की भारी भूल कोई न करे
कि ऐसा कहके गीता ने भी आत्मा को विनाशी माना है। सारी की सारी गीता इस सिद्धान्त
के खिलाफ है। सैकड़ों बार आत्मा की अमरता और एकरसता उसमें दुहराई गयी है।
इसके बाद
अध्यात्मवाद के बारे में कुछ भी कहना रह जाता नहीं। फलत:
31-37
श्लोकों में धर्मशास्त्रों के विधि-विधान और दुनिया में नेकनामी बदनामी एवं
आत्मसम्मान के आधार पर उसी स्वधर्म के करने की पुष्टि की गयी है। लोग ऐसा न
समझ बैठें कि जब गीता ने अध्यात्म ज्ञान से ही शुरू किया है तो उसे
सांसारिक हानि-लाभों से कोई वास्ता नहीं है;
इसीलिए गीता की दृष्टि इनकी तरफ कतई नहीं है;
यही वजह है कि इन सभी सांसारिक बातों और खयालों को भी उसने सामने ला दिया
है। यदि ऐसा न होता तो गीता की बात एकांगी एवं अधूरी रह जाती जैसा कि शुरू
में ही कहा है। गीता को सब तरह से पूर्ण और व्यावहारिक बनना था,
पूर्ण अनुभवी बनके ही पथदर्शन करना था और वही चीज न हो पाती,
अगर यश-अपयश,
आत्मसम्मान आदि की ओर से वह नजर फेर लेती। उस दशा में अनुभवी लोग उसमें कमी
पाते और उसकी ओर सहसा खिंच आते नहीं। इसीलिए इस पहलू को भी उसने नहीं छोड़ा
है। विधि-विधान के अनुसार स्वर्ग-नरक आदि भी इसी पहलू के भीतर आ जाते हैं।
इनका स्थान न तो अध्यात्म दृष्टि में है और न योगदृष्टि में ही। इसीलिए वे
भी यहीं दिखाये गये हैं।
(शीर्ष पर वापस)
सांख्य और योग में अन्तर
इसके
बाद योग वाली दृष्टि की ओर जाने के पहले एक ही श्लोक-38वाँ-रह
जाता है। वह यों है; ''सुखदु:खे समे कृत्वा
लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय
युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।''
इसका अर्थ है कि ''जय पराजय,
हानि-लाभ और सुख-दु:ख को समान समझ के-यानी इनकी परवाह न
करके-लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फिर तो तुम्हारे पास पाप फटकने भी न पायगा।''
लड़ाई में हार या जीत-दो में एक-जरूरी है। फलत: तदनुसार
ही हानि या लाभ भी अनिवार्य है। फिर तो दु:ख या सुख खामख्वाह आता ही है।
यही है
साधारण
नियम। ये चीजें बदली जा सकती
हैं
भी नहीं। इसलिए इन्हें समान बनाना असम्भव है। इसीलिए गीता कहती है कि इनका
बाहरी रूप ज्यों का त्यों रहते हुए भी हम इन्हें समान इस तरह बना सकते
हैं
कि दिल-दिमाग पर इनका कोई खास असर न होने दें।
अध्यात्मवाद
या वेदान्त का यह अटल सिद्धान्त
है कि सुख-दु:ख के कारण बाहरी पदार्थ नहीं
हैं।
हम अपने दिल-दिमाग में उन्हें जो स्थान देते या उनका जैसा स्वरूप खड़ा करते
हैं
तदनुसार ही वे सुख-दु:ख आदि के कारण बनते
हैं
और नहीं भी बनते
हैं।
इन्हीं को मानसिक या मनोराज्य के पदार्थ कहते
हैं।
दृष्टान्त
लिए किसी स्त्री को ले सकते हैं। वह तो एक ही प्रकार की होती है-उसका
बाहरी रूप तो एक ही होता है। अब यदि वही भली या बुरी हो या सुख-दु:ख
पहँचाने वाली मानी जाय तो सभी को उसके करते समान रूप से ही सुख या दु:ख
होना चाहिए। मगर ऐसा तो होता नहीं। एक ही स्त्री किसी के लिए सुखद,
किसी के लिए दु:खद और किसी के लिए दोनों में एक भी नहीं होती। जो पुरुष उसे
बहन,
बेटी या
माता मानता है उसकी कुछ और हालत होती है,
जो
उसे स्त्री मानता है उसकी दूसरी ही और जो उसकी तरफ से निरा उदासीन या
लापरवाह है उसकी तीसरी ही दशा होती है। पहली दो हालतों में राग-द्वेष या
प्रेम और जलन की जो बातें पायी जाती हैं। वह तीसरी दशा में कतई लापता हैं।
वेश्या,
धर्मपत्नी और माता के बाहरी रूप में कोई भी अन्तर नहीं होता है। एक ही
स्त्री किसी की माँ,
किसी की पत्नी और किसी के लिए वेश्या भी परिस्थितिवश हो सकती है। इसी से वह
आरामदेह या तकलीफदेह बन सकती है। सो भी एक ही समय में किसी को आराम देने
वाली और किसी को तकलीफ देने वाली। क्यों?
इसीलिए न कि पत्नी,
वेश्या,
माता,
बहन आदि
के रूप में एक ही स्त्री की जुदा-जुदा कल्पना अलग-अलग लोग अपने मनों में
कर लेते हैं?
और
जो विरागी या मस्तराम ऐसी कोई भी कल्पना नहीं करके लापरवाह रहता है उसे उस
स्त्री से सुख या दु:ख कुछ नहीं होता। इसलिए सिद्ध हो जाता है कि किसी भी
पदार्थ का बाहरी रूप कुछ नहीं करता। किन्तु उसका मानसिक रूप जैसा खड़ा किया
जाता है तदनुसार ही वह सुख-दु:खादि का कारण बनता है-उसे वैसा बनना पड़ता है।
इसीलिए
38वें
श्लोक में गीता ने इसकी जड़ ही काट दी है। उसने कह दिया है कि अपने
दिल-दिमाग पर जय-पराजय,
लाभ-हानि और सुख-दु:ख का असर होने ही न दो,
दिल-दिमाग को यह मौका ही न दो कि इन चीजों का रूप अपने भीतर खड़ा कर सके,
ऐसा न होने पाये कि दिल-दिमाग की स्वाभाविक एकरसता,
गम्भीरता और शान्ति को,
ये
सभी अपनी छाया और अपना प्रतिबिम्ब उस पर डाल के,
भंग करें,
बिगाड़ें। फिर तो पौ बारह है,
फिर तो सब कुछ ठीक है,
फिर तो पाप-पुण्य की जड़ ही कट जाती है। पाप-पुण्य के बाप तो ये मानसिक रूप
ही हैं,
चीजों का मानस पटल पर पड़ा हुआ असर और प्रतिबिम्ब ही है,
छाया ही है। इस प्रकार अध्यात्मवाद और वेदान्त के सिद्धान्त के ही आधार पर
कर्म करने की बात का प्रतिपादन पूरा किया गया है। क्योंकि जब आत्मा
निर्विकार और निर्गुण है,
निर्लेप और अजर-अमर है तब तो मानसिक कल्पना के ही चलते वह भटकती है और
पाप-पुण्य में पड़ती है,
जैसे जंगल में भटक जाने वाला काँटेकुशों में बिधता या चोर-डाकुओं से लुटता
है। और जब वही चीज नहीं रही,
जब
मानसिक समता (balance)
बिगड़ने
न पायी,
तो फिर खतरा ही कहाँ रहा?
अब विचार
पैदा होता है कि जिस समता का उल्लेख यहाँ किया गया है उसी का जिक्र आगे
कर्मयोग के प्रकरण के
48वें
श्लोक में आया है। यहाँ भी
'सुखदु:खे
समे कृत्वा'
है
और वहाँ भी 'सिद्धयसिद्धयो:
समो भूत्वा'
लिखा है। ऐसी दशा में दोनों एक ही चीज हो जाती है। फिर अध्यात्मवाद के
प्रकरण के अन्त और योग के आरम्भ के पहले जो
39
श्लोक में
बड़ी तपाक के साथ कहा है कि
'तत्तवज्ञान
की बात कह चुके अब योग की बात सुनो',
उसका तो कोई मतलब रही नहीं जाता। वह बेकार और निरर्थक मालूम पड़ता है। मगर
ऐसा मान भी तो नहीं सकते। गीताकार को क्या इतनी मोटी भी बुद्धि न थी कि यह
बात समझ जायें?
और
जो गीता में सांख्य एवं योग के दो मार्गों का बार-बार जिक्र आया है उसका
क्या होगा?
यह
कोई बच्चों की तो बात है नहीं। इसीलिए कुछ अजीबसा घपला यहाँ आ खड़ा होता है।
यह बात तो
जरूर है। यहाँ दिक्कत तो मालूम होती ही है। इसीलिए जरा गौर से कई बातें
विचारना है। पहली बात यह है कि हम अध्यात्मवाद के उपसंहार वाले
38वें
श्लोक के 'नैवं
पापमवाप्स्यसि'
तथा कर्मयोग की भूमिका के
39वें
श्लोक के 'कर्मबन्धां
प्रहास्यसि'
शब्दों पर भी विचार करें। पहले शब्द तो इतना ही कहते हैं कि
'ऐसा
होने से तुम्हारे पास पाप फटकने न पायेगा।'
उनका इस बात से कोई तात्पर्य नहीं है,
कोई भी प्रयोजन नहीं है कि आया कर्म पाप-पुण्य पैदा करते हैं या नहीं,
कर्मों में पाप-पुण्य पैदा करने की शक्ति है या नहीं। तत्तवज्ञान और
अध्यात्मवाद को इससे कोई भी गर्ज नहीं होती। वह इन बातों की ओर दृष्टि
डालना फिजूल समझता है। बल्कि यों कहिये कि वह ऐसा करने को पतन एवं
पथभ्रष्टता की निशानी मानता है। वह यह बाल की खाल क्यों खींचने लगा?
वह
तो इतना ही कहता है कि जब आत्मा निर्लेप है,
अकर्ता है,
जब
उसमें कर्म हुई नहीं,
तो
फिर कर्म का फल वह क्यों भोगे?
कर्म का फल उसके निकट आये भी क्यों?
आने की हिम्मत भी क्यों करे?
हाँ,
एक ही बात
है कि मन में-दिल-दिमाग में-उसकी कल्पना कर ली जाय तो गड़बड़ हो सकती है,
होती है। इसीलिए उसने उसी चीज को अन्त में रोक दिया है और साफ कह दिया है
कि खबरदार,
दिल-दिमाग की गम्भीरता (serenity)
बिगड़ने न पाये। फिर मजाल किसकी कि फँसा सके?
ऐसी दशा में जहाँ आग का सम्बन्ध ही नहीं वहाँ उसकी लपट,
गर्मी या ऑंच आयेगी कैसे?
और
39वें
श्लोक वाले शब्द?
यह
तो कुछ और ही कहते हैं। वह तो कहते हैं कि
''ऐसा
होने पर कर्मों में जो बन्धकता या बाँधने और फँसाने की शक्ति है वही खत्म
हो जायगी।''
मतलब यह है कि ये शब्द आत्मा के अकर्तव्यत्व आदि का खयाल न करके कर्म के
स्वरूप का ही खयाल करते हैं-इनकी नजर उसी तरफ है। वह कर्मों में फल देने की
ताकत और शक्ति को मान के ही ऐसा उपाय सुझाते है कि वह शक्ति बेकार हो जाए,
मारी जाए। जिस तरह भुने जाने पर बीज में अंकुर पैदा करने की ताकत नहीं रहती,
खत्म हो जाती है,
ठीक उसी तरह कर्म को भी भून देने की बात ये वचन बताते हैं। आत्मा निर्गुण
है,
कर्तव्यशून्य है,
निर्लेप या कि सगुण,
कर्त्तृत्वयुक्त
और लिपटनेवाली-लिपटानेवाली,
इस
खोद विनोद में वे नहीं पड़ते। इस गहरे पानी में वे उतरना नहीं चाहते-उतरते
नहीं। आत्मा चाहे कुछ भी क्यों न हो,
वह
करने वाली ही क्यों न हो,
फिर भी ऐसी युक्ति की जा सकती है कि कर्म ही भून दिये जायँ और सब पँवारा ही
खत्म हो जाय। अतएव यही कहना ठीक है कि इन वचनों की दृष्टि पहले वालों से
ठीक उल्टी दिशा में है-दूसरे किनारे है। यदि इसी श्लोक के बाद का
40वाँ
श्लोक देखें तो वहाँ की
'प्रत्यवायो
न विद्यते'-''पाप
होता ही नहीं रहता ही नहीं'-ऐसा
ही लिखा है। इससे भी यही बात निकलती है कि योगवाली हिकमत या योग की जानकारी
से पाप पैदा होने पाता ही नहीं-उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता-उसकी सत्ता
होने ही नहीं पाती। फिर वह जायेगा किसके निकट?
जो
चीज हुई नहीं,
उससे किसी को खतरा ही क्या। इस प्रकार सांख्य और योग की विशेषता सिद्ध हो
जाती है।
दूसरी बात
भी है। 38वें
श्लोक में युद्धरूप क्रिया या काम के बारे में समत्वबुद्धि की बात नहीं कही
गयी है। किन्तु उसके फलों के ही बारे में। जय-पराजय,
लाभ-हानि और सुख-दु:ख तो युद्ध के परिणामस्वरूप ही क्रमश: एक के बाद दीगरे
होते हैं और उन्हीं के असर से दिल-दिमाग को बचा रखने को कहा है। मगर
48वें
श्लोक में जो सिद्धि-असिद्धि में समता या एकरसता की बात कही गयी है,
वह
कर्मों के ही बारे में है और प्रकृत में युद्ध को ही लेकर है। लड़ाई अन्त तक
हो या बीच में ही रह जाय,
खत्म हो जाय इस बात की परवाह कतई न हो यही योग है। इस बात का दिल पर जरा भी
असर न हो,
यही चीज वहाँ कही गयी है। इस प्रकार जहाँ पहली खूबी में कर्म को भूनने की
बात है,
तहाँ इसमें उसका कोई भी प्रभाव दिल पर न आने देने की बात है। इसी के
फलस्वरूप कर्म भुने जायँगे। यह बुनियादी चीज को ही पकड़ता है। कर्मों का ही
असर न होने दिया जाय तो योग हो गया और उनके नतीजों को ही पास में फटकने न
दिया गया तो सांख्य हो गया।
तीसरी बात
भी है जिससे योग का निरूपण अलग किया गया है। यह ठीक है कि कर्म की
सिद्धि-असिद्धि की लापरवाही को ही योग कहते हैं। मगर सवाल तो यह है कि वह
हो क्योंकर?
जरा देखिये तो सही यह कितनी कठिन चीज है। फल की इच्छा को स्थान न देना,
फल
की ओर से लापरवाह होना,
कर्म में आसक्ति का न होना और कर्मत्याग में आग्रह न रहना-ये चार चीजें
बताई गयी हैं। इनके बताने और इन पर अमल करने का सीधा मतलब यही है कि हमारी
दृष्टि कर्म के ऊपर इस हद तक बँधा गयी हो,
हमारे मन की एकाग्रता (concentration)
कर्म
के ऊपर इस तरह पूर्ण और इतनी पक्की हो गयी हो कि वह फलेच्छा और फल की तो
बात ही जाने दीजिये,
वह तो जुदी चीजें
हैं,
कर्म के त्याग और उसके करने की ओर भी न जा सके! क्या
कमाल है ! कैसी लासानी एकाग्रता की बात है ! किस अलौकिक मनोयोग का निरूपण
है ! मन कर्म में इतना बँधा
है और उस
बन्धन
की सीमा इतनी संकुचित एवं
निर्धारित
है कि कर्म के आगे जो उसका करना या न करना है उसे भी वह देख नहीं सकता,
वहाँ भी वह जा नहीं सकता,
वहाँ जाने की भी उसे इजाजत नहीं है! वहाँ भी उसके लिए 'नो
एडमिशन' (No admission)
ही है।
जो बात दिमाग में आने वाली नहीं जँचती वही लिखी गयी प्रतीत होती है! क्या
खूब!
यह तो ऐसा
ही है जैसा कि छुरे की धार पर होकर गुजरना और फिर भी पाँव को कटने से
बाल-बाल बचा लेना! यह तो सबके लिए सम्भव नहीं। यह तो कोई बिरला ही माई का
लाल कर सकता है! इस अनोखी दैवी कला का पारंगत तो शायद ही कोई होता है,
हो
सकता है। ऐसा वही हो सकता है जो प्राणायाम की क्रिया से समूचे शरीर को तौल
के ऐसा ऊपर-इतना ऊपर उठा ले कि पाँवों का केवल सम्बन्ध ही उस धार पर हो और
शरीर का जरा भी भार उस पर न होने पाये। शरीर न तो इतना ऊँचा उठ जाय कि छुरे
से सम्बन्ध ही टूट जाय,
क्योंकि तब तो उसकी धार पर का चलना कहा जायगा नहीं! और न ऐसा ही उठे कि धार
पर जरा भी-नामममात्र को भी-उसका बोझ पड़े,
क्योंकि तब तो पाँव ही कट जायगा! फिर भी पाँव के द्वारा शरीर का सम्बन्ध भी
धार से बना रहे! उफ,
गजब की करामात है! ठीक यही करामात कर्म के बारे में भी करने की बात
48वें
श्लोक में कही गयीहै!
प्रश्न
होता है कि यह हो कैसे?
यहीं पर मदद करने और इस महान् संकट से उबारने के लिए सांख्य या
अध्यात्मज्ञान आ जाता है। ठीक,
छुरे पर जुटे शरीर की ही तरह यहाँ मन को बहुत ऊँचा उठना होगा,
ऊँचा उठाना होगा। वह इतना ऊपर चला जाय कि कर्म के अलावा बाकी सभी चीजें
अनन्त दूरी पर-बहुत नीचे दूर-पड़ जायँ। उन सबों से मन बेलाग हो जाय। मगर उसी
के साथ कर्म से सम्बन्ध भी जुटा रहे-वह टूटने न पाये। जब तक वह
अध्यात्मदर्शन और तत्तवज्ञान की पूर्णता के फलस्वरूप बड़ी ऊँचाई
(high plane)
पर चला
नहीं जाता,
खामख्वाह गड़बड़ी होगी और खतरा बराबर बना रहेगा कि कभी
इधर
और कभी
उधर
जाय। मन की इसी दशा को-इसी ऊँचाई को-चौथे अध्याय
के 'गतसंगस्य
मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस:' (23) श्लोक में
'ज्ञानावस्थितचेता:'
या ज्ञानावस्थित
चित्त
कहा है। वह ज्ञान में डूब जाता है। तीसरे अध्याय
के 'यस्त्वात्मरतिरेव'
श्लोक में इसे ही 'आत्मरति:'
और 'आत्मतृप्त:'
कहा है। जो अमृत में डूबा है उसे शर्बत की परवाह क्यों
हो? यही बात यहाँ है। जो आत्मानन्द में मस्त है,
उसी में तृप्त है, उसी में
डूबा है वह
इधर-उधर
क्यों
जाय?
फिर भी एक ओर-सिर्फ कर्म की ओर-जाना भी है ! यही तो
निरालापन है! गीता में इस हालत का वर्णन बार-बार आया है। यही ज्ञान की असली
अवस्था है और इसी की मदद से मन कर्म के आगे-पीछे बाल भर भी नहीं बहकेगा।
नहीं तो वहीं कट जायगा! यही योग है जिसमें आत्मज्ञान मददगार है।
योग में
आत्मज्ञान निहायत जरूरी है और उसी के फलस्वरूप जो सिर्फ कर्म तक ही मन
पहुँचने दिया जाता है इसी युक्ति,
इसी हिकमत और इसी कला की आगे भी प्रशंसा की गयी है। दरअसल योग में तीन
चीजें हैं। एक तो कर्म है। दूसरी उसी तक मन या बुद्धि की पहुँच और तीसरी
चीज है इसी के लिए जरूरी तथा आधारभूत आत्मदर्शन या आत्मा का साक्षात्कार।
इनमें कर्म के सिवाय शेष दो को ही एक साथ मिला के योग के सम्बन्ध की बुद्धि,
जानकारी या कला कहा गया है
'बुद्धिर्योगेत्विमां
शृणु' (2।
39)
में। इन
दोनों में भी असली चीज वही आत्मज्ञान है। क्योंकि उसी के बल पर ऊँचे उठ के
मन कर्म से आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए
'दूरेण
ह्यवरं कर्म'
(2।
49)
और
'बुद्धियुक्तो
जहातीहं' (2।
50)
श्लोकों
में कह दिया है कि
''इस
बुद्धि या ज्ञान के योग यानी सम्बन्ध को हटा देने पर बचा-बचाया कर्म तो
रद्दी चीज है,
बहुत बुरा है। इसलिए कर्म से पैदा होने वाले अनर्थों से बचने के लिए इसी
बुद्धि की शरण जाओ। इसके बिना तो फल की आकांक्षा आदि के चलते दुर्दशा होती
है।'' ''विपरीत
इसके यदि वह इस बुद्धि से युक्त-इससे सम्बन्ध-हो जाय,
तो
पुण्य-पाप दोनों से ही उसका पिण्ड छूट जाता है। अतएव योग की ही प्राप्ति के
लिए कोशिश करो वही तो कर्म की कला,
हिकमत या विशेषज्ञता है।''
यहाँ
50वें
श्लोक में जो पुण्य-पाप से पिण्ड छूटने की बात कही गयी है वह ठीक वैसी ही
प्रतीत होती है जैसी आत्मज्ञान के फलस्वरूप
38वें
श्लोक में बताई गयी है। इससे यह खयाल हो सकता है कि ज्ञान और योग में कोई
फर्क नहीं है। मगर इसी के बाद के
51वें
श्लोक में जो
'हि'
शब्द दिया गया है और जिसका अर्थ है
'क्योंकि'
उससे पता लगता है कि वह श्लोक पहले के मतलब को स्पष्ट करता है। पहले में जो
कुछ इस तरह के शक की गुंजाइश है उसे खुद समझ के ही वह इस पर और भी प्रकाश
डालता है। अब जरा
'कर्मजं
बुद्धियुक्ता हि'
आदि उस श्लोक का अर्थ देखिये। वह यों है,
''क्योंकि
बुद्धियुक्त (बुद्धिवाले) मनीषी लोग कर्मों से पैदा होने वाले फलों को छोड़
के जन्ममरण रूप बन्धन से छुटकारा पा जाते और निरुपद्रव स्थान में पहुँच
जाते हैं।''
पहले श्लोकों में जो पुण्य-पाप के त्यागने या उनसे पिण्ड छूटने की बात कही
गयी है ठीक उसी का उल्लेख इस श्लोक में
''कर्मों
से पैदा होने वाले फलों को छोड़ के'
इन
शब्दों में किया है और कहा है कि जन्ममरण रूप बन्धन से वे छूट जाते हैं।
पहले श्लोक के
'बुद्धियुक्ता:'
की
ही जगह यहाँ
'मनीषिण'
कहाहै।
अब यदि इन
सभी बातों को मिला के गौर करें तो पता चलेगा कि भूमिका वाले
39, 40
श्लोकों में जो कुछ कहा गया है कि योग के करते कर्मों की बन्धनशक्ति खत्म
हो जाती है और पुण्य-पाप होने पाते ही नहीं,
वही बात यहाँ समर्थन के रूप में दुहराई गयी है। इसीलिए श्लोक में
'बन्धा'
शब्द भी आया है। असलियत यह है कि कर्मों में ही जो मन बुद्धि जम गयी है
उसका परिणाम यह होता है कि बन्धन से छुटकारा मिलता है। कर्म से हट के एकाएक
बन्धन पर जा पहुँचे और उसे खत्म किया! कर्म और बन्धन के बीच में कई सीढ़ियाँ
पड़ती हैं। योगवाले उन्हें फाँद जाते हैं! कर्म का तो सबसे पहले तत्काल फल
होता ही है जय-पराजय आदि के रूप में। फिर उसके बाद दूसरा फल आता है जिसे
पुण्य-पाप कहते हैं। तब कहीं जाके बन्धन आता है उन्हीं पुण्य-पापों के
फलस्वरूप। योग के चलते कर्म और बन्धन के बीच के इन दो फलों-दो सीढ़ियों से
सबका पड़ता ही नहीं। उनसे कोई भी नाता नहीं होता-वह होते ही नहीं। फिर बन्धन
यानी जन्ममरण कैसा?
सांख्य या ज्ञान में भी बन्धन तो होता नहीं। मगर बीच के दो फल होते हैं
जरूर;
हालाँकि
आत्मा से उनका कोई भी नाता न होने के कारण वे उसमें सटते नहीं। क्योंकि
कर्म ही जब उसमें सटता नहीं,
है
नहीं,
तो उसके
फल कैसे आयेंगे?
विपरीत इसके योग में कर्म आत्मा में आये और सटे तो क्या और न सटे तो क्या?
वहाँ इससे कोई मतलब हुई नहीं। मगर बीचवाले फल नहीं सटते यह पक्का है। पहले
पक्ष में पक्कापक्की कर्म ही नहीं सटता है और इसी से ये फल नहीं सटते। मगर
इस पक्ष में पक्कापक्की यह नहीं सटते हैं। फिर कर्म सटके भी क्या करेगा?
दोनों का यही मौलिक भेद-बुनियादी फर्क-यहाँ साफ हो जाता है।
(शीर्ष पर वापस)
व्यवसायात्मक बुद्धि
अब एक
ही बात इस योग के मुतल्लिक रह जाती है जिसका जिक्र
'व्यवसायात्मिका'
आदि 41वें श्लोक में है। उसी
का स्पष्टीकरण आगे के 42-44 श्लोकों में भी किया
गया है, बल्कि प्रकारान्तर से 45-46
में भी। इन श्लोकों में कहा गया है कि योगवाली बुद्धि
एक ही होती है,
एक ही प्रकार की होती है और होती है वह निश्चित,
निश्चयात्मक
(definite)।
उसमें सन्देह आगा-पीछा या अनेकता की गुंजाइश होती ही नहीं। विपरीत इसके जो
योग से अलग
हैं,
जिनका ताल्लुक योग से
हुई
नहीं उनकी बुद्धियाँ
बहुत होती
हैं
और एक-एक की अनेक शाखा-प्रशाखाएँ होती
हैं।
वे अनिश्चित तो होती ही
हैं।
कहने का मतलब यह है कि जहाँ योगी के खयाल पक्के और एक ही तरह के होते
हैं
तहाँ दूसरों के अनेक तरह के,
कच्चे और
सन्दिग्ध
होते
हैं।
बात सही
भी है। पहले जो कुछ योग के बारे में कहा गया है उससे यह बात इतनी साफ हो
जाती है कि समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होती,
जब
यह कह दिया गया है कि सिवाय कर्म के उसके करने,
न
करने,
छूटने,
न
छूटने,
फल,
उसकी इच्छा,
कर्म की जिद या उसके न करने की जिद-इनमें किसी भी-की तरफ मन या बुद्धि को
जाने का हक नहीं है,
जाने देना नहीं चाहिए,
जाने दिया जाता ही नहीं या यों कहिये कि जाने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती,
तो
फिर बुद्धि या खयाल का एक ओर निश्चित होना अवश्यम्भावी है। पहले से ही
निश्चित एक ही चीज-कर्म-से जब वह डिगने पाता नहीं,
तो
फिर गड़बड़ी की गुंजाइश हो कैसे और अनेकता या सन्देह इसमें घुसने भी पाए कैसे?
मगर जहाँ
यह बात नहीं है और खयाल को-बुद्धि या मन को-आजादी और छूट है कि फलों की ओर
दौडे,
सो भी
पहले से निश्चित फलों की ओर नहीं,
किन्तु मन में कल्पित फलों की ओर,
वह
बुद्धि तो हजार ढंग की खामख्वाह होगी ही। एक तो कर्मों के फलों की ही तादाद
निश्चित है नहीं। तिस पर तुर्रा यह कि कर्म करने वाले रह-रह के अपनी-अपनी
भावना के अनुसार फलों के बारे में हजार तरह की कल्पनाएँ-हजार तरह के
खयाल-करते रहते हैं। यही कारण है कि फल और फल की इच्छा या कल्पना को
जुदा-जुदा रखा है। क्योंकि कर्मों के फल तो पहले से निर्धारित या बने-बनाये
होते नहीं। वे तो नये सिरे से बनते हैं,
बनाये जाते हैं। हर आदमी चाहता है कि एक ही कर्म का फल अपने-अपने मन के
अनुसार जुदी-जुदी किस्म का हो। यह भी होता है कि एक ही आदमी खुद रह-रह के
अपने खयाल फलों के बारे में बदलता रहता है। परिस्थिति उसे मजबूर करती है।
एक ही युद्ध के फलों की कल्पना हर लड़नेवाले जुदी-जुदी करते हैं। साथ ही एक
आदमी की जो कल्पना शुरू में होती है मध्य या अन्त में वह बदल जाती है,
ठीक उसी हिसाब से जिस हिसाब से उसे अपनी शक्ति और मौके का अन्दाज लगता है।
इसी के साथ यदि कर्मों के करने न करने या उनके छोड़ने न छोड़ने के हठों की
बात मिला दें,
तब
तो बुद्धि और खयालों के परिवार की अपार वृद्धि हो जाती है। वह पक्की चीज तो
होती ही नहीं। कभी कुछ खयाल तो कभी कुछ। एक ही फल के विस्तार का रूप भी
विभिन्न होता है।
मगर योग
में तो सारा झमेला ही खत्म रहता है। वहाँ तो
'न
नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी'
वाली बात होती है। इसीलिए उसकी महत्ता बताई गयी है।
52
से लेकर 72
तक-अध्याय के अन्त तक-के श्लोकों में उसी बुद्धि का विशद चित्र खींचा गया
है। वह कितनी कठिन है,
दु:साध्य है यह भी बताया गया है। मस्ती की अवस्था ही तो ठहरी आखिर। इसीलिए
तीसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में उसी बुद्धि की यह महिमा जान के अर्जुन
ने कर्म के झमेलों से भागने और उस बुद्धि का ही सहारा लेने की इच्छा जाहिर
की है। मगर यह तो ठीक ऐसी ही है जैसी कि किसी की एकाएक गुरु बन जाने की ही
इच्छा।
गीता - 3
(शीर्ष पर वापस)