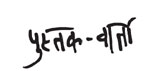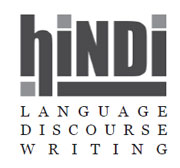अठारहवाँ
अध्याय-
I
(श्लोक
01 -
44)
पीछे
के सत्रह
अध्यायों
में ही गीता के सभी विषयों का आद्योपान्त निरूपण हो गया। अब कुछ भी
कहना बाकी न रहा। इसीलिए कृष्ण को भी स्वयं आगे कुछ भी कहने की
आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। इसीलिए अर्जुन के प्रश्न के
उत्तर
में ही बची-खुची बातें कहते हुए,
या यों कहिए कि कही हुई बातों को ही दुहराते एवं
शब्दान्तर से उनका स्पष्टीकरण करते हुए,
उनने सबों का उपसंहार इस
अध्याय
में किया। यदि गौर से देखा जाय तो इस
अध्याय
में न तो कोई नयी बात ही कही गयी है और न किसी बात को कोई ऐसा रूप ही
दिया गया है जो पहले दिया गया न रहा हो,
या जो बिलकुल ही नया हो। त्याग का ब्योरा,
कर्ता,
बुध्दि आदि की त्रिविधाता,
वर्णों के स्वाभाविक कर्म आदि में एक भी बात नयी
नहीं है और न यहाँ किसी को नया रूप ही मिला है। या तो गीता के बाहर
ही ये बातें प्रचलित रही हैं या, ऐसा न
होने पर भी, गीता में ही पहले आ गयी हैं।
जो लोग इससे पहले के
अध्यायों
को
ध्यान
से पढ़ गये हैं उन्हें यह बात साफ मालूम होती है। त्याग के बारे में
कई मत कह देना यह गीता की बात न भी हो तो कोई नयी तो है नहीं। इसकी
बुनियादी चीजें,
जिन्हें फलेच्छा और आसक्ति का त्याग कहते हैं,
पहले जानें बीसियों बार कही जा चुकी हैं।
सात्तिवकादि तीन विभाग तो चौदहवें में और
सत्रहवें
में भी आया ही है। कुछ चुने-चुनाये और भी दृष्टान्त देने से ही
नवीनता आ जाती नहीं। आत्मा का
अकर्तव्य
और गुणों का
कर्तव्य
भी पहले आयी चुका है। सो भी अच्छी तरह। इस तरह प्रारम्भ के चौवालीस
श्लोकों तक पहुँच जाते हैं।
उसके बाद के
पूरे 22
श्लोक में कुछ में जो स्वधर्मानुष्ठान की महत्ता बताई गयी है और उसी
के द्वारा कल्याण की बात कही गयी है वह भी पहले खूब ही आयी है। फिर
संन्यास यानी स्वरूपत: कर्मों के त्याग की बात जरूरी बता के जिसके
लिए वह जरूरी है उस समाधि या ध्यान का भी वर्णन कुछ श्लोकों में
किया है। अनन्तर उसी समदर्शन का वर्णन किया है जिसका बार-बार वर्णन
आता रहा है। उसी में ज्ञानीभक्त नामक चौथे भक्त का भी जिक्र है। जो
लोग ज्ञान के बाद भगवान् में ही कर्मों को छोड़ के लोकसंग्रह के काम
करते हैं उनका वर्णन करके हठ के साथ उलट-पलट करने या बातें न मानने
से अर्जुन को रोका-समझाया है। यह भी कहा है कि यकीन रखो,
तुम्हें प्रिय समझ के ही यह उपदेश दे रहा हूँ;
न कि
इसमें मेरा कुछ दूसरा भी मतलब है। फिर भी ऑंखें मूँद के कुछ भी करने
को नहीं कहता। करो,
मगर
खूब सोच-समझ के! अन्धपरम्परा अच्छी नहीं है। अन्त में
66वें
श्लोक में संन्यास यानी कर्मों के स्वरूपत: त्यागने का,
जिसके
बारे में अर्जुन का प्रश्न था,
वर्णन
कर दिया है। इस तरह गीतोपदेश पूरा किया है। अन्त में ऐसा कहने का
मौका भी इसीलिए आ गया है कि आत्मा में मन को हर तरह से बाँध देने का
जो अन्तिम उपदेश अर्जुन को दिया है वह तब तक सम्भव नहीं जब तक
नित्य-नैमित्तिक या नियत धर्मकर्मों से छुट्टी न ली जाए
?
इसके बाद से
अन्त तक गीतोपदेश के नियम,
शिष्टाचार और परम्परा आदि का ही वर्णन है। अन्त में कृष्ण ने पूछा है
कि बातें समझ में आयीं या नहीं
? इस
पर अर्जुन ने उत्तर दिया है कि हाँ,
सब समझ
गया और आपकी बातें मानूँगा। इसके बाद के पाँच श्लोक तो संजय की उस
समय की मनोवृत्ति की विचित्रता बताने के साथ ही कौन जीतेगा,
कौन
हारेगा यही बातें कहते हैं। एक श्लोक कृष्ण के उस निराले तथा अलौकिक
स्वरूप की याद दिलाता है जो अर्जुन को उपदेश देने के समय था और जिसका
वर्णन हमने पहले ही अच्छी तरह कर दिया है। अब इनमें नयी बात कौन सी आ
गयी है जिसके पीछे माथापच्ची की जाय
?
यही वजह है कि
अर्जुन ने आरम्भ में प्रश्न भी नहीं किया। उसने तो केवल इच्छा जाहिर
की। सो भी संन्यास या त्याग का न तो अर्थ ही जानने के लिए है और न
उनके लक्षण ही। दोनों शब्दों के अर्थ तो एक ही हैं यह पहले ही बता
चुके हैं। यह भी दिखा चुके हैं प्रश्न के बाद दोनों शब्द यहाँ भी एक
ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। लक्षण की भी बात नहीं है। क्योंकि
यहाँ लक्षण न कह के त्याग के बारे में नाना मत ही बताये गये हैं। इसे
लक्षण तो कहते नहीं। चार मतों के सिवाय कृष्ण ने जो अपना मत कहा है
वह भी न तो नया है और न लक्षण ही है। किन्तु केवलर् कर्तव्यता की
बात ही उसमें है। असल में ज्ञान के अलावे गीता की तो दोई खास बातें
हैं। उनमें एक को कर्मों का संन्यास या स्वरूपत: त्याग कहते हैं तथा
दूसरे को साधारणत: केवल
'त्याग'
कहते
हैं। मगर हैं ये दोनों कठिन तथा विवादग्रस्त। इसीलिए पहले बार-बार
इनका जिक्र आया है। संन्यास का तो आया ही है। त्याग का भी
'संगं
त्यक्त्वा धनंजय'
(2।48),
'त्यक्त्व
कर्मफलासंगं' (4।20)
'संग
त्यक्वात्मशुध्दये'
(5।11),
'युक्त:
कर्मफलं त्यक्त्वा'
(5।12)
तथा
अन्त में 'सर्वकर्मफलत्यागं'
(12।11)
आदि
में जिक्र आया है। इसलिए अन्त में अर्जुन यही जानना चाहता है कि जब
ये दोनों इतने विलक्षण हैं,
गहन
हैं,
और
'कवयोऽप्यत्रमोहिता:'
(4।16)
में यह
भी कहा गया है कि बड़े से बड़े चोटी के विद्वान् भी इनके बारे में घपले
में पड़ जाते हैं,
तो इन
दोनों की अलग-अलग हकीकत,
असलियत
या तत्तव क्या है। उसके कहने का यही मतलब है कि इनके बारे में जो भी
विभिन्न विचार हों उन्हें जरा सफाई और विस्तार के साथ कह दीजिए,
ताकि
सभी बातें जान लूँ। इसीलिए त्याग के ही बारे में पहले पाँच तरह के
विचार कृष्ण ने दिखाये हैं-चार दूसरों के और एक अपना। संन्यास के
बारे में तो ऐसे अनेक विचार हैं नहीं। इसीलिए अर्जुन के शब्दों में
पहले आने पर भी कृष्ण के शब्दों में वह पीछे आया है। उसके बारे में
केवल यही बात विस्तार से कहने की थी कि उसका मौका कब और कैसे आता है।
यही उनने बताई भी है। वह अन्तिम चीज भी तो है। इसलिए अन्त में ही उसे
कहना उचित भी था। कुछ लोग नादानी से कर्मों को हर हालत में छोड़ देना
ही संन्यास समझते हैं। उससे निराली ही चीज संन्यास है,
यह भी
बात संन्यास का तत्तव बताने से मालूम हो गयी है। नहीं तो मालूम हो न
पाती। इसीलिए जो लोग संन्यास के सम्बन्ध की जिज्ञासा का उत्तर पहले
ही मान लेते हैं वह मेरे जानते भूलते हैं। क्योंकि उनके मन से तो
पीछे संन्यास का जिक्र निरर्थक हो जाता है।
इसी अभिप्राय
से ही-
अर्जुन
उवाच
संन्यासस्य महाबाहो तत्तवमिच्छामि वेदितुम्।
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन॥1॥
अर्जुन ने कहा
(कि) हे महाबाहो,
हे
हृषीकेश,
हे केशिनाशक,
संन्यास और त्याग दोनों ही की अलग-अलग हकीकत जानना चाहता हूँ।1।
श्रीभगवानुवाच
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु:।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा:॥2॥
त्याज्यं दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिण:।
यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यमिति चापरे॥3॥
श्री भगवान्
ने कहा (कि) (कुछ) विद्वान् सकाम कर्मों के त्याग को ही त्याग मानते
हैं, (दूसरे)
विवेकी जन सभी कर्मों के फलों के त्याग को ही त्याग कहते हैं,
कोई-कोई मनीषी-मननशील पुरुष-कहते हैं कि कर्ममात्र का ही त्याग करना
चाहिए जैसे बुराई का त्याग किया जाता है। और चौथे दलवाले कहते हैं कि
यज्ञ,
दान और तप
जैसे कर्मों को छोड़ना चाहिए ही नहीं।2।3।
यहाँ चार
स्वतन्त्र मत बताए गए हैं और चारों का ताल्लुक त्याग से ही है। अपना
पाँचवाँ मत कृष्ण आगे बताते हैं। इनमें तीसरा ही मत ऐसा है जो कर्मों
का त्याग हर हालत में हमेशा मानता है और कहता है कि जैसे दोष का
त्याग हमेशा हर हालत में करते हैं वैसे ही कर्म का भी होना चाहिए।
यहाँ 'दोषवत्'
का
अर्थ है दोष की तरह ही। दोषवत् का अर्थ दोषवाला भी होता है। इस तरह
यह अर्थ होगा कि कर्म तो दोषवाला हुई। इसी से उसे छोड़ ही देना ठीक
है। मगर कर्म का यह स्वरूपत: त्याग संन्यास नहीं है यही गीता का मत
है। यह मानती है कि ऐसा न करके केवल समाधि के पहले ही उसे त्यागने को
संन्यास कहते हैं। यही बात
'सर्वधर्मान्
परित्यज्य'
में
आगे लिखी गयी है। पूर्ण ज्ञान के परिपाक के हो जाने पर मस्ती की दशा
में भी कर्मों का त्याग स्वरूपत: हो जाता है ऐसा गीता का मान्य है,
जैसा
कि 'यस्त्वात्मरतिरेव
स्यात्' (3।17)
में
स्पष्ट है। मगर हर हालत में कर्मों का त्याग न तो उसे मान्य है और न
सम्भव,
जैसा कि
'नहि
कश्चित्' (3।5)
से
स्पष्ट है।
निश्चयं
शृणु मे तत्रा त्यागे भरतसत्तम।
त्यागो
हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा: संप्र्रकीत्तित:॥4॥
हे भरत
श्रेष्ठ,
हे पुरुषसिंह,
उस
त्याग के बारे में मेरा निश्चय भी सुन लो। क्योंकि त्याग तीन तरह के
होते हैं।4।
इस श्लोक के
उत्तारार्ध्द का यह भी आशय हो सकता है कि
''क्योंकि
त्याग के बारे में तीन बातें कही जा सकने के कारण वही तीन ढंग से
जानने योग्य है।''
इनमें
पहली बात वह है जो पाँचवें श्लोक के पूर्वार्ध्द में आयी है कि यज्ञ,
दान,
तप को
न छोड़ के करना ही चाहिए। दूसरी उत्तारार्ध्द में पहले कथन के हेतु के
रूप में ही आयी है कि ये यज्ञादि मनीषियों को भी पवित्र करने वाले
हैं। इसीलिए इन्हें करना ही चाहिए। तीसरी बात छठे श्लोक में है कि
आसक्ति और फल दोनों को ही छोड़ के इन्हें करना चाहिए। इस प्रकार तीन
बातें हो गईं। सारांश रूप में पहली यह कि यज्ञ,
दान,
तप को
कभी न छोड़ें। दूसरी यह कि उन्हें जरूर करें;
क्योंकि यह पवित्र करने वाले हैं। तीसरी यह कि इनके करने में भी कर्म
की आसक्ति और फल की इच्छा को छोड़ ही देना होगा। यही तीन तरह की बातें
त्याग को लेकर हो गयीं।
यज्ञदानतप: कर्म न त्याज्यं कार्यमेव च।
यज्ञो
दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥5॥
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च।
कर्त्तव्यानीति
मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥6॥
यज्ञ,
दान,
तप इन
कर्मों को (कभी) नहीं छोड़ना,
(किन्तु)
अवश्य ही करना चाहिए। (क्योंकि) यज्ञ,
दान,
तप ये
मनीषियों को भी पवित्र करते हैं। (फिर औरों का क्या कहना
?) (लेकिन)
इन कर्मों को भी,
इनमें
आसक्ति और फलेच्छा को छोड़ के ही,
करना
चाहिए,
यही मेरा
निश्चित उत्तम मत है।
5।6।
चौथे श्लोक
में जो सीधा-साधा अर्थ करके त्याग के तीन प्रकार कहे हैं वह ये हैं-
नियतस्य
तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्यते।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीर्तित्तत:॥7॥
दु:खमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्तयजेत्।
स
कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥8॥
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन।
संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग: सात्तिवको मत:॥9॥
जो कर्म जिसके
लिए तय कर दिया गया है उसका त्याग तो उचित नहीं (और अगर) मोह से उसका
त्याग (कर दिया गया) तो वह तामस (त्याग) कहा जाता है। शरीर के कष्ट
के भय से दु:खदायी समझ के ही कर्म का त्याग जो करता है वह (इस तरह)
राजस त्याग करके त्याग का फल हर्गिज नहीं पाता। हे अर्जुन,र्
कर्तव्य समझ के ही आसक्ति एवं फल के त्यागपूर्वक जो निश्चित कर्म
किया जाता है वही सात्तिवक त्याग माना जाता है।7।8।9।
आगे के तीन
श्लोक इस सात्तिवक त्याग की रीति और आकार बताने के साथ ही उसके कारण
और परिणाम भी कहते हैं। ये तीनों बातें क्रमश: तीन श्लोकों में पायी
जाती हैं।
नद्वेष्टयकुशलंकर्मकुशलेनानुषज्जते।
त्यागी
सत्तवसमाविष्टो मेधावी
छिन्नसंशय:॥10॥
न हि
देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषत:।
यस्तु
कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥11॥
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधां कर्मण: फलम्।
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्॥12॥
संशयरहित
विवेकी सात्तिवक त्यागी न तो बुरे कर्म से द्वेष करता है। (और) न
अच्छे में आसक्त हो जाता है। जब कि देहधारी के लिए सभी कर्मों का
त्याग करना सम्भव ही नहीं है,
तो जो
केवल कर्म के फल का त्याग करता है। वही (सात्तिवक) त्यागी कहा जाता
है। बुरा,
भला और
मिश्रित यह तीन तरह का कर्म फल मरने के वाद सात्तिवक त्याग न करने
वालों को ही मिलता है;
न कि
त्यागियों को भी कहीं (मिलता है)।10।11।12।
पतंजलि ने
योगदर्शन में लिखा है कि साधारण मनुष्यों के कर्म तीन प्रकार के होते
हैं,
जिन्हें शुक्ल,
कृष्ण
और शुक्ल-कृष्ण या मिश्रित कहते हैं। इन्हीं को भले,
बुरे
और मिले हुए भी कहते हैं। इनके फल भी क्रमश: भले,
बुरे
और मिश्रित ही होते हैं। इन्हीं को इष्ट,
अनिष्ट
और मिश्र इस आखिरी श्लोक में कहा है। इसके विपरीत योगियों का कर्म
चौथे प्रकार का होता है,
जिसे
अशुक्ल-कृष्ण कहते हैं। इसका अर्थ है-न भला,
न
बुरा। 'कर्माशुक्ल
कृष्णं योगिनस्त्रिविधामितरेषाम्'
(4।7)
योगसूत्र और उसके भाष्य को ध्यानपूर्वक पढ़ने से इसका पूरा ब्योरा
मालूम होगा। बारहवें श्लोक के सात्तिवक त्यागी को उसी योगी के स्थान
में माना गया है। बेशक,
राजस
और तामस त्यागी साधारण लोगों में ही आते हैं।
यहाँ प्रश्न
होता है कि जब कर्मों का कर्ता आत्मा ही है,
तो
आसक्ति या फलों के त्याग मात्र से ही कर्मों के फलों से उसका पिण्ड
कैसे छूट जायगा ?
अगर
कोई चोरी करे तो क्या आसक्ति और फलेच्छा के ही छोड़ देने से उसे चोरी
का दण्ड भोगना न होगा
? इसका
उत्तर आगे के पाँच श्लोक देते हैं। उनका आशय यही है कि आत्मा कर्मों
की करने वाली हुई नहीं। करने-कराने वाले तो और ही हैं और हैं भी वे
पूरे पाँच। ऐसी दशा में जो आत्मा को कर्ता मानता है वह नादान है,
मूर्ख
है। चोरी की बात और है। वहाँ जिस शरीर से वह काम करते हैं वही
जेल-यन्त्रणा भी भोगता है।
पंचैतानिमहाबाहोकारणानिनिबोधमे।
सांख्ये
कृतांते प्रोक्तानि सिध्दये सर्वकर्मणाम्॥13॥
अधिष्ठानं
तथा
कर्ता
करणं च पृथग्विधाम्।
विविधश्च
पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्रा पंचमम्॥14॥
शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नर:।
न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतव:॥15॥
तत्रौवं सति कत्तर्रमात्मानं केवलं तु य:।
पश्यत्यकृतबुध्दित्वान्न स पश्यति दुर्मति:॥16॥
यस्य
नाहंकृतो भावो बुध्दिर्यस्य न लिप्यते।
हत्वापि
स इमाँल्लोकान्न हन्ति न
निबध्यते॥17॥
हे महाबाहो,
सभी
कर्मों के पूरे होने के लिए सांख्य सिध्दान्त में बताये इन (आगे
लिखे) पाँच कारणों को मुझसे जान लो। (वे हैं) आश्रय या शरीर,
आत्मा
की संसर्गवाली बुध्दि,
जुदी-जुदी इन्द्रियाँ,
प्राणों की अनेक क्रियाएँ और पाँचवाँ प्रारब्ध कर्म। शरीर,
वचन या
मन से मनुष्य जो भी कर्म-कायिक,
वाचिक,
मानसिक-शुरू करता है चाहे वह उचित हो या अनुचित,
उसके
यही पाँच कारण होते हैं। ऐसी दशा में अपरिपक्व समझ होने के कारण
निर्लेप आत्मा को जो कोई कर्ता मानता है वह दुर्बुध्दि कुछ जानता ही
नहीं। (इसलिए) जिसके भीतर
'हम
करते हैं'
ऐसा ख्याल
नहीं और जिसकी बुध्दि (कर्म या फल में) लिप्त नहीं होती,
वह इन
सभी लोगों को मार के भी न तो मारता है और न (कर्म में फलस्वरूप)
बन्धन में फँसता है।13।14।15।16।17।
कर्ता का अर्थ
है कर्तव्य का अभिमान जिसमें वस्तुगत्या रहे। दरअसल बुध्दि को ही
कर्ता कहते हैं। मगर बिना आत्मा के संसर्ग के वह खुद जड़ होने के कारण
कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए आत्मा के संसर्ग या प्रतिबिम्ब से युक्त
बुध्दि को ही कर्ता कहते हैं। इसी प्रकार दैव का अर्थ प्रारब्ध पहले
ही कह चुके हैं। यह भी बता चुके हैं कि इसे दिव्य या दैव क्यों कहते
हैं और यह क्यों कारण माना जाता है। यह भी जान लेना चाहिए कि कारणदो
प्रकार के होते हैं-साधारण और असाधारण। साधारण उसे कहते हैं जो सबों
को या अनेक कार्यों को पैदा करे। प्रारब्ध ऐसा ही है। वह समस्त संसार
का कारण है। किन्तु शरीर,
बुध्दि,
इन्द्रियाँ तथा प्राण की क्रियाएँ या पाँच प्राण अलग-अलग कार्यों के
कारण हैं। इसीलिए ये असाधारण या विशेष कारण कहे जाते हैं। अपने-अपने
शरीर आदि से ही अपने-अपने कर्म होते हैं। प्राणों के निकल जाने पर या
इन्द्रियों के खत्म हो जाने पर भी क्रिया नहीं होती। बुध्दि की भी
जरूरत हर काम में होती ही है। बिना जाने कुछ कर नहीं सकते।
आखिरी श्लोक
में जो कुछ कहा गया है उसका आशय यही है कि जैसे दूसरे की चोरी का माल
अपने घर में रखने वाला नाहक अपराधी बनता है और परेशानी में पड़ता है,
ठीक
वही हालत आत्मा की है। कर्मों के करने वाले तो ठहरे शरीर आदि। मगर
उनकी क्रिया को धोखे में,
भूल से
अपने भीतर मानने के कारण ही इस निर्लेप और निर्विकार आत्मा को फँसना
पड़ता है। पुत्र के साथ ज्यादा ममता होने से कभी-कभी ऐसा होता है कि
पुत्र की मौत का निश्चय होते ही पिता उससे भी पहले एकाएक चल बसता है।
शरीर दुबला और मोटा होने से आत्मा को ख्याल होता है कि हमीं दुबले
या मोटे हैं। यही है गैर के साथ एकता या तादात्म्य-तदात्मा का
अभिमान। इसे तादात्म्याध्यास भी कहते हैं। आत्मा का शरीर,
इन्द्रियादि के साथ तादात्म्याध्यास हो गया है। फलत: उनके कामों एवं
गुणों को अपना मानने का स्वभाव इसका हो गया है। इसे ही मिटाने का
अर्थ है अहंकार का त्याग,
'हमीं
करते हैं'
इस भावना और
ख्याल का त्याग।
लेकिन इसके
होने पर भी कर्म में आसक्ति होने पर,
आग्रह
हो जाने पर और फल की भावना होने पर भी फँस जाता है। यह है दूसरा खतरा
और भारी खतरा। इस पर पूरा प्रकाश पहले डाला जा चुका है। आत्मा का
साक्षात्कार होने के बाद अहंकार वाला भाव मिट जाने पर भी यह खतरा बना
रहता है। इसीलिए बुध्दि के लिप्त न होने की बात कह के इसी खतरे से
बचने की हिकमत सुझाई गयी है। फिर तो पौ बरह समझिए। इस तरह एक प्रकार
से आत्मा को कर्म से निर्लिप्त और अलग बता के काम निकाल लिया है।
अब आगे दूसरे
ढंग से भी आत्मा का कर्मों से असंसर्ग सिध्द करते हैं। ऐसा भी होता
है कि स्वयं कर्म न भी करें तो भी दूसरों से करवा सकते हैं। इसे ही
प्रेरणा कहते हैं। इसी को शास्त्रों में चोदना कहा है। ऐसों को करने
वाले तो नहीं,
लेकिन
कराने वाले मान के ही अपराधी बताते हैं और दण्ड देते हैं। हिंसा,
चोरी
आदि में ऐसा होता है कि ललकारने या राय देने वाले भी फँसते हैं और
दण्ड भोगते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमने न तो चोरी की,
न
उसमें राय-सलाह ही दी और न ललकारा ही। यह भी नहीं जानते कि कहीं चोरी
हुई या नहीं। मगर यदि किसी से शत्रुता हुई तो चुपके से चोरी का माल
हमारे यहाँ रख के फँसा देता है। अकसर गैरकानूनी रिवॉल्वर वगैरह चुपके
से किसी के घर में रख के फँसा देते हैं। यदि कर्म का प्रेरक ही आत्मा
हो जाय,
या वस्तुत:
कर्म उसी में रहते हों,
हर
हालत में उसे उनके फलों में खामख्वाह फँसना होगा। इसीलिए आगे के पूरे
ग्यारह श्लोकों में यह बताया है कि कर्म के प्रेरक भी दूसरे ही हैं
और कर्म रहता भी अन्य ही जगह है। यहाँ कर्मचोदना का अर्थ है कर्म के
प्रेरक और कर्मसंग्रह का अर्थ है जिनमें कर्म देखा जा सके-जिनके
देखने से ही कर्म का पता लग सके।
ज्ञानं
ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा
कर्मचोदना।
करणं
कर्मर् कत्तोति त्रिविधा: कर्मसंग्रह:॥18॥
ज्ञान,
ज्ञेय,
ज्ञाता
यही तीन कर्मों के प्रेरक हैं। (और) करण (इन्द्रियादि साधन) कर्म,
(जो
बने,
जहाँ कुछ हो),
कर्ता
इन्हीं तीन में कर्म का संग्रह होता है।18।
इस श्लोक में
ज्ञाता और कर्ता का एक ही अर्थ है। इन दोनों में केवल उपाधि या काम
करने के तरीके का फर्क है। जब किसी बात की जानकारी होती है तब वह
ज्ञाता या जानकार कहा जाता है। जब जानकारी के बाद काम करने लगता है
तो वही कर्ता कहा जाता है। अकेली बुध्दि एक चीज है और उसे बुध्दि ही
कहते हैं भी। उसका विवेचन आगे आयेगा। मगर जब वही आत्मा के संसर्ग के
फलस्वरूप उसके आभास,
उसके
प्रकाश से युक्त हो जाती है,
जैसी
कि आईने की चमक पड़ने पर दीवार उतनी दूर तक चमक उठती तथा ज्यादा
प्रकाशवाली बन जाती है जितनी दूर तक आईने की रोशनी का असर उस पर होता
है,
तो वही बुध्दि
ज्ञाता और कर्ता दोनों ही कही जाती है। इसीलिए ज्ञाता और कर्ता को एक
ही कहा है। अतएव आगे सात्तिवक आदि रूपों का विचार करने के समय कर्ता
का ही विचार करके सन्तोष करेंगे। क्योंकि कर्म की दृष्टि से ज्ञाता
तथा कर्ता दोनों का एक ही असर कर्म पर माना जाता है। चाहे ज्ञाता
सात्तिवक हो या कर्ता-और जब एक होगा तो दूसरा भी होईगा,
क्योंकि हैं तो दोनों एक ही-कर्म सात्तिवक ही होगा और उसकी
सात्तिवकता में कमी-बेशी न होगी,
चाहे
दोनों का नाम लें,
या एक
का। यहाँ कर्म का विचार और ही दृष्टि से हो रहा है। इसीलिए दोनों का
कहना जरूरी हो गया। जो जानता है वही करता भी है। जब तक हम यह न जान
लें कि हल कैसे चलाया जाता है तब तक उसे चलायेंगे कैसे
? जब
तक जान जायें नहीं कि कपड़ा कैसे बनता है,
उसे
बनायेंगे तब तक क्योंकर
?
इसी तरह ज्ञेय
और कर्म की भी बात है। पूर्वार्ध्द के तीन में जो ज्ञेय और
उत्तारार्ध्द के तीन में जो कर्म आया है ये दोनों भी एक ही हैं।
ज्ञेय का अर्थ ही है जिसका ज्ञान हो,
जिसके
बारे में ज्ञान हो। कर्म का अर्थ है जो किया या बनाया जाय,
जिस पर
या जहाँ हाथ-पाँव चलें। पूर्व के ही दृष्टान्त में हल या कपड़े को
लीजिए। पहले उनकी जानकारी होती है,
ज्ञान
होता है। पीछे उन्हीं पर हाथ-पाँव आदि चलते हैं। फर्क इतना ही है कि
हल पहले से ही मौजूद है और उसी पर क्रिया होती है। मगर कपड़ा मौजूद
नहीं है। किन्तु सूत वगैरह पर ही क्रिया शुरू करके उसे तैयार करते
हैं। वह क्रिया के ही सिलसिले में तैयार होता है। इसीलिए क्रिया का
विषय,
उसका आधार वह
भी बन जाता है। मगर कपड़ा बुनना शुरू करने के पहले उसकी जानकारी जरूरी
है। इसलिए इस श्लोक में जो दो त्रिपुटियाँ या त्रिक-तीन-तीन
(trinity)
हैं उन
दोनों के ज्ञेय और कर्म एक ही हैं। यह कर्म वही है जिसे पाणिनीय
सूत्र
ने 'कर्तारीप्सिततमं
कर्म' (पा.
1।4।49)
के रूप में बताया है। इन दोनों के सात्तिवक या
राजस, तामस होने,
न होने पर कर्म या क्रिया में कोई अन्तर नहीं
पड़ता है। इसीलिए इन दोनों का आगे विचार नहीं किया गया है। हाँ,
आगे जिस कर्म को तीन प्रकार का बताया है वह इस
श्लोक के अन्त के 'कर्म-संग्रह:'
वाला कर्म ही है,
जिसका विचार पहले से ही हो रहा है और जिसे काम,
क्रिया
(action)
कहते हैं।
वह जरूर सात्तिवक,
राजस, तामस होता है।
इन तीनों गुणों का उस पर असर जरूर होता है। इसीलिए उसका विचार आगे भी
जरूरी हो गया है।
अब इन दोनों
त्रिपुटियों में केवल ज्ञान और करण बच रहे। इनमें ज्ञान का आगे और भी
विचार किया गया है। ज्ञान कहिए,
जानकारी कहिए,
इहसास
(Knowledge)
कहिए सब
एक ही चीज है। इसके बिना कुछ होई नहीं सकता है। इस पर सत्तवादि गुणों
का असर भी होता है। साथ ही ज्ञान जैसा सात्तिवक,
राजस या तामस होगा कर्म भी वैसा ही होगा। वह कर्म
दरअसल किसमें है, किसमें नहीं इस निश्चय
पर भी उसका असर खामख्वाह होगा। इसीलिए ज्ञान की तीन किस्मों का
विवेचन इस कर्म-विवेचन के ही सिलसिले में आगे जरूरी हो गया है।
इस तरह करण
कहते हैं कर्म या क्रिया के साधन को। जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी चीरते
हैं और बसूले से भी। इसीलिए लकड़ी चीरने की क्रिया में,
कर्म
में कुल्हाड़ी और बसूला करण हो गये। इन्द्रियों की ही मदद से हम कोई
भी क्रिया कर सकते हैं। इसीलिए हाथ-पाँव आदि कर्म-इन्द्रियाँ भी कर्म
में करण बन गईं। मगर इस करण के सात्तिवक,
राजस,
तामस
होने पर भी कर्म के बारे में,
कि वह
दरअसल किसमें है,
किसमें
नहीं,
कोई असर नहीं
होगा। इसलिए आगे इस करण का और भी विचार जरूरी नहीं माना गया है।
बुध्दि और
धृति या धैर्य का भी असर कर्म पर पड़ता है। ये जिस तरह की हों कर्म भी
वैसे ही सात्तिवकादि बन जाते हैं। कम से कम उनके ऐसा होने में इन
दोनों का असर पड़ता ही है। इन्द्रियों की सी बात इनकी नहीं है कि
इन्द्रियाँ चाहे कैसी भी हों और उनके करते काम पूरा या अधूरा भले ही
रहे,
फिर भी
सात्तिवक राजस या तामस नहीं हो सकता है। ये दोनों तो कर्म पर उसके
सात्तिवकादि बनने में ही बहुत बड़ा असर डालती है। पीछे इस निश्चय में
भी कि वह वाकई आत्मा में है या नहीं,
इनका
काफी असर पड़ता है। बुध्दि का तो यह सब काम हुई,
यह सभी
जानते हैं। धृति का भी यही काम है। जिसमें धैर्य या हिम्मत न हो वही
दब्बू और डरपोक होने के कारणदबाव पड़ने पर अण्ट-सण्ट कर डालता है।
कमजोर ही तो दबाव पड़ने पर झूठा बयान देता है। हिम्मतवाला तो कभी ऐसा
करता नहीं। इसलिए इस प्रसंग में इन दोनों का विचार भी उचित ही है।
अब रह गया
अकेला सुख,
जिसका
त्रिविध विवेचन आगे आया है। वह उचित ही है। सुख के ही लिए तो सब कुछ
करते हैं। स्वर्ग,
धन,
पुत्रादि के ही लिए सारी क्रियाएँ की जाती हैं। लोगों की जो धारणा है
कि स्वयं ही-हमीं-भला-बुरा कर्म करते हैं वह है भी तो इसीलिए न,
कि
दूसरे के करने से दूसरे को सुख होगा कैसे
? यदि
इस सुख की फिक्र-चिन्ता छूट जाये तो मनुष्य की सारी विपदा और परेशानी
ही कट जाये। तब तो वह रास्ता पकड़ के पार ही हो जाये। बुरे कर्म तथा
दु:ख तो सुख की फिक्र के ही करते आ जाते हैं। सुख की लालसा के मारे
हम इतने परेशान और बेहाल रहते हैं कि बुरे-भले की तमीज उस हाय-हाय
में रही नहीं जाती। फलत: बुरे से भी बुरे सुख के ही लिए कर बैठते
हैं।
सुख के विवेचन
में भी जो सबसे पहले सात्तिवक सुख ही बताया है उससे स्पष्ट हो जाता
है कि असली सुख केवल बुध्दि की सात्तिवकता और निर्मलता से ही मिलता
है,
न कि कर्मों
से । कर्मों से मानना भारी भूल है। वह सुख तो भीतर ही है,
आत्मा
में ही है,
मौजूद
ही है। केवल निर्मल बुध्दि चाहिए जो उसे देख सके,
जान
सके। उसे कहीं बाहर से लाना थोड़े ही है। इस तरह कर्मों को आत्मा में
मानने की जरूरत रही नहीं जाती है। जिस तरह इन्हीं कर्मों के सिलसिले
में पहले त्रिविध त्यागों का वर्णन आया है वैसे ही यह भी वर्णन है,
न कि
नये सिरे त्रिगुणात्मक सृष्टि का कोई खास वर्णन है। पहले ही कही गयी
बातों का कर्म के सम्बन्ध में यहाँ केवल उपयोग कर लिया गया है।
इसीलिए ये 'न
तदस्ति पृथिव्यां वा'
(18।40)
में एक
ही बार कह दिया है कि सभी भौतिक पदार्थ तो त्रिगुणात्मक ही हैं।
इसीलिए यह कोई नयी बात नहीं है।
इस तरह कई
प्रकार से कर्मों का असम्बन्ध आत्मा के साथ सिध्द कर चुकने पर आगे के
श्लोक प्रकारान्तर से यही बात बताते हैं। इनका आशय केवल इतना ही है
कि यदि ज्ञान,
कर्म,
कर्ता,
बुध्दि
और धृति सात्त्विक हों और सात्तिवक सुख की असलियत भी हम जान जायें,
तो फिर
वह नौबत आये ही नहीं जिससे इन कर्मों को जबर्दस्ती आत्मा पर थोपें।
आत्मा में इनके दरअसल न रहने और उससे हजार कोस दूर रहने पर भी जो
इनकी कल्पना और थोपा-थोपी आत्मा में हो जाती है उसकी असली वजह यही है
कि हमारे ज्ञान,
कर्म
आदि सात्तिवक न हो के राजस या तामस ही होते हैं। यदि यह बात न रहे,
यदि
सबके सब ठीक हो जायें,
सात्तिवक ही हो जायें और हम सात्तिवक सुख को बखूबी समझ के उसी की
प्राप्ति में लग जायें,
तो
सारी आफतें मिट जायें। यह सही है कि सबों के ठीक होने पर भी यदि
हमारी लगन सात्तिवक सुख में न रहे,
तो सब
किया-कराया चौपट ही समझिए। इसीलिए वह सबसे जरूरी है। अन्त में वह आया
भी है इसलिए। आगे के
22
श्लोकों का सारांश यही है।
ज्ञानं
कर्म च
कर्ता
च त्रिधौव गुणभेदत:।
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि॥19॥
(तीनों)
गुणों के भिन्न-भिन्न होने से ज्ञान,
कर्म
और कर्ता भी सांख्यशास्त्र में तीन प्रकार के कहे गए हैं। उन्हें भी
ठीक-ठीक सुन लो।19।
सर्वभूतेषुऐनैकंभावमव्ययमीक्षते।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विध्दि सात्तिवकम्॥20॥
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान्।
वेत्ति
सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विध्दि राजसम्॥21॥
यत्तु
कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्।
अतत्तवार्थवदल्पं च तत्तमसमुदाहृतम्॥22॥
जिस ज्ञान के
फलस्वरूप सभी जुदे-जुदे पदार्थों में सर्वत्र एकरस,
व्याप्त और अविनाशी वस्तु ही देखते हैं वही ज्ञान सात्तिवक समझो। सभी
पदार्थों में भिन्न-भिन्न अनेक वस्तुओं की जो जुदी-जुदी जानकारी है
वही ज्ञान राजस जानो। जो ज्ञान कुछ भौतिक पदार्थों तक ही सीमित,
उन्हीं
को सब कुछ मानने वाला,
बेबुनियाद मिथ्या और तुच्छ है वही तामस कहा जाता है।20।21।22।
नियतंसंगरहितमरागद्वेषत:कृतम्।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्तिवकमुच्यते॥23॥
यत्तु
कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुन:।
क्रियते
बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्॥24॥
अनुबन्धां क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्।
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते॥25॥
फलेच्छा न
रखने वाले के द्वारा जो कर्म निश्चित रूप से आसक्ति से शून्य हो के
बिना रागद्वेष के ही किया जाय वही सात्तिवक कहा जाता है। जो कर्म
फलेच्छापूर्वक अहंकार या आग्रह के साथ किया जाए और जिसमें बहुत
परेशानी हो वही राजस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम,
बीच के
नफा-नुकसान,
हिंसा
और अपनी शक्ति का ख्याल न करके भूल से ही किया जाय वही तामस कहा
जाता है। 23।24।25।
यहाँ
साहंकारेण शब्द का अर्थ है कर्म में हठ या आसक्ति। क्योंकि फल की
इच्छा और कर्म की आसक्ति ये दो चीजें हैं जिन्हें पहले बखूबी समझाया
जा चुका है। पहले श्लोक में दोनों का त्याग कहा गया है इसीलिए इसमें
दोनों का आना जरूरी है। मगर
'कामेप्सुना'
शब्द
तो फलेच्छा को ही कहता है। इसीलिए
'साहंकारेण'
का ऐसा
अर्थ हमने किया है। ठीक भी है यही। जब जिद्द होती है तभी तो
'मैं
जरूर ही कर डालूँगा'
यह
ख्याल होता है। इसी प्रकार क्षय शब्द का भी अर्थ हमने चलती भाषा में
'नफा-नुकसान'
किया
है,
जिसे घाटा या
टोटा भी कहते हैं। मगर यह अन्तिम घाटा नहीं है। क्योंकि उसके लिए तो
अनुबन्ध शब्द आया ही है। इसीलिए दरम्यानी टोटा ही अर्थ ठीक है।
मुक्तसंगोऽनहंवादीधात्युत्साहसमन्वित:।
सिध्दयसिध्दयोर्निर्विकार:
कर्ता
सात्तिवक उच्यते॥26॥
रागी
कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचि:।
हर्षशोकान्वित
कर्ता
राजस: परिकीर्तित:॥27॥
अयुक्त:
प्राकृत स्तब्ध: शठो नैष्कृतिकोऽलस:।
विषादी
दीर्घसूत्री
च
कर्ता
तामस उच्यते॥28॥
जो आसक्ति से
शून्य हो,
जो बहुत बहके
न,
जो धैर्य और
उत्साहवाला हो (तथा) कर्म के पूर्ण होने,
न होने
में जो बेफिक्र हो वही कर्ता सात्तिवक कहा जाता है। रागयुक्त,
फलेच्छुक,
लोभी,
हिंसा
में लगा हुआ,
नापाक
और (कर्म के पूरे होने,
न होने
में) हर्ष और शोकाकुल कर्ता राजस है। बुध्दि को ठिकाने न रखने वाला,
गँवार,
अकड़ा
हुआ,
ठग,
दूसरे
की हानि करने वाला,
आलसी,
रोने-धोने वाला और असावधन कर्ता तामस कहा जाता है।
26।27।28।
बुध्देर्भेदं
धातेश्चैव
गुणतस्त्रिविधां शृणु।
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन
धनंजय॥29॥
हे धनंजय,
गुणों
के भेद से बुध्दि और धृति के भी जो तीन प्रकार हैं उन्हें भी
पूरा-पूरा अलग-अलग कहे देता हूँ,
सुन
लो। 29।
प्रवृत्तिं
च निवृत्तिं
च कार्याकार्ये भयाभये
बन्धां
मोक्षं च या
वेत्ति
बुध्दि: सा पार्थ सात्त्विको॥30॥
यया
धर्ममधार्मंचकार्यंचाकार्यमेव
च।
अयथावत्प्रजानाति बुध्दि: सा पार्थ राजसी॥31॥
अधार्मं
धर्ममिति
या मन्यते तमसावृता।
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुध्दि: सा पार्थ तामसी॥32॥
हे पार्थ,
जो
बुध्दिर् कर्तव्य-अकर्तव्य,
हो
सकने,
न हो सकने
वाली चीज,
डर-निडरता,
बन्धन
और मोक्ष (इन सबों) को (बखूबी) जानती है वही सात्तिवक है। जिसे
बुध्दि से धर्म-अधर्म तथा कार्य-अकार्य को ठीक-ठीक न जान सकें वही
राजस है। हे पार्थ,
तम से
घिरी जो बुध्दि अधर्म को धर्म और सभी बातों को उलटे ही जाने वही
तामसी है।30।31।32।
यहाँ पहले
श्लोक में जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है उसी के अर्थ में शेष दो
श्लोकों में धर्म-अधर्म शब्द आये हैं। इसीलिए हमने
प्रवृत्ति-निवृत्ति का अर्थर् कर्तव्य-अकर्तव्य किया है।
धर्म-अधर्म का भी वही अर्थ है। कार्य-अकार्य के मानी यह हैं कि पहले
से ही अच्छी तरह देख लेना कि यह काम हमसे हो सकता है,
साध्य
है या नहीं।र् कर्तव्य-अकर्तव्य के निश्चय के बाद भी
साध्य-असाध्य का निश्चय जरूरी हो जाता है। क्योंकि जोर् कर्तव्य
हो वह जरूर ही साध्य हो यह बात नहीं है। इसीलिए असाध्य काम में
भीर् कर्तव्यता के निश्चय के बाद बिना सोचे-बूझे पड़ जाना ठीक नहीं
है,
नादानी है।
बन्धा और मोक्ष तो प्रवृत्ति-निवृत्ति की कसौटी के रूप में ही लिखे
गये हैं। जिसका चरम परिणाम बन्धन और जन्म-मरण हो वही अकर्तव्य और
जिसका मोक्ष हो वहीर् कर्तव्य माना जाना चाहिए। अतएव
31वें
श्लोक में न लिखे जाने पर भी इसे समझ लेना ही होगा। यही वजह है कि
32वें
मेंर् कर्तव्य-अकर्तव्य को कह के एक ही साथ बाकियों के बारे में कह
दिया है कि जो सभी बातें उलटे ही समझे। सभी बातों में बन्धा-मोक्ष,
कार्य-अकार्य भी आ गये।
इन तीनों
श्लोकों का सारांश यही है कि सात्तिवक बुध्दि सभी बातें ठीक-ठीक
समझती है। वह मनुष्य का ठीक पथदर्शन करती है। मगर राजस बुध्दि में
किसी भी बात का ठीक-ठीक निश्चय हो पाता नहीं। न तो यथार्थ निश्चय और
न उलटा। हर बात में पसोपेश,
दुविधा
और घपला पाया जाता है,
जिससे
कर्ता किर्कत्ताव्यविमूढ़ हो जाता है। ऐन मौके पर उसका उचित
पथप्रदर्शन नहीं हो पाता। दोनों के विपरीत तामस बुध्दि हर बात में
उलटा ही निश्चय करती-कराती है और गलत रास्ते पर ही बराबर ले जाती है।
इसमें न तो दुविधा होती है और न कभी यथार्थ निश्चय हो पाता है।
धात्या
यया धारयते
मन: प्राणेन्द्रियक्रिया:।
योगेनाव्यभिचारिण्या
धाति:
सा पार्थ सात्तिवकी॥33॥
यया तु
धर्मकामार्थान्धात्या
धारयतेऽर्जुन।
प्रसंगेन फलाकांक्षी
धाति:
सा पार्थ राजसी॥34॥
यया
स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च।
न
विमुंचति दुर्मेधा
धाति:
सा पार्थ तामसी॥35॥
हे पार्थ,
योग से
जिसका सम्बन्ध कभी टूटने वाला न हो ऐसी जिस धृति-विशेष प्रकार के
यत्न-के बल से मन,
प्राण
और इन्द्रियों की क्रियाओं को काबू में रखते हैं वही सात्तिवकी धृति
है। हे अर्जुन,
हे
पार्थ,
जिस धृति के
बल से कर्म में आसक्त (एवं) फलेच्छुक (पुरुष)
(केवल)
धर्म,
काम और अर्थ
की ही बातें करता है वही राजसी है। जिस धृति के बल से आलस्य,
डर,
शोक,
घबराहट,
मद (इन
सबों) को भ्रष्ट बुध्दिवाला (मनुष्य) छोड़ नहीं सकता वही तामसी मानी
जाती है।33।34।35।
कहीं-कहीं
'पार्थ
तामसी'
की जगह
'तामसी
मता'
पाठ है। शंकर
ने यही पाठ माना है। हमने सम्मिलित अर्थ कर दिया है। क्योंकि
'मता'
शब्द न
देने पर भी उसका अर्थ तो यहाँ हुई। उसके बिना तो काम चलता नहीं। यहाँ
पहले श्लोक में जो योग है उसका अर्थ कर्मों में आसक्ति एवं फलेच्छा
का न होना यह पहले ही कह चुके हैं। इसका मूलाधार आत्मदर्शन बता चुके
हैं। सात्त्विक धृति का आधार यही बातें हैं। इन्हीं के बल से मन,
प्राण
और इन्द्रियों को डँटा देते और जरा भी डिगने नहीं देते,
चाहे
हजार बलायें आयें। ऐसी ही धृतिवाले मोक्ष तक को ध्यान में रखके ही
कोई काम हिम्मत के साथ करते हैं। मगर राजसी धृति वाले मोक्ष को छोड़
के भटक जाते हैं। वे कर्मों में आसक्त एवं फलेच्छा के गुलाम बन जाते
हैं। जहाँ सात्तिचक धृतिवाले धर्म,
अर्थ,
काम,
मोक्ष
चारों की परवाह रख के ही कुछ भी करते हैं,
तहाँ
राजस धृतिवाले मोक्ष को भूल जाते और पूरे चतुर सांसारिक बन के धर्म,
अर्थ,
काम
तीन की ही परवाह रखते हैं। यही बात दूसरे श्लोक में कही गयी है। काम
का अर्थ है वही आसक्ति और इच्छा। छोटी सी बातों से लेकर स्वर्ग तक की
कामना को ही काम कहते हैं। अर्थ कहते हैं धन को,
सम्पत्ति को। सम्पत्ति के भीतर सभी पदार्थ आ गये। उनके धर्म,
अर्थ
और काम का परस्पर सम्बन्ध है- तीनों एक-दूसरे से मिले रहते हैं। फलत:
यदि एक भी हट जाये तो तीनों गड़बड़ी में पड़ जायें। यह भी खास बात है कि
उनके धर्म और अर्थ को एक साथ जोड़ने की बात यह काम ही करता है। किन्तु
सात्तिवक धृत्ति में यह बात नहीं है। उसमें तो काम आसक्ति के रूप में
प्रबल न हो के मामूली इच्छा के ही रूप में नजर आता है। जिससे हरेक
क्रिया में प्रगति मिलती है।
अब रही तामसी
धृति की बात। ऐसी धृति को धृति कहना उसका निरादर ही माना जाना चाहिए।
फिर भी हरेक पदार्थ त्रिगुणात्मक ही हैं। इसलिए लाचारी है। असल में
तामसी धृतिवालों के मन,
प्राण
और इन्द्रियों पर अपना काबू नहीं रहने से उनकी क्रियाएँ मनमानी
चलती-बिगड़ती रहती हैं। ऐसे लोगों में हिम्मत तो होती ही नहीं। इसीलिए
डर,
अफसोस,
मनहूसी
में पड़े रहते हैं। एक तरह का नशा भी उन पर हर घड़ी चढ़ा रहता है। आलस्य
का तो पूछिए मत। इसीलिए नींद का अर्थ हमने आलस्य किया है। स्वप्न का
अर्थ गाढ़ी नींद तो सम्भव नहीं। जग के उठ बैठने को उनका जी नहीं
चाहता। इसीलिए ऐसे लोग कुछ भी कर पाते नहीं।
सुखं
त्विदानीं त्रिविधां शृणु मे भरतर्षभ।
अभ्यासाद्रमते यत्रा दु:खान्तं च निगच्छति॥36॥
हे भरतश्रेष्ठ,
अब तीन
प्रकार के सुखों को भी मुझसे सुन लो,
(उन्हीं
सुखों को),
जिनके
बार-बार के मिलने से उनमें मन रम जाता है और दु:ख भूल जाते हैं।36।
जिस ढंग से इस
श्लोक में शब्द दिये गये हैं उनसे भी यही स्पष्ट हो जाता है कि सभी
कामों का आखिरी ध्येय यह सुख ही है। इसीलिए कहते हैं कि अब आखिर में
उसे भी जरा सुन लो। नहीं तो बात अधूरी ही रह जायगी। इसके बाद
उत्तारार्ध्द में उसी सुख का सर्वसामान्य या साधारण रूप कह दिया है।
इसमें दो बातें कही गयी हैं। एक यह कि सुख वही है कि जिसके अभ्यास या
देर तक के या बार-बार के अनुभव से ही उसमें मन रमता है। वह बिजली की
चमक,
नीलकण्ठ का
दर्शन या तीर्थ के जल का स्पर्श नहीं है कि जरा से अनुभव या संसर्ग
से ही काम चल जाता है। ऐसा होने से तो सुख के बजाय दु:ख ही होता है।
जबान पर हलवा रख के फौरन उठा लें तो सुख तो कुछ होगा नहीं,
झल्लाहट और तकलीफ भले ही होगी। ऐसा भी होता है कि बहुत सी चीजों के
प्रथम संसर्ग से कुछ मजा या सुख नहीं मिलता। किन्तु निरन्तर के अनुभव
और संसर्ग से ही,
प्रयोग
और इस्तेमाल से ही उनमें मजा आने लगता है। जो लोग असभ्य हैं,
जंगली
हैं उन्हें सभ्यता की चीजों का चस्का लगाना होता है। पहले तो वे उलटे
झल्लाते हैं। मगर धीरे-धीरे उनकी आवृत्ति और अभ्यास होते-होते मन
उनमें रम जाता है। क्योंकि मन के बिना रमे तो मजा आता ही नहीं। यही
वजह है कि सुख निरन्तर बना रहे,
वह कम
से कम बार-बार मिलता रहे,
सो भी
अल्प से अल्प विलम्ब के बाद ही,
इसी
ख्याल से लोग उसी की हाय-धुन में लगे रहते और बुरा-भला सब कुछ कर
डालते हैं। कर्म को आत्मा में घुसेड़ने का यह एक बहुत बड़ा कारण है।
दूसरी बात है
दु:ख के खात्मे को पा जाना,
जिसे
हमने दु:ख का भूल जाना लिखा है। सुख की इच्छा अधिकांश में कष्टों से
ऊब के ही तो होती है। लोग आराम चाहते ही हैं इसीलिए कि वेदना और पीड़ा
से पिण्ड छूटे। इसीलिए तकलीफ कम होते ही कहने लगते हैं कि आराम हो
रहा है। बीमार लोगों के बारे में प्राय: ऐसा कहा जाता है। इसीलिए
हितोपदेश में इसी रोग की कमी के दृष्टान्त को ही ले के यहाँ तक कह
दिया है कि दुनिया में सुख तो हुई नहीं,
केवल
दु:ख ही है। इसी से बीमार की तकलीफ कम होने पर उसे ही सुख कह देते
हैं, ''दु:खमेवास्ति
न सुखं यस्मात्तादुपलक्ष्यते। दु:र्खात्तास्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा
विधीयते''।
मगर हमें इतने गहरे पानी में यहाँ उतरना है नहीं और न इसकी जरूरत ही
है। गीता का यह सिध्दान्त है भी नहीं। वह तो स्वतन्त्र आत्मानन्द को
मानती है। यह यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि सुख मिलते ही या तो
दु:ख खत्म हो जाता है,
वह रही
नहीं जाता,
या कम
से कम वह भूल तो जरूर जाता है,
जब तक
सुख का अनुभव रहे। इसलिए भी सुखकर अभ्यास चाहते हैं। क्योंकि जब तक
ऐसा रहेगा दु:ख भूला रहेगा। दु:ख के भूल जाने में दोनों बातें आ जाती
हैं,
दु:ख के खत्म
हो जाना भी और खत्म न होने पर भी उसका अनुभव तत्काल न होना भी।
इसीलिए हमने यही अर्थ किया है। यह दु:ख के भूलने की भी चाट ऐसी है कि
हमें सभी तरह के कर्मों को करने को विवश करती है। साथ ही,
आतुरतावश आत्मा को ही हम कर्मों का करने वाला तथा आधार मान लेते हैं।
अतएव सुख के बारे में कही गयी ये दोनों बातें बड़े काम की होने के साथ
ही प्रसंग के अनुकूल भी हैं।
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्।
तत्सुखं
सात्तिचकं प्रोक्तमात्मबुध्दिप्रसादजम्॥37॥
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्।
परिणामे
विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्॥38॥
यदग्रे
चानुबन्धो च सुखं मोहनमात्मन:।
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तमसमुदाहृतम्॥39॥
जो सुख अपने
आरम्भ के समय विष की तरह कड़वा और अन्त में अमृत की तरह लगे,
अपनी
ही बुध्दि को निर्मलता मात्र से ही पैदा होनेवाला वही सुख सात्तिवक
कहा गया है। विषयों के साथ इन्द्रियों के सम्बन्ध से होनेवाला जो सुख
शुरू में अमृत जैसा,
(लेकिन)
अन्त में विष की तरह काम करे,
वही
राजस माना गया है। ज्यादा नींद,
आलस्य
और असावधनी में मालूम होने वाला जो मजा शुरू से लेकर अन्त तक आत्मा
को मोह में डालने-भटकाने-वाला ही होता है वही तामस कहा जाता है।37।38।39।
यहाँ पहले
श्लोक में आत्मानन्द का ही वर्णन है। इसीलिए उसके वास्ते किसी और बात
की जरूरत नहीं बताई गयी है। केवल अपनी बुध्दि को ही निर्मल और स्वच्छ
करने की आवश्यकता कही गयी है। वह तो मौजूद ही है,
पास ही
है। सिर्फ बुध्दि को एकाग्र और समाधिस्थ करने की जरूरत है। बुध्दि का
अर्थ मन,
चित्त या
अन्त:करण है। ऐसा होते ही वह आनन्द आप ही आप मिलने लगता है। कहा भी
है कि ''दिल
के आईने में है तस्वीरे यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली''।
गर्दन झुकाने का मतलब मन की एकग्रता से ही है।
'आत्मबुध्दि
प्रसादजम्'
में जो
आत्म शब्द है वह इन्हीं बातों का सूचक है। यह मन की एकाग्रता और
समाधि बहुत ही कष्टसाध्य है। इसीलिए उस सुख को शुरू में जहर जैसा
कहा है। वह जहर जैसा है के मानी हैं कि उसके लिए जो कुछ करना होता है
वह बहुत ही कठिन है।
विषय सुख को
राजस कहा है। वह पहले तो बहुत ही अच्छा लगता है और मन को रमाता है।
मगर परिणाम उसका बुरा होता है। क्योंकि बाल-बच्चों और सांसारिक
पदार्थों में ही जिसे चस्का हो गया वह परलोक और कल्याण् की बात कुछ
भी करी नहीं सकता। उससे समाजहित का भी कोई काम नहीं हो सकता है।
मनोरथों की न कभीर पूर्ति होती है और न इनसे और इनके करते होने वाले
झंझटों से छुटकारा ही मिलता है। फिर और बात हो तो कैसे
?
इसीलिए सौभरि ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उनने समाधि को त्यागकर
पूरे पचास विवाह किये! फिर महल बना के सांसारिक सुख का भोग शुरू
किया! बच्चे,
पोते,
परपाते
आदि हो गये,
भारी
परिवार बढ़ गया और
'गीता
फैल गयी'!
अन्त में ऊब
के उनने सबको लात मारी और कहा कि लाखों वर्षों में भी मनोरथों की,
पूर्ति हो नहीं सकती,
आदि-आदि-''मनोरथानां
न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि तथाब्दलक्षै:। पूर्णेषु पूर्वेषु
पुनर्नवानामुत्पत्ताय: संति मनोरथानाम्। पद्भयां गता यौवनिनश्च याता
दारैश्च संयोगमिता: प्रसूता:। दृष्ट्वा सुतं तत्तानयप्रसू¯त
दुरष्टुं पुनर्वा×छति
मेऽन्तरात्मा। आमृत्युतो नैव मनोरथानामन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं
मयाऽद्य। मनोरथासक्तिपरस्य चित्तो न जायते वै परमात्मसंग:''।
यही आशय इस श्लोक का है; न कि
वेश्यागामियों या दूसरे कुकर्मियों से यहाँ मतलब है। उनका वर्णन तो
तामस सुख में ही आया है। क्योंकि उस सुख का काम ही है आत्मा को
भटकाना। प्रमाद से ही वह पैदा भी होता है। कुकर्म तो प्रमाद और भटकना
ही है न ? दिन-रात पड़े-पड़े ऊँघते रहें और
आलस में दिन गुजारें यही तो तामसी वृत्ति
है। ऐसे लोगों को इसी में मजा भी मिलता है। यहाँ निद्रा का अर्थ है
ज्यादा निद्रा। क्योंकि साधारण
नींद में तो सभी को मजा मिलता है। गाढ़ी नींद के बाद हरेक आदमी कहता
भी है कि खूब आरम से सोये,
ऐसा सोये कि कुछ मालूम ही न पड़ा-'सुखमहमस्वाप्सन्न
किंचिदवेदिषम्'।
इस प्रकार
त्रिगुण रूप में सुख आदि का वर्णन कर दिया। इसका प्रयोजन हम पहले ही
कह चुके हैं। शायद कोई कहे कि केवल सात्तिवक कर्म,
ज्ञान,
कर्ता
आदि के ही वर्णन से काम चल सकता था और लोग सहज हो के आत्मा को कर्म
से अलग मान सकते थे। फिर राजस,
तामसों के वर्णन की क्या जरूरत थी
?
बात तो सही
है। मगर जब सात्तिवक का नाम लेंगे तो खामख्वाह फौरन आकांक्षा होगी कि
राजस,
तामस क्या
हैं। जरा उन्हें भी तो जानें। और अगर यह इच्छा पूरी न हो तो निरूपण
बेकार जायगा। बातें भी अच्छी तरह समझ में आ न सकेंगी। मन दुविधो में
जो पड़ गया और समझना ठहरा उसे ही। एक बात और भी है। यदि राजस,
तामस
का पूरा ब्योरा और वर्णन न हो तो लोक चूक सकते हैं। वे दरअसल राजस या
तामस को ही भूल से सात्तिवक मान बैठ सकते हैं। इसीलिए साफ-साफ तीनों
को एक ही साथ रख दिया है;
ताकि
आईने की तरह देख लें और धोखे से बचें।
इस प्रकार सब
कुछ कह चुकने के बाद इसका उपसंहार करते हुए,
जैसा
कि कहा है,
अगला
श्लोक बताये देता है कि यह तो आश्चर्य की कोई बात है नहीं।
जमीन-आसमान कहीं भी जो चीज होगी उसमें तीनों गुण होंगे ही। इसीलिए
केवल सजग होने की जरूरत है। नहीं तो इनके सिवाय औरों से भी धोखा हो
सकता है।
न
तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन:।
सत्तवं
प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभि: स्यात्त्रिभिर्गुणै:॥40॥
भूमण्डल में
या आकाश और स्वर्ग के निवासी देवताओं तक में भी ऐसा एक भी पदार्थ
नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो।
40।
पृथिवी के
किसी पदार्थ का नाम न लेकर स्वर्ग के देवताओं का नाम लेने का प्रयोजन
इतना ही है कि पार्थिव पदार्थों को तो सभी लोग त्रिगुणात्मक
मानते-जानते हैं। अन्य स्वर्गीय पदार्थों को भी ऐसा शायद समझ सकते
हैं। स्वर्ग में देवताओं के अलावे और भी पदार्थ यक्षादि होते ही हैं।
साथ ही,
दिव तो आकाश
को भी कहते हैं और उसमें प्रेतादि भी रहते ही हैं। वे भी
त्रिगुणात्मक हो सकते हैं। किन्तु देवताओं को दिव्य या अलौकिक ख्याल
करके कोई शायद त्रिगुण न माने,
इसीलिए
उनको खास तौर से कह दिया। वजह भी दे दिया कि सभी तो प्रकृति से ही
बने हैं। इसीलिए किसी पर भी भरोसा न करके अपनी बुध्दि की निर्मलता का
ही सहारा लेना होगा।
इसी तरह सत्तव
का अर्थ पदार्थ है,
न कि
सत्तव गुणमात्र। यह ठीक है कि सत्तवगुण कहीं भी विशुध्द नहीं है।
उसमें भी रज और तम का मेल कभी कम,
कभी
ज्यादा रहता ही है। इसी से सत्तव का अर्थ पदार्थ हो भी गया। क्योंकि
किसी में कम और किसी में अधिक सत्तव तो रहता यही है। आशय यही है कि
खबरदार,
विशुध्द सत्तव
कहीं नहीं है। इसलिए सतर्क रहना ही होगा। नहीं तो बुध्दि की पूरी
सफाई के बाद भी उस पर रज,
तम का
धावा हो सकता है।
अब प्रश्न
पैदा होता है कि इसका उपाय क्या है कि सात्तिवक कर्म,
ज्ञान,
बुध्दि,
सुख
आदि ही रहें और राजस,
तामस,
रहने न
पायें-लोग इन दोनों के फेर में न पड़ के सात्तिवक के ही पीछे लगे रहें
?
बिना उपाय
जाने काम चलेगा भी कैसे
?
साथ ही,
जो
उपाय हो भी वह किस तरह काम में लाया जाय,
जिसमें
कभी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे,
यह भी
प्रश्न होना स्वाभाविक है। इसीलिए आगे के श्लोकों में इन्हीं दोनों
का उत्तर देते हुए समूचा अध्याय पूरा करके गीता का भी उपसंहार कर
दिया गया है। इसमें भी पहले के चार (41-44)
श्लोकों में उपायों को बता के शेष श्लोकों में उन्हीं का प्रयोग
बताया गया है। यह ठीक ही है कि दवा का प्रयोग निरन्तर तो होता है
नहीं। बीच-बीच में विराम तो करते ही हैं। कभी-कभी तो लम्बी मुद्दत तक
दवा छोड़ के देखते हैं कि मर्ज गया या नहीं। उस समय दवा का छोड़ देना
ही दवा का काम करता है। नहीं तो आवश्यकता से अधिक दवा का प्रयोग कर
देने का खतरा आ सकता है। ठीक यही बात कर्मों की है। वर्णों के कर्म
तो उपाय के रूप में ही कहे गये हैं। मगर उन्हें छोड़ देने की भी जरूरत
दवा की ही तरह हो जाती है। नहीं तो इनका जरूरत से ज्यादा प्रयोग हो
जाने से ही हानि हो सकती और काम बिगड़ सकता है। इस प्रकार कर्मों के
स्वरूपत: त्याग की भी बात इसी सिलसिले में आ जाती है,
आ गयी
है और वह उचित ही है। जलचिकित्साशास्त्र का तो यह एक नियम ही है कि
बीच-बीच में जरूर हो जलचिकित्सा बन्द कर दी जानी चाहिए। नहीं तो वह
मनुष्य का एक तरह का स्वभाव बन जाती है। फिर तो उसका कुछ भी असर नहीं
होता है।
हाँ,
तो आगे
के चार श्लोकों में जो वर्णों के धर्म कहे गये हैं वह त्रिगुणों से
बने विभिन्न स्वभावों के अनुसार ही माने गये हैं। बार-बार उन श्लोकों
में यह बात कही गयी है। यहाँ तक कि हरेक वर्ण के बारे में अलग-अलग
उसका जिक्र किया है। पहले श्लोक में चारों के बारे में एक साथ भी कह
दिया है कि ये कर्म स्वाभाविक होते हैं,
प्रकृति के अनुसार ही होते हैं। हमने इस बात पर बहुत ज्यादा प्रकाश
पहले ही डाल दिया है। इस प्रसंग में इनके कहे जाने का आशय यही है कि
यदि गुण-तारतम्य के अनुसार बनी हुई मानव प्रकृति की जाँच करके उसी के
अनुसार उसके कर्म निर्धारित किये जायें,
तो
राजस-तामस का झमेला खड़ा होगा ही नहीं। क्योंकि सात्तिवक प्रकृतिवाले
तो उनसे यों ही बच जायेंगे। उन्हें दूसरे कर्म मिलेंगे ही नहीं।
इसीलिए राजस-तामस सुखों का भी मौका ही उन्हें न लगेगा। उनकी बुध्दि
और धृति भी वैसी ही होगी। यदि कुछ कसर भी रहेगी तो ये कर्म ही उसे
ठीक कर देंगे।
रह गये राजस
तथा तामस प्रकृति वाले। जब इन्हें भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करने
की विवशता होगी तो वे उसमें विशेषज्ञ और पारंगत हो जायँगे। नतीजा यह
होगा कि उनकी हकीकत और असलियत समझने लगेंगे। फिर तो धीरे-धीरे अपने
भीतर ऐसी भावना और ऐसे संस्कार पैदा करेंगे कि स्वयमेव उनकी प्रकृति
बदलेगी। फलत: इस जन्म में नहीं,
तो आगे
सात्तिवक मार्ग पर आयी जायँगे। विशेषज्ञता का तो मतलब ही है उसका
रस-रेशा पहचान लेना। उसका सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि उस पर अमल
अच्छी तरह किया जाय। किन्तु उसकी कमजोरियाँ,
बुराइयाँ और हानियाँ भी मालूम हो जाया करती हैं,
ऑंखों
के सामने नाचने लगती हैं और यही चीज आगे का रास्ता साफ करती है।
वर्णाश्रमों के धर्मों की इस तरह सख्ती के साथ पाबन्दी की जो बात
पहले जमाने में थी उसका यही मतलब था। हम यह पहले ही अच्छी तरह सिध्द
कर चुके हैं। आज जो श्रम-विभाजन
(division of labour)
का
सिध्दान्त बहुत व्यापक रूप में काम में लाया जाकर पराकाष्ठा को
पहुँचा दिया गया है,
वह कोई नयी बात नहीं है। वर्णाश्रम
धर्मों
के विभाग के मूल में यही सिध्दान्त काम करता है। इससे ही समाज की
प्रगति पहले के ऋषि-मुनि मानते थे। आश्चर्य है कि आधुनिक
विज्ञान भी यही बात रूपान्तर में मानता है। डॉ. ऐडम स्मिथ ने
अठारहवीं सदी के उत्तारार्ध्द में जो एक महत्तवपूर्ण पुस्तक राजनीतिक
अर्थशास्त्र
के बारे में लिखी है और जिसका नाम है
'राष्ट्रों
की सम्पत्ति'
(The wealth of Nations by Dr.
Adam Smith),
उसके शुरू
में,
पहले ही परिच्छेद में,
वह यही बात यों लिखते हैं-
“In the progress of
society philosophy or speculation becomes, like every other
employment, the principal or sole trade and occupation of a
particular class of citizens. Like every other employment, too it
is subdivided in to a great number of different branches each of
which affords occupation to a peculiar tribe of class of
philosophers; and this subdivision or employment in philosophy as
well as in every other business, improves dexterity, and saves
time. Each individual becomes more expert in his own peculiar
branch, more work is done upon the whole, and the quantity of
science is considrably increased by it.”
इसका आशय यह
है, ''समाज
की प्रगति के सिलसिले में हरेक दूसरे कामों की ही तरह दर्शन या
मनन-चिन्तन भी नागरिकों के एक खास वर्ग का मुख्य या सोलहों आना काम
और पेशा बन जाता है। फिर दूसरे कामों की ही तरह यह भी अनेक विलक्षण
विभागों में बँट जाता है और हरेक विभाग एक विलक्षण वर्ग या जाति के
दार्शनिकों और दिमागदारों के लिए काम दे देता है। दर्शन और चिन्तन का
यह विभाग हरेक दूसरे पेशों के विभाग की ही तरह कुशलता एवं विशेषज्ञता
की प्रगति करता है और समय भी बचाता है। इस तरह हरेक व्यक्ति अपने खास
विभाग या उसकी शाखा में अधिक कुशल हो जाता है,
सब
मिला के इस तरह काम भी ज्यादा होता है और विज्ञान के प्रसार में
प्रगति ज्यादा हो जाती है।''
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप।
कर्माणि
प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै:॥41॥
हे परन्तप,
स्वभाव
को बनाने वाले तीनों गुणों के (तारतम्य के) फलस्वरूप ब्राह्मणों,
क्षत्रियों,
वैश्यों तथा शूद्रों के कर्म बिलकुल ही बँटे हुए हैं।
41।
शमो
दमस्तप: शौचं क्षांतिरार्जवमेव च।
ज्ञानं
विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्॥42॥
शम,
दम,
तप,
पवित्रता,
क्षमा,
नम्रता
या सिधाई,
ज्ञान,
विज्ञान और आस्तिकता,
(ये)
ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं।42।
आस्तिकता का
अर्थ श्रध्दा है।
शौर्यं
तेजो
धातिर्दाक्ष्यं
युध्दे चाप्यपलायनम्।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रां कर्म स्वभावजम्॥43॥
शूरता,
दब्बूपन का न होना,
धैर्य
(युध्द शासनादि में) कुशलता,
युध्द
से न भागना,
दान और
शासन की योग्यता,
(ये)
क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं।43।
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्॥44॥
खेती,
पशुपालन (और) व्यापार (ये) वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। शूद्रों
का भी स्वाभाविक कर्म सेवा-रूप ही है।44।
यहाँ
ब्राह्मणों और क्षत्रियों के स्वतन्त्र रूप में विस्तृत कर्मों का
जुदा-जुदा वर्णन और शूद्रों तथा वैश्यों के कर्मों का एक ही श्लोक
में संक्षेप में ही वर्णन यह सूचित करता है कि उस समय वैश्य और शूद्र
का दर्जा प्राय: समकक्ष,
परतन्त्रा और छोटा माने जाने लगा था। मगर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय
प्राय: समकक्ष होने के साथ ही ऊँचे एवं स्वतन्त्र माने जाते थे।
शूद्र के काम का तो खास नाम भी नहीं दिया है किन्तु
'सेवा-रूप'
कह
दिया है। इससे ख्याल होता है कि जरूरत होने पर उससे हर तरह का काम
करवा के उस काम को सेवा का रूप दे दिया जाता था। इससे यह भी स्पष्ट
है कि समाज के लिए वह फिर भी बहुत ही उपयोगी और जरूरी था। आखिर सेवा
के बिना समाज टिकेगा भी कैसे
?
हमने इस पर
पूरा प्रकाश पहले ही डाला है। इस श्लोक में
'शूद्रस्यापि'
में
शूद्र के साथ 'भी'
के
अर्थ में 'अपि'
आया
है। उससे यह भी साफ झलकता है कि उस समय सेवा धर्म शेष तीन वर्णों का
भी था और आज उसे जितना बुरा मानते हैं,
पहले
यह बात न थी। इसी के साथ यह भी सिध्द हो जाता है कि शूद्रों का कोई
अपना खास पेशा या काम न था। जरूरत होने पर वह तीनों वर्णों का काम
करते रहते थे। हमने इस पहलू पर भी पहले ही ज्यादा प्रकाश डाला है।
शेष तीन के साथ 'अपि'
न दे
के केवल शूद्र के साथ ही देने का दूसरा आशय हो नहीं सकता। ऐसी दशा
में शूद्रों को छोटे या नीच मानने का एक ही कारण हो सकता है और वह यह
कि उनकी स्वतन्त्र हस्ती न थी,
जैसी
कि शेष तीन की थी। क्योंकि उनका कोई निजी पेशा न था। और जान पड़ता है,
उस समय
निजी पेशे का होना जरूरी एवं प्रतिष्ठा का चिद्द माना जाता था।
इसीलिए शूद्र छोटे समझे गये। वैश्यों के भी छोटे माने जाने की
प्रवृत्ति शायद इसीलिए हुई कि खेती,
व्यापार या पशुपालन की उस समय कोई खास जरूरत न थी। या तो इनके द्वारा
होने वाला समाज का काम आसानी से चला जा रहा था और खेती,
पशुओं
या व्यापार की प्रचुरता थी;
या यह
कि अभी उस ओर समाज का विशेष ध्यान न गया था। फलत: ये बीज रूप में ही
थे। भरसक यह दूसरी ही बात थी। मगर इस पर अधिक विचार यहाँ हो नहीं
सकता।
फिर भी इतना
तो जान ही लेना होगा कि जब तीन ही गुणों के अनुसार वर्णों के कर्म
बँटे हैं और यह बँटवारा स्वाभाविक है,
न कि
जबर्दस्ती बना या बनावटी,
तब तो
दरअसल ब्राह्मण,
क्षत्रिय और वैश्य इन्हीं तीन वर्णों की संभावना रहती है,
न कि
चौथे की। यों तो हमने भी पहले इसी तरह के प्रसंग में चारों वर्णों का
बँटवारा कर दिया है। मगर वह बात हमारी अपनी न हो के परम्परासिध्द ही
है। वहाँ हमने अपनी ओर से इस तीन या चार के बारे में कुछ न कह के उसी
का उल्लेख कर दिया है। अपनी बात तो हमने अलग ही कही है। शूद्र नाम
का कोई स्वतन्त्र वर्ण न था,
हमने
यही लिखा है। लेकिन जब यहाँ इन श्लोकों के शब्दों और प्रसंगों को
देखते हैं तो हमें साफ कहना ही पड़ता है कि शब्दों के अर्थ से भी तीन
ही वर्ण सिध्द होते हैं। अगर सत्तव,
रज,
तम की
मिलावट में कमी-बेशी करके चौथे का भी रास्ता निकाल लें,
जैसा
कि किया जाता है और हमने भी लिखा है,
तो इस
तरह चार से ज्यादा जानें कितनी ही वर्ण बन सकते हैं। क्योंकि मिलावट
में जो कमी-बेशी होगी वह तो हजारों तरह की हो सकती है न
?
आधा,
चौथाई,
दशमांश,
शतांश,
सहस्रांश आदि के हिसाब से वह सम्मेलन,
वह
मिश्रण हजारों तरह का हो जायगा। इसलिए हमारे जानते यह बात दार्शनिक
युक्ति से शून्य है।
देखिए न,
41वें
श्लोक में ही तो
'प्रविभक्तानि'
लिखा
है,
जिसका अर्थ है
कि सबों के कर्म बिलकुल ही जुदे-जुदे हैं। मगर जब सेवा सबों का धर्म
बन गयी और शूद्र के लिए दूसरा कुछ बताया ही नहीं,
तो
उसके कर्म को प्रविभक्त कहना कैसे उचित होगा
?
और अगर यह बात
न हो तो उसे स्वतन्त्र वर्ण कैसे माना जाय
?
इसी
41वें
श्लोक में ही एक मजेदार बात और है। आगे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को
अलग-अलग श्लोकों में कह के शूद्र और वैश्य को एक ही में कह दिया और
जैसे-तैसे काम चला लिया है। पहले भी
'स्त्रियो
वैश्यास्तथा शूद्रा:'
(9।32)
में
इसी तरह की बात आयी है। हमने वहीं इसका इशारा भी कर दिया है। मगर
41वें
श्लोक में ब्राह्मण,
क्षत्रिय,
वैश्य तीनों
का एक ही समस्त पद बना के
'ब्राह्मण
क्षत्रियविशां'
कह
दिया है। केवल शूद्र को अलग
'शूद्राणा'
कहा
है। समास करने पर श्लोक में अक्षर न बढ़ जाय और छन्द में गड़बड़ न हो
जाय इसके लिए वैश्य की जगह उसी अर्थ में विशब्द रखना पड़ा है। फिर भी
चाहते तो 'विप्राणांक्षत्रियाणां
च विट्शूद्राणां च भारत'
ऐसा
श्लोक बना दे सकते थे। किन्तु ऐसा न करके तीनों को एक जगह जोड़ने में
यही आशय प्रतीत होता है कि दरअसल विभक्त कर्म तीन के ही हैं और
स्वतन्त्र वर्ण भी यही हैं। हाँ,
शूद्र
भी माना जाता है। मगर उसके कर्म ऐसे नहीं हैं।
और जब सब
चीजें तीन ही तीन गिनाई गयी भी हैं तो वर्णों को एकाएक चार कह देना
भी प्रसंग से अलग सा हो जाता है। वैश्य के व्यापार को सत्यानृत या
झूठ-सच की चीज कहते भी हैं और खेती भी हिंसामय ही है,
और ये
दोनों तामसी ही हैं। इसलिए उसे तामस,
क्षत्रिय को राजस और ब्राह्मण को सात्तिवक मानना ही उचित है। यही बात
खूब जँचती भी है। क्षत्रिय तो राजा भी कहा जाता है और उसकी राजसी ही
बात मानी भी जाती है। ज्ञान तो सात्तिवक हुई। बस,
अधिक
आगे के लिए।
अगला पृष्ठ
: अठारहवाँ अध्याय (भाग-2)
(शीर्ष पर वापस)