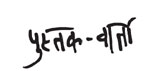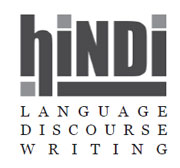|
3. गीता की शेष बातें
गीता की प्रमुख बातें और मुख्य मन्तव्यों के
विवेचन के सिलसिले में ही हमने जो 'गीता का धर्म और मार्क्सवाद' का
स्वतन्त्र रूप से विचार किया है उसका कारण तो बताई चुके हैं। उस लम्बे
विवेचन से भी उसके स्वतन्त्र निरूपण की आवश्यकता का पता लोगों को लग जाता
है। अतएव हमें फिर उसी साधारण मार्ग पर आ जाना और गीता की बची-बचाई प्रमुख
बातों पर कुछ विशेष प्रकाश डाल देना है। बेशक, अब जिन बातों का विवेचन हम
करेंगे वह भी अहमियत तथा महत्व रखती हैं और गीता
में उनका भी अपना स्थान है। मगर यह ठीक है कि उन्हें वैसी महत्ता मिल नहीं
सकती जो अब तक कही गयी गीताधर्म की बातों को मिली है। आगे वाली बातों में
भी कुछ मौलिक जरूर हैं। मगर उनका जिक्र किसी न किसी रूप में पहले आ चुका
है। फलत: यहाँ उनका कुछ विस्तार मात्र कर दिया है। हाँ, जो नयी हैं उनकी
विशेषता यही है कि गीता ने उन्हें नये ढंग से रखा है और इस तरह उन पर अपनी
मुहर लगा दी है।
गीता में ईश्वर
सबसे पहली बात आती है ईश्वर की। गीता में
ईश्वर का नाम और उसकी चर्चा बहुत आयी है, इसमें शक नहीं है। मगर यह चर्चा
कुछ निराले ढंग की है। अठारहवें अध्याय के 'ईश्वर: सर्वभूतानां' (61) श्लोक
में ईश्वर शब्द से ही उसका उल्लेख आया है। जितना स्पष्ट वहाँ लिखा गया है
उतना और कहीं नहीं। और जगह दूसरे-दूसरे शब्दों के द्वारा उसका उल्लेख होने
से वह सफाई नहीं है। एक बात और भी है। तेरहवें अध्या-य के 'समं पश्यन्हि
सर्वत्र' (28) में भी ईश्वर शब्द आया है। उससे पहले के 27वें श्लोक में
परमेश्वर शब्द भी आया है। मगर उसमें वह सफाई नहीं है जो अठारहवें अध्या'य
के उस ईश्वर शब्द में है। वहाँ तो कुछ ऐसा मालूम होता है कि सबों से अलग और
सबों के ऊपर कोई पदार्थ है जिसे ईश्वर कहते हैं और उसकी शरण जाने से ही
उद्धार होगा। इस प्रकार जैसा आमतौर से ईश्वर के बारे में खयाल है ठीक उसी
रूप में वहाँ आया मालूम होता है। मगर यहाँ जो ईश्वर और परमेश्वर है वह उस
रूप में उसे बताता मालूम नहीं पड़ता है। 'प्रकृतिं पुरुषं चैव' इस 19वें
श्लोक से ही शुरू करके यदि देखा जाय तो देह और जीव या प्रकृति और पुरुष का
ही वर्णन इस प्रसंग में है। उन्हीं को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी पहले तथा
इस प्रसंग में भी कहा है। फिर 22वें श्लोक में तो साफ ही कहा है कि इसी
पुरुष को पर, परमात्मा, महेश्वर आदि भी कहते हैं जो इसी देह में मौजूद है।
आगे चलके 26वें में उसे ही क्षेत्रज्ञ कहके 27-28 में परमेश्वर और ईश्वर
कहा है। इसलिए वह सफाई यहाँ है कहाँ? यहाँ तो जीव और ईश्वर एक ही प्रतीत
होते हैं। 31वें श्लोक में भी 'परमात्माऽयमव्यय:' शब्दों के द्वारा इसी
पुरुष को ही अविनाशी परमात्मा कह दिया है।
बेशक पन्द्रहवें अध्यातय के 17-18 श्लोकों में परमात्मा, उत्ताम पुरुष,
पुरुषोत्ताम तथा ईश्वर शब्दों से ऐसे ही ईश्वर का उल्लेख आया है जो प्रकृति
एवं पुरुष के ऊपर-दोनों से निराला और उत्ताम-बताया गया है। लेकिन यहाँ वाला
ईश्वर शब्द मुख्य नहीं है, ऐसा लगता है। चौदहवें अध्यातय के 19वें श्लोक
में पर शब्द आया है। उसी के साथ 'मद्भाव' शब्द है। 26 और 27 श्लोकों में
'माँ' या 'अस्मत्' शब्द है। इससे पता लगता है कि पर शब्द भी परमात्मा का
वाचक है। मगर वह जीवात्मा से अलग यहाँ प्रतीत नहीं होता। हाँ, सोलहवें
अध्याहय के 'असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्' (8) में जो अनीश्वर शब्द
के भीतर ईश्वर है वह उसी ईश्वर का वाचक है, यद्यपि सफाई में कुछ कमी है।
आगे चौदहवें श्लोक का ईश्वर शब्द तो मालिक या शासक के ही अर्थ में आया है।
हाँ, 18, 19, 20 श्लोकों में जो 'अहं' और 'माँ' शब्द आये हैं वह जरूर ईश्वर
के मानी में हैं। सत्रहवें अध्याय के छठे श्लोक में 'माँ' शब्द स्पष्ट
ईश्वर के अर्थ में नहीं है। किन्तु जीवाभिन्न ईश्वर ही उसका आशय मालूम पड़ता
है। बेशक, 27वें श्लोक में जो 'तदर्थीय' शब्द है उसका 'तत्' शब्द ईश्वरवाचक
है। लेकिन वह व्यापक अर्थ में ही आया है।
अठारहवें अध्याय के 46वें श्लोक में 'तं' शब्द ईश्वर के ही मानी में आया
है, चाहे स्पष्टता उतनी भले ही न हो। उससे पहले के 43वें श्लोक का ईश्वर
शब्द शासक के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 50-58 श्लोकों में ब्रह्म और
अस्मत् शब्द बार-बार आये हैं और ईश्वरार्थक हैं। यही बात 65-66 श्लोकों के
'अहं', 'मत्' आदि शब्दों की है। इस पर आगे विशेष बातें लिखी जायँगी। 68वें
श्लोक में भी यही बात है। ग्यारहवें अध्याबय के 5-55 श्लोकों में 'अहं',
'माम्', 'मत्', 'मे', 'मम्', 'ऐश्वरम्' आदि शब्द ईश्वरवाची ही हैं। दसवें
के 2-42 श्लोकों में भी बार-बार 'अहं' शब्द 'परमात्मावाची' ही है। यही
हालत नवें अध्याहय की भी है। सातवें के 29-30 श्लोक में और आठवें के शुरू
के चार श्लोकों में भी ब्रह्म, अधियज्ञ आदि शब्द ईश्वर के ही अर्थ में
प्रयुक्त हुए हैं। आगे के 'अक्षर' शब्द का भी यही मतलब है। अव्यक्त,
परपुरुष आदि शब्द भी इसी मानी में आये हैं। यहाँ 'अस्मत्' शब्द के जितने
रूप हैं सभी ईश्वर के ही अर्थ में हैं। सातवें अध्याहय के 'वासुदेव' तथा
'अनुत्तामागति' ईश्वरार्थ कही हैं। वहाँ 'माम्', 'अहम्' आदि बार-बार आने
वाले शब्द भी उसी मानी में आये हैं। छठे अध्याय की भी यही बात है। पाँचवें
के 10वें श्लोक का 'ब्रह्म' शब्द और 29वें श्लोक में 'महेश्वर' शब्द
निस्सन्देह ईश्वरवाचक हैं। 'अहं' या 'मां' आदि शब्द भी वैसे ही हैं। चौथे
अध्या2य के पहले श्लोक का 'अहं' शब्द ईश्वरार्थक है। मगर तीसरे के 'मया' और
'मे' कृष्ण के ही अर्थ में आये हैं। छठे के 'अज' एवं 'ईश्वर' शब्द ईश्वर के
अर्थ में आये हैं। फिर 14 श्लोक तक 'अस्मत्' शब्द का प्रयोग भी उसी मानी
में है। 23वें का यज्ञ शब्द व्यापक अर्थ में ईश्वर को भी कहता है। उसके बाद
का ब्रह्म शब्द परमात्मा का ही वाचक है। 31वें में भी ब्रह्म का वही अर्थ
है। 35वें का 'मयि' शब्द ईश्वरार्थ है।
तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में 'मया' शब्द ईश्वर के ही अर्थ में आया है।
दसवें का प्रजापति ईश्वर ही है और पन्द्रहवें का अक्षर भी वही है। 30वें
में 'मयि' शब्द ईश्वर को ही कहता है। मगर 31-32 में जो 'मे' शब्द है वह
कृष्ण का वाचक है। जिस प्रकार अठारहवें अध्यावय में अत्यन्त सफाई के साथ
ईश्वर का जिक्र अन्त में आया है, ठीक उसके उल्टाा दूसरे अध्याधय में उसकी
चर्चा तक कहीं हुई नहीं! वह वहाँ कतई बेदखल कर दिया गया है! वहाँ तो आत्मा
ही परमात्मा बना बैठा है। इस प्रकार स्पष्ट रूप में तो बहुत ही कम, लेकिन
अस्पष्ट रूप में ईश्वर का उल्लेख गीता में पद-पद पर पाया जाता है।
इस तरह मालूम हो गया है कि गीता में ईश्वर की किसी न किसी रूप में सैकड़ों
बार से ज्यादा चर्चा आयी है। मगर असली रूप में हम उसे केवल अठारहवें
अध्यांय के 61वें श्लोक में ही साफ-साफ पाते हैं। कृष्ण ने खुद जो 'मैं' और
'मेरा' आदि के रूप में सैकड़ों बार कहा है उसमें कुछी बार अपने लिए-साकार
वसुदेवपुत्र के लिए-कहा है। मगर आमतौर से अपने ईश्वरीय स्वरूप को ही लक्ष्य
करके बोल गये हैं। यदि पूर्वापर का विचार करके देखा जाय या शरीरी कृष्ण में
वे बातें लागू होई नहीं सकती हैं, जिनका उल्लेख उनने ऊपर बताये स्थानों में
जानें कितनी बार किया है। जब चौथे अध्याहय के शुरू में ही उनने कहा है कि
मैंने यह योग पहले विवस्वान् को बताया था और विवस्वान् ने मनु को, तो यह
बात शरीरी कृष्ण में कथमपि लागू हो सकती है नहीं। उसी के आगे जब अवतार की
बात के प्रसंग में कहा है कि मैं समय-समय पर पैदा हो जाता हूँ, तो यह भी
शरीरधारी के लिए सम्भव नहीं। कोई नहीं मानता कि कृष्ण बार-बार जन्म लेते
हैं। यों तो हर मनुष्य भी बार-बार जन्मता ही है। मगर उसे अवतार नहीं कहते।
चार्तुण्यंय की रचना भी कृष्ण के शरीर से नहीं होती। हालाँकि उनने कहा है
कि मैं ही चार्तुण्यंष बनाता हूँ। सातवें अध्याय में अपने को अधियज्ञ कहा
है। यह भी ईश्वर के ही लिए सम्भव है, न कि शरीर वाले के लिए। अधियज्ञ का
आशय आगे मालूम होगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्रसंग के देखने से पता चलता है
कि आत्मज्ञान के बल से कृष्ण अपनी आत्मा को परमात्मस्वरूप ही अनुभव करते थे
और वैसा ही बोलते भी थे। वह उपदेश के समय आत्मा का ब्रह्म के साथ तादात्म्य
मानते हुए ही बातें करते थे। मालूम होता है, जरा भी नीचे नहीं उतरते थे!
उसी ऊँचाई पर बराबर कायम रहते थे। इसीलिए तो इन उपदेशों में अपूर्व
आकर्षणशक्ति और मोहनी है। बृहदारण्यक उपनिषद् में वामदेव के इसी प्रकार के
अनुभव का उल्लेख आया है। वहाँ लिखा है कि ''तद्वैतत्पश्यन्नृषिर्वामदेव:
प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेति। तदिदमप्येतहि य एवं वेदाहं
ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व भवति'' (1।4।10)।
इसका अर्थ यह है कि ''वामदेव ऋषि को जब अपनी ब्रह्मरूपता का साक्षात्कार हो
गया तो उनने कहा कि ऐं, हमीं तो मनु, सूर्य आदि बने! आज भी जिसे ठीक वैसा
ही अनुभव अपनी ब्रह्मरूपता का हो जाय वह भी यही मानता है कि वही यह सारा
संसार बन गया है।'' संसार तो ईश्वर का ही रूप माना जाता है। गीता में तो
इसकी घोषणा है। इसलिए जो अपने को ब्रह्मरूप ही मानने लगेगा वह तो यह समझेगा
ही कि सारी दुनिया उसी का रूप है। कृष्ण का अनुभव ऐसा ही था। इसीलिए सातवें
अध्याय के 3-12 श्लोकों में, नवें के 16-19 श्लोकों में और दसवें के प्राय:
सभी श्लोकों में विभूति के रूप में उनने सबको अपना ही रूप बताया है।
ग्यारहवें अध्यामय में अपने आपको ही उनने कालरूपी कहा है। फलत: गीता के
अहम् और मम आदि शब्दों को देख के जो ऐसा मानते हैं कि सगुण ईश्वर का वर्णन
गीता में है वह भूलते हैं। अठारहवें अध्यायके 'सर्वधार्मान्परित्यज्य
मामेकं' (66) इत्यादि पूरे श्लोक में भी निर्गुण तथा निराकार से ही मतलब
है, न कि साकार से। क्योंकि यदि कृष्ण का अभिप्राय अपने साकार रूप से होता
तो सिर्फ 'मेरी ही शरण जाओ'-'मामेकं शरणं व्रज' की जगह वह कह देते कि मेरी
ही शरण आओ-'मामेकं शरणमाव्रज'। 'व्रज' का अर्थ है जाओ और आव्रज का अर्थ है
आओ। जब वह सामने ही मौजूद थे तो जाओ कहना ठीक न था। जाओ तो परोक्ष या
दूरवर्ती पदार्थ के ही लिए कहा जा सकता है। 'मामेकं शरणं चेहि' कह देने से
श्लोक भी ठीक रहता। 'एहि' का अर्थ है आना। या कुछ दूसरा ही पद कह देते
जिसका अर्थ आओ होता। इस पर ज्यादा विचार आगे मिलेगा।
(शीर्ष पर वापस)
ईश्वर हृदयग्राह्य
हमें यहाँ ईश्वर के सम्बन्ध की एक खास बात
की ओर ध्यान देना है। वह यह है कि गीता के मत से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार
करने का एक ही परिणाम होता है कि हमारा आचरण प्रशंसनीय और लोकहितकारी हो
जाता है। इसीलिए गीता ने ईश्वर की सत्ता की स्वीकृति की तरफ उतना ध्या न
नहीं दिया है, जितना हमारे आचरण की ओर। इस सम्बन्ध में ज्यादा महत्तवपूर्ण
बात कहने के पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। उसकी ओर ध्यासन जाना जरूरी है।
ईश्वर के बारे में तेरहवें अध्याय में कहा है कि ''वह ज्ञान है,
ज्ञेय-ज्ञान का विषय-है, ज्ञान के द्वारा अनुभवनीय है और सबों के हृदय में
बसता है''-''ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्'' (17)।
अठारहवें अध्याय के 61वें श्लोक में तो यह कहने के साथ ही और भी बात कही
गयी है। वहाँ तो कहते हैं कि ''अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में
ही रहता है और अपनी माया (शक्ति) से लोगों को ऐसे ही घुमाता रहता है जैसे
यन्त्रा (चर्खी आदि) पर चढ़े लोगों को यन्त्रा का चलाने वाला-''ईश्वर:
सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्ररूढाणि
मायया''॥
यहाँ दो बातें विचारणीय हैं। पहली है हृदय में रहने की। यह कहना कि हृदय
ईश्वर का घर है, कुछ ठीक नहीं जँचता है। वह जब सर्वत्र है, व्यापक है, तो
हृदय में भी रहता ही है, फिर इस कथन के मानी क्या? यदि कहा जाय कि हृदय में
विशेष रूप से रहता है, तो भी सवाल होता है कि विशेष रूप से रहने का क्या
अर्थ? यह तो कही नहीं सकते कि वहाँ ज्यादा रहता है और बाकी जगह कम। यह भी
नहीं कि जैसे यन्त्रा का चलाने वाला बीच में बैठ के चलाता है तैसे ही ईश्वर
भी बीच की जगह-हृदय-में बैठ के सबों को चलाता है। यदि इसका अर्थ यह हो कि
हृदय के बल से ही चलाता है तो यह कैसे होगा? जिस यन्त्रा के बल से चलाते
हैं उसका चलानेवाला उससे तो अलग ही रहता है। मोटर या जहाज वगैरह के चलाने
और घुमाने-फिरानेवाले यन्त्रा से अलग ही रह के ड्राइवर वगैरह उन्हें
चलाते-घुमाते हैं। हृदय में बैठ के घुमाना कुछ जँचता भी नहीं, यदि इसका
मतलब व्यावहारिक घुमाने-फिराने जैसा ही हो।
इसीलिए मानना पड़ता है कि हृदय में रहने का अर्थ है कि वह हृदय-ग्राह्य है।
सरस और श्रद्धालु हृदय ही उसे ठीक-ठीक पकड़ सकता है। दिमाग या बुद्धि की
शक्ति हुई नहीं कि उसे पकड़ सके या अपने कब्जे में कर सके। ईश्वर या ब्रह्म
तर्क-दलील से जाना नहीं जा सकता, यह बात छान्दोग्योपनिषद् में भी उद्दालक
ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कही है। वहाँ कहा है कि अक्ल बघारना और बाल की
खाल खींचना छोड़ के श्रद्धा करो ऐ मेरे प्यारे,-'श्रद्धत्स्व सोम्य'
(6।12।3)। और यह श्रद्धा हृदय की चीज है। यह पहले ही कहा जा चुका है। इसलिए
गीता के मत से ईश्वर हृदयग्राह्य है। फलत: जो सहृदय नहीं वह ईश्वर को जान
नहीं सकता।
(शीर्ष पर वापस)
हृदय की शक्ति
अब दूसरी बात रही लोगों के चलाने की। सो भी
ठीक ही है। जिस हृदय ने भगवान् को जान लिया, पकड़ लिया, कब्जे में कर लिया
वह दुनिया को चाहे जिस ओर घुमा सकता है। नरसी, नामदेव, सूर, तुलसी आदि
भक्तजनों की बातें ऐसी ही कही जाती हैं। बताया जाता है कि भीष्म ने कहा कि
''आज मैं हरिसों अस्त्रा गहाऊँ।'' उनने अपने प्रेम के बल से अपनी प्रतिज्ञा
रख ली थी और कृष्ण की तुड़वा दी थी। सूरदास ने कहा था कि ''हिरदयसे जौं
जाहुगे बली बखानौ तोहिं''। रामकृष्ण ने विवेकानन्द जैसे नास्तिक को एक शब्द
में आस्तिक बना दिया। वह सच्चे हृदय की ही शक्ति थी जिसने भगवान् को पकड़
लिया था। इसीलिए जिसने शुद्ध हृदय से श्रद्धा के साथ भगवान् को अपना लिया
है वह दुनिया को इधर से उधर कर सकता है।
गीता के इस कथन में एक बड़ी खूबी है। संसार के लोगों को हम तीन भागों में
बाँट सकते हैं। या यों कहिये कि पहले दो भाग करके फिर एक भाग के दो भाग कर
देने पर तीन भाग हो जाते हैं। आस्तिक और नास्तिक यही पहले दो भाग हैं। फिर
आस्तिक के दो भाग हो जाते हैं-साकार ईश्वरवादी और निराकारवादी। इस प्रकार
साकारवादी, निराकारवादी और निरीश्वरवादी ये तीन भाग हो गये। हमने देखा है
कि ये तीनों ही आपस में तर्क-दलीलें करते और लड़ते रहते हैं। यह झमेला इतना
बड़ा और इतना पुराना है कि कुछ कहिये मत। जब से लोगों को समझ हुई तभी से ये
तीनों मतवाद चल पड़े। इन पर सैकड़ों पोथे लिखे जा चुके हैं।
मगर गीता इन तीनों पर तरस खाती और हँसती है। उसने जो ईश्वर को हृदय की चीज
बना के बुद्धि के दायरे से उसे अलग कर दिया है, उसके चलते ये सभी झगड़े
बेकार मालूम होते हैं और गीता की नजरों में ये झगड़ने वाले सिर्फ भटके हुए
सिद्ध हो जाते हैं। इन झगड़ों की गुंजाइश तो बुद्धि के ही क्षेत्र में है न?
इसीलिए जहाँ हृदय आया कि इन्हें बेदखल कर देता है, कान पकड़ के हटा देता है।
क्यों? इसीलिए कि यदि ईश्वर है तो वह तो यह नहीं देखने जाता है कि किसके
ऊपर आस्तिक या नास्तिक की छाप (label) लगी है, या साकारवादी और निराकारवादी
की छाप। वह तो हृदय को देखता है। वह यही देखता है कि उसे सच्चाई से ठीक-ठीक
याद कौन करता है।
(शीर्ष पर वापस)
आस्तिक-नास्तिक का भेद
जब इस प्रकार देखते हैं तो पता लगता है कि
साकारवादी और निराकारवादी तो याद करते ही हैं। मगर निरीश्वरवादी भी उनसे कम
ईश्वर को याद नहीं करते! यदि भक्ति का अर्थ यह याद ही है तो फिर नास्तिक भी
क्यों न भक्त माने जायँ? बेशक, प्रेमी याद करता है और खूब ही याद करता है,
यदि सच्चा प्रेमी है। मगर पक्का शत्रु तो उससे भी ज्यादा याद करता है।
प्रेमी तो शायद नींद की दशा में ऐसा न भी करे। मगर शत्रु तो अपने शत्रु के
सपने देखा करता है, बशर्ते कि सच्चा और पक्का शत्रु हो। इसीलिए मानना ही
होगा कि ईश्वर का सच्चा शत्रु भक्तों से नीचे दर्जे का हो नहीं सकता, यदि
ऊँचे दर्जे का न भी माना जाय। पहले जो कहा है कि धर्म तो व्यक्तिगत और अपने
समझ के ही अनुसार ईमानदारी से करने की चीज है, उससे भी यही बात सिद्ध हो
जाती है। यदि हमें ईमानदारी से यही प्रतीत हो कि ईश्वर हुई नहीं और हम
तदनुसार ही अमल करें तो फिर पतन की गुंजाइश रही कहाँ जाती है?
इसीलिए प्रौढ़ नैयायिक उदयनाचार्य ने ईश्वर-सिद्धि के ही लिए बनाये अपने
ग्रन्थ 'न्यायकुसुमांजलि' को पूरा करके उपसंहार में यही लिखा है कि वे साफ
ही सच्चे और ईमानदार नास्तिकों के लिए ही वही स्थान चाहते हैं जो सच्चे
आस्तिकों को मिले। उनने प्रार्थना के रूप में अपने भगवान् से यही बात बहुत
सुन्दर ढंग से यों कही है-''इत्येवं श्रुतिनीति
संप्लवजलैर्भूयोभिराक्षालिते; येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शैलसाराशया:।
किन्तु प्रस्तुतविप्रतीप विधायोऽप्युच्चैर्भवच्चिन्तका:; काले कारुणिक
त्वयैव कृपया ते भावनीया नरा:।'' इसका आशय यही है कि ''कृपासागर, इस प्रकार
वेद, न्याय, तर्क आदि के रूप में हमने झरने का जल इस ग्र्रन्थ में प्रस्तुत
किया है और उससे उन नास्तिकों के मलिन हृदयों को अच्छी तरह धो दिया भी है,
ताकि वे आपके निवास योग्य बन जायँ। लेकिन यदि इतने पर भी आपको वहाँ स्थान न
मिले, तो हम यही कहेंगे कि वे हृदय इस्पात या वज्र के हैं। लेकिन यह याद
रहे कि प्रचंड शत्रु के रूप में वे भी तो आपको पूरी तौर से आखिर याद करते
ही हैं। इसलिए उचित तो यही है कि समय आने पर आप उन्हें भी भक्तों की ही तरह
संतुष्ट करें।'' कितना ऊँचा खयाल है! कितनी ऊँची भावना है! गीता इसी खयाल
और इसी भावना का प्रसार चाहती है।
(शीर्ष पर वापस)
दैव
तथा आसुर सम्पत्ति
अच्छा, अब जरा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार
करने का परिणाम क्या होता है, क्या होना चाहिए, इस पर भी गीता की दृष्टि
देखें। गीता के सोलहवें अध्याय के शुरूवाले छह श्लोकों में दैवी तथा आसुरी
सम्पत्तियों का संक्षेप में वर्णन कर दिया है। इन दोनों का तात्पर्य मनुष्य
के ऐसे गुणों और आचरणों से है जिनसे समाज का हिताहित, भला-बुरा होता है।
कल्याणकारी और मंगलमय गुणों एवं आचरणों को दैवी सम्पत्ति और विपरीतों को
आसुरी सम्पत्ति कहा है। पाँचवें श्लोक में यही बात साफ कह दी है कि दैवी
सम्पत्ति मुक्तिसम्पादक और कल्याणकारी है, जब कि आसुरी सभी बन्धानों और
संकटों को पैदा करती है। साथ ही यह भी कहा है कि अर्जुन के लिए चिन्ता की
तो कोई बात हुई नहीं। क्योंकि वह तो दैवी सम्पत्तिवाला है। इसके बाद छठे
श्लोक के उत्तारार्ध्द में कहा है कि अब तक तो दैव सम्पत्ति का ही विस्तृत
विवेचन किया गया है। मगर आसुरी तो छूटी ही है। इसलिए उसे भी जरा खोल के बता
दें तो ठीक हो। फिर सातवें से लेकर अध्याय के अन्त तक के शेष 18 श्लोकों
में यही बात लिखी गयी है। बेशक, अन्त के 22-24 श्लोकों में निषेध के रूप
में ही यह बात कही गयी है। शेष श्लोकों में साफ-साफ निरूपण ही है।
यहाँ जो यह कहा गया है कि अब तक तो विस्तार के साथ दैव सम्पत्ति का ही
वर्णन आया है, उससे साफ हो जाता है कि गीता के शुरू से लेकर सोलहवें अध्याय
के कुछ श्लोकों तक मुख्यत: वही बात कही गयी है। यह तो निर्विवाद है कि पहले
अध्यासय में खुल के समाज-संहार की कड़ी से कड़ी निन्दा की गयी है। दूसरे में
भी जो अर्जुन को यह कहा गया है कि लोग तुम्हें गालियाँ देंगे और तुम पर
थूकेंगे वह भी सामाजिक दृष्टि से ही तो है। तीसरे अध्याय में तो समाज
रक्षार्थ यज्ञ का विस्तार ही बताया गया है और कहा गया है कि समाज के लिए
उसे मूलभूत मानना चाहिए। इसी प्रकार चौथे के 'नायं लोकोऽस्त्यज्ञस्य' (31)
आदि के द्वारा तथा छठे के 'आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति' (32) के जरिये
लोक-कल्याणकारी भावनाओं एवं आचरणों का ही महत्तव दिखाया है। सातवें से लेकर
पन्द्रहवें अध्याय तक यही बात जगह-जगह किसी न किसी रूप में बराबर पायी जाती
है। इसलिए स्पष्ट है कि समाज के कल्याण से ही गीता का मतलब है। यों तो योग
का जो स्वरूप पहले बताया जा चुका है वह समाज के कल्याण की ही चीज है। दसवें
अध्याय के अन्त के 41वें श्लोक में तो साफ ही कह दिया है कि संसार में जोई
चमत्कार वाली गुणयुक्त चीज है वह भगवान् का ही रूप है, उसी का अंश है। इससे
तो स्पष्ट है कि गीता की दृष्टि में भगवान् का मतलब ही है जगन्मंगलकर्ता
से। गीता वैसे भगवान् को कहाँ देखती और मानती है जो केवल स्वर्ग और नर्क
में भेजने का इन्तजाम करता हो, या मुक्ति देता हो? गीता ने तो ऐसे भगवान्
का खयाल ही नहीं किया है।
यही बात सोलहवें अध्याय के 7-24 श्लोकों से भी सिद्ध होती है। आमतौर से यही
होता है, यही बात देखी जाती है कि जो कुकर्मों को करता हुआ ईश्वर की सत्ता
में विश्वास नहीं करता हो उसकी निन्दा या उसके खण्डन-मण्डन का जब प्रसंग
आये तो इसी बात से शुरू करते हैं कि देखिए न, यह तो ईश्वर को ही नहीं मानता
है और साफ ही कहता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति या इसके काम के संचालन के
लिए उसकी जरूरत हुई नहीं! फिर और लोगों की इसे क्या परवाह होगी? उनके हितों
को क्यों न पाँव तले रौंदेगा? आदि-आदि। ठीक भी यही प्रतीत होता है और
स्वाभाविक भी। भगवान् तो लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है और जो उसे ही नहीं
मानता वह बाकी को क्यों मानने लगा? लोगों का गुस्सा भी यदि उस पर उतरेगा तो
यही कहके कि जब यह शालिग्राम को ही भून देता है तो इसे बैंगन भूनने में
क्या देर? अन्त में भी सब कुछ लानत-मलामत के बाद यही कहेंगे कि इसकी ऐसी
हिम्मत कि भगवान् तक को भी इनकार कर जाये?
मगर गीता में कुछ और ही देखते हैं। वहाँ तो असुरों का लक्षण बताते हुए पूरे
सातवें श्लोक में ईश्वर का नाम ही नहीं आया है। आसुर-सम्पत्ति वाले इस
संसार के मूल में ईश्वर को नहीं मानते यह बात सिर्फ आठवें श्लोक के
पूर्वार्ध्द के अन्त मेंयों पायी जाती है कि देखो न, ये लोग संसार के मूल
में उसे नहीं मानते-'जगदाहुरनीश्वरम्'। इसके पहले सातवें में तो यही कहा है
कि ''असुर लोग तो क्या करें क्या न करें यह-कर्तव्याकर्तव्य-जानते ही नहीं,
उनमें पवित्रता भी नहीं होती और न उनका आचरण ही ठीक होता है। सत्य का तो
उनमें नाम भी नहीं होता''-''प्रवृ¯त्ता च निवृ¯त्ता च जना न विदुरासुरा:। न
शौचं नापिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।'' आठवें के शुरू में भी कहा है कि
''वे जगत् को बेबुनियाद और इसीलिए निष्प्रयोजन मानते
हैं''-'असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहु:।' और जब ऐसी बात है तो फिर ईश्वर की
क्या जरूरत? वह तो तभी होती जब यह संसार किसी खास मकसद या उद्देश्य को लेकर
बनाया गया होता-बना होता। इसीलिए वे कहते हैं कि ईश्वर की कोई जरूरत हुई
नहीं।
(शीर्ष पर वापस)
समाज का कल्याण
इस प्रकार हम देखते हैं कि अनीश्वरवाद या
नास्तिकता को पीछे धकेल दिया गया है। उसे वह महत्तव नहीं मिला है जो आमतौर
से दिया जाता है। गीता ने तो महत्तव दिया है उन्हीं चीजों को जिनसे संसार
के उत्थान-पतन का-इसकी उन्नति-अवनति का-गहरा सम्बन्ध है। भले-बुरे की पहचान
होना, कर्तव्य-अकर्तव्य की जानकारी, उत्ताम आचरण, बाहर-भीतर पवित्रता और
सच्चा व्यवहार-यही चीजें तो समाज की बुनियाद हैं। इनके बिना न तो हमीं एक
मिनट टिक सकते और न यह समाज ही चल सकता है। ईश्वर को आप मानिये, या मत
मानिये। मगर ये चीजें मानिये खामख्वाह। आपका अमल अगर इन्हीं के अनुसार हो
तो हमें आपके अनीश्वरवाद से-आपकी नास्तिकता से-कोई मतलब नहीं, उसकी परवाह
हम नहीं करते। हम जानते हैं कि उसका जहरीला डंक खत्म हो गया है। फलत: वह
कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप तो पिंजड़े में बन्द पक्षी हो गये हैं इन्हीं बातों
के करते। इसलिए समाज के ही गीत गायेंगे। न तो स्वच्छन्द उड़ान ही मार सकते
और न मनचाही डाल पर बैठ के स्वतन्त्र गीत ही गा सकेंगे। यही है गीता का इस
सम्बन्ध में वक्तव्य, यही है उसका कहना।
मगर जिनमें यही चीजें नहीं हैं-जो असुर हैं-जो देव नहीं हैं उनका क्या
कहना? वे ईश्वर को क्यों मानने लगे? यह परस्पर विरोधी बातें जो हैं। यह होई
नहीं सकता कि सदाचार और कर्तव्यपरायणता न रहे तथा बाहर-भीतर एक समान ही
सच्चा व्यवहार भी न रहे; मगर ईश्वरवादी बने रहें। गीता की नजरों में ये
दोनों बातें एक जगह हो नहीं सकती हैं। बेशक, आज तो धर्म और ईश्वर की
ठेकेदारी लिये फिरने वाले ऐसे लोगों की ही भरमार है जिनमें ये बातें जरा भी
पायी नहीं जाती हैं। एक ओर देखिए तो कण्ठी-माला, जटा, टीका-चन्दन,
दण्ड-कमण्डल और क्या-क्या नहीं हैं। सभी के सभी धर्म वाले ट्रेडमार्क पाये
जाते हैं। मगर दूसरी ओर ऐसे लोगों में न तो कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान है,
न तदनुकूल आचरण है, न बाहर-भीतर सर्वत्र होने वाली पवित्रता ही है और न
सच्चाई तथा ईमानदारी ही। आज तो यही बात धार्मिक संसार में सर्वत्र ही पायी
जाती है। सब जगह इसी की छूट है। कोई पूछनेवाला ही नहीं कि यह क्या अन्धे
रखाता है। जिस हृदय में भगवान् बसे वह कितना पवित्र और कितना उदार होगा!
उसकी गम्भीरता और उच्चता कैसी होगी! वह विश्वप्रेम से कितना ओतप्रोत होगा!
(आखिर ईश्वर तो प्रेममय, सत्य, शुद्ध, आनन्दरूप और निर्विकार है न? और वही
हमारे हृदय में बसता भी है। फिर भी यह गन्दगी और बदबू? कस्तूरी जहाँ हो
वहाँ उसकी सुगन्ध न फैले, यह क्या बात? और ईश्वर की गन्ध तो भौतिक कस्तूरी
के गन्ध से लाख गुना तेज है। फिर हमारे दिलों में, जहाँ वही मौजूद है,
सत्य, प्रेम, दया, पवित्रता, सदाचार और आनन्द क्यों नहीं पाया जाता? इन
चीजों का स्रोत उमड़ क्योंत नहीं पड़ता?
कहने के लिए तो लोग कहेंगे कि हम धार्मात्मा हैं, ईश्वरवादी हैं। मगर हैं
ये लोग दरअसल पापात्मा और अनीश्वरवादी। नास्तिक लोग तो जबान से ही ईश्वर की
सत्ता इनकार करते हैं। मगर ये भलेमानस तो अमली तौर पर उसे जहन्नुम पहुँचाते
हैं। हम तो महान् से महान् नास्तिकों को जानते हैं जो अनीश्वरवादी तो थे,
मगर जिनका आचरण इतना ऊँचा और लोकहितकारी था कि बड़े-बड़े पादरी, पण्डित और
धर्मवादी दाँतों तले उँगली दबाते थे। हिम्मत नहीं होती थी कि उनके विरुद्ध
कोई चूँ भी करे, उँगली उठाये। मार्क्स वाद वैसे नास्तिकों को ही चाहता है
जिनके काम से आस्तिक लोग भी शर्मिन्दा हो जायँ। वह बेशक उन धार्मात्माओं से
अपना और समाज का पिण्ड खामख्वाह छुड़ाना चाहता है जो व्यवहार में ठीक उल्टा
चलते हैं। हमें तो अमल चाहिए, काम चाहिए, न कि जबानी हिसाब और जमाखर्च। हम
तो 'कह-सुनाऊँ' नहीं चाहते; किन्तु 'कर-दिखाऊँ' चाहते हैं।
यदि गीता के सोलहवें अध्या'य के 9-18 श्लोकों पर गौर करें तो हमें पता चल
जायगा कि जो धर्म के ठेकेदार आज जनता के हकों की लड़ाई का विरोध करते फिरते
हैं और इस मामले में धर्म और ईश्वर का ही सहारा लेते हैं उन्हीं का चित्र
वहाँ खींचा गया है। यह चित्र ऐसा है कि देखते ही बनता है। इसमें शक नहीं कि
9-14 श्लोकों से तो यह साफ पता नहीं चलता कि धर्म के ठेकेदारों का ही यह
चित्रण है। मगर पन्द्रहवें के 'यक्ष्ये दास्यामि' पदों से, जिनका अर्थ है
कि 'यज्ञ करेंगे और दान देंगे' तथा 'यजन्ते नामयज्ञैस्ते
दम्भेनाविधिपूर्वकम्' (17) से तो यह बात बिलकुल ही साफ हो जाती है। जहाँ
पहले वचनों में सिर्फ यज्ञ करने और दान देने की बात है तहाँ आखिरवाले तो
साफ ही कहते हैं कि-''वे लोग दिखावटी यज्ञ ख्याति आदि के लिए ही करते हैं।
यज्ञों के विधि-विधान से तो उन्हें कोई मतलब होता ही नहीं।'' यह
'अविधिपूर्वकम्' शब्द दूसरे मानी में आई नहीं सकता है। यह इसीलिए धर्म के
ठेकेदारों की नकाब उतार फेंकता है, इसमें शक नहीं।
उनका चित्र खड़ा करना शुरू ही किया है यह कहते हुए कि ''संसार के तो वे
शत्रु ही होते हैं। फलत: उसे चौपट करने के बड़े से बड़े उग्र काम कर डालने की
ताकत रखते हैं''-''प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय जगतोऽहिता:।'' ''संसार से
तात्पर्य यहाँ समाज से ही है। वहाँ बताया गया है कि उनका तो काम ही है समाज
को तहस-नहस करना। ऐसा करते हुए वे खुद भी चौपट हो जाते हैं। क्योंकि समाज
से बाहर तो जा सकते नहीं। उनकी वासनाएँ तथा आकांक्षाएँ इतनी ज्यादा और बड़ी
होती हैं कि उनकी पूर्ति हो सकती नहीं। उनका ठाटबाट और ढोंग इतना ज्यादा
होता है, गरूर इस कदर होता है और प्रभुत्व, प्रभाव या शक्ति का नशा ऐसा
होता है कि कुछ पूछिये मत। जिद में ही पड़के अंट-संट कर बैठते हैं। उन्हें
पवित्रता का तो कोई खयाल रहता ही नहीं। दुनिया भर की फिक्र उन्हीं के माथे
सवार रहती है, ऐसा मालूम होता है। खूब चीजें प्राप्त करो और खाओ, पिओ, मौज
करो, यही उनका महामन्त्र होता है। जानें कितनी उम्मीदें उन्हें होती हैं।
काम और क्रोध ही यही दो उनके पक्के और सदा के साथी होते हैं। विषयवासना की
तृप्ति और शान बढ़ाने के लिए वे हजार जुल्म और अत्याचार कर डालते हैं। बराबर
यही सोचते रहते हैं कि अमुक काम तो हमने कर लिया, अब तो सिर्फ फलाँ-फलाँ
बाकी हैं। इतनी सम्पत्ति तो मिल चुकी ही है। मगर अभी तो कितनी ही गुनी
हासिल करेंगे! बहुत दुश्मनों को खत्म कर डाला है। बचे हुओं को भी न
छोड़ेंगे। हमीं सबसे बड़े हैं, महलों में रहते हैं, जो चाहते हैं करके ही
छोड़ते हैं। हमसे बड़ा ताकतवर है कौन? सुखी भी तो हमीं हैं। न तो हमसे बढ़के
कोई धानी है और न संगी-साथियों वाला ही। हमारे मुकाबिले में कौन खड़ा हो
सकता है? वे दिन-रात खुद अपने ही मुँह से अपनी बड़ाई करते रहते हैं।
रुपये-पैसे, गरूर और नशा की गर्मी में ही चूर रहते हैं। यज्ञ और दान तो वे
केवल दिखाने और ठगने के ही लिए करते हैं। उनमें अहंकार इतना ज्यादा होता है
कि मत कहिये। वे आत्मा-परमात्मा को तो समझते भी नहीं कि क्या चीज हैं-उनके
नाम से ही उन्हें नफरत होती है। नतीजा यह होता है कि उनका पतन होता ही जाता
है। ऊपर तो वे उठ सकते नहीं। दूसरे, तीसरे आदि जन्मों में भी अधिकाधिक नीचे
गिरते ही जाते हैं। ईश्वर या आत्मा तक उनकी पहुँच कभी होती ही नहीं।''
इसी रूप में असुरों या धर्मध्वजजियों का चित्र गीता ने खींचा हैं। 18वें और
20वें श्लोक में एक बार फिर परमात्मा का उल्लेख यद्यपि किया है। मगर वह है
आत्मा के रूप में ही। चाहे ईश्वर के रूप में भी मानें, तो भी जो कुछ उसके
साथ-साथ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि ऊपर लिखे आसुरी व्यवहारों और आचरणों
के करते ही उनकी परमात्मा तक पहुँच हो पाती नहीं। इससे भी यही सिद्ध हो
जाता है कि असल चीज आचरण ही हैं। 21-22 श्लोकों में तो खुल के कही दिया
है-और यह बात उपसंहार की है-कि ''नर्क या पतन के तीन ही रास्ते हैं जिन्हें
काम, क्रोध और लोभ कहते हैं। ये तीनों आत्मा को भी चौपट कर देते हैं। इसलिए
इनसे अपना पिण्ड छुड़ाना जरूरी है। जहन्नुम में ले जाने वाले इन तीनों से
पल्ला छूटने पर ही कल्याणकारी रास्ता सूझता और सदाचरण होता है। फिर तो हर
तरह से मौज ही मौज समझिये''-''त्रिविधां नर-नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन:।
काम: क्रोधस्तथा- लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् ड्ड एतैर्विमुक्त: कौन्तेय
तमोद्वारेस्त्रिभिर्नर:। आचरत्यामन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥'' आखिर
में कार्य-अकार्य या कर्तव्य-अकर्तव्य के जानने और तदनुसार ही काम करने का
आदेश देके यह अध्या'य पूरा किया गया है।
इस तरह देखते हैं कि जिस कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान से ही शुरू किया था उसी
से प्रकरण का अन्त भी किया गया है। यह नहीं कहा गया है कि भगवान् के ज्ञान,
उसकी भक्ति या पूजा-पाठ को ही अपनाना चाहिए। यह कहते भी कैसे? गीता ने तो
पहले ही कह दिया है और उसे आगे भी यही कहना है कि कर्तव्य का पालन ही
भगवान् की पूजा है। फिर उल्टी बात यहाँ कैसे कही जाती? और जब सभी बातों का
पर्यवसान समाज के कल्याण एवं क्षेम में ही है-जब लोकसंग्रह ही गीता का ध्ये
य है-तो दूसरी बात कही जाय कैसे? जब भगवान् का ज्ञान, ध्या न वगैरह भी
मनुष्य को ऐसे साँचे में ढालने के ही लिए है कि उसकी प्रत्येक क्रिया, हरेक
साँस और हर काम संसार के लिए मंगलप्रद बन सके, तो और बातों का अवसर ही कहाँ
रह जाता है? गीता ने ईश्वर-अनीश्वरवाद के झमेले को जिस तरह सुलझाया है और
खुद इस गड़बड़ से जो वह बहुत ऊपर पहुँची हुई है वही उसकी इस सम्बन्ध की खूबी
है।
(शीर्ष पर वापस)
कर्म और धर्म
अब जरा कर्म और धर्म की बातों को भी देखें।
आमतौर से ऐसी धारणा पायी जाती है कि कर्म, क्रिया या अमल तो सभी बुरे-भले
कामों को ही कहते हैं। मगर धर्म कुछ खास कर्मों या कामों का ही नाम है।
धर्म के ही मानी में मजहब और रिलिजन (Religion) शब्दों का भी प्रयोग करके
उनके बारे में भी यही खयाल सर्वत्र पाया जाता है। इसका परिणाम भी बुरा से
बुरा होता है। जब हमने मान लिया कि सिर्फ सन्ध्याह, पूजा, नमाज, रोजा,
प्रार्थना वगैरह धर्म हैं, तब तो स्वाभाविक रूप से बाकी कामों में एक
प्रकार की स्वतन्त्रता का अनुभव करेंगे ही। धर्मों के सम्बन्ध में तो
सैकड़ों तरह के बन्धन होते हैं-कब करें, कैसे करें, कितनी देर तक करें
आदि-आदि। गड़बड़ होने पर नर्क, दोजख आदि के भय भी माथे पर सवार रहते हैं।
भगवान् की रंजिश का भी सबसे बड़ा खतरा इस बात में बना रहता है। इसीलिए
स्वभावत: उनकीपाबन्दी ठीक-ठीक की जाती है-कम से कम पाबन्दी की कोशिश तो
जरूर होती है।
लेकिन बाकी कामों में? उनमें तो कोई डर-भय उस तरह का नहीं होता। हाँ,
लोक-लाज या कानून-वानून का डर जरूर रहता है। मगर लोगों से छिप-छिपाके और
कानून-फन्दे से बच-बचाके भी काम किये जा सकते हैं, किये जाते हैं। कानून की
ऑंख में धूल डालना चतुर खिलाड़ियों के लिए बायें हाथ का खेल है। वे तो कानून
को बराबर चराते फिरते हैं। इसलिए उन्हें स्वतन्त्रता तो करीब-करीब रहती ही
है। क्योंकि भगवान् तो यहाँ दखल देता नहीं और न धर्मराज या यमराज ही। यह तो
धर्म से बाहर की चीजें हैं, जहाँ उनका अधिकार नहीं। यदि थोड़ा-बहुत मानते भी
हैं कि वह दखल देंगे तो भी यह बात अधूरी ही रह जाती है। क्योंकि सन्ध्या ,
नमाज की तरह सच बोलने या शराब न पीने की बात नहीं है। यदि ये चीजें धर्म
में किसी प्रकार आ भी जायें तो भी इनका स्थान गौण है, मुख्य नहीं। देखते ही
हैं कि सन्ध्याह, नमाज वगैरह की पाबन्दी में जो सख्ती पायी जाती है वह सच
बोलने और सूद न लेने या शराब न पीने में हर्गिज नहीं है। बड़े-बड़े
धर्माधिकारी भी बड़े-बड़े कारबारों और जमींदारियों के चलाने वाले होते हैं,
जहाँ झूठ बोलने और जाल-फरेब के बिना काम चलता ही नहीं। मैनेजर, प्रबन्धक और
कारपर्दाज वगैरह के जरिये वह काम करवा के अपने पिण्ड को बचाने की बात केवल
अपने आपको धोखा देना है-आत्मप्रवंचना है। जब कारबार उनका है, जमींदारी उनकी
है तो उसके मुतल्लिक होने वाले झूठ और जाल-फरेब की जवाबदेही उन्हीं पर होगी
ही। यह डूबके पानी पीना और खुदा से चोरी करना ठीक नहीं। यदि कारबार और
जमींदारी के फायदे के लिए वह झूठ और जाल न हो तो बात दूसरी है। मगर यहाँ तो
उन्हीं के चलाने के ही लिए ऐसा किया जाता है।
इसीलिए गीता ने न तो धर्म की श्रेणियाँ बताके मुख्य, अमुख्य या प्रधान और
गौण धर्म जैसा उसका विभाग ही किया है और न कोई दूसरी ही तरकीब निकाली है।
गीता की नजरों में तो धर्म और कर्म या क्रिया (अमल या काम) एक ही चीज है।
जिसे हम अंग्रेजी में ऐक्शन (action) कहते हैं उसमें और धर्म में जरा भी
फर्क गीता नहीं मानती। इसका मोटा दृष्टान्त ले सकते हैं। हिन्दू लोग चार
वर्णों को मानते हुए उनके पृथक्-पृथक् धर्म मानते हैं। उनके सिद्धान्त में
वर्णधर्म एक खास चीज है। मगर चौथे अध्याउय के 12, 13 श्लोकों की अजीब बात
है। 13वें में तो वर्णधर्मों की ही बात है। फिर भी कृष्ण कहते हैं कि
''हमने चारों वर्णों की रचना कर्मों के विभाग के ही मुताबिक की है और ये
कर्म गुणों के अनुसार बने स्वभावों के अनुकूल अलग-अलग होते
हैं'',-''चार्तुण्यंऔ मया सृष्टं गुणकर्मविभागश:।'' यहाँ धर्म की जगह कर्म
ही कहा गया है। 12वें श्लोक में भी कहा है कि ''मर्त्यलोक में कर्मों की
सिद्धि जल्द होती है। इसीलिए यहाँ उसी सिद्धि (इष्टसिद्धि) के लिए देवताओं
का यज्ञ किया करते हैं''-''काङ्क्षन्त: कर्मणां सिध्दिं यजन्त इह देवता:।
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।'' यहाँ यज्ञ को कर्म कहा है,
न कि धर्म; हालाँकि यह तो पक्का धर्म है। धर्मों की सिद्धि न कहके कर्मों
की सिद्धि कहने का भी यही मतलब है कि धर्म और कर्म एक ही चीज है और गीता इन
दोनों में कोई भेद नहीं रखती।
इसी प्रकार अठारहवें अध्याभय के 41-44 श्लोकों में भी चारों वर्णों के ही
धर्मों की बात आयी है। 45-46 श्लोकों में भी उसी सम्बन्ध में यह बताया गया
है कि उन धर्मों के द्वारा ही भगवान् की पूजा कैसे हो सकती है और
इष्टसिद्धि क्योंकर होती है। चारों वर्णों के कुछ चुने-चुनाये धर्मों को
गिनाया भी गया है, जो पक्के और स्वाभाविक माने जाते हैं। सारांश यह कि ये
छह श्लोक वर्णों के धर्मों की जितनी सफाई के साथ कहते हैं उतनी सफाई शायद
ही कहीं मिलेगी। मगर एक बार भी उनमें धर्म शब्द नहीं आया है। खूबी तो यह कि
उन्हीं में कर्म शब्द पूरे आठ बार आया है। धर्म के बारे में जिनका बड़ा जोर
है उन्हें इस बात से काफी धक्का लग सकता है कि जहाँ धर्म शब्द का बार-बार
आना निहायत जरूरी था वहाँ उसे गीता भूल सी गयी! और अगर ऐसे ही अवसर पर धर्म
की बात नहीं आती है, किन्तु उसकी जगह कर्म कहके ही सन्तोष किया जाता है, तो
फिर यह कहने की गुंजाइश रही जाती कहाँ है कि धर्म और कर्म दो चीजें हैं?
जो लोग फिर भी हठ करते रहें और ऐसा कहने का साहस करें कि यद्यपि सभी धर्म
तो कर्म ही होते हैं, तथापि सभी कर्म कदापि धर्म हो नहीं सकते, इसीलिए धर्म
की जगह कर्म कहके काम चलाया जा सकता है और यही बात यहाँ पायी जाती है, उनके
लिए कोई भी समझदारी की बात क्या कही जाय? यों ही कभी-कभी धर्म का नाम ले
लेना और हर विशेष अवसर पर बार-बार कर्म का ही जिक्र करना, जबकि धर्म का
उल्लेख ज्यादा मौजूँ और उचित होता, क्या यह बात नहीं बताता कि गीता इस
झमेले से हजार कोस दूर है? यदि धर्म का नाम कहीं-कहीं आ गया भी तो यों ही,
न कि किसी खास अभिप्राय से, यही कथन ज्यादा युक्तियुक्त प्रतीत होता है। यह
ठीक है कि एकाध जगह धर्म शब्द से ही काम निकलता देख और कर्म कहने में
दिक्कत या कठिनाई समझ के गीता ने धर्मशास्त्रों के अर्थ में ही धर्म शब्द
कहा है। मगर वह ज्यों का त्यों बोल दिया गया है, न कि प्रतिपादन किया गया
है कि धर्म खास चीज है। जैसा कि 'स्वधर्मपि चावेक्ष्य' (2।31) में पाया
जाता है। और जब दूसरे अध्याय में योग का सिद्धान्त एवं स्वरूप बताते समय,
तीसरे अध्याय में यज्ञ की महत्ता दिखाते वक्त, चौथे में यज्ञ का विस्तार
एवं विवरण बताते समय और अठारहवें में अपने-अपने (स्व) धर्मों के रूप में ही
कैसे भगवत्पूजा होती है यह सिद्ध करते समय भी सिर्फ कर्म की ही चर्चा आती
है, न कि धर्म की एक बार भी, तो गीता में प्रतिपादन किसका माना जाय? वहाँ
रहस्य और सिद्धान्त किसके सम्बन्ध का बताया गया माना जाय? धर्म का या कर्म
का? अगर कर्म का, क्योंकि धर्म का कहने की तो कोई भी गुंजाइश हुई नहीं, तो
फिर अन्ततोगत्वा यही बात रही कि गीता ने धर्म और कर्म में कोई भी अन्तर
नहीं किया है। उसने कर्म के ही दार्शनिक विवेचन से सन्तोष करके दिखा दिया
है कि असली चीज कर्म ही है।
एक बात और भी है। गीता ने बार-बार कहा है कि कर्मों से ही बन्धन होता है और
उसी से छुटकारा मिलने को मुक्ति कहते हैं। अर्जुन ने इसी बन्धन के डर से ही
तो आगा-पीछा किया था। यदि दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक से शुरू करके देखें
तो प्राय: हरेक अध्यायय में बार-बार कर्म की इस ताकत का और उससे छुटकारा
पाने की हिकमत का जिक्र मिलेगा। चाहे उस हिकमत को योग कहें, निर्लेपता
कहें, अनासक्ति कहें, समत्व बुद्धि कहें, या इन सबों को मिलाके कहें, यह
बात दूसरी है। मगर यह तो पक्की चीज है कि बार-बार यही बात शुरू से अन्त तक
आयी है। अर्जुन की धारणा कुछ ऐसी थी कि धर्म उन कामों को ही कहते हैं
जिनमें कोई भी बुराई न हो, जिनसे स्वजन-वधा आदि संभव न हों, जैसा ध्या न,
समाधि, पूजा आदि। उसका भी खयाल था कि जिसके करते बुराई हो, हत्या हो या इसी
तरह की और बात हो वह धर्म माना जाने पर भी वस्तुगत्या अधर्म-धर्म विरोधी-ही
है। युद्ध से विरक्त होने और लम्बी-चौड़ी दलीलें पेश करने का उसका यही मतलब
था। दूसरा मतलब हो भी क्या सकता था? इसका उत्तर भी कृष्ण ने साफ ही दे दिया
कि ''सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारंभा हि दोषेण
धूमेनाग्निरिवावृता:'' (18।48), 'श्रेयान्स्वधार्मो विगुण:' (3।35,
18।47),-''बुराई-भलाई तो सर्वत्र मिली हुई हैं। ऐसा काम हो नहीं सकता
जिसमें बुराई न हो या भलाई न हो। इसलिए बुराईवाला होने पर भी स्वधर्म ही
ठीक है। उसी को करना चाहिए।'' गीता में जो धर्म, अधर्म शब्द कहीं-कहीं आ
गये हैं वह अर्जुन की इसी भ्रान्त धारणा को ही लेके, और उसे ही कृष्ण ने
दूर किया है।
इससे एक और भी गड़बड़ हो जाती है। ऐसी धारणा के करते धर्म और अधर्म अजीब सी
चीज बन जाते हैं। क्षत्रिय के लिए युद्ध जैसा महान् धर्म भी अधर्म की कोटि
में-उसी श्रेणी में-आ जाता है। यह कितनी गलत बात है! ऐसा समझना कि जो
निर्दोष हो, हिंसारहित हो वही धर्म और शेष अधर्म है, कितनी नादानी है! साँस
लेने एवं पलक मारने में भी तो लक्ष-लक्ष कीटाणुओं का संहार होता रहता ही
है। पुराने लोगों ने भी कहा ही है कि वायुमण्डल में ऐसे अनन्त जीव भरे पड़े
हैं जिनका संहार पलक मारने से ही हो जाता है-''पक्ष्मणोऽपि विपातेन येषां
स्यात्पर्वसंक्षय:।'' जब यही बात है तो फिर साँस का क्या कहना? वह तो बराबर
चलती और गर्मागर्म रहती है। फलत: कत्लेआम ही होता रहता है उसके चलते भी! तो
क्या किया जाय? क्या पलक न मारें? साँस न लें? क्योंकि अधर्म जो हो जायगा!
और जब इस प्रकार जीवन ही अधर्म हो गया तो आगे क्या कहा जाय?
धर्मशास्त्रियों ने जिस जीवनरक्षा के लिए सब कुछ कर डालने और खा-पी लेने तक
की छूट दे दी है वही अधर्म? और पूजा-पाठ? माला जपो, जबान हिलाओ, चन्दन
रगड़ो, फूल तोड़ो, आरती करो, दीप जलाओ, भोग लगाओ और पद-पद पर अनन्त निर्दोष
जीवों का संहार करो। फिर भी यह कहना कि यह पूजा-पाठ धर्म है, महज नादानी
है,यदि धर्म की वही परिभाषा मानी जाय जो अर्जुन के दिमाग में थी। तब तो
कहीं भीकिसी प्रकार गुजर नहीं और धर्म महाराज यहाँ से सदा के लिए विदाई ही
लेके चले जायँ!
इसीलिए तो कृष्ण को कसके सुनाना पड़ा कि यह तो तुम्हारी अजीब पण्डिताई
है-''प्रज्ञावादांश्च भाषसे'' (2।11)। धर्म की यह परिभाषा तो जहन्नुम में
भेजे जाने की चीज है, उनने ऐसा समझ के ही अध्या2त्म विवेचन से ही शुरू किया
और अर्जुन को ललकारा। अर्जुन की गलती भी इसमें क्या कही जाय? जब धर्म-अधर्म
के बारे में इसी प्रकार की मोटी बातें कही और लिखी जाती हैं और धर्म पालन
के साथ ही 'अहिंसा परमोधर्म:' की दुहाई दी जाती है, तो उसका ऐसे मौके पर
घपले में पड़ जाना अनिवार्य था। दरअसल कर्म का असली रूप और उसका दार्शनिक
विश्लेषण न जानने के कारण ही तो धर्म-अधर्म और हिंसा-अहिंसा का यह घपला आ
खड़ा होता है। इसलिए जरूरी हो गया कि वही विश्लेषण किया जाय। गीता ने यही
किया भी। इससे तो साफ हो जाता है कि धर्म-अधर्म की सर्वसाधारण धारणा निहायत
ही थोथी और ऐन मौके पर खतरनाक हो जाती है। अर्जुन को जो धोखा हुआ वह उसी के
चलते। इसलिए आमतौर से जिसे लोग धर्म या अधर्म मानते हैं वह बच्चों की-सी
बात हो जाती है। गीता ने यह बात दिखला दी है। वह धर्म ही क्या जिसके या
जिसकी सर्वसाधारण समझ के चलते ऐन मौके पर, जब कि जीवन-मरण का संग्राम
उपस्थित है, गड़बड़घोटाला हो जाय? धर्म को उस समय ठीक पथ-प्रदर्शन करना
चाहिए। मगर वह तो उल्टीम गंगा बहाने लगता है! इसलिए धर्मशास्त्रियों की
बातों को ताक पर रख के उसका नये सिरे से विवेचन और विश्लेषण जरूरी हो जाता
है। यही जरूरत शुरू में ही बड़ी खूबी के साथ दिखा के गीता ने उसका नया
विवेचन कर्म के ही दार्शनिक विश्लेषण (Philosophical analysis) के आधार पर
किया है। क्योंकि इसके बिना दूसरा रास्ता हुई नहीं।
यह भी तो देखिये कि जहाँ गीता में शुरू से लेकर अन्त तक का कर्म का उल्लेख
सैकड़ों बार कर्म शब्द से करने के अलावे कार्य, कर्तव्य, युद्ध, यज्ञ, यत्न,
योग आदि शब्दों से किया है, तहाँ धर्म शब्द मुश्किल से किसी न किसी रूप
में-अधर्म, धार्म्य, साधार्म्य के रूप में भी-सिर्फ तैंतीस बार आया है।
खूबी तो यह है कि गीता के पहले श्लोक का धर्म तो नाम के साथ ही लगा है। वह
कोई धर्म जैसी चीज को खास तौर से कहने के लिए नहीं आया है। कुरुक्षेत्र की
प्रसिद्धि धर्मक्षेत्र के नाम से उस समय थी और यही बात श्लोक में भी आ गयी!
अठारहवें अध्याय के 70वें श्लोक में जो 'धार्म्य' शब्द है वह भी कुछ ऐसा ही
है। वह तो केवल 'संवाद' का विशेषण होने से उसके औचित्य को ही बताता है।
उसका कोई खास प्रयोजन नहीं है। चौदहवें अध्याय के दूसरे श्लोक के
'साधार्म्य' का धर्म शब्द भी दूसरे ही मानी में बोला गया है, न कि कर्तव्य
के अर्थ में। वह तो समानता का ही सूचक है। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक का
धर्म शब्द भी गीता के योग के ही अर्थ में आया है, न कि धर्मशास्त्रों के
धर्म के मानो में। इसी प्रकार नौवें अध्याय के 2-3 श्लोकों में जो धार्म्य
और धर्म शब्द आये हैं वह ज्ञान-विज्ञान के ही लिए आये हैं, न कि अपने खास
मानी में। बारहवें के 20वें श्लोक का धार्म्य शब्द भी कुछ ऐसा ही है। वह
समस्त अध्यानय के प्रतिपादित विषय को ही कहता है। इसी प्रकार अठारहवें
अध्याय के 46वें श्लोक में जो धर्म शब्द है उसी के अर्थ में उसी श्लोक में
आगे कर्म शब्द आने के कारण वह भी संकुचित अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है।
उसी अध्याय के 66वें श्लोक का धर्म शब्द भी व्यापक अर्थ में ही आया है और
धर्म, अधर्म तथा दूसरे कर्मों का भी वाचक है। यह बात प्रसंगवश आगे कही
जायगी और इस पर विशेष प्रकाश पड़ेगा। यह ठीक है कि उस धर्म को कर्म की जगह
पर प्रयोग नहीं किया है। क्योंकि ऐसा करना असम्भव था। कहने का आशय यह है कि
जितना व्यापक अर्थ कर्म शब्द का है उस अर्थ में वह धर्म शब्द नहीं आया है
और इसकी वजह है जो प्रसंगवश लिखी जायगी।
इस प्रकार देखने से पता चलता है कि पाँच से लेकर सत्रह अध्याय तक कुल तेरह
अध्याय में यह धर्म आया ही नहीं है। हालाँकि इन्हीं में कर्म का दार्शनिक
विवेचन खूब ही हुआ है। जिस समत्वरूप योग का वर्णन दूसरे अध्याहय में पाया
जाता है और जो कर्मों की कुंजी है वही पाँच, छह, नौ, बारह, तेरह और चौदह
अधयायों में किसी न किसी रूप में आया ही है। सोलह और सत्रह अध्या,य तो
गीताधर्म की दृष्टि से काफी महत्तव रखते हैं, यह पहले कही चुके हैं और
विस्तार के साथ वह बात सिद्ध की जा चुकी भी है।
अब रहे सिर्फ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और अठारहवें अध्यासय। इन्हीं में
धर्म शब्द कुल मिला के केवल चौबीस बार अपने विशेष मानी में प्रयुक्त हुआ
मालूम पड़ता है। इसमें भी खूबी यह है कि पहले अध्याय के 40वें में तीन बार
और तीसरे के 35वें में ही चार बार आया है। पहले के तैंतालीसवें में, दूसरे
के बत्ती स-तैंतीस में, चौथे के सातवें में और अठारहवें के एकतीस-बत्तींस
श्लोकों में दो-दो बार आ जाने के कारण कुल उन्नीस बार तो सिर्फ आठ ही
श्लोकों में आया है। शेष 5वें श्लोकों में 5 बार। इनमें भी पहले अध्याय के
41 तथा 44वें, दूसरे के 7वें में, चौथे के 8वें में और अठारहवें के 34वें
में-इस प्रकार एक-एक बार का बँटवारा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछी
जगहों में वह पाया जाता है। इसमें भी खूबी यह है कि पहले अध्याटय में सात
बार और दूसरे में एक-कुल आठ-बार तो खुद अर्जुन ने ही यह शब्द कहा है। फलत:
वह तो गीता के सिद्धान्त के भीतर यों ही नहीं आता है। हाँ, सत्रह बार जो
कृष्ण ने कहा है उसी पर कुछ भरोसा कर सकते हैं।
मजा तो यह है कि दूसरे अध्याय के 31वें तथा 33वें श्लोकों में जो कुल चार
बार धर्म शब्द कृष्ण ने कहा है वह अर्जुन के ही कथनानुसार धर्मशास्त्रवाला
ही है, न कि कृष्ण का खास। वहाँ तो अर्जुन की ही बात के अनुसार ही उसे
माकूल करते हैं। इसी प्रकार तीसरे अध्याय के 35वें में जो चार बार आया है
वह ठीक वैसा ही है जैसा कि अठारहवें अध्याय के 47वें का। क्योंकि
'श्रेयान्स्वधार्मो विगुण: परधार्मात्स्वनुष्ठितात्' यह श्लोक का आधा ज्यों
का त्यों दोनों ही जगह पूर्वार्ध्द में आया है। फलत: यदि अठारहवें अध्याय
में धर्म का अर्थ कर्म ही है, तो तीसरे में भी यही बात है-होनी चाहिए। यह
भी बात है कि तीसरे अध्यायय के शुरू से लेकर इस श्लोक के पूर्व तक कर्म की
ही बात लगातार आयी है। उसकी ऋंखला टूटी नहीं है। इसलिए धर्म शब्द भी कर्म
के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यही मानना उचितहै।
इस प्रकार देखने पर तो सिर्फ चौथे अध्याय के 7-8 तथा अठारहवें के 31-32 एवं
34 श्लोकों में जो धर्म शब्द कृष्ण के मुख से निकले हैं केवल वही, मालूम
पड़ता है, धर्म के विशेष या पारिभाषिक अर्थ में आये हैं। मगर यहाँ भी कुछ
बातें विचारणीय हैं। चौथे अध्यामय में तो धर्म का उल्लेख अवतार के ही
प्रसंग में हुआ है। वहाँ कहा गया है कि जब समाज में उपद्रव होने लगता है और
दुष्टों की वृद्धि हो जाती है तो अवतारों की जरूरत होती है। ताकि भले लोगों
की, सत्पुरुषों की रक्षा हो सके। अब यदि इस वर्णन की मिलान सोलहवें अध्यातय
के असुरों के आचरणों से करें और तुलसीदास के 'जब जब होइ धर्म की हानी।
बाढ़हिं असुर महा अभिमानी' वचन को भी इस सिलसिले में खयाल करें, तो पता लग
जाता है कि धर्म का मतलब यहाँ समाज-हितकारी समस्त आचरणों से ही है। जिन
कामों से समाज का मंगल हो वही धर्म है, ऐसा ही अभिप्राय कृष्ण का प्रतीत
होता है।
बेशक, सिर्फ अठारहवें अध्यायय के 31-32 तथा 34 श्लोकों में यह बात जरूर
मालूम होती है कि सामान्य कर्तव्य-अकर्तव्य से अलग धर्म-अधर्म हैं। 30वें
श्लोक में प्रवृत्ति-निवृत्ति शब्दों से इन्हीं धर्म और अधर्म को कहा है।
इसके सिवाय जिस प्रकार वहाँ कार्याकार्य-कार्य-अकार्य-अलग बताया गया है, न
कि इन्हें धर्म-अधर्म- प्रवृत्ति-निवृत्ति-के ही भीतर ले लिया है, ठीक उसी
प्रकार 31वें में भी अधर्म और धर्म तथा अकार्य एवं कार्य जुदा-जुदा लिखा
है। इससे साफ हो जाता है कि सामान्य कार्य और अकार्य से अलग ही धर्म एवं
अधर्म हैं-ये विशेष पदार्थ हैं । मगर जब 32वें श्लोक पर विशेष ध्याोन देते
हैं तो यह पहेली सुलझ जाती है और पता चल जाता है कि धर्म-अधर्म शब्द भी
व्यापक अर्थ में ही आये हैं। पहले-31वें-श्लोक में आम लोगों की धारणा के ही
अनुसार इन्हें अलग रखा है जरूर। मगर यह बात विवरण के ही रूप में है, यह
मानना ही पड़ेगा।
बात असल यह है कि सात्तिवक, राजस और तामस बुद्धियों की पहचान इन तीन-30 से
32-श्लोकों में बताई गयी है। पहले में कहा गया है कि प्रवृत्ति-निवृत्ति या
धर्म-अधर्म तथा कर्तव्य-अकर्तव्य को ठीक-ठीक बताना सात्तिवक बुद्धि का काम
है। इसी से उसकी पहचान होती है। फिर भी 31वें में कहा गया है कि इन चीजों
को जो ठीक-ठीक न बताये-कभी ठीक बताये और कभी नहीं-वही राजस बुद्धि है। उसकी
यही पहचान है। यहाँ तक तो ठीक है। दोनों की पहचान में धर्म (प्रवृत्ति),
अधर्म (निवृत्ति) तथा कार्य-अकार्य का उल्लेख आया है। मगर जब तामस बुद्धि
का प्रसंग 32वें श्लोक में आया है तो कार्य-अकार्य को छोड़के केवल धर्म और
अधर्म का ही उल्लेख है और कहा गया है कि जो अधर्म को ही धर्म माने और इस
प्रकार सभी बातें उल्टीा ही बताये वही तामसी बुद्धि है। यदि पहला क्रम रखते
तो कहते कि जो अधर्म को धर्म और अकार्य को कार्य समझे वही तामसी बुद्धि है।
क्योंकि उसका काम न तो ठीक-ठीक बताना है और न कुछ गड़बड़ करना, किन्तु बिलकुल
ही उल्टा बताना। मगर यहाँ कार्य-अकार्य को छोड़ के केवल धर्म-अधर्म का ही
उल्लेख यही बताता है कि इन्हीं के भीतर कार्य-अकार्य भी आ जाते हैं और ये
शब्द व्यापक अर्थ में ही आये हैं। फलत: कार्य-अकार्य का पहले दो श्लोकों
में उल्लेख यों ही विवरण के ही रूप में है। 34वें श्लोक का धर्म शब्द तो
प्रचलित प्रणाली के ही अनुसार धर्म, अर्थ, काम में एक को कहता है और जब
पहले ही उसका अर्थ ठीक हो गया तो यहाँ दूसरा क्या होगा?
इस प्रकार यह बात निर्विवाद हो गयी कि गीता ने धर्म को कर्म, काम या अमल से
भिन्न नहीं मान के दोनों को एक ही माना है-धर्म ही कर्म है और कर्म ही
धर्म। अर्जुन ने जो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि ''धर्म के
बारे में कोई भी निश्चय न कर सकने के कारण ही आपसे सवाल कर रहा
हूँ''-''पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेता:'', उसका भी मतलब कर्तव्य, कर्म या
काम से ही है। इसीलिए तो उसे जो उत्तर दिया गया है उसमें कर्म के ही स्वरूप
और उसके सभी पहलुओं का विवेचन किया गया है। यही तो खूबी है कि शुरू से लेकर
अन्त तक जो भी विवेचन किया गया है वह कर्म का ही है, न कि धर्म का। एक भी
स्थान पर धर्म का उल्लेख करके विश्लेषण या विवेचन पाया जाता है नहीं।
अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहना शुरू हुआ है वह भी मरने-मारने
और युद्ध करने की ही बात लेके। इन्हीं बातों को धर्म कहके शुरू करते तो भी
एक बात थी। मगर वहाँ तो सीधे कौन मारता है, कौन मरता है आदि प्रश्न ही
उठाये गये हैं और उन्हीं का उत्तर दिया गया है। युद्ध करो, तैयार हो जाओ,
लड़ने का निश्चय कर लो, आदि के ही रूप में बार-बार उपसंहार किया गया है, न
कि धर्म करो, ये धर्म हैं, इसलिए इन्हें करो, आदि के रूप में। खूबी तो यह
है कि यह सभी बातें स्वतन्त्र रूप से कहके आगे 31-33 श्लोकों में यह भी बात
कहते हैं कि धर्मबुद्धि से भी यही काम कर सकते हो-यह युद्ध और मरने-मारने
का काम धर्म समझ के भी करना ही होगा। इससे तो साफ है कि पहले धर्म समझ के
इन्हें करने पर जोर नहीं देके कर्तव्यबुद्धि या विवेकबुद्धि से ही इन्हें
करने को कहा गया है।
इस प्रकार सभी कामों को धर्म के भीतर डाल देने का मतलब यह हो जाता है कि
धर्म बहुत बड़ा एवं व्यापक बन जाता है और उसका सर्वजनप्रसिद्ध संकुचित रूप
जाता रहता है। फलत: लोगों में जो धर्माचरण की प्रवृत्ति आमतौर से पायी जाती
है उससे काफी फायदा उठाके सभी समाजोपयोगी कामों को उसी व्यापक एवं उदार
बुद्धि से धर्म समझ के ही कराया जा सकता है। गीता के इस ढंग से कर्तव्य के
संसार में बहुत बड़ा लाभ हो जाता है।
मगर दूसरा और असली महत्तवपूर्ण लाभ इससे यह होता है कि धर्म के नाम पर
धर्मशास्त्रों, धर्मशास्त्रियों तथा धर्माचार्यों का जो नाहक का नियन्त्रण
लोगों की समझ और उनके कामों पर रहा करता है वह खत्म हो जाता है। जब धर्म
अत्यन्त व्यापक बन जाता है, जब सभी काम उसमें आ जाते हैं तब धर्म के
ठेकेदारों की गुंजाइश रही कहाँ जाती है? जब तक कोई खास चीज और कुछ
चुनी-चुनाई बातें न हों तब तक उन्हें पूछे कौन? जीवन के हरेक काम में कौन
किससे पूछने जाता है? किस धर्माचार्य की जरूरत इस बात के लिए होती है कि हम
कैसे आगे-पीछे पाँव दें, कैसे साँस लें, कैसे खाने में मुँह चलायें, कैसे
दाँतों से अन्न को खूब चबायें, कैसे कपड़े पहनें, आदि-आदि? ये बातें पूछना
असम्भव भी तो है। हाँ, स्वास्थ्यशास्त्रों और ऐसी ही दूसरी पोथियों की
सहायता से इन्हें भले ही जान ले सकते हैं। मगर ऐसा तो नहीं होगा कि साल में
एक या दो-चार गुरु और पीर या पण्डित-पुरोहित इन्हीं के लिए खास तौर से आया
करेंगे और 'पूजा' लिया करेंगे, ठीक जैसे एकादशी, रोजा आदि के सिलसिले में
आते ही रहते हैं। तब तो रोजा, नमाज, सन्ध्याा, पूजा वगैरह भी साँस लेने आदि
की ही श्रेणी में आ जायँगे और वहाँ से भी धर्मध्वगजियों की बेदखली होई
जायगी, चाहे देर से हो या सवेरे।
तीसरी बात यह होगी कि जब हरेक बात को धर्म के फन्दे से निकाल के व्यावहारिक
और सामाजिक दुनिया में ला देंगे तो उसके भले-बुरे पर जाँच स्वर्ग और नर्क
की दृष्टि से न करके देखेंगे कि इससे अपना और समाज का भौतिक लाभ क्या है,
इससे सामाजिक, वैज्ञानिक या सांस्कृतिक विकास में कहाँ तक फायदा पहुँचता
है, समाज के स्वास्थ्य की उन्नति इससे कहाँ तक होती है। बिना इस व्यावहारिक
दृष्टि के ही तो सब गुड़ गोबर हो रहा है। नहाने में भी जब धर्म की बात घुसती
है तो उससे शरीर या वस्त्रदि की स्वच्छता न देखके स्वर्ग-नर्क को ही देखने
लगते हैं! जैसे ऊँट की नजर हमेशा पश्चिम के रेगिस्तान की तरफ होती है, ऐसा
कहा जाता है, ठीक उसी तरह हमें हर काम में ठेठ स्वर्ग, बैकुण्ठ या नर्क ही
सूझता है। इस पतन का कोई ठिकाना है! इस अन्धीा धर्मबुद्धि ने हमें-मानव
समाज को-निरा भोंदू और बुद्धिहीन बना डाला है, मशीन करार दे दिया है! गीता
का यह रास्ता इस बला से हमारा निस्तार कर देता है और हमें आदमी बना देता
है।
चौथी और आखिरी बात यह होती है कि कर्म भले हैं या बुरे, इनके करते हम नर्क
में जायेंगे या स्वर्ग में आदि बातों और प्रश्नों का भी निर्णय जो अब तक
पण्डितों एवं मौलवी लोगों के हाथों में रहा है उसे गीता इस प्रकार उनसे छीन
लेती और इन्हें ऐसी कसौटी पर कसती है जो सर्वत्र सुलभ हो, जिसे हम खुद
हासिल कर सकते हैं, यदि चाहें। अब तक तो धर्म के नाम पर फैसला करने वाले
पण्डित आदि ही थे। मगर अब जब धर्म हो गया कर्म और कर्म के जाँचने की एक
दूसरी ही कसौटी गीता ने तैयार कर दी, जो दूसरे के पास न होके हरेक आदमी के
पास अपनी-अपनी अलग होती है, तो फिर पण्डितों और मौलवियों को कौन पूछे ? यह
भी नहीं कि दूसरे की कसौटी-गैर की तराजू-दूसरे के काम आए। यहाँ तो
अपनी-अपनी ही बात है। यहाँ ''अपनी-अपनी डफली, अपनी-अपनी गीत'' है। फलत:
परमुखापेक्षिता के लिए स्थान रही नहीं जाता। सोलह आना स्वावलम्बन ही उसकी
जगह ले लेता है। तब धर्म के नाम पर झमेले और झगड़े भी क्यों होंगे?
(शीर्ष पर वापस)
गीता का साम्यवाद
गीता में समता या साम्यवाद की भी बात है और
उसे लेके बहुत लोग मार्क्सवादी साम्यवाद को खरी-खोटी सुनाने लगते हैं। उनके
जानते मार्क्स का साम्यवाद भौतिक होने के कारण हलके दर्जे का है, तुच्छ है
गीता के आध्या त्मिक साम्यवाद के मुकाबिले में। वह तो यह भी कहते हैं कि
हमारा देश धर्मप्रधान एवं धर्मप्राण होने के कारण भौतिक साम्यवाद के निकट
भी न जायगा। यह तो आध्या त्मिक साम्यवाद को ही पसन्द करेगा। असल में इस युग
में जो साम्यवाद की हवा बह निकली है उसी से घबरा के यह बातें उसी के जवाब
में कही जाती हैं। उस तरह की दूसरी चीज न रहने पर तो लोग खामख्वाह उधर ही
झुकेंगे। इसीलिए गीता की यह बात लोगों के सामने ला खड़ी कर दी जाती है, ताकि
स्वभावत: लोग इधर ही आकृष्ट हों और दूसरे साम्यवाद का खतरा न रह जाय। खूबी
तो यह है कि जिन्हें अध्यात्मवाद से लाख कोस दूर रहना है वह भी गीता की यही
बात रटते फिरते हैं! उनके स्थायी स्वार्थों को भौतिक साम्यवाद से बहुत बड़ा
खतरा होने के कारण ही वे गीता का नाम लेके टट्टी की ओट से शिकार खेलते हैं।
हर हालत में इस चीज पर प्रकाश डालना जरूरी है।
असल में गीता में प्राय: बीस जगह या तो सम शब्द का प्रयोग मिलता है या उसी
के मानी में तुल्य जैसे शब्द का प्रयोग। दूसरे अध्यायय के 38वें तथा 48वें,
चौथे के 22वें, पाँचवें के 18-19वें, छठे के 8, 9, 13, 29, 32, 33वें, नवें
के 29वें, बारहवें के 13, 18वें, तेरहवें के 9, 27, 28वें, चौदहवें के
24वें तथा अठारहवें के 54वें श्लोकों में सम, समत्व या साम्य शब्द आया है।
किसी-किसी श्लोक में दो बार भी आया है। चौदहवें के 24वें श्लोक में सम के
साथ ही तुल्य शब्द भी आया है और 25वें में सिर्फ तुल्य शब्द ही दो बार
मिलता है। इनमें केवल छठे के 13वें श्लोक वाला सम शब्द 'सीधा' (Straight)
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए उसका साम्यवाद से कोई भी ताल्लुक नहीं
है। शेष सम शब्दों या उन्हीं के अर्थ में प्रयुक्त तुल्य शब्दों का
साम्यवाद से सम्बन्ध जरूर जुट जाता है। यदि असक्त, अनासक्त, परित्यागी या
परित्याग आदि शब्दों को, जो सम के ही अर्थ में-उसी अभिप्राय से ही-प्रयुक्त
हुए हैं, भी इसी सिलसिले में गिन लें; तब तो गीता के अंग-प्रत्यंग में यह
बात पायी जाती है, यही मानना पड़ेगा। कर्म के विश्लेषण और इस समत्व या
साम्यवाद का ऐसा सम्बन्ध है कि दोनों एक दूसरे के बिना रही नहीं सकते।
अब देखना है कि गीता की यह समता, उसका यह समत्व, समदर्शन या साम्यवाद है
क्या चीज। जब तक उसकी असलियत और रूपरेखा का ही पता हमें न हो उसकी तुलना
भौतिक साम्यवाद के साथ कर कैसे सकते हैं? तब तक हमें यह भी कैसे पता लग
सकता है कि कौन भला, कौन बुरा है? यदि भला या बुरा है तो भी किस दृष्टि से,
यह भी तो तभी जान सकते हैं। हरेक चीज हर दृष्टि से तो कभी भी अच्छी या बुरी
होती नहीं। आखिर पदार्थों के पहलू तो होते ही हैं और उन्हें हर पहलू से
अलग-अलग देखना जरूरी हो जाता है, यदि किसी और के साथ मिलान या तुलना करना
हो। यही कारण है कि गीता के समदर्शन या साम्यवाद के हर पहलू पर प्रकाश
डालना और विचार करना आवश्यक है।
जैसा कि पहले भी कहा गया है, गीता का साम्यवाद, समदर्शन, समत्वबुद्धि या
साम्ययोग तो दिल-दिमाग की ही दशा विशेष है। दरअसल यूरोप में हीगेल आदि
दार्शनिकों ने जिस विचारवाद या आइडियलिज्म को प्रश्रय दिया और उसका समर्थन
किया है वह बहुत कुछ गीता के समदर्शन से मिलता-जुलता है। यह भी नहीं कि यह
कोरी मानसिक अवस्था विशेष है जिसे ज्ञान की एक विलक्षण कोटि या दशा कह सकते
हैं। निस्सन्देह पाँचवें अध्याय के 18-19-दो-श्लोकों में जो कुछ कहा है वह
तो दर्शन या ज्ञानात्मक ही है। क्योंकि वहाँ साफ ही लिखा है कि पंडित लोग
समदर्शी होते या सम नाम की चीज को ही देखते हैं, 'पण्डिता: समदर्शिन:',
'साम्ये स्थितं मन:।' छठे अध्याय के 8-9 श्लोकों में भी
'समलोष्ठाश्मकांचन:', 'समबुद्धिर्विशिष्यते' के द्वारा कुछ ऐसा ही कहा है।
हालाँकि 'समलोष्ठाश्मकांचन:' का व्यापक भाव माना जाता है जो आगे बताया
जायगा। यही बात उस अध्याय के 32-33 श्लोकों में भी है। क्योंकि 32वें में
'समं पश्यति' लिखा गया है और उसी का उल्लेख 33वें में है। यद्यपि तेरहवें
अध्याय के 9वें श्लोक में यह बात इतनी स्पष्ट नहीं है और उसका दूसरा आशय भी
संभव है; तथापि 27-28 दो श्लोकों में 'पश्यति' एवं 'पश्यन्' शब्दों के
द्वारा उसे ज्ञान ही बताया है। बस।
(शीर्ष पर वापस)
नकाब और नकाबपोश
इसका आशय यह है कि जिस तरह स्वाँग बनानेवाले
की बाहरी वेशभूषा के रहते हुए भी समझदार आदमी उससे धोखे में नहीं पड़ता है;
किन्तु असली आदमी को पहचानता और देखता रहता है; ठीक यही बात यहाँ भी है।
संसार के पदार्थों का जो बाहरी रूप नजर आता है उसे विवेकी या गीता का योगी
एकमात्र नट,र् नत्ताक या स्वाँग बनानेवाले की बाहरी वेशभूषा ही मानता है।
इसलिए इन सभी बाहरी आकारों के भीतर या पीछे किसी ऐसी अखण्ड, एकरस,
निर्विकार-सम-वस्तु को देखता है जो उसकी अपनी आत्मा या ब्रह्म ही है। उसे
समस्त दृश्य भौतिक संसार उसी आत्मा या ब्रह्म की नटलीला मात्र ही बराबर
दीखता है। वह तो इस नटलीला की ओर भी दृष्टि न करके उसी सम या एक रस पदार्थ
को ही देखता है वह जो बाहरी पर्दा या नकाब है उसे वह उतार फेंकता है और
पर्दानशीन या नकाबपोश को हू-ब-हू देखता रहता है।
नरसी मेहता एक ज्ञानी भक्त हो गये हैं। उनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहते
हैं कि वह एक बार कहीं से आटा और घी माँग लाये। फिर घी को अलग किसी पात्र
में रख के कुछ दूर पानी के पास आटा गूँधा के रोटी पकाने लगे। जब रोटी तैयार
हो गयी तो सोचा कि घी लगा के भगवान् को भोग लगाऊँ और यज्ञशिष्ट या प्रसाद
स्वयं ग्रहण करूँ। बेशक, आजकल के नकली भक्तों की तरह ठाकुरजी की मूर्ति तो
वह साथ में बाँधो फिरते न थे। वे थे तो बहुत पहुँचे हुए मस्तराम। उनके
भगवान् तो सभी जगह मौजूद थे। खैर, उनने रोटियाँ रख के घी की ओर पाँव बढ़ाया
और उसे लेके जो उल्टेस पाँव लौटे तो देखा के एक कुत्ता रोटियाँ लिए भागा जा
रहा है! फिर क्या था? कुत्तो के पीछे दौड़ पड़े। कुत्ता भागा जा रहा है
बेतहाशा और नरसी उसके पीछे-पीछे हाथ में घी लिए आरजूमिन्नत करते हुए
हाँफते-हाँफते दौड़े जा रहे हैं कि महाराज रूखी रोटियाँ गले में अटकेंगी।
जरा घी तो लगा देने दीजिए! मुझे क्या मालूम कि आप इतने भूखे हैं कि घी
लगाने भर की इंतजार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि मुझे ऐसा पता होता तो और
सवेरे ही रोटियाँ बना लेता! अपराधा क्षमा हो! अब आगे ऐसी गलती न होगी!
कृपया रुक जाइये, आदि-आदि। बहुत दौड़-धूप के बाद तब कहीं कुत्ता रुका और
नरसी ने भगवान् के चरण पकड़े!
नरसी को तो असल में कुत्ता नजर आता न था। कुत्तो की शकल तो बाहरी नकाब थी,
ऊपरी पर्दा था। वह तो नकाब को फाड़ के उसके भीतर अपने भगवान् को ही देखते
थे। उनकी ऑंखें तो दूसरी चीज देख पाती न थीं। उनके लिए सर्वत्र सम ही सम
था, सर्वत्र उनकी आत्मा ही आत्मा थी, ब्रह्म ही ब्रह्म था। नटलीला का पर्दा
वह भूल चुके थे-देखते ही न थे। यदि किसी वैज्ञानिक के सामने पानी लाइये तो
वह उसमें और ही कुछ देखता है। उसकी दूरदर्शी एवं भीतर घुसनेवाली-पर्दा फाड़
डालनेवाली ऑंखें उसमें सिवाय ऑक्सिजन और हाइड्रोजन (Oxygen and Hydrogen)
नामक दो हवाओं की खास मात्रओं के और कुछ नहीं देखती हैं, हालाँकि
सर्वसाधारण की नजरों में वह सिर्फ पानी है, दूसरा कुछ नहीं। वैज्ञानिक की
भी स्थूल दृष्टि पानी देखती है, यदि उसे वह मौका दे। नहीं तो वह भी देख
नहीं पाती। मगर सूक्ष्म दृष्टि-और वही यथार्थ दृष्टि है-तो उस दृश्य जल को
न देख अदृश्य वायुवों को ही देखती है। यही दशा नरसी की थी। यही दशा गीता के
योगी या समदर्शी की भी समझिये।
यदि नौ मन बालू के भीतर दो-चार दाने चीनी के मिला दिये जायँ तो हमारी तेज
से तेज ऑंखें भी उनका पता लगा न सकेंगी, चाहे हम हजार कोशिश करें। मगर
चींटी? वह तो खामख्वाह ढूँढ़-ढाँढ़ के उन दानों तक पहुँची जायगी। उसे कोई रोक
नहीं सकता। समदर्शी भक्तों की भी यही दशा होती है। जिस प्रकार चींटी की लगन
तथा नाक तेज और सच्ची होने के कारण ही वह चीनी के दानों तक अवश्य पहुँचती
और उनसे जा मिलती है; बालू का समूह जो उन दानों और चींटी के बीच में पड़ा है
उसका कुछ कर नहीं सकता; ठीक वही बात ज्ञानी एवं समदर्शी प्रेमीजनों की होती
है। उनके और भगवान् के बीच में खड़े ये स्थूल पदार्थ हर्गिज उन्हें रोक नहीं
सकते। शायद किसी विशेष ढंग का एक्सरे (X-ray) या खुर्दबीन उन्हें प्राप्त
हो जाता है। फिर तो शत्रु-मित्र, मिट्टी-पत्थर, सोना, सुख-दु:ख, मानापमान
आदि सभी चीजों के भीतर उन्हें केवल सम ही सम नजर आता है। पर्दा हट जो गया,
नकाब फट जो गयी है। यही है गीता के साम्यवाद के समदर्शन का पहलू और यही है
उस ज्ञान की दशाविशेष।
(शीर्ष पर वापस)
रस का त्याग
मगर यह तो एक पहलू हुआ। मन या बुद्धि का पदार्थों के साथ सम्बन्ध होने पर
भी उनके बाहरी या भौतिक आकार एवं रूप की छाप उन पर लगने न पाये और ये इन
पदार्थों के इन दृश्य आकारों एवं रूपों से अछूते रह जायँ, यह तो समदर्शन या
गीता के साम्यवाद का केवल एक पहलू हुआ। उसका दूसरा पहलू तो अभी बाकी ही है
और गीता ने उस पर काफी जोर दिया है। वही तो आखिरी और असली चीज है। इस पहले
पहलू का वही तो नतीजा है और यदि वही न हो तो अन्ततोगत्वा यह एक प्रकार से
या तो बेकार हो जाता है या परिश्रम के द्वारा उस दूसरे को सम्पादन करने में
प्रेरक एवं सहायक होता है। यही कारण है कि गीता में पहले की अपेक्षा उसी पर
अधिक ध्या न दिया गया है।
बात यों होती है कि मन का भौतिक पदार्थों से संसर्ग होते ही उनकी मुहर उस
पर लग जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फोटोग्राफी में फोटोवाली पटरी या
शीशे पर सामने वाले पदार्थों की। सहसा देखने से यह पता नहीं चलता कि सचमुच
उस शीशे पर सामने की वस्तु की छाप लगी है; हालाँकि वह होती है जरूर। इसीलिए
तो उसे स्पष्ट करने के लिए पीछे यत्न करना पड़ता है। मन या बुद्धि पर भी लगी
हुई पदार्थों की छाप प्रतीत नहीं होती। क्योंकि वे तो अदृश्य हैं-अत्यन्त
सूक्ष्म हैं। मन या बुद्धि को देख तो सकते नहीं। उनका काम है पदार्थों की
छाप या प्रतिबिम्ब लेके बाहर का अपना काम खत्म कर देना और भीतर लौट आना।
मगर भीतर आने पर ही तो गड़बड़ पैदा होती है। मन ने बाहर जाके पदार्थों को
प्रकट कर दिया-जो चीजें अज्ञान के अन्धाकार में पड़ी थीं उन्हें ज्ञान के
प्रकाश में ला दिया। अब उन चीजों की बारी आयी। उनकी छाप के साथ जब मनीराम
(मन) भीतर घुसे तो उन पदार्थों ने अब अपना तमाशा और करिश्मा दिखाना शुरू
किया। जहाँ पहले भीतर शान्ति सी विराज रही थी, तहाँ अब ऊधाम और
बेचैनी-उथल-पुथल-शुरू हो गयी! मालूम होता है, जैसे बिरनी के छत्तो में किसी
ने कोई चीज घुसेड़ दी और पहले जो वे भीतर चुपचाप पड़ी थीं भनभना के बाहर निकल
आयीं। किसी छूतवाली या संक्रामक बीमारी को लेके जब कोई किसी घर या समाज में
घुसता है तो एक प्रकार का आतंक छा जाता है, चारों ओर परेशानी छा जाती है और
वह छूत की बीमारी जानें कितनों को तबाह करती है। मन पर अपनी मुहर लगा के जब
भौतिक पदार्थ उसी रूप में मन के साथ भीतर-शरीर में-घुसते हैं तो ठीक
संक्रामक रोग की सी बात हो जाती है और भीतर की शान्ति भंग हो जाती है। वह
मन अंग-प्रत्यंग में अपनी उस छाप का असर डालता है। या यों कहिये कि मन के
द्वारा बाहरी भौतिक पदार्थ ही ऐसा करते हैं। फलत: हृदय या दिल पूर्ण रूप से
प्रभावित हो जाता है। दिल का काम तो खोद-विनोद करना या जानना है नहीं। वह
तो ऊँट की पकड़ पकड़ता है। जब उस पर भौतिक पदार्थों का प्रभाव इस प्रकार हुआ
तो वह उन्हें जैसे का तैसा पकड़ लेता और परेशान होता है। यदि उसमें विवेक
शक्ति होती तो उनसे भाग जाता। मगर सो तो है नहीं, और जिस मन और बुद्धि में
यह शक्ति है उनने तो खुद ही यह काम किया है-बाहरी पदार्थों के भीतर
पहुँचाया है, या कम से कम उनके कीटाणुओं को ही। फिर हो क्या?
पहले भी कहा जा चुका है कि भौतिक पदार्थ खुद कुछ कर नहीं सकते-ये बुरा-भला
कर नहीं सकते, सुख-दु:ख दे नहीं सकते। किन्तु मन में जो उनका रूप बन जाता
है वही सुख-दु:खादि का कारण होता है। इस बात का विशेष रूप से विवरण ऊपर की
पंक्तियों से हो जाता है। जब मन पर भौतिक पदार्थों की छाप पड़ती है तो उसमें
एक खास बात पायी जाती है। पहले भी कहा जा चुका है कि उदासीन या लापरवाह
आदमी को ये पदार्थ बुरे-भले नहीं लगते। क्योंकि उसके मन पर इनकी मुहर लग
पाती नहीं। उनका मन बेलाग जो होता है। जिनके मन में लाग होती है, जिसे लस
बोलते हैं, उन्हीं की यह दशा होती है। इसी लाग को गीता ने रस कहा है
'रसवर्जं रसोऽप्यस्य' (2।59) श्लोक में। राग-द्वेष या काम, क्रोध के नाम से
भी इसी चीज को बार-बार याद किया है। यही लाग या रागद्वेष-रस-सब तूफानों का
मूल है। यदि यह न हो तो सारी बला खत्म हो जाय। गीता ने इस रस को खत्म करने
पर इसीलिए काफी जोर भी दिया है।
अब हालत यह होती है कि भौतिक पदार्थों के इस प्रकार भीतर पहुँचते ही मैं,
मेरा, तू, तेरा, अपना-पराया, शत्रु-मित्र, हित-अहित, अहन्ता-ममता आदि का
जमघट लग जाता है-भीतर इनका बाजार गर्म हो जाता है। जैसे मांस का टुकड़ा
देखते ही, उसकी गन्ध पाते ही गीधा, चील, कौवे आदि रक्तपिपासु पक्षियों की
भीड़ लग जाती है और वे इर्द-गिर्द-मँडराने लगते हैं; ठीक वही बात यहाँ भी हो
जाती है। मैं-तू, मेरा-तेरा, शत्रु-मित्र आदि जो जोड़े हैं-द्वन्द्व हैं-वे
जम के एक प्रकार का आपसी युद्ध-एक तरह की कुश्ती-मचा देते हैं और कोई किसी
की सुनता नहीं। ये द्वन्द्व होते हैं बड़े ही खतरनाक। ये तो फौरन ही आपस में
हाथापाई शुरू कर देते हैं। पहलवानों की कुश्ती में जैसे अखाड़े की धूल उड़
जाती है इनकी कुश्ती में ठीक उसी प्रकार मनुष्य के दिल की दुर्दशा हो जाती
है, एक भी फजीती बाकी नहीं रहती। फिर तो सारे तूफान शुरू होते हैं। इसी के
बाद बाहरी लड़ाई-झगड़े जारी हो जाते हैं, हाय-हाय मच जाती है। बाहर के
झगड़े-झमेले इसी भीतरी कुश्तम-कुश्ता के ही परिणाम हैं। नतीजा यह होता है कि
मनुष्य का जीवन दु:खमय हो जाता है। क्योंकि इन भीतरी कशमकशों का न कभी अन्त
होता है और न बाहरी शान्ति मिलती है। भीतर शान्ति हो तब न बाहर होगी?
गीता के आध्यात्मिक साम्यवाद की आवश्यकता यहीं पर होती है। वह इसी भीतरी
कशमकश और महाभारत को मिटा देता है, ताकि बाहर का भी महायुद्ध अपने आप मिट
जाये। ज्योंही मन बाहरी पदार्थों की छूत भीतर लाये या लाने की कोशिश करे,
त्योंही उसका दरवाजा बन्द कर देना यही उस साम्यवाद का दूसरा पहलू है। इसके
दोई उपाय हैं। या तो मन में भौतिक पदार्थों की छूत लगने पाये ही न, जैसा कि
समदर्शन वाले पहलू के निरूपण के सिलसिले में कहा जा चुका है। तब तो सारी
झंझट ही खत्म हो जाती है। और अगर लगने पाये भी, तो भीतर घुसते ही मन को ऐसी
ऊँची सतह या भूमिका में पहुँचा दें कि वह अकेला पड़ जाय और कुछ करी न सके;
जिस प्रकार छूतवाले को दूर के स्थान में अलग रखते हैं जब तक उसकी छूत मिट न
जाये। मन को ध्या न, धारणा या चिन्तन की ऐसी ऊँची एवं एकान्त अट्टालिका में
चढ़ा देते हैं कि वह और चीजें देख सकता ही नहीं। अगर उसे किसी चीज में फँसा
दें तो दूसरी को देखेगा ही नहीं। उसका तो स्वभाव ही है एक समय एक ही में
फँसना। कहते हैं कि ब्रज में गोपियों को जब ऊधव ने ज्ञान और निराकार भगवान्
के ध्याँन का उपदेश दिया तो उनने चट उत्तर दे दिया कि मन तो एक ही है और वह
चला गया है कृष्ण के साथ। फिर ध्यादन किससे किया जाय? ''इक मन रह्यो सो गयो
स्याम संग कौन भजै जगदीस?'' यही बात यहाँ हो जाती है और सारी बला जाती रहती
है।
(शीर्ष पर वापस)
मस्ती और नशा
दूसरा उपाय मन की मस्ती है, पागलपन है, नशा
है। चौबीसों घण्टे बेहोश बनी रहती है। जिसे प्रेम का प्याला या शौक की शराब
कहा है उसी का नशा दिन-रात बना रहता है। बाहरी संसार का खयाल कभी आता ही
नहीं। असल में तो यह बात होती है हृदय में, दिल में। यह मस्ती मन का काम न
होके दिल की ही चीज है। मन तो बड़ा ही नीच है, लम्पट है। उसे तो किसी चीज
में जबर्दस्ती बाँध रखना होता है। मगर दिल तो गंगा की धारा है, बहता दरिया
है जिसका जल निर्मल है। उसी में यह मस्ती आती है, यह पागलपन होता है, यह
नशा रहता है और वही मन को मजबूर कर देता है कि चुपचाप बैठ जाये, नटखटी या
शैतानियत न करे। इसीलिए इसे मन की भी मस्ती कहा करते हैं। खतरनाक फोड़े के
चीरने-फाड़ने के समय डॉक्टर लोग मनुष्य को क्लोरोफार्म के प्रभाव से बेहोश
कर देते हैं; ताकि उसे चीर-फाड़ का पता ही न चले। उसका मन कहीं जाता
नहीं-किसी चीज में बँधा जाता नहीं। किन्तु निश्चेष्ट और निष्क्रिय हो जाता
है, उसकी सारी हरकतें बन्द हो जाती हैं, जैसे मुर्दा हो गया हो। यही बात
मस्ती की दशा में भी मन की होती है। जब दिल अपने रंग में आता है और प्रेम
के प्याले में लिपट जाता है तो गोया मन को क्लोरोफार्म दे दिया और वह
मुर्दा बन जाता है। फिर तो कुछ भी कर नहीं सकता। दिल की इसी दशा को
साम्यावस्था या साम्ययोग कहते हैं। मन की छूत का ऐसी दशा में न दिल पर असर
होता है और न आगे वाला तूफान चालू होता है। जब डंक का ही असर न हो तो
हायतोबा, चिल्लाहट और रोने-धोने या मरने का सवाल ही कहाँ?
इस दशा में भीतर की शान्ति ज्यों कि त्यों अखण्ड बनी रह जाती है। हृदय की
गम्भीरता (Serenity) नहीं टूटती और कोई खलबली मचने पाती नहीं। जब बाहरी
चीजों का उस पर असर होता ही नहीं तो शान्तिभंग हो कैसे? चट्टान से टकरा के
जैसे लहरें लौट जाती हैं; छिन्न-भिन्न हो जाती हैं, ठीक यही हालत मन के
द्वारा भीतर आनेवाले भौतिक पदार्थों की होती है। वे कुछ कर पाते नहीं। फलत:
अपने-पराये, शत्रु-मित्र, हानि-लाभ, बुरे-भले का द्वन्द्व भीतर हो पाता
नहीं। वहाँ तो सभी चीजें एक सी ही रह जाती हैं। जब उनका असर ही नहीं हो
पाता तो क्या कहा जाय कि कैसी हैं? इसीलिए उन्हें एकसी कहते हैं। वे खुद एक
सी बन तो जाती हैं नहीं। मगर जब उनकी विभिन्नता का, उनके भले-बुरेपन का
अनुभव होता ही नहीं तो, उन्हें समान, सम या तुल्य कहने में हर्ज हुई क्या?
यही बात गीता ने भी कही है। और जब भीतर असर हुआ ही नहीं तो बाहरी महाभारत
की तो जड़ ही कट गयी। वह तो भीतरी घमासान का ही प्रतिबिम्ब होता है न?
दूसरे अध्याय में सुख-दु:खादि परस्पर विरोधी जोड़ों-द्वन्द्वों-को सम करने
की जो बात 'सुखदु:खे समेकृत्वा' (2।38) आदि के जरिये कही गयी है और
'सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा' (2।48) में जो काम के बनने-बिगड़ने में
एकरस-लापरवाह- बने रहने की बात कही गयी है, वह यही मस्ती है। चौथे अध्याय
के 'सम: सिद्धावसिध्दौ च' (22) में भी यही चीज पायी जाती है। छठे के 'लोहा,
पत्थर, सोना को समान समझता है'-'समलोष्ठाश्मकांचन:' (8) का भी यही अभिप्राय
है। नवें में जो यह कहा है कि 'मैं तो सबके लिए समान हूँ, न मेरा शत्रु है
न मित्र'-'समोऽहंसर्वभूतेषु न मे द्वेषयोऽस्ति न प्रिय:' (29) वह भी इसी का
चित्रण है। बारहवें में जो 'अहन्ता-ममता से शून्य, क्षमाशील और सुख-दु:ख
में एकरस'-'निर्ममो निरहंकार: सम-दु:खसुख: क्षमी' (13), कहा है तथा जो
''शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दु:ख में एक सा लापरवाह रहे और
किसी चीज में चिपके नहीं''-''सम: शत्रौ च मित्रो च तथा मानापमानयो:।
शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: संगविवर्जित:'' (18) कहा है, वह इसी चीज का विवरण
है। चौदहवें के 24-25 श्लोकों में 'समदु:खसुख: स्वस्थ:' आदि जो कुछ कहा है
वह भी यही चीज है। यहाँ जो 'स्वस्थ:' कहा है उसका अर्थ है ''अपने आपमें
स्थिर रह जाना।'' यह उसी मस्ती या पागलपन की दशा की ही तरफ इशारा है।
अठारहवें अध्याहय के 54वें श्लोक में भी इसी बात का एक स्वरूप खड़ा कर दिया
है 'ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा' आदि शब्दों के द्वारा। यों तो जगह-जगह यही
बात कही गयी है; हालाँकि सर्वत्र सम शब्द नहीं पाया जाता।
(शीर्ष पर वापस)
ज्ञानी और पागल
जनसाधारण को यह सुन के आश्चर्य होगा कि यह क्या बात है कि जो परले दर्जे का
तत्तवज्ञानी हो वही पागल भी हो और बाहरी सुध-बुध रखे ही न। मगर बात तो ऐसी
ही है। वामदेव, जड़भरत आदि की ऐसी बातें बराबर कही जाती हैं भी, यही नहीं कि
हिन्दुओं के ही यहाँ यह चीज पायी जाती है, या गीता ने ही यही बात 'या निशा
सर्वभूतानां' (2।69) में कही है, या सुरेश्वराचार्य ने अपने र्वात्तिक में
खुल के कह दिया है कि ''बुद्धतत्तवस्य लोकोऽयं जड़ोन्मत्तापिशाचवत्।
बुद्धतत्तवोऽपि लोकस्य जड़ोन्मत्तापिशाचवत्''-''पहुँचे हुए तत्तवज्ञानी की
नजरों में यह सारी दुनिया जड़, पागल और पिशाच जैसी है और दुनिया की नजरों
में वह भी ऐसा ही है।''किन्तु प्राचीनतम ग्रीक विद्वान् अरिस्टाटिल
(अरस्तू) ने भी प्राय: ढाई हजार साल पूर्व यही बात अपनी पुस्तक 'जीवन की
बुद्धिमत्ता' (Wisdom of life) में यों कही है :-
“Men distinguished in philosophy, politics, poetry or art appear to be
all of a melancholy temperament.” (page. 19)
“By a diligent search in lunatic asylums I have found individual cases
of patients who were unquestionably endowed with great talents, and
whose genius distinctly appeared through their madness” (I, 247).
''जिन लोगों ने दर्शन, राजनीति, कविता या कला में विशेषज्ञता प्राप्त की है
उन सबों का ही स्वभाव कुछ मनहूस जैसा रहा है।'' ''पागलखानों में यत्नपूर्वक
अन्वेषण करने पर हमने ऐसे भी पागल पाये हैं जिनका दिमाग निस्सन्देह आले
दर्जे का था और पागलपन की दशा में भी उनकी चमत्कारशील प्रतिभा साफ झलकती
थी।'' पश्चिमी दर्शनों का इतिहास का लेखक दुरान्ती (Duranti) भी लिखता है
कि “The direct connection of madness and genius is established by the
biographics of great men, such as Rousseau, Byron, Alfieri etc.”
''पागलपन और प्रतिभा का सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है यदि हम रूसो,
बायरन, आलफीरी जैसे महापुरुषों की जीवनियाँ गौर से पढ़ें।''
(शीर्ष पर वापस)
पुराने समाज की झाँकी
बेशक, इस जमाने में यह बात ताज्जुब की मालूम होगी चाहे हजार पुराने
दृष्टान्त दिये जायँ, या महापुरुषों के वचन उध्दृयत किये जायँ। आज तो ऐसे
लोग नजर आते ही नहीं। जीते-जी सदा के लिए हमारी माया-ममता मिट जाये और हम
किसी को भी शत्रु-मित्र न समझें, यह बात तो इस संसार में इस समय अचम्भे की
चीज जरूर है। गीता ने इस पर मुहर दी है अवश्य। मगर इससे क्या? दिमाग में भी
तो आखिर बात आये। ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता जाता है, मालूम होता
है, यह बात भी त्यों-त्यों दूर पड़ती और असम्भव सी होती जाती है। असल में
दिन पर दिन हम इतना ज्यादा भौतिक पदार्थों में लिपटते जाते हैं कि कोई हद
नहीं। इसीलिए यह बात असम्भव हो गयी है। मगर पुराने जमाने के समाज में
माया-ममता का त्याग इतना कठिन न था। गीता ने जिस समय यह बात कही है उस समय
यह बात इतनी कठिन बेशक नहीं थी। उस समय का समाज ही कुछ ऐसा था कि यह बात हो
सकती थी। और तो और, यदि हम बर्बर एवं असभ्य कहे जाने वाले लोगों का
प्रामाणिक इतिहास पढ़ें तो पता लग जायगा कि उनके लिए यह बात कहीं आसान थी।
उनकी सामाजिक परिस्थिति तथा रहन-सहन ही ऐसी थी कि वे आसानी से इस ओर अग्रसर
हो सकते थे।
जीसुइत सम्प्रदायवादी शारलेवो नामक फ्रांसीसी पादरी ने एक पुस्तक लिखी है
जिसका नाम है 'हिस्तोरिया द ला नूवेल फ्रांस' (Historia dela Nouvelle
France)। वह अमेरिका के रक्तवर्ण आदि वासियों में घूमता और प्रचार करता था।
उसने तथा लहोतन नामक विचारशील पुरुष ने अपने अनुभव एवं दूसरों को भी
जानकारी के आधार पर उस पुस्तक के अनेक पृष्ठों में उन असभ्य रक्तवर्ण लोगों
के बारे में लिखा है, जिसे पाल लाफार्ग ने अपनी (Evolution of Property) के
32-33 पृष्ठों में यों उध्दृत किया है:-
“The brotherly sentiments of the Redskins are doubtless in part,
ascribable to the fact that the words ‘mine and thine’, ‘those cold
words;’ as Saint John Chrysostomos calls them, are all unknown as yet to
the savages. The protection they extend to the orphans, the widows and
the infirm, the hospitality which they exercise in so admirable a
manner, are, in their eyes, but a consequece of the conviction which
they hold that all things should be common to all men.”
“The free thinker Lahotan saya in his ‘Voyage de Lahetan II,’ Savages do
not distinguish between mine and thine, for it may be affirmed that what
belongs to the one belongs to the other. It is only among the Christain
savages, who dwell at the gates of cities, that money is in use. The
other will neither handle it nor even look upon it. They call it : the
serpent of the white-men. They think it strange that some should possess
more than others, and that those who have most should be more highly
esteened than those who have least. They neither quarrel nor fight among
themselves; they neither rob nor speak ill of one another.”
''बेशक रक्तवर्ण असभ्य लोगों में जो परस्पर
भ्रातृभाव पाया जाता है वह किसी हद तक इसीलिए है कि उन लोगों को अब तक
'मेरा और तेरा' का ज्ञान हुई नहीं-वही 'मेरा' और 'तेरा', जिन्हें महात्मा
जौन्क्रिसोस्तमो ने 'ठण्डे शब्द' ऐसा कहा है। अनाथों, विधावाओं एवं कमजोरों
की रक्षा वे लोग जिस तरह करते हैं और जिस प्रशंसनीय ढंग से वे लोग
आगन्तुकों का आदर-सत्कार करते हैं वह उनकी नजरों में इसलिए अनिवार्य और
स्वाभाविक है कि उनका विश्वास है कि संसार की सभी चीजें सभी लोगों की
हैं।''
''स्वतन्त्र विचारक लहोतन ने अपनी 'द्वितीय लहोतन की समुद्रयात्त्रा
पुस्तक में लिखा है कि असभ्य लोगों में 'मेरे' और 'तेरे' का भेद होता ही
नहीं। क्योंकि यह बात उनमें देखी जाती है कि जो चीज एक ही है वही दूसरे की
भी है। जो असभ्य लोग क्रिस्तान हो गये हैं और हमारे शहरों के पास रहते हैं
केवल उन्हीं लोगों में रुपये-पैसे का प्रचार पाया जाता है। शेष असभ्य न तो
रुपया-पैसा छूते और न उनकी ओर ताकते तक हैं। उन्हें यह बात विचित्र लगती है
कि कुछ लोगों के पास ज्यादा चीजें होती हैं बनिस्बत औरों के, और जिनके पास
ज्यादा हैं उनकी ज्यादा इज्जत होती है बनिस्बत कम रखने वालों के। वे असभ्य
न तो आपस में झगड़ते और न लड़ते हैं। वे न तो किसी की चीज चुराते और न एक
दूसरे की शिकायत ही करते हैं।''
कितनी आदर्श स्थिति है! कैसी उच्च भावनाएँ हैं! खूबी तो यह है कि ये लोग
निरे अपढ़ और निरक्षर हैं! यह ठीक है कि सभ्यता की हवा उन्हें लगी नहीं है।
आज से डेढ़ सौ वर्ष पहले तक जिनने उनकी यह बातें खुद देखी हैं उन्हीं के ये
बयान हैं, न कि हजार-दो हजार साल पहले वालों के! इसलिए जो लोग ऐसासमझते हैं
कि अहन्ता-ममता के त्याग की बातें कोरी गप्पबाजी है उन्हें होश सँभालना
चाहिए।वे ऑंखें खोलें और देखें कि हकीकत क्या है। पुरानी पोथियों में जो
बातें ऋषि-मुनियों के लिए,
आदर्श एवं वांछनीय मानी गयी हैं वही असभ्य लोगों में पायी जाती
हैं!बेशक,इसमामले में हम सभ्यों से वे असभ्य ही भले हैं! हमने तो
अपने-पराये के इस मर्जके चलतेसमूचे समाज को ही नर्क बना डाला है-सारे संसार
को जलती भट्ठी जैसा कर दिया है!
(शीर्ष पर वापस)
तब और अब
लेकिन अब हम अपने प्रसंग में आते हैं तो
देखते हैं कि गीता का जो आध्यात्मिक साम्यवाद है और जिसकी दुहाई आज बहुत
ज्यादा दी जाने लगी है, वह इस युग की चीज हो नहीं सकती, वह जनसाधारण की
वस्तु हो नहीं सकती। बिरले माई के लाल उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी कठिनता
को लक्ष्य करके कठोपनिषद् में कहा गया है कि ''बहुतों को तो इसकी चर्चा
सुनने का भी मौका नहीं लगता और सुनकर भी बहुतेरे इसे हासिल नहीं कर
सकते-जान नहीं सकते। क्यों कि एक तो इस बात का पूरा जानकार उपदेशक ही
दुर्लभ है और अगर कहीं मिला भी तो उसके उपदेश को सुनके तदनुसार प्रवीण हो
जाने वाले ही असंभव होते हैं''-''श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य:
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यु:। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा'।।श्चर्यो
ज्ञाता कुशलानुशिष्ट:'' (1।2।7) यही बात ज्यों की त्यों गीता ने भी कुछ और
भी विशद रूप से इसकी असंभवता को दिखाते हुए यों कही है कि
''आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य:। आश्चर्यवच्चन
मन्य: शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्'' (2।29)।
पहले भी तो इस चीज की अव्यावहारिकता का वर्णन किया जाई चुका है। आमतौर से
सांसारिक लोगों के लिए तो यह चीज पुराने युग में भी कठिनतम थी-प्राय:
असम्भव थी ही। मगर वर्तमान समय में तो एकदम असम्भव हो चुकी है। जो लोग इसकी
बार-बार चर्चा करते तथा मार्क्सी के भौतिक साम्यवाद के मुकाबिले में इसी
आध्याीत्मिक साम्यवाद को पेश करके इसी से लोगों को सन्तोष करना चाहते हैं
वे तो इससे और भी लाखों कोस दूर हैं। वे या तो पूँजीवादी और जमींदार हैं या
उनके समर्थक और इष्ट-मित्र या संगी-साथी। क्या वे लोग सपने में भी इस चीज
की प्राप्ति का खयाल कर सकते हैं, करते हैं? क्या वे मेरा-तेरा,
अपना-पराया, शत्रु-मित्र, हानि-लाभ आदि से अलग होने की हिम्मत
जन्म-जन्मान्तर भी कर सकते हैं? क्या यह बात सच नहीं है कि उनको जो यह भय
का भूत सदा सता रहा है कि कहीं भौतिक साम्यवाद के चलते उन्हें सचमुच
हानि-लाभ, शत्रु-मित्र आदि से अलग हो जाना पड़े और सारी व्यक्तिगत सम्पत्ति
से हाथ धोना पड़ जाय, उसी के चलते इस आध्या त्मिक साम्यवाद की ओट में अपनी
सम्पत्ति और कारखाने को बचाना चाहते हैं? वे लोग बहुत दूर से घूम के आते
हैं सही। मगर उनकी यह चाल जानकार लोगों में छिप नहीं सकती है। ऐसी दशा में
तो यह बात उठाना निरी प्रवंचना और धोखेबाजी है। पहले वे खुद इसका अभ्यास कर
लें। तब दूसरों को सिखायें। 'खुदरा फजीहत, दीगरे रा नसीहत' ठीक नहीं है।
मुकाबिला भी वे करते हैं किसके साथ? असम्भव का सम्भव के साथ, अनहोनी का
होनी के साथ। एक ओर जहाँ यह आध्यात्मिक साम्यवाद बहुत ऊँचा होने के कारण आम
लोगों के पहुँच के बाहर की चीज है, तहाँ दूसरी ओर भौतिक साम्यवाद
सर्वजनसुलभ है, अत्यन्त आसान है। यदि ये भलेमानस केवल इतनी ही दया करें कि
अडंग़े लगाना छोड़ दें, तो यह चीज बात की बात में संसार व्यापी बन जाय। इसमें
न तो जीते-जी मुर्दा बनने की जरूरत है और न ध्या न या समाधि की ही। यह तो
हमारे आये दिन की चीज है, रोज-रोज की बात है; इसकी तरफ तो हम स्वभाव से ही
झुकते हैं, यदि स्थायी स्वार्थ (Vested interests) वाले हमें बहकायें और
फुसलायें न। फिर इसके साथ उसकी तुलना क्या? हाँ, जो सांसारिक सुख नहीं
चाहते वह भले ही उस ओर खुशी-खुशी जायें। उन्हें रोकता कौन है? बल्कि इसी
साम्यवाद के पूर्ण प्रचार से ही उस साम्यवाद का भी मार्ग साफ होगा, यह पहले
ही कहा जा चुका है।
(शीर्ष पर वापस)
यज्ञचक्र
गीता में यज्ञ और यज्ञचक्र की भी बात आयी
है। यों तो हिन्दुओं की पोथियों में इस बात की चर्चा भरी पड़ी है। उपनिषदों
में भी यह बात कुछ निराले ढंग से ही आयी है। मगर गीता का ढंग कुछ दूसरा ही
है, जो ज्यादा व्यावहारिक एवं आकर्षक है। उपनिषद् रूपक के ढंग से यज्ञ और
हवन का आलंकारिक वर्णन करते हैं और धर्मशास्त्र या पुराण इन्हें स्वर्ग,
नर्क या मुक्ति और वैकुण्ठ ही लिए करने की आज्ञा देते हैं। उनने यज्ञों को
पूरा धार्मिक रूप दे दिया है। फिर तो स्वर्ग-नर्क की बात आई जाती है और
हुक्म या आज्ञा (Order or command) की भी जरूरत होई जाती है। हाँ,
मनुस्मृति में ''अग्नौप्रास्ता।।हुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं तत: प्रजा:'' (3।76) वचन आया है। इसमें
गीता की बातों का कुछ स्थूल आभास पाया जाता है। यह श्लोक इतना तो कहता ही
है कि ''यज्ञ-यागादि के समय अग्नि में जो कुछ ठीक-ठीक हवन किया जाता है वह
सूर्य तक पहुँचता है, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और
अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति तथा वृद्धि होती है।'' महाभारत के
शान्तिपर्व के 261वें अध्याय का ग्यारहवाँ श्लोक भी ऐसा ही है। इससे इतना
तो साफ होई जाता है कि उस समय लोगों का खयाल यज्ञ के सम्बन्ध में केवल
स्वर्गादि तक ही सीमित न रह के समाज की व्यवस्था और उसके भरण-पोषण तक भी
गया था। लोग यह मानने लगे थे कि समाज कल्याण के लिए-प्राणियों के सीधे
भरण-पोषण आदि के लिए-भी यज्ञ एक जरूरी चीज है। धर्म के रूप में यज्ञ के
करने से पुण्य के जरिये लोगों को अन्न-वस्त्रदि प्राप्त होंगे इस खयाल के
सिवाय यह विचार भी जड़ पकड़ चुका था कि यज्ञ से सीधे ही वृष्टि में सहायता
होती है और उससे अन्नादि उत्पन्न होते हैं।
बेशक, मीमांसकों ने कारीरी नामक याग के बारे में यह भी कहा है कि उसके करने
से अवर्षण मिट जाता है और वृष्टि होती है-''कारीर्या वृष्टिकामो यजेत।''
मगर आमतौर से सभी यज्ञयागों के बारे में उनका ऐसा मत है नहीं। इसीलिए
मनुस्मृति और शान्तिपर्व के उक्त वचन उस समय के लोगों के विचारों की प्रगति
के सूचक हैं। उससे पता चलता है कि किस प्रकार सामान्य रूप से
पुण्यप्राप्ति, स्वर्गप्राप्ति आदि से आगे बढ़ के क्रमश: कारीरी यज्ञ के
द्वारा सामान्यत: सभी यज्ञों का उपयोग समाजहित के काम में सीधे होने लगा।
उपनिषदों के समय में ऋषियों ने और पीछे दार्शनिकों ने भी जो यह स्वीकार
किया कि अग्नि से जल और जल से पृथिवी के द्वारा अन्नादि उत्पन्न हुए और इस
प्रकार प्राणि-सृष्टि का विकास हुआ उसका भी सम्बन्ध इस यज्ञवाली प्रक्रिया
से है या नहीं और अगर है तो कितना यह कहना असम्भव है। यज्ञ और अग्नि का
सम्बन्ध पुराने लोग अविच्छिन्न मानते थे। इसीलिए यह खयाल स्वाभाविक है कि
शायद वह बात भी इसी सिलसिले में आयी हो। मगर हमें तो उतने गहरे पानी में
उतरना है नहीं। हम तो गीता की ही बात देखना चाहतेहैं।
इससे पहले कि हम इस यज्ञ के बारे में गीता का मन्तव्य या उसकी विशेषता
बतायें यह जान लेना आवश्यक है कि गीता में कहाँ-कहाँ यज्ञ का जिक्र है और
किस प्रसंग में। यों तो यज्ञ के बारे में गीता का एक रुख और भाव हम बहुत
पहले बता चुके हैं और कह चुके हैं कि उसमें क्या खूबी है। मगर यहाँ उसके
दूसरे ही पहलू का वर्णन करना है। इस विवेचन से पहले कही गयी बात पर भी काफी
प्रकाश पड़ जायगा। गीता की यह यज्ञ वाली बात जो अपना निरालापन रखती है उसे
भी हम बखूबी जान सकेंगे।
गीता में तीसरे ही अध्याय से यज्ञ की बात शुरू होके चौथे में उसका खूब
विस्तार है। पाँचवें में भी यज्ञ शब्द अन्त के 29वें श्लोक में आया है।
सिर्फ छठे में वह पाया नहीं जाता। फिर लगातार सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और
बारह अधयायों में यज्ञ की बात आती है। यह ठीक है कि बारहवें में यज्ञ शब्द
नहीं आता। मगर तीसरे अध्या,य में 'यज्ञार्थ' (3।9) शब्द आया है और 'अहं
क्रतुरहं यज्ञ:' (9।16) में भगवान् को ही यज्ञ कहा है। 'यज्ञानां
जपयज्ञोऽस्मि' (10।25) में भी भगवान् को ही जप यज्ञ कहा है। फिर बारहवें के
10वें श्लोक में 'सत्कर्म', तथा 'मदर्थ कर्म' शब्द आये हैं। इसीलिए उसे भी
जप यज्ञ ही माना है। बीचवाले 13, 14, 15 अधयायों में यज्ञ की चर्चा नहीं
है। उसके बाद 16, 17, 18 में स्थान-स्थान पर आयी है। इससे स्पष्ट है कि
गीता की दृष्टि से यज्ञ की महत्ता बहुत है, और है वह व्यापक चीज। गीता की
खास-खास बातों में एक यह भी है।
अब जरा उसके स्वरूप का विचार करें। सबसे पहले तीसरे अध्याभय के 9-16
श्लोकों को ही लें। इन आठ श्लोकों में यज्ञ और यज्ञचक्र की बात आयी है।
यहाँ यज्ञ का कोई भी ब्योरा नहीं दिया गया है और न उसका विशेष विश्लेषण ही
किया गया है। केवल इतना ही कहा गया है कि ''जो कर्म यज्ञ के लिए हो उससे
बन्धन नहीं होता है, किन्तु और-और कर्मों से
ही''-''यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन:'' (3।9)। इसके बाद
यज्ञ को प्राणियों के लिए जरूरी और कल्याणकारी कहके 14-16 श्लोकों में एक
ऋंखला ऐसी बनायी है जो चक्र की तरह गोल हो जाती है और उसके बीच में यज्ञ आ
जाता है। इसी को यज्ञचक्र कह के इसे निरन्तर चालू रखने पर बड़ा ही जोर दिया
है। 13वें तथा 16वें श्लोकों में यज्ञ न करनेवालों की सख्त शिकायत भी की
गयी है। यहाँ तक कह दिया है कि जो इस चक्र को निरन्तर चालू न रखे वह पतित
तथा गुनहगार है और उसका जीना बेकार है!
चौथे अध्याय की यह दशा है कि उसके 23-33 श्लोकों में यज्ञ का बहुत ज्यादा
ब्योरा दिया गया है। इन ग्यारह श्लोकों में जो पहला-23वाँ-है उसमें तो वही
बात कही गयी है जो तीसरे के 9वें में कि ''यज्ञार्थ कर्म सोलहों आना जड़-मूल
से विलीन हो जाता है। फिर बन्धन में कौन डालेगा?''-''यज्ञायाचरत: कर्म
समग्रं प्रविलीयते।'' इसके बाद यज्ञों की किस्में 24वें से शुरू होके 33वें
तक बताई गयी हैं। बीच के 31वें में तो यहाँ तक-साफ कह दिया है कि ''जो यज्ञ
नहीं करता उसका दुनियावी काम तक तो चली नहीं सकता, परलोक की बात तो दूर
रहे''-''नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य: कुरुसत्ताम।'' इससे एक तो यज्ञ
की व्यापकता तथा समाजोपयोगिता सिद्ध होती है-यह बात पक्की हो जाती है कि वह
समाज को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। दूसरे यह कि पूर्व के सात श्लोकों
में जिन यज्ञों को गिनाया है वह केवल नमूने की तौर पर ही हैं। इसीलिए 28वें
श्लोक में गोल-गोल बात ही कही भी गयी है कि-''द्रव्यों से सम्बन्ध रखने
वाले, तप-सम्बन्धी, योग-सम्बन्धी, ज्ञान-सम्बन्धी और सद्ग्रन्थसम्बन्धी
अनेक यज्ञ हैं''-''द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे।
स्वाध्या-यज्ञानयज्ञाश्च यतय: संशितव्रता:।'' फिर 32वें श्लोक में भी इसकी
पुष्टि कर दी गयी है कि ''इस प्रकार के अनेक यज्ञ वेदादि सद्ग्रन्थों में
बताये गये हैं और सभी के सभी क्रियात्मक या क्रियासाध्यी हैं''-''एवं
बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्विद्धितान्सर्वान्।'' आखिर में
ज्ञानयज्ञ को और यज्ञों से उत्ताम कह के इस प्रसंग को पूरा किया है। फिर
ज्ञान की प्राप्ति का विचार शुरू किया है।
पाँचवें अध्याय में तो एक ही बार अन्तिम-29वें श्लोक में यज्ञ शब्द आया ही
है। उसमें इतना ही कहा गया है कि परमात्मा ही यज्ञों तथा तपों को स्वीकार
करने वाला एवं सभी पदार्थों का बड़ों से बड़ा शासक और नियन्त्रणकर्ता है।
लेकिन यह बात भी है कि सबों का कल्याण भी वह चाहता है-'भोक्तारं यज्ञतपसां'
आदि। यह दूसरी बात है कि चौथे अध्याय में जिस प्राणायाम को यज्ञ कहा है उसी
का कुछ अधिक विवरण और तरीका इस अध्याय में दिया गया है। छठे में तो
प्राणायाम की ही विधि विशेष रूप से दी गयी है। फलत: इस दृष्टि से तो वह भी
यज्ञ प्रतिपादक ही है।
सातवें अध्याय की यह हालत है कि उसके 20 से 23 तक के चार श्लोकों में निचले
दर्जे के-जघन्य-यज्ञों का वर्णन करके अन्त में कह दिया है कि जो भगवान् के
लिए यज्ञ करता है वही सबसे अच्छा है। यह एक अजीब सी बात है कि जिसकी मर्जी
जिस चीज में हो उसकी श्रद्धा उसी में मजबूत कर दी जाती है। यह काम खुद
भगवान् करते हैं ऐसी बात ''तस्यतस्याचलां श्रध्दां'' (21) में साफ ही कही
गयी है। इसका एक मतलब तो यही है कि छोटी-छोटी चीजों में एकाग्रता होने और
श्रद्धा जम जाने पर मनुष्य का अपने दिल-दिमाग पर काबू होने लगता है। इसलिए
मौका पड़ने पर ऊँची चीज में भी वह उसे लगा सकता है। एकाएक वैसी चीज में
लगाना असम्भव होता है। इसीलिए पतंजलि ने योगसूत्रों में साफ ही कहा है कि
''यथाभिमतधयानाद्वा'' (1।39)। इसके भाष्य में व्यास ने लिखा है कि
''यदेवाभिमतं तदेव धयायेत्। तत्र लब्धास्थितिकमन्यत्रपि स्थितिपदं
लभते''-''जिसी में मन लगे उसी का ध्यायन करे। जब उसमें मन जमते-जमते स्थिर
होने लगेगा तो उससे हटा के दूसरे में भी स्थिर किया जा सकता है।'' दूसरी
बात यह है कि धर्म तो श्रद्धा की ही चीज है, यह पहले ही कहा जा चुका है। वह
न छोटा है न बड़ा, और न ऊँचा है न नीचा। वह कैसा है यह सब कुछ निर्भर करता
है इस बात पर कि उसमें हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारे दिल-दिमाग, हमारी जबान
और हमारे हाथ-पाँवों में-इन चारों में-सामंजस्य कहाँ तक है और हम सच्चे तथा
ईमानदार कहाँ तक हैं। इसीलिए यह सामंजस्य पूर्ण न होने के कारण ही कमअक्ल
लोगों के कर्मों को तुच्छ फलवाला कहा है ''अन्तवत्तु फलं तेषां
तद्भवत्यल्पमेधासाम्'' (7।23)। लेकिन जिनका सामंजस्य दूसरा हो गया है उनके
लिए कहा है कि वे भगवान् रूप ही हैं-''मद्भक्ता यान्ति मामपि'' (7।23)। इस
अध्याहय के अन्त के 30वें श्लोक में 'अधियज्ञ' के रूप में यज्ञ का नाम लेकर
प्रश्न किया है कि वह क्या है, कौन है? अधियज्ञ आदि की बात हम स्वतन्त्र
रूप से आगे लिखेंगे।
आठवें अध्याय के तो आरम्भ में ही उसी अधियज्ञ के बारे में दूसरे ही श्लोक
में प्रश्न किया गया है कि वह है कौन सा पदार्थ? फिर इसी का उत्तर चौथे
श्लोक में आया है कि भगवान् ही इस शरीर के भीतर अधियज्ञ
हैं-''अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर।'' मगर इससे पूर्व के तीसरे
श्लोक में कर्म किसे कहते हैं, पूर्व के इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है
कि ''पदार्थों के उत्पादन और पालन का कारण जो त्याग या विसर्जन है वही कर्म
कहा जाता है''-''भूतभावोद्भवकरो विसर्ग: कर्मसंज्ञित:'', वह भी यज्ञ का ही
निरूपण है। क्योंकि जैसा कि कह चुके हैं, तीसरे अध्याय में तो वृष्टि आदि
के द्वारा यज्ञ का यही काम कहा ही गया है। इसी अध्याय के अन्तिम-28वें
श्लोक में भी यज्ञ शब्द आया है। मगर उसका यही मतलब है कि यज्ञ कोई उत्ताम
चीज है जिसका फल बहुत ही सुन्दर और रमणीय होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं
कहा गया है।
नवें अध्याय के 15-16, तथा 20-28 श्लोकों में इस यज्ञ का विस्तार पाया जाता
है। 15वें में ज्ञान-यज्ञ का ही विभिन्न रूप बता के दिखाया है कि उसके
द्वारा कैसे भगवान् की पूजा होती है। 16वें में भगवान् को ही यज्ञ करार दे
के वैदिक यज्ञ के साधन घी, अग्नि आदि को भी भगवान् का ही स्वरूप कह दिया
है। 20-21 श्लोकों में वैदिक सोम-यागादि का क्या परिणाम होता है और स्वर्ग
पहुँच के उस यज्ञ के करने वाले फिर क्योंकर कुछी दिनों बाद लौट आते तथा
जन्म लेते हैं, यह बताया गया है। 22वें में पुनरपि उसी ज्ञान-यज्ञ के
महत्तव का वर्णन है। 23-25 श्लोकों में सातवें अध्याय की ही तरह
दूसरे-दूसरे देवताओं के यज्ञों की बात कह के उसमें इतना और जोड़ दिया है कि
वह भी भगवान् की ही पूजा है; हालाँकि जैसी चाहिए वैसी नहीं है। क्योंकि उसे
करने वाले यह बात तो समझ पाते नहीं कि यह भी भगवत्पूजा ही है। इसीलिए वे
चूकते हैं-उनका पतन होता है। जिस चीज में मन लगाइये वहीं पहुँचियेगा-वही
बनियेगा, यही तो नियम है और वे लोग तो दूसरों में-भूत-प्रेत, पितर आदि
में-ही मन लगाते हैं, उसी भावना से यज्ञ या पूजन करते हैं। फिर उन्हें
भगवान् कैसे मिलें? यही उनका चूकना है।
इस अध्याय के 26-28 तीन श्लोकों में जो कुछ कहा गया है वह है तो यज्ञ ही।
मगर है वह बहुत बड़ी चीज। कोई भी काम, जो निश्चित कर दिया गया हो, करते
रहिये। बस, वही भगवत्पूजा होती है यदि इसी भावना से वह काम किया जाय, यही
अमूल्य मन्तव्य इन श्लोकों में कहा गया है। कर्मों के छुटकारे के लिए खुद
कर्म ही किस प्रकार साबुन का काम करते हैं, यही चीज यहाँ पायी जाती है। इन
श्लोकों के सिवाय पीछे के 19वें श्लोक में भी कुछ ऐसी बात कही गयी है जिससे
पता चलता है कि उसमें भी यज्ञ का ही निरूपण है। भगवान् को तो उससे पूर्व के
16वें श्लोक में यज्ञ कहा ही है। मगर इसमें जो यह कहा गया है कि ''मैं ही
वर्षा रोकता हूँ और उसे जारी भी करता हूँ''-''अहं वर्षं निर्गृम्यत्सृजामि
च'', उससे पता चलता है कि यज्ञ का ही उल्लेख है। क्योंकि तीसरे अध्या-य में
तो कही दिया है कि ''यज्ञ से ही वृष्टि होती है''-''यज्ञाद्भवति
पर्जन्य:।'' 'उत्सृजामि' शब्द का अर्थ है उत्सर्ग या छोड़ना-बाधा हटा देना।
आठवें में जो विसर्ग कहा गया है वही है यह उत्सर्ग। यज्ञों से वृष्टि की
बाधा हटके पानी बरसता है। नवें अध्याय के अन्त के 34वें श्लोक में भी
'मद्याजी' शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है 'मेरा-भगवान् का-यज्ञ
करनेवाला-भगवत्पूजा'। इसी श्लोक के प्राय: तीन चरण अठारहवें अध्याय के
65वें श्लोक में भी ज्यों के त्यों पाये जाते हैं। अर्थ भी यही है।
दसवें अध्यायके तो केवल 25वें श्लोक में जप यज्ञ की बात आयी है। इसके बारे
में हम भी इस प्रसंग के शुरू में ही कह चुके हैं। ग्यारहवें अध्याय के
'नवेदयज्ञाधययनैर्नदानै:' (48), तथा 'नदानेन नचेज्यया' (53) श्लोकों में
यज्ञ और इज्या शब्द आये हैं। इज्या का वही अर्थ है जो यज्ञ का। यहाँ केवल
यज्ञ का उल्लेख है। कोई खास बात नहीं है। बारहवें अध्याय के 10वें श्लोक
में 'मदर्थ' या भगवान् के लिए किये जाने वाले कर्मों का उल्लेख है और
यज्ञार्थ कर्म की बात तो कही चुके हैं। इसीलिए वहाँ भी यज्ञ की ही बात है।
सोलहवें अध्यायमें यज्ञ का जिक्र है केवल 15वें तथा 17वें श्लोकों में । यह
बात बहुत अच्छी तरह ईश्वरवाद के प्रसंग में लिखी जा चुकी है। हाँ, सत्रहवें
अध्या1य में यज्ञ की बात बार-बार अनेक रूप में आयी है। पहले और चौथे श्लोक
में श्रद्धापूर्वक यज्ञादि करने और सात्तिवक यज्ञों का साधारण उल्लेख है।
कोई विवरण नहीं है। हाँ, इतना कह दिया है कि कैसों की यज्ञपूजा किस प्रकार
की होती है। यज्ञ के सात्तिवक आदि तीन प्रकार यजनीय और पूजनीय पदार्थों के
ही हिसाब से बताये गये हैं। फिर आगे के 11-13-तीन-श्लोकों में यज्ञ के
कर्ता के अपने ही भावों और विचारों के अनुसार यज्ञ के वही सात्तिवक आदि तीन
भेद बताये गये हैं। इसके बाद 23-25-तीन-श्लोकों में और कुछ न कह के यज्ञादि
कर्मों की त्रुटियों के पूरा करने का सीधा उपाय बताया गया है कि श्रद्धा के
साथ-साथ यदि ओंतत्सत् बोल के उन्हें किया जाय तो उनमें अधूरापन रही नहीं
जाता-वे सात्तिवक बन जाते हैं। यही बात 27-28 श्लोकों में भी पायी जाती है।
28वें में हुत शब्द का अर्थ यज्ञ ही है। 27वें का 'तदर्थीयकर्म' भी इसी
मानी में आया है। यज्ञार्थ और तदर्थ एक ही चीज है।
अठारहवें अध्या'य के 65वें के सिवाय 70वें श्लोक में भी ज्ञानयज्ञ का
उल्लेख है। गीता के उपसंहार में ज्ञानयज्ञ का नाम लेना कुछ महत्तव रखता है।
पहले भी तो कही चुके हैं कि और यज्ञों से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। वही बात
यहाँ याद हो आयी है। खूबी तो यह है कि उस श्लोक में गीता के पढ़नेवाले को ही
कहा है कि वही ज्ञानयज्ञ के द्वारा भगवान् की पूजा करता है। इस प्रकार
पठन-पाठन को ज्ञानयज्ञ के भीतर डाल के गीता ने सुन्दर पथ-प्रदर्शन किया है।
यज्ञ का अर्थ समझने के लिए वुं+जी भी दे दी है। इस अध्याय के प्रारम्भ के
3, 5, 6 श्लोकों में भी यज्ञ, दान, तप इन तीन कर्मों का बार-बार उल्लेख
किया है और कहा है कि ये बुनियादी कर्म हैं। इन्हें किसी भी दशा में छोड़
नहीं सकते। इस तरह यज्ञ का महत्तव सिद्ध कर दिया है।
इतनी दूर तक गीता के यज्ञ का सामान्य तथा विशेष विचार कर लेने के बाद अब
हमें मौका मिलता है कि उसकी तह में घुस के देखें कि यह क्या चीज है। तीसरे
अध्याबय में जो यज्ञचक्र बताया गया है वह अत्यन्त महत्तवपूर्ण है। उससे इस
मामले पर काफी प्रकाश पड़ता है। इसलिए पहले उसे ही देखें कि उसकी हकीकत क्या
है। वहाँ यह क्रम पाया जाता है कि कर्मों से यज्ञ का स्वरूप तैयार होता है,
वह पूर्ण होता है-यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से
भूतों यानी पदार्थों तथा प्राणियों का भरण-पोषण होता है और उनकी उत्पत्ति
भी होती है। इस प्रकार जो एक ऋंखला तैयार की गयी है उसके एक सिरे पर भूत आ
जाते हैं। भूत का असल तात्पर्य है ऐसे पदार्थों से जिनका अस्तित्व पाया
जाय-यानी सत्ताधारी पदार्थमात्र। उसी ऋंखला के दूसरे सिरे पर कर्म पाया
जाता है, ऐसा खयाल हो सकता है। होना भी ऐसा ही चाहिए। क्योंकि कर्म का ही
सम्बन्ध पदार्थ से मिलाना है और यही चीज गीता को अभिमत भी है। मगर इससे
चक्र तैयार हो पाता नहीं। क्योंकि जब तक ऋंखला के दोनों सिरे-छोर-मिल न
जायँ, जुट न जायँ, चक्र होगा कैसे? चक्र का तो मतलब ही है कि ऋंखला के भीतर
वाले सभी पदार्थों का लगाव एक सिरे से रहे और कहीं भी वह लगाव टूटने न
पाये। फलत: एक बार एक पदार्थ को शुरू कर दिया और वह चक्र खुद-ब-खुद चालू
रहेगा। केवल ऋंखला रहने पर और चक्र न होने पर यह बात नहीं हो सकती। तब तो
बार-बार ऋंखला की लड़ियों के किनारे पहुँच के नये सिरे से शुरू करने की बात
आ जायगी। मगर चक्र में किनारे की बात ही नहीं होती। सभी लड़ियाँ बीच में ही
होती हैं।
यह ठीक है कि भूतों का तो कर्मों से ताल्लुक हुई। भूतों में ही तो क्रिया
पायी जाती और क्रिया से यज्ञ का सम्बन्ध होके चक्र चालू रहता है। किनारे का
सवाल भी अब नहीं उठता। यही सर्वजनसिद्ध बात है भी। मगर इसमें दो चीजों की
कमी रह जाती है। एक तो यह बात निरी मशीन जैसी चीज हो जाती है। भूतों की
क्रिया के पीछे कोई ज्ञान, दिमाग या पद्धति है, या कि योंही वह क्रिया चालू
है, जैसे घड़ी की सुइयों की क्रिया चालू रहती है? यह प्रश्न उठता है और इसका
उत्तर जरूरी है। मगर इस चक्र में इसका उत्तर नहीं मिलता है। दूसरी बात यह
है कि हमें तो अपने ही दिल-दिमाग के अनुसार कर्मों के करने का हक है, गीता
का यह सिद्धान्त बताया जा चुका है इस चक्र में यह बात भी साफ हो पाती नहीं
और इसके बिना काम ठीक होता नहीं।
इसीलिए तीसरे अध्याय में उस ऋंखला में दो लड़ें और भी जुटी हैं जो इस कमी की
पूर्ति कर देती हैं। दोई कमियाँ थीं और दो लड़ें जुट गयीं। वहाँ कहा गया है
कि अक्षर से ब्रह्म और ब्रह्म से कर्म पैदा होता है। कर्म का तो यज्ञ के
द्वारा उस ऋंखला में लगाव हुई। मगर प्रश्न यह होता है कि चक्र बनता है
कैसे? अक्षर से शुरू करके भूतों पर खात्मा हो जाने पर मिलान तो होती नहीं।
भूत और अक्षर तो दो जुदी चीजें हैं न? यह भी नहीं कि जैसे भूतों से कर्म
बनते हों-उनके ही द्वारा कर्म होते हों-वैसे ही भूतों से अक्षर होता हो या
बनता हो। फलत: भारी अड़चन आ जाती है। दोनों कमियों की पूर्ति कैसे हो गयी यह
बात तो अलग ही है-इसका भी पता नहीं चलता।
इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ब्रह्म और अक्षर को पहले जान लेना होगा कि
ये दोनों हैं क्या। पहले ही ब्रह्म को लें। गीता में ब्रह्म शब्द तीन
अर्थों में आया है। यों तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहत् या बड़ा-बहुत बड़ा,
सबसे बड़ा। आमतौर से ब्रह्म कहते हैं परमात्मा या भगवान् को ही। उसे इसीलिए
समंब्रह्म, परंब्रह्म या परब्रह्म और अक्षरब्रह्म भी कहा करते हैं। ब्रह्म
शब्द गीता में कुल मिला के प्राय: तिरपन बार आया है। अध्याय और श्लोक
जिनमें यह शब्द मिलता है इस तरह हैं-(2।72), (3।15), (4।24, 25, 31, 32),
(5।16, 10, 19, 20, 21, 24, 25, 26), (6।14, 28, 38, 44), (7।29), (8।1, 3,
11, 13, 16, 17, 24), (10।12), (11।15, 37), (13।4, 12), (14।3, 4, 26,
27), (17।14, 23, 24), (18।42, 50, 53, 54)। किसी-किसी श्लोक में कई-कई बार
आने के कारण 50 बार से ज्यादा हो जाता है।
मगर यदि पूर्वा पर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि पाँच ही अर्थों में यह
शब्द प्रयुक्त हुआ है। परमात्मा के अर्थ में तो बार-बार आया है और सबसे
ज्यादा आया है। ब्राह्मण जाति के अर्थ में केवल एक बार अठारहवें अध्याय के
42वें श्लोक में पाया जाता है। यों तो इसी ब्रह्म शब्द से बना ब्राह्मण
शब्द कई बार आया है। प्रकृति या माया के अर्थ में चौदहवें अध्याय के 3, 4
श्लोकों में पाया जाता है। असल में उसके साथ महत् शब्द लगा है और उसका अर्थ
है महान् या महत्तात्तव। प्रकृति से जिस तत्तव की उत्पत्ति वेदान्त और
सांख्यदर्शनों में मानी जाती है उसे ही महान्, महत् या महत्तात्तव कहते
हैं। तेरहवें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसे बुद्धि कहा है वह यही महत् है।
यह है समष्टि या व्यापक बुद्धि, न कि जीवों की जुदा-जुदा। वहाँ जिसे
अव्यक्त कहा है वही है प्रकृति और चौदहवें में उसी को ब्रह्म कहा है।
सातवें अध्याय के चौथे श्लोक में भी उसे बुद्धि और अव्यक्त को अहंकार कह
दिया है। वहाँ मन का अर्थ है अहंकार और अहंकार का प्रकृति अर्थ है। चौदहवें
में महत् शब्द के सम्बन्ध से ब्रह्म का अर्थ प्रकृति हो जाता है। प्रकृति
से ही तो विस्तार या सृष्टि का पसारा शुरू होता है और सबसे पहले समष्टि
बुद्धि पैदा होती है। इसीलिए प्रकृति का विशेषण महत् दे दिया है।
महत्तात्तव भी तो प्रकृति से जुदा नहीं है, जैसे मिट्टी से घड़ा।
ब्रह्म शब्द का चौथा अर्थ है हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा। उसी को अव्यक्त भी कहा
है। आठवें अध्यातय के 16, 17 श्लोकों में ब्रह्मा के ही अर्थ में ब्रह्म
शब्द और अठारहवें में अव्यक्त शब्द आया है। ग्यारहवें अध्याय के 15वें में
भी ब्रह्म शब्द का ब्रह्मा ही अर्थ है। छठे के 14वें तथा सत्रहवें अध्याय
के 14वें श्लोक में ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचर्यवाला ब्रह्म शब्द वेद के ही
अर्थ में सर्वत्र आता है और वहाँ भी आया है। चौथे के 'ब्रह्मणोमुखे' का
ब्रह्म शब्द भी वेद का ही वाचक है। इसी प्रकार छठे अध्याहय के 44वें श्लोक
में जो ब्रह्म शब्द है वह भी वेदार्थक ही है। उसके पूर्व में 'शब्द' शब्द
लग जाने से दूसरे अर्थ की गुंजाइश वहाँ रही नहीं जाती। तीसरे अध्याउय में
जो यज्ञचक्र के सिलसिले में ब्रह्म शब्द आया है वह भी वेद का ही वाचक है।
शेष ब्रह्म शब्द परब्रह्म या परमात्मा के ही अर्थ में आये हैं। शायद ही
कहीं परमात्मा के सिवाय उक्त शेष चार अर्थों में किसी में आये हों।
असल में तो ब्रह्म शब्द के तीन ही मुख्य अर्थ गीता में पाये जाते हैं और ये
हैं वेद, परमात्मा, प्रकृति। यह भी कही चुके हैं कि आमतौर से ब्रह्म का
अर्थ परमात्मा ही होता है। शेष अर्थ या तो प्रसंग से जाने जाते हैं, या
किसी विशेषण के फलस्वरूप। दृष्टान्त के लिए प्रकृति के अर्थ में ब्रह्म
शब्द का प्रयोग होने के समय प्रसंग तो हुई। पर, उसी के साथ महत् विशेषण भी
जुटा है। यही बात वेद के अर्थ में भी है। शब्द ब्रह्म की बात अभी कही गयी
है। 'ब्रह्मणोमुखे' में जो ब्रह्म का अर्थ वेद होता है वह प्रसंगवश ही समझा
जाता है। यज्ञों का विस्तार वेदों में ही है। उसे ही वेद का मुख कह दिया
है। मुख है प्रधान अंग। इसीलिए मुख और मुख्य शब्द प्रधानार्थक हैं। वेदों
के प्रधान अंशों में यज्ञों का ही विस्तार पाया जाता भी है। जिन लोगों ने
यहाँ 'ब्रह्मणोमुखे' में ब्रह्म का अर्थ परमात्मा किया है उन्हें क्या कहा
जाय ? यज्ञों का विस्तार वेदों में ही तो है। भगवान् के मुख में विस्तार
है, यह अजीब बात है। हमें आश्चर्य तो तब और होता है जब वही लोग 'त्रिविद्या
मां सोमपा:' (9।20), तथा 'त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना:' (9।21), में खुद स्वीकार
करते हैं कि त्रयी या तीनों वेदों में यज्ञयागादि का ही विशेष वर्णन है।
फिर यहाँ वही अर्थ क्यों नहीं किया जाय? तीसरे अध्यासय में भी ब्रह्म का
विशेषण सर्वगत है। गम् धातु संस्कृत में ज्ञान के अर्थ भी प्रयुक्त होती
है। इसीलिए अवगत शब्द का अर्थ है जाना हुआ। इस प्रकार सर्वगत शब्द का अर्थ
है सब चीजों को जनाने या बतानेवाला। खुद वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान
से ही तो सब चीजें प्रकाशित होती हैं या जानी जाती हैं। इसीलिए यहाँ अर्थ
हो जाता है कि सभी बातों को अवगत कराने वाले वेदों से ही कर्म आते हैं,
पैदा होते हैं या जाने जाते हैं। वेद का तो काम केवल बताना ही है न?
यह तो सभी वेदज्ञ जानते हैं कि यज्ञयागादि सभी प्रकार के कर्मों पर बहुत
ज्यादा जोर वेदों ने दिया है। मीमांसा दर्शन उन्हीं वेदवाक्यों के आधार पर
कर्मों का विस्तृत विवेचन करता है। श्रौत तथा स्र्मात्ता सूत्रग्रन्थ
इन्हीं वैदिक कर्मों की विधियाँ बताते हैं। यहाँ तक कि यजुर्वेद के
अन्तिम-चालीसवें-अध्यातय के दूसरे मन्त्र में साफ ही कह दिया है कि
''कर्मों को करते रहके ही इस दुनिया में सौ साल जीने की इच्छा करे; क्योंकि
मनुष्य में कर्मों का लेप न हो-वे मनुष्य को बन्धन में न डालें-इसका दूसरा
उपाय हुई नहीं''-''कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा:। एवं त्वयि
नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥'' यह तो कही चुके हैं कि गीता ने भी
कर्मों को ही उनके बन्धन के धोने का साबुन बताया है। उसने इसकी तरकीब भी
सुझाई है।
परन्तु दरअसल ब्रह्म के दोई भेद किये गये हैं। मुण्डक उपनिषद् के प्रथम
खण्ड में ही जिसे परा एवं अपरा विद्या के रूप में 'द्वे विद्ये वेदितव्ये'
कहा है, उसी चीज को सफाई के साथ महाभारत के शान्तिपर्व के (231-6।269-1) दो
श्लोकों में, जो हू-ब-हू एक ही हैं, कह दिया है कि ''ब्रह्म तो दोई हैं-पर
तथा अपर या शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। जो शब्दब्रह्म में प्रवीण हो जाता है
वही परब्रह्म को जान पाता है''-''द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं
च यत्। शब्दब्रह्मणि निष्णात: परं ब्रह्माधिगच्छति॥'' इन्हीं दो में से
शब्द-ब्रह्म को गीता के तृतीय अध्याय में सर्वगत ब्रह्म और पर-ब्रह्म को
अक्षर कहा है। आठवें (8।3) में उसे ही अक्षरब्रह्म और परमब्रह्म भी कहा है।
और भी स्थान-स्थान पर यही बात पायी जाती है।
इस प्रकार सर्वगत वेद से यदि कर्मों की जानकारी होती है तो यह शंका कि
कर्मों के पीछे ज्ञान और दिमाग है या नहीं, अपने आप मिट जाती है। वेद तो
ज्ञान को कहते ही हैं। इसलिए मानना पड़ता है कि यज्ञयागादि कर्म घड़ी की सुई
की चाल जैसे न हो के ज्ञानपूर्वक होते हैं। इनकी व्यवस्था ही ऐसी है।
इसीलिए तो जवाबदेही भी करने वालों पर आती है। अब सिर्फ दूसरी शंका रह जाती
है कि लोगों को समझ-बूझ के करने की बात है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि
किसी की प्रेरणा से विवश हो के ही कर्म करने पड़ते हैं। इसका उत्तर ''ब्रह्म
अक्षर से पैदा हुआ''-ब्रह्माक्षर समुद्भवम्'' पद देते हैं। श्वेताश्वर
उपनिषद् के अन्तिम-छठे-अध्यातय में एक मंत्र आता है कि ''जो परमात्मा सबसे
पहले ब्रह्मा को पैदा करके उसे वेदों का ज्ञान कराता है''-''यो ब्रह्माण
विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोत तस्मै'' (6।18)। जगह-जगह वैदिक
ग्रन्थों में यही बात पायी जाती है। मनु आदि ने भी यही लिखा है। ब्राह्मण
ग्रंथों में भी बार-बार यही कहा गया है। इससे यह बात तो निर्विवाद है कि
अविनाशी या अक्षरब्रह्म से वेद पैदा हुए। या यों कहिये कि उसने ही वेद
बनाये। और जब ऐसा नहीं कह के कि परमात्मा ने कर्म बनाये, यह कहा है कि उसने
वेद बनाये, तो स्पष्ट है कि हम वेदों को पढ़ के जानकारी हासिल करें और
कर्मों को समझ-बूझ के करें। अगर यह कह दिया होता कि परमात्मा ने कर्म ही
बनाये, तो यही खयाल होता है कि कर्म करने की उसकी आज्ञा या मर्जी है। उसमें
सोचने-विचारने का प्रश्न है नहीं।
तब सवाल यह होता है कि चक्र कैसे बनेगा? भूतों का अक्षर ब्रह्म से कौन-सा
सम्बन्ध है? जब तक या तो भूतों से अक्षरब्रह्म की उत्पत्ति न मानी जाय, या
दोनों की एकता स्वीकार न की जाय तब तक ऋंखला के दोनों छोर पृथक्-पृथक्
रहेंगे। वे मिलेंगे हर्गिज नहीं। मगर इन दोनों में एक भी सम्भव नहीं। भूतों
में तो सभी पदार्थ आ जाते हैं, चाहे जड़ हों या चेतन। फिर सबकी एकता ब्रह्म
के साथ होगी कैसे? उनमें ब्रह्म की उत्पत्ति तो कोई भी नहीं मानता। तब यह
गुत्थी सुलझे कैसे? यहाँ हमें फिर उपनिषदों की ओर देखना पड़ता है। तभी यह
गाँठ सुलझेगी। गीता तो उपनिषद् हुई। सभी अधयायों के अन्त में ऐसा ही कहा
गया भी है।
वृहदारण्यक उपनिषद् के चतुर्थ अध्या।य के पाँचवें ब्राह्मण के 11वें मन्त्र
में याज्ञवल्क्य एवं मैत्रोयी के संवाद के सिलसिले में याज्ञवल्क्य ने
मैत्रोयी से कहा है कि ''यथाद्रैधाग्नेरभ्याहितस्य पृथगधूमा
विनिश्चिरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य नि:श्वसितमेतदृग्वेदो यजुर्वेद:
सामवेदोऽथर्वारस इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषद: श्लोका:
सूत्रण्यनुव्याख्यानिव्याख्यानीष्टं हुतमाशितं पायितमयं च लोक: परश्च लोक:
सर्वाणि च भूतान्स्यैवैतानि सर्वाणि नि:श्वसितानि।'' इसका आशय यह है कि
''जिस तरह गीले ईंधान से अग्नि का सम्बन्ध होने पर उससे चारों ओर धुऑं
फैलता है, ठीक उसी तरह इस महान् भूत की साँस के रूप में ही ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, कला, उपनिषद, श्लोक, सूत्र,
व्याख्यान, व्याख्यानों के व्याख्यान, हवन के पदार्थ, यज्ञ के भोज्य तथा
पेय पदार्थ, यह लोक-परलोक, सभी भूत चारों ओर फैले हैं।''
यहाँ कई बातें हैं। एक तो वेदादि जितनी ज्ञान की राशियाँ हैं उनका केन्द्र
परमात्मा ही माना गया है। दूसरे सृष्टि के सभी पदार्थों का पसारा उसी से
बताया गया है। तीसरे भूतों को भी उसी की साँस की तरह कहा गया है। यानी भूत
उससे जुदा नहीं है। चौथी बात यह है और यही सबसे अधिक महत्तवपूर्ण है कि उस
परमात्मा को महाभूत कहा गया है। आगे के 14-15 मन्त्रों में उसी को अविनाशी
आत्मा कहा है, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो पकड़ा जा सकता नहीं, जो
गलता-पचता नहीं, जो सटता नहीं, जिसे व्यथा नहीं होती और जो घटता नहीं तथा
सभी को जानता है-''अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधार्मा। अगृह्यो नहि
गृह्यतेऽशीर्यो नहि शीर्यतेऽस ú ो नहि सज्जतेऽसितो न व्यथते न रिष्यते
विज्ञातारमरेकेन विजानीयात्।''
भूतों का महाभूत के साथ सम्बन्ध तो बताई दिया है कि भूत उसी महाभूत के रूप
हैं। सिर्फ व्यष्टि और समष्टि का विभेद है। मगर है वह सबों की आत्मा ही।
समष्टि होने के कारण ही उसे महाभूत कह दिया है। वह ज्ञान का आगार है।
इसीलिए तो सबों की समझ का प्रश्न हल हो जाता है। जबर्दस्ती कोई कुछ नहीं
करता। जबर्दस्ती या प्रेरणा का सवाल यहाँ हुई नहीं। सभी विवेक से काम लेकर
जिसे उचित समझें उसे करने को स्वतन्त्र हैं। व्यष्टि और समष्टि का ताल्लुक
होने से अक्षर का भूतों के साथ लगाव भी होई गया। दोनों तो एक ही ठहरे। इस
प्रकार चक्र पूरा हो गया। इसी यज्ञचक्र के जारी रखने पर जोर दिया गया है।
इसमें कर्म न कह के यज्ञ कहने या इसे यज्ञचक्र बताने में खूबी यही है कि
लोग यज्ञ की ओर आसानी से आकृष्ट हो जाते हैं। लोगों के दिल-दिमाग में उसका
महत्तव भरा पड़ा जो है। यह बात कर्म के सम्बन्ध में नहीं है, हालाँकि कर्मों
को यज्ञ से अलग नहीं कर सकते। कर्मों से ही यज्ञ सम्पन्न होता है। फिर भी
उसे ऊँचा स्थान मिला है। यह बात भी है कि यज्ञ के भीतर आत्मा, ईश्वर और
ज्ञान भी आ जाते हैं। मगर कर्म कहने से इनका ग्रहण हो नहीं सकता है। यज्ञ
को इतना व्यापक बना दिया है कि उसके भीतर सभी चीजें आ जाती हैं। समाज की
वृद्धि, रक्षा और प्रगति के लिए जो कुछ भी किया जाय वह यज्ञ के भीतर आ जाता
है। आत्मा को नीचे गिरने से रोकना यह बहुत बड़ा यज्ञ है। पतन से उसे बचाना
आवश्यक है। सत्रहवें अध्याेय के छठे श्लोक में जो आत्मा-परमात्मा के कृश
करने की बात कही गयी है या घसीटने की-खींचने की-उसका भी मतलब नीचे
गिराने-गिरने या पतन से ही है। यह बात आसुरी कामों से होती है। इसीलिए उनकी
निन्दा और यज्ञ की प्रशंसा की गयी है। देखिये न, दुनियावी बातों में ऐसे
लोग अपनी एवं ईश्वर की कितनी झूठी कसमें खाते हैं और इस प्रकार अपने आपको
तथा ईश्वर को भी कितना नीचे घसीट लाते हैं!
जैसे भूत का अर्थ है सत्ताधारी, ठीक उसी प्रकार अन्न का अर्थ है जिसे
खाया-पिया जाय या जो औरों को खा-पी जाय-'अद्यतेऽत्ति वा भूतानीत्यन्नम्।'
वृष्टि या पानी की सहायता से जो भी चीजें तैयार हों या शुद्ध हों सभी अन्न
के भीतर आ जाती हैं। वैदिक यज्ञादि से या वैज्ञानिक रीति से जो वृष्टि कराई
जाय, नहर आदि के जरिये या कुएँ से पानी वहाँ पहुँचाया जाय जहाँ जरूरत हो,
वृक्षादि की वृद्धि के जरिये वृष्टि को उत्तोजना दी जाय-क्योंकि यह मानी
हुई बात है कि जंगलों की वृद्धि से पानी ज्यादा बरसता है और काट देने पर
कम-या दूसरा भी जो तरीका अख्तियार किया जाय और जितनी भी वैज्ञानिक
प्रक्रियाएँ सिखाई-पढ़ाई जायँ सभी यज्ञ के भीतर आ जाती हैं। औषधियों के
जरिये, स्वच्छता का खूब प्रसार करके या जैसे हो जल की शुद्धि के सभी उपाय
यज्ञ ही हैं। फिर आगे जो कुछ भी जल के प्रभाव से हमारे काम के लिए-समाज के
लाभ के लिए-किया जाय, बनाया जाय,-फिर चाहे वह शुद्ध हवा हो, खाद्य पदार्थ
हों, जमीन हो, घर हों या दूसरी ही चीजें-सभी अन्न के भीतर आ जाती हैं।
ज्ञान, ध्यालन, समाधि के जरिये जो शक्ति पैदा होती है उससे क्या नहीं होता।
योगसिद्धियों का पूरा वर्णन योगसूत्रों में है। इसलिए यह सब कुछ यज्ञ ही
है। जो भी काम आत्मा, समाज तथा पदार्थों की सर्वांगीण उन्नति के लिए जरूरी
हो उससे चूकना पाप है। यही गीता का उपदेश है, यही यज्ञचक्र का रहस्य है।
(शीर्ष पर वापस)
अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ
अब हमें जरा सातवें अध्याय के अन्त और आठवें के शुरू में कहे गये गीता के
अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का भी विचार कर लेना चाहिए। गीता में
ये बातें पढ़ के सर्वसाधारण की मनोवृत्ति कुछ अजीब हो जाती है। ये शब्द कुछ
ऐसे नये और निराले मालूम पड़ते हैं जैसे विदेशी हों। असल में यज्ञ, भूत,
दैव, आत्मा शब्द या इनके अर्थ तो समझ में आते हैं। इसीलिए इनके सम्बन्ध में
किसी को कभी गड़बड़ी मालूम नहीं होती। मगर अध्यात्म आदि शब्द एकदम नये मालूम
पड़ते हैं। इसीलिए कुछ ठीक जँचते नहीं। यही कारण है कि ये बातें पहेली जैसी
मालूम पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी और ही दुनिया की चीजें हैं।
एक बात और भी है। छान्दोग्य आदि उपनिषदों में अध्याीत्म, अधिभूत और अधिदैव
या आधिदैवत शब्द तो पाये जाते हैं। इसलिए जो उपनिषदों का मन्थन करते और
उनका अर्थ समझते हैं वह इन शब्दोंज के अर्थ गीता में भी समझने की कोशिश कर
सकते हैं, करते हैं। इनके अर्थ भी वे लोग जैसे-तैसे समझ पाते हैं। मगर
अधियज्ञ बिलकुल ही नया है। यह तो उपनिषदों में भी पाया जाता है नहीं। इसलिए
न सिर्फ यह अकेला एक पहेली बन जाता है, बल्कि अपने साथ अध्यात्म आदि को भी
वैसी ही चीज बना डालता है। जब हम अधियज्ञ का ठीक-ठीक आशय समझ नहीं पाते तो
खयाल होता है कि हो न हो, अध्याधत्म आदि भी कुछ इसी तरह की अलौकिक चीजें
हैं। आठवें अध्याहय के 3-4 श्लोकों में जो इनके अर्थ बताये गये हैं उनसे तो
यह उलझन सुलझने के बजाय और भी बढ़ जाती है। जिस प्रकार कहते हैं कि ''मघवा
मूल और विडौजा टीका''। यानी मघवा शब्द का अर्थ किसी ने विडौजा किया सही।
मगर उससे सुननेवालों को कुछ पता ही न लगा। वे तो और भी परेशानी में पड़ गये
कि यह विडौजा कौन सी बला है। मघवा में तो मघ शब्द था जो माघ जैसा लगता था।
मगर विडौजा तो एकदम अनजान ही है। ठीक यही बात यहाँ हो जाती है। ये शब्द तो
कुछ समझ में आते भी हैं, कुछ परिचित जैसे लगते हैं। मगर इनके जो अर्थ बताये
गये हैं वे? वे तो ठीक विडौजा जैसे हैं और समझ में आते ही नहीं।
बेशक यह दिक्कत है। इसलिए भीतर से पता लगाना होगा कि बात क्या है। एतदर्थ
हमें उपनिषदों से ही कुंजी मिलेगी। मगर वह कुंजी क्या है यह जानने के पहले
यह तो जान लेना ही होगा कि अधियज्ञ गीता की अपनी चीज है। गीता में नवीनता
तो हुई। फिर यहाँ भी क्यों न हो ? गीता ने यज्ञ को जो महत्तव दिया है और
उसके नये रूप के साथ जो इसकी नयी उपयोगिता उसने सुझाई है उसी के चलते
अध्यात्म आदि तीन के साथ यहाँ अधियज्ञ का आ जाना जरूरी था। एक बात यह भी है
कि यज्ञ तो भगवत्पूजा की ही बात है। गीता की नजरों में यज्ञ का प्रधान
प्रयोजन है समाज कल्याण के द्वारा आत्मकल्याण और आत्मज्ञान। गीता का यज्ञ
चौबीस घण्टा चलता रहता है यह भी कही चुके हैं। इसलिए गीता ने आत्मज्ञान के
ही सिलसिले में यहाँ अधियज्ञ शब्द को लिख के शरीर के भीतर ही यह
जानना-जनाना चाहा है कि इस शरीर में अधियज्ञ कौन है? बाहर देवताओं को या
तीर्थ और मन्दिर में भगवान् को ढूँढ़ने के बजाय शरीर के भीतर ही यज्ञ-पूजा
मान के गीता ने उसी को तीर्थ तथा मन्दिर करार दे दिया है और कह दिया है कि
वहीं आत्मा-परमात्मा की ढूँढ़ो। बाहर भटकना बेकार है। प्रश्न और उत्तर दोनों
में ही जो 'इस शरीर में'-'अत्र देहेऽस्मिन्' कहा गया है उसका यही रहस्य है।
इस सम्बन्ध में एक बात और भी जान लेना चाहिए। अगस्त कोन्त नामक
फ्रांसीसी दार्शनिक ने तथा और भी पश्चिमी दार्शनिकों ने किसी चीज के और
खासकर समाज और सृष्टि के विवेचन के तीन तरीके माने हैं, जिन्हें पॉजिटिव
(Positive) थियोलौजिकल (Theological) और मेटाफिजिकल (Metaphysical) नाम
दिया गया है। मेटाफिजिक्स अध्या(त्मशास्त्र को कहते हैं, जिसमें
आत्मा-परमात्मा का विवेचन होता है और थियोलौजी कहते हैं, धर्मशास्त्र को,
जिसमें स्वर्ग, नर्क तथा दिव्यशक्ति-सम्पन्न लोगों का, जिन्हें देवता कहते
हैं, वर्णन और महत्तव पाया जाता है। पॉजिटिव का अर्थ है निश्चित रूप से
प्रतिपादित या सिद्ध किया हुआ, बताया हुआ। कोन्त के मत से किसी पदार्थ को
दैवी या आध्याेत्मिक कहना ठीक नहीं है। वह इन बातों को बेवकूफी समझता है।
उसके मत से कोई चीज स्वाभाविक (Natural) भी नहीं कहा जा सकती। ऐसा कहना
अपने आपके अज्ञान का सबूत देना है। किन्तु हरेक दृश्य पदार्थों का जो कुछ
ज्ञान होता है वही हमें पदार्थों के स्वरूपों को बता सकता है और उसी के
जरिये हम किसी वस्तु के बारे में निर्णय करते हैं कि कैसी है, क्या है आदि।
बेशक, यह ज्ञान आपेक्षिक होता है-देश, काल, परिस्थिति और पूर्व जानकारी की
अपेक्षा करके ही यह ज्ञान होता है, न कि सर्वथा स्वतन्त्र। इसी ज्ञान के
द्वारा उसके पदार्थों का विश्लेषण करके जो कुछ स्थिर किया जाता है वही
पॉजिटिव है, असल है, वस्तुतत्तव है। इसी प्रणाली को लोगों ने आधिभौतिक
विवेचन की प्रणाली कहा है। इसे ही मैटिरियलिस्टिक मेथड (Materialistic
method) भी कहते हैं। शेष दो को क्रमश: आधिदैवत एवं आध्यासत्मिक विवेचन
प्रणाली कहते हैं।
आधिदैवत प्रणाली में दिव्य शक्तियों की सत्ता स्वीकार करके ही आगे बढ़ते
हैं। उसमें मानते हैं कि ऐसी अलौकिक ताकतें हैं जो संसार के बहुत से कामों
को चलाती हैं। बिजली का गिरना, चन्द्र-सूर्य आदि का भ्रमण तथा निश्चित समय
पर अपने स्थान पर पहुँच जाना, जिससे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, आदि बातें
ऐसे लोग उस दैवी-शक्ति के ही प्रभाव से मानते हैं। ये बातें मानवीय शक्ति
के बाहर की हैं। हमारी तो वहाँ पहुँच हुई नहीं। सूर्य से निरन्तर ताप निकल
रहा है। फिर भी वह ठण्डा नहीं होता! ऐसा करने वाली कोई दिव्य-शक्ति ही मानी
जाती है। हम किसी चीज को कितना भी गर्म करें। फिर भी खुद बात की बात में वह
ठण्डी हो जाती है। मगर सूर्य क्यों ठण्डा नहीं होता? उसमें ताप कहाँ से आया
और बराबर आता ही क्यों कहाँ से रहता है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर वे लोग यही
देते हैं संसार का काम चलाने के लिए वह ताप और प्रकाश अनिवार्य होने के
कारण संसार का निर्माण करने वाली वह दैवी-शक्ति ही यह सारी व्यवस्था कर रही
है। इसी प्रकार प्राणियों के शरीरों की रचना वगैरह को भी ले सकते हैं। जाने
कितनी बूँदें वीर्य की यों ही गिर जाती हैं और पता नहीं चलता कि क्या हुईं
। मगर देखिये उसी की एक ही बूँद स्त्रीक के गर्भ में जाने से साढ़े तीन हाथ
का मोटा-ताजा, विद्वान् और कलाकार मनुष्य के रूप में तैयार हो जाता है
सिंह, हाथी आदि जन्तु बन जाते हैं! यह तो इन्द्रजाल ही मालूम होता है! मगर
है यह काम किसी अदृश्य हाथ या दिव्य शक्ति का ही। इसलिए उसकी ही
पूजा-आराधना करें तो मानव-समाज का कल्याण हो। वह यदि जरा सी भी नजर फेर दे
तो हम क्या से क्या हो जायँ। शक्ति का भण्डार ही तो वह देवता आखिर है न?
जिस प्रकार आधिभौतिकवादी जड़-पदार्थों की पूजा करते हैं या यों कहिये कि
इन्हीं के अधययन में दिमाग खर्चना ठीक मानते हैं, ठीक वैसे ही आधिदैवतवादी
देवताओं के ही ध्याेन, अन्वेषण आदि को कर्तव्य समझतेहैं।
आध्या्त्मिक पक्ष इन दोनों को ही स्वीकार न करके यही मानता है कि हर चीज की
अपनी हस्ती होती है, सत्ता होती है, अपना अस्तित्व होता है। वही उसकी अपनी
है, स्व है, आत्मा है। उसे हटा लो, अलग कर दो। फिर देखो कि वह चीज कहाँ चली
गयी, लापता हो गयी! मगर जब तक उसकी आत्मा मौजूद है, सत्ता कायम है तब तक
उसमें कितनी ताकतें हैं! बारूद या डिनामाइट से पहाड़ों को फाड़ देते हैं।
बिजली के क्या-क्या करामाती काम नहीं होते! आग क्या नहीं कर डालती!
दिमागदार वैज्ञानिक क्या-क्या अनोखे आविष्कार करते हैं! हाथी पहाड़ जैसा
जानवर कितना बोझ ढो लेता है! सिंह कितनी बहादुरी करता है! मनुष्यों की
हिम्मत और वीरता का क्या कहना! मगर ये सब बातें तभी तक होती हैं जब तक इन
चीजों की हस्ती है, सत्ता है, आत्मा है। उसे हटा दो, सत्ता मिटा दो। फिर
कुछ न देखोगे। अतएव यह आत्मा ही असल चीज है, इसी की सारी करामात है। इसका
हटना या मिटना यही है कि हम इसे देख नहीं पाते। यह हमसे ओझल हो जाती है।
इसका नाश तो कभी होता नहीं, हो सकता नहीं। आखिर नाश की भी तो अपनी आत्मा
है, सत्ता है, हस्ती है। फिर तो नाश होने का अर्थ ही है आत्मा का रहना। यह
भी नहीं कि वह आत्मा जुदा-जुदा है। वह तो सबों में-सभी पदार्थों में-एक ही
है। उसे जुदा करे कौन? जब एक ही रूप, एक ही काम, एक ही हालत ठहरी, तो
विभिन्नता का प्रश्न ही कहाँ उठता है? जो विभिन्नता मालूम पड़ती है वह
बनावटी है, झूठी है, धोखा है, माया है। यह ठीक है कि शरीरों में ज्ञान के
साधन होने से चेतना प्रतीत होती है। मगर पत्थर में यह बात नहीं। लेकिन
आत्मा का इससे क्या? आग सर्वत्र है। मगर रगड़ दो तो बाहर आ जाय। नहीं तो
नहीं! ज्ञान को प्रकट करने के लिए इन्द्रियाँ आग के लिए रगड़ने के समान ही
हैं। इस तरह आध्यानत्मिक पक्षवाले सर्वत्र आत्मा को ही देखते हैं, ढूँढ़ते
हैं। उसे ही परमात्मा मानते हैं।
(शीर्ष पर वापस)
अन्य मतवाद
कुछ लोगों का खयाल है कि इन्हीं आधिभौतिक,
आदिदैवत एवं आध्या त्मिक-तीनों-पक्षों का जिक्र गीता में किया गया है। उनके
मत से गीता का यही कहना है कि हमें इन सभी पक्षों को जानना चाहिए। जिन्हें
मुक्ति लेना है और जन्म-मरण से छुटकारा पाना है उन्हें इन सभी पक्षों का
मन्थन करना ही होगा। वे खामख्वाह इन सबों का मन्थन करते हैं। सातवें अध्याय
के अन्त के जिन दो श्लोकों में ये बातें कही गयी हैं और इसीलिए आठवें के
शुरू में इनके बारे में पूछने का मौका अर्जुन को मिल गया है, उनमें पहले
यानी 29वें श्लोक में तो उनके मत से कुछ ऐसा ही लिखा भी गया है। वह श्लोक
यों है, ''जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदु:
कृत्स्नमधयात्मं कर्म चाखिलम्॥'' इसका अर्थ यह है कि ''जो लोग भगवान् का
आश्रय लेकर जन्म, मरणादि से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं वे उस ब्रह्म
को पूरा-पूरा जान लेते हैं, सभी कर्मों को जान जाते हैं और अध्याकत्म आदि
को भी जानते हैं।'' इससे वे लोग अपना खयाल सही साबित करते हैं।
मगर बात दरअसल ऐसी है नहीं। वस्तुओं के विवेचन के उक्त तीन तरीके हैं सही।
इन्हें लोग अपनी-अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुसार ही अपनाते भी हैं। मगर
यहाँ उन तरीकों तथा प्रणालियों से मतलब हर्गिज है नहीं। यदि इन श्लोकों से
पहले के सिर्फ सातवें अध्याभय के ही श्लोकों पर गौर किया जाय तो साफ मालूम
हो जाता है कि आत्मा-परमात्मा की एकता के ज्ञान का ही वह प्रसंग है। इसीलिए
वही बात किसी न किसी रूप में कई प्रकार से कही गयी है। 16-19 श्लोकों में
तो भक्तों के चार भेदों को गिना के ज्ञानी को ही चौथा माना है और कहा है कि
''ज्ञानी तो मेरी-भगवान् की-आत्मा ही है''-''ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्''
(7।18)। इसकी वजह भी बताते हैं कि ''वह तो हमसे-परमात्मा से-बढ़ के किसी को
मानता ही नहीं और हमीं में डूब जाता है''-''आस्थित: सहि युक्तात्मा
मामेवानुत्तामां गतिम्'' (7।18) लेकिन इसके बाद ही जो यह कहा है कि ''संसार
में जो कुछ है वह सबका सब वासुदेव-परमात्मा-ही है, ऐसा जो समझता है, वह तो
अत्यन्त दुर्लभ महात्मा है''-''वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ:''
(7।19), वह तो बाकी बातों को हवा में मिला देता है। उससे तो स्पष्ट हो जाता
है कि यही एक ही चीज दरअसल जानने की है।
इतना ही नहीं। इसके आगे 20-27 श्लोकों में उन लोगों की काफी निन्दा भी की
गयी है जो दूसरे देवताओं या पदार्थों की ओर झुकते हैं। उनकी समझ घपले में
पड़ी हुई बताई गयी है, ''हृतज्ञाना:'' (7।20)। ''इसीलिए तुच्छ एवं विनाशशील
फलों को ही वे लोग प्राप्त कर पाते हैं।''-''अन्तवत्तुथ फलं तेषां''
(7।23)। भौतिक दृष्टिवालों के बारे में तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे
असली रूप को न जान के ही ऐसे बुद्धिहीन लोग स्थूल रूप में ही हमें देखते
हैं-''अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय:'' (7।24)। आगे के तीन
श्लोकों में इसी बात का स्पष्टीकरण हुआ है। अन्त में तो यहाँ तक कह दिया है
कि रागद्वेष के चलते जो अपने-पराये और भले-बुरे की गलत धारणा हो जाती है
उसी का यह नतीजा है कि लोग इधर-उधर इस सृष्टि के भौतिक पदार्थों में भटकते
फिरते हैं-''इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं
सर्गे यान्ति परन्तप'' (7।27)। इसके विपरीत जिन सत्कर्मियों में यह
रागद्वेषादि ऐब नहीं हैं वे अपने-पराये आदि के झमेले में न पड़ के पक्के
निश्चय एवं दृढ़संकल्प के साथ केवल हमीं-परमात्मा-में रम जाते हैं-''येषां
त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्। ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां
दृढ़व्रता:'' (7।28)। इसी के बाद वे श्लोक आये हैं। तब कैसे कहा जाय कि
उनमें आधिभौतिक आदि विवेचनों पर जोर दिया गया है या ऐसे विवेचनों की
जानकारी अवश्य प्राप्तव्य बताई गयी है?
इसके सिवाय उक्त तीन बातों के अलावा ब्रह्म और कर्म की जानकारी की भी तो
बात वही लिखी है। शंका भी इन दोनों ही के बारे में की गयी है। उत्तर भी
दिया गया है। भला अधियज्ञ को तो उन्हीं तीनों के साथ जैसे-तैसे जोड़ के वे
लोग पार हो जाते हैं। मगर मरने के समय भगवान् की जानकारी कैसे होती है, यह
भी तो एक प्रश्न है। पता नहीं वे लोग इसे किस पक्ष में डालते हैं ऐसा तो
कोई पुराना पक्ष है नहीं। और अधियज्ञवाला पक्ष तो बिलकुल ही नया है। फिर
पुरानों के साथ इसका मेल कैसे होता है? खूबी तो यह है कि उनने 'अधिदेह' नाम
का एक दूसरा भी पक्ष यहीं पर खड़ा कर दिया है और यह ऐसा है कि ''न भूतो न
भविष्यति।'' यदि वे लोग यह समझ पाते कि अध्यायत्म शब्द में जो आत्मा शब्द
है वह देह के ही मानी में है और जहाँ-तहाँ यह शब्द छान्दोग्य, बृहदारण्यक
आदि उपनिषदों या और जगह आया है इसी मानी में आया है, तो शायद अधिदेह की बात
बोलने की हिम्मत ही न करते। ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमारा उनसे यही अनुरोधा
है कि छान्दोग्य के पहले अध्याय का दूसरा, खण्ड बृहदारण्यक के पहले अध्याैय
के पाँचवें ब्राह्मण का 21वाँ मन्त्र तथा कौषीत की उपनिषद् के चौथे अध्याय
के 9-17 मन्त्रों को गौर से पढ़ जायें। तब उन्हें पता लगेगा कि अध्यादत्म
में जो आत्मा शब्द है वह शरीर का ही वाचक है या नहीं।
लेकिन जब कर्म, ब्रह्म और मरण काल का ब्रह्मज्ञान किसी पुराने पक्ष की चीज
नहीं है तो फिर अध्यानत्म वगैरह को ही क्यों पुराने पक्ष में घसीटा जाय? और
इन पक्षों को जानने से लाभ ही क्या? किसी विश्वविद्यालय की न तो परीक्षा ही
देनी है और न कोई उपाधि ही लेनी है। कोई पुस्तक भी नहीं लिखनी है कि
पाण्डित्य का प्रदर्शन किया जायगा या खण्डन-मण्डन ही होगा, जिसके लिए इन
अनेक पक्षों की जानकारी जरूरी हो जाती है। यहाँ तो ब्रह्मज्ञान और मोक्ष का
ही सवाल है। सो भी मरणकाल की जानकारी की बात उठा के यह भी जनाया है कि
विशेष रूप से मरण समय के लिए जरूरी बातें यहाँ बता दी गयी हैं। यही कारण है
कि चार श्लोकों में ये बातें खत्म करके पाँचवें के ही 'अन्तकाले च' आदि
शब्दों से शुरू करके उसी अन्तकाल या मरण समय की ही बातें अन्त तक लिखी गयी
हैं। तरीका भी बताया गया है कि किस प्रकार उस समय आत्मा और ब्रह्म का
साक्षात्कार होता है। मरने पर लोग किन-किन रास्तों से हो के जाते हैं यह
बात भी अन्त में कही गयी है। ऐसी हालत में आधिभौतिक आदि मतवादों का तो यहाँ
अवसर ही नहीं है। इसीलिए मानना पड़ता है कि इन बखेड़ों से यहाँ कोई भी मतलब
नहीं है।
(शीर्ष पर वापस)
अपना पक्ष
असल बात यह है कि प्राचीन समय में कुछ ऐसी
प्रणाली थी कि हम क्या हैं, यह संसार क्या है और हमारा इसके साथ सम्बन्ध
क्या है, इन्हीं तीन प्रश्नों को लेकर जो अनेक दर्शनों की विचारधाराएँ हुई
थीं और आत्मा-परमात्मा आदि का पता लगा था, या यों कहिए कि इनकी कल्पना की
गयी थी, उन्हीं में एक व्यावहारिक या अमली धारा ऐसी भी थी कि उसके
माननेवाले निरन्तर चिन्तन में लगे रहते थे। उनकी बात कोई शास्त्री य-विवेचन
की पद्धति न थी। वे तो खुद दिन-रात सोचने-विचारने एवं ध्या न में ही लगे
रहते थे। इसीलिए हमने उनकी धारा या प्रणाली को अमली और व्यावहारिक
(Practical) कहा है। इस प्रणाली के सैद्धान्तिक पहलू पर लिखने-पढ़ने या
विवाद करने वाले भी लोग होंगे ही। मगर हमारा उनसे मतलब नहीं है और न गीता
का ही है। गीता में तो अमली बात का वह प्रसंग ही है। वही बात वहाँ चल रही
है। आगे भी मरण समय की बात आ जाने के कारण अमली या व्यावहारिक चीज की ही
आवश्यकता हो जाती है। मरणकाल में कोरे दार्शनिकवादों से सिवाय हानि के कुछ
मिलने-जुलनेवाला तो है नहीं।
ऐसे लोगों ने दृश्य-बाहरी-संसार को पहले दो भागों में बाँटा। पहले भाग में
रखा अपने शरीर को। अपने शरीर से अर्थ है चिन्तन करनेवालों के शरीर से। फिर
भी इस प्रकार सभी जीवधारियों के शरीर, या कम से कम मनुष्यों के शरीर इस
विभाग में आ जाते हैं। क्योंकि सोचने-विचारने का मौका तो सभी के लिए है।
हालाँकि एक आदमी के लिए दूसरों के भी शरीर वैसे ही हैं जैसे अन्न, वस्त्र,
पृथिवी, वृक्ष आदि पदार्थ। शरीर के अतिरिक्त शेष पदार्थों को भूत या भौतिक
माना गया। पीछे इन भौतिक पदार्थों के दो विभाग कर दिये गये। एक तो ऐसों का
जिनमें कोई खास चमत्कार नहीं पाया जाता। इनमें आ गये वृक्ष, पर्वत, नदी,
समुद्र, पृथिवी आदि। दूसरा हुआ उन पदार्थों का जिनमें चमत्कार पाया गया।
इनमें आये चन्द्र, सूर्य, विद्युत आदि। इस प्रकार शरीर, पृथिवी आदि सूर्य
प्रभृति, इन तीन विभागों में दृश्य संसार को बाँट दिया गया। शुरू में तो
शरीर के सिवाय आत्मा, स्व, या निज नाम की और चीज का पता था नहीं। इसलिए
शरीर को ही आत्मा भी कहते थे। पृथिवी आदि स्थूल पदार्थों को, जिनमें
चमत्कार या दिव्य-शक्ति नहीं देखी गयी, भूत कहने लगे। भूत का अर्थ है ठोस।
इन्हें छू के इनका ठोसपन जान सकते थे। मगर जो आदमी की पहुँच के बाहर के
सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, आदि पदार्थ थे उन्हें देवता, देव या दिव्य कहते
थे। इनके ठोसपन का पता तो लगा सकते न थे। ये चीजें आकाश में ही नजर आती
हैं। इसलिए आकाश को भी दिव् या द्यु कहते थे। वह ठोस भी तो नहीं है। जिस
स्वर्ग नामक स्थान में इन दिव्य पदार्थों का निवास माना गया वह भी दिव् या
द्यु कहा जाने लगा।
इस प्रकार आत्म या आत्मा, भूत और देव या देवता इन-तीन-विभागों के हो जाने
के बाद सोचने-विचारने, चिन्तन या ध्याान की प्रक्रिया आगे बढ़ी। आगे चल के
शरीर के विश्लेषण करने पर इन्द्रिय प्राण, बुद्धि आदि को शरीर से स्वतन्त्र
स्वीकार करना पड़ा। भौतिक शरीर को छोड़ देने के बाद भी इन्द्रिय, प्राणादि
रहते हैं। तभी तो जन्म, मरण, पुनर्जन्म आदि की बात मानी जाती है। यदि ये
अलग न होते तो कौन जाता, कौन आता और किसका जन्म बार-बार होता? फलत: आत्मा
या शरीर में रहने के कारण ही इन्द्रियादि को अध्याित्म कहा गया। उपनिषदों
में यही बात रह-रह के लिखी पायी जाती है। पाणिनीय व्याकरण के अव्ययीभाव
समास के नियमानुसार यही अर्थ भी अध्यात्म शब्द का है कि आत्मा में रहने
वाला। 'अधि' को अव्यय कहते हैं। उसी का आत्म शब्द के साथ समास हो के
अध्यात्म बना है। फिर कालान्तर में जब अन्वेषण और भी आगे बढ़ा तो शरीर,
इन्द्रियादि से अलग आत्मा नामक एक अजर-अमर पदार्थ की कल्पना हुई। उसकी भी
जानकारी तो शरीर में ही होती है। उसे भी इसीलिए अध्या-त्म कह दिया। उसी
आत्मा को जब परमात्मा मान लिया और इसका विवेचन भी किया गया तो सभी विवेचनों
को अध्यात्मशास्त्र, आध्या त्मिकशास्त्र या आध्याऔत्मिक विवेचन नाम दिया
गया।
इसी प्रकार भौतिक पदार्थों या भूतों का भी विश्लेषण एवं विवेचन किया गया और
उनमें जो रूप, रस, गन्ध आदि खूबियाँ या विशेषताएँ पायी गयीं उन्हें अधिभूत
कहा गया। वे भूतों में ही जो पायी गयीं। कुछ अन्वेषणकर्ता यहीं टिक गये और
आगे न बढ़े। दूसरे लोग आगे बढ़े और इन भूतों में भी सत्ता, अस्तित्व आदि जैसी
चीजों का पता लगाया। इनके बारे में हमने पहले ही बहुत कुछ कहा है। इसी
प्रकार देव या देवता कहे जाने जानेवालों की भी जाँच-पड़ताल होती रही। भूतों
के अन्वेषण होने पर जिन पदार्थों को अधिभूत कहा गया उनके सम्बन्ध के विवेक,
विचार और मन्थन आदि को ही आधिभौतिक नाम दिया गया। इसी तरह देवों या देवताओं
में जो भी विभूति, खूबी, चमक, आभा वगैरह जान पड़ी उसे अधिदेव, अधिदैव या
अधिदैवत नाम दिया गया। तत्सम्बन्धीी चिन्तन, ध्या न या विवेचन भी आधिदैवत,
आधिदैव या आधिदैविक कहा जाने लगा। पीछे तो लोगों ने अधिभूत और अधिदैव को एक
में मिलाके सबों के भीतर एक अन्तर्यामी पदार्थ को मान लिया, जो सबों को
चलाता है, कायम रखता है, व्यवस्थित रखता है। उसी अन्तर्यामी को ब्रह्म या
परमात्मा कहने लगे। सबसे बड़ा होने के कारण ही उसे ब्रह्म कहना शुरू किया।
शरीर के भीतरवाली आत्मा को व्यष्टि मान के ब्रह्म को परमात्मा, बड़ी आत्मा
या समष्टि आत्मा कहने की रीति चल पड़ी।
ऊपर हमने जो कुछ लिखा है वह शुरू से लेकर आज तक की स्थिति का संक्षिप्त
वर्णन है। शुरू से ही यह हालत तो थी नहीं। यह परिस्थिति तो क्रमिक विकास
होते-होते पैदा हो गयी है। जब स्वतन्त्र रूप से लोगों का चिन्तन चलता था तो
कोई अध्या-त्म-विमर्श में लगे थे, कोई अधिदैव-विचार में और कोई
अधिभूत-विवेचन में। यह तो सम्भव न था कि सभी लोग सभी बातें सोच सकें। तब तो
सभी बातें अधूरी ही रह जातीं। कोई भी पूरी न हो पाती, अन्त तक पहुँच पाती
नहीं। और ज्ञान की वृद्धि के लिए वह अधूरापन सर्वथा अवांछनीय है, त्याज्य
है। यही कारण है कि अलग-अलग सोचने वाले अपने-अपने कामों में लीन थे। यही
कारण है कि जब तक सब लोग गोष्ठी या परस्पर विमर्श नहीं कर लेते थे तब तक
अनेक स्वतन्त्र निश्चयों पर पहुँचते थे। यह बात स्वाभाविक थी। श्वेताश्वतर
उपनिषद् के पहले ही दो मन्त्रों 'ब्रह्मवादिनो वदन्ति, किं कारणं ब्रह्म
कुत: स्म जाता:' आदि, तथा 'काल: स्वभावो नियतिर्यदृच्छा' आदि में यही मतभेद
और विचारभेद बताया गया है। साथ ही सभी सोचने वालों को ब्रह्मवादी ही कहा
है, न कि किसी को भी कमबेश। उसी के छठे अध्याय के पहले मन्त्र में भी इसी
प्रकार के विचार-विभेद का उल्लेख 'स्वभावमेके कवयो वदन्ति' आदि के द्वारा
किया है। वहाँ सबों को कवि या सूक्ष्मदर्शी कहा है। छान्दोग्य के छठे
अध्याय के दूसरे खण्ड के पहले ही मन्त्र में ''सदेव सोम्येदमग्र
आसीदेकमेवाद्वितीयम् तध्दैक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्'' आदि के
जरिये यही विचार विभिन्नता बताई गयी है और अगले 'कुतस्तु खलु' मन्त्र में
इसी का खण्डन-मण्डन लिखा गया है। फलत: विभिन्न विचारों के प्रवाह होने
जरूरी थे।
वैसी हालत में जो परम कल्याण या मोक्ष की आकांक्षा रखता हो उसके दिल में यह
बात स्वभावत: उठ सकती है कि कहीं धोखा और गड़बड़ न हो जाय; कहीं ऐसा रास्ता न
पकड़ लें कि या तो भटक जायँ या परेशानी में पड़ जायँ; कहीं ऐसे मार्ग में न
पड़ें जो अन्त तक पहुँचने वाला न हो के मुख्य मार्ग से जुटने वाली पगडण्डी
या छोटी-मोटी सड़क हो; राजमार्ग के अलावा कहीं दूसरे ही मार्ग के पथिक न बन
जायँ; कहीं ऐसा न हो कि मार्ग तो सही हो, मगर उसके लिए जरूरी सामान सम्पादन
करने वाले उपाय या रास्ते छूट जायँ और सारा मामला अन्त में खटाई में पड़
जाय। जो सभी विचारपद्धतियों एवं चिन्तनमार्गों को बखूबी नहीं जानते और न
उनके लक्ष्य स्थानों का ही पता रखते हैं उनके भीतर ऐसी जिज्ञासा का पैदा
होना अनिवार्य है। जिन्हें सभी विचार प्रवाहों का समन्वय या एकीकरण विदित न
हो और जो यह समझ सके न हों कि पुष्पदन्त के शब्दों में रुचि या प्रवृत्ति
के अनुसार अनेक मार्गों को पकड़ने वाले अन्त में एक ही लक्ष्य तक-परमात्मा
तक-पहुँचते हैं-''रुचीनां वैचित्रयादृजुकुटिलनानापथ जुषाम्, नृणामे को
गम्यवत्वमसि पयसामर्णव इव,'' वे तो घबरा के सवाल करेंगे ही कि ''परमात्मा
का ध्यानन तो हम करेंगे सही, लेकिन अध्याात्म, अधिदैव, अधिभूत का क्या
होगा? उनकी जानकारी हमें कैसे होगी? यदि न हो तो कोई हानि तो नहीं?''
सबसे बड़ी बात यह है कि उस काम में फँस जाने पर कर्मों से तो अलग हो जाना ही
होगा। यह तो संभव नहीं कि ध्या न और समाधि भी करें और कर्मों को भी पूरा
करें। ऐसी दशा में संसार का एवं समाज का कल्याण कहीं गड़बड़ी में न पड़ जाय यह
खयाल भी परेशान करेगा ही। उनका यह काम ऐसे मंगलकारी कर्मों के भीतर तो शायद
ही आये। कम से कम इसके बारे में उन्हें सन्देह तो होगा ही। फिर काम कैसे
चलेगा? और अगर जानकार लोग ही समाज के लिए मंगलकारी कामों को छोड़ के अपने ही
मतलब में-अपनी ही मुक्ति के साधन में-फँस जायँ, तो फिर संसार की तो खुदा ही
खैर करे। तब तो संसार पथदर्शन के बिना चौपट ही हो जायगा। इसके अतिरिक्त
यज्ञवाला प्रश्न भी उन्हें परेशान करेगा। जब पहले ही कहा जा चुका है कि
''यज्ञों के बिना तो यहीं खैरियत नहीं होती, परलोक का तो कुछ कहना ही
नहीं''-''नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य: कुरुसत्ताम'' (4।31), तो काम
कैसे चलेगा? तब तो सब खत्म ही समझिये। यज्ञ के ही बारे में एक बात और भी उठ
सकती है। यदि कहा जाय कि यज्ञ तो व्यापक चीज है। अतएव ध्याञन और समाधि के
समय भी होता ही रहता है, तो सवाल होता है कि यज्ञ में असल लक्ष्य, असल
ध्येय कौन है जिसे सन्तुष्ट किया जाय? कहीं वह कोई दूसरा तो नहीं है।
ज्ञान, ध्यालन तो शरीर के भीतर ही होता है और यह यदि यज्ञचक्र में आ गया तब
तो अच्छी बात है। तब तो बीमारी, दुर्बलता, अशक्ति और मरणावस्था में भी यह
हो सकता है। इसलिए तब खासतौर से यह जानना जरूरी हो जाता है कि शरीर के भीतर
जब यज्ञ होता है तो उससे किसकी तृप्ति होती है, कौन सन्तुष्ट होता है? कहीं
नास्तिकों की तरह खाओ-पिओ, मौज करो की बात तो नहीं होती और केवल अपना ही
सन्तोष तो नहीं होता? असल में उस यज्ञ से परमात्मा तक पहुँचते हैं या नहीं
यही प्रश्न है। इसीलिए देह के भीतर ही अधियज्ञ को जानने की उत्कण्ठा हुई
है। क्योंकि सबसे महत्तवपूर्ण चीज यही है और सबसे सुलभ भी। मगर यदि इससे
इन्द्रियादि की ही पुष्टि हुई तो सारा गुड़ गोबर हो जायगा। इसीलिए सभी
प्रश्न किये गये हैं। यह ठीक है कि सातवें अध्याुय के अन्त में कृष्ण ने कह
दिया है कि वह ज्ञान सर्वांगपूर्ण है-इसमें कोई कमी नहीं है; क्योंकि
अधिभूत आदि को भी ऐसा पुरुष बखूबी जानता है। लेकिन जब तक अर्जुन को पता न
लग जाय कि आखिर ये अधिभूत आदि हैं क्या, तब तक सन्तोष हो तो कैसे? इसलिए
आठवें के शुरू में उसने यही पूछा है, यही प्रश्न किये हैं।
उनके उत्तर भी ठीक वैसे ही हैं जिनसे पूछने वाले को पूरा सन्तोष हो जाय।
मरने के समय भगवान् को जानने की जो उत्कण्ठा दिखाई गयी थी उसका सम्बन्ध
अधियज्ञ से ही है। इसीलिए उसे उसके बाद ही रखा है और उसका उत्तर शेष समूचे
अध्याधय में दिया गया है। क्योंकि सब प्रश्नों का मतलब चौपट हो जाय, यदि वह
बात न हो सके। अर्जुन को यह भी खयाल था कि कृष्ण कहीं अपने आपकी ही भक्ति
की बात न करते हों, और इस प्रकार ब्रह्मज्ञान से नाता ही न रह जाने पर
कल्याण में बाधा न पड़ जाय। इसीलिए अर्जुन ने पूछा कि आखिर वह ब्रह्म क्या
है? आपसे या ईश्वर से अलग है या एक ही चीज? उसका यह भी खयाल था कि कहीं
ब्रह्म या परमात्मा भी वैसा ही चन्दरोजा न हो जैसी यह दुनिया। तब तो मुक्ति
का यत्न ही बेकार हो जायगा। हिरण्यगर्भ को भी तो ब्रह्मा या ब्रह्म कहते
हैं और उसका नाश माना जाता है। यही कारण है कि उस ब्रह्मा से पृथक् परम
अक्षर या अविनाशी ब्रह्म का निरूपण आगे किया गया है। वहाँ बताया गया है कि
क्यों ब्रह्मा का नाश होता है और कैसे, लेकिन अक्षर ब्रह्म का क्यों नहीं?
उत्तर से सभी बातों की पूरी सफाई हो जाती है। परम अक्षर को ब्रह्म कहा है।
असल में पन्द्रहवें अध्याय के 'द्वाविमौ पुरुषौ लोके' (16) श्लोक में जीव
को भी अक्षर कहा है। इसीलिए परम आत्मा-परमात्मा-की ही तरह यहाँ परम अक्षर
कहने से परमात्मा का ही बोध होता है। नहीं तो गड़बड़ होती।
अध्यात्म को स्वभाव कहा है। ब्रह्म के बाद स्वभाव शब्द आने से इसमें स्व का
अर्थ वही ब्रह्म ही है। उसी का भाव या स्वरूप स्वभाव कहा जाता है। अर्थात्
अध्याात्म, जीव या आत्मा ब्रह्म का ही रूप है। गीता में स्वभाव शब्द कई जगह
आया है। अठारहवें अध्याय के 41-44 श्लोकों में कई बार यह शब्द प्रकृति या
गुणों के अनुसार दिल-दिमाग की बनावट के ही अर्थ में आया है। उसी अध्यातय के
60वें श्लोक वाले का भी वही अर्थ है। पाँचवें अध्याेय के 'नर् कत्ताव्यं'
(14) श्लोक में जो स्वभाव है उसका अर्थ है सांसारिक पदार्थों या सृष्टि का
नियम। मगर जैसे अठारहवें अध्याय के स्वभाव शब्द में स्व का अर्थ है गुण और
तदनुसार रचना, उसी तरह पाँचवें अध्याय में स्व का अर्थ है इसके पहले के
सांसारिक पदार्थ, जिनका जिक्र उसी श्लोक में हैं। सातवें अध्याय के ही
20वें श्लोक में जो भाव शब्द है उसका अर्थ है पदार्थ या हस्ती-अस्तित्व।
ठीक उसी प्रकार इस श्लोक में भी स्वभाव का अर्थ हो जाता है ब्रह्म का भाव,
अस्तित्व या रूप। दूसरा अर्थ ठीक नहीं होगा।
कम का जो स्वरूप बताया गया है वह भी व्यापक है। ''भूतभावोद्भवकरो विसर्ग:''
यही उसका स्वरूप है। इसका अर्थ है जिससे पदार्थों का अस्तित्व, वृद्धि या
उत्पत्ति हो उस त्याग, जुदाई या पार्थक्य को कर्म कहते हैं। यहाँ विसर्ग
शब्द और सातवें के 27वें का सर्ग शब्द मिलते-जुलते हैं। संस्कृत के धातुपाठ
में जो धातुओं का अर्थ लिखा गया है वहाँ सृज धातु का विसर्ग ही अर्थ लिखा
है। पहले कह चुके हैं कि 'तपाम्यमहं वर्षं' (9।19) श्लोक में उत्सृजामिका
जो उत्सर्ग अर्थ है वही विसर्ग का भी है। दोनों में सृज धातु ही है।
वर्णमाला में आखिर अक्षर जो स्वरगणना में पाया जाता है उसे भी विसर्ग एवं
विसर्जनीय कहते हैं। ब्राह्मणग्रन्थों में 'वैसर्जन होम' आता है। वहाँ भी
विसर्जन का अर्थ है समाप्ति या खात्मा, या छोड़ देना। स्वरों का अन्त होने
के कारण ही विसर्ग आखिरी स्वरवर्ण है। वहाँ भी उस सिलसिले का अन्त है।
मल-मूत्रदि के त्याग या वीर्यपात को भी विसर्ग कहते हैं। सारांश यह है कि
जिस चीज के छोड़ने, अलग करने, पूरा करने, प्रयोग करने, त्यागने से सृष्टि की
उत्पत्ति, रक्षा, वृद्धि आदि हो सके वही कर्म है। इस प्रकार इस व्यापक अर्थ
में ज्ञान, ध्या्न, समाधि वगैरह का भी समावेश हो जाता है और इस तरह
प्रश्नकर्ता का शक जाता रहता है। यह कम कल्याणकारी चीजें नहीं हैं। गीता का
कर्म कोई पारिभाषिक या खास ढंग की चीज नहीं है, यही आशय है।
'अधिभूतं क्षरोभाव:' का अर्थ है कि पदार्थों का जो क्षर स्वरूप है, या यों
कहिए कि उनकी विनाशिता है वही अधिभूत है। भाव शब्द तीन बार इतनी ही दूर में
आ गया है और तीनों का एक ही अर्थ है सत्ता, अस्तित्व या रूप। पहले कह चुके
हैं कि आखिर दृश्यजगत् या भौतिक पदार्थों में जो विनाशिता है वह तो अजर-अमर
है। यदि वह ऐसी न हो और सदा रहने वाली न हो तो पदार्थ ही अविनाशी बन जायें।
इसीलिए वही उनका असली रूप है, स्व है, आत्मा है। आत्मा को तो गीता ने
बार-बार अविनाशी कहा है। इस सम्बन्ध में वृहदारण्यक का वचन भी पहले ही लिखा
जा चुका है। इस प्रकार अधिभूत भी आत्मा या परमात्मा से जुदा नहीं है। मगर
उसे जिस ढंग से कहा है उसमें सुन्दर दार्शनिकता पायी जाती है। इसी अध्यातय
के 20वें श्लोक में भाव शब्द जिस अर्थ में आया है वही अर्थ यहाँ भी
है-पदार्थों का असल मूल वही है जिसे आत्मा या परमात्मा कहते हैं।
'पुरुषश्चाधिदैवतम्' का अर्थ है कि 'पुरुष ही अधिदैवत है।' गीता के
'द्वाविमौ पुरुषौ' श्लोक की बात कह चुके हैं। उसमें पुरुष आता है। उसी में
'क्षर: सर्वाणि भूतानि' भी लिखा है, जिससे अधिभूत का अर्थ साफ होता है। मगर
प्रकृति तथा जीव दोनों को ही पुरुष कहा गया है, यह बात याद रखने की है।
उससे आगे के 17वें श्लोक में 'उत्ताम: पुरुष:' शब्दों में परमात्मा को
उत्ताम पुरुष या दोनों से ही पृथक् बताया है और 18वें में उसी को
पुरुषोत्ताम भी कहा है। इससे सिद्ध हो जाता है कि आधिदैवत भी वही परमात्मा
या पुरुष है और है वह सभी का स्वरूप 'वासुदेव: सर्वम्।'
अन्त में 'अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे' के द्वारा यह कह दिया है कि
मैं-परमात्मा-ही सभी शरीरों के भीतर अधियज्ञ हूँ। जो दिन-रात,
श्वास-प्रश्वास, खानपान, निद्रा, बोलचाल, विचार, ध्यासन आदि के रूप में
'यत् करोऽषि यदश्नासि' (9।27) के अनुसार अखण्ड यज्ञ जारी है उससे भगवान् की
ही पूजा हो रही है, यही इसका आशय है। यह पूजा सुलभ और सुकर है। फलत: चिन्ता
का अवसर रही नहीं जाता।
सातवें अध्याय के अन्तिम-29, 30-श्लोकों में जो कुछ कहा है वह भी हमारे
पूर्व के बताये इसी अर्थ का पोषक है। उन दोनों श्लोकों का पूरा विचार किया
जाये तो यही अभिप्राय व्यक्त होता है कि जन्म-मरण आदि के संकटों से छुटकारा
सदा के लिए पा जाने के विचार से जो लोग भगवान् में ही रमते और यही काम करते
हैं वह उस पूर्ण ब्रह्म को भी जानते हैं, अध्यात्म को भी और सभी कर्मों को
भी। अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के रूप में भी भगवान् को वही जानते हैं।
इसीलिए पूर्ण योगी होने के कारण मरण समय में भी परमात्मा को साक्षात् जान
लेते हैं। दूसरे शब्दों में इसका आशय यह है कि जो लोग अधिभूत, अधिदैव,
अधियज्ञ, अध्याहत्म, ब्रह्म और कर्म को जानते हैं वही परमात्मा को अन्त में
भी जानते हैं। वही जरामरण-जन्ममरण-से छुटकारा पाने का यत्न भी ठीक-ठीक करते
हैं। हर हालत में जानने से ही मतलब है; न कि शास्त्री य पद्धति एवं
वादविवाद से। ये सभी एक ही चीज हैं यह इससे साफ हो जाता है। 'एकै साधो सब
सधौ' भी चरितार्थ हो जाता है। इसलिए भगवान् में रमनेवाले के लिए चिन्ता की
कोई गुंजाइश रह जाती नहीं।
एक ही बात और कहके इस लम्बे विवेचन को पूरा करेंगे। जिस सातवें अध्याय में
अध्यारत्म आदि आये हैं और आठवें तक चले गये हैं उसके शुरू का ही श्लोकऐसा
है, ''ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत:। यज्ज्ञात्वा नेह
भूयोन्यज्ज्ञातव्यम विशिष्यते'' (7।2)। इसका भाव यह है कि ''हम तुम्हें
ज्ञान-विज्ञान दोनों ही बतायेंगे, सो भी पूरा-पूरा। उसके बाद तो कुछ जानना
बाकी रही नहीं जायेगा।'' इससे यह स्पष्ट होता है कि आगे जो कुछ कहा गया है
वह ज्ञान और विज्ञान के ही सिलसिले में विस्तार के साथ आया है। ज्ञान और
विज्ञान की बात यहीं से शुरू हो के सत्रहवें अध्याय के अन्त तक पायी जाती
है। अठारहवें में भी बहुत कुछ वही है। सातवें अध्याय का तो नाम ही है
ज्ञान-विज्ञान योग। नवें अध्याय के पहले श्लोक में भी 'ज्ञानंविज्ञानसहितं'
आया ही है। इस पर आगे और भी लिखेंगे। लेकिन ज्ञान-विज्ञान की बात चालू है
यह तो मानना ही होगा। उसी प्रसंग से अध्याखत्म आदि आये हैं यह
भीनिर्र्विवाद है।
और यह ज्ञान एवं विज्ञान है क्या चीज? ज्ञान तो है जानकारी या अनुभव और
उसमें जब विशेषता या खूबी आ जाय तो वह हुआ विज्ञान। किसी ने हमें कह दिया
या हमने कहीं पढ़ लिया कि सफेद और पीले रंगों को मिला के लाल तैयार करते
हैं। यही हुआ लाल रंग के बारे में ज्ञान। इसे सामान्य जानकारी भी कह सकते
हैं। मगर जब हमने खुद दोनों रंगों को मिला के लाल रंग तैयार कर लिया और
उसकी पूरी जानकारी हासिल कर ली, तो वही हो गया विज्ञान। दूसरा दृष्टान्त
लीजिए। कहीं पढ़ लिया या जान लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक हवाओं को
विभिन्न अनुपात में मिलाने से ही जल तैयार हो जाता है। यह ज्ञान हुआ। और जब
किसी प्रयोगशाला में जा के हमने इसका प्रयोग खुद करके देख लिया या दूसरों
से प्रयोग करा लिया तो वही विज्ञान हुआ। विज्ञान से वस्तु के रगरेशे की
जानकारी हो जाती है।
प्रकृत में भी यही बात है। यों ही आत्मा-परमात्मा या जीव-ब्रह्म और संसार
की बात कह देने से काम नहीं चलता। वह बात दिल में बैठ पाती नहीं। यदि
बैठाना है तो उसका प्रयोग करके देखना होगा-यह देखना होगा कि किस पदार्थ से
कौन कैसे बनता है, रहता है, खत्म होता है। यदि परमात्मा ही सब कुछ है तो
कैसे, इसका विश्लेषण करना होगा। जब तक ब्योरेवार सभी चीजों को अलग-अलग करके
न देखेंगे तब तक हमारा ज्ञान पक्का न होगा, विज्ञान न होगा, दिल में बैठेगा
नहीं। फलत: उससे कल्याण न होगा। इसीलिए अध्यात्म, अधिभूत आदि विभिन्न रूपों
में आत्मा या परमात्मा का जानना जरूरी हो जाता है और इसीलिए उसका उल्लेख
आया है। बिना इसके जिज्ञासुओं को सन्तोष कैसे हो?
इसीलिए सातवें के आखिरी-30वें-श्लोक का जो लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि भगवान्
के ज्ञान के साथ ही अधिभूत आदि का पृथक् ज्ञान होना चाहिए, यही गीता की
मंशा है, वह भूलते हैं। वहाँ तो सबों को परमात्म स्वरूप ही-'वासुदेव:
सर्वमिति'-जानना है। ब्रह्म तथा अधियज्ञ को तो परमात्म-रूप साफ ही कहा है।
जीव-अध्यावत्म-भी तो वही है। हाँ, कर्म शायद अलग हो। मगर वह तो व्यापक है।
फलत: अन्ततोगत्वा वह भी जुदा नहीं है।
गीता - 5
(शीर्ष पर वापस)
|