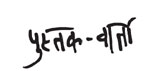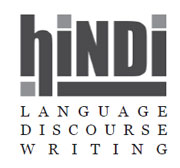|
स्वामी
सहजानन्द सरस्वती रचनावली
सम्पादक
-
राघव शरण शर्मा
खंड-3
(गीता हृदय)
पहला-अन्तरंग भाग : 4. कर्मवाद
और अवतारवाद
|
मुख्य सूची |
खंड - 1 |
खंड - 2 |
खंड - 3 |
खंड - 4 |
खंड - 5 |
खंड - 6 |
4. कर्मवाद और अवतारवाद
ईश्वरवाद
कर्मवाद
|
कर्मों के भेद और उनके काम
अवतारवाद
...अगला पृष्ठ
|
|
4.
कर्मवाद और अवतारवाद
गीता
की अपनी निजी बातों पर ही अब तक प्रकाश डाला गया है। मगर गीता में कुछ ऐसी
बातें भी पायी जाती
हैं,
जो उसकी खास अपनी न होने पर भी उनके वर्णन में विशेषता
है, अपनापन है, गीता
की छाप लगी है। वे बातें तो
हैं
दार्शनिक। उन पर दर्शनों ने खूब माथापच्ची की है,
वाद-विवाद किया है। गीता ने उनका उल्लेख अपने मतलब से
ही किया है। लेकिन खूबी उसमें यही है कि उन पर उसने अपना रंग चढ़ा दिया है,
उन्हें अपना जामा पहना दिया है। गीता की निरूपणशैली
पौराणिक है। इसके बारे में आगे विशेष लिखा जायेगा। फलत: इसमें पौराणिक
बातों का आ जाना अनिवार्य था। हालाँकि ज्यादा बातें इस तरह की नहीं आयी
हैं।
एक तो कुछ ऐसी
हैं
जिन्हें ज्यों की त्यों लिख दिया है। इसे दार्शनिक भाषा में अनुवाद कहते
हैं।
वैसा ही लिखने का प्रयोजन कुछ और ही होता है। जब तक वे बातें लिखी न जायें
आगे का मतलब सिद्ध
हो पाता नहीं। इसलिए गीता ने ऐसी बातों का उपयोग अपने लिए इस तरह कर लिया
है कि उनके चलते उसके उपदेश का प्रसंग खड़ा हो गया है।
मगर ऐसी
भी एकाध पौराणिक बातें आयी हैं जिन्हें उसने सिद्धान्त के तौर पर,
या
यों कहिए कि एक प्रकार से अनुमोदन के ढंग पर लिखा है। वे केवल अनुवाद नहीं
हैं। उनमें कुछ विशेषता है,
कुछ तथ्य है। ऐसी ही एक बात अवतारवाद की है। चौथे अध्याय के
5-10
श्लोकों में यह बात आयी है और बहुत ही सुन्दर ढंग से आयी है। यह यों ही कह
नहीं दी गयी है। लेकिन गीता की खूबी यही है कि उस पर उसने दार्शनिक रंग चढ़ा
दिया है। यदि हम उन कुल छह श्लोकों पर गौर करें तो साफ मालूम हो जाता है कि
पुराणों का अवतारवाला सिद्धान्त दार्शनिक साँचे में ढाल दिया गया है। फलत:
वह हो जाता है बुद्धिग्राह्म। यदि ऐसा न होता,
तो
विद्वान् और तर्क-वितर्क करने वाले पण्डित लोग उसे कभी स्वीकार नहीं कर
सकते। मजा तो यह है कि दार्शनिक साँचे में ढालने पर भी वह रूखापन,
वह
वाद-विवाद की कटुता आने नहीं पायी है जो दार्शनिक रीतियों में पायी जाती
है। सूखे तर्कों और नीरस दलीलों की ही तो भरमार वहाँ होती है। वहाँ सरसता
का क्या काम?
दार्शनिक तो केवल वस्तुतत्तव के ही खोजने में परेशान रहते हैं। उन्हें
फुर्सत कहाँ कि नीरसता और सरसता देखें?
(शीर्ष पर वापस)
ईश्वरवाद
हम उसी
चीज पर यहाँ विशेष प्रकाश डालने चले
हैं।
लेकिन उस अवतारवाद की जड़ में कर्मवाद है और है यह दार्शनिकों की चीज। गीता
ने उसी को ले लिया है इसलिए जब तक कर्मवाद का विवेचन नहीं कर लिया जाता,
अवतारवाद का रहस्य समझ में आ सकता नहीं। यही कारण है कि
हम पहले कर्मवाद की ही बात उठाते
हैं।
यह कर्म का सिद्धान्त
किसी न किसी रूप में अन्य देशों के भी बहुतेरे दार्शनिकों ने-पुरानों ने और
नयों ने भी-माना है। यह दूसरी बात है कि उनने खुल के ऐसा न लिखा हो। उनके
अपने लिखने के तरीके भी तो निराले ही थे और सोचने के भी। इसीलिए उनने यह
बात निराले ही ढंग से-अपने ही ढंग से-मानी या लिखी है। मगर हमारे देश के तो
आस्तिक-नास्तिक सभी दार्शनिकों ने यह कर्मवाद स्वीकार किया है,
सिवाय चार्वाक के। न्याय,
सांख्य आदि दर्शनों के अलावे जैन, बौद्ध,
पाशुपत आदि ने भी इसे साफ स्वीकार किया है। यह बात तो
पहले ही कही जा चुकी है कि गीता ने भी कर्मवाद को माना है। मगर वह पौराणिक
ढंग के कर्मवाद को स्वीकार न करके दार्शनिक कर्मवाद को ही मानती है,
यह भी बताया जा चुका है। गीता के और और स्थानों में भी
यह बात पायी जाती है। अठारहवें अध्याय
के 'दैव
चैवात्र
पंचमम्' (18।
14) में यही बात 'दैव'
शब्द से कही गयी है, यह भी
कह चुके
हैं।
चौथे अध्याय
के 'जन्म
कर्म च मे दिव्यम्' (4। 9)
में दैव की जगह दिव्य शब्द आया है। मगर बात वही है।
दोनों शब्दों का अर्थ भी एक ही है। दिव् शब्द से ही दिव्य या दैव शब्द बनते
भी
हैं।
यों तो उसके
7, 8-दो-श्लोकों में जो कुछ कहा गया है वह कर्मवाद के
ही
आधार
पर कहा जा सकता है। दूसरे ढंग से वह कभी भी युक्तिसंगत होई नहीं सकता।
हाँ,
तो
आइये जरा इस कर्मवाद की दार्शनिक तह में पहले घुसें और देखें कि इसकी हकीकत
क्या है। हम पहले कह चुके हैं कि पदार्थों में बराबर परिवर्तन जारी है।
फलत: कुछी दिनों बाद चीजें बदल के एकदम नयी बन जाती है। यद्यपि हमें ऐसा
पता नहीं चलता और न हम यही समझ पाते हैं कि सचमुच कोई चीज बदल चुकी है। इस
बात में वैज्ञानिकों की भी सम्मति दी जा चुकी है। गीता ने भी यह बात शुरू
में ही 'देहिनोऽस्मिन्'
(2।
13)
में
स्वीकार की है। हमने वहीं पर इस परिवर्तन के दृष्टान्त के रूप में किसी
कोठी यार् बत्तान में बन्द करके रखे गये चावल का दृष्टान्त भी दिया है और
बताया है कि किस तरह नया चावल कुछ दिनों में बदल के बिलकुल ही दूसरा बन
जाता है। यहाँ भी हम फिर उसी दृष्टान्त को लेंगे। हालाँकि जो कुछ विचार अब
करेंगे वह दूसरे ढंग से,
दूसरे पहलू से होगा। मगर इसे समझने के लिए वहाँ लिखी सभी बातें स्मरण कर
लेने की हैं। दुबारा लिखनाव्यर्थ है। वैज्ञानिक की प्रयोगशाला की भी जो बात
वहाँ लिखी है,
खयाल कर लेनेकीहै।
जब हम
देखते हैं कि प्रतिक्षण,
प्रति सेकण्ड हरेक पदार्थ से अनन्त परमाणु निकलते और उनकी जगह नये-नये आ
धामकते हैं तो हमें आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। इसलिए प्रयोगशाला में बैठ
के ही यह बात सोचने की है। क्योंकि दूसरे ढंग से इस पर आमतौर से लोगों को
विश्वास होई नहीं सकता। लोगों के दिमाग में यह बात समाई नहीं सकती कि
प्रतिक्षण हरेक पदार्थ के भीतर से असंख्य परमाणु निकलते और भागते रहते हैं
और उनकी जगह ले लेते हैं नये-नये बाहर से आ के। विज्ञान के प्रताप से यह
बात अब लोगों के दिमाग में आसानी से आ जाती है। मगर पुराने जमाने में जब ये
वैज्ञानिक यन्त्रा कहीं थे नहीं और न ये प्रयोगशालाएँ थीं तब हमारे
दार्शनिक विद्वानों ने ये बातें कैसे सोच निकालीं यह एक पहेली ही है। फिर
भी इसमें तो कोई शक हुई नहीं-यह तो सर्वमान्य बात है-कि उनने ये बातें सोची
थीं,
ढूँढ़
निकाली थीं। इन्हीं के अन्वेषण,
पर्यवेक्षण और सोच-विचार ने उन्हें अगत्या कर्मवाद के सिद्धान्त तक
पहुँचाया और उसे मानने को मजबूर किया। या यों कहिए कि इन्हीं को
ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उनने कर्मवाद का सिद्धान्त ढूँढ़ निकाला।
हमारे
नैयायिक दार्शनिकों का एक पुराना सिद्धान्त है कि एक ही स्थान में दो
द्रव्यों का समावेश नहीं होता। पार्थिव,
जलीय आदि सभी पदार्थों को उनने द्रव्य नाम दिया है। रूप,
रस
आदि गुणों में कोई भी जिन पदार्थों में पाये जायँ उन्हीं को उनने द्रव्य
कहा है। वे यह भी मानते आये हैं कि कई द्रव्यों के संयोग से नया द्रव्य
तैयार होता है। दृष्टान्त के लिए कई सूतों के परस्पर जुट जाने से कपड़ा बनता
है। सूत भी द्रव्य हैं और कपड़ा भी। फर्क यही है कि सूत अवयव हैं और कपड़ा
अवयवी। सूतों के भी जो रेशे होते हैं उन्हीं से सूत तैयार होते हैं। फलत:
रेशों की अपेक्षा सूत हुआ अवयवी और रेशे हो गये अवयव। रेशों के भी अवयव
होते हैं और उन अवयवों के भी अवयव। इस प्रकार अवयवों की धारा-परम्परा-चलती
है। उधर कपड़े को भी काट-छाँट के और जोड़-जाड़के कुर्ता,
कोट वगैरह बनाते हैं। वहाँ पर कपड़ा अवयव हो जाता है और कोट,
र्कुत्तो अवयवी। जितने नये सूत जुटते जाते हैं उतना ही लम्बा कपड़ा होता
जाता है-नया-नया कपड़ा बनता जाता है। उधर अवयवों के भी अवयव करते-करते कहीं
न कहीं रुक जाना जरूरी होता है,
जहाँ से यह काम शुरू हुआ है। क्योंकि अगर कहीं रुकें न और हर अवयव के अवयव
करते जायँ तो पता ही नहीं लगता कि आखिर अवयवी का बनना कब और कहाँ से शुरू
हुआ। इसीलिए जहाँ जाके रुक जायँ उसी को नैयायिकों ने परमाणु कहा है। परमाणु
(Atom)
का
अर्थ ही सबसे छोटा,
छोटे से छोटा-जिससे छोटा हो न सके। परमाणुवाद के बारे
में और भी दलीलें
हैं।
मगर हमें यहाँ उनमें नहीं पड़ना है। उन पर कुछ प्रकाश आगे डाला गया है।
गुणवाद के प्रकरण में।
इस प्रकार
परमाणुओं के जुटने-संजोग-से चीजें बनती रहती हैं। अब मान लें कि कुछ
परमाणुओं ने मिल के एक चीज बनायी। लेकिन,
जैसा कि कह चुके हैं कि पुराने परमाणुओं का निकलना और नयों का जुटना जारी
है,
जब कुछ और
भी परमाणु पुरानों के साथ,
जिनने आपसे में मिल के कोई चीज बनायी थी,
आ
जुटे तो अब जो चीज बनेगी वह तो दूसरी ही होगी। पहली तो यह होगी नहीं।
क्योंकि पहली में तो नये परमाणु थे नहीं। इसी प्रकार कुछ सूतों को जुटाकर
कपड़ा बना। मगर सूत तो जुटते ही रहते हैं। इसलिए नये सूतों को पुरानों के
साथ जुटने पर कपड़ा भी बनता ही जायेगा। हाँ,
यह
नया होगा,
न
कि वही पहले ही वाला। क्योंकि पहले तो ये नये सूत जुटे न थे। यही हालत
सर्वत्र जारी रहती है। अब यहीं पर नैयायिकों की वह बात आती है कि एक ही
स्थान में दो द्रव्यों का समावेश नहीं हो सकताहै।
चाहे
परमाणुओं वाली बात में या सूतों वाली। हम हर हालत में देखेंगे कि नये-नये
कपड़े या नयी-नयी चीजें बनती जाती हैं। मगर सवाल तो यह होता है कि जिन सूतों
से पहला कपड़ा बना है उन्हीं के साथ कुछ दूसरों के जुटने से दूसरा और तीसरा
बनता है। यह बात चाहे जैसे भी देखें,
यह
तो मानना ही होगा कि पहले कि जिन सूतों से पहला कपड़ा बना और उन्हीं में
उसका समावेश है,
ऍंटाव है। उन्हीं में दूसरा भी बनता है और उसके बादवाले कपड़े भी बनते हैं;
हालाँकि दूसरे-तीसरे आदि का ऍंटाव कुछ नये सूतों में भी रहता है। मगर पहले
सूतों में भी तो रहता ही है। पीछेवाले कपड़े पहलेवाले सूतों के बिलकुल ही
बाहर तो चले जाते नहीं। ऐसी हालत में उन्हीं सूतों में कई कपड़े कैसे
ऍंटेंगे,
यही तो पहेली है। कपड़े तो द्रव्य हैं। और द्रव्य तो जगह घेर लेते हैं। इसी
से नैयायिक कहते हैं कि एक ही स्थान में एक से ज्यादा द्रव्यों का ऍंटाव या
समावेश नहीं हो सकता।
तब सवाल
होता है कि यदि एक ही कपड़ा उनमें रहेगा तो साफ ही है कि जोई पीछे या नया
बनेगा,
तैयार होगा,
तैयार होता जायगा वही सभी-नये पुराने-सूतों में समाविष्ट होगा। फलत: पहले
वाले हट जायँगे,
नष्ट हो जायँगे,
खत्म हो जायँगे। जैसे-जैसे नये सिरे से कपड़ा बनता जायगा तैसे-तैसे पहले बने
कपड़े नष्ट होते जायँगे। इस प्रकार के सभी पदार्थों में यही प्रक्रिया जारी
रहती है-पहलेवालों के नाश का यह सिलसिला जारी रहता है। दूसरा उपाय है
नहीं-दूसरा चारा है नहीं। बात तो कुछ अजीब और बेढंगी सी मालूम पड़ती है। मगर
हमें इस दुनिया में कितनी ही बेढंगी बात माननी ही पड़ती है। जब बुद्धि और
तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो जो बातें खरी उतरें उनके मानने में उज्र क्या
है?
किसी
जमाने में सूर्य स्थिर है और पृथिवी चलती है;
इस
बात के कहनेवालों को बड़ी आफतें झेलनी पड़ीं। मगर गणित और हिसाब-किताब की
मजबूरी जो थी। वे लोग करते क्या?
नतीजा यह हुआ कि आज आमतौर से वही बात मानी जाने लगी है।
पहले
विज्ञान का यह विकास न होने के कारण लोगों को इसमें झिझक हुई। मगर आज तो
विज्ञान ने ही बता दिया है कि जरूर ही पुराने वस्त्र,
पुराने चावल,
पुराने पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और नये पैदा हो जाते हैं। भला कपड़े के बारे
में तो नैयायिक दार्शनिक यह भी कहते थे कि साफ ही नये सूत जुटे हैं। देखने
वाले देखते भी थे। मगर कोठी में बन्द चावलों में कौन देखता है कि चावलों के
नये परमाणु जुटते और पुराने भागते जाते हैं। पुराने सूतों की ही सूरत-शक्ल
के नये सूत कपड़े में जुटते हैं। मगर चावलों के पुराने परमाणुओं में जो
स्वाद या रस होता है उसी स्वाद और रस के नये परमाणुओं को आते और पुरानों की
जगह लेते कौन देखता है?
चावल का स्वाद दस साल के बाद बदल के गेहूँ का तो हो जाता नहीं। उसमें स्वाद,
रस
वगैरह चावल का ही रहता है। इससे मानना पड़ेगा कि जो नये परमाणु आये वे चावल
के ही स्वाद और रस के थे। बात तो यह भी कम अजीब और बेढंगी सी है नहीं।
इसीलिए नैयायिकों की बात अब समझ में आ जाती है-आ सकती है। चावलों के ही
परमाणुओं का-वैसे ही स्वाद,
रस,
रूप-रेखाओं का-खजाना किसने कहाँ जमा कर रखा है जो बराबर आते-जाते हैं?
यह
नहीं कि चावलों की ही बात हो। गेहूँ,
चने,
मटर आदि
की भी तो यही बात है। पशु,
पक्षी,
मनुष्य,
खाक,
पत्थर
सबों की यही हालत है। सबों में अपनी ही जाति के परमाणु आ मिलते हैं! फलत:
यह तो मानना ही पड़ेगा कि सबों का अलग कोष,
खजाना (Stock)
कहीं
पड़ा है। मगर पता नहीं कहाँ,
कैसे पड़ा है। यही तो पहेली है। बत्तान या कोठी के मुँह
तो ऐसे बन्द
हैं
कि जरा भी हवा आ-जा न सके। मगर ये अनन्त परमाणु बराबर आते-जाते रहते
हैं!
यही तो माया है,
जादू है!
यहाँ तक
तो हमने इस पहेली की उधोड़-बुन दार्शनिक ढंग से की। मगर सवाल हो सकता है कि
इसका कर्मवाद से ताल्लुक क्या है?
ताल्लुक है और जरूर है। इसीलिए तो जरा विस्तार से हमने यह बात लिखी है।
नहीं तो आगे की बात समझ में नहीं आती। बात यह है कि अनन्त परमाणुओं का
आना-जाना और पुरानी की जगह नयी चीज का बन जाना एक पहेली है यह तो मान चुके।
अब जरा सोचें कि आखिर यह होता है क्यों और कैसे?
पुराने चावलों की जगह नये क्यों बने?
वैसे ही परमाणु क्यों आये और उतने ही ही क्यों आये जितने निकले?
यदि कमीबेशी भी हुई तो बहुत ही कम। गेहूँ में चावल के और चावल में गेहूँ के
क्यों नहीं आ गये?
गाय में भैंस के और भैंस में गाय के क्यों न घुसे?
आदमी में पशु के तथा पशु में आदमी के क्यों न प्रवेश पा सके?
मर्द में औरत के और औरत में मर्द के क्यों न चले आये?
वृक्षों में पत्थर के और पत्थरों में वृक्षों के क्यों न जुटे?
मूर्खों में पण्डितों के तथा पण्डितों में निरक्षरों के क्यों न लिपटे?
ऐसे प्रश्न तो हजार-लाख हो सकते हैं,
होते हैं।
इन
परमाणुओं का वर्गीकरण कहाँ कैसे किया गया है?
यदि काम कौन करता है?
जिसमें जरा भी गड़बड़ी न हो,
किन्तु सभी ठीक-ठीक अपनी-अपनी जगह जायें-आयें यह पक्का प्रबन्ध क्यों,
किसने,
कैसे किया?
इसमें कभी गड़बड़ न हो इस बात का क्या प्रबन्ध है और कैसा है?
परमाणुओं के कोष में कमी-बेशी हो तो उसकी पूर्ति कैसे हो?
यदि यह माना जाय कि हरेक पदार्थ से निकलने वाले परमाणु अपने सजातियों के ही
कोष में जा मिलते हैं,
तो
प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों होता है और उन्हें कौन,
कहाँ,
कैसे ले
जाता है ?
साथ ही यह भी प्रश्न होता है कि निकलने वाले परमाणुओं की जो हालत होती है
वह तो कुछ निराली होती है,
न
कि कोष में रहनेवालों की ही जैसी। ऐसी दशा में उनके मिलने से वह कोष खिचड़ी
बन जायगा या नहीं?
नये चावल का भात भारी होता है और मीठा ज्यादा होता है,
बनिस्बत पुराने चावलों के। इसलिए यह तो मानना ही होगा कि चावल के भी परमाणु
सबके-सब एक ही तरह के नहीं होते। ऐसी हालत में चावल के परमाणुओं के भी कई
प्रकार के कोष मानने ही होंगे। अब यदि यह कहें कि नये चावलों के परमाणु
पुनरपि वैसे ही नये चावलों में जा मिलेंगे और जब तक जाकर मिल जाते नहीं तब
तक कहीं शान्त पड़े रहेंगे,
तो
सवाल होता है कि यह बारीक देखभाल कौन करता है और क्यों?
ठीक समय पर वैसे ही चावलों में उन्हें कहाँ,
कैसे पहुँचाया जायगा यह व्यवस्था भी कैसे होती है?
यह
तो ऐसा लगता है कि कोई सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक देखने वाला चारों ओर
ऑंखें फाड़ के हर चीज को बारीकी से देखता हो और ठीक समय पर सारी व्यवस्था
करता हो। यह कैसी बात है,
यह
प्रश्न स्वाभाविक है?
यह
कौन है?
क्यों है?
कैसे है?
ये
प्रश्न भी होते हैं। उसके हाथ बँधे हैं या स्वतन्त्र हैं?
यदि बँधे हैं तो किससे?
और
तब वह सारे काम ठीक-ठीक करेगा कैसे?
यदि स्वतन्त्र हैं तो भी वही बात आती है कि सारे काम नियमित रूप से क्यों
होते हैं?
कहीं-कहीं मनजानी घरजानी क्यों नहीं चलती?
चावलों को
ही लेके और भी बातें उठती हैं। माना कि चावलों से असंख्य परमाणु निकलते
रहते हैं। तो फिर जरूरत क्या है कि उनकी जगह खाली न रहे और दूसरे परमाणु
खामख्वाह आ के जम जायँ?
धीरे-धीरे चावल पतले पड़ जायँ तो हर्ज क्या?
आखिर घुनों के खा जाने से तो ऐसा होई जाता है। कपूर के परमाणु निकलते हैं
और उनमें नये आते नहीं। इसीलिए वह जल्द खत्म हो जाता है। वही बात चावलों
में भी क्यों नहीं होती?
यदि कहा जाय कि चावलवाला मर जो जायगा,
तो
प्रश्न होता है कि आग लगने या चोरी होने पर क्या वह भूखों नहीं मर जाता जब
चावल लुट जाते या जल जाते हैं
?
और कपूर
वाले पर भी यही दलील क्यों न लागू हो
?
चावल जलने
पर या लुट जाने पर जो होता है वही बात यों भी क्यों नहीं हो?
किसी समय चावलों के परमाणु ज्यादा निकल जायँ और वह गल-सड़ जाए और किसी समय
नहीं,
ऐसा क्यों
होता है?
इसी तरह के हजारों सवाल उठ खड़े होते हैं यदि हम इन पदार्थों के खोद-विनोद
और अन्वेषण में पड़ जायँ। हमने तो यहाँ थोड़े से प्रश्न नमूने के तौर पर ही
दिये हैं।
इसी
खोद-विनोद,
इसी जाँच-पड़ताल,
इसी अन्वेषण के सिलसिले में इन जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ते-ढूँढ़ते हमारे
प्राचीन दार्शनिकों को विवश हो के ईश्वर और कर्मवाद की शरण लेनी पड़ी,
यह
सिद्धान्त स्थिर करना पड़ा। मनुष्य अपनी पहुँच के अनुसार ही कल्पना करता है।
हम तो देखते हैं कि नियमित व्यवस्था बुद्धिपूर्वक ही होती है। बिना समझ और
ज्ञान के यह बात हो पाती नहीं। और अगर कभी घड़ी या दूसरे यन्त्रों को
नियमित काम करते देखते हैं तो उसी के साथ यह भी देखते हैं कि उनके मूल में
कोई बुद्धि है जिसने उन्हें तैयार करके चालू किया है। वही उनके बिगड़ जाने
पर पुनरपि उन्हें ठीक कर देती है। जड़ पदार्थों में तो यह शक्ति नहीं होती
कि अपनी भूल या गड़बड़ देखें,
त्रुटि का पता लगायें और उसे सँभालें। इसके बाद हम बाकी दुनिया में भी ऐसी
ही व्यापक या समष्टि बुद्धि की कल्पना करते हैं,
क्योंकि हम सभी मिल-मिला के भी बहुत से कामों को नहीं कर सकते। वे हमारी
ताकत के बाहर के हैं। दृष्टान्त के लिए चावल वगैरह के बारे में जो बातें
पूछी गयी हैं उन्हीं को ले सकते हैं। वे हमारी पहुँच के बाहर की बातें हैं।
जिन्हें हम देख पाते नहीं उनकी व्यवस्था क्या करें?
और
अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि हमीं सब लोग उन्हें करते हैं,
कर
लेते हैं,
कर
सकते हैं,
तो
भी हम सबों के कामों की मिलान (Co-ordination)
तो
होनी ही चाहिए न । नहीं तो फिर वही गड़बड़ होगी। अब इस मिलान का करनेवाला कोई
एक तो होगा ही जो सब कुछ बखूबी जानता हो।
जो लोग इन
प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रकृति,
नैसर्गिक-नियम,
शाश्वत विधान (Nature, Natural
Law, Eternal Law)
आदि कह
के बातें टाल देते
हैं
वे शब्दान्तर से अपनी अनभिज्ञता मान लेते
हैं।
हमारा काम है गुप्त रहस्यों का पता लगाना,
प्रकृति के-संसार के-नियमों को ढूँढ़ निकालना। दिमाग,
अक्ल, बुद्धि
का दूसरा काम है भी नहीं। इन बातों से किनाराकशी करना भी हमारा काम नहीं
है। कोई समय था जब कहा जाता था कि योगियों का आकाश में यों ही चला जाना
असम्भव है,
दूर देश का समाचार जान लेना गैरमुमकिन है। पक्षी उड़ते
हैं
तो उड़ें। उनकी तो प्रकृति ही ऐसी है। मगर आदमी के लिए यह बात असम्भव है।
अपेक्षाकृत कुछ कम-बेश दूरी पर हमारी आवाज दूसरों को भले ही सुनाई दे। मगर
हजारों मील दूर कैसे सुनाई देगी?
शब्द का स्वभाव ऐसा नहीं है,
आदि-आदि। मगर अन्वेषण और विज्ञान ने सब कुछ सम्भव और सही बता दिया-करके
दिखा दिया! फलत: स्वभाव की बात जाती रही। मामूली सी बात में भी तर्क-दलील
करते-करते जब हम थक जायँ और
उत्तर
न दे सकें,
तो क्यों न स्वभाव या प्रकृति की शरण ले के पार हो जायँ
? तब हम भी क्यों न कह दें कि यही प्रकृति का
नियम है, नित्य नियम है?
बात तो एक ही है। ज्यादा बुद्धिवाले
कुछ ज्यादा दूर तक जा के प्रकृति की शरण लेते
हैं।
मगर हम कम अक्लवाले जरा नजदीक में ही और यह कैसे पता चला कि यह प्रकृति का
नियम है,
नित्य नियम है? प्रकृति क्या
चीज है? नियम क्या चीज है?
किसे नियम कहें और किसे नहीं?
पहले तो कहा जाता था कि पृथिवी स्थिर है और सूर्य चलता
है। क्यों? यही नित्य नियम है यही
उत्तर
मिलता था। अब
उल्टी
बात हो गयी इसीलिए प्रकृति,
नेचर, प्राकृतिक नियमों की
बात करना दूसरे शब्दों में अपने अज्ञान, अपनी
संकुचित समझ, अपनी अविकसित बुद्धि
को कबूल करना है। यह बात पुराने दार्शनिक नहीं करते थे। और जब जड़ नियमों को
मानते ही
हैं,
तो फिर चेतन ईश्वर को ही क्यों न मानें?
अन्धे
से तो ऑंखवाला ही ठीक है न?
नहीं तो फिर भी अड़चन आ सकती है।
इसीलिए
उनने उस व्यापक हाथ,
शक्ति या पुरुष को स्वीकार किया,
या
यों कहिए कि ढूँढ़ निकाला। उसके बिना इस संसार का काम उन्हें चलता नहीं
दीखा। इसीलिए उसे पुरुष कहा,
पुरुष का अर्थ ही है जो सर्वत्र पूर्ण या व्यापक हो। यदि उसमें अविद्या,
भले-बुरे कर्म,
सुख-दु:ख,
राग-द्वेष या भले-बुरे संस्कार मनुष्यों जैसे ही रहे तो फिर वही गड़बड़ होगी।
पुरुष तो जीवों को भी कहते हैं। आत्माएँ भी तो व्यापक हैं। इसीलिए उसे
निराला पुरुष माना और पतंजलि ने योगसूत्रों में साफ ही कह दिया कि
''क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट:
पुरुषविशेष ईश्वर:''
(1।
24)
इसका अर्थ
यही है कि अविद्या आदि से वह सर्वथा रहित है। इसीलिए उसे रत्ती-रत्ती
चीजों का जानकार होना चाहिए। नहीं तो फिर भी दिक्कत होगी और संसार की
व्यवस्था ठीक हो न सकेगी। उसका ज्ञान ऐसा हो कि उसकी कोई सीमा न हो-वह भूत,
भविष्य,
वर्तमान सभी काल के सभी पदार्थों को जान सके। इसीलिए पतंजलि ने कहा कि
'तत्र
निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्'
(1।25)।
अगर वह मरे-जिये,
कभी रहे कभी न रहे तो भी वही दिक्कत हो। इसलिए कह दिया कि वह समय की सीमा
से बाहर है-नित्य है,
अजर-अमर है। जितने जानकार,
विद्वान्,
दार्शनिक और तत्तवज्ञ अब तक हो चुके उसके सामने सब फीके हैं-तुच्छ हैं।
क्योंकि देशकाल से सीमित तो सभी ठहरे और वह ठहरा इससे बाहर। इसीलिए वह सबों
का दादागुरु है-'पूर्वेषामपि
गुरु: कालेनानवच्छेदात्'
(1।26)
(शीर्ष पर वापस)
कर्मवाद
मगर
इतने से भी काम चलता न दीखा। यदि ऐसा ईश्वर हो कि जो चाहे सोई करे तो उस पर
स्वेच्छाचारिता (Autocracy)
का
आरोप आसानी से लग सकता है। सर्वज्ञ,
सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने के कारण उसकी
स्वेच्छाचारिता बड़ी ही खतरनाक सिद्ध
होगी। जिस व्यवस्था और नियमितता के लिए हम उसे स्वीकार करते
हैं
या उसका लोहा मानते
हैं,
वही न रह पायेगी। क्योंकि उसकी
स्वतन्त्रता
ही कैसी यदि उस पर
बन्धन
लगा रहा?
वह
स्वतन्त्र
ही कैसा यदि उसने किसी बात की परवाह की?
यदि उस पर कोई भी अंकुश रहे,
चाहे वह कैसा भी क्यों न हो, तो वह
परतन्त्र
ही माना जायगा। यह प्रश्न मामूली नहीं है। यह एक बहुत बड़ी चीज है। जब हम
किसी बात को बुद्धि
और तर्क की तराजू पर तौलते
हैं,
तो हमें उसके नतीजों के लिए तैयार रहना ही होगा। यह
दार्शनिक बात है। कोई खेल, गप्प या कहानी तो है
नहीं। इस प्रकार के ईश्वर को मानने पर क्या होगा यह बात ऑंखें खोल के देखने
की है। पुराने महापुरुषों ने-दार्शनिकों ने-इसे देखा भी ठीक-ठीक। वे इस
पहेली को सुलझाने में सफल भी हुए, चाहे संसार
उसे गलत माने या सही। और हमारी सभी बातें सदा
ध्रुव
सत्य
हैं
यह दावा तो समझदार लोग करते ही नहीं। ज्ञान का ठीका तो किसी ने लिया है
नहीं। तब हमारे दार्शनिक ऐसी गलती क्यों करते?
उन्हें जो सूझा उसे उनने कहा दिया।
इस दिक्कत
से बचने के ही लिए उनने कर्मवाद की शरण ली। असल में यह बात भी उनने अपने
अनुभव और ऑंखों देखी के ही अनुसार तय की। उनने सोचा कि प्रतिदिन जो कुछ भी
बुरा-भला होता है वह कामों के ही अनुसार होता है। चाहे खेती-बारी लें या
रोजगार-व्यापार,
पढ़ना-लिखना,
पारितोषिक,
दण्ड और हिंसा-प्रतिहिंसा के काम। सर्वत्र एक ही बात पायी जाती है। जैसे
करते हैं वैसा पाते हैं। जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। गाय पालते हैं तो
दूध दुहते हैं। साँप पाल के जहर का खतरा उठाते हैं। सिंह पाल के मौत का।
जान मारी तो जान देनी पड़ी। पढ़ा तो पास किया। न पढ़ा तो फेल रहे। अच्छे काम
में इनाम मिला और बुरे में जेल या बदनामी हाथ आयी। असल में यदि कामों के
अनुसार परिणाम की व्यवस्था न हो तो संसार में अन्धेरखाता ही मच जाय। जब
इससे उल्टा किया जाता है तो बदनामी और शिकायत होती है,
पक्षपात का आरोप होता है। यदि इसमें भी गड़बड़ होती है तो वह काम के नियम का
दोष न हो के लोगों की कमजोरी और नादानी से ही होती है। अगर काम के अनुसार
फल का नियम न हो तो कोई कुछ करे ही न। पढ़ने में दिमाग खपानेवाला फेल हो जाय
और निठल्ला बैठा पास हो। खेती करनेवाले को गल्ला न मिले और बैठे-ठाले की
कोठी भरे। ऐसा भी होता है कि एक के काम का परिणाम वंशपरम्परा को भी भुगतना
पड़ता है। यदि अपनी नादानी से कोई पागल हो जाय तो वंश में भी उसका फल बच्चों
और उनके बच्चों तक पहुँचता है। ऐसी ही दूसरी भी बीमारियाँ हैं। एक के किये
का फल सारा वंश,
गाँव या देश भी भुगतताहै।
इस प्रकार
एक तो कर्म ही सारी व्यवस्था के करने वाले सिद्ध हुए। दूसरे उनके दो विभाग
भी हो गये। एक का ताल्लुक उसी व्यक्ति से होता है जो उसे करे। यह हुआ
व्यष्टि कर्म। दूसरे का सम्बन्ध समाज,
देश या पुश्त-दरपुश्त से होता है। यही है समष्टि कर्म। ऐसा भी होता है कि
हरेक आदमी अपने काम से अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। नदी से पानी ला के
प्यास बुझा ली। मिहनत से पढ़ के पास कर लिया। बेशक इसमें विवाद की गुंजाइश
है कि कौन व्यक्तिगत या व्यष्टि कर्म है और समष्टि। मगर इसमें तो शक नहीं
कि व्यष्टि कर्म है। जहर खा लिया और मर गये। हाँ,
समष्टि कर्म में एक से ज्यादा लोग शरीक होते हैं। कुऑं अकेले कौन खोदे?
खेती एक आदमी कर नहीं सकता। घर-बार सभी मिल के उठाते हैं। समष्टि कर्म यही
हैं। सभी मिलके करते और फल भी सभी भोगते हैं। कभी-कभी एक का किया भी अनेक
भुगतते हैं। फलत: वह भी समष्टि कर्म ही हुआ।
बस,
तत्तवदर्शियों ने इस सृष्टि का यही सिद्धान्त सभी बातों में लागू कर दिया।
उनने माना कि जन्म-मरण,
सुख-दु:ख,
बीमारी,
आराम वगैरह सभी के मूल में या तो व्यष्टि या समष्टि कर्म हैं। उनने सभी की
स्वतन्त्रता मर्यादित कर दी। चावलों या पदार्थों के परमाणुओं के आने-जाने
से लेकर सारे संसार के बनाने-बिगाड़ने या प्रबन्ध का काम ईश्वर के जिम्मे
हुआ और सभी पदार्थ उसके अधीन हो गये। ईश्वर भी जीवों के कर्मों के अनुसार
ही व्यवस्था करेगा। यह नहीं कि अपने मन से किसी को कोढ़ी बना दिया तो किसी
को दिव्य;
किसी को राजा तो किसी को रंक;
किसी को लूटने वाला तो किसी को लुटानेवाला। जीवों के कर्मों के अनुसार ही
वह सब व्यवस्था करता है। जैसे भले-बुरे कर्म हैं वैसी ही हालत है,
व्यवस्था है। कही चुके हैं कि बहुतेरे कर्म पुश्त-दर-पुश्त तक चलते हैं।
इसीलिए इस शरीर में किये कर्मों में जिनका फल भुगताना शेष रहा उन्हीं के
अनुसर अगले जन्म में व्यवस्था की गयी। जैसे भले-बुरे कर्म थे वैसी ही
भली-बुरी हालत में सभी लोग लाये गये। इस तरह ईश्वर पर भी कर्मों का
नियन्त्रण हो गया। फिर मनमानी घरजानी क्यों होगी?
तब
वह निरंकुश या स्वेच्छाचारी क्यों होगा?
कर्म भी खुद कुछ कर नहीं सकते। वह भी किसी चेतन या जानकार के सहारे ही अपना
फल देते हैं। वे खुद जड़ या अन्धे जो ठहरे। इस तरह उन पर भी ईश्वर का अंकुश
या नियन्त्रण रहा-वे भी उसके अधीन रहे। सारांश यह है कि सभी को सबकी
अपेक्षा है। इसीलिए गड़बड़ नहीं हो पाती। किसी का भी हाथ सोलह आना खुला नहीं
कि खुल के खेले।
(शीर्ष पर वापस)
कर्मों के भेद और उनके काम
यह तो
पहले ही कह चुके
हैं
कि जब कर्म अपना फल देते
हैं
तो उस फल की सामग्री को जुटाकर ही। कर्मों का कोई दूसरा तरीका फल देने का
नहीं है। एकाएक आकाश से कोई चीज वे टपका नहीं देते। अगर जाड़े में आराम
मिलना है तो घर,
वस्त्र
आदि के ही रूप में कर्मों के फल मिलेंगे। इन्हीं कर्मों के तीन दल
प्रकारान्तर से किये गये
हैं।
एक तो वे जिनका फल भोगा जा रहा हो। इन्हें
प्रारब्ध
कहते
हैं।
प्रारब्ध
का अर्थ ही है कि जिनने अपना फल देना प्रारम्भ कर दिया। लेकिन बहुत से कर्म
बचे-बचाये रह जाते
हैं।
सबों का नतीजा बराबर भुगता जाय यह सम्भव नहीं। इसलिए बचे-बचायों का जो कोष
होता है उसे संचित कर्म कहते
हैं।
संचित के मानी
हैं
जमा किये गये या बचे-बचाये। इसी कोष में सभी कर्म जमा होते रहते
हैं।
इनमें जिनकी दौर शुरू हो गयी,
जिनने फल देना शुरू कर दिया वही
प्रारब्ध
कहे गये। इन दोनों के अलावे क्रियमाण कर्म
हैं
जो आगे किये जायँगे और संचित कोष में जमा होंगे। असल में तो कर्मों के
संचित और
प्रारब्ध
यही दो भेद
हैं।
क्रियमाण भी संचित में ही आ जाते
हैं।
यों तो
प्रारब्ध
भी संचित ही
हैं।
मगर दोनों का फर्क बता चुके
हैं।
यही है संक्षेप में कर्मों की बात।
अब जरा
इनका प्रयोग सृष्टि की व्यवस्था में कर देखें। पृथिवी के बनने में समष्टि
कर्म कारण हैं। क्योंकि इससे सबों का ताल्लुक है-सबों को सुख-दु:ख इससे
मिलता है। यही बात है सूर्य,
मेघ,
जल,
हवा आदि के बारे में भी। हरेक के व्यक्तिगत सुख-दु:ख अपने व्यष्टि कर्म के
ही फल हैं। अपने-अपने शरीरादि को एक तरह से व्यष्टि कर्म का फल कह सकते
हैं। मगर जहाँ तक एक के शरीर का दूसरे को सुख-दु:ख पहुँचाने से ताल्लुक है
वहाँ तक वह समष्टि कर्म का ही फल माना जा सकता है। यही समष्टि और व्यष्टि
कर्म चावल वगैरह में भी व्यवस्था करते हैं। जिस किसान ने चावल पैदा करके
उन्हें कोठी में बन्द किया है उसके चावलों से उसे आराम पहुँचना है। ऐसा
करने वाले उसके व्यष्टि या समष्टि कर्म हैं जो पूर्व जन्म के कमाये हुए
हैं। यदि चावलों के परमाणु निकलते ही जायँ और आयें नहीं,
तो
किसान दिवालिया हो जायगा। फिर आराम उसे कैसे होगा?
इसलिए उसी के कर्मों से यह व्यवस्था हो गयी कि नये परमाणु आते गये और चावल
कीमती बन गया। यदि पुराने नहीं जाते और नये नहीं आते तो यह बात न हो पाती।
परमाणुओं का कोष भी कर्मों के अनुसार बनता है,
बना रहता है। ईश्वर उसका नियन्त्रण करता है। जब बुरे कर्मों की दौर आयी तो
घुन खा गये,
चावल सड़
गये। या और कुछ हो गया। उनमें अच्छे परमाणु आ के मिले भी नहीं। यही तरीका
सर्वत्र जारी है,
ऐसा
प्राचीन दार्शनिकों ने माना है। यों तो कर्मों के और भी अनेक भेद हैं। ऐसे
भी कर्म होते हैं जिनका काम है केवल कुछ दूसरे कर्मों को खत्म
(Negative)
कर
देना। ऐसे भी होते
हैं
जो अकेले ही कई कर्मों के बराबर फल देते
हैं।
मगर इतने लम्बे पँवारे से हमें क्या मतलब?
योगसूत्रों
के भाष्य और दूसरे दर्शनों को पढ़ के ये बातें जानी जा सकतीहैं।
(शीर्ष पर वापस)
अवतारवाद
इतने
लम्बे विवरण के बाद अब मौका आता है कि हम अवतारवाद के
सम्बन्ध
में इन कर्मों को लगा के देखें कि कर्मवाद वहाँ किस प्रकार लागू होता है।
यह तो कही चुके
हैं
कि समष्टि कर्मों के फलस्वरूप पृथिवी आदि पदार्थ बनते
हैं
जिनका ताल्लुक एक-दो से न हो के समुदाय से है,
समाज से है, मानव-संसार से
है। सभी पदार्थों से है। यदि यह ढूँढ़ने लगें कि पृथिवी को किस व्यक्ति के
कर्म ने तैयार किया-कराया, तो यह हमारी भूल
होगी। एक से तो उसका
सम्बन्ध
है नहीं। पृथिवी के चलते हजारों-लाखों को सुख-दु:ख भोगना है,
गल्ला पैदा करना है, घर
बनाना है, कपड़ा तैयार करना है-होना है। उससे
तलवारें, भाले, तोपें,
गोले, लाठियाँ बन के जाने
कितने मरें-मारेंगे। फिर एक के कर्म का क्या सवाल?
पृथिवी आदि पदार्थ एक के कर्म से क्यों बनेंगे?
जरा यही
बात अवतारों के विषय में भी लगा देखें। आखिर अवतारों का काम क्या है?
उनसे होता क्या है?
उनकी भली-बुरी उपयोगिता है क्या?
गीता कहती है कि
''भले
लोगों की रक्षा,
बुरों के नाश और धर्म-सत्कर्मों,
पुण्य-कार्यों,
समाज-हितकारी कामों-की मजबूती एवं प्रचार के लिए बार-बार-समय-समय पर-अवतार
होते हैं'',-''परित्रणाय
साधूनां विनाशाय च दृष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगेयुगे''
(4।8)।
अवतार के पहले की भी समाज की दशा यों कही गयी है,
''जब-जब
धर्म-सत्कर्मों-का खात्मा या अत्यन्त
Ðास
हो जाता है और अधर्म-बुरे
कर्मों-की वृद्धि
हो जाती है तभी-तभी भगवान् खुद आते
हैं''-यदायदाहि
धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्''
(4।7)। इन श्लोकों में जो
'यदा यदा'-जब-जब-तथा
'युगे-युगे'-समय-समय
पर-कहा है उसका तात्पर्य यही है कि ऐसी ही परिस्थिति के साथ अवतार का
ताल्लुक है। जिस प्रकार खेती-बारी के लिए जमीन और सींचने के लिए पानी की
जरूरत है, साँस के लिए जैसे हवा जरूरी है;
ठीक वैसे ही ऐसी परिस्थिति आ जाने पर उसका समुचित सामना
करने, उसके प्रतिकार के लिए अवतार जरूरी है।
पृथिवी, जल, वायु आदि
का काम जिस प्रकार दूसरों से नहीं हो सकता है-जिस तरह पृथिवी आदि के बिना
काम चल नहीं सकता-ठीक उसी तरह अवतार का काम और तरह से,
दूसरों से चल नहीं सकता-उसके बिना काम हो नहीं सकता।
इससे साफ हो जाता है कि जिस प्रकार पृथिवी आदि पदार्थ बनते
हैं,
पैदा होते
हैं
लोगों के समष्टि कर्मों के ही करते उन्हीं के फलस्वरूप,
ठीक वैसे ही अवतार होते
हैं
लोगों के समष्टि कर्मों के ही फलस्वरुप उन्हीं के करते। अब यही देखना है कि
यह बात होती है कैसे।
इसमें
विशेष दिक्कत की तो कोई बात है नहीं। राम,
कृष्ण आदि अवतारों के शरीरों से भले लोगों को-साधु-महात्माओं,
देवताओं,
तपस्वियों,
सदाचारियों और भोलीभाली जनता को-तो बेशक आराम पहुँचता है,
शान्ति मिलती है,
उनकी चिन्ता और परेशानी मिटती है,
उनके कर्मों में आसानी होती,
सहायता पहुँचती है और वे निर्द्वन्द्व विचरते रहते हैं। जैसा कि खुद कृष्ण
ने ही कहा है कि
''लोक-संग्रह
या लोगों के पथदर्शन के खयाल से भी तो कर्म करना ही चाहिए''-''लोक-संग्रहमेवापि
सम्पश्यन्कत्तर्ाुमर्हसि''
(3।20)।
उनने यह भी साफ ही कह दिया है कि
''मेरे
अपने लिए तो कुछ भी करना-धारना शेष नहीं है,
क्योंकि मुझे कोई चीज हासिल करनी जो नहीं है। फिर भी कर्म तो मुस्तैदी से
करता रहता ही हूँ क्योंकि यदि ऐसा न करूँ तो सब लोग मेरी ही देखा-देखी
कर्मों को छोड़ बैठेंगे। नतीजा यह होगा कि सारी गड़बड़ पैदा हो जायगी। फिर तो
अव्यवस्था होने के कारण लोग चौपट ही हो जायँगे-''
''न
मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिाषु लोकेषु किंचन'',
आदि (3।22-26)।
इसके अनुसार तो सभी को अच्छे से अच्छा पथ दर्शन एवं नेतृत्व मिलता है,
जिससे सभी बातों की मर्यादा चल पड़ती है और समाज मजबूती के साथ उन्नति के पथ
में अग्रसर होता है। इस तरह जितनों का कल्याण होता है उतनों का सत्कर्म या
उनके पूर्व जन्म के अच्छे कामों का ही यह फल माना जाना चाहिए। यदि वे आराम
पाते और निर्बाधा आगे बढ़ते हैं तो इसमें दूसरों की कमाई,
प्रारब्ध या पूर्व जन्मार्जित कर्मों की कोई बात आती ही नहीं। जिन्हें सुख
मिलता है,
सुविधाएँ मिलती हैं उनके अपने ही कर्मों के ये फल हैं,
यही मानना होगा।
दूसरी ओर
ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मिटाने के लिए अवतारों के शरीर होते हैं।
जिनकी शैतानियतें मिटानी हैं,
जिन्हें तबाह-बर्बाद करना है अवतारों के करते जितनों को आठ-आठ ऑंसू रोने
पड़ते हैं,
जो
खुद और जिनके सगे-सम्बन्धी भी चौपट होते हैं,
रो-रो मरते हैं,
जिनकी भीषण से भीषण यन्त्रणाएँ होती हैं,
जिनकी स्वेच्छाचारिता बन्द हो जाती और निरंकुशता एवं स्वच्छन्दता पर पाले
पड़ जाते हैं,
उनकी यह दशा होती है यद्यपि अवतारों के शरीरों से ही,
उनके कामों से ही। फिर भी इसका कारण उन्हीं दुराचारियों,
दुष्कृत-दुष्ट-लोगों के अपने ही बुरे कर्म मानने होंगे। यदि किसी की लाठी
से सिर फूटा या तलवार से गला काटा तो यह ठीक है कि सिर फूटने एवं गला कटने
का प्रत्यक्ष कारण लाठी या तलवार है। मगर ऐसे कारणों के सम्पादन करने वाले
वे दुष्कर्म माने जाते हैं जो पहले या पूर्वजन्म में ऐसे लोगों ने किये थे
जिनके सिर फूटे या गले कटे। यह तो कर्मों का मोटा-मोटी हिसाब माना ही जाता
है। इसलिए अवतारों के शरीरों के निर्माण में भी इन दुष्ट जनों के ही बुरे
कर्म कारण हैं। पहले कही चुके हैं कि यदि किसी के शरीर से दूसरों को कष्ट
या आराम पहुँचे तो उनके भी भले-बुरे कर्म उस शरीर के कारण होते हैं।
शरीरवाले के कर्म तो होते ही हैं। फलत: जिस प्रकार साधारण शरीर के निर्माण
में समष्टि कर्म कारण बनते हैं। उसी तरह अवतारों के शरीरों के निर्माण में
भी।
एक बात और
भी जान लेने की है। यह जरूरी नहीं कि पूर्व जन्म के ही भले-बुरे कर्म
वर्तमान जन्म के सुख-दु:खों के कारण हों। इसी देह के अच्छे या गन्दे काम भी
कारण बन सकते हैं,
बन
जाते हैं। बासी या पुराने ही कर्म ऐसा करें यह कोई नियम नहीं है। सब कुछ
निर्भर करता है कर्मों की शक्ति पर,
उनकी ताकत पर,
उनकी भयंकरता या उत्तामता पर। इसीलिए नीतिकारों ने माना है कि
''तीन
साल,
तीन महीने,
तीन पखवारे या तीन दिनों में भी जबर्दस्त कर्मों के भले-बुरे फल यहीं मिल
जाते हैं''-''त्रिभिर्वर्षैस्त्रिभिर्मासैस्त्रिभि:
पक्षैस्त्रिभिर्दिनै:। अत्युत्कटै: पुण्यपापैरिहैव फलमश्नुते।''
इसीलिए तो यह भी कहा जाता है कि
''इस
हाथ दे,
उस
हाथ ले।''
इसलिए दुष्ट जनों के जिन भयंकर कुकर्मों के करते हाहाकार मच जाता है,
बहुत सम्भव है कि अवतारों के कारण वही हों या वह भी हों। इसी प्रकार महान्
पुरुषों के तप और सदाचरण भी,
जो
उन पापी जनों से त्रण पाने के लिए किये जाते हैं,
अवतारों के कारण बन जाते हैं,
बन
सकते हैं। मीमांसकों ने जानें कितने ही ऐसे कर्म माने हैं जिनके फल जल्दी
ही मिलते हैं।
इस प्रकार
समष्टि कर्मों के चलते ही पृथिवी आदि की ही तरह अवतारों के शरीर बनते हैं
यह बात समझ में आ जाती है। जो लोग ऐसा सोचते हों कि हमारे भले-बुरे समष्टि
कर्म भगवान् को नहीं खींच सकते;
क्योंकि वह तो सबके ऊपर माना जाता है,
उनके लिए तो पहले ही कहा जा चुका है कि कर्मों के अनुसार ही तो भगवान् को
चलना पड़ता है। उसे भी कर्म की अधीनता एक अर्थ में स्वीकार करनी ही पड़ती है।
यदि लोगों के कर्मों के अनुसार उसे हजार परेशानी उठानी पड़ती हो,
दौड़-धूप और चिन्ता,
फिक्र करनी पड़ती हो,
तो
यह तो मामूली सी बात ठहरी। जब लोगों ने ऐसा भी माना है कि भक्तजन भगवान् को
नचाते हैं,
तो
फिर अवतार बनना क्या बड़ी बात है?
जिनके कर्मों के करते पूर्व बताये ढंग से परमाणुओं की क्रियाएँ,
दौड़धूप और चावल पेड़,
मनुष्य के शरीर आदि बनना-बिगड़ना निरन्तर जारी है,
अवतारों के शरीर भी उन्हीं की क्रियाओं के भीतर क्यों न आ जायँ,
उन्हीं से तैयार क्यों न हो जायँ?
आखिर ये सारी चीजें होती ही हैं संसार का काम चलाने के ही लिए न?
फिर यदि अवतारों के बिना कोई काम रुकता हो या न चल सकता हो,
तो
उनके शरीर भी वैसे कामों के ही लिए क्यों न बन जायँगे?
यह ठीक है
कि जितनी चीजें बनती हैं सभी अनिवार्य आवश्यकताओं और जरूरतों के ही चलते।
प्रकृति या संसार के भीतर व्यर्थ और फिजूल पदार्थों की गुंजाइश हुई नहीं।
बल्कि प्रकृति तो ऐसी चीजों की दुश्मन है। इसीलिए उन्हें जल्द मिटा देती
है। वैसी ही आवश्यकताओं के चलते अवतार भी होते हैं। यही कारण है कि
आवश्यकताओं की पूर्ति होते ही अवतारों का काम पूरा हो जाता है और उनके शरीर
खत्म हो जाते हैं। किन्हीं का काम कुछ देर से होता है और किन्हीं का जल्द।
कहते हैं कि नृसिंह के बिना हिरण्यकशिपु को कोई मार नहीं सकता था। कहानी तो
ऐसी है कि उसने अपने लिए ऐसा ही सामान कर लिया था। यही वजह है कि भगवान् को
नृसिंह बनना और उसे मार के फौरन विलीन हो जाना पड़ा। पीछे नृसिंह का शरीर रह
न सका। यही बात राम,
कृष्ण आदि के बारे में भी है। जो जो काम उनने किए,
जो
पथदर्शन उनसे हुए वे औरों से हों नहीं सकते थे। मगर उन कामों के लिए कुछ
ज्यादा समय चाहता था। इसीलिए वे लोग देर तक रहे। हमारा मतलब यहाँ पौराणिक
आख्यानों पर मुहर लगाने या उन्हें अक्षरश: सही बताने से नहीं है। हमें तो
यहीं दिखाना है कि अवतारों के लिए दार्शनिक युक्ति के अनुसार जो परिस्थिति
चाहिए वह सम्भव है या नहीं।
यह बात भी
अब साफ होई चुकी कि अवतारों के शरीरों में भगवान् को खिंच आना ही पड़ता है।
अवतार शब्द का तो अर्थ ही है। उतरना या खिंच आना अगर संसार में बुरे-भले
कर्म माया-ममताशून्य जनों तक को अपनी ओर खींच सकते हैं और उनमें दया या रोष
पैदा करवा के हजारों कठिनतम काम उनसे करवा सकते हैं,
तो
फिर भगवान् का खिंच जाना कोई आश्चर्य नहीं है यदि बाँसुरी का स्वर मृग या
साँप को खींच सकता है,
उन्हें मुग्धा एवं बेताब कर सकता है;
यदि बछड़े की आवाज गाय को बहुत दूर से खींच सकती है;
यदि किसी प्रेमी का प्रेम हजारों कोस से किसी को घसीट सकता है,
तो
सृष्टि की जरूरत या लोगों के भले-बुरे कर्म तथा प्रेम और द्वेष भगवान् को
उस शरीर में क्यों नहीं खींच लेंगे। न्याय और वैशेषिक दर्शनों ने तो स्पष्ट
कहा है कि लोगों के कर्मों से ही परमाणुओं में क्रिया जारी होती है और वे
आपस में खिंच के मिलते-मिलते महाकाय पृथिवी,
समुद्र आदि बना डालते हैं। फिर प्रलय के समय उल्टी क्रिया होने से अलग
होते-होते वही सबको मिटा देते हैं। ऐसी दशा में उन्हीं कर्मों से भगवान् के
शरीर क्यों न बन जायँ?
उनमें वह खिंच जाय क्यों नहीं?
अब एक ही
सवाल और रह जाता है। कहा जा सकता है कि शरीर बन जाने पर तो भगवान् की भी
वही हालत हो जायगी जो साधारण जीवों की। वही तकलीफ-आराम,
वही माया-ममता और वही हैरानी-परेशानी होगी ही। इसका उत्तर गीता ने चौथे
अध्याय में ही दे दिया है। वहाँ लिखा है कि,
''अविनाशी
एवं जन्मशून्य होते हुए और सभी पदार्थों का शासक रहते हुए भी मैं अपनी माया
के बल से शरीर धारण करता हूँ। मगर अपने स्वभाव को कायम रखता हूँ जिससे माया
मुझ पर अपना असर नहीं जमा पाती''-''अजोऽपि
सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
संभवाम्यात्ममायया''
(4।6)।
माया कहने और अपने स्वभाव को कायम रखने की बात बोलने का मतलब यह है कि एक
तो भगवान् का शरीर साधारण लोगों जैसा देखने पर भी वैसा नहीं है;
किन्तु मायामय और नटलीला जैसा है। नट की कला की कितनी ही बातें असाधारण
होती हैं। वे देखने में चाहे जो लगें;
मगर उनकी हकीकत कुछ और ही होती है। देखने वाले चकाचौंध में पड़ के और का और
समझ बैठते हैं। यही बात अवतारों के भी शरीरों की हैं। दूसरी बात यह है कि
साधारण लोगों की तरह माया-ममता में वे दबते नहीं। उनका अपना स्वभाव,
अपना ज्ञान,
अपनी अनासक्ति और अपना बेलागपन बराबर कायम रहता है। खानपान आदि सारी
क्रियाएँ उस शरीर के लिए आवश्यक होने के कारण ही होती हैं जरूर।मगर उनमें
वे अवतार लिपटते नहीं,
चिपकते नहीं। वे इन सब बातों से बहुत ऊपर रहतेहैं।
यह भी जान
लेना जरूरी है कि गीता में इस माया को दैवी या अलौकिक शक्तिवाली कहा है,
जिसमें हजारों गुण,
खूबियाँ या करिश्मे होते हैं-''दैवीह्येषा
गुणमयी मममाया''
(7।14)।
इसीलिए उस माया के चलते जो शरीर बनेगा उसमें मामूली नटों के करिश्मों से
हजार गुने अधिक करिश्मे होंगे-चमत्कार होंगे। वह तो महान् इन्द्रजाल होगा।
इसी के साथ-साथ यह भी बात है कि जिस तरह कर्मों की व्यवस्था बता के भगवान्
के शरीर बनने की रीति कही जा चुकी है। वह असाधारण है,
गैरमामूली है। इसीलिए जो निराले,
अलौकिक काम अवतार करते हैं वह औरों में पाये नहीं जाते,
पाये जा नहीं सकते। यह तो सारी प्रणाली ही अलौकिक है,
निराले कर्मों का खेल है,
भगवान् की लीला है। भगवान् भी दिव्य हैं,
निराले हैं। उनकी माया भी वैसी ही है। अनोखे कर्मों से ही उनके शरीर बनते
हैं,
न कि
मामूली कर्मों से। इसीलिए गीता ने कह दिया है कि इन सारी निराली बातों को
जो ठीक-ठीक समझता है,
भगवान् के दिव्य जन्म एवं दिव्य कर्म को जो बखूबी जान जाता है,
मरने के बाद वह पुनरपि जन्म नहीं ले के भगवान् ही बन जाता है-''जन्म
कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्तवत:। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति
मामेति सोऽर्जुन''
(4।9)।
अवतारों
के सम्बन्ध में गीता की बातें सामान्य रूप से बताई जा चुकीं। अब एक खास बात
कहके यह प्रसंग पूरा करना है। हमने जो परमाणुओं के जुटने से पृथिवी आदि के
बनने और अलग होने से उनके नष्ट हो जाने तथा प्रलय के आ जाने की बात कह दी
है उससे यह तो पता लगी गया कि प्रलय और कुछ चीज नहीं है,
सिवाय इसके कि वह कर्मों के,
और
इसीलिए सभी पदार्थों के जो उस समय रह जाते हैं,
विराम का समय है,
विश्राम का काल है। संसार में विश्राम का भी नियम पाया जाता है। इसीलिए
कर्मवाद के माननेवालों ने कर्मों के सिलसिले में ही उसे माना है। इसीलिए वे
प्रलय को कर्मों का विश्राम काल और सृष्टि को उनके काम या फल देने का समय
मानते हैं।
इसी नियम
के अनुसार जब-जब जहाँ-जहाँ समष्टि कर्मों की प्रेरणा से अवतारों की
आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है तब-तब तहाँ-तहाँ अवतार पाये जाते हैं,
होते हैं। किसी खास देश या खास समय में ही अवतारों का मानना भारी भूल है।
गीता को यह बात मान्य नहीं है। इसीलिए अवतार के प्रकरण में सिर्फ
'जब-जब,
या
समय-समय पर'
'यदायदाहि',
'युगे-युगे'
(4।7-8)
यही कहा है। वहाँ किसी देश या मुल्क की बात पायी नहीं जाती है।
पुराण-इतिहासों में भी सिर्फ भूलोक या मत्तर्यलोक ही कहा है और यही बात
प्रधान है। यदि कहीं एकाध जगह भारतवर्ष आया है तो वह या तो यों ही आ गया है
दृष्टान्त के रूप में,
या
अवतार विशेष के सिलसिले में ही,
जो
भारतवर्ष में ही हुए हैं। मगर दरअसल देश या मुल्क का कोई नियम नहीं है।
मानव-समाज के ही कल्याण के लिए अवतार होते हैं और वह समाज सभी देशों में
है। इसलिए यहूदी,
इस्लाम या ईसाई धर्मों में जिन महापुरुषों या प्रमुख आचार्यों की बात आती
है,
जो धर्म
संस्थापक माने जाते हैं,
उन्हें अवतार मानने में गीता को कोई उज्र नहीं है। गीता के अनुसार तो वे
सबके-सब अवतार हईं। यों तो
'यद्यद्विभूतिमत्'
(10।41)
में सभी प्रकार के विलक्षण पुरुषों या पदार्थों को भगवान् की ही विभूति
आम-तौर से माना है।
इस प्रकार
हमने देखा कि यदि ईश्वर या कर्मवाद की शरण ली गयी है तो सिर्फ सृष्टि के
कामों को पूरी तौर से चलाने के लिए। मालूम होता है कि इनके बिना कोई स्थान
खाली था,
गैप-gap-था।
उसी की पूर्ति के लिए इन्हें माना गया। मगर पीछे हमारा पतन ऐसा हो गया कि
हम अपना सारा यत्न छोड़ के इन्हीं भगवान् और भाग्य-कर्म-के भरोसे बैठने लगे!
यही बात अब तक जारी है।
गीता - 6
(शीर्ष पर वापस)
|
|