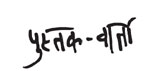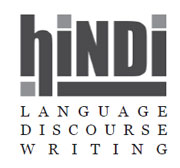5.
गुणवाद और अद्वैतवाद
कर्मवाद एवं अवतारवाद की ही तरह गीता में गुणवाद तथा अद्वैतवाद की भी बात
आयी है। इनके
सम्बन्ध
में भी गीता का वर्णन अत्यन्त सरस,
विलक्षण एवं हृदयग्राही है। यों तो यह बात भी गीता की
अपनी नहीं है। गुणवाद दरअसल वेदान्त, सांख्य और
योगदर्शनों की चीज है। ये तीनों ही दर्शन इस सिद्धान्त
को मानते
हैं
कि सत्तव,
रज और तम इन तीन ही गुणों का पसारा,
परिणाम या विकास यह समूचा संसार है-यह सारी भौतिक
दुनिया है। इसी तरह अद्वैतवाद भी वेदान्त दर्शन का मौलिक सिद्धान्त
है। वह समस्त दर्शन इसी अद्वैतवाद के प्रतिपादन में ही तैयार हुआ है।
वेदान्त ने गुणवाद को भी अद्वैतवाद की पुष्टि में ही लगाया है-उसने उसी का
प्रतिपादन किया है। फिर ये दोनों ही चीजें गीता की निजी होंगी कैसी?
लेकिन इनके वर्णन, विश्लेषण,
विवेचन और निरूपण का जो गीता का ढंग है वही उसका अपना
है, निराला है। यही कारण है कि गीता ने इन पर भी
अपनी छाप आखिर लगाई दी है।
(शीर्ष पर वापस)
परमाणुवाद और आरंभवाद
असल
में प्राचीन दार्शनिकों में और अर्वाचीनों में भी,
फिर चाहे वह किसी देश के हों,
सृष्टि के
सम्बन्ध
में दो मत
हैं-तो
दल
हैं।
एक दल है न्याय और वैशेषिक का,
या यों कहिए कि गौतम और कणाद का। जैमिनि भी उन्हीं के
साथ किसी हद तक जाते
हैं।
असल में उनका मीमांसादर्शन तो प्रलय जैसी चीज मानता नहीं। मगर न्याय तथा
वैशेषिक उसे मानते
हैं।
इसीलिए कुछ अन्तर पड़ जाता है। असल में गौतम और कणाद दोई ने इसे अपना
मन्तव्य माना है। दूसरे लोग सिर्फ उनका साथ देते
हैं।
इसी पक्ष को परमाणुवाद ( Atomic
Theory)
कहते
हैं।
यह बात पाश्चात्य देशों में भी पहले मान्य थी। मगर अब विज्ञान के विकास ने
इसे अमान्य बना दिया। इसी मत को आरम्भवाद
(Theory of creation)
भी
कहते
हैं।
इस पक्ष ने परमाणुओं को नित्य माना है। हरेक पदार्थ के टुकड़े करते-करते
जहाँ रुक जायँ या यों समझिये कि जिस टुकड़े का फिर टुकड़ा न हो सके,
जिसे अविभाज्य अवयव
(Absolute or indivisible particle)
कह
सकते
हैं
उसी का नाम परमाणु (Atom)
है।
उसे जब छिन्न-भिन्न कर सकते ही नहीं तो उसका नाश कैसे होगा?
इसीलिए वह अविनाशी-नित्य-माना गया है।
परमाणु के
मानने में उनका मूल तर्क यही है कि यदि हर चीज के टुकड़ों के टुकड़े होते ही
चले जायँ और कहीं रुक न जायँ-कोई टुकड़ा अन्त में ऐसा न मान लें जिसका खण्ड
होई न सके-तो हरेक स्थूल पदार्थ के अनन्त टुकड़े,
अवयव या खण्ड हो जायँगे। चाहे राई को लें या पहाड़ को;
जब
खण्ड करना शुरू करेंगे तो राई के भी असंख्य खण्ड होंगे-इतने होंगे जिनकी
गिनती नहीं हो सकती,
और
पर्वत के भी असंख्य ही होंगे। वैसी हालत में राई छोटी क्यों और पर्वत बड़ा
क्यों?
यह
प्रश्न स्वाभाविक है। अवयवों की संख्या है,
तो
दोनों की अपरिमित है,
असंख्य है,
अनन्त है। इसीलिए बराबर है,
एक
सी है। फिर छुटाई,
बड़ाई कैसे हुई?
इसीलिए उनने कहा कि जब कहीं,
किसी भाग पर,
रुकेंगे और उस भाग के भाग न हो सकेंगे,
तो
अवयवों की गिनती सीमित हो जायगी,
परिमित हो जायगी। फलत: राई के कम और पर्वत के ज्यादा टुकड़े होंगे। इसीलिए
राई छोटी हो गयी और पर्वत बड़ा हो गया। उसी सबसे छोटे अवयव को परमाणु कहा
है। परमाणुओं के जुटने से ही सभी चीजें बनीं।
(शीर्ष पर वापस)
गुणवाद
और विकासवाद
दूसरा
दल गुणवादियों का है। उनके गुणवाद को परिणामवाद या विकासवाद
(Evolution Theory)
भी
कहते
हैं।
इसे वही तीन दर्शन-वेदान्त,
सांख्य तथा योग-मानते
हैं।
इनके आचार्य
हैं
क्रमश: व्यास,
कपिल और पतंजलि। ये लोग परमाणुओं की
सत्ता
स्वीकार न करके तीन गुणों को ही मूल कारण मानते
हैं।
इन्हें परमाणुओं से इनकार नहीं। मगर ये उन्हें अविभाज्य नहीं मानते
हैं।
इनका कहना यही है कि कोई भी भौतिक पदार्थ अविभाज्य नहीं हो सकता है।
विज्ञान ने भी इसे सिद्ध
कर दिया है कि जिसे परमाणु कहते
हैं
उसके भी टुकड़े होते
हैं।
परमाणुवाद के मानने में जो मुख्य दलील दी गयी है उसका
उत्तर
गुणवादी आसानी से देते
हैं।
वे तो यही कहते
हैं
कि पर्वत के टुकड़े करते-करते एक दशा ऐसी जरूर आ जायेगी जब सभी टुकड़े राई
जैसे ही हो जायँगे। उनकी संख्या भी निश्चित होगी,
फिर चाहे जितनी ही लम्बी हो। अब आगे जो टुकड़े हरेक राई
जैसे टुकड़े के होंगे वह अनन्त-असंख्य-होंगे। नतीजा यह होगा कि इन अनन्त
टुकड़ों से हरेक राई या राई जैसी ही लम्बी-चौड़ी चीज तैयार होगी,
जिसकी संख्या निश्चित होगी। अब यहीं से एक ओर राई रह
जायेगी अकेली और दूसरी ओर उसी जैसे टुकड़ों को,
जिनकी संख्या निश्चित है,मिला के पर्वत बना
लेंगे। इसीलिए वह बड़ा भी हो जायगा। फिर परमाणु का क्या सवाल?
गीता में परमाणुवाद की
गन्ध
भी नहीं है-चर्चा भी नहीं है,
यह
विचित्रबात
है।
इसीलिए
परमाणुवाद और तन्मूलक आरम्भवाद की जगह उनने गुणवाद और तन्मूलक परिणामवाद या
विकासवाद स्थिर किया। उनने अन्वेषण करके पता लगाया कि देखने में चाहे
पृथिवी,
जल
आदि पदार्थ भिन्न हों;
मगर उनका विश्लेषण (Analysis)
करने
पर अन्त में सबों में तीन ही चीजें,
तीन ही तत्तव, तीन ही मूल
पदार्थ पाये जायँगे, पाये जाते
हैं।
इन तीनों को उनने सत्तव,
रजस् और तमस् नाम दिया। आमतौर से इन्हें सत्तव,
रज, तम कहते
हैं।
इन्हीं का
सर्वत्र
अखण्ड राज्य है-सर्वत्र
बोलबाला है। चाहे स्थूल पदार्थ अन्न,
जल, वायु,
अग्नि आदि को लें, या क्रिया,
ज्ञान, प्र्रयत्न,
धैर्य
आदि सूक्ष्म पदार्थों को लें। सबों में यही तीन गुण पाये जाते
हैं।
इसीलिए गीता ने साफ ही कह दिया है कि
''आकाश,
पाताल, मत्तर्यलोक में-संसार
भर में-ऐसा एक भी
सत्ताधारी
पदार्थ नहीं है जो इन तीन गुणों से अछूता हो,
अलग हो''-''न तदस्ति
पृथिव्यां वा दिवि देवेषु व पुन:। सत्तवं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभि:
स्यात्त्रिभिर्गुणै:'' (18। 40)।
यों तो अठारहवें अध्याय
के 7वें
सें लेकर 44 तक के श्लोकों में विशेष रूप से
कर्म,
धैर्य,
ज्ञान, सुख,
दु:खादि सभी चीजों का विश्लेषण करके उन्हें
त्रिगुणात्मक
सिद्ध
किया है। सत्रहवें
अध्याय के शुरू के
22
श्लोकों में भी दूसरी अनेक चीजों का ऐसा ही विश्लेषण
किया गया है। गीता में और जगह भी गुणों की बात पायी जाती है। चौदहवें अध्याय
में यही बात है। वह तो सारा अध्याय
गुणनिरूपण
का ही है। मगर वहाँ गुणों का सामान्य वर्णन है। इसका महत्तव आगे बतायेंगे।
यहाँ पर
आरम्भवाद और परिणामवाद या विकासवाद के मौलिक भेदों को भी समझ लेना चाहिए।
तभी आगे बढ़ना ठीक होगा। आरम्भवाद में यही माना जाता है कि परमाणुओं के
संयोग या जोड़ से ही पदार्थों के बनने का काम शुरू होता है-आरम्भ होता है।
वे ही पदार्थों का आरम्भ या श्रीगणेश करते हैं। वे इस तरह एक नयी चीज तैयार
करते हैं जैसे सूत कपड़ा बनाते हैं। जो काम सूतों से नहीं हो सकता है वह तन
ढँकने का काम कपड़ा करता है। यही उसका नवीनपन है। मगर परिणामवाद या विकासवाद
में तो किसी के जुटने,
मिलने या संयुक्त होने का प्रश्न ही नहीं होता। वहाँ पहले से बनी चीज ही
दूसरे रूप में परिणत हो जाती है,
विकसित हो जाती है। जैसे दूध ही दही के रूप में परिणत हो जाता है। इस मत
में तीनों गुण ही सभी भौतिक पदार्थों के रूप में परिणत हो जाते हैं। कैसे
हो जाते हैं यह कहना कठिन है,
असम्भव है। मगर हो जाते हैं यह तो ठोस सत्य है। जब परमाणुओं को निरवयव
मानते हैं,
तो
फिर उनका संयोग होगा भी कैसे?
संयोग तो दो पदार्थों के अवयवों का ही होता है न?
जब
हम हाथ से लोटा पकड़ते हैं तो हाथ के कुछ भाग या अवयव लोटे के कुछ हिस्सों
के साथ मिलते हैं। मगर निरवयव चीजें कैसे परस्पर मिलेंगी?
इसीलिए आरम्भवाद को मानने से इनकार कर दिया गया। क्योंकि इस मत के मानने से
दार्शनिक ढंग से पदार्थों का निर्माण सिद्ध किया जा सकना असम्भव जँचा।
(शीर्ष पर वापस)
गुण और
प्रधान
सत्तव,
रज, तम को गुण नाम क्यों
दिया गया यह भी मजेदार बात है। जब यही सृष्टि के मूल में है तब तो यही प्रधान
ठहरे,
मुख्य ठहरे, असल ठहरे,
अग्रणी ठहरे। लेकिन इन्हें गुण कहते
हैं!
गुण या गौण का अर्थ है अप्रधान,
जो मुख्य न हो, अग्रणी न हो।
और प्रधान
किसे कहा है?
प्रकृति को, जो इन तीनों
गुणों के मिल जाने से बन जाती है। जब ये तीनों गुण अपनी विषमता छोड़ के सम
रूप से मिल जाते
हैं,
जब इनकी साम्यावस्था हो जाती है तो उसे ही प्रकृति और
प्रधान
कहते
हैं;
हालाँकि वह पीछे की चीज होने से गुण या गौण ठहरी।
साम्यावस्था ही प्रलय की अवस्था है। उस दशा में सृष्टि का काम कुछ भी नहीं
हो पाता-सब कुछ खत्म हो जाताहै।
यद्यपि
चौदहवें अध्याय के
5वें
से 25वें
तक के श्लोकों में इन गुणों की बात विशेष रूप से कही गयी है,
तथापि 5-18
तक के 14
श्लोकों के पढ़ने से,
अभी जो शंका उठी है,
उसका उत्तर मिल जाता है। दूसरी भी बातें विदित हो जाती हैं। इसीलिए इस
अध्याय का विशेष महत्तव हमने माना है। इन्हें गुण क्यों कहते हैं,
इस
सम्बन्ध में पाँचवाँ श्लोक खास महत्तव रखता है। मगर उसका अर्थ करने या और
भी विचार करने के पूर्व हमें सृष्टि की एक बात जान लेने की है जो उससे पहले
के 3,4
श्लोकों में कही गयी है। हम तो हमेशा सृष्टि के ही सम्बन्ध में सोचते हैं
कि यह कैसे बनी,
इसका विकास या पसारा कैसे हुआ। दर्शनों का श्रीगणेश तो इसी बात को लेके
होता ही है,
यह
पहले ही कहा जा चुका है। प्रलय या सृष्टि न रहने की दशा को तो हम पहले
सोचते नहीं। वह तो हमारे सामने की चीज है नहीं। विचार के ही सिलसिले में जब
उसकी बात पीछे आ जाती है,
तो
उस पर भी सोचते हैं। मगर उस दशा में भी वह महज ख्याली और दिमागी चीज होती
है। वह सामने की या ठोस वस्तु तो होती नहीं। फिर पहले उधर खयाल जाये तो
कैसे ?
एक बात और
है। सृष्टि का अर्थ ही है अनेकता,
विभिन्नता (Diversity,
Heterogeniety)।
इसी विभिन्नता को लेके हम शुरू करते
हैं
और अन्वेषण चालू होता है। प्रलय तो इससे
उल्टी
चीज है। उसमें तो एकता और अभिन्नता है,
एकरूपता और समता
(Uniformily & Homogeneity)
है।
जैसा कि गीता ने चौदहवें अध्याय
के 6-18
श्लोकों में बताया है, गुणों
में तो परस्पर
विरोध
है-वे ऐसे
हैं
कि एक दूसरे को खा जायँ। यदि हम तीनों के प्रतिनिधि
के रूप में
पित्त,
वात और कफ को मान लें तो इनकी बात कुछ समझ में आ जाये।
क्रमश: सत्तव, रज, तम
की जगह स्थूल शरीर में
पित्त,
वात, कफ माने जाते भी
हैं।
पित्तदि
में सत्तवादि की ही यों भी प्रधानता
रहती है। सत्तव में प्रकाश,
उजाला, हल्कापन आदि माने
जाते
हैं।
पित्त
में भी यही चीजें
हैं।
पित्त
आग या गर्म है। और उसी में ये बातें होती
हैं।
रज में क्रिया होती है और वायु तो सतत क्रियाशील है। तम भारी है और कफ भी
जकड़ने वाली चीज है। शरीर के लिए जैसे
पित्तदि
तीनों की जरूरत है,
वैसे ही संसार के लिए सत्तवादि की आवश्यकता है। हाँ,
पित्त
आदि की
मात्र
निश्चित रहे तो ठीक हो,
नहीं तो गड़बड़, बेचैनी,
बीमारी हो। यही बात सत्तवादि की भी है। उनकी भी निश्चित
मात्र
है और जहाँ वह बिगड़ी कि गड़बड़ शुरू हुई। जैसे शरीर में एक समय एक ही
पित्त
या
वायु या कफ प्रधान
हो के रहता है,
वैसी ही बात इन गुणों की भी है। एक समय एक ही प्रधान
रहेगा;
बाकी उसी के मातहत। यही बात गीता ने 'रजस्तमश्चाभिभूय'
(14।10) श्लोक में साफ कही
है।
इन गुणों
का परस्पर विरोध तो मानते ही हैं। वायु,
कफ,
पित्त की भी यही बात है। मगर जरा और भी देख लें। ज्ञान के लिए,
हल्केपन के लिए और प्रकाश के लिए क्रिया नहीं चाहिए,
भारीपन नहीं चाहिए। ज्यादा हलचल से प्रकाश रुक जाता है,
ज्ञान नहीं हो पाता,
मन
की एकाग्रता नहीं हो पाती। भारीपन से या तो नींद आती है या बेचैनी होती है।
ज्ञान है सत्तव का काम। हल्कापन और प्रकाश भी उसी का काम है। उसकी विरोधी
क्रिया है रज का काम और भारीपन है तम का। साफ ही देखते हैं कि ज्ञान होने
से मन उसमें लगे तो क्रिया रुक जाये। निद्रा या भारीपन भी जाता रहे।
हल्कापन उसका विरोधी जो है। भारीपन हो तो सारी चीजें दब के रह जायँ,
नींद आ जाय और क्रिया न हो सके। ज्ञान की तो बात ही मत पूछिये।
6
से 9
तथा 11
से 18
तक के श्लोकों में इसी बात का सुन्दरविवरणहै।
मगर खूबी
यह है कि इन तीनों का आपस में समझौता है कि हम लोग मिल के रहेंगे;
नहीं तो किसी की खैर नहीं! राजनीति में आज तो धर्मों और देशों का परस्पर
विरोध है वह तो इनके सामने फीका पड़ जाता है-वह इनके विरोध के सामने कुछ
नहीं है। मगर चाहे हमारी नादानी से धर्मविरोध और राजनीति का विरोध मिटे या
न मिटे,
भाई-भाई की लड़ाई खत्म हो या न हो। मगर इनने तो पारस्परिक विरोध मिटा लिया
है,
समझौता
(Pact)
कर
लिया है। इन्हें दुनिया में सिर ऊँचा करके रहना जो है। और हमें?
हमें तो गैरों के जूते सहने और गुलामी करनी है न?
फिर हमारा मेल कैसे हो? हाँ,
तो इनने यह समझौता कर लिया है कि एक वक्त में हममें एक
ही प्रधान
होगा,
नेता होगा, मुखिया होगा;
बाकी दो उसी के साथ, उसी के
अनुकूल चलेंगे, उसी की मदद करेंगे,
बावजूद इसके कि ये दोनों ही उसके सख्त दुश्मन
हैं!
फिर मौके पर जरूरत के अनुसार हममें दूसरा प्रधान
तथा लीडर होगा और पहला उस जगह से हटेगा। उस समय भी बाकी दो उसी प्रधान
के सहायक होंगे। आवश्यकतानुसार उसे हटाके जब तीसरा मुखिया बनेगा तो बाकी दो
उसके ही सहायक और साथी बनेंगे। यही है इन तीनों का अलिखित समझौता
(Convention)।
पूर्वोक्त दसवें श्लोक का यही अभिप्राय है।
यहीं पर
इन्हें गुण कहने का एक कारण मिल जाता है। जैसा कि अभी कहा गया है,
सृष्टि के रहते हुए इन तीन में दो या अधिकांश हमेशा एक के पीछे रहते हैं,
उसी के सहायक और मददगार होते हैं;
यहाँ तक कि अपना स्वभाव छोड़ के उसके विपरीत उसकी मदद करते हैं,
जैसे बलपूर्वक किसी गुलाम से कोई काम कराया जाय। फर्क यही है कि इनके लिए
बल प्रयोग नहीं है। दूरअन्देशी से खुद ही ये वैसा करते हैं। और इनमें जो एक
कभी प्रधान होता है वही पीछे अप्रधान बन जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि
ये तीनों गुण सृष्टि के मूल कारण होते हुए यद्यपि प्रधान कहे जाने योग्य
हैं,
तथापि
इनकी असली खूबी है दूसरों के अनुयायी बनना,
उनकी सहायता करना,
उनके अनुकूल होना। सृष्टि की दृष्टि से इनकी यह खूबी जरूरी है भी। इसी
विशेषता के खयाल से,
इसी ओर खयाल आकृष्ट करने के ही लिए इन्हें गुण कहा है। दसवें श्लोक से यही
पता चलता है।
अब जरा
दूसरा पहलू देखिए। यदि
5-9
श्लोकों को देखें तो पता चलता है कि ये तीनों ही गुण बाँधने का काम करते
हैं। कोई ज्ञान,
सुख आदि में मनुष्य को लिप्त करके,
लिपटा के उन्हीं चीजों से उसे बाँध देते हैं;
क्योंकि किसी चीज की ज्यादती ही ऐब है,
बन्धन है,
तो
कोई क्रिया और लोभ आदि में फँसा देते हैं। यह नहीं हुआ,
वह
नहीं हुआ,
यह
काम शेष है,
वह
बाकी है इसी हाय-हाय में जिन्दगी गुजरती है। जिस प्रकार सत्तव गुण,
ज्ञान आदि में फँसा के बाँध देता है,
उसी प्रकार रज क्रिया और लोभ आदि में। जाल में फँसाने का काम करने में
ज्ञान सुख,
क्रिया,
लोभ चारे की जगह प्रयुक्त होते हैं। तम का तो फँसाना काम प्रसिद्ध ही है।
वह तो हमेशा का ही बदनाम है। मगर जो उससे अच्छा रज है और जो महान् माने
जानेवाला सत्तव है वह भी फँसाने में किसी से पीछे नहीं है!
''छोटी
बहू तो छोटी,
बड़ी बहू शुभानल्ला !''
और
यह तो जानते ही हैं कि फाँसने और बाँधने का काम रस्सी करती है। फिर चाहे वह
सूत की बारीक या मोटी हो,
या,
और
चीजे की हो। संस्कृत में रस्सी को गुण कहते हैं। इसी का अपभ्रंश हो के गोन
शब्द हो गया। नाव खींचने की रस्सी को गोन कहते हैं। फलत: फँसाने और बाँधने
की ताकत इन गुणों में होने के ही कारण इन्हें गुण कहा है;
ताकि लोग इनसे सजग रहें।
5-9
श्लोकों
से यह स्पष्ट है।
5वें
के उत्तारार्ध्द में तो एक ही साथ तीनों को बाँधनेवाले कह दिया है-'निबधनन्ति
महाबाहो।'
इसीलिए अर्जुन को कहा गया है कि इन गुणों से ऊपर जाओ-'निस्त्रौगुण्यो
भवार्जुन' (2।45)।
इसी चौदहवें अध्याय में भी कहा है कि इन गुणों से अलग ब्रह्मात्मा को
जानने वाले की मुक्ति होती है-'गुणेभ्यश्च
परं वेत्ति'
(14।19),
तथा इन गुणों से ऊपर उठने पर ही मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है-'स
गुणान्समतीयैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते'
(14।26)।
गुणों में
यह परस्पर विरोध और मिलके काम करने की-दोनों-बात योगसूत्र-''परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च
दु:खमेव सर्वं विवेकिन:''
(2।15)-में
और इसके भाष्य में भी अत्यन्त विशद रूप से बताई गयी है। वहीं पर यह भी कह
दिया है कि तीनों गुण परस्पर मिल के ही हर चीज पैदा करते हैं। इसीलिए तो
सभी पदार्थों में तीनों ही गुण पाये जाते हैं। ईश्वरकृष्ण ने
सांख्यकारिकाओं में भी
''सत्तवं
लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रज:। गुरु वर्णकमेव तम: प्रदीवच्चार्थतो
वृत्ति:''
(13)
के द्वारा
इन तीनों गुणों को परस्पर विरोधी बता के बाद में तीनों के मिल के काम करने
का बहुत ही सुन्दर दृष्टान्त दिया है। इनके परस्पर मिलने का कारण भी बताया
है। वह कहता है कि जिस प्रकार दीपक में तेल,
बत्ती और तेज या अग्नि तीनों ही परस्पर विरोधी हैं तथापि तीनों को मिलाये
बिना रोशनी होई नहीं सकती। आग बत्ती और तेल दोनों को ही खत्म करने वाली
है। तेल ज्यादा दे दिया जाय जलना बन्द हो जाय,
बुझ जाय। बत्ती को भी भिगो के विकृत बना देता है। बत्ती भी तेल को सोखती
है अगर सख्त बत्ती या कपड़े का बण्डल डाल दें तो चिराग बुझ जाय। मगर
प्रयोजनवश तीनों को हिसाब से रख के काम चलाते हैं। इस तरह परस्पर मेल से ही
दीपक जलता है। इसी प्रकार संसार के कामों के चलाने औरगुणों के अपने
स्वतन्त्र अस्तित्व के ही लिए तीनों का मिल के काम करना जरूरीहो जाताहै।
(शीर्ष पर वापस)
तीनों गुणों की जरूरत
अब
हमें एक ही बात का विचार करना शेष है जिसका सृष्टि से ही ताल्लुक है। बाद
में प्रलय की बात कह के आगे बढ़ेंगे। सृष्टि की रचना कैसे होती है यह बात तो
प्रलय के ही निरूपण में आगे आयेगी। अभी तो हमें यह देखना है कि इन तीनों
परस्पर
विरोधी
गुणों की क्या जरूरत है। क्या सचमुच ही इन तीनों की आवश्यकता है,
यह
प्रश्न होता है।
उत्तर
में ''हाँ''
कहना
ही पड़ता है। यह कैसे है यह बात और ये तीनों एक दूसरे की मदद कैसे करते
हैं
यह भी एक ही साथ मालूम हो जायगी। यदि सिर्फ सत्तव रहे तो हम ज्ञान,
प्रकाश
तथा सुख से ऊब जायँगे। एक ही चीज का निरन्तर होना
(Monotony)
ही तो
ऊबने का प्रधान
कारण है। इसीलिए तो परिवर्तन जरूरी होता है। ज्ञान के मारे न नींद,
न
खाना-पीना,
न और
कुछ होगा। प्रकाश में
चकाचौंध
हो जायगी। हलका हो के यह संसार कहाँ उड़ जायगा कौन कहे?
यदि
सिर्फ तम हो तो भी दबते-दबते कहाँ जायगा पता नहीं। निरन्तर नींद,
भारीपन,
जड़ता,
ऍंधोरा,
अज्ञान
कौन बर्दाश्त करेगा?
पत्थर
की दशा भी उससे अच्छी होगी। संसार का कोई काम होगा ही नहीं। इसलिए यदि
सत्तव और तम दोनों को ही मानें तो दोनों
एक दूसरे को दबा के खत्म या बेकार (neutralised)
कर
देंगे। फलत: दो में एक का भी काम न होगा। इसीलिए रज आ के दोनों में क्रिया
पैदा करता है,
दोनों को चलाता है; ताकि
दोनों सारी ताकत से आपस में भिड़ न सकें। न दोनों जमेंगे,
स्थिर होंगे और न जम के लड़ेंगे। फिर एक दूसरे को बेकार
कैसे बनाएँगे? यदि रज ही रहे और बराबर क्रिया
होती रहे तो भी वही बेचैनी! सारी दुनिया जल्द घिस जाय,
मिट जाय। इसलिए तम उसे दबा के बीच-बीच में क्रिया को
रोकता है। सत्तव क्रिया का पथ-प्रदर्शन करता है प्रकाश और ज्ञान दे के। मगर
जब तम प्रकाश को रोक देता है तो ज्ञान के अभाव में भी क्रिया रुकती है।
ज्ञान और क्रिया के बिना कुछ होई नहीं सकता। अत्यन्त हलकी चीज स्थिर हो
सकती ही नहीं। फिर उसमें ज्ञान या क्रिया हो कैसे?
उसे वजनी बनाने के लिए भी तो तमोगुण चाहिए ही इस प्रकार
तीनों की जरूरत और परस्पर सहायता स्पष्ट सिद्धहै।
(शीर्ष पर वापस)
सृष्टि और प्रलय
रह गयी
सृष्टि की प्रारम्भिक दशा तथा प्रलय की बात। जब सृष्टि का विचार करने लगे
तो अन्त में यह बात उठी कि जब ये चीजें न थीं तो क्या था?
आखिर न रहने पर ही तो बनने का सवाल पैदा होता है। यह भी
बात है कि जब ये गुण परस्पर
विरोधी
हैं
तो यदि ये कभी
स्वतन्त्र
बन जायें और एक दूसरे की न सुनें,
तब क्या होगा? यह निरी
ख्याली
बात तो है नहीं। इनके प्रतिनिधि
कफ,
वायु,
पित्त
जब
स्वतन्त्र
हो जाते और एक दूसरे की नहीं सुनते तो
त्रिदोष
और सन्निपात होता है और मौत आती है। वही जो कभी एक दूसरे के अनुयायी थे,
आज आजाद हो गये! यही बात गुणों में हो तो?
और जब विश्राम का नियम संसार में लागू है तो ये भी तो
विश्राम करेंगे ही, फिर चाहे देर से करें या
जल्द करें। उस समय क्या हालत होगी और ये किस तरह रहेंगे?
और जब विश्राम का समय पूरा होगा तब कैसे,
क्या होगा? इसी ढंग के सवाल
उठाने पर सृष्टि तथा प्रलय की बात आ जातीहै।
दार्शनिकों ने इन प्रश्नों पर बहुत ही उधड़-बुन करके जवाब दिया कि जब तक ये
गुण ऐसे के ऐसे ही रहेंगे तब तक इनका काम जारी रहेगा ही,
तब
तक तो चूहा बिल खोदता ही रहेगा। इनका स्वभाव ही जो यह ठहरा। इसीलिए,
और
कभी तन जाने पर भी,
तीनों आजाद हो जायँगे,
समान हो जायँगे। फिर तो कोई काम हो न सकेगा। बिना विषमता के,
बिना एक दूसरे की मातहती के तो सृष्टि का काम चल सकता है नहीं और यहाँ तो
''नाई
की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर ठहरे।''
फलत: आजादी या साम्यावस्था में ही विश्राम होगा और यह सारा पसारा रुका
रहेगा। क्योंकि
''रहे
बाँस न बाजे बाँसुरी।''
उसी साम्यावस्था को प्रलय कहते हैं,
प्रकृति कहते हैं और प्रधान भी कहते हैं। ये गुण उसी हालत में जाते और फिर
वहीं से लौटते हैं। इनका यह चरखा रह-रह के चालू रहता है। उससे आगे तो इनकी
पहुँच है नहीं। वही इनकी अन्तिम दशा है। इसीलिए उसे प्रधान कहते हैं।
प्रधान कहते हैं उसे जो सबके अन्त में हो,
आखिर में हो। उसी प्रधान की अपेक्षा इनको गुण कहते हैं। क्योंकि इनकी आखिरी
कृति वही है जिसे ये बनाते हैं अपनी प्रधानता,
मुख्यता को गँवा के। जब इनकी क्रिया रही ही नहीं तो तने भले ही हों और आजाद
भले ही रहें,
फिर भी इनका पता कहाँ रहता है?
वही प्रधान फिर इन्हीं गुणों के द्वारा अपना विस्तार करती है,
सारा पसारा फैलाती है। इसी से उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अर्थ ही है
कि जो खूब करे,
ज्यादा फैले-फैलाये।
कागज
काटने के लिए जो मशीन (Cutting
machine)
आजकल
बनी है। उसकी एक खूबी यह है कि
हैंडिल-चलाने
वाला भाग-पकड़ के मशीन चलाते रहिए और उसकी तेज
धार
कागज तक पहुँच के उसे काट देगी। फिर ऊपर वापस भी चली जायगी। चलाने वाले का
काम बराबर एक ही तरह चलता रहेगा। वह जरा भी
इधर-उधर
या
उलट-फेर न करेगा। मगर उसी चलाने की क्रिया-कर्म-के-फलस्वरूप तेज
धार
ऊपर से नीचे उतर के काटेगी और फिर ऊपर लौट जायगी। जितनी देर तक चलाते रहिए
यही आना-जाना जारी रहेगा। सृष्टि और प्रलय की भी यही हालत है। हमारे काम,
कर्म
(actions)
ही सब
कुछ करते हैं। उन्हीं के करते कभी सृष्टि और कभी प्रलय होती
हैं।
ये दोनों चीजें परस्पर
विरोधी
हैं,
जैसे मशीन की
धर
का नीचे आना और ऊपर जाना। मगर उन्हीं- एक ही-कर्मों के फलस्वरूप ये दोनों
ही होती हैं। कभी भी जीवों को विश्राम मिल जाता
हैं
जिसे प्रलय कहते हैं। गीता ने उसी को
'कल्पक्षय'
(9।7) भी कहा
हैं।
उसे भूतसंप्लव भी कहते हैं। फिर कभी सृष्टि का काम चालू हो जाता
हैं।
प्रलय शब्द भी गीता (14।2)
में आया ही
हैं।
यद्यपि यह
ख्याल हो सकता हैं कि सभी की दशा तो एक सी नहीं हैं। सभी के कर्मों,
कर्मफलभोगों तथा अन्य बातों में भी कोई समानता तो हैं नहीं। यहाँ तो
''अपनी-अपनी
डफली,
अपनी-अपनी
गीत,''
हैं। यहाँ तो
''मुण्डे-मुण्डे
मतिर्भिन्ना तुण्डे-तुण्डे सरस्वती।''
फिर यह कैसे सम्भव हैं कि सभी जीव किसी समय विश्राम में चले जाये और प्रलय
हो जाये?
यदि गीता ने ऐसा माना हैं और अगर दर्शनों ने भी इसे स्वीकार किया हैं तो
इससे क्या?
सभी का कार्य-विराम एक ही साथ हो,
यह
क्या बात?
संसार कोई एक कारखाना या एक ही कम्पनी के अनेक कारखानों का समूह तो हैं
नहीं,
कि
निश्चित समय पर काम से छुट्टी मिल जाये,
या
काम बन्द हो जाया करे। यहाँ तो साफ ही उल्टी बात देखी जाती हैं। तब
कल्पक्षय की बात कैसे मानी जाये?
प्रलय क्यों मानी जाये?
बात तो
हैं कुछ पेचीदगी से भरी जरूर। मगर असम्भव नहीं हैं। ऐसी बातें दुनिया में
होती रहती हैं। यों तो रात में विराम और दिन में काम की बात आमतौर से
सर्वत्र हैं। यह तो सभी के लिए हैं। मगर जहाँ दिन-रात बड़े होते हैं,
जैसे उत्तर ध्रुव के आस-पास,
वहाँ भी और नहीं तो छह मास का दिन एवं उतनी ही लम्बी रात तो होती ही हैं।
प्रकृति की ओर से जब तूफान आता हैं,
बर्फीली आँधियाँ चलती हैं तब तो सभी को एक ही साथ काम बन्द कर देना ही पड़ता
हैं। मगर इन सभी को न भी मानें और अगर इनमें भी कोई गड़बड़ सूझे तो भी तो यह
बात देखी जाती हैं कि किसी गोल घेरे या रास्ते पर चक्कर लगाने वाले यद्यपि
भिन्न-भिन्न चालों वाले होते हैं,
फिर भी ऐसा मौका आता हैं कि कभी न कभी सभी एक साथ मिल जाते हैं। फिर फौरन
आगे-पीछे हो जाते हैं। यों तो आमतौर से आगे-पीछे चलते ही रहते हैं। मगर
चक्कर लगाते-लगाते बहुत चक्करों के बाद देर या सवेर एक बार तो सभी इकट्ठे
हो जाते हैं। फिर आगे-पीछे होके चलते-चलते उतनी ही देर बाद दूसरी-तीसरी बार
भी एकत्र हो जाते हैं। यही सिलसिला चलता रहता हैं। बस,
यही हालत प्रलय या कल्पक्षय की मानिए। इसीलिए हिसाब लगा के एक निश्चित समय
के ही अन्तर पर इसका बारम्बार होना गीता ने भी माना हैं। इस प्रलय को गीता
ने रात भी कहा हैं (8।17-19
में)।
हाँ,
तो
उस प्रलय की दशा से सृष्टि का श्रीगणेश कैसे होता हैं यह बात भी जरा देखें।
गीता के (7।4-6),
(8।17-19),
(9।7-10),
(13।5)
तथा (14।3-5)
में यह बात खास तौर से लिखी गयी हैं। यों छिटपुट एकाध बात प्रसंग से कह
देने का तो कुछ कहना ही नहीं। आठ और नौ अध्यायों में कुछ ज्यादा प्रकाश
डाला गया हैं। जीवों के कर्मों की मजबूरी से उन्हें बार-बार जनमना-मरना
पड़ता हैं। प्रलय के बाद भी यही चीज चालू रहती हैं,
यही गोलमोल बातें वहाँ कही गयी हैं। बेशक,
चौदहवें अध्याय में सृष्टि के श्रीगणेश की खास बात कही गयी हैं और बताया
गया हैं कि यह किस तरह होती हैं। मगर इसे जब हम सातवें और तेरहवें अध्याय
के वर्णन से मिला के तीनों का अर्थ एक साथ करते हैं और चौदहवें के समूचे
गुण-वर्णन को भी उसी के साथ ध्यान में रखते हैं तभी इस बात पर पूरा प्रकाश
पड़ता हैं। चौदहवें अध्याय के
5वें
श्लोक में कहा गया हैं कि
''तीनों
गुण प्रकृति से निकलते हैं''-''गुणा:
प्रकृतिसम्भवा:।''
निकलने का अर्थ तो कही चुके हैं कि साम्यावस्था छोड़ के अपनी विषम अवस्था
में-अपनी असली सूरत में-आते हैं;
न
कि पैदा होते हैं। कैसे बाहर आते हैं यही बात उससे पहले के दो श्लोकों में
माँ के पेट से बच्चे के बाहर आने का दृष्टान्त देकर बताई गयी हैं। उसी का
विशेष विवरण सातवें एवं तेरहवें अध्याय में दिया गया हैं।
यह तो
पहले ही कह चुके हैं कि प्रधान या प्रकृति तो साम्यावस्था हैं,
एकरसता हैं,
अविभिन्नता (homogeneity)
हैं।
उसके विपरीत उस अवस्था को भंग करके ही सृष्टि होती
हैं
जिसमें अनेकता और विभिन्नता (heterogeneity and diversity)
हैं।
यह चीज कैसे होती
हैं,
इनकी प्रक्रिया या क्रम क्या
हैं,
इस पर भी दार्शनिकों ने सोच के जो कुछ तय किया
हैं
वही बात उन दोनों
अध्यायों
में पाई जाती
हैं।
उसमें भी सातवें में बहुत कुछ कमी रह गयी
हैं।
उसकी पूर्ति तेरहवें में हो जाती
हैं।
हाँ,
कुछ ब्योरे की बातें वहाँ नहीं कही गयी हैं,
या
एकाध
में कुछ फर्क भी मालूम पड़ता
हैं।
मगर वह कोई खास चीज नहीं
हैं।
असल बातें ठीक-ठीक मिल जाती हैं। ब्योरा कहाँ तक गिनाया जा सकता
हैं?
ब्योरे में तो जानें कितनी ही बातें होती हैं। अगर
उनमें कुछ छूटें तो फर्क तो मालूम होगा ही।
सांख्यदर्शन की एक कारिका हैं
''मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या:
प्रकृति-विकृतय: सप्त। षोडशकस्तुविकारो न प्रकृतिर्न विकृति: पुरुष:''
(3)।
इसका आशय यह हैं कि
''सृष्टि
की जड़ में प्रकृति हैं। वह किसी से भी पैदा नहीं होती। हाँ,
उससे महान,
अहंकार और आकाश,
वायु,
तेज,
जल,
पृथ्वि के
सूक्ष्म स्वरूप-जिन्हें पंचतन्मात्र कहते हैं-यही सात पदार्थ पैदा होते
हैं। फिर उनसे दूसरी चीजें पैदा होती हैं। इसीलिए इन्हें प्रकृति-विकृत नाम
से पुकारते हैं। वे दूसरी चीजें हैं सोलह-पाँच कर्म-इन्द्रिय,
पाँच ज्ञान-इन्द्रिय,
पाँच महाभूत और अन्त:करण। ये सोलहों विकृति कहाते हैं। पुरुष या जीव तो न
प्रकृति हैं और न विकृति।''
यद्यपि इस कारिका में महान आदि सातों या शेष सोलह का भी नाम नहीं दिया हैं;
तथापि एक और कारिका
''प्रकृतेर्महाँस्ततोऽहंकारस्तमाद्
गणश्च षोडशक:''
(16)
आदि में
सभी को गिना दिया हैं और सातों का क्रम भी बताया हैं कि पहले महान,
तब
अहंकार,
तब
पाँच तन्मात्रएँ। आगे का भी क्रम दे दिया गया हैं। मगर आगे बढ़ने के पहले इन
बातों का थोड़ा स्पष्टीकरण जरूरी हैं।
सांख्यदर्शन ने जीव या पुरुष को तो सबसे निराला कहा हैं। वह न तो किसी से
पैदा होता हैं और न किसी को पैदा करता हैं। वह न प्रकृति हैं,
न
विकृति। प्रकृति कहते हैं कारण को और विकृति कहते हैं कार्य को। वह दो में
एक भी नहीं हैं। रह गये संसार के पदार्थ। सो इन्हें तीन दलों में बाँटा
हैं। पहली हैं मूल प्रकृति या प्रधान। गीता ने इसी को प्रकृति या
महद्ब्रह्म के अलावे भूतप्रकृति भी भूत प्रकृतिमोक्षं च (13।34)
में कहा हैं। अपरा भी कहा हैं जैसा कि आगे लिखा हैं। इससे पंचभूत पैदा होते
हैं। इसी से इसे भूतप्रकृति कहा हैं। यह किसी से पैदा तो होती नहीं;
मगर खुद पैदा करती हैं-यह किसी का कार्य नहीं हैं। इसीलिए इसे अविकृति भी
कहा हैं। दूसरे दल में महान आदि सात आ जाते हैं। इन्हें प्रकृति-विकृति कहा
हैं। ये खुद तो आगे के सोलह पदार्थों को पैदा करते हैं। इसीलिए प्रकृति या
कारण कहाये। मूल प्रकृति से ही ये पैदा होने की वजह से विकृति भी कहे गये।
अब इनसे जो सोलह पदार्थ पैदा हुए वह विकृति कहे जाते हैं। क्योंकि वे इनसे
पैदा होने के कारण ही कार्य या विकृति हो गये। मगर उनसे दूसरी चीजें बनती
हैं नहीं। दस इन्द्रियों या पाँच प्राणों से अन्य पदार्थ पैदा तो होते
नहीं। अन्त:करण या बुद्धि से भी नहीं पैदा होते। चक्षु आदि बाहरी
इन्द्रियाँ हैं और बुद्धि या मन भीतर की। इसीलिए उसे अन्त:करण कहते हैं।
करण नाम हैं इन्द्रिय का। अन्त: का अर्थ हैं भीतरी। गीता ने पुरुष को मिला
के यह चार विभाग नहीं किया हैं। किन्तु सभी को-चारों को-ही प्रकृति कहके
जीव या पुरुष को परा या ऊँचे दर्जे की और शेष तीन को अपरा या नीचे दर्जे की
प्रकृति 'अपरेयमितस्त्वन्यां'
(7।5)
आदि में कहा हैं।
दोनों में
यह दो या चार भेदों का होना कोई खास बात नहीं हैं। मगर पुरुष को भी प्रकृति
कहना जरूर निराला हैं। क्योंकि सांख्य ने साफ ही कहा हैं कि वह प्रकृति
नहीं हैं। असल में गीता वेदान्त दर्शन को ही मानती हैं,
न
कि सांख्य को। इसीलिए सांख्य को जो बातें वेदान्त से मिलती हैं उन्हें तो
माने लेती हैं। लेकिन जो नहीं मिलती हैं वहाँ स्वतन्त्र बात कहती हैं।
वेदान्त ने तो माना ही हैं कि पुरुष या भगवान ने ही पहले सोचा;
पीछे संसार बनाया। वेदान्तदर्शन के दूसरे सूत्र
'जन्माद्यस्य
यत:'
में साफ
ही माना हैं कि भगवान से ही आकाशादि पदार्थों का जन्म होता हैं। इसलिए वही
कारण हैं । यदि वह कारण न होता तो उसे सिद्ध करना असम्भव था। उसकी तब जरूरत
ही क्या थी?
वेदान्त
ने जीव को भगवान का रूप ही माना हैं और दोनों को ही पुरुष कहा हैं। हाँ,
व्यष्टि और समष्टि के भेद के हिसाब से पर पुरुष एवं अपर पुरुष या पुरुष तथा
पुरुषोत्ताम यही दो नाम उसने जीव और ईश्वर को अलग-अलग दिये हैं। गीता ने भी
'उत्तम:
पुरुषस्त्वन्य:' (15।17)
में यही कहा हैं । इसीलिए 'मम
योनि:' (14।3-4)
आदि में पुरुष को ही सृष्टि का पिता और प्रधान या प्रकृति को माता कहा हैं।
गीता सृष्टि-रचना को अन्धे का खेल नहीं मानती। किन्तु सोच-समझ के बनाई चीज
(Planned creation)
मानती
हैं।
(शीर्ष पर वापस)
सृष्टि का क्रम
सोचने-समझने का यह मतलब नहीं कि चलना-फिरना,
उठना-बैठना, खेती-गिरस्ती
आदि हरेक कामों को हरेक आदमियों के बारे में पहले से ही तय कर लिया था। यह
तो भाग्यवाद (Fatalism)
तथा
''ईश्वर
ने जो तय कर दिया वही होगा''
(determinism)
वाली
बात
हैं।
फलत: इसमें करने वालों की जवाबदेही जाती रहती
हैं।
वह तो मशीन की तरह ईश्वर की मर्जी पूरा करने वाले मान लिये जाते हैं। फिर
उन पर जवाबदेही किसी भी काम की क्यों हो और वे पुण्य-पाप के भागी क्यों
बनें?
मशीन की तो यह बात होती नहीं और इस काम में वे ठहरे
मशीन ही। सोचने-समझने का सिर्फ यही आशय
हैं
कि मूलस्वरूप कौन-कौन पदार्थ कैसे बनें कि यह सृष्टि चालू हो,
इसका काम चले, यही बात उसने
सोची और इसी के अनुसार सृष्टि बनायी। यह तो हमारा काम
हैं
कि हममें हरेक आदमी खुद भला-बुरा सोच के अपना रोज का काम करता रहे। इसीलिए
तो हमें बुद्धि
दी गयी
हैं।
उसे देकर ही तो ईश्वर जवाबदेही से हट गया और उसने हम पर अपने कामों की जवाब
देही लाद दी।
अब जरा यह
देखें कि ईश्वर के सोचने और तदनुसार सृष्टि बनाने के मानी क्या हैं। वह
हमारे जैसा देहधारी तो हैं नहीं कि इसी प्रकार सोचे-विचारेगा। यह तो कही
चुके हैं कि प्रलय में प्रधान या प्रकृति समान थी,
एक
रूप थी। उसमें अनेकता और विभिन्नता लाने के लिए सबसे पहले क्रिया होना
जरूरी हैं। क्योंकि क्रिया से ही अनेकता और विभिन्नता होती हैं। मिट्टी का
एक धोंधा हैं। क्रिया के करते ही उसे अनेक टुकड़ों में कर देते या उससे अनेक
बर्त्तन तैयार कर लेते हैं। मगर क्रिया के पहले जानकारी या ज्ञान जरूरी
हैं। यह तो हम कही चुके हैं कि सोच-विचार के यह सृष्टि बनी हैं। एक बात यह
हैं कि यदि फिजूल और बेकार चीजें न बनानी हों,
साथ ही सृष्टि की सभी जरूरतें पूरी करनी हों तो जो कुछ भी किया जाए वह
सोच-विचार के ही होना चाहिए। कुम्हार सोच-साच के ही बर्त्तन बनाता हैं।
किसान खेती इसी तरह करता हैं। नहीं तो अन्धेरखाता ही हो जाये और घड़े की
जगह हांडी तथा गेहँ की जगह मटर की खेती हो जाये। यही कारण हैं कि सांख्य ने
ईश्वर को न मान के भी सृष्टि के शुरू में यह सोचना-समझना या ज्ञान माना
हैं। मगर ज्ञान तो जड़ प्रकृति में होगा नहीं और जीव का काम सांख्य के मत से
सृष्टि करना हैं नहीं। इसीलिए वेदान्त ने और गीता ने भी सृष्टि के मूल में
ईश्वर को माना हैं। वह हैं भी परम-आत्मा या श्रेष्ठ-आत्मा।
वह ज्ञान
होगा भी हम लोगों के ज्ञान जैसा कुछ बातों का ही नहीं,
छोटा या हल्का सा ही नहीं। वह तो सारी सृष्टि के सम्बन्ध का होगा,
व्यापक और बड़े से बड़ा होगा। इसीलिए उसे महत्व या महान कहा हैं। उसके बाद जो
क्रिया होगी उसी को अहम् या अहंकार कहा हैं। यह हम लोगों का अहंकार नहीं हो
के सृष्टि के मूल की क्रिया हैं। समष्टि या व्यापक ज्ञान की ही तरह यह भी
व्यापक या समष्टि क्रिया हैं। नींद के बाद जब ज्ञान होता हैं तो उसके बाद
पहले अहम् या मैं और मेरा होने के बाद ही दूसरी क्रिया होती हैं,
और
प्रलय तो नींद ही हैं न
?
इसीलिए
उसके बाद की समष्टि क्रिया को अहंकार नाम दिया गया हैं। इस अहंकार या
क्रिया के बाद प्रकृति की समता खत्म हो के विभिन्नता आती हैं। और आकाश,
वायु,
तेज
(प्रकाश),
जल,
पृथ्वि इन पाँचों की सूक्ष्म या अदृश्यर् मूर्त्तियाँ (शक्लें) बनती हैं।
इन्हीं से आगे सृष्टि का सारा पसारा होता हैं।
इन पाँच
सूक्ष्म पदार्थों या भूतों के भी,
जिन्हें तन्मात्र भी कहते हैं,
वही तीन गुण होते हैं,
जैसा कि कह चुके हैं। उनमें पाँचों के सात्तिविक अंशों या सत्त्व गुणों से
क्रमश: श्रोत्र,
त्वक्,
चक्षु,
रसना,
घ्राण ये
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बनती हैं,
जिनसे शब्दादि पदार्थों के ज्ञान होते हैं। ज्ञान पैदा करने के ही कारण ये
ज्ञानेन्द्रियाँ कहाती हैं। उन्हीं पाँचों के जो राजस भाग या रजोगुण हैं
उनसे ही क्रमश: वाक,
पाणि (हाथ),
पाँव,
मूत्रोन्द्रिय,
मलेन्द्रिय ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ बनती हैं। इन पाँचों से ज्ञान न हो के
कर्म या काम ही होते हैं। फलत: ये कर्मेन्द्रियाँ कही गईं। और इन पाँचों के
रजोगुणों को मिला के पाँच प्राण-प्राण,
अपान,
व्यान,
समान,
उदान-बने।
ये पाँचों के रजोगुणों के सम्मिलित होने पर ही बनते हैं। उसी तरह,
पाँचों के सत्त्वगुणों को सम्मिलित करके भीतरी ज्ञानेन्द्रिय या अन्त:करण
बनता हैं,
जिसे कभी एक,
कभी दो-मन और बुद्धि-और कभी चार-मन,
बुद्धि,
चित्त,
अहंकार-भी कहते हैं। उसके ये चार भेद चार कामों के ही चलते होते हैं,
जैसे पाँच काम करने से ही एक ही प्राण पाँच प्रकार का हो गया। हमें यह न
भूलना होगा कि जब हम सत्त्व या रजोगुण की बात करते हैं तो यह मतलब नहीं
होता हैं कि खाली वही गुण रहते हैं। यह तो असम्भव हैं। गुण तो तीनों ही
हमेशा मिले रहते हैं। इसीलिए इन्हें एक दूसरे से चिपके हुए-''अन्योन्यमिथुनवृत्तय:-''
सांख्य कारिका (12)
मेंलिखा हैं। इसलिए सत्त्व कहने का यही अर्थ हैं कि उसकी प्रधानता रहती
हैं। इसी प्रकार रज का भी अर्थ हैं। रजोगुण-प्रधान अंश। दोनों में हरेक के
साथ बाकी गुण भी रहते हैं सही;
मगर अप्रधान रूप में।
अब बचे
पाँचों तन्मात्रओं के तम:प्रधान अंश जिन्हें तमोंऽश या तमोगुण भी कहते हैं।
उन्हीं से ये स्थूल पाँच महाभूत-आकाश आदि-बने। जो पहले सूक्ष्य थे,
दीखते न थे,
जिनका ग्रहण या ज्ञान होना असम्भव था,
वही अब स्थूल हो गये। जैसे अदृश्य हवाओं-ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन-को विभिन्न
मात्रओं में मिला के दृश्यजल तैयार कहते हैं;
ठीक वैसे ही इन सूक्ष्म पाँचों तन्मात्रओं के तम प्रधान अंशों को परस्पर
विभिन्न मात्र में मिला के स्थूल भूतों को बनाया गया। इसी मिलाने को
पंचीकरण कहते हैं। पंचीकरण शब्द का अर्थ हैं कि जो पाँचों भूत अकेले-अकेले
थे-एक-एक थे। उन्हीं में चार दूसरों के भी थोड़े-थोड़े अंश आ मिले और वे पाँच
हो गये,
या
यों कहिए कि वे पाँच-पाँच की खिचड़ी या सम्मिश्रण बन गये। दूसरे चार के
थोड़े-थोड़े अंश मिलाने पर भी अपना-अपना अंश। ज्यादा रहा ही। हरेक में आधा
अपना रहा और आध में शेष चार के बराबर अंश तो इसीलिए अपने आध भाग के करते ही
हरेक भूत अलग-अलग रहे। नहीं तो पाँचों में कोई भी एक दूसरे से अलग हो नहीं
पाता। फलत: यह हालत हो गयी कि पृथ्वि में आधा अपना भाग रहा और आधे में शेष
जल आदि चार रहे। यानी समूची पृथ्वि का आधा वह खुद रही और बाकी आधे में शेष
चारों बराबर-बराबर रहे। इस तरह समूची में इन प्रत्येक का आठवाँ भाग रहा।
इसीलिए उसे पृथ्वि कहते ही रहे। जल आदि की भी यही बात समझी जानी चाहिए।
यह ठीक
हैं कि इस विवरण में सांख्य और वेदान्त में थोड़ा सा भेद हैं। पाँच प्राणों
को सांख्यवाले पाँच कर्मेन्द्रियों से जुदा नहीं मानते। इसलिए उनके मत से
पाँच तन्मात्र,
दस
इन्द्रियाँ और अन्त:करण यही सोलह पदार्थ अहंकार के बाद बने। उनके मत में
पाँच तन्मात्र की ही जगह पाँच महाभूत हैं। क्योंकि तन्मात्रओं के तामसी
अंशों को ही मिलाने से ये पाँच भूत हुए। इसीलिए वे तन्मात्रओं और भूतों को
अलग-अलग नहीं मानते। महाभूतों के बनने के बाद तन्मात्रएँ तो रह जाती भी
नहीं। उनके सात्त्विक तथा राजस भागों से ज्ञानेन्द्रियाँ,
कर्मेन्द्रियाँ,
प्राण और अन्त:करण बने। बचे-बचाये तामस अंश से,
महाभूत। बाकी संसार तो इन्हीं महाभूतों का ही पसारा या विकास हैं,
परिणाम हैं,
रूपान्तर हैं,
करिश्मा हैं। इस प्रकार उनके ये सोलह तत्त्व या विकार सिद्ध होते हैं।
वेदान्तियों ने पाँच कर्मेन्द्रिय,
पाँच ज्ञानेन्द्रियों,
मन
और बुद्धि ये दो अन्त:करण-और कभी-कभी मन,
बुद्धि,
चित्त,
अहंकार ये चार अन्त:करण-मान के सत्रह या उन्नीस पदार्थ मान लिये। पाँच
भूतों को मिला लेने पर वे चौबीस हो गये। महान तथा अहंकार को जोड़ने पर
छब्बीस और प्रकृति को ले के सत्ताईस हो गये। सांख्य के मत से तेईस रहे। मगर
यह तो कोई खास बात हैं नहीं। यह ब्योरे की चीज हैं। ये पदार्थ तो सभी-दोनों
ही-मानते ही हैं।
एक बात
और। हम पहले कह चुके हैं कि गीता के मत से गुण प्रकृति से निकले हैं,
बने हैं। मगर हमने अभी-अभी जो कहा हैं उससे तो गुणों के बजाये बुद्धि,
ज्ञान या महत्व,
अहंकार और पंचतन्मात्रएँ-यही चीजें-प्रकृति से निकली हैं। भले ही यह चीजें
गुणमय ही हों। मगर गुणों का निकलना न कह के इन्हीं का निकलना कहने का मतलब
क्या हैं?
बात तो सही हैं। गुणों का बाहर आना सीधे नहीं कहा गया हैं। लेकिन ज्ञान या
महत्व हैं क्या चीज,
यदि सत्त्विगुण नहीं हैं?
ज्ञान तो सत्त्व का ही रूप हैं न?
उसी प्रकार अहंकार हैं क्या यदि रजोगुण या क्रिया हैं नहीं?
अहंकार को तो समष्टि क्रिया ही कहा हैं और क्रिया रजोगुण का ही रूप हैं न?
अब
रह गये पंचभूत जिन्हें तन्मात्र कहते हैं। वह तो तम के ही रूप हैं। आगे जब
पंचीकरण के द्वारा वे दृश्य और स्थूल बनते हैं तब तो उन्हें तम का रूप कहते
ही हैं। फिर पहले भी क्यों न कहें?
यह
ठीक हैं कि तम के साथ भी सत्त्व और रज तो रहेंगे ही,
जैसे इनके इनके साथ तम भी रहता ही हैं। इसीलिए तो पंचतन्मात्रओं के
सत्त्व-अंश से ज्ञानेन्द्रियाँ और रज-अंश से कर्मेन्द्रियाँ बनती हैं।
इसलिए यह तो निर्विवाद हैं कि
'गुणा:
प्रकृति सम्भवा:'-प्रकृति
से गुण ही बाहर होते हैं।
चौदहवें
अध्याय के
3-4
श्लोकों में जो गर्भाधन की बात कही गयी हैं उसका मतलब भी अब स्पष्ट हो जाता
हैं। गर्भाधन के बाद ही गर्भाशय में क्रिया पैदा हो के सन्तान का स्वरूप
धीरे-धीरे तैयार होता हैं। उसके पहले उसमें बच्चे का नाम भी नहीं पाया
जाता। ठीक उसी तरह महान या समष्टि ज्ञानरूप चिन्तन,
संकल्प या सोच-विचार के बाद ही प्रकति के भीतर अहंकार या समष्टि क्रिया
पैदा होके पंचतन्मात्रदि की रचना होती हैं। जब तक भगवान के इस समष्टि ज्ञान
का सम्बन्ध प्रकृति से नहीं होता,
जब
तक वह ख्याल नहीं करता,
तब
तक प्रकृति में कोई भी क्रिया-मन्थन-पैदा नहीं होती जिससे सृष्टि का प्रसार
हो सके। प्रकृति की शान्ति,
समता या एकरसता-घोर गम्भीरता-भंग होती हैं अहंकार रूप मन्थन क्रिया ही से
और वह पैदा होती हैं। महत्वत्तव,
महान या समष्टि ज्ञान के बाद ही। इसी को उपनिषदों में ईक्षण या संकल्प कहा
हैं,
जैसा कि
छान्दोग्य में
'तदैक्षत
बहुस्यां प्रजायेय'
(6।2।3)।
'प्रजायेय'
शब्द का अर्थ हैं कि प्रजा या वंश पैदा करें। इससे गर्भाधन की बातसिद्धहो
जाती हैं। गीता ने भी यही कहा हैं। गीता में गर्भाधन के बाद
'संभव:'
औरर्'मूत्ताय:'लिखने
का मतलब भी ठीक ही हैं। स्वरूप ही तैयार होते हैं,
पैदा होते हैं,
आकृतियाँ बनती हैं।
हमने जो
प्रकृति,
महान अहंकार,
पंचतन्मात्र आदि की बात कही हैं उसका मतलब अब साफ हो गया। यहाँ सचमुच ही
बच्चे या फल की तरह पैदा होने का सवाल तो हैं नहीं। प्रकृति तो पहले से ही
होती हैं। महान का उसी से पीछे सम्बन्ध होता हैं। इसीलिए प्रकृति के बाद ही
उसका स्थान होने से प्रकृति से उसकी उत्पत्ति अकसर लिखी मिलती हैं। महान के
बाद ही आता हैं अहंकार। इसीलिए वह महान से पैदा होने वाला माना जाता हैं;
हालाँकि वह प्रकृति की ही क्रिया हैं। उसके बाद पंचतन्मात्रयें प्रकृति से
ही बनती हैं। मगर कहते हैं कि अहंकार से तन्मात्रएँ पैदा हुईं। यह तो कही
चुके हैं कि ये तन्मात्रएँ महाभूतों के सूक्ष्म रूप हैं। इसीलिए इन्हें भूत
और महाभूत भी कहा करते हैं।
तेरहवें
अध्याय के
''महाभूतान्यहंकारो
बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रियगोचरा:''
(13।5)
का
अर्थ यह हैं कि पाँच महाभूत (तन्मात्रएँ),
अहंकार,
समष्टि बुद्धि (महान),
अव्यक्त या प्रकृति (प्रधान),
ग्यारह इन्द्रियाँ-दस बाहरी और एक अन्त:करण-और इन्द्रियों के पाँच विषय,
यही क्षेत्र के भीतर आते हैं,
क्षेत्र कहे जाते हैं। क्षेत्र का अर्थ हैं शरीर। मगर यहाँ समष्टि शरीर या
सृष्टि की बुनियादी-शुरूवाली-चीज से मतलब हैं। इस श्लोक में वही बातें हैं
जिनका वर्णन अभी-अभी किया हैं। श्लोक के पूर्वार्ध्द में तन्मात्रओं से ही
शुरू करके उल्टे ढंग से प्रकृति तक पहुँचे हैं। मगर ठीक क्रम समझने में
प्रकृति से ही शुरू करना होगा। श्लोक में क्रम से तात्पर्य नहीं हैं। वहाँ
तो कौन-कौन से पदार्थ क्षेत्र के अन्तर्गत हैं,
यही बात दिखानी हैं। इसीलिए उत्तरार्ध्द में ग्यारह इन्द्रियाँ आयी हैं।
नहीं तो उल्टे क्रम में इन्द्रियों से ही शुरू करते। इन्द्रियों के बाद जो
उनके पाँच विषय लिखे हैं उनका कोई सम्बन्ध सृष्टिक्रम से या उसके मूल
पदार्थों से नहीं हैं। पाँच तन्मात्र,
महान आदि के अलावे क्षेत्र के अन्तर्गत जो विषय,
राग,
द्वेष आदि
अनेक चीजें आगे गिनाई गयी हैं उन्ही में ये पाँच विषय भी हैं।
सातवें
अध्याय में इन्द्रियों का नाम न लेकर शेष पदार्थों का उल्लेख
''भूमिरापोनलो
वायु: खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा''
(7।4)
श्लोक में आया हैं। जैसा कि पहले कहा गया हैं,
यह
अपरा या नीचेवाली प्रकृति का आठ भेद या प्रसार बताया गया हैं। तेरहवें
अध्याय के 'महाभूतानि'
की
जगह यहाँ पाँचों भूतों का नाम ही ले लिया हैं
''भूमि,
जल,
अनल (तेज),
वायु और आकाश (ख)।''
मगर उत्तरार्ध्द में जो
''मनो
बुद्धिरेव च अहंकार:''
शब्दों में मान,
बुद्धि और अहंकार का नाम लिया हैं उसके समझने में थोड़ी दिक्कत हैं। जिस
क्रम से तेरहवें अध्याय में नीचे से ही शुरू किया हैं,
उसी क्रम से यहाँ भी नीचे से ही शुरू हैं,
यह
तो साफ हैं। मगर पृथ्वि जल,
तेज,
वायु और
आकाश के बाद तो क्रम हैं अहंकार,
महान और प्रकृति का। इसलिए मन,
बुद्धि,
अहंकार का अर्थ क्रमश: अहंकार,
महान,
और
प्रकृति ही करना होगा। दूसरा चारा हैं नहीं। इसमें बुद्धि का अर्थ महान तो
ठीक ही हैं। वे दोनों तो एक ही अर्थवाले हैं। हाँ मन का अर्थ अहंकार और
अहंकार का प्रकृति करने में जरा उलट-फेर हो जाता हैं। लेकिन किया जाये क्या?
इस
प्रकार गुणवाद और सृष्टि का क्रम तथा उसकी प्रणाली आदि बातें संक्षेप में
स्पष्ट हो गयीं। गीता के मत का इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण भी हो गया। इससे
उसके समझने में आसानी भी होगी।
(शीर्ष पर वापस)
अद्वैतवाद
अब अद्वैतवाद की कुछ बातें भी जान लेने की हैं। गीता का
क्या
ख्याल
इस
सम्बन्ध
में
हैं
यही बात समझनी
हैं।
हालाँकि जब वेदान्त के ही अनुकूल चलना गीता के बारे में कह चुके,
तो एक प्रकार से उसका अर्थ तो मालूम भी हो गया। फिर भी
गीता के वचनों को
उद्धृत
करके ही यह बात कहने में मजा भी आयेगा और लोग मान भी सकेंगे। अद्वैतवाद का
अभिप्राय क्या
हैं,
वह भी तो कुछ न कुछ कहना ही होगा। क्योंकि सभी लोग आम
तौर से क्या जानने गये कि यह क्या बला
हैं?
हमने पहले
यह कहा हैं कि गौतम और कणाद तथा अर्वाचीन दार्शनिक डाल्टन के परमाणुवाद और
तन्मूलक आरम्भवाद की जगह सांख्य,
योग एवं वेदान्त तथा अर्वाचीन दार्शनिक डारविन की तरह गीता भी गुणवान तथा
तन्मूलक परिणामवाद या विकासवाद को ही मानती हैं। इस पर प्रश्न हो सकता हैं
कि क्या वेदान्त और सांख्य का परिणामवाद एक ही हैं?
या
दोनों में कुछ अन्तर हैं?
कहने का आशय यह हैं कि जब दोनों के मौलिक सिद्धान्त दो हैं। तो सृष्टि के
सम्बन्ध में भी दोनों में कुछ तो अन्तर होगा ही। और जब वेदान्त का मन्तव्य
अद्वैतवाद हैं तब वह परिणाम वाद को पूरा-पूरा कैसे मान सकता हैं?
क्योंकि ऐसा होने पर तो गुणों को मान के अनेक पदार्थ स्वीकार करने ही
होंगे। फिर एक ही चेतन पदार्थ-आत्मा या ब्रह्म-को स्वीकार करने का वेदान्त
का सिद्धान्त कैसे रह सकेगा?
यदि सभी गुणों को और उनसे होने वाले पदार्थों को प्रकृति से जुदा न भी
मानें-क्योंकि सभी तो प्रकृति के ही प्रसार या परिणाम ही माने जाते हैं- और
इस प्रकार जड़ पदार्थों की एकता या अद्वैत
(Monism)
मान भी
लें,
जिसे जड़ाद्वैत
(Material monism)
कहते
हैं;
साथ ही आत्मा एवं ब्रह्म की एकता के द्वारा चेतनाद्वैत
(Spiritual monism)
भी मान
लें,
तो भी जड़ और चेतन ये दो तो रही जायेंगे। फिर तो द्वित्व
या द्वैत-दो-होने से द्वैतवाद ही होगा, न कि
अद्वैतवाद। वह तो तभी होगा जब द्वित्व-दो चीज-न हो। अद्वैत का तो अर्थ ही
हैं
द्वैत या दो का न होना।
असल में
वेदान्त का अद्वैतवाद परिणाम और वर्वत्तावाद को मानता हैं। अद्वैतवाद को
विकासवाद या परिणामवाद से विरोध नहीं हैं,
यदि उसकी जड़ में वर्वत्तावाद हो। इसका मतलब यह हैं कि अद्वैतवादी मानते हैं
कि यह दृश्य जगत ब्रह्म या परमात्मा,
जिसे ही आत्मा भी कहते हैं,
में आरोपित हैं,
कल्पित हैं;
यह
कोई वास्तविक वस्तु हैं नहीं। इसकी कल्पना,
इसका आरोप ब्रह्म में उसी तरह किया गया हैं जैसे रस्सी में साँप की कल्पना
अँधरे में हो जाती हैं। या यों कहिए कि नींद की दशा में मनुष्य अपना ही सिर
कटता देखता हैं,
या
कलकत्ता,
दिल्ली आदि की सफर करता हैं। यह आरोप ही तो हैं,
कल्पना ही तो हैं। इसी को अभास भी कहते हैं। किसी पदार्थ में एक दूसरे
पदार्थ की झूठी कल्पना करने को ही अभास कहते हैं। रस्सी में साँप तो हैं
नहीं। मगर उसी की कल्पना अँधरे में करते और डर के भागते हैं। सोने के समय
अपना सिर तो कटता नहीं फिर भी कटता नजर आता हैं। बिस्तर पर घर में पड़े हैं।
फिर कलकत्ता या दिल्ली कैसे चले गये?
मगर साफ ही मालूम होता हैं कि वहाँ गये हैं भर पेट खा के पलंग पर सोये हैं।
मगर सपना देखते हैं कि भूखों दर-दर मारे फिरते हैं! सुन्दर वस्त्र पहने
सोये हैं। मगर नंगे या चिथड़े लपेटे जाने कहाँ-कहाँ भटकते मालूम होते हैं!
यही अभास हैं। इसी को आरोप,
कल्पना आदि नाम देते हैं। इसे भ्रम या भ्रान्ति भी कहते हैं। मिथ्या ज्ञान
और मिथ्या कल्पना भी इसको ही कहा हैं। अद्वैतवादी कहते हैं कि ब्रह्म में
इस समूचे संसार का-स्वर्ग-नरकादि सभी के साथ-अभास हैं,
आरोप हैं। जैसे सपने में सिर कटना,
भूखों चिथड़े लपेटे मारे फिरना आदि सभी बातें मिथ्या हैं,
झूठी हैं;
ठीक वैसे ही यह समूचे संसार-का नजारा झूठा ही ब्रह्म में दीख रहा हैं।
इसमें तथ्य का लेश भी नहीं हैं। यह सरासर झूठा हैं। असत्य हैं। केवल ब्रह्म
या आत्मा ही सत्य हैं। ब्रह्म और आत्मा तो एक ही के दो नाम हैं-''ब्रह्म
सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापर:।''
(शीर्ष पर वापस)
स्वप्न और मिथ्यात्ववाद
जो लोग
इन बातों में अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर पाते वह चटपट कह बैठते हैं कि सपने
की बात तो साफ ही झूठी
हैं।
उसमें तो शक की गुंजाईश
हैं
नहीं। उसे तो कोई भी सच कहने को तैयार नहीं
हैं।
मगर संसार को तो सभी सत्य कहते हैं। सभी यहाँ की बातों को सच्ची मानते हैं।
एक भी इन्हें मिथ्या कहने को तैयार नहीं। इसके सिवाय सपने का संसार केवल
दो
ही-चार
मिनट या घण्टे-आधा घण्टे की ही चीज
हैं,
उतनी ही देर की खेल
हैं-
यह तो निर्विवाद
हैं।
सपने का समय होता ही आखिर कितना लम्बा?
मगर हमारा यह संसार तो लम्बी मुद्दतवाला
हैं,
हजारों-लाखों वर्ष कायम रहता
हैं।
यहाँ तक कि सृष्टि और प्रलय के सिलसिले में वेदान्ती भी ऐसा ही कहते हैं कि
प्रलय बहुत दिनों बाद होती
हैं
और लम्बी मुद्दत के बाद ही पुनरपि सृष्टि का कारबार शुरू होता
हैं।
गीता (8।17।19)
के वचनों से भी यही बात सिद्ध
होती
हैं।
फिर सपने के साथ इसकी तुलना कैसी?
यह तो वही हुआ कि ''कहाँ
राजा भोज, और कहाँ भोजवा तेली!''
मगर ऐसे
लोग जरा भूलते हैं। सपने की बातें झूठी हैं,
झूठी मानी जाती हैं सही। मगर कब?
सपने के ही समय या जगने पर?
जरा सोचें और उत्तर तो दें?
इस
अपने संसार को थोड़ी देर के लिए भूल के सपने में जा बैठें और देखें कि क्या
सपने के भी समय वहाँ की देखी-सुनी चीजें झूठी मानी जाती हैं। विचारने पर
साफ उत्तर मिलेगा कि नहीं। उस समय तो वह एकदम सच्ची और पक्की लगती हैं।
उनकी झुठाई का तो वहाँ ख्याल भी नहीं होता। इस बात का सवाल उठना तो दूर
रहे। हाँ,
जगने पर वे जरूर मिथ्या प्रतीत होती हैं। ठीक उसी प्रकार इस जाग्रत संसार
की भी चीजें अभी तो जरूर सत्य प्रतीत होती हैं। इसमें तो कोई शक हैं नहीं।
मगर सपने में भी क्या ये सच्ची ही लगती हैं?
क्या सपने में ये सच्ची होती हैं,
बनी रहती हैं?
यदि कोई हाँ कहे,
तो
उससे पूछा जाये कि भरपेट खा के सोने पर सपने में भूखे दर-दर मारे क्यों
फिरते हैं?
पेट तो भरा ही हैं और वह यदि सच्चा हैं,
तो
सपने में भूखे होने की क्या बात?
तो
क्या भूखे होने में कोई भी शक उस समय रहता हैं?
इसी प्रकार कपड़े पहने सोये हैं। महल या मकान में ही बिस्तर हैं भी। ऐसी दशा
में सपने में नंगे या चिथड़े लपेटे दर-दर खाक छानने की बात क्यों मालूम होती
हैं?
क्या इससे
यह नहीं सिद्ध होता कि जैसे सपने की चीजें जागने पर नहीं रह जाती हैं,
ठीक उसी तरह जाग्रत की चीजें भी सपने में नहीं रह जाती हैं?
जैसे सपने की अपेक्षा यह संसार जाग्रत हैं,
तैसे ही इसकी अपेक्षा सपने का ही संसार जाग्रत हैं और यही सपने का हैं।
दोनों में जरा भी फर्क नहीं हैं।
सपने की
बात थोड़ी देर रहती हैं और यहाँ की हजारों साल,
यह
बात भी वैसी ही हैं। यहाँ भी वैसा ही सवाल उठता हैं कि क्या सपने में भी
वहाँ की चीजें थोड़ी ही देर को मालूम पड़ती हैं?
या
वहाँ भी सालों और युग गुजरते मालूम पड़ते हैं?
सपने में किसे ख्याल होता हैं कि यह दस ही पाँच मिनट का तमाशा हैं?
वहाँ तो जानें कहाँ-कहाँ जाते,
हफ्तों,
महीनों,
सालों गुजरते,
सारा इन्तजाम करते दीखते हैं,
ठीक जैसे यहाँ कर रहे हैं। हाँ,
जागने पर वह चन्द मिनट की चीज जरूर मालूम होती हैं। तो सोने पर इस संसार का
भी तो यही हाल होता हैं। इसका भी कहाँ पता रहता हैं?
अगर ऐसा ही विचार करने का मौका वहाँ भी आये तो ठीक ऐसी ही दलीलें देते
मालूम होते हैं कि वह तो चन्द ही मिनटों का तमाशा हैं! उस समय यह जाग्रत
वाला संसार ही चन्द मिनटों की चीज नजर आती हैं और सपने की ही दुनिया स्थायी
प्रतीत होती हैं! इसलिए यह भी तर्क बेमानी हैं। इसलिए भुसुण्डी ने अपने
सपने या भ्रम के बारे में कहा था कि
''उभय
घरी मँह कौतुक देखा।''
हालाँकि तुलसीदास ने उनका ही बयान दिया हैं कि उस समय मालूम होता था कि
कितने युग गुजर गये। गौड़ पादाचार्य ने माण्डूक्य उपनिषद की कारिकाओं में
दोनों की हर तरह से समानता तर्क-दलील से सिद्ध की हैं और बहुत ही सुन्दर
विवेचन के बाद उपसंहार कर दिया हैं कि
''मनीषी
लोग स्वप्न और जाग्रत को एक सा ही मानते हैं। क्योंकि दोनों की हरेक बातें
बराबर हैं और यह बिलकुल ही साफ बात हैं''-''स्वप्नजागरिते
स्थाने ह्येकमाहुर्मनीषिण:। भेदानां हि समत्वेन प्रसिध्देनैव हेतुना।''
(शीर्ष पर वापस)
अनिर्वचनीयतावाद
संसार
के
सम्बन्ध
के इस मन्तव्य को मिथ्यात्ववाद और अनिर्वचनीयतावाद भी कहते हैं।
अनिर्वचनीयता का अर्थ
हैं
कि इन चीजों का निर्वचन या निरूपण होना असम्भव
हैं।
इनकी सत्यता तो सिद्ध
हो ही
नहीं सकती। यदि इनको अत्यन्त निर्मूल मानें और कहें कि ये अत्यन्त असत्य
हैं,
जैसे आदमी की सींग न कभी हुई,
न
हैं
और न होगी,
तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि सींग तो कभी दीखती नहीं।
मगर ये तो प्रत्यक्ष ही दीखते हैं। इसलिए मनुष्य की सींग जैसे तो नहीं ही
हैं। यदि इन्हें सत्य और असत्य का मिश्रण मानें,
तो यह और भी बुरा
हैं।
क्योंकि परस्पर
विरोधी
चीजों का मिश्रण असम्भव
हैं।
फलत: मानना ही पड़ता
हैं
कि इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता
हैं-ये
अनिर्वचनीय हैं। मगर यह सही
हैं
कि ये मिथ्या हैं। मिथ्या का मतलब ही यही
हैं
कि मालूम तो हो कि कुछ
हैं;
मगर ढूँढ़ने पर इसका पता ही न लगे। यह विचार कुछ नया और
निराला प्रतीत होता
हैं
सही। मगर रेखागणित में जो बिन्दु का लक्षण बताया गया
हैं
कि उसमें लम्बाई-चौड़ाई कुछ भी होती नहीं,
या रेखा के बारे में जो कहा गया
हैं
कि उसमें केवल लम्बाई होती
हैं,
चौड़ाई नहीं, क्या यह अक्ल
में आने की चीज
हैं?
जिसमें लम्बाई-चौड़ाई कुछ भी न हो या जो सिर्फ लम्बाई
रखता हो ऐसा पदार्थ दिमाग में कैसे घुसेगा? फिर
भी उसे मानते ही हैं।
यह ठीक
हैं कि काम चलाने के लिए-केवल वाद-विवाद और विचार के लिए-वेदान्त ने तीन
प्रकार के पदार्थ माने हैं। एक तो सदा रहने वाला,
वस्तुतत्त्व या परमार्थ पदार्थ,
जिसे ब्रह्म कहिए या आत्मा कहिए। इसीलिए ब्रह्म या आत्मा की हस्ती,
उसके अस्तित्व या उसकी सत्ता को परमार्थ सत्ता भी कहते हैं। दूसरे हैं सपने
या भ्रम के पदार्थ,
जैसे रस्सी में साँप,
सीप में चाँदी या सपने का सिर कटना। ये जब तक प्रतीत होते हैं तभी तक रहते
हैं। प्रतीत या ज्ञान को ही प्रतिभास भी कहते हैं। इसीलिए ये पदार्थ
प्रतिभासिक हैं और इनकी सत्ता हैं प्रतिभासिक सत्ता। तीसरे हैं हमारे इस
जाग्रत संसार के पृथ्वि आदि पदार्थ,
जिनसे हमारा व्यवहार चलता हैं,
काम निकलता हैं। सपने के साँप का जहर तो नहीं चढ़ता। मगर इस साँप का चढ़ता
हैं। यही हैं व्यवहार या काम-काज का चलना। ये चीजें कामचलाऊ हैं,
व्यावहारिक हैं। इसलिए इनकी सत्ता को व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। इस तरह
तीन प्रकार के पदार्थ और उनकी तीन सत्ताएँ हो जाती हैं।
(शीर्ष पर वापस)
प्रतिभासिक
सत्ता
मगर दर
हकीकत व्यावहारिक तथा
प्रतिभासिक
पदार्थ दो नहीं हैं। दोनों ही बराबर ही हैं। यह तो हम सभी सिद्ध
कर चुके हैं।
दोनों
की
सत्ता
में
रत्तीभर
भी अन्तर
हैं
नहीं। इसलिए
दो ही
पदार्थ-परमार्थिक एवं
प्रतिभासिक-माने
जाने योग्य हैं। और
दो ही
सत्ताएँ
भी। लेकिन हम लिखने-पढ़ने और वाद-विवाद में जाग्रत तथा स्वप्न को दो मान के
उनकी चीजों को भी दो ढंग की मानते हैं। यों कहिए कि जाग्रत को सत्य मान के
सपने को मिथ्या मानते हैं। जाग्रत की चीजें हमारे
ख्याल
में सही और सपने की झूठी हैं। इसीलिए खामख्वाह दोनों की दो
सत्ता
भी मान बैठते हैं। लेकिन वेदान्ती तो जाग्रत को सत्य मान सकता नहीं। इसीलिए
लोगों के सन्तोष के लिए उसने व्यावहारिक और
प्रतिभासिक
ये दो भेद कर दिये। इस प्रकार काम भी चलाया। विचार करने या लिखने-पढ़ने में
आसानी भी हो गयी। आखिर अद्वैतवादी वेदान्ती भी जाग्रत और स्वप्न की बात उठा
के और स्वप्न का दृष्टान्त दे के लोगों को समझायेगा कैसे,
यदि दोनों को दो तरह के मन के ही शुरू न करे?
(शीर्ष पर वापस)
मायावाद
जो लोग
ज्यादा समझदार हैं वह वेदान्त के उक्त
जगत-मिथ्यात्व
के सिद्धान्त
पर जिसे
अभासवाद
और मायावाद भी कहते हैं,
दूसरे प्रकार से आक्षेप करते हैं। उनका कहना
हैं
कि यदि यह
जगत
भ्रममूलक
हैं
और इसीलिए यदि इसे
भगवान
की माया का ही पसारा मानते हैं,
क्योंकि माया कहिए, भूल या
भ्रम कहिए, बात तो एक ही
हैं,
तो वह माया रहती
हैं
कहाँ?
वह भ्रम होता
हैं
किसे?
जिस प्रकार हमें नींद आने से सपने में भ्रम होता
हैं
और
उल्टी
बातें देख पाते हैं,
उसी तरह यहाँ नींद की जगह यह माया किसे सुला के या भ्रम
में डाल के
जगत
का दृश्य खड़ा करती
हैं
और किसके सामने?
वहाँ तो सोनेवाले हमीं लोग हैं। मगर यहाँ?
यहाँ यह माया की नींद किस पर सवार
हैं?
यहाँ कौन सपना देख रहा
हैं?
आखिर सोनेवाले को ही तो सपने नजर आते हैं। निर्विकार
ब्रह्म या आत्मा में ही माया का मानना तो ऐसा ही
हैं
जैसा यह कहना कि समुद्र में आग लगी
हैं
या सूर्य पूर्व से पच्छिम निकलता
हैं।
यह तो
उल्टी
बात
हैं,
असम्भव चीज
हैं।
ब्रह्म या आत्मा और उसी में माया?
निर्विकार में विकार? यदि
ऐसा मानें भी तो सवाल
हैं
कि ऐसा हुआ क्यों?
उनका
दूसरा सवाल यह हैं कि माना कि यह दृश्य जगत मिथ्या हैं,
कल्पित हैं। मगर इसकी बुनियाद तो कहीं होगी ही। तभी तो ब्रह्म में या आत्मा
में यह नजर आता हैं,
आरोपित हैं,
अध्यस्त हैं,
ऐसा माना जायेगा। जब कहीं असली साँप पड़ा हैं तभी तो रस्सी में उसका आरोप
होता हैं,
कल्पना होती हैं। जब हमारा सिर सही साबित हैं तभी तो सपने में कटता नजर आता
हैं। जब कोई भूखा-नंगा दर-दर सचमुच घूमता रहता हैं तभी तो हम अपने आपको
सपने में वैसा देखते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि जो वस्तु कहीं हो ही न,
उसी की कल्पना की जाये,
उसी का आरोप किया जाये कल्पित वस्तु की भी कहीं तो वस्तु सत्ता होती ही
हैं। नहीं तो कल्पना या भ्रम हो ही नहीं सकता। इसलिए इस संसार को कल्पित या
मिथ्या मान लेने पर भी कहीं न कहीं इसे वस्तुगत्या मानना ही होगा,
कहीं न कहीं इसकी वस्तुस्थिति स्वीकार करनी ही होगी। ऐसी दशा में मायावाद
बेकार हो जाता हैं। क्योंकि आखिर सच्चा संसार भी तो मानना ही पड़ जाता हैं।
फिर अभासवाद की क्या जरूरत हैं?
लेकिन यदि
हम इनकी तह में घुसें तो ये दोनों शंकाएँ भी कुछ ज्यादा कीमत नहीं रखती हैं,
ऐसा मालूम हो जाता हैं। यह ठीक हैं कि यह नींद,
यह
माया निर्विकार आत्मा या ब्रह्म में ही हैं और उसी के चलते यह सारी खुराफात
हैं। दृश्य जगत का सपना वही निर्लेप ब्रह्म ही तो देखता हैं। खूबी तो यह
हैं कि यह सब कुछ देखने पर भी,
यह
खुराफात होने पर भी वह निर्लेप का निर्लेप ही हैं। मरुस्थल में सूर्य की
किरणों में पानी का भ्रम या कल्पना हो जाने पर भी जैसे मरुभूमि उससे भीग
नहीं जाती,
या
साँप की कल्पना होने पर भी रस्सी में जहर नहीं आ जाता,
ठीक यही बात यहाँ हैं। सपने में सिर कटने पर भी गर्दन तो हमारी ज्यों की
त्यों ही रहती हैं-वह निर्विकार ही रहती हैं। यही तो माया की महिमा हैं।
इसलिए तो गीता ने उसे
'दैवी'
(7।14)
कहा हैं। इसका तो मतलब ही कि इसमें निराली करामातें हैं। यह ऐसा काम करती
हैं कि अचम्भा होता हैं। ब्रह्म या आत्मा में ही सारे जगत की रचना यह कर
डालती हैं जरूर। मगर आत्मा का दरअसल कुछ बनता-बिगड़ता नहीं।
हाँ यह
सवाल हो सकता हैं कि आखिर उसमें यह माया पिशाची लगी कब और कैसे?
हमें नींद आने या भ्रम होने की तो हजार वजहें हैं। हमारा ज्ञान संकुचित हैं,
हम
भूलें करते हैं,
चीजों से लिपटते हैं,
खराबियाँ रखते हैं। मगर वह तो ऐसा हैं नहीं। वह तो ज्ञान रूप ही माना जाता
हैं,
सो भी
अखण्ड ज्ञानरूप,
जो
कभी जरा भी ईधर-उधर न हो। वह निर्लेप और निर्विकार हैं। वह भूलें तो इसीलिए
कर सकता ही नहीं। फिर उसी में यह छछूँदर माया?
यह
अनहोनी कैसे हुई?
यह
बात तो दिमाग में आती नहीं कि वह क्यों हुई,
कैसे हुई,
कब
हुई?
कोई वजह
तो इसकी नजर आती ही नहीं।
(शीर्ष पर वापस)
अनादिता का सिद्धान्त
यही
कारण
हैं
कि ब्रह्म में माया का
सम्बन्ध
अनादि मानते हैं। इस
सम्बन्ध
का ऐसा श्रीगणेश यदि कभी माना
जाये
तो यह सवाल हो सकता
हैं
कि ऐसा क्यों हुआ?
मगर
इसका श्रीगणेश,
इसकी
इब्तदा,
इसका
आरम्भ (beginning)
तो
मानते ही नहीं। इसे तो अनादि कहते हैं। अनादि का तो मतलब ही
हैं
कि जिसकी आदि,
जिसका
श्रीगणेश हुआ न हो। फिर तो सारी शंकाओं की बुनियाद ही चली गयी। संसार में
अनादि चीजें तो
हुईं।
यह कोई
नई
या निराली कल्पना केवल माया के ही बारे में तो
हैं
नहीं। यदि किसी से पूछा
जाये
कि आम का वृक्ष पहले-पहल हुआ या उसकी गुठली हुई?
पहले
वृक्ष हुआ या बीज?
तो
क्या
उत्तर
मिलेगा?
दो में
एक भी नहीं कह के यही कहना पड़ेगा कि बीज और वृक्ष की परम्परा अनादि
हैं।
अक्ल में तो यह बात आती नहीं कि पहले बीज कहें या वृक्ष;
क्योंकि वृक्ष कहने पर फौरन सवाल होगा कि वह तो बीज से ही होता
हैं।
इसलिए उससे पहले बीज जरूर रहा होगा। और अगर पहले बीज ही मानें,
तो
फौरन ही वृक्ष की बात आ
जायेगी।
क्योंकि बीज तो वृक्ष से ही होता
हैं।
कब,
क्या
हुआ यह देखनेवाले हम तो थे नहीं। हमें तो अभी जो चीजें हैं उन्हीं को देख
के इनके पहले क्या था यही ढूँढ़ना
हैं
और यही बात हम करते भी हैं। मगर ऐसा करने में कहीं ठिकाना नहीं लगता और
पीछे बढ़ते ही चले जाते हैं। यही तो
हैं
अनादिता की बात। इसी प्रकार
जगत
और ब्रह्म के
सम्बन्ध
में माया की कल्पना करने में भी हमें अनादिता की शरण लेनी ही पड़ती
हैं।
हमारे लिए कोई चारा
हैं
नहीं। दूसरी चीज मानने या दूसरा रास्ता पकड़ने में हम आफत में पड़
जायेगे
और निकल न सकेंगे। हमें तो वर्तमान को देख के पीछे की बातें सोचनी हैं,
उनकी
कल्पना करनी
हैं,
जिससे
वर्तमान काम चल सके,
निभ
सके। जो चाहें मान सकते नहीं। यही तो हमारी परेशानी
हैं,
यही तो
हमारी सीमा (Limitation)
हैं।
किया क्या
जाये?
इसीलिए मीमांसादर्शन के श्लोकर्वात्तिक
में कुमारिल को कहना पड़ा कि हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि दुनिया की
वर्तमान व्यवस्था के बारे में यदि कोई शक-शुबहा हो तो तर्कदलील से उसे दूर
करके अड़चन हटा दें। हम ऐसा तो हर्गिज कर नहीं सकते कि बे सिर-पैर की बातें
मान के वर्तमान व्यवस्था के प्रतिकूल
जाये-''सिद्धानुगममात्रां
हि कत्तरुं युक्तं परीक्षकै:। न सर्वलोकसिद्धस्य
लक्षणेन नरिवर्त्तनम्''
(1।1।4।133)।
(शीर्ष पर वापस)
निर्विकार में विकार
इसीलिए
निर्विकार में विकार या माया का
सम्बन्ध
साफ ही
हैं।
इसमें झमेले की तो गुंजाइश
हुई
नहीं। सारा संसार जब उसी में
हैं
तो फिर माया का क्या कहना?
हमें तो यही जानना
हैं
कि वह निर्लेप
हैं
या नहीं। विचार से तो सिद्ध
भी हो जाता
हैं
कि वह सचमुच निर्लेप
हैं।
नहीं तो भरपेट खा के सोने पर भूखा क्यों नजर आता?
खाना तो पेट में मौजूद ही
हैं
न?
इसका तो एक ही
उत्तर हैं
कि पेट में खाना भले ही हो,
मगर आत्मा तो उससे निर्लेप
हैं।
वह उससे चिपके,
उसे अपना माने तब न? जगने पर
ऐसा मालूम पड़ता था कि अपना मानती
हैं।
मगर सोने पर साफ पता लग गया कि वह तो निराली
हैं,
मौजी
हैं।
उसे इन खुराफातों से क्या काम?
वह तो लीला करती
हैं,
नाटक करती
हैं।
इसलिए जब चाहा छोड़ के अलग हो गयी और निर्लेप का निर्लेप
हैं।
सपने में भी एक को छोड़ के दूसरे पर और फिर तीसरे पर जाती
हैं
और अन्त में सबको खत्म करती
हैं।
वहाँ कुछ नहीं होने पर भी सब कुछ बना के बच्चों के घरौंदे की तरह फिर चौपट
कर देती
हैं।
असंग जो रही। उसे न किसी मदद की जरूरत
हैं
और न सूर्य-चाँद या चिराग की ही। वह तो खुद सब कुछ कर लेती
हैं।
वह तो स्वयं प्रकाश रूप ही
हैं।
वृहदारण्यक
उपनिषद
के चौथे अध्याय
के तीसरे ब्राह्मण में यह वर्णन इतना सरस
हैं
कि कुछ कहा नहीं जाता। वह पढ़ने ही लायक
हैं।
वहाँ कहते हैं कि-
''स
यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतोमात्रमुपादाय स्वयं विहत्य स्वयं
निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रयं पुरुष: स्वयं
ज्योतिर्भवति।9।
न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्नथयोगान्पथ: सृजते,
न
तत्रनन्दा मुद: प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्मुद: प्रमुद: सृजते,
न
तत्र वेशान्ता: पुष्करिण्य: स्रवंत्योभवन्त्यथवेशान्तान् पुष्करिणी:
स्रवन्ती: सृजते सहि कर्ता।10।
स वा एष एतस्मिन्सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुन:
प्रतिन्यायं प्रतियोन्या-द्रवति स्वप्नायेव सय त्तात्र कि×चत्पश्यत्यनन्वागतस्तेन
भवत्यसोह्ययं पुरुष: (15)।''
अब केवल
दूसरी शंका रह जाती हैं कि जब तक कहीं असल चीज न हो तब तक दूसरी जगह उसकी
मिथ्या कल्पना हो नहीं सकती। इसीलिए कहीं न कहीं संसार को भी सत्य मानना ही
होगा। इसका तो उत्तर आसान हैं। दूसरी जगह उस चीज का ज्ञान होना जरूरी हैं।
तभी और जगह उसकी मिथ्या कल्पना हो सकती हैं। बस,
इतने से ही काम चल जाता हैं। जहाँ उसका ज्ञान हुआ हैं वहाँ वह चीज सच्ची
हैं या मिथ्या,
इसकी तो कोई जरूरत हैं नहीं। कल्पना की जगह वही चीज प्रतीत होती हैं,
यही देखते हैं। न कि उसको सारी बातें प्रतीत होती हैं,
या
उसकी सत्यता और मिथ्यापन भी प्रतीत होता हैं। यदि किसी ने बनावटी,
इन्द्रजाल का या इसी तरह का साँप,
फल
या फूल देख लिया;
उससे पहले उसे इन चीजों की कहीं भी जानकारी न रही हो;
उसी के साथ यह भी मालूम हो जाये कि ये चीजें मिथ्या हैं,
सच्ची नहीं;
तो
क्या कहीं उनका भ्रम होने पर यह भी बात भ्रम के साथ ही मालूम हो जायेगी कि
ये मिथ्या हैं,
बनावटी हैं?
यदि ऐसा ज्ञान हो जाये तो फिर भ्रम कैसा?
ऐसी जानकारी तो भ्रम हटने पर ही होती हैं। यह तो कही नहीं सकते कि झूठी
चीजें ही जिनने देखी हैं न कि सच्ची भी,
उन्हें भ्रम हो ही नहीं सकता। भ्रम होता हैं अपनी सामग्री के करते और यदि
वह सामग्री जुट जाये तो सच्ची-झूठी चीज के करते वह रुक नहीं सकता। इसलिए
जिस चीज का भ्रम हो उसका अन्यत्र सत्य होना जरूरी नहीं हैं;
किन्तु उसकी जानकारी ही असल चीज हैं। जानकारी बिना सत्य वस्तु का भी कहीं
भ्रम नहीं होता हैं। जानें ही नहीं,
तो
दूसरी जगह उसकी कल्पना कैसे होगी?
इसी प्रकार इस संसार का भी कहीं अन्यत्र सत्य होना जरूरी नहीं हैं। किन्तु
किसी एक स्थान पर भ्रम से ही यह बना हैं। उसी की कल्पना दूसरी जगह और इसी
तरह आगे भी होती रहती हैं। एक बार जिसकी कल्पना आत्मा में हो गयी उसी की
बार-बार होती रहती हैं। यह कल्पित ही संसार अनादिकाल से चला आ रहा हैं।
मगर हमें
इन दार्शनिक विवादों में न पड़ के केवल अद्वैतवाद का सिद्धान्त मोटा-मोटी
बता देना हैं और यह काम हमने कर दिया। यहीं पर यह भी जान लेना होगा कि जहाँ
एक बार इस दृश्य जगह का अभास या आरोप आत्मा या ब्रह्म में हो गया कि
वर्वत्तावाद का काम हो गया। चेतन ब्रह्म में इस जड़ जगत के आरोप को ही
वर्वत्तावाद कहते हैं। जहाँ तक इस दृश्यजगत का ब्रह्म से ताल्लुक हैं वहीं
तक वर्वत्तावाद हैं। मगर इस जगत की चीजों के बनने-बिगड़ने का जो विस्तार या
ब्योरा हैं वह तो गुणवाद के आधार पर विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार ही
होता हैं। वर्वत्तावाद ने इन्हें मिथ्या सिद्ध कर दिया। अब परिणाम या
विकासवाद से कोई हानि नहीं। क्योंकि इससे इन पदार्थों की सत्यता तो हो सकती
नहीं। वर्वत्तावाद ने इनकी जड़ ही खत्म जो कर दी हैं। उसके न मानने पर ही यह
खतरा था,
द्वैतवाद आ जाने की गुंजाइश थी। बस,
इतने के ही लिए वर्वत्तावाद आ गया और काम हो गया।
(शीर्ष पर वापस)
गीता,
न्याय और परमाणुवाद
आश्चर्य की बात कहिए या कुछ भी मानिए;
मगर यह सही
हैं
कि गीता में गौतम और कणाद का परमाणुवाद पाया नहीं जाता। इसकी कहीं चर्चा तक
नहीं
हैं
और न गौतम या कणाद की ही। विपरीत इसके
गुर्णकीर्त्तन
और गुणवाद तो भरा पड़ा
हैं,
जैसा कि पहले बताया जा चुका
हैं।
इतना ही नहीं। जिन योग,
सांख्य या वेदान्तदर्शनों ने इसे मान्य किया
हैं
उनका भी उल्लेख
हैं
और उनके आचार्यों का भी। यह ठीक
हैं
कि योगदर्शन के
प्रर्वतक
पतंजलि का जिक्र नहीं
हैं।
मगर योग की विस्तृत चर्चा पाँच,
छह, आठ और अठारह
अध्यायों
में खूब आयी
हैं।
यों तो प्रकारान्तर से यह बात और
अध्यायों
में भी मन के
निरोध
या आत्मसंयम के नाम से बार-बार आयी ही
हैं।
पतंजलि से इसी बात को
'योगश्चित्तवृत्ति
निरोध:'
(1।2) तथा 'अभास
वैराग्याभ्यां तन्निरोधा:'
(2।12) आदि सूत्रों
में साफ ही कहा
हैं।
गीता के छठे अध्याय
में मालूम होता
हैं,
यह दूसरा
सूत्र
ही जैसे
उध्दृत
कर दिया गया हो
'अध्यासेन
तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते' (6।35)।
चौथे अध्याय
के 'आत्मसंयमयोगाग्नौ'
(4।27) में तो साफ ही मन के
संयम को ही योग कहा
हैं।
और स्थानों में भी यही बात
हैं।
पाँचवें अध्याय के
27, 28
श्लोकों में, छठे अध्याय के
10-26 श्लोकों में तथा आठवें अध्याय के
12, 13 श्लोकों में तो साफ ही योग के प्राणायाम की बात
लिखी गयी
हैं।
अठारहवें के
51-53 श्लोकों में भी जिस
ध्यानयोग
की बात आयी
हैं,
उसी का उल्लेख पतंजलि ने 'यथाभिमतध्यानाद्वा'
(1।35), 'यमनियमासन
प्राणायाम प्रत्याहार
ध्यानधारणासमाधायोऽष्टावंगानि'
(2।29) तथा 'तत्र
प्रत्ययैकतानता
ध्यानम्'
(3।2) सूत्रों
में किया
हैं।
(शीर्ष पर वापस)
वेदान्त,
सांख्य और गीता
सांख्य
और वेदान्त का तथा उनके
प्रर्वतक
आचार्यों का भी तो नाम आया ही
हैं।
सांख्य के
प्रर्वतक
कपिल का उल्लेख
'कपिलोमुनि:'
(10।26) में तथा वेदान्त के
आचार्य व्यास का 'मुनीनामप्यहं व्यास:'
(10।37) में आया
हैं।
पहले कपिल का और पीछे व्यास का। इन दर्शनों का क्रम भी यही माना जाता
हैं।
इसी प्रकार 'वेदान्तकृद्वेदविदेव
चाहम्' (15।15) में
वेदान्त का और 'सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि'
(18।13) तथा 'प्रोच्यते
गुणसंख्याने' (18।19)
में सांख्यदर्शन का उल्लेख
हैं।
कृतान्त और सिद्धान्त
शब्दों का एक ही अर्थ
हैं।
इसलिए 'सांख्ये
कृतान्ते' का अर्थ
हैं
'सांख्यसिद्धान्त
में।'
सांख्यवादी भी तो आत्मा को अकर्ता,
केवल तथा निर्विकार मानते हैं और यही बात यहाँ लिखी गयी
हैं।
इसी प्रकार गुणसंख्यान शब्द का अर्थ
हैं
गुणों का वर्णन जहाँ पाया
जाये।
सांख्य शब्द का भी तो अर्थ
हैं
गिनना,
वर्णन करना। सांख्य ने तो गुणों का ही ब्योरा ज्यादातर
बताया
हैं।
इसीलिए उसे गुणसंख्यानशास्त्र
भी कह दिया
हैं।
शेष सांख्य और योग शब्द ज्ञान आदि के ही अर्थ में गीता में आये हैं।
(शीर्ष पर वापस)
गीता में मायावाद
यह ठीक
हैं
कि मायावाद की साफ चर्चा गीता में नहीं आती। मगर माया का और उसके भ्रम में
डालने आदि कामों को बार-बार जिक्र उसमें आया ही
हैं।
'सम्भवाम्यात्ममायया'
(4।6) 'दैवी ह्येषा गुणमयी
मम माया दुरत्यया' (7।14), 'माययापहृतज्ञाना'
(7।15), 'योगमाया समावृत:'
(7।25), 'यन्त्रारूढानि
मायया' (18।61)
में जिस प्रकार माया का उल्लेख
हैं,
जैसा चौदहवें अध्याय में प्रकृति का वर्णन आया
हैं, 'मयाध्यक्षेण
प्रकृति:' (9।0)
में जिस तरह प्रकृति का नाम लिया
हैं,
तेरहवें अध्याय
के 'भूतप्रकृतिमोक्षं
च' (13।34) आदि
श्लोकों में बार-बार प्रकृति का उल्लेख जिस प्रसंग में आया
हैं
तथा 'महाभूतान्यहंकारो
बुद्धिरव्यक्तमेव
च' (13।5)
में जो अव्यक्त शब्द
हैं
ये सभी माया के ही अर्थ में आ के वेदान्त के मायावाद के ही समर्थक हैं
तेरहवें अध्याय
के शुरू में जो
क्षेत्रज्ञ
का बार-बार जिक्र आया
हैं
और 'एतत्क्षेत्रां
समासेन सविकारमुदाहृतम्' (13।6)
में
क्षेत्र
का उसके घास-पात-विकार-के साथ जो वर्णन आलंकारिक ढंग से किया गया
हैं
वह भी इसी चीज का समर्थक
हैं।
क्षेत्र
तो खेत को कहते हैं और जैसे खेतिहर खेत के घास-पात को साफ करके ही सफल खेती
कर सकता
हैं,
ठीक उसी प्रकार यह
क्षेत्रज्ञ-आत्मा-रूपी
खेतिहर भी रागद्वेष आदि घास-पत्तों
को निर्मूल करके ही अपने कल्याण का उत्पादन इस खेत-शरीर-में कर सकता
हैं,
यही बात वहाँ कही गयी
हैं।
मगर वहाँ समष्टि शरीर या माया को ही
क्षेत्र
कहने का तात्पर्य
हैं।
व्यष्टि शरीर तो उसके भीतर आई जाते हैं। शुरू में जो महाभूत,
अहंकार आदि का उल्लेख
हैं
वह इसी बात का सूचक
हैं।
(शीर्ष पर वापस)
ब्रह्मज्ञान और लोकसंग्रह
जहाँ
तक गीता का ताल्लुक इस मिथ्यात्व के सिद्धान्त
से और तन्मूलक अद्वैतवाद से
हैं
उसे बताने के पहले यह ज्ञान लेना जरूरी
हैं
कि संसार को मिथ्या मानने के बाद अद्वैतवाद एवं अद्वैततत्त्व
के ज्ञान का व्यवहार में कैसा रूप होता
हैं।
क्योंकि गीता तो केवल एकान्त में बैठ के समाधि
लगानेवालों के लिए
हैं
नहीं। वह तो व्यावहारिक संसार का पारमार्थिक दुनिया के साथ मेल स्थापित
करती
हैं।
उसकी नजर में तो अद्वैतब्रह्म के ज्ञान के बाद संसार के व्यवहारों में
खामख्वाह रोक होती नहीं। यह ठीक
हैं
कि कुछ लोगों की
मनोवृत्ति
बहुत ऊँचे चढ़ जाने से वे संसार के व्यवहार से अलग हो जाते हैं। मगर ऐसे लोग
होते हैं कम ही। ज्यादा तो ऐसे ही होते हैं जो लोकसंग्रह का काम करते रहते
ही हैं। गीता की इसी दृष्टि का मेल अद्वैतवाद से होता
हैं।
इसीलिए पहले उस अद्वैतवाद का इस दृष्टि से जरा विचार कर लेना जरूरी
हैं।
असल में
ब्रह्म ही सत्य हैं,
जगत मिथ्या हैं और आत्मा ब्रह्मरूप ही हैं,
उससे पृथक् नहीं हैं,
इस
दृष्टि के,
इस
विचार के दो रूप हो सकते हैं। या यों कहिए कि इस विचार को दो प्रकार से
प्रकाशित किया जा सकता हैं। रस्सी में साँप का भ्रम होने के बाद जब चिराग
आने या नजदीक जाने पर वह दूर हो जाता तथा साँप मिथ्या मालूम पड़ता हैं,
तो
इस बात को प्रकाशित करते हुए या तो कहते हैं कि यह तो रस्सी ही हैं,
या
साँप-वाँप कुछ भी नहीं हैं। यदि दोनों को मिला के भी बोलें तो यही कहेंगे
कि वह तो रस्सी ही हैं और कुछ नहीं,
या
रस्सी के अलावे साँप-वाँप कुछ नहीं हैं। इन दोनों कथनों में और कुछ बात
नहीं हैं,
सिवाय इसके कि पहले कथन में विधिपक्ष
(Positive side)
पर
विशेष जोर
हैं,
वही मुख्य चीज
हैं।
उसमें
निषेध
पक्ष (Negative side)
अर्थ-सिद्ध
हैं।
उस पर जोर नहीं
हैं।
यदि वह बात बोलते भी हैं तो विधिपक्ष
की मजबूती के ही लिए। विपरीत इसके दूसरे कथन में
निषेध
पक्ष पर ही जोर
हैं,
वही
प्रधान
बात
हैं।
यहाँ विधिपक्ष
पर जोर न दे के उसे निषेध की दृढ़ता के ही लिए कहते हैं।
ठीक इसी
तरह संसार के बारे में भी अद्वैत पक्ष को ले के कह सकते हैं कि यह तो
ब्रह्म ही हैं और कुछ नहीं,
या
ब्रह्म के अलावे यह जगत कुछ चीज नहीं हैं। यहाँ भी पहले कथन में ब्रह्म की
ही प्रधानता और उसकी जगद्रूपता ही विवक्षित हैं-उसी पर जोर हैं। जगत का
निषेध तो अर्थ-सिद्ध हो जाता हैं जो उसी ब्रह्मरूपता को दृढ़ करता हैं।
दूसरे कथन में जगत का निषेध ही असल चीज हैं। विधिपक्ष उसी को पुष्ट करता
हैं। इसी तरह आत्मा ब्रह्म रूप ही हैं,
उससे जुदा नहीं हैं ऐसा कहने में भी विधि और निषेधपक्ष आ जाते हैं।
ब्रह्मरूप कहना विधिपक्ष हैं और आत्मा से अलग ब्रह्म नहीं हैं यह
निषेधपक्ष। बात तो वही हैं। मगर कहने और जोर देने में फर्क हैं और गीता के
लिए वह बड़े ही काम की चीज हैं। गीता इस फर्क पर पूर्ण दृष्टि रख के चलती
हैं। दरअसल यदि पूछा जाये तो गीता ने निषेधपक्ष को एक प्रकार से भुला दिया
हैं। उसने उस पर जोर न दे के विधिपक्ष पर ही जोर दिया हैं और इसकी वजह हैं।
(शीर्ष पर वापस)
असीम प्रेम का मार्ग
कर्म
का मार्ग तो
निषेध
का रास्ता
हैं
नहीं। वह तो विधि
का ही मार्ग
हैं
और गीताकर्म से ही शुरू करके अकर्म या कर्मत्याग पर-संन्यास पर-पहुँचती
हैं।
उसके संन्यास की परख,
उसकी जाँच कर्म से ही होती
हैं।
गीता में कर्म शुरू करके ही संन्यास को आगे हासिल करते और उसे पक्का बनाते
हैं। ऐसी हालत में
निषेधपक्ष
उसके किस काम का
हैं?
सो भी पहले ही? वह तो अन्त
में खुद-ब-खुद आ ही जाता
हैं।
यदि उसका अवसर आये। वह खामख्वाह आये ही यह हठ भी तो गीता में नहीं
हैं।
जब ब्रह्म को अपनी आत्मा का ही रूप मानते हैं तो अपना होने से कितना अलौकिक
प्रेम उसमें होता
हैं!
दो रहने से तो फिर भी जुदाई रही गयी यद्यपि वह उतनी दु:खद नहीं
हैं।
इसीलिए प्रेम में-उसके साक्षात प्रकट करने में,
प्रकट होने में-कमी तो रही जाती
हैं,
बाधा
तो रही जाती
हैं।
दो के बीच में वह बँट जाता जो
हैं-कभी
ईधर
तो कभी
उधर।
यदि एक ओर पूरा
जाये
तो दूसरी ओर खाली! यदि
ईधर
आये तो वह सूना! दोनों की चिन्ता में कहीं जम पाता नहीं । किसी एक को छोड़ना
भी असम्भव
हैं।
यह बँटवारे की पहेली बड़ी बीहड़
हैं,
पेचीदा
हैं।
मगर
हैं
जरूर।
देशकोश,
गाँव,
परिवार,
घर,
स्त्री,
पुत्र,
शरीर,
इन्द्रियाँ,
आत्मा वगैरह को देखें तो पता चलता हैं कि जो चीज अपने आपसे जितनी ही दूर
पड़ती हैं उसमें प्रेम की कमी उतनी ही होती हैं। दूर तक पहुँचने में समय और
दिक्कत तो होती हैं और ताँता भी तो रहना ही चाहिए। नहीं तो स्रोत ही टूट
जाये,
सूख जाये
और अपने आप से ही अलग हो जायें। इसीलिए ज्यों-ज्यों नजदीक आइये,
दिक्कत कम होती जाती हैं और ताँता टूटने या स्रोत सूखने का डर कम होता जाता
हैं। मगर फिर भी रहता हैं कुछ न कुछ जरूर। इसीलिए जब ऐसा मौका आ जाये कि
देश और गाँव में एक ही को रख सकते हैं तो आमतौर से देश को छोड़ देते हैं और
गाँव को ही रख लेते हैं। प्रेम की कमी-बेशी का यही सबूत हैं। इसी तरह
हटते-हटते पुत्र,
शरीर और इन्द्रियों तक चले जाते हैं। मगर आत्मा की मौज या आनन्द में उसके
मजा में किरकिरी डालने पर,
या
कम से कम ऐसा मालूम होने पर कि शरीर या इन्द्रियों के करते आत्मा
का-अपना-मजा किरकिरा हो रहा हैं,
आत्महत्या-शरीर का नाश-या इन्द्रियों का नाश तक कर डालते हैं! क्यों?
इसीलिए न,
कि
आत्मा तो अपने से आप ही हैं। अपने से अत्यन्त नजदीक हैं?
यही बात याज्ञवल्क्य ने मैत्रोयी से वृहदारण्यक में कही हैं और सभी के साथ
के प्रेमों को परस्पर मुकाबिला करके अन्त में आत्मा में होने वाले प्रेम को
सबसे बड़ा-सबसे बढ़ के-यों ठहराया हैं-
''नवा
अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति''(4।5।6)।
(शीर्ष पर वापस)
प्रेम और अद्वैतवाद
यदि
ब्रह्म या परमात्मा में असली प्रेम करना
हैं
जो सोलह आना हो और निर्बध हो,
अखण्ड हो, एकरस हो,
निरन्तर हो, अविच्छिन्न हो,
तो आत्मा और ब्रह्म के बीच का भेद मिटाना ही होगा
- उसे जरा भी न रहने देकर दोनों को एक करना ही होगा। यदि सच्ची भक्ति चाहते
हैं तो दोनों को-आशिक और माशूक को-एक करना ही होगा। यही असली भक्ति
हैं
और यही असली अद्वैतज्ञान भी
हैं।
इसीलिए गीता ने भक्तों के चार भेद गिनाते हुए अद्वैतज्ञानी को भी न सिर्फ
भक्त कहा
हैं,
किन्तु
भगवान
की अपनी आत्मा ही कह दिया
हैं-अपना
रूप ही कह दिया
हैं,-'ज्ञानी
त्वात्मैव मे मतम्' (7।18)।
जरा सुनिए, गीता क्या कहती
हैं।
क्योंकि पूरी बात न सुनने में मजा नहीं आयेगा। गीता का कहना
हैं
कि, ''चार
प्रकार के सुकृती-पुण्यात्मा- लोग मुझमें-भगवान
में-मन लगाते,
प्रेम करते हैं, वे हैं
दुखिया या कष्ट में पड़े हुए, ज्ञान की इच्छावाले,
धन-सम्पत्ति
चाहने वाले और ज्ञानी। इन चारों में ज्ञानी तो बराबर ही मुझी में लगा रहता
हैं।
कारण,
उसकी नजरों में तो दूसरा कोई
हुई
नहीं। इसीलिए वह
सभी
से श्रेष्ठ
हैं।
क्योंकि वह मेरा अत्यन्त प्यारा
हैं
और मैं भी उसका वैसा ही हूँ। यों तो सभी अच्छे ही हैं;
मगर ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही
हैं
न?
मुझसे बढ़ के किसी और पदार्थ को वह समझता ही नहीं।
इसीलिए निरन्तर मुझी में लगा हुआ मस्त रहता
हैं''-''चतुर्विधा
भजन्ते मां जना: सुकृतिनोऽर्जुन। आत्तरो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी न
भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि
ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय: उदारा: सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे
मतम्। आस्थित: सहियुक्तात्मा मामेवानुत्तामां गतिम्''
(7।16-18)
(शीर्ष पर वापस)
ज्ञान और अनन्य भक्ति
इस
प्रकार हमने देखा कि जिस भक्ति के नाम पर बहुत चिल्लाहट और नाच-कूद मचाई
जाती
हैं
और जिसे ज्ञान से जुदा माना जाता
हैं
वह तो घटिया चीज
हैं।
असल भक्ति तो अद्वैत भावना,
'अहं ब्रह्मास्मि'-मैं ही
ब्रह्म हूँ-यह ज्ञान ही
हैं।
इसीलिए ''अनन्याश्चिन्तयन्तो
मां ये जना: पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्''
(9।22) में यही कहा गया
हैं
कि ''भगवान
को अपना स्वरूप-अपनी आत्मा-ही समझ के जो उसमें लीन होते हैं,
रम जाते हैं तथा बाहरी बातों की सुधा-बुधा नहीं रखते,
उनकी रक्षा और शरीर यात्र
का काम खुद
भगवान
करते हैं।''
यहाँ अनन्य शब्द का अर्थ
हैं भगवान
को अपने से अलग नहीं मानने वाले। इसीलिए अगले श्लोक
'येऽप्यन्य
देवताभक्ता:' (9।23)
में अपने से भिन्न देवता या आराध्यदेव
की भक्ति का फल दूसरा ही कहा गया
हैं।
''अनन्यचेता:
सततं यो मां स्मरति नित्यश:। तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन:''
(8।14) में भी यही बात कही
गयी
हैं
कि ''जो
भगवान
को अपनी आत्मा ही समझ के उसी में प्रेम लगाता
हैं
उसे
भगवान
सुलभ हैं-कहीं
अन्यत्र
ढूँढ़े जाने की चीज
हैं
नहीं।''
यदि असल और
सर्वोत्तम
भक्ति ज्ञान रूप नहीं
''भक्त्या
मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि
तत्त्वत:।
ततो मां
तत्त्वतो
ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्'
(18।55) श्लोक में क्यों
कहते कि ''उस भक्ति से ही मुझे बखूबी जान लेता
हैं
और उसके बाद ही मेरा रूप बन जाता
हैं''।
जानना तो ज्ञान से होता
हैं,
न कि दूसरी चीज से। इससे पूर्व के श्लोक 'ब्रह्मभूत:
प्रसन्नात्मा' आदि में उसे ब्रह्मरूप कह के
समदर्शन का ही वर्णन किया
हैं।
समदर्शन तो ज्ञान ही
हैं
यह पहले ही कहा गया
हैं।
यहाँ उसी समदर्शन को भक्ति कहा
हैं।
इस
सम्बन्ध
में और बातें आगे लिखी हैं।
इससे इतना
सिद्ध हो गया कि जब ब्रह्म हमीं हैं ऐसा अनुभव करते हैं,
तो
प्रेम के प्रवाह के लिए पूरा स्थान मिलता हैं और उसका अबोध स्रोत उमड़ पड़ता
हैं। क्योंकि वह प्रवाह जहाँ जा के स्थिर होगा वह वस्तु मालूम हो गयी। मगर
निषेधात्मक मनोवृत्ति होने पर ब्रह्म हमसे अलग या दूसरी चीज नहीं हैं,
ऐसी भावना होगी। फलत: इसमें प्रेम-प्रवाह के लिए वह गुंजाइश नहीं रह जाती
हैं। मालूम होता हैं,
जैसे मरुभूमि की अपार बालुका-राशि में सरस्वती की धारा विलुप्त हो जाती हैं
और समुद्र तक पहुँच पाती नहीं,
ठीक वैसे ही,
इस
निषेधात्मक बालुका-राशि में प्रेम की धारा लापता हो जाती और लक्ष्य को पा
सकती हैं नहीं। यही कारण हैं कि विधि-भावना ही गीता में मानी गयी हैं।
भक्ति की महत्व भी इसी मानी में हैं।
(शीर्ष पर वापस)
सर्वत्र
हमीं हम और लोकसंग्रह
अब जरा
जगत
के बारे में भी देखें। यहाँ भी यह
जगत
तो ब्रह्म ही
हैं
ऐसा विधिरूप
ज्ञान ही गीता को मान्य
हैं।
क्योंकि इसमें हमारे कर्मों के लिए,
लोकसंग्रह के लिए पूरी गुंजाइश रहती
हैं।
निषेध में यह बात नहीं रहती। मालूम पड़ता
हैं
कि निठल्ले जैसा बैठने की बात आ जाती
हैं।
आज जो वेदान्त के अद्वैतवाद में इस
निषेध
पक्ष या संसार के मिथ्यात्व के ही पहलू पर जोर देने के कारण लोगों में
अकर्मण्यता आ गयी
हैं
वह गीताधर्म
और गीता के इस महान मार्ग के छोड़ देने का ही परिणाम
हैं।
वेदान्त के नाम पर आज प्रचलित महान पतन की यही वजह
हैं।
जब कोई विधानात्मक
चीज
हुई
नहीं,
तो फिर कुछ भी करने-धरने की जरूरत ही क्या
हैं?
फलत: वेदान्तवाद एवं अद्वैतवाद को इस पतन के गम्भीर
गत्ता से निकालने के लिए
जगत
के मिथ्यात्व पर जोर देने वाले
निषेधात्मक
पक्ष की ओर दृष्टि न करके हमें
'जगत
ब्रह्म ही
हैं,
हमारी आत्मा ही
हैं'
इस विधानात्मक
पक्ष की ओर ही दृष्टि देना जरूरी
हैं।
इससे यही होगा कि हम चारों ओर अपनी ही आत्मा को देख के उसके कल्याणार्थ ठीक
वैसे ही उतावले हो पड़ेंगे,
दौड़ पड़ेंगे जैसे अपने पाँवों में फोड़ा-फुंसी होने,
खुद भूख-प्यास लगने या अपने पेट में दर्द होने पर
उतावले और बेचैन हो के प्रतीकार में लग जाते हैं। और जरा भी विलम्ब या
आलस्य, अपना या गैरों का,
बर्दाश्त कर नहीं सकते।
गीता इसी
दृष्टि पर जोर देती हुई कहती हैं कि
''बहुत
जन्मों में लगातार यत्न करके,
यह
जो कुछ देखा-सुना जाता हैं सब भगवान ही हैं,
ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाये वही इस संसार में अत्यन्त दुर्लभ महात्मा
हैं''-''बहूनां
जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। वासुदेव: सर्वमिति स महत्मा सुदुर्लभ:''
(7।19)।
ऐसा अद्वैत तत्त्वज्ञानी दूसरे के सुख-दु:ख को अपने में ही अनुभव करता हैं।
यदि किसी को भी एक लाठी मारो तो उसकी चोट उसे ही लगती हैं। इसीलिए उसका
हृदय द्रवीभूत हो के दत्ताचित्तता के साथ लोकसंग्रह में उसे दिन-रात लग
जाने को विवश कर देता हैं। इस बात का कितना मार्मिक वर्णन गीता के छठे
अध्याय के ये श्लोक करते हैं,
''सर्वभूतस्थमात्मानं
सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन:। योमां पश्यति
सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न
प्रणश्यति।सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित:। सर्वथार वत्तामानोऽपि
स योगी मयिर् वत्ताते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा
यदि वा दु:खं स योगी परमोमत:''
(6।29-32)।
इनका आशय
यह हैं कि ''जिसका
मन सब तरफ से हटके आत्मा-ब्रह्म-में लीन हो गया हैं और जो सर्वत्र समदर्शी
हैं (समदर्शन का पूरा विवेचन पहले किया गया हैं) वह अपने आपको सभी पदार्थों
में और पदार्थों को अपने आप में ही देखता हैं। इस प्रकार जो भगवान को भी
सर्वत्र-सभी पदार्थों में-देखता हैं और पदार्थों को भगवान में,
वह
न तो भगवान-ब्रह्म-से जरा भी जुदा हो सकता हैं और न भगवान ही उससे जुदा हो
सकता हैं-दोनों एक ही जो हो गये-जो योगी सभी पदार्थों में रहने
वाले-पदार्थों के रग-रग में रमने वाले-एक हो भगवान को अपने से जुदा नहीं
देखता,
वह
चाहे किसी भी हालत में रहे,
फिर भी परमात्मा में ही रमा हुआ रहता हैं। जो योगी किसी भी प्राणी या
पदार्थ के दु:ख-दु:ख को अपना ही समझता हैं,
अनुभव करता हैं,
वही सर्वोत्तम हैं।''
इसी ज्ञान के बारे में पुनरपि गीता कहती हैं कि
''उसे
हासिल करके फिर इस प्रकार भूल-भुलैया में हर्गिज न पड़ोगे। तब हालत यह होगी
कि संसार के सभी पदार्थों को अपने आप में देखोगे और मुझमें भी-अर्थात तुम
में,
हममें-परमात्मा में-और इस जगत में कोई विभिन्नता रहेगी ही नहीं-सभी एक ही
बन जायेगे''-''यज्ज्ञात्वा
न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि''(4।25)।
हमने शुरू
में ही कर्मों के भेदों के निरूपण के प्रसंग में बता दिया हैं कि आगे
बढ़ते-बढ़ते सभी भौतिक पदार्थों और परमात्मा के साथ आत्मा की तन्मयता कैसे हो
जाती हैं। वही बात गीता बार-बार कहती हैं। इसीलिए जो प्रत्येक शरीर में
आत्मा को जुदा-जुदा मानते हैं वह तो गीता से अनन्त दूरी पर हैं। उनसे और
गीताधर्म से कोई ताल्लुक हैं नहीं। सबकी एकता-एकरसता-के पहले सभी शरीरों की
आत्मा की एकता तो अनिवार्य हैं। ऐसी बुद्धि और भावना सबसे पहले होनी चाहिए।
यहीं से तो गीता का श्रीगणेश होता हैं। इसीलिए
''अन्तवन्त
इमे देहानित्यस्योक्ता शरीरिण:''
(2।
18)
आदि
श्लोकों में अनके शरीरों में रहने वाले शरीरी-आत्मा-को एक ही कहा हैं। जहाँ
'देहा:'
यह
बहुवचन दिया हैं,
तहाँ 'शरीरिण:'
एकवचन ही रखा हैं। आगे भी यही बात हैं।
'क्षेत्रज्ञं
चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रोषु भारत'
(13।2)
में भी सभी क्षेत्रों में-शरीरों में-एक ही क्षेत्रज्ञ-शरीरी-को कह के साफ
सुना दिया हैं कि शरीर और शरीरी-आत्मा-भगवान के ही स्वरूप हैं।
'मयि
ते तेषु चाप्यहम्'
(9।29)
में भी यही बात कही गयी हैं कि भक्तजनों में भगवान हैं और भगवान में भक्तजन
हैं-अर्थात दोनों एक हैं।
'अनन्येनैव
योगेन मां ध्यायन्त उपासते'
(12।6)
में भी दोनों की अभिन्नता-एकता-ही कही गयी हैं। ऐसे ज्ञानियों की हालत यह
होती हैं कि न तो उनसे किसी को उद्वेग या जरा सी भी दिक्कत मालूम होती हैं
और न उन्हें दूसरों से। यही बात
'यस्मान्नोद्विजते
लोक:' (12।15)
में कही गयी हैं। यही हैं ज्ञानी जनों की पहचान।
'मयि
चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी'
(13।10)
में इसी अद्वैततत्त्वज्ञान को अव्यभिचारिणी भक्ति नाम दिया हैं।
'मां
च योऽव्यभिचारेणा'
(14।26)
में इसे ही अव्यभिचारी भक्ति योग भी कहा हैं।
गीता - 7
(शीर्ष पर वापस)