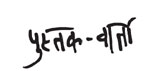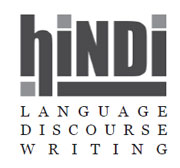गीता
के 'ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव'
(13।4) में बहुत से लोग
ब्रह्मसूत्र
का शारीरक
सूत्र
या वेदान्तदर्शन के
सूत्र
यही अर्थ करते हैं। क्योंकि ब्रह्मसूत्र
शब्द एक प्रकार से वेदान्तसूत्रों
का नाम ही
हैं।
मगर शंकर ने अपने भाष्य में ऐसा न करके ब्रह्म के प्रतिपादक वचन का ही अर्थ
किया
हैं।
क्योंकि वेदान्तसूत्र
के अर्थ करने में एक भारी दिक्कत
हैं।
ऐसा अर्थ करने पर गीता से पहले ही वेदान्तसूत्रों
का अस्तित्व उपनिषदों और वेदों की ही तरह मानना पड़
जायेगा।
तभी तो इन
सभी
का उल्लेख गीता में सम्भव
हैं।
किन्तु ऐसा मानने में अड़चन यह
हैं
कि ब्रह्मसूत्रों
में ही कई जगह स्मृति शब्द से साफ ही गीता का उल्लेख आया
हैं।
खासकर 'अंशोनानाव्य-पदेशात्'
(वेदां. 2।3।43)
में जीव को परमात्मा का अंश लिख के उसमें प्रमाणस्वरूप
गीता के 'ममैवांशो जीवलोके' (15।7)
का उल्लेख 'अपि च स्मर्यते'
(2।3।45)
सूत्र
में स्मृति शब्द से किया
हैं।
यहाँ दूसरी स्मृति की सम्भावना
हुई
नहीं,
यह सभी मानते हैं। इसी प्रकार गीता में 'यत्र
काले त्वनावृत्तिम'
(8।23-27) में जो
उत्तरायण-दक्षिणायन का वर्णन
हैं
उसी का उल्लेख
'योगिन:
प्रति च स्मर्यते' (4।2।21)
में आया
हैं।
क्योंकि गीता में भी
'आवृत्तिं
चैव योगिन:'
(8।23) में यही 'योगिन:'
शब्द आया
हैं।
इस प्रकार जब गीता का स्पष्ट और असंदिग्धा उल्लेख ब्रह्म-सूत्रों
में
हैं;
तो मानना पड़ेगा कि ब्रह्म-सूत्रों
से पहले ही गीता थी। फिर गीता में ब्रह्म-सूत्रों
का उल्लेख कैसे सम्भव एवं युक्तियुक्त हो सकता
हैं?
इसीलिए हमें ब्रह्म-सूत्र
का वैसा अर्थ करना पड़ा
हैं।
लेकिन कुछ
लोग फिर भी इसे न मान के वेदान्त सूत्र ही अर्थ कर डालते हैं। वे इस दिक्कत
का सामना करने के लिए दो महाभारत और इसीलिए दो गीताएँ मानते हैं। उनके मत
से पहले महाभारत न लिखा जा के भारत ही लिखा गया था। उसी में गीता भी थी।
उसी के बाद वेदान्त सूत्र बने और उनमें गीता को प्रमाण के रूप में उध्दृत
किया गया। इसके बाद समय पाके भारत तखड़-पखड़ और छिन्न-भिन्न हो गया। इसीलिए
व्यास ने उसे फिर से एकत्र किया और कुछ ईधर-उधर से उसमें जोड़ा-जाड़ा भी। इसी
से भारत का अब महाभारत हो गया। आखिर बड़ा होने का कोई कारण भी तो चाहिए और
जब तक उसमें कुछ और न जुटता तब तक वह भारत ही न कहा जा के महाभारण क्यों
कहा जाता?
इस
प्रकार तर्क-युक्ति के साथ वे महाभारत का पुनर्निर्माण मानते हैं। या यों
कहिए कि भारत में ही संशोधन और संवर्धन करके उसे महाभारत बनाते हैं। गीता
भी उसी में थी। इसलिए स्वभावत: उसमें भी जरामरा संशोधन हुआ और यह
'ऋषिभिर्बहुधा'
श्लोक उसी संशोधन के फलस्वरूप पीछे से उसमें जुट गया। इस प्रकार यह महाभारत
वेदान्त-सूत्रों के बाद ही तैयार होने के कारण गीता में वेदान्तसूत्रों का
उल्लेख 'ब्रह्मसूत्र'
शब्द से होने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती हैं। यही हैं संक्षेप में उनके
तर्कों और युक्तियों का निचोड़।
अब प्रश्न
यह होता हैं कि यदि महाभारत को भारत का संशोधित एवं परिवर्ध्दित रूप ही
मानें और बड़ा होने से ही उसका नाम भी युक्ति-युक्त मानें,
तो
सामवेद के ताण्डय महाब्राह्म और पाणिनीय सूत्रों के पातंजल महाभाष्य के
बारे में क्या कहा जायेगा?
यह
तो सभी संस्कृतज्ञ जानते हैं कि सामवेद के ब्राह्मण भाग को अन्य वेदों के
ब्राह्मण भागों की तरह केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण,
वाजसनेय ब्राह्मण आदि जैसा न कह के ताण्डय महाब्राह्मण कहते हैं। इसी तरह
व्याकरण के भाष्य को महाभाष्य ही कहते हैं। इतना बोलने से ही और भाष्यों को
न समझ केवल पातंजल भाष्य ही समझा जाता हैं। तो क्या इसी दलील से यह भी माना
जाये कि पहले छोटा सा ताण्डय ब्राह्मण और छोटा पातंजल भाष्य बना था,
पीछे उन्हीं दोनों का आकार बढ़ाया गया?
लेकिन यह तो कोरी कल्पना ही होगी न?
कहा जाता हैं कि आश्वलायन गृह्यसूत्र (3।4।4)
में भारत और महाभारत दोनों ही का उल्लेख हैं। इसीलिए इन दो की कल्पना की
गयी हैं। मगर ताण्डय या पातंजल भाष्य के बारे में तो ऐसा कोई आधार नहीं
हैं। यह भी बात हैं कि भारत एवं महाभारत दो तो मिलते नहीं। महाभारत ही तो
मिलता हैं। और जब उसी में कुछ और जोड़ा गया हैं तो दो लिखने या कहने के मानी
क्या?
जब तक
जुदे-जुदे पाये न जायें,
दो
कैसे कहे जा सकते हैं?
आखिर गृह्यसूत्रों का समय उपनिषदों,
ब्राह्मणों या वेदों से पुराना तो हैं नहीं। फलत: यदि उस समय भारत और
महाभारत दोनों थे तो और ग्रन्थों की तरह दोनों का पता तो चाहिए आज भी। नहीं
तो गीता भी दो क्यों न मानी और लिखी जाये,
लिखी जाती?
सिर्फ एक सूत्र ग्रन्थ में एक शब्द को लिखा या छपा देख के इतनी लम्बी उड़ान
उचित नहीं। लिखने और छपने में भूल से एक ही नाम,
एक
ही शब्द दो बार लिख या छप जाते हैं। ऐसा प्राय: देखा जाता हैं। हाँ,
यदि विभिन्न समयों के लिखे और छपे दो-चार सूत्रग्रन्थों में ऐसी चीज मिलती,
तो
शायद कुछ कहा जा सकता था।
यह भी तो
जरा सोचें कि महात्मा और महेश्वर शब्द पहुँचे हुए बड़े लोगों या भगवान के
लिए प्रयुक्त होते हैं। मगर इसका यह आशय नहीं होता कि खामख्वाह महात्माओं
के पहले आत्मा शब्द से भी किसी को कहा जाता था,
या
भगवान को महेश्वर कहने के पहले जरूर ही औरों को ईश्वर कहते थे। भगवान की
सत्ता तो सबसे पहले मानी जाती हैं। फिर उससे पहले कैसे कोई हुआ?
'मायिनं
तु महेश्वरम्'
(4।10)
में श्वेताश्वतर उपनिषद ने ब्रह्म को ही महेश्वर कहा हैं। मगर वहाँ ईश्वर
का कोई मुकाबला हैं नहीं। क्योंकि उसी उपनिषद में और वेदों में भी महेश्वर
को ही ईश्वर भी कहा हैं। आत्मा नाम से न तो किसी को कभी बोलते ही और न यह
विशेषण ही किसी में लगाते हैं। स्वभावत: ही महान होने से ही महात्मा या
महेश्वर कहने की परिपाटी पड़ गयी हैं। इसी प्रकार ताण्डय,
पातंजल भाष्य और महाभारत को भी स्वभावत: बहुत बड़े होने के कारण ही
महाब्राह्मण,
महाभाष्य और महाभारत कहने लग गये। यहाँ बाल की खाल खींचने की जरूरत हुई
नहीं। उसी में उसे कहीं भारत और कहीं महाभारत लिखा हैं।
जरा यह भी
तो सोचें कि भारत में महज थोड़ा-बहुत जोड़ने से ही तो महाभारत होता नहीं।
इसके लिए तो जरूर ही बहुत ज्यादा जोड़-जाड़ करना होगा। जहाँ अपेक्षाकृत
महत्व दिखानी होती हैं तहाँ पहले से दूसरे में बहुत ज्यादा अन्तर का होना
अनिवार्य हैं। जाल और महाजाल इस बात के मोटे दृष्टान्त हैं,
समुद्र में डाले जाने वाले महाजाल के भीतर जाने कितने ही जाल आसानी से समा
सकते हैं,
आ
सकते हैं। अन्य मारक-बीमारियों की अपेक्षा हैंजा या प्लेग को हजार गुना
मारक और खतरनाक समझ के ही इन्हें महामारी कहते हैं। ऐसी दशा में भारत की
अपेक्षा महाभारत में बहुत ज्यादा-कई गुना-पदार्थ घुसने से ही उसे महाभारत
कह सकते थे। फिर तो दोनों की पृथक् सत्ता अनिवार्य हैं। यह असम्भव हैं कि
महाभारत के रहते भारत सर्वथा लुप्त हो जाये। वराहमिहिर के वृहज्जातक के
रहते लघुजातक कहीं गायब नहीं हो गया। और न मंजूषा के रहते व्याकरण की
लघुमंजूषा कहीं चली गयी। वराहमिहिर की बृहत्संहिता के मुकाबिले में उनकी
कोई लघुसंहिता या केवल संहिता नहीं मानी जाती। महान तथा बृहत् का एक ही
अर्थ हैं भी। सबसे बड़ी बात यह हो जायेगी कि गीता में भी तब बहुत ज्यादा
परिवर्तन मानना होगा। यह नहीं हो सकता कि जो गीता भारत में थी वही जरा-मरा
परिवर्तन के साथ महाभारत में आ गयी!
परन्तु
गीता के बारे में ऐसा कह सकते नहीं। यह इतनी लोकप्रिय रही हैं कि इसमें एक
शब्द का प्रक्षेप होना या मिलाना असम्भव हो गया हैं। तेरहवें अध्याय में
एक श्लोक घुसेड़ने की कोशिश कभी किसी ने की जरूर। लेकिन वह सफल न हो सका।
वैदिक मन्त्रों,
ब्राह्मणों या प्रधान उपनिषदों में जैसे कोई प्रक्षेप होना सम्भव न हुआ,
वही हालत गीता की भी रही हैं। मालूम होता हैं,
उन्हीं की तरह इसे भी लोग जबान पर ही रखते थे। इसकी भी
'श्रुति'
जैसी ही दशा रही हैं। प्रत्युत इसमें तो और भी विशेषता हैं कि वेदों और
उपनिषदों को प्राय: भूल जाने पर भी इसे लोग भूल न सके। आज भी वैसा ही मानते
हैं,
पढ़ते-लिखते हैं,
कद्र करते हैं। जैसा कि पहले करते थे। इसलिए यदि कभी किसी भी हालत में
इसमें एक भी शब्द या श्लोक जोड़ा जाता तो खामख्वाह पकड़ा जाता,
यह
पक्की बात हैं। किन्तु
'ऋषिभिर्बहुधा'
श्लोक के बारे में ऐसी धारणा किसी की भी पायी नहीं जाती। यही कारण हैं कि
सात या ज्यादा श्लोकों की छोटी-छोटी गीताओं के थोड़ा-बहुत प्रचार होने पर भी,
ऐसी गीता नहीं पायी जाती जिसमें यह
'ऋषिभिर्बहुधा'
या
ऐसे ही कुछ श्लोक न हों। भारत को ही महाभारत मनाननेवाले भी तो नहीं बताते
कि कितने श्लोक इसमें पीछे जुटे थे। इसलिए यह सिद्धान्त मान्य नहीं हो
सकता।
एक बात
और। छान्दोग्य के सातवें अध्याय में कई बार इतिहास,
पुराण आदि का उल्लेख हैं। इसी प्रकार वृहदारण्यक के दूसरे अध्याय में भी
इतिहास,
पुराण,
सूत्र,
व्याख्यान आदि का उल्लेख चौथे ब्राह्मण में आया हैं। तो क्या इससे यह समझें
कि सचमुच वेदान्तसूत्रों की तरह इनसे पहले भी सूत्रग्रन्थ और आज के
इतिहासों और पुराणों की ही तरह पहले भी इतिहास पुराण थे?
क्या पहले भाष्य और व्याख्यान भी ऐसे ही थे यह माना जाये?
यह
तो सभी मानते हैं कि पुराणों का समय बहुत ईधर का हैं। सूत्रों का समय भी
ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद का ही हैं। फिर यह कैसे माना जाये कि इस प्रकार
आमतौर से सूत्रों और उनके व्याख्यानों का उल्लेख करने मात्र से वे भी
ब्राह्मण ग्रन्थों से पहले थे?
खूबी तो यह हैं कि जब एक ही तरह का उल्लेख कई उपनिषदों में मिलता हैं तो
मानना ही होगा कि वे सूत्र और व्याख्यान प्रसिद्ध होंगे और ज्यादा संख्या
में होंगे। इतिहास-पुराण भी काफी होंगे। ऐसी दशा में इन शब्दों का रूढ़ अर्थ
न मान के यौगिक ही मानने में गुजर हैं। जैसा कि इस श्लोक में हमने
ब्रह्मसूत्र शब्द का अर्थ रूढ़ न करके यौगिक ही किया हैं। दूसरा उपाय हुई
नहीं। इसलिए हमने जो अर्थ इस श्लोक का लिखा हैं वह कोई एकाएक नई कल्पना
नहीं हैं। किन्तु ऐसी कल्पना पहले भी होती आयी हैं। शंकर ने उसी का अनुसरण
किया हैं। बेशक,
यह
विषय और भी अधिक विवेचन चाहता हैं। मगर वह यहाँ के लिए नहीं हैं। किन्तु
आगे होगा।
लेकिन दो
एक ऐसी बातें और भी यहीं कह देना जरूरी हैं जिनके बारे में विशेष अन्वेषण
एवं जाँच-पड़ताल की जरूरत नहीं हैं। सबसे पहली बात यह हैं यह जानते हुए भी
कि ब्रह्मसूत्रों ने गीता को ही प्रमाण-स्वरूप उध्दृत किया हैं,
गीताकार के लिए यह कब सम्भव था कि उन्हीं ब्रह्म-सूत्रों को प्रमाण के रूप
में स्वयं उध्दृत करते?
यह
तो बिलकुल ही अनहोनी बात हैं। व्यवहार में तो यह बात कभी देखने में आती
नहीं। चाहे कितनी ही महत्त्वपूर्ण और बड़ी पोथी क्यों न हो। मगर ज्यों ही एक
बार उसने किसी दूसरी को अपनी बातों के समर्थन में उध्दृत किया कि उसके
सामने उसकी अपनी महत्व वैसी नहीं रह जाती। फलत: कोई भी समझदार आदमी इस
दूसरी के समर्थन में पहली की किसी बात को प्रमाण-स्वरूप पेश नहीं करता,
पेश करने की हिम्मत नहीं करता। फिर गीता जैसे महान ग्रन्थ में ऐसी बात का
होना कथमपि सम्भव होगा यह कौन माने?
दूसरी बात
भी इसी से मिलती-जुलती ही हैं। जो लोग यह मानते हैं कि ज्ञानोत्तर कर्म
करना गीता के मत से अनिवार्य हैं,
जिनके मत से गीता की आवश्यकता ही इसीलिए हुई थी,
वही यह भी मानते हैं कि उस समय
''ज्ञानोत्तर
कर्म करना अथवा न करना,
हर
एक की इच्छा पर अवलम्बित था,
अर्थात् वैकल्पिक समझा जाता था''
(गीतारह.
पृ. 554)।
वे इसके सम्बन्ध में उन्हीं वेदान्तसूत्रों या ब्रह्म-सूत्र (3।4।15)
को
प्रमाण के लिए उध्दृत भी करते हैं। ऐसी दशा में यह बात तो समझ में आ जाती
हैं कि ब्रह्म-सूत्र गीता को अपने समर्थन में उध्दृत कर लें। लेकिन गीता
में उन्हीं ब्रह्म-सूत्रों का हवाला कैसे दिया जा सकता हैं?
क्योंकि ज्यों ही यह बात हुई कि गीता पढ़नेवालों की नजर में उन सूत्रों की
महत्व आ जायेगी। फलत: ऐसे लोग वेदान्तसूत्रों की उन बातों पर भी स्वभावत:
आकृष्ट होंगे ही जिनमें ज्ञानोत्तर कर्म करना जरूरी नहीं माना गया हैं।
परिणाम क्या होगा?
यही न,
कि
गीता में भी वही चीज मानने की ओर उनकी प्रवृत्ति हो जायेगी?
अतएव बड़ी मुसीबत और कठिनाई के बाद गीतारहस्य में जो यह सिद्ध करने की कोशिश
की गयी हैं कि ज्ञानोत्तर कर्म करते-करते ही मरना गीताधर्म और गीताउपदेश
हैं,
उसकी जड़
में ही इस प्रकार कुठाराघात हो जायेगा। जिस बात की पुष्टि के लिए यह चीज
पेश की गयी उसी को कमजोर करने लगेगी! और खुद गीता अपने ही सिद्धान्त को
दुर्बल करने का रास्ता इस तरह ब्रह्मसूत्र का नाम लेकर साफ कर दे,
यह
असम्भव हैं।
एक तरफ तो
यह कहा जाता हैं कि महाभारत का तथा उसी के भीतर आ जाने वाली गीता का भी
निर्माण 'बुद्ध
के जन्म के बाद-परन्तु अवतारों में उनकी गणना होने के पहले ही'
हुआ होगा। इसीलिए विष्णु के अवतारों में बुद्ध की गणना महाभारत में कहीं
पायी नहीं जाती। गीतारहस्य में यह भी माना गया हैं कि यद्यपि महाभारत के
युद्ध के समय भागवत धर्म का उदय हो गया था। तथापि उसकी प्रधान पोथी के रूप
में इस गीता की रचना तत्काल न हो के प्राय: पाँच सौ वर्ष बाद हुई होगी।
क्योंकि किसी भी सिद्धान्त या धर्म के प्रतिपादक ग्रन्थ फौरन न बन के पीछे
बनते हैं। इसी से पाँच सौ साल इसके लिए मान लिया हैं। मगर ब्रह्मसूत्रों (2।2।18-26)
का
हवाला दे के उन्होने यह भी लिखा हैं कि
''आत्मा
या ब्रह्म में से कोई भी नित्य वस्तु जगत के मूल में नहीं हैं। जो कुछ देख
पड़ता हैं वह क्षणिक या शून्य हैं,''
अथवा ''जो
कुछ देख पड़ता हैं वह ज्ञान हैं,
ज्ञान के अतिरिक्त जगत में कुछ भी नहीं हैं,
इस
निरीश्वर तथा अनात्मवादी बौद्ध मत को ही क्षणिकवाद,
शून्यवाद और विज्ञानवाद कहते हैं''
(गीता
र. 580)।
भला ये दोनों बातें कैसे सम्भव होंगी यदि ब्रह्मसूत्रों को गीता के पहले
मान लें?
क्योंकि बुद्धधर्म के भीतर इन अनेक मतों और पन्थों के खड़े होने और उनके
ग्रन्थों के बनने में तो कई सौ साल लगे ही होंगे और बिना प्रामाणिक बात के
केवल मौखिक बातों में तो खण्डन ब्रह्मसूत्र जैसा ग्रन्थ करता नहीं। इस तरह
यदि बुद्ध के बाद पाँच सौ साल भी इन बातों के लिए मान लें तो ब्रह्मसूत्रों
का समय सन् ईस्वी के आरम्भ में ही माना जायेगा। फिर गीता ने उन्हें कैसे
उध्दृत किया या हवाले में दिया?
एक ही बात
और। ''सुमन्तु
जैमिनि वैशंपायन पैल सूत्र भाष्य भारत महाभारत धर्माचार्या:''
(3।4।4)
इसी आश्वलायन गृह्यसूत्र में भारत और महाभारत देख के कल्पना की गयी हैं कि
दोनों दो हैं। इस सूत्र में पहले जो सुमन्तु आदि नाम आये हैं उन्हीं का
सम्बन्ध भारत महाभारत से जोड़ते हुए उन्होने लिखा हैं कि
''इससे,
अब
यह भी मालूम हो जाता हैं,
कि
ऋषितर्पण में भारत महाभारत शब्दों के पहले सुमन्तु आदि नाम क्यों रखे गये
हैं'' (गी.
र. 524)।
मगर हमें अफसोस हैं कि ऐसा लिखते समय यह बात उन्हें कैसे नहीं सूझी कि नाम
तो चार ही ॠषियों के आये हैं,
मगर ग्रन्थ हो जाते हैं सूत्र,
भाष्य,
भारत,
महाभारत
और धर्म ये पाँच! हाँ,
यदि यह मान लें कि भारत अलग न हो के भूल से महाभारत का ही
'भारत
महाभारत'
ऐसा लिखा गया हैं,
तब
ठीक हो सकता हैं। तभी चार ऋषियों के लिए क्रमश: चार ग्रन्थ आ सकते हैं और
उन्हीं के आचार्य उन्हें मान सकते हैं। यह तो गीतारहस्य के लेखक भी नहीं
मानते कि सभी ने पाँचों ग्रन्थ बनाये हैं। यह असम्भव भी हैं। धर्म शब्द शेष
ग्रन्थों के साथ होने से ग्रन्थ का ही वाचक माना जाना भी चाहिए।
इस प्रकार
इस विस्तृत विवेचन ने गुणवाद और अद्वैतवाद के सभी पहलुओं पर संक्षेप में ही
इतना प्रकाश डाल दिया हैं कि उनके सम्बन्ध की गीता की सभी बातों को समझने
में आसानी हो जायेगी। इसके मुतल्लिक गीता की जो खास दृष्टि हैं-तत्त्वज्ञान
एवं वास्तविक भक्ति में जो गीता की दृष्टि में कोई अन्तर नहीं हैं,
किन्तु दोनों ही एक ही हैं- इस बात के निरूपण से इस चीज पर पूरा प्रकाश पड़
गया कि अद्वैतवाद और जगन्मिथ्यात्ववाद के विधानात्मक पहलू पर ही गीता का
विशेष आग्रह क्यों हैं?
(शीर्ष पर वापस)
9.
'सर्व
धर्मान्परित्यज्य'
अब
हमें विशेष कुछ नहीं कहना
हैं।
फिर भी गीता के अठारहवें अध्याय
के अन्त में जो
''सर्वधर्मान्परित्यज्य
मामेकं शरणं ब्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:''
(66) श्लोक आया
हैं
उसके ही
सम्बन्ध
में कुछ लिखना हम जरूरी समझते हैं। इसका यह मतलब नहीं
हैं
कि अब तक के हमारे कथन ने उस पर प्रकाश नहीं डाला
हैं।
उसकी चर्चा तो बार-बार आयी
हैं।
यह भी नहीं कि हम कोई
नई
बात खास तौर से यहाँ कहने जा रहे हैं। इस
सम्बन्ध
में इतना कहा जा चुका
हैं
कि
नई
बात मालूम पड़ती ही नहीं। यों तो गीता हीरा ठहरी। इसीलिए इसे जितना ही कसो,
इस पर जितना ही विचार करो यह उतनी ही खरी निकलती
हैं
और इसकी चमक उतनी ही बढ़ती
हैं।
बात असल यह
हैं
कि एक तो अठारहवें अध्याय
को ही गीता का उपसंहार-अध्याय
माना जाता
हैं।
उसमें भी अन्त में यह श्लोक आया
हैं।
इसलिए गीता के उपसंहार का भी उपसंहार इसे मान के लोगों ने अपने-अपने मत और
सम्प्रदाय के अनुसार इसके अर्थ की काफी खींच-तान की
हैं।
यदि यह कहें कि यह श्लोक एक प्रकार से गीतार्थ का कुरुक्षेत्र
बना दिया गया
हैं
तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसलिए हम यहाँ यही दिखाना चाहते हैं कि
साम्प्रदायिकता के आग्रह में गीता को उसके अत्यन्त
महान
एवं उच्च स्थान से बेदर्दी के साथ घसीट के गहरे गढ़े में गिराने की कोशिश
बड़े से बड़े विद्वान् भी किस प्रकार करते हैं। इसी बात का यह एक नमूना
हैं।
इसी से समूची गीता में की गयी खींच-तान और जबर्दस्ती का पता लग
जायेगा।
हमारा काम यह नहीं रहा
हैं
कि इतने लम्बे लेख में किसी का भी खासतौर से खण्डन-मण्डन करें। हम इसे
अनुचित समझते हैं। इसके लिए तो
स्वतन्त्र
रूप से लिखने का हमारा विचार
हैं।
मगर अन्त में थोड़ा सा नमूना पेश किये बिना शायद यह प्रयास अपूर्ण रह
जायेगा।
इसीलिए यह यत्न
हैं।
इस श्लोक
का अक्षरार्थ तो यही हैं कि
''सभी
धर्मों को छोड़ के एक मेरी - भगवान की-ही शरण में जा। मैं तुझे सब पापों से
मुक्त कर दूँगा। सोच मत कर।''
गीता को तो उपनिषदों का ही रूप या निचोड़ मानते हैं और उपनिषदों में
धर्म-अधर्म के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा चुका हैं कि उन्हें कैसे,
कब
और क्यों छोड़ना चाहिए।
'त्यज
धर्ममधाम च'
ये
स्मृति वचन धर्म-अधर्म सभी के त्याग की बात कहते हैं। कठोपनिषद के भी
'अन्यत्र
धर्मादन्यत्रधर्मात्'
(2।14)
तथा 'नाविरतो
दुश्चरितात्'
(2।23)
में धर्म-अधर्म सभी के छोड़ने की बात मिलती हैं। वृहदारण्यक (4।4।22)
से
धर्मों का संन्यास आवश्यक सिद्ध होता हैं यह हमने पहले ही सिद्ध किया हैं।
आत्मा और उसके ज्ञान को न सभी झमेलों से बहुत दूर की बात इन वचनों ने कही
हैं। इसके सिवाय गीता में ही
'सर्वभूतस्थितं
यो मां भजत्येकत्वमास्थित:'
(6।31),
'एकत्वेन
पृथक्त्वेन'
(9।15)
आदि वचनों के द्वारा यही कहा गया हैं कि असली भजन या भक्ति यही हैं कि हम
अपने को परमात्मा के साथ एक समझें और जगत को भी अपना ही रूप मानें। यहाँ एक
शब्द का अर्थ गीता ने स्पष्ट कर दिया हैं। यह भी बात हैं कि यद्यपि गीता का
धर्म कर्म से जुदा नहीं हैं,
बल्कि गीता ने दोनों को एक ही माना हैं;
तथापि सभी कर्मों का त्याग तो असम्भव हैं। गीता ने तो कही दिया हैं कि
''यदि
सभी कर्म छोड़ दें तो शरीर का रहना भी असम्भव हो जाये''-''शरीरयात्रपि
च ते न प्रसिद्धयेदकर्मण:''
(3।8)।
इसीलिए इस श्लोक में कर्म की जगह धर्म शब्द दिया गया हैं;
हालाँकि इससे पहले के बीसियों श्लोकों में केवल कर्म शब्द ही पाया जाता हैं,
धर्म-शब्द लापता हैं। इसीलिए परिस्थितिवश धर्म शब्द सामान्य कर्म के अर्थ
में न बोला जाकर कुछ संकुचित अर्थ में ही यहाँ आया हुआ माना जाना उचित हैं।
फलत: कुछ विस्तृत एवं व्यापक रूप में शास्त्रीय विधि-विधन के अनुसार ही
यहाँ धर्म शब्द का अर्थ लिया जाना उचित प्रतीत होता हैं। दूसरे अध्याय के
'स्वधर्ममपि'
(2।31)
में जिस अर्थ में यह प्रयुक्त हुआ हैं,
या
खुद अर्जुन ने ही
'धर्मसंमूढ़चेता:'
(2।7),
'कुलधर्मा:
स्नातना:' (1।40)
आदि वचनों में जिस संकुचित अर्थ में इसे कहा हैं यहाँ भी वही अर्थ या उसी
से मिलता-जुलता ही मान लेना ठीक हैं। छान्दोग्योपनिषद में
'एकमेवाद्वितीयम्'
(6।2।1)
में ब्रह्म को एक कहा भी हैं।
इसीलिए
शंकर ने अपने गीताभाष्य में धर्मशास्त्रीय बन्धनों को छोड़ के और उनमें
लिखे धर्मों-अधर्मों से पल्ला छुड़ाके
'अहं
ब्रह्मास्मि'-'मैं
खुद ब्रह्म ही हूँ'
इसी अद्वैतज्ञाननिष्ठा के प्राप्त करने का प्रतिपादन इस श्लोक में माना
हैं। हम तो पहले अच्छी तरह बता चुके हैं कि बिना शास्त्रीय धर्मों को छोड़े
या उनका संन्यास किये ज्ञाननिष्ठा गैरमुमकिन हैं। उसी जगह इस श्लोक का भी
उल्लेख हमने किया हैं। यह भी बताई चुके हैं कि अठारहवें अध्याय के शुरू
में जिस संन्यास और त्याग की असलियत और हकीकत जानने के लिए अर्जुन ने सवाल
किया हैं वह संन्यास इसी श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया हैं। इससे पहले
49वें
श्लोक में सिर्फ उसका उल्लेख आया हैं। उससे पहले तो त्याग की ही बात को ले
के बहुत कुछ कहा गया हैं। इसी श्लोक में जो
'परित्यज्य'
शब्द आया हैं और जिसका अर्थ हैं
'परित्याग
करके या छोड़के',
उससे ही साफ हो जाता हैं कि अद्वितीय या जीव से अभिन्न ब्रह्म की शरण जाने
और उसका ज्ञान प्राप्त करने के पहले धर्मों को कतई छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि
'समान
कर्त्तर्कयो: पूर्वकाले क्त्तवा'
(3।4।21)
इस
पाणिनीय सूत्र के अनुसार पहले किये गये के मानी में ही
'क्त्तवा'
और
'ल्यप्'
प्रत्यय हुआ करते हैं। परित्याग में त्याग के अलावे जो
'परि'
शब्द हैं वह यही बताने के लिए हैं कि धर्म-अधर्म के झमेले से अपना पिण्ड
कतई छुड़ा लेना होगा। विपरीत इसके अगर धर्म का अर्थ धर्मों का फल लेते हैं
तो उसका त्याग तो भगवान की शरण में जाने पर भी होता ही रहेगा। क्योंकि ऐसा
अर्थ करनेवाले तो श्रवण,
कीर्त्तन आदि नौ प्रकार की भक्ति को ही असल चीज मानते हैं। उनके मत से शरण
जाने का अर्थ ही हैं यही नवधा-नौ प्रकार की-भक्ति करना। अन्य धर्मों को भी
करते रहना वे मानते ही हैं। ऐसी दशा में उनके फलों का त्याग तो बाद में भी
होता ही रहेगा। फिर यह कहने के क्या मानीकि सभी धर्मों से अपना पिण्ड पहले
ही छुड़ा लो,
अगर धर्मों का अर्थ हैं उनका फलमात्र?
अब जरा
दूसरों का अर्थ भी देखें। माधव सम्प्रदाय के आचार्य अपने इसी श्लोक के
भाष्य में लिखते हैं कि
'यहाँ
धर्मों के त्याग का अर्थ हैं उनके फलों का ही त्याग,
न
कि खुद धर्मों का ही। क्योंकि तब युद्ध करने की जो आज्ञा दी गयी हैं वह
कैसे ठीक होगी। इसके अलावे खुद गीता के अठारहवें अध्याय के
11वें
श्लोक में तो कही दिया हैं कि जो कर्मों के फलों का त्याग करता हैं उसे ही
त्यागी कहते हैं-'धर्मत्याग:
फलत्याग:। कथमन्यथा युद्धविधि:?'
'यस्तुकर्मफलत्यागी
स त्यागीत्यभिधीयत'
इति चोक्तम्।'
रामानुज-सम्प्रदाय के आचार्य स्वयं रामानुज के भाष्य में भी कुछ इसी तरह की
बात लिखी गयी हैं। वह कहते हैं कि
''मुक्ति
के साधन के रूप में जितने भी काम कर्मयोग,
ज्ञानयोग एवं भक्तियोग के नाम से प्रसिद्ध हैं वे सभी भगवान की आराधना ही
हैं। इसलिए प्रेम के साथ जिसे जो धर्म करने को शास्त्रों ने कहा हैं उसे
करते हुए ही पूर्व बताये तरीके से उनके फलों एवं कर्त्तरृत्व के अभिमान को
छोड़ के केवल हमीं को सबका कर्ता तथा आराध्यदेव मानो''-''कर्मयोग
ज्ञानयोग भक्तियोग-रूपान्सर्वान्धर्मान् परमनि: श्रेयससाधनभूतान
मदाराधनत्वेनातिमात्रप्रीत्या यथाधिकारं कुर्वाण एवोक्तरीत्या
फलकर्र्मकत्तृत्वादिपरित्यागेन परित्यज्य मामेकमेव कर्तारमाराध्यं
प्राप्यमुपायं चानुसन्धात्स्व।''
''एष
एव सर्वधर्माणां शास्त्रीय परित्याग''-
''यही-फलादि
का त्याग ही-सब धर्मों का शास्त्र रीति के अनुसार त्याग माना जाता हैं,
न
कि स्वयं धर्मों का त्याग ही।''
ये दो तो
पुराने आचार्यों के अर्थ हुए। अब जरा हाल-साल के लोकमान्य तिलक के हाथों
लिखे गये गीता रहस्य में माने गये अर्थ को भी देखें। वह पहले यह लिखते हैं
कि ''यहाँ
भगवान श्रीकृष्ण अपने व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे हैं। इस कारण
हमारा यह दृढ़ मत हैं कि यह उपसंहार भक्ति प्रधान ही हैं।''
फिर कहते हैं कि
''परन्तु
इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य धर्म के अनुरोध से भगवान का यह निश्चयात्मक
उपदेश हैं कि उक्त नाना धर्मों के गड़बड़ में न पड़कर मुझे अकेले को भज,
मैं तेरा उद्धार कर दूँगा,
डर
मत।''
मगर आखिर
में कहते हैं कि
''मेरी
दृढ़ भक्ति करके मत्परायण बुद्धि से स्वधर्मानुसार प्राप्त होने वाले कर्म
करते जाने पर इहलोक और परलोक दोनों जगह तुम्हारा कल्याण होगा;
डरो मत।''
इसे पढ़ने से तो एक अजीब झमेला खड़ा हो जाता हैं। एक ओर सब धर्म करते रहने की
बात और दूसरी ओर उन्हें छोड़ने की बात! लेकिन तिलक ने कुछ खास धर्मों को
यहाँ गिना के कहा हैं कि इन अहिंसा,
दान,
गुरुसेवा,
सत्य,
मातृपितृसेवा,
यज्ञयाग और संन्याय आदि धर्मों को,
जो
परमेश्वर की प्राप्ति के साधन माने जाते हैं,
छोड़ के साकार भगवान की ही भक्ति करो। इस श्लोक के धर्म से उनका मतलब उन्हीं
चन्द गिनेगिनाये धर्मों से ही हैं। उन्होने धर्म शब्द का अर्थ धर्मों का फल
करना मुनासिब न समझ यह नवीन मार्ग स्वीकार किया हैं। कुछ नवीनता भी तो आखिर
चाहिए ही।
हमने
साम्प्रदायिक अर्थों की बानगी दिखा दी। यह ठीक हैं कि तिलक ने अपने अर्थ को
साम्प्रदायिक नहीं माना हैं। बल्कि उन्होने शंकर,
रामानुज आदि के ही अर्थों को साम्प्रदायिक कह के निन्दा की हैं। मगर
साम्प्रदायिकता के कोई सींग-पूँछ तो होती नहीं। जो बात पहले से चली आती हो
उसी का समर्थन करना यही तो साम्प्रदायिकता हैं। तिलक ने यही किया हैं भी।
भक्तिमार्ग तो पुराना हैं। व्यक्त या साकार भगवान की उपासना करना ही
भक्तिमार्ग माना जाता हैं। तिलक ने न सिर्फ इसी श्लोक में,
बल्कि गीतारहस्य में सैकड़ों जगह इसी भक्तिमार्ग पर जोर दिया हैं। वह तो
गीता का विषय ही मानते हैं
'तत्त्वज्ञानमूलक
भक्ति प्रधानकर्मयोग।'
उन्होने भक्तिमार्गियों के ज्ञानकर्म-समुच्चय के समर्थन में भी बहुत ज्यादा
जोर दिया हैं। यदि और नहीं तो गीतारहस्य के
'भक्तिमार्ग'
तथा 'संन्यास
और कर्मयोग'
इन
दो प्रकरणों को ही पढ़ के और खासकर रहस्य के
358-365
पृष्ठों
को ही देख के कोई भी कह सकता हैं कि उसमें घोर साम्प्रदायिकता हैं।
भक्तिमार्ग की आधुनिक वकालत तो ऐसी और कहीं मिलती ही नहीं। श्लोकों के अर्थ
करने में प्राचीन लोगों की अपेक्षा कुछ नई बात कह देने से ही
साम्प्रदायिकता से पिण्ड छूट नहीं सकता। हरेक सम्प्रदाय के टीकाकारों में
पाया जाता हैं कि वे लोग शब्दार्थ में कुछ न कुछ फर्क रखते ही हैं। वे
प्रतिपादन की नई शैली भी निकालते हैं। आखिर पुराने अर्थों एवं तरीकों में
जो दोष विरोधी लोग निकालते हैं उनका समाधन भी तो करना जरूरी होता हैं।
हाँ,
तो
इन अर्थों पर विचार कर देखें कि ये कहाँ तक युक्तिसंगत और सही हैं। सबसे
पहले तिलक की बात लें उनके अर्थ में दो बातें हैं। एक तो वे कृष्ण के साकार
या व्यक्त स्वरूप की ही उपासना,
पूजा या भक्ति का निरूपण इस श्लोक में मानते हैं। दूसरे धर्म का अर्थ कुछ
खास धर्ममात्र करके सन्तोष कर लेते हैं। अब जहाँ तक व्यक्त कृष्ण की उपासना
की बात हैं वह तो कुछ जँचती नहीं। चाहे और बातें कुछ हों या न हों,
लेकिन क्या कृष्ण जैसे महान पुरुष के लिए कभी भी उचित था कि अपने व्यक्त
स्वरूप की पूजा और उपासना की बात कहें?
यह
कितनी छोटी बात हैं! यह उनके दिमाग में आ भी कैसे सकती थी?
वे
ठहरे महान विभूति। फिर इतनी सी मामूली बात को भी क्या वे समझ न सके कि खुद
अपनी पूजा-प्रशंसा की बातें कितनी बुरी और निन्दनीय होती हैं?
वे
इतने नीचे उतरने की बात सोच भी कैसे सकते थे?
उनकी ऐसी हिम्मत हो भी कैसे सकती थी?
यदि यह मान लें कि उन्होने अपने साकार स्वरूप की उपासना की बात नहीं कह के
भगवान के ही वैसे रूप की भक्ति का उपदेश किया,
तो
फिर यह लिखने का क्या अर्थ हैं कि
''यहाँ
भगवान श्रीकृष्ण अपने व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे हैं?''
इस
वाक्य में 'श्रीकृष्ण
अपने'
इन शब्दों
की क्या जरूरत थी?
इनसे तो कृष्ण की अपनी ही प्रशंसा का प्रतिपादन सिद्ध होता हैं।
अच्छा,
यदि यही मान लें कि भगवान के ही व्यक्त रूप की उपासना हैं और कृष्ण अपने को
भगवान समझ के ही ऐसा उपदेश करते हैं;
इसीलिए उन्हें अपनी व्यक्तिगत बड़ाई से कोई भी मतलब नहीं हैं;
तो
दूसरी ही दिक्कत आ खड़ी हो जाती हैं। यदि गीतारहस्य में लिखे इस श्लोक का
शब्दार्थ पढ़ें तो वहाँ लिखा हैं कि
''सब
धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त
करूँगा,
डर
मत।''
यहाँ जो
'आ
जा'
लिखा गया
हैं वह श्लोक के
'व्रज'
का
ही अर्थ हैं। मगर
'व्रज'
का
तो अर्थ होता हैं
'जा'।
व्रज धातु तो जाने के ही अर्थ में हैं,
न
कि आने के अर्थ में। इसलिए जब तक श्लोक में
'आवाज'
नहीं हो तब तक
'आ
जा'
अर्थ होगा
कैसे?
यह तो
उल्टी बात होगी। हमने पहले भी यह लिखा हैं और बताया हैं कि उस दशा में इस
श्लोक का क्या रूप बन जायेगा। जब तक
'आ
जा'
या
'आओ'
अर्थ नहीं करते तब तक अर्जुन के सामने खड़े कृष्ण के व्यक्त स्वरूप की शरण
जाने की बात इस श्लोक से सिद्ध हो सकती ही नहीं। क्योंकि जब कृष्ण खुद
सामने खड़े हैं तो अर्जुन से अपने बारे में
'मेरी
शरण आ जा'
यही कह सकते हैं। अगर
'मेरी
शरण जा'
कहें तब तो प्रत्यक्ष साकार रूप को छोड़ के अपने किसी और या निराकार रूप से
ही उनका मतलब होगा। जो चीज सामने नहीं हो,
किन्तु परोक्ष में या दूर हो,
उसी के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता हैं कि उसकी शरण में जाओ। परन्तु ऐसी
चीज-कृष्ण का ऐसा परोक्ष स्वरूप-तो केवल वही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हो
सकता हैं और यही अर्थ शंकर ने किया भी हैं। तो फिर इसीलिए शंकर पर तिलक के
बहुत ज्यादा बिगड़ने और उन्हें खरी-खोटी सुनाने का मौका ही कहाँ रह जाता हैं?
दूसरी दिक्कत भी सुनिए। धर्म शब्द का इतना संकुचित अर्थ करने के लिए कारण
क्या हैं?
यदि इस प्रकार अर्थ किया जाने लगे तो क्या यह भद्दी खींचतान न होगी?
जिस खींचतान का आरोप तिलक ने खुद शंकर पर बार-बार लगाया हैं उसके शिकार तो
वे इस प्रकार स्वयं हो जाते हैं। इतना ही नहीं। स्वयं गीतारहस्य के
440
और
848
पृष्ठों में महाभारत के अश्वमेध पर्व के
49
और शान्तिपर्व के
354
अध्यायों का हवाला दे के जिन खास-खास धर्मों को गिनाया हैं और जिनमें
'क्षत्रियों
का रणांगण में मरण',
'ब्राह्मणों
का स्वाध्याय',
मातृपितृसेवा,
राजधर्म,
गृहस्थ धर्म आदि सभी का समावेश हैं,
उन्हीं के त्यागने की बात इस श्लोक में कही गयी हैं ऐसी मान्यता तिलक की
हैं। तो क्या इससे यह समझा जाये कि अर्जुन को युद्ध करने से भी उन्होने
रोका हैं?
गृहस्थ धर्म से भी उन्हें हटाया हैं?
माता-पिता की सेवा और क्षत्रिय के धर्म-राजधर्म-से भी उसे उन्होने रोका हैं
और इन सभी को झंझट कहा हैं?
यह तो अजीब बात होगी। युद्ध करने का आदेश बार-बार देते हैं,
यहाँ तक कि उस श्लोक के पहले तक उसी पर जोर दिया हैं;
और
'चातुरर्वण्य
मया सृष्टं'
(4।13)
तथा
'ब्राह्मणक्षत्रियविशां'
(18।41-44)
में न सिर्फ वर्णों के धर्मों पर ही जोर दिया हैं,
बल्कि उन्हें स्वाभाविक,
'स्वभावज'
(Natural)
कहा
हैं।
तो क्या अन्त में सब किये-कराये पर लीपा-पोती करते हैं?
और अगर स्वाभाविक
धर्मों
के छोड़ने की बात का कहना माना
जाये
तो सिंह को अहिंसक होने की भी शिक्षा व्यावहारिक मानी जानी चाहिए। शंकर के
अर्थ में तो यह दिक्कत नहीं
हैं।
क्योंकि वह तो ज्ञानोत्पत्ति
के ही लिए
धर्मों
का त्याग कुछ समय के लिए जरूरी मानते हैं। वे ज्ञान के बाद का त्याग सबके
लिए जरूरी नहीं मानते। मगर जो लोग ऐसा नहीं मान के
धर्म
करने की बात के साथ ही इन
धर्मों
के इमेले से छुटकारे की बात बोलते हैं उनके लिए ही तो आफत
हैं।
और अगर अर्जुन इस प्रकार के
धर्मों
को छोड़ ही दे तो फिर वह करेगा कौन से
'स्वधर्मानुसार
प्राप्त होने वाले कर्म?'
और भी तो देखिये। यदि कुछ इने-गिने धर्मों का ही त्याग करना इस श्लोक में
बताया माना जाये,
तो फिर धर्म शब्द के पहले सर्व शब्द की क्या जरूरत थी?
'धर्मान'
यह बहुवचन शब्द ही तो काफी हैं। उन धर्मों को इसी से समझ ले सकते हैं। ऐसी
हालत में सर्व कहने का तो यही मतलब हो सकता हैं कि कहीं ऐसा न हो कि बहुवचन
धर्म शब्द से कुछी धर्मों को ले के बस कर दें। इसीलिए सर्वधर्मान कह दिया।
ताकि गिन-गिन के सभी धर्मों को ले लिया जाये। पूर्व मीमांसा के
कपिंजलाधिकरण नामक प्रकरण में
'कपिंजलानालभेत'-'कपिंजल
पक्षियों को मारे',
इस वचन में बहुवचन के ख्याल से तीन ही पक्षियों की बात मानी गयी हैं। जब
तीन पक्षी भी बहुत हुईं और उतने ही लेने से
'कपिंजलान्',
बहुवचन सार्थक हो जाता हैं,
तो नाहक ज्यादा पक्षियों का संहार क्यों किया जाये?
यही बात वहाँ मानी गयी हैं। वही यहाँ भी लागू हो सकती थी। इसीलिए
'सर्व'
विशेषण सार्थक हो सकता हैं। मगर तिलक के अर्थ में तो यह एकदम बेकार हैं।
उन्होने खुद गीतारहस्य में शब्दों के अर्थ में जगह-जगह बाल की खाल खींची
हैं और दूसरों को नसीहत की हैं। मगर यहाँ?
यहाँ तो वही
'खुदरा
फजीहत,
दीगरे रा नसीहत'
हो गयी। यहाँ
'अन्यहिं
राह दिखा वहीं आप अँधरे जाहिं''
वाली बात हो गयी!
सबसे बड़ी बात यह हैं कि गीता के उपदेश का यही आखिरी श्लोक हैं। इसके बाद जो
बातें कही गयी हैं वे तो शिष्टाचार वगैरह की हैं कि गीता की ये बातें
किन्हें सुनाई जाये,
किन्हें नहीं आदि-आदि। मगर इस श्लोक में जो पेचीदगी आ जाती हैं। उससे बात
की सच्चाई के बदले घपला और भी बढ़ जाता हैं। यहाँ धर्म कहने से सभी धर्मों
को लें या कुछेक को ही। यदि कुछेक को ही लेने की बात कहें तभी गड़बड़ होती
हैं। सभी के लेने में तो रास्ता एकदम साफ हैं-कहीं रोक-टोक नहीं। कुछेक
लेने में किन्हें लें,
किन्हें नहीं,
यह सवाल खामख्वाह खड़ा हो जाता हैं। यदि यह भी लिखा होता कि शान्ति पर्व या
अश्वमेध पर्व के उन दो अध्यायों में लिखे धर्मों को ही ले सकते हैं,
दूसरों को नहीं,
तो भी काम चल जाता और घपला न होता। मगर ऐसा तो लिखा हैं नहीं। यहाँ तो धर्म
शब्द से ही अटकल लगाना हैं कि किनको लें किनको न लें। ऐसी हालत में यदि कुछ
ऐसे धर्म छूट गये जिन्हें लेना जरूरी हैं,
या कुछ ऐसे लिए गये जिनका लेना ठीक नहीं,
तो क्या होगा?
तब तो सारा मामला ही गड़बड़ी में पड़ जायेगा। ऐसा नहीं होगा यह कैसे कहा जाये?
आखिर अटकलपच्चू बात ही तो ठहरी। फलत: अर्जुन का दिमाग साफ होने के बजाये और
भी आगा-पीछा में पड़ जायेगा-अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना आगा-पीछा में
तो जरूर,
जितना गीताउपदेश के शुरू में था। ऐसी हालत में इसके बाद ही अर्जुन का यह
कहना कैसे ठीक हो सकता हैं कि
''आपकी
कृपा से मेरा मोह दूर हो गया,
मुझे सारी बातें याद हो आयीं और अब मुझे जरा भी शक किसी भी बात में नहीं
हैं;
इसलिए आपकी बात मान लूँगा''-''नष्टोमोह:
स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मिगतसन्देह: करिष्ये वचनं
तवं''
(18।73)?
यह तो उल्टी बात हो जाती हैं। अन्त में कृष्ण की आज्ञा क्या हुई इसका पता
भी लगता नहीं। फिर उनकी किस बात को मानने का वादा अर्जुन ने किया?
और जब रणांगण में मरनेवाला धर्म आखिर में छोड़ देने को ही कहा गया था तो
अर्जुन कृष्ण की बात मान के लड़ने क्यों लगा?
गीतारहस्य में लिखे अर्थ के बारे में जो कुछ कहा गया हैं उससे शेष दो
अर्थों की भी बहुत कुछ बातों पर प्रकाश पड़ जाता हैं। असल में रामानुज भाष्य
में आगे एक दूसरा भी अर्थ किया गया हैं जो तिलक के अर्थ से बहुत कुछ
मिलता-जुलता हैं। वहाँ धर्म का अर्थ कृच्छ्र,
चन्द्रायण,
वैश्वानर आदि अनेक यज्ञ-याग और व्रत विशेष ही किया गया हैं। इसीलिए जो
बातें इस तरह के अर्थ में गीतारहस्य पर लागू हैं,वही उस अर्थ पर भी। यह ठीक
हैं कि तिलक ने एक ही धर्म शब्द के दो अर्थ कर डाले हैं। क्योंकि एक ओर तो
वह कुछ गिने-चुने धर्मों को ही धर्म-शब्दार्थ मान के उनका त्याग चाहते हैं।
लेकिन दूसरी ओर उसी शब्द का यह भी अर्थ करते हैं कि
''स्वधर्मानुसार
प्राप्त होने वाले कर्म करते जाने पर।''
इसीलिए उनके यहाँ ज्यादा गड़बड़ हैं। मगर धर्म शब्द का जो कुछ इने-गिने
धर्मों से ही अभिप्राय माना गया हैं और उसके सम्बन्ध में जो आपत्ति हमने
अभी-अभी बताई हैं वह तो दोनों पर ही लागू हैं।
एक बात और भी दोनों ही में समान रूप से पाई जाती हैं। यदि इस श्लोक के माधव
एवं रामानुज भाष्यों को उनके उन भाष्यों के साथ पढ़ें जो गीता के अन्यान्य
श्लोकों के ऊपर और खासकर ग्यारहवें तथा बारहवें अध्याय के ऊपर लिखे गये
हैं,
तो पता लग जाता हैं,
कि वे लोग सगुण ब्रह्म या साकार कृष्ण भगवान की उपासना को ही इस श्लोक का
विषय मानते हैं। ऐसी दशा में जो भी आपत्ति तिलकवाले अर्थ में
'व्रज'
को ले के या और तरह से उठाई गयी हैं वह तो इनमें भी अक्षरश: लागू हैं। यह
कहना कि गीता का पर्यवसान साकार भगवान की शरणागति में ही हैं,
दूसरा मानी नहीं रखता और इसमें घोर से घोर आपत्ति बताई जा चुकी हैं। हम तो
पहले ही
'अहम्',
'माम्'
आदि शब्दों के अर्थों को समझाते हुए बता चुके हैं कि उन शब्दों से साकार या
व्यक्त कृष्ण को समझना असम्भव हैं-ऐसी कोशिश करना भारी से भारी भूल हैं। जो
कुछ हमें इस सम्बन्ध में कहना था वही कह चुके हैं। उसे इन भाष्यों के भी
सम्बन्ध में पूरा-पूरा लागू किया जा सकता हैं।
रह गयी इन दोनों भाष्यकारों की यह दलील कि धर्म का अर्थ उसका फल और
कर्त्तरृत्वादि हैं,
न कि धर्म का स्वरूप;
क्योंकि गीता के इसी अठारहवें अध्याय के शुरू में ही त्याग का यही अर्थ
माना गया हैं। हमने पहले योग या कर्म तथा फल में अनासक्ति एवं बेलगाव की
बात पर विचार करते हुए गीता के श्लोकों के बीसियों दृष्टान्त दिये हैं।
उनके देखने से साफ हो जाता हैं कि गीता ने बार-बार कर्म और उसके फल का
साथ-साथ वर्णन करके दोनों ही की आसक्ति को मना किया हैं। यही नहीं।
'सुखदु:खे
समेकृत्वा'
(2।38)
जैसे अनेक श्लोकों में कर्म का जिक्र न भी करके उसके फलों को ही साफ-साफ
लिखा और उनमें आसक्ति को सख्ती से रोका हैं। जैसा कि पहले विस्तार के साथ
समदर्शन की बात कही जा चुकी हैं,
यह समदर्शन कर्मों के सम्बन्ध में न हो के अनेक स्थानों पर कर्म के फलों से
ही ताल्लुक रखता हैं।
'यदृच्छालाभसंतुष्ट:'
(4।22),
'न
प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य'
आदि (5।20-22),
'सुहृन्मित्रर्युदासीन'
(6।9),
'अद्वेष्टा
सर्वभूतानां'
आदि (12।13।19)
तथा
'उदासीनवदासीन:'
आदि (14।23-25)
श्लोकों को यदि गौर से देखा जाये तो कर्मों का जिक्र न भी करके फलों से ही
अलग रहने की बात पर जोर देते हैं। दूसरे अध्याय के स्थितप्रज्ञ,
बारहवें के भक्त और चौदहवें के गुणातीत-ये तीनों ही-हैं क्या यदि कर्मों के
फलों से कतई निर्लेप रहने वाले लोग नहीं हैं?
इस प्रकार गीता ने असल चीज फल को ही माना हैं और उसी से बचने,
उसी के त्याग और उसी की अनासक्ति पर खास तौर से जोर दिया हैं। यही कारण हैं
कि कर्मों के साथ तो फलों को अलग लिखा ही हैं;
मगर स्वतन्त्र रूप से भी जगह-जगह लिखा हैं। दूसरे अध्याय में जब गीता की
अपनी चीज-योग-का स्वरूप उसे
'कर्मण्येवाधिकारस्ते'
(2।47-48)
में बताया हैं,
तो फल को अलग कहने की जरूरत पड़ी हैं। उसके बिना काम चली नहीं सकता था। यदि
उसे अलग नहीं कहते तो योग ही चौपट हो जाता। उसकी असली शक्ल बन सकती न थी।
गीता तो कर्म को न देख उसकी आसक्ति को ही देखती और उसी को रोकती हैं। उसी
के साथ उसके फल की इच्छा और आसक्ति को भी हटाती हैं। यह बात हम बहुत अच्छी
तरह सिद्ध कर चुके हैं। यह भी बखूबी बता चुके हैं कि अठारहवें अध्याय के
'निश्चयं
शृणु मे तत्र'
(18।4)
से लेकर
'स
त्यागीत्यभिधीयते'
(18।11)
तक के श्लोकों में साफ ही उसी कर्मासक्ति तथा फलासक्ति का त्याग कहा गया
हैं। फिर भी हमें आश्चर्य होता हैं कि उन भाष्यों के रचयिता महापुरुष
इन्हीं
4
से
11
तक के श्लोकों के आधार पर
'सर्वधर्मान'
में धर्म का अर्थ उसका फल और धर्म के करने का अभिमान यह अर्थ कर डालते हैं!
दोनों की आसक्ति अर्थ करते तो एक बात थी।
यदि उन श्लोकों या गीता के योग-कर्मयोग-की बात यहाँ होती और उसी का उपसंहार
इस श्लोक में माना जाता तो क्या कभी यह बात सम्भव थी कि कर्म और फल या धर्म
और फल को साफ-साफ न कहते और दोनों की आसक्ति का अत्यन्त साफ शब्दों में
निषेध न करते?
गीता की तो यही रीति हैं और इसे उसने कहीं एक जगह भी नहीं छोड़ा हैं। यह बात
हम दावे के साथ कह सकते हैं। बीसियों जगह यह बात गीता भर में आयी हैं। मगर
सभी जगह नियमित रूप से कर्मासक्ति और फलासक्ति का त्याग साथ कहा हैं। फिर
उपसंहार में भी वही बात क्यों न की जाती?
ऐसा न करने से तो अर्जुन के लिए साफ ही शंका की गुंजाईश रह जाती कि कहीं
दूसरा ही तो मतलब नहीं हैं?
उपसंहार में साफ न बोलने से जरूर शंका होती और उसके बाद अर्जुन हर्गिज यह
नहीं कहता कि
''स्थितोऽस्मि
गतसन्देह:।''
इसीलिए दोनों भाष्यकारों का अर्थ गीता को मान्य नहीं यह बात निर्विवाद हो
गयी। यह भी तो उन्हें सोचना चाहिए था कि यदि इस श्लोक में भी संन्यास के
तत्त्व का निरूपण नहीं हैं और इसके पहले तो और किसी श्लोक में हुआ ही नहीं,
जैसा कि अच्छी तरह दिखाया जा चुका हैं,
तो आखिर वह हैं कहाँ?
और अगर कहीं नहीं हैं तो अर्जुन की शंका तो रही जाती हैं। फिर
'नष्टोमोह:'
कैसा?
शंकर के अर्थ में तो ऐसी एक आपत्ति भी नहीं हो सकती। वह तो गीता के कर्मयोग
या योग का निरूपण इसमें मानते ही नहीं। फिर धर्म और फल को अलग- अलग लिख के
उसकी आसक्ति के त्याग की बात का उनके मत से यहाँ अवसर ही कहाँ रह जाता हैं?
वह तो तत्त्वज्ञान के पहले शास्त्रीय विधि विधन के अनुसार कर्तव्य धर्मों
का संन्यास ही इस श्लोक में ज्ञान के साधन के रूप में मानते हैं और वहकाम
'सर्वधर्मान'
से ही चल जाता हैं। मुख्यतया पुराने संस्कार के वश किसी एकाध धर्म में लोग
चिपके न रह जाये इसीलिए सर्वधर्मान कह दिया हैं। सभी से पिण्ड छुड़ाना जरूरी
हैं। एक भी रहेगा तो बाधक होगा जरूर। इस सम्बन्ध में अब और लिखना यहाँ ठीक
नहीं हैं। इसका स्वतन्त्र विचार श्लोकार्थ के प्रसंग से किया जायेगा।
गीता - 8
(शीर्ष पर वापस)