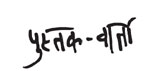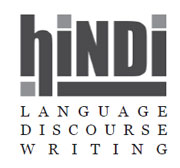त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो
निर्योगक्षेम आत्मवान्॥45।
हे अर्जुन,
वेद तो
(प्रधानतया) त्रैगुण्य या सांसारिक बातों के ही प्रतिपादक हैं। तुम
इन बातों को छोड़ो,
राग-द्वेषादि द्वन्द्व-जोड़े-दो दो-से रहित हो,
हमेशा
सत्त्विगुण की ही शरण लो,
योगक्षेम की परवाह छोड़ दो,
मन को
वश में करो और आत्मतत्त्व में रम जाओ।45।
यहाँ कुछ
बातें जान लेने की हैं। साधारणतया ख्याल हो सकता हैं कि जब त्रैगुण्य
शब्द यहाँ आया हैं जिसका अर्थ हैं तीनों गुणों से बनाया त्रिगुणात्मक,
तो
यहाँ तीनों ही गुण बुरे बताये गये हैं। मगर सत्त्वगुण तो प्रकाशमय
होने से ज्ञानवर्ध्दक हैं। इसलिए उसे क्यों बुरा कहा। इतना ही नहीं।
आगे उत्तरार्ध्द में लिखते हैं कि बराबर सत्त्विगुण की शरण लो-'नित्यसत्त्वस्थ:'।
यदि बुरा होता तो सत्त्व की शरण जाने की बात कहते क्यों?
तब तो
परस्पर विरोध हो जाता न?
इसलिए
सत्त्व को बुरा कहना ठीक नहीं। हाँ,
रज और
तम तो बुरे जरूर ही हैं। उनके बारे में कोई शक नहीं।
असल में तीनों
गुणों का क्या स्वरूप हैं,
काम
हैं और यह करते क्या हैं,
इसका
पूरा विवरण गीता के चौदहवें अध्याय में मिलता हैं। वहाँ देखने से
पता चलता हैं कि जीवात्मा को बाँधने और फँसाने का काम तीनों ही करते
हैं। इसमें जरा भी कसर नहीं होती। सत्त्व यदि ज्ञान और सुख में फँसा
देता हैं तो बाकी और-और चीजों में। मगर फँसाते सभी हैं। इसलिए
'बध्नाति',
'निबध्नन्ति'
आदि
बन्धन वाचक पद वहाँ बार-बार सभी के बारे में समानरूप से आये हैं।
इसीलिए जो मनुष्य इनके पंजे से छूट जाता हैं उसे उसी अध्याय के अन्त
में गुणातीत-तीनों गुणों से रहित उनके पंजे से बाहर-कहा गया हैं। इन
तीनों से अपना पल्ला कैसे छुड़ाया जाये,
यह
प्रश्न करके उत्तर भी लिखा गया हैं। इसी तरह
'त्रिभिर्गुणभयैर्भावै:'
(7।13-14)
आदि दो
श्लोकों में,
बल्कि
इनके पूर्व के 12वें
में भी यही लिखा हैं कि त्रिगुणात्मक पदार्थ ही लोगों को मोह में,
भ्रम
में,
घपले में
डालते हैं।
तब सवाल यह
जरूर होता हैं कि आगे इसी श्लोक में सत्त्व की शरण की बात क्यों कही
गयी?
बात असल यह
हैं कि आखिर इन तीनों से पिण्ड छूटने का उपाय भी तो होना चाहिए,
और
जैसा कि चौदहवें अध्याय के अन्त में कहा हैं,
'विषस्य
विषमौषधाम्'
के
अनुसार जैसे जहर को जहर से ही मिटाते हैं,
और
'कण्टकेनेव
कण्टकम्'
के अनुसार
काँटे से ही काँटे को हटाते हैं,
ठीक
उसी तरह गुण की ही मद से गुणों से पिण्ड छुड़ाना होगा। दूसरा उपाय हैं
नहीं। गुणों में भी दो तो चौपट ही ठहरे। हाँ,
सत्त्व
का काम हैं ज्ञान,
प्रकाश,
सुझाव,
आलस्य
त्याग,
फुर्ती और
मुस्तैदी। इसीलिए कहा गया हैं कि सत्त्व का ही आश्रय बराबर ले के
उक्त विशेषताएँ हासिल करो और अन्त में तीनों से ही छुटकारा लो। बराबर,
निरन्तर,
नित्य
सत्त्विगुण का आश्रय लेने को कहने का आशय यही हैं। जब-जब रज और तम
दबा के आलस्य आदि में फँसाना चाहें तब-तब मुस्तैद हो के सत्त्विगुण
की मदद से लड़ना और उन्हें भगाना होगा। तभी काम चलेगा। यही बात
शान्तिपर्व के धर्मानुशासन के
110वें
अध्याय के ''ये
च संशान्तरजस: संशान्ततमसश्च ये। सत्तवे स्थिता महात्मनो
दुर्गाण्यतितरन्ति ते''
(15),
में भी 'सत्तवे
स्थित:'
शब्द से बताई
गयी हैं। पहले यह कहा हैं कि उनके रज और तम एकबारगी दब गये हैं। फिर
सत्त्व के कायम रहने की बात आयी हैं। इससे साफ हो जाता हैं कि सत्त्व
नित्य रहता हैं,
बराबर
रहता हैं। क्योंकि दोनों शत्रु शान्त जो हो गये! खत्म जो हो गये!
शान्तिपर्व के
इसी श्लोक का 'महात्मान:'
शब्द
गीता के 'आत्मवान'
के ही
अर्थ को कहता हैं। महात्मा लोगों की आत्मा महान होती हैं। इसका
तात्पर्य यह हैं कि उनका मन छोटी-छोटी,
संसार
की क्षुद्र बातों में न पड़ के बहुत ऊपर चला जाता हैं,
बड़ा बन
जाता हैं,
आत्मतत्त्व
में लग जाता हैं। यही वजह हैं कि वह द्वन्द्व या राग-द्वेष,
शत्रु-मित्र,
सुख-दु:ख आदि से अलग हो जाता हैं। उसे इस बात की भी फिक्र नहीं होती
कि अमुक चीज नहीं हैं,
उसे
कैसे लाऊँ और मिली हुई की रक्षा कैसे हो आदि-आदि। इसे ही योग-जोड़ना
या प्राप्त करना और क्षेम-रक्षा करना-कहते
हैं। वह इससे भी मुक्त हो जाता हैं। हमने यही लिखा भी हैं।
शान्तिपर्व के
52वें
तथा 158वें
अध्यायों में जो कुछ भीष्म को आशीर्वाद तथा अर्जुन को उपदेश दिया गया
हैं वहाँ भी बार-बार यह
'सत्त्वस्थ'
पद आया
हैं। 'ज्ञानानि
च समग्राणि प्रतिभास्यन्ति तेऽनघ। नच ते क्वचिदासत्तिर्बुध्दे:
प्रादुर्भविष्यति॥ सत्त्वस्थं च मनो नित्यं तव भीष्म भविष्यति।
रजस्तमोऽभ्यां रहितं घनैर्मुक्तइवोडुराट्'
(52।17-18),
'ये न
हृष्यन्ति लाभेषु नालाभेषु व्यथन्ति च। निर्ममा निरहंकारा:
सत्त्वस्था: समदर्शिन:॥ लाभालाभौ सुखदु:खे च तात प्रियाप्रिये मरणं
जीवितं च। समानि येषां स्थिरविक्रमाणां बुभुत्सतां सत्त्वपथे
स्थितानाम्। धर्मप्रियांस्तान् सुमहानु भावान्दान्तोऽ प्रमत्ताश्च
समर्च्चयेथा:'
(158।33-35)
इन
श्लोकों में अक्षरश: गीता के इस श्लोक की ही बात हैं।
यावानर्थ उदपाने सर्वत: संप्लुतोदके।
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत:॥46॥
(जिस
तरह) जितना काम छोटे-बड़े जलाशयों से निकलता हैं वह सभी केवल एक ही
विस्तृत जलराशिवाले समुद्र या जलाशय से चल जाता हैं;
(उसी
तरह) वेदों से जितना काम चलता हैं आत्मज्ञानी विद्वान् का वह सबका-सब
(यों ही) चल जाता हैं-पूरा हो जाता हैं।46।
इस श्लोक में
जो कुछ कहा गया हैं उसका निष्कर्ष यही हैं कि छोटे जलाशय का काम बड़े
से,
दोनों का उससे
भी बड़े से और अन्त में सभी का काम सबसे बड़े-से-बड़े से बड़े से-चल जाता
हैं। अत: उसके मिलने पर बाकियों की परवाह नहीं की जाती। आत्मज्ञान हो
जाने पर सांसारिक सुखों और भौतिक पदार्थों की परवाह नहीं रह जाती
हैं। क्योंकि आत्मा तो आनन्द सागर ही ठहरी। वृहदारण्यक के चौथे
अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के
32वें
मन्त्र के ''ऐषोऽस्य
परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रमुपजीवन्ति''
से
शुरू करके समूचे लम्बे
33वें
मन्त्र में लोक-परलोक के सभी सुखों एवं आनन्दों का तारतम्य दिखाते
हुए आखिर में आत्मानन्द को ही सबके ऊपर माना हैं। कहा हैं कि भी उसी
के भीतर शेष सभी समा जाते हैं। अन्य उपनिषदों में भी यही बात आती
हैं। यहाँ इसी की ओर इशारा हैं।
इस श्लोक में
ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति न हो के आत्मज्ञानी ही हैं,
यह बात
पहले ही कृपण शब्द की व्याख्या के सिलसिले में कही जा चुकी
हैं।इसीलिए 'ब्राह्मणस्य'
के आगे
'विजानत:'
शब्द
आया हैं जो विज्ञ या विद्वान् का वाचक हैं।
इस श्लोक का
अर्थ करने में किसी-किसी ने उस अर्थ पर तानाजनी की हैं और उसे
खींचतानवाला बताया हैं जो हमने किया हैं। ऐसे लोगों का कहना हैं कि
'सर्वत:
संप्लुतोदके'
का
अर्थ समुद्र या समुद्र जैसा महान जलाशय न करके बाढ़ या जल-प्लावन कर
लेना ही ठीक हैं। इससे श्लोक का यह अर्थ हो जायेगा कि जैसे जल-प्लावन
होने पर जितना प्रयोजन ताल-तलैया का रह जाता हैं,
अर्थात् कुछ भी प्रयोजन रह जाता नहीं,
वैसे
ही आत्मज्ञानी विद्वान् के लिए भी उतना ही प्रयोजन वेदों से रह जाता
हैं-अर्थात् कुछ भी नहीं रह जाता हैं। इस प्रकार आत्मज्ञानी के लिए
वेदों की निष्प्रयोजनता का प्रतिपादन खुले शब्दों में वे लोग इस
श्लोक में मानतेहैं।
बेशक,
इस
अर्थ में वैसी खींचतान नहीं हैं। जैसी हमारे अर्थ में हैं। हालाँकि,
उनके
अर्थ में भी द्रविड़ प्राणायाम जरूर हैं। क्योंकि कुछ भी प्रयोजन नहीं
रह जाता यह बात श्लोक के शब्दों से सिद्ध न हो के अर्थात् सिद्ध होती
हैं। लेकिन ऐसा अर्थ मानने में एक बड़ी अड़चन हैं। असल में साफ-साफ
वेदों को निष्प्रयोजन या बेकार कह देने की हिम्मत किसी भी सनातनी
ग्रन्थ या महापुरुष को नहीं होती। वेदों का स्थान हिन्दू-समाज में
इतना ऊँचा हैं कि उनके बारे में स्पष्ट निन्दासूचक शब्द बोला और लिखा
जा सकता नहीं। ऐसी बात अब तक तो पायी गयी हैं नहीं। ऐसी दशा में गीता
जैसे सर्वप्रिय ग्रन्थ यह बात कहे,
सो भी
स्वयं मर्यादा पुरुषोत्ताम श्रीकृष्ण के ही मुखों से,
यह बात
ठीक जँचती नहीं। इसीलिए तो इससे पहले के
'त्रैगुण्यविषया'
श्लोक
में जहाँ मुनासिब था यह कह देना कि तुम तीनों वेदों की परवाह छोड़ो-'निस्त्रिवेदो
भवार्जुन'
या
'निस्त्रैविद्यो
भवार्जुन',
वहाँ
यही कहा कि तुम त्रैगुण्य-रहित या संसार के पदार्थों से अलग हो जाओ-'निस्त्रैगुण्यो
भवार्जुन'।
यदि श्लोक को गौर से पढ़ा जाये और उसका आशय देखा जाये तो वह यही हैं
कि वेदों के इस जाल से बच जाओ। मगर ऐसा न कहके यही बात घुमा के कहो
कि सांसारिक बातों की लालसा छोड़ दो। इससे भी अर्थात् वैदिक कर्मकाण्ड
छूट ही जायेगे। फिर भी स्पष्टत: ऐसा नहीं कहा। ठीक इसी तरह यहाँ भी
कह दिया हैं कि वेदों का काम आत्मज्ञान से भी चल जाता हैं। मगर उस
सीधे अर्थ में तो कुछ न कुछ छींटा वेदों पर आई जाता हैं। यदि गौर से
देखा जाये। इसी से शंकर ने वह अर्थ नहीं किया हैं। हमने भी उन्हें का
अनुसरण किया हैं।
एक बात और भी
हैं। यदि 'सर्वत:
संप्लुतोदके'
शब्दों
का सर्वत्र जल-प्लावन अर्थ होता हैं,
तो
'संप्लुतोदके'
की जगह
'संप्लुते
दके'
लिखना कहीं
अच्छा होता। दक और उदक शब्दों का अर्थ एक ही हैं पानी। मगर उदक शब्द
रखने पर संप्लुत के साथ उसका समास करना पड़ता हैं,
जिसकी
जरूरत उन लोगों के अर्थ में कतई रह जाती नहीं। वह तो तब होती हैं जब
समुद्र अर्थ करना हो इसीलिए बहुब्रीहि समास करना पड़ता हैं।
'संप्लुतोदके'
लिखने
पर समास की गुंजाइश रह जाने से लोग वैसा कर डालते हैं। मगर यदि वैसा
अर्थ इष्ट न होता तो साफ-साफ
'संप्लुते
दके'
लिख देते। फिर
तो झमेला ही मिट जाता। इससे भी पता चलता हैं कि ऐसा अभिप्राय हुई
नहीं।
शान्तिपर्व के
मोक्षधर्म के 241वें
अध्याय वाला 'ये
स्म बुध्दिं परां प्राप्ता धर्मनैपुण्यदर्शिन:। न ते कर्म प्रशंसन्ति
कूपं नद्यां पिवन्निव'
(10)
श्लोक देखने से पता लगता हैं कि वह भी परमज्ञान या आत्मज्ञान की ही
बात कहता हैं। उसमें साफ ही कहा हैं कि इस परा या सर्वोच्च
बुद्धि-ब्रह्म-विद्या-क्योंकि उपनिषदों में ब्रह्मविद्या को ही परा
विद्या कहा हैं-को जिनने हासिल कर लिया हैं वे कर्मों की बड़ाई नहीं
करते,
उनकी ओर रुजू
नहीं होते। इसमें दृष्टान्त देते हैं कि पीने आदि के लिए जो मनुष्य
नदी में पानी पा लेता हैं वह कूप की परवाह नहीं करता। इससे भी पता
लगता हैं कि जल-प्लावन से यहाँ अभिप्राय न हो के क्रमश: छोटे-बड़े और
उनसे भी बड़े जलाशयों से ही मतलब हैं। इसी मानी में नदी और कूप का नाम
लेना ठीक हो सकता हैं।
इस प्रकार
यहाँ तक कर्मयोग की भूमिका पूरी करके अगले दो श्लोकों में उसी योग का
स्वरूप बताया गया हैं। कर्म के सम्बन्ध की हिकमत,
तरकीब,
चातुरी
या उपाय होने के कारण ही इसे कर्मयोग कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा
विवेचन और विश्लेषण पहले किया जा चुका हैं। शान्तिपर्व के
राजधर्मानुशासन के
112वें
अध्याय में भी योग शब्द उपाय या हिकमत के मानी में यों आया हैं,
''त्वमप्येवंविर्धां
हित्वा योगेन नियतेन्द्रिय: वत्तास्व बुद्धिमूलं तु विजयं मनुरब्रवीत''
(17)।
यहाँ 'योगेन'
शब्द
का अर्थ नीलकण्ठ ने अपनी टीका में
'उपायेन'
ऐसा ही
किया हैं। शान्तिपर्व के
130वें
अध्याय में भी
''अविज्ञानादयोगो
हि पुरुषस्योपजायेते। विज्ञानादपि योगश्च योगो भूतिकर पर''
(12)
श्लोक में नीलकण्ठ लिखता हैं कि
'अयोग
उपायाभाव:'-''अयोग
शब्द का अर्थ हैं उपाय का न होना।''
इससे
भी योग शब्द उपायवाचक सिद्ध होता हैं। योग का स्वरूप दो श्लोकों को
मिला के पूरा हुआ हैं-
कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन।
मा
कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥47॥
योगस्थ:
कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धानंजय।
सिद्धयसिद्धयो:
समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥48॥
तुम्हारा
अधिकार केवल कर्म में हैं;
(कर्मों
के) फलों में हर्गिज नहीं। कर्मों के फलों का ख्याल (भी) न करो। कर्म
के त्याग में तुम्हारा हठ न रहे। हे धानंजय,
योग
में ही कायम रह के,
आसक्ति
या करने का हठ छोड़ के तथा वे खामख्वाह पूरे हों यह परवाह छोड़ के
कर्मों को करो। इसी समता या लापरवाही-बेफिक्री और मस्तागी-को ही योग
कहते हैं।47।48।
पहले दो बार
कहे गये समत्व में और इसमें क्या अन्तर हैं और इसका मतलब क्या हैं ये
सारी बातें पहले ही अत्यन्त विस्तार के साथ लिखी चा चुकी हैं। यह
तीसरा समत्व कुछ और ही हैं यह भी वहीं लिखा गया हैं।
कर्मयोग में
असल चीज योग ही हैं,
जिसका
रूप अभी बताया गया हैं। वह विवेक या ज्ञानस्वरूप ही हैं। यह बात पहले
कही जा चुकी हैं।
46वें
श्लोक में इसी योग के सम्बन्ध की भूमिका स्वरूप जो
'विजानत:
ब्राह्मणस्य'
कहा
हैं उससे यह बात निस्सन्देह सिद्ध हो जाती हैं कि इस योग के मूल में
आत्मतत्त्व का पूर्ण विवेक ही काम करता हैं। उसके बिना इस
योग-कर्मयोग-का स्वरूप तैयार हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो लोग ऐसा
समझते हैं कि कर्मयोग में भी वास्तविक चीज एवं मूलाधार कर्म ही हैं
और योग या बुद्धि-हिकमत,
तरकीब-के रूप में जो ऊँची मनोवृत्ति काम करती हैं,
वह
सिर्फ सहायक हैं,
उसके
स्वरूप को मार्जित और शुद्ध होने में केवल मदद करती हैं,
वह
भूलते हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बहती हैं। कर्म तो उसका एक
कार्यक्षेत्र जैसा हैं। असल चीज तो वह बुद्धि ही हैं। उसके मुकाबिले
में कर्म को ऊँचा दर्जा देने का सवाल हुई नहीं। किन्तु-
दूरेण
ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय।
बुध्दौ
शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतव:॥49॥
हे धानंजय,
विवेक-बुद्धिरूपी योग की अपेक्षा कर्म कहीं छोटी चीज हैं। (इसलिए)
उसी विवेक बुद्धि की ही शरण जा। क्योंकि जो लोग उस विवेक बुद्धि से
रहित होते हैं वही तो फल की आकांक्षा करते (और इसलिए कर्म करते हैं)।49।
यहाँ भी कृपण
शब्द का वही अर्थ हैं जो पहले कहा गया हैं,
अर्थात् विवेक बुद्धि या आत्मतत्त्व के ज्ञान से रहित।
बुद्धियुक्तो
जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्॥50॥
इस संसार में
(उस) विवेकबुद्धिवाला (मनुष्य ही तो) पुण्य-पाप दोनों से पिण्ड छुड़ा
लेता हैं। इसलिए (उस) बुद्धयात्मक योग (की ही प्राप्ति) के लिए यत्न
करो। वह योग ही तो कर्मों (के करने) की चातुरी या विशेषज्ञता हैं,
कुशलता
हैं।50।
कर्मजं
बुद्धियुक्ता
हि फलंत्यक्त्वा मनीषिण:।
जन्मबन्धाविनिर्मुक्ता: पदं गच्छन्त्यनामयम्॥51॥
क्योंकि
बुद्धियुक्त मनीषी-पहुँचे हुए-लोग ही कर्मों से होने वाले (सभी) फलों
से नाता तोड़ के जन्म (मरण) के बन्धनों से छुटकारा पा जाते (तथा)
निरुपद्रव पद-निर्वाणमुक्ति-प्राप्त कर लेते हैं।51।
अब सवाल यह
होता हैं कि तो यह बुद्धि प्राप्त होती हैं कब और इसकी प्राप्ति की
पहचान क्या हैं?
यह तो
कोई विचित्र सी चीज हैं,
अलौकिक
सा पदार्थ हैं,
नायाब
वस्तु हैं,
और
जैसा कि पहले दिखलाया जा चुका हैं,
जीते
ही मौत के समान असम्भव सी हैं। इसलिए इसकी प्राप्ति आसान तो हो सकती
नहीं। यह भी नहीं कि यह कोई स्थूल या साधारण भौतिक पदार्थ हो। यह तो
असाधारण चीज हैं। बाहरी नजरों से देखी भी नहीं जा सकती। तब हम कैसे
जानेंगे कि अब यह हासिल हो गयी?
इसका
उत्तर यह हैं-
यदा ते
मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति।
तदा
गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥52॥
जब तेरी अक्ल
इस बुद्धि भ्रम के कीचड़ से पार हो जायेगी (तो) उस समय तुझे सभी बातों
से विराग हो जायेगा,
(फिर
चाहे वह) जानी-सुनी हों या जानने योग्य हों।52।
शुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला।
समाधावचला
बुद्धिस्तदा
योगमवाप्स्यसि॥53॥
(इस
प्रकार वेदशास्त्रों की सभी बातों से मन के विरागी हो जाने पर) उनके
करते घपले तथा दुविधो में पड़ी तेरी अक्ल जब अन्त:करण या दिमाग के
भीतर ही रुक के वहीं सदा के लिए जम जायेगी तभी (समझना कि) बुद्धिरूपी
योग प्राप्त हो गया।53।
इन दोनों
श्लोकों में जो बातें कही गयी हैं। उनका जरा सा स्पष्टीकरण जरूरी
हैं। यह तो पहले ही कर्तव्याकर्तव्य के विवेचन में बता चुके हैं कि
वेदशास्त्रों के अनेक वचनों और ऋषि-मुनियों के बहुतेरे उपदेशों के
करते लोगों की अक्ल कर्तव्याकर्तव्य का निश्चय कर पाने के बदले और भी
दुविधो में पड़ जाती हैं। उसकी हालत ठीक वही हो जाती हैं जैसे अँधेरी
गुफा में पड़ी कोई चीज अन्दाज से ही टटोलने वाले की। वह कोई निश्चय कर
पाता नहीं और भीतर ही भीतर ऊब जाता हैं। निश्चय की जितनी ज्यादा
कोशिश वह करता हैं उतना ही ज्यादा दुविधा और पचड़ा बढ़ जाता हैं। ठीक
''ज्यों-ज्यों
भीगै कामरी त्यों-त्यों भारी होय''
या
''मर्ज
बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की''
की
हालत हो जाती हैं। मगर करे क्या?
वेदशास्त्रों को छोड़ते भी तो नहीं बनता। जितना पढ़-सुन चुका होता हैं
उसका भी बार-बार खोद-विनोद करता ही जाता हैं। नये-नये जो भी वचन
पढ़ने-सुनने योग्य होते हैं उन्हें भी पढ़ता जाता हैं। समझदारी की यही
तो दिक्कत हैं। यदि अपढ़-अजान होता तो यह कुछ नहीं होता। तब तो
गलत-सही किसी बात को पकड़ के बैठ रहता कि यही ठीक हैं। इसीलिए तो
नादानी को बहुत हद तक दिक्कतों की ढाल माना हैं। मगर हो क्या?
यह
बेचारा तो समझदार ठहरा।
इसीलिए पहले
श्लोक में कहा हैं कि जब योगरूपी विवेक बुद्धि मिल जायेगी तो यह सभी
पढ़ने-पढ़ाने एवं विचार-विमर्श की परेशानी एकाएक जाती रहेगी। तब दिल
चाहेगा ही नहीं कि एक भी पन्ना उल्टे या एक बात का भी खोद-विनोद
करें। जैसे पका फल डाल से अकस्मात अलग हो जाता हैं,
वैसे
ही ये सभी बातें दिल से हट जाती हैं या दिल ही इनसे अलग हो जाता हैं।
वह इन्हें पूछता भी नहीं। इसी को निर्वेद या वैराग्य कहा हैं।
जब मन या दिल
विरागी बन गया तो फिर वेदशास्त्र के हजार तरह के वचनों के करते जो
बुद्धि की परेशानी थी,
बेकली
और बेचैनी थी उस पर भी पर्दा पड़ जाता हैं,
वह भी
आप ही आप जाती रहती हैं-मिट जाती हैं। जैसे कोई आदमी बड़ी परेशानी में
चारों ओर दौड़-धूप करता-कराता तबाह हो,
मगर
अन्देशे या परेशानी के मिटते ही शान्त हो जाये और सुख की साँस लें।
ठीक वही हालत बुद्धि की हो जाती हैं। उसकी सारी दौड़-धूप बन्द हो जाती
हैं। हमेशा के लिए वह निश्चल एवं निश्चिन्त बन जाती हैं। यही बात
दूसरे श्लोक में कही गयी हैं। यह भी बात योग के प्रताप से ही होती
हैं। इसलिए इसे भी योगप्राप्ति की पहचान बताया हैं।
यहाँ पर अचला
और निश्चला ये दो शब्द आये हैं जिनका अर्थ एक ही हैं। इसीलिए ख्याल
हो सकता हैं कि दो में एक बेकार हैं। मगर बात यह हैं कि बुद्धि में
जो स्थिरता आ गयी वह दो तरह की हो सकती हैं। एक तो तात्कालिक या कुछ
समय के ही लिए। दूसरी हमेशा के लिए। कहीं ऐसा न समझ लें कि तात्कालिक
शान्ति और स्थिरता से ही काम चल जाता हैं। इसीलिए लिखा हैं कि निश्चल
बुद्धि जब अचल हो जाती हैं। निश्चल को अचल कह देने से ही उसकी शान्ति
एवं स्थिरता में स्थायित्व का अभिप्राय सिद्ध हो जाता हैं। निश्चल का
अक्षरार्थ भी हैं। चलने से बरी और अचल का अर्थ हैं जो कभी न चले। बरी
तो थोड़े समय के लिए भी रहा जा सकता हैं।
समाधि शब्द का
भी मनमाना अर्थ किया जाता हैं। अभी तक केवल दो ही बार यह शब्द आया
हैं। एक बार इस श्लोक में। दूसरी बार इससे पूर्व
'समाधौ
न विधीयते' (44)
में।
हमने दोनों जगह एक ही अर्थ अन्त:करण या दिमाग किया हैं। समाधि का
अर्थ हैं जिस दशा में या जहाँ मन स्थिर हो,
बुद्धि स्थिर हो,
और
दिमाग या अन्त:करण ही ऐसी चीज हैं जहाँ से मन या बुद्धि की दौड़
बार-बार हुआ करती हैं। मगर ज्योंही यह दौड़ रुकी कि वहीं वे दोनों
शान्त हो जाते हैं। एकाग्रता की दशा में यही होता हैं। इसीलिए हमने
यही अर्थ मुनासिब समझा हैं। जहाँ के हैं वहीं रुक गये,
यही तो
शान्ति,
स्थिरता या
निश्चलता हैं और यही निश्चयात्मकता भी हैं। क्योंकि निश्चय न रहने पर
बीस चीजों में उनकी दौड़ जारी ही रहती हैं।
इतना कह देने
से यह तो हो गया कि योगी की पहचान मालूम हो गयी। मगर इतने से ही तो
काम चलता नहीं दीखता। पहले जब गोलमटोल बात थी तो अर्जुन भी चुप थे।
कृष्ण ने भी अपने ही मन से शंका उठा के जवाब दे दिया। मगर कर्मयोगी
की पहचान सुनने के बाद स्वभावत: अर्जुन को नई जिज्ञासाएँ पैदा हुईं
और उसे पूछना पड़ा। उसे यह सुनते ही एकाएक ख्याल आया कि जो कुछ भी
पहचान योगी की बताई गयी हैं वह तो भीतरी हैं,
बाहरी
नहीं। बुद्धि की स्थिरता या पढ़ने-लिखने से वैराग्य यह तो मनोवृत्ति
ही हैं न?
फिर यह बाहर
कैसे हो और दूसरों की पहचान में कैसे आये?
अपना
काम तो शायद इससे चल जाये। क्योंकि हर आदमी अपनी मनोवृत्ति को बखूबी
समझ सकता हैं। मगर बाहर के लोग कैसे जानें कि कौन योगी हैं?
यह
नहीं कि दूसरों के जानने की जरूरत ही न हो। यदि दूसरे न जानें तो
उन्हें उपदेशक कैसे मिलेगा?
क्योंकि जो खुद योगी न हो वह तो उपदेश कर सकता नहीं। फलत: यदि हमें
योग का रहस्य जानना हैं तो योगी के पास ही जाना होगा। मगर बिना
पहचाने जायेगे कैसे?
इसीलिए
पहचान की जरूरत हैं,
और
इसके लिए बाहरी लक्षण,
जो
उठने-बैठने,
बोलने
आदि से ही जाना जा सके,
मालूम
होना चाहिए।
इसके सिवाय जो
लक्षण,
जो पहचान बताई
गयी हैं वह बहुत ही संक्षिप्त हैं। उसमें एक ही बात हैं,
या
ज्यादे से ज्यादे दो बातें हैं। मगर ज्यादा बातें पहचान के रूप में
मालूम हो जाये तो आसानी हो। इन ज्यादा लक्षणों और बाहरी पहचानों से
यह भी लाभ होगा कि जो खुद योगी होगा वह भी अपने आपको समय-समय पर
तौलता रहेगा। आखिर योग की पूर्णता एकाएक तो हो जाती नहीं। इसमें तो
समय लगता ही हैं। इस दरम्यान में त्रुटियों एवं कमजोरियों का पता
लगा-लगा के उन्हें दूर करना जरूरी हो जाता हैं। इन्हीं त्रुटियों और
कमजोरियों का आसानी से पता लगता हैं। बाहरी लक्षणों से ही। क्योंकि
अपनी कमजोरी अपने आपको जल्द मालूम न होने पर भी दूसरे चटपट जान जाते
हैं। फलत: उनकी बातों से सजग हो के योगी खुद अपनी मनोवृत्ति पर कड़ी
नजर रखता और उसे ठीक करता हैं। यही सब ख्याल करके-
अर्जुन
उवाच
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य
केशव।
स्थितधी: किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्॥54॥
अर्जुन ने
पूछा-हे केशव,
जिसकी
बुद्धि स्थिर तथा समाधि में अचल हो गयी हैं-जो योगी बन चुका हैं-उसकी
परिभाषा-लक्षण-क्या हैं?
वह किस
तरह बोलता हैं,
कैसे
बैठता और कैसे चलता?।54।
यहाँ
'समाधिस्थ'
शब्द
का वही अर्थ हैं जो
'योगस्थ:
कुरु कर्माणि'
में
'योगस्थ'
का
हैं। यदि गौर से देखा जाये,
और हम
पहले विस्तार के साथ लिख भी चुके हैं,
तो इस
योगी की भी वैसी ही समाधि होती हैं जैसी पतंजलि के योगी की। यह
प्राणायाम भले ही नहीं करे। फिर भी कर्म से बालभर भी ईधर-उधर इसकी
दृष्टि,
इसकी बुद्धि
जाने पाती ही नहीं। वहीं जम जाती हैं,
रम
जाती हैं। इसीलिए यह समाधिस्थ और योगस्थ कहा जाता हैं।
श्रीभगवानुवाच
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥55॥
श्रीभगवान ने
कहा,
हे पार्थ,
जब मन
के भीतर घुसी सभी कामनाओं को जड़-मूल से खत्म कर देता और आत्मा में
ही-अपने आप में ही-अपने से ही-खुद-ब-खुद सन्तुष्ट रहता हैं तभी उसे
स्थितप्रज्ञ या अचलबुद्धिवाला कहते हैं।55।
दु:खेष्वनुद्विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृह:।
वीतरागभयक्रोध:
स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥56॥
दु:खों से
जिनका मन उद्विग्न न हो सके,
सुखों
(की प्राप्ति) के लिए जो परेशान न हो और राग,
भय एवं
द्वेष-क्रोध-ये तीनों ही-जिसके बीत गये या खत्म हो चुके हों वही
मननशील-मुनि-स्थितप्रज्ञ कहा जाता हैं।56।
इन दो श्लोकों
में योगी या स्थितप्रज्ञ का लक्षण बताया गया हैं। इस प्रकार अर्जुन
के पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता हैं। बाद के
57वें
में 'किस
तरह बोलता हैं'
का और
58वें
में 'कैसे
बैठता हैं'
का
उत्तर दिया गया हैं। उसके बाद के (59-70)
बारह
श्लोकों में उसी उत्तर के प्रसंग में आयी बातों पर विचार करके
71वें
में 'कैसे
चलता हैं'
का उत्तर दिया
गया हैं। इस तरह सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में कर्मयोगी का पूर्ण
परिचय दे के उसकी वास्तविक दशा का चित्र खींचा गया हैं। उसी दशा को
ब्रह्मनिष्ठा या ब्राह्मीस्थिति भी कहते हैं,
यही
बात अन्तिम श्लोक में कह के समूचे प्रकरण एवं अध्याय का भी उपसंहार
कर दिया गया हैं।
यहाँ जो दो
श्लोकों में दो लक्षण कहे गये हैं उनमें पहला तो नितान्त भीतरी
पदार्थ हैं जिसका पता बाहर से लगना प्राय: असम्भव हैं। किसे पता लग
सकता हैं कि दूसरे आदमी की सभी वासनाएँ खत्म हो गयीं?
अपने
ही भीतर वह मस्त हैं यह भी जानना क्या सम्भव हैं?
आसान
हैं?
इसीलिए दूसरे
श्लोक वाली बातें कही गयी हैं। इन बातों के जानने में आसानी जरूर
हैं। तकलीफों में सिर और छाती पीटना,
हाय-हाय करना आसानी से जाना जा सकता हैं। इसी तरह आराम पाने के लिए
जो बेचैनी होती हैं उसका भी पता लगे बिना रहता नहीं । सबसे बड़ी बात
यह हैं कि राग,
भय और
क्रोध तो छिपनेवाली चीजें हैं नहीं। खासकर भय और उससे भी बढ़ के क्रोध
हर्गिज छिप सकता नहीं। इस प्रकार इन लक्षणों से योगी को आसानी से
पहचान सकते हैं। सभी तरह के लोग इन लक्षणों से फायदा उठा सकते हैं,
यही
इनकी खूबी हैं।
य:
सर्वत्रनभिस्नेहस्तत्तात्प्राप्य
शुभाशुभम्।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥57॥
जो किसी भी
पदार्थ में ममता नहीं रखता-चिपका नहीं होता;
इसीलिए
जो बुरे-भले (पदार्थों) के मिल जाने पर न तो उनका अभिनन्दन ही करता
हैं और न उन्हें कोसता ही हैं,
उसी की
बुद्धि स्थिर मानी जाती हैं।57।
इसके
उत्तरार्ध्द में योगी के बोलने की बात अभिनन्दन न करने और न कोसने की
बात के रूप में साफ ही आयी हैं। योगी के बोलने की यही खास बात हैं कि
वह न तो किसी की स्तुति करता हैं और न निन्दा।
यदा
संहरते चायं कूर्मोनीव सर्वश:।
इन्द्रियाणोन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥58।
जब यह (योगी)
अपनी इन्द्रियों को उनके विषयों से एकबारगी ठीक उसी तरह समेट लेता
हैं जैसे (संकट के समय) कछुआ अपने सभी अंगों को,
(तब)
उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती हैं।58।
कछुए के
चलने-फिरने से एकाएक रुक जाने और सभी गर्दन,
पाँव
आदि को खींच लेने की बात कहके
'योगी
कैसे बैठता हैं'
का
उत्तर दिया गया हैं। वह अपनी सभी इन्द्रियों का दरवाजा ही बन्द कर
देता हैं। फिर न तो किसी मनोरंजन पदार्थ के लिए कहीं आना होता हैं और
न जाना। यों शरीर-यात्रर्थ
नित्य क्रियादि के करने में आने-जाने पर कोई भी रोक नहीं होती।
61वें
श्लोक में भी इन्द्रियों के ही रोकने की बात दुहराई गयी हैं और कहा
गया हैं कि इन्द्रियाँ जिसके वश में हों वही स्थिर बुद्धिवाला हैं।
इन्द्रियों को
विषयों से रोक देने की बात सुन के सवाल होता हैं कि यदि योगी की यही
बात हैं तो हठयोगी तपस्वी को भी क्या कभी गीता का कर्मयोगी कह सकते
हैं?
वह भी तो आखिर
विषयों से किनाराकशी करी लेता हैं। अपनी इन्द्रियों पर वह इतनी सख्ती
के साथ लगाम चढ़ाता हैं कि वे टस से मस होने पाती हैं नहीं।
सर्दी-गर्मी और भूख-प्यास पर उसका कब्जा साफ ही नजर आता हैं। मगर ऐसे
हठी तपस्वियों और योगियों में तो जमीन-आसमान का अन्तर हैं। यह कैसे
होगा कि गीता का योगी तपस्वी के साथ मिल जाये-उसी तपस्वी से जिसका
वर्णन स्मृतिग्रन्थों में पाया जाता हैं?
तब तो
यह योगी और योग गीता की अपनी चीज रह जायेगी नहीं। वह एक प्रकार से
बहुत ही आसान चीज हो जायेगी। इसीलिए इसका स्पष्टीकरण आगे के बारह
श्लोकों में करना जरूरी हो गया। क्योंकि यह विषय जरा गहन हैं। यह भी
बात हैं कि क्या केवल विषयों के रोकने मात्र की ही जरूरत होती हैं,
या और
कुछ भी जरूरी होता हैं,
यह भी
जान लेना आवश्यक हैं। नहीं तो धोखा हो सकता हैं,
होता
हैं।
विषया
विनरिवत्तान्ते निराहारस्य देहिन:।
रसवर्जं
रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा नरिवत्ताते॥59॥
आहार छोड़ देने
वाले मनुष्य के विषय तो (स्वयं) हट जाते हैं। (मगर उनके प्रति)
रागद्वेष बने रह जाते हैं। ये भी निवृत्त हो जाते हैं (सही;
लेकिन)
ब्रह्म-रूपी आत्मा को देखने पर ही,
आत्मतत्त्व के ज्ञान के बाद ही।59।
यहाँ आहार
शब्द विचित्र हैं। सर्वसाधारण में प्रचलित आहार शब्द का अर्थ हैं
भोजन। यह भी माना जाता हैं कि केवल खाना-पीना-अन्न-छोड़ देने से ही
सभी इन्द्रियाँ अपने आप शिथिल हो के पस्त और अकर्मण्य हो जाती हैं।
फलत: विषयों तक पहुँच नहीं सकती हैं। हालत यहाँ तक हो जाती हैं कि
निराहार या अनशन करनेवाले के कान में हारमोनियम बजाइये तो भी उसे कुछ
पता ही नहीं चलता हैं। नासिका के पास इतर-गुलाब लाइए तो भी उसे गन्ध
का पता नहीं चलता। इसीलिए छान्दोग्योपनिषद् के सातवें
प्रपाठक-अध्याय-के नवें खण्ड में लिखा भी हैं कि यदि दस दिन भोजन न
करे तो उसके प्राण भले ही न जायें,
फिर भी
सुनना,
सोचना,
विचारना वगैरह तो खत्म ही हो जाता हैं-''यद्यपि
दशरात्रीर्ना श्नीयाद्यद्युहजीवेदथवाऽद्रष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽ-
बोद्धाऽकर्ताऽविज्ञाता भवति''
(9।1)
दूसरी ओर यह
मानने वाले भी बहुत से लोग हैं कि आहार का अर्थ केवल अन्न न हो के
इन्द्रियों के पदार्थ या विषय को ही आहार कहना उचित हैं। आहार शब्द
का अर्थ भी यही होता हैं कि जो अपनी ओर खींचे। विषय तो खामख्वाह
इन्द्रियों को खींचते ही हैं। पहले श्लोक में सिर्फ भोजन की बात न आ
के विषयों की ही बात आयी हैं। बादवाले श्लोक में भी इन्द्रियों के
विषयों की ओर ही खिंच जाने और मन को खींच ले जाने की बात कही गयी
हैं। छान्दोग्योपनिषद् के सातवें प्रपाठक के अन्त में यह भी लिखा गया
हैं कि आहार की शुद्धि से सत्त्व की शुद्धि और सत्त्व की शुद्धि से
पक्की एवं चिरस्थायी स्मृति,
जिसे
स्मरण या तत्त्वज्ञान कहते हैं,
होती
हैं,
जिससे सारे
बन्धन कट के मुक्ति होती हैं-''आहारशुध्दौ
सत्त्वशुद्धि: सत्त्वशुध्दौ धा्रुवा स्मृति: स्मृतिलम्भे
सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष:''
(7।26।2)।
यदि इस वचन से पहले वाले इसी
26वें
खण्ड के ही वाक्य पढ़े जाये या सारा प्रकरण देखा जाये तो साफ पता चलता
हैं कि यहाँ आहार शब्द का अर्थ इन्द्रियों के विषय ही उचित हैं,
न कि
भोजन। यही ठीक भी हैं। केवल भोजन तो ठीक हो और बाकी काम ठीक न रहें
तो सत्त्विगुण या उस गुण वाले अन्त:करण की शुद्धि कैसे होगी और उसकी
मैल कैसे दूर होगी?
तब तो
खामख्वाह रज और तम का धावा होता ही रहेगा। फलत: वे सत्त्व या
सत्त्व-प्रधान अन्त:करण को रह-रह के दबाते ही रहेंगे। इसीलिए चौदहवें
अध्याय के अन्त में गीता में भी गुणों से पिण्ड छूटने के लिए ऐसी
चीजें बताई गयी हैं जो भोजन से निराली और विभिन्न विषय रूप ही हैं।
यह ठीक हैं कि
जब अनशन करने वाले लोग कहें कि इन्द्रियों को वश में करने के लिए
आत्मतत्त्व विवेक की जरूरत हैं नहीं;
केवल
निराहार होने से ही काम चल जायेगा,
तो
उनके उत्तर में इस श्लोक में यह कहने का सुन्दर मौका हैं कि हाँ,
इन्द्रियाँ तो रुक जाती हैं जरूर। मगर रस या चस्का तो बना ही रहता
हैं,
जिसे राग और
द्वेष के नाम से पुकारते हैं इसीलिए तत्त्वज्ञान की जरूरत हैं।
क्योंकि वह रस तो उसी से खत्म होता हैं। इस प्रकार श्लोक की संगति भी
बैठ जाती हैं। मगर यह संगति तो विषयों की बात मान लेने पर भी बैठ
जाती ही हैं। क्योंकि हठी तपस्वी लोग एकदम निराहार तो नहीं हो जाते।
शरीररक्षार्थ कुछ तो खाते-पीते हुईं। हाँ,
काम-चलाऊ मात्र ही स्वीकार करते और शीत-उष्ण की सख्ती के साथ सह के
इन्द्रियों को बलपूर्वक रोक रखते हैं। आखिर उनका भी तो जवाब चाहिए।
ऐसे ही लोग ज्यादा होते हैं भी। इसीलिए गीता ने उनका और दूसरों का भी
उत्तर इसी श्लोक में दिया हैं। राग और द्वेष को ही यहाँ रस कहा गया
हैं। इन्हीं का दूसरा नाम काम एवं क्रोध और भय तथा प्रीति भी हैं।
इसे गीता ने खासतौर से संग कहा हैं।
इसी के लिए
आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जरूरी माना गया हैं। वही योग का
मूलाधार हैं। उसी के लिए सबसे पहले महान यत्न करना जरूरी हैं। मगर
कुछ लोग ऐसा गुमान कर सकते हैं कि आत्मज्ञान जैसी दुर्लभ चीज के लिए
परेशान होने और मरने की क्या जरूरत हैं?
इन्द्रियों के रोकने का ही ज्यादे से ज्यादा यत्न और अभ्यास करके यह
काम हो सकता हैं कि वे आगे चल के कभी भी विषयों की ओर न ताकें। आखिर
राग-द्वेष लाठी से तो मारते नहीं। होता हैं यही कि उनके रहते
इन्द्रियों के लिए खतरा बना रहता हैं कि कभी विषयों में जा फँसेंगी।
यही बात न होने का उपाय अभ्यास हैं। अभ्यास करते-करते ऐसी आदत पड़
जायेगी कि अन्त में विषय भूल जायेगे। मगर ऐसे गुमानवाले न तो
इन्द्रियों की ही ताकत जानते हैं और न राग-द्वेष की मोहनी और महिमा
ही। यह राग-द्वेष ही ऐसी रस्सी हैं जो विषयों को इन्द्रियों से और
इन्द्रियों को मन से जोड़ती हैं। जब तक यह रस्सी जल न जाये कोई उपाय
नहीं। तब तक इन्द्रियाँ खुद तो विषयों में जायेगी ही। मन को भी घसीट
लेंगी। यही बात आगे यों कहते हैं-
यततो
ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित:।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन:॥60॥
हे कौन्तेय,
पूरा
समझदार पुरुष के (हजार) यत्न करते रहने पर भी (ये) बेचैन कर देने
वाली इन्द्रियाँ मन को (अपनी ओर) बलात् खींच लेती हैं।60।
इस श्लोक में
'पुरुषस्य
विपश्चित:'
कहने
का प्रयोजन यही हैं कि ऐरे-गैरे की तो बात ही मत पूछिए। विवेकी और
मुस्तैद-मर्दाने-लोगों की भी दुर्गति ये बदजात इन्द्रियाँ कर डालती
हैं। इसी तरह 'हरन्ति'
शब्द
का आशय यह हैं कि हमें पता नहीं लगने पाता और चुपके से मन उधर खिंच
जाता हैं। हम हजार चाहें कि ऐसा न हो। मगर इन्द्रियाँ तो ललकार के
ऐसा करती हैं और हमें पता तब चलता हैं जब एकाएक देखते हैं कि मनीराम
गायब हैं!
इस बात का
बहुत ही सुन्दर आलंकारिक वर्णन कठोपनिषद् के प्रथमाध्याय की
द्वितीयवल्ली में इस तरह किया गया हैं। जब कोई भला आदमी घोड़ागाड़ी पर
चढ़के पक्की सड़क के रास्ते कहीं जाये तो उसे सजग रह के चलना तो होता
ही हैं। नहीं तो घोड़े कहीं बहक जायें और गाड़ी नीचे जा गिरे। उसकी
यात्र में वह खुद होता हैं। कोचवान,
लगाम,
घोड़े,
गाड़ी
ये भी होते ही हैं। सड़क भी होती हैं और उसके किनारे दोनों ओर अकसर
नीचे और गहरे गढ़े भी होते हैं। यदि उस नीची जगह में हरी घास लहलहाती
हो तो क्या कहना?
घोड़े
तो घास की ओर जरूर ही जोर मारते हैं। उन्हें लक्ष्य स्थान पर पहुँचने
से क्या मतलब?
वह यह
भी क्या समझने गये कि यदि नीचे उतरे तो गाड़ी और गाड़ी के मालिक वगैरह
के साथ खुद भी उन्हें जख्मी होना या मरना होगा?
उन्हें
तो हरी घास की चाट होती हैं,
उसका
चस्का होता हैं। बस,
बाकी
बातें भूल जाती हैं। ऐसी दशा में यदि कोचवान जरा भी लापरवाह हुआ या
ऊँघा और लगाम जरा भी ढीली हुई तो सारा गुड़ गोबर हुआ। रथ या गाड़ी के
मालिक को भी पूरा सतर्क रहना होता हैं।
उपनिषद में
आत्मा को रथी या गाड़ी का मालिक और सवार करार दे के बुद्धि को
कोचवान-सारथी,-मन
को लगाम-प्रग्रह-और इन्द्रियों को घोड़े की जगह माना हैं। शरीर ही
रथ-गाड़ी-और संयतजीवन ही पक्की सड़क मानी हैं। इस संयम से हटना खन्दक
में जाना हैं जहाँ इन्द्रियों के विषय लहलहाती घास हैं। लक्ष्य स्थान
हैं निर्वाणमुक्ति या ब्रह्मनिष्ठा। जीवन की लम्बी यात्र तय करनी
हैं। फलत: आत्मा यदि सतर्क न रहे,
बुद्धि
को ताकीद न करे कि लगाम को कस के पकड़ो तो घोड़े जरूर ही में जाये और
सबको चौपट करें। कितना सरस,
पर
कितना काम का,
यह
वर्णन हैं! इसलिए वहाँ कह दिया हैं कि जिसकी बुद्धि चुस्त और मन
कब्जे में हैं वही जीवनयात्र सकुशल पूरी करके विष्णु के परम
पद-मोक्ष-तक पहुँच जाता हैं-
आत्मानं
रथिनं विद्धि
शरीरं रथमेव तु।
बुध्दिं
तु सारथिं विद्धि
मन: प्रग्रहमेव च॥3॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीषिण:॥4॥
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे:॥5॥
यस्तु
विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा।
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे:॥6॥
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्क: सदाऽशुचि:।
न स
तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति॥7॥
यस्तु
विज्ञानवान भवति समनस्क: सदाशुचि:।
स तु
तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न
जायेते॥8॥
विज्ञान-सारथिर्यस्तु मन:-प्रग्रहवान्नर:।
सोऽधवन:
पारमाप्नोति तद्विष्णो: परमं पदम्॥9॥
इसलिए इस विषय
की विषमता को समझ के हमेशा सजग रहना ही होगा तभी काम चल सकता हैं।
इसीलिए आत्मज्ञान की भी जरूरत हैं। यदि रथ का मालिक ही जगा न हो तो
खुदा ही खैर करे। तब तो सारा मामला ही चौपट। इसलिए-
तानि
सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर:।
वशे हि
यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥61॥
उन
सभी-इन्द्रियों-को रोक-कब्जे में कर-के आत्मा में ही मन को रमाये हुए
डटा रहे। क्योंकि (इस प्रकार) जिसके वश में इन्द्रियाँ हों वही
स्थितप्रज्ञ हैं ।61।
यहाँ
'मत्पर:'
में
'मत्'
का
अर्थ साकार कृष्ण नहीं हैं। इसका तो प्रसंग हुई नहीं। यहाँ तो
आत्मज्ञान का ही प्रसंग हैं। इसीलिए ब्रह्म या परमात्मा रूपी आत्मा
से ही यहाँ तात्पर्य हैं। कहते हैं कि,
जिस
प्रकार अत्यन्त चंचल और क्रियाशील भूत को शान्त करने की लिए कभी किसी
चतुर व्यक्ति ने बहुत लम्बे बाँस पर लगातार चढ़ने-उतरने का काम उसे
दिया था-क्योंकि वह उससे काम माँगता ही रहता था और इस तरह बेचैन कर
डालता था,
यहाँ तक कि
झपकी मारने भी न देता था,-ठीक
उसी तरह आत्मा में ही जब मन रम जाये-जब अन्त:करण से आत्मा तक ही
आने-जाने की उसे इजाजत हो,
न कि
जरा भी ईधर-उधर-तभी वह शान्त होता हैं। तभी इन्द्रियाँ भी कब्जे में
रहती हैं। इस मामले में कितना सतर्क रहने की जरूरत हैं,
किस
तरह लोग धोखा खा जाते हैं। और नीचे जा गिरते हैं,
पद-पद
पर इसमें कितना खतरा हैं और अनजान में भी जरा सी रिआयत करने से किस
तरह सब किये-कराये पर पानी फिर जाता हैं,
इसका
बारीक से बारीक विवेचन और ब्योरा आगे के दो श्लोक यों करते हैं-
ध्यायतो
विषयान्पुंस: संगस्तेषूपजायेते।
संगात्संजायेते
काम: कामात्क्रोधोऽभिजायेते॥62॥
क्रोधद्भवति
सम्मोह: सम्मोहातस्मृतिविभ्रम:।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो
बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥63॥
विषयों-इन्द्रियों के विषयों या भौतिक पदार्थों-का ख्याल करते ही
मनुष्य के (दिल में उनके प्रति) राग या आसक्ति पैदा हो जाती हैं। राग
से (उनकी प्राप्ति की) इच्छा होती हैं। इच्छा से क्रोध होता हैं।
क्रोध से जबर्दस्त अन्धकार जैसा मोह पैदा हो जाता हैं। उस सम्मोह का
फल होता हैं। हर तरह की स्मृति-स्मरण या याद-का खात्मा। स्मृति के
खत्म हो जाने से विवेक शक्ति जाती रहती हैं। विवेकशक्ति के चौपट हो
जाने पर वह खुद चौपट हो जाता हैं।
62-63।
यहाँ जितनी
बातें एक के बाद दीगरे कही गयी हैं उनका क्रम क्या हैं और प्रक्रिया
कैसी हैं,
इसे अच्छी तरह
समझ लेना आवश्यक हैं। यह ठीक हैं कि जब तक किसी चीज का ख्याल न हो
उससे मन चिपकता नहीं,
उसमें
सटता नहीं। देखते हैं कि फोटोग्राफ के प्लेट या पटरी पर उस हर पदार्थ
का बहुत बारीक असर (impression)
पड़
जाता
हैं
जो उसके सामने से गुजरता
हैं।
इसी को संस्कार कहते हैं। यदि किसी सुगन्धित
वस्तु को कहीं रख दें तो उसके हट जाने पर भी उसका कुछ न कुछ असर रही
जाता
हैं।
इसी तरह दिमाग के सामने जो चीज आती
हैं
उसका भी असर उस पर पड़ता ही
हैं।
दिमाग तो भीतर
हैं।
इसलिए उसके सामने बाहरी चीजें इन्द्रियों की खिड़कियों से ही होकर
पहुँचती हैं। सो भी वे खुद नहीं;
किन्तु अन्त:करण या मन हू-ब-हू उन्हीं के आकार का
बन के भीतर लौटता
हैं।
इसी तरह वे दिमाग के सामने आती हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता
हैं
कि इन्द्रियों की खिड़कियाँ बन्द रहने पर भी चीजों के आकार को मन
दिमाग के सामने खड़ा कर देता
हैं।
यह इसीलिए होता
हैं
कि पहले इन्द्रियों के रास्ते कभी वे भीतर आयी थीं और अपना असर छोड़
गयी थीं। बस उसी असर के
आधार
पर मन उनका स्वरूप तैयार कर लेता
हैं।
इसी को
ख्याल,
स्मरण, या
ध्यान
कहते हैं,
चिन्तन कहते हैं। इन श्लोकों में पहली बात यही
कही गयी
हैं।
उसका नतीजा यह
होता हैं कि उन चीजों से मनीराम लिपट जाते हैं,
उनमें
आसक्त हो जाते हैं,
फिदा
हो जाते हैं। यह ठीक हैं कि यह आसक्ति यों ही नहीं हो जाती। कितनी ही
चीजें रोज दिमाग के सामने गुजरा करती हैं। मगर सभी के साथ संग या
आसक्ति कहाँ देखते हैं?
हाँ,
जो
चीजें बार-बार सामने आ जाये,
जिनका
बार-बार ख्याल हो उनमें आसक्ति होती हैं। या ऐसा भी होता हैं कि यदि
चीज में कोई विलक्षणता हो तो पहली बार सामने आने पर ही मनीराम उस पर
लट्टू हो जाते हैं। यह बात वस्तु की अपनी विशेषता और सामने आने की
परिस्थिति पर ही अवलम्बित हैं। यही हैं दुनिया का तरीका। यही दूसरी
बात यहाँ कही गयी हैं।
आसक्ति होने
पर उसे प्राप्त करने की इच्छा,
आकांक्षा या तमन्ना होती ही हैं। उसी के लिए रास्ता साफ करना आसक्ति
का काम हैं। इच्छा को ही काम भी कहते हैं। इसका दर्जा तीसरा हैं। यह
असम्भव हैं कि इच्छा हो ही न और आसक्ति यों ही रह जाये।
काम के बाद
क्रोध का दर्जा आता हैं-उसी का चौथा नम्बर हैं। जिसे काम या इच्छा न
हो उसे क्रोध से क्या ताल्लुक?
उसमें
तो क्रोध का दर्शन भी न होगा। इच्छा से क्रोध यों ही नहीं होता।
किन्तु उसके मौके आते रहते हैं। इच्छित वस्तु न प्राप्त हुई,
उसकी
प्राप्ति में देर हुई या बीच में कोई जरा भी अड़ंगा आ गया,
तो चट
क्रोध उमड़ पड़ता हैं। इच्छा जितनी ही तेज होगी,
क्रोध
भी उतना ही तेज होगा और शीघ्र होगा भी। क्योंकि तब तो जरा भी बाधा या
विलम्ब बर्दाश्त हो सकेगी नहीं। यह भी होता हैं कि मिली हुई चीज किसी
वजह से दूर हो जाती हैं,
हट
जाती हैं और क्रोध भड़क उठता हैं। तात्पर्य यह हैं कि बलवती इच्छा के
बाद इच्छित पदार्थ की जुदाई,
उसका
पार्थक्य या अलग होना ही इच्छा को क्रोध में परिणत कर देता हैं। जैसी
इच्छा होगी वैसा ही क्रोध भी होगा।
यहाँ एक बात
याद रखने की हैं। बहुत लोग गीता के
'कामात्क्रोधोऽभिजायेते'
का
सीधा अर्थ 'काम
से क्रोध होता हैं'
करने
के बजाये बीच में अपनी ओर से पुछल्ला लगा देते हैं कि काम-इच्छा-की
पूर्ति में बाधा पड़ने से क्रोध होता हैं। वे यह भी समझते हैं कि
उन्होने अर्थ का स्पष्टीकरण कर दिया। मगर ऐसा करने में वह भूल जाते
हैं कि गीता का असली अभिप्राय ही चौपट हो जाता हैं। गीता के काम से
क्रोध की उत्पत्ति सीधे ही कहने का मतलब यही हैं कि क्रोध की असल
बुनियाद और अनर्थ का मूल कामना ही हैं। इसलिए उसी को दूर करना होगा।
उन लोगों के अर्थ में यह बात-कामना को ही अनर्थ बताने की बात-नहीं रह
जाती हैं। क्योंकि ज्यों ही उन्होने बाधा का नाम लिया कि सबने समझ
लिया कि असली बला कामना नहीं हैं। क्योंकि कामना होने पर भी तो
खामख्वाह क्रोध होता ही नहीं। वह होता तो हैं जब कामना की पूर्ति में
बाधा आ जाये। और अगर बाधा न आये तो?
तब
क्रोध क्यों होगा?
इस तरह
जो महत्त्व कामना को मिलना चाहिए वही मिल जाता हैं बाधा को। फलत:
कामना से ध्यान हट जाता हैं-जैसा चाहिए वैसा ख्याल कामना के
मुतल्लिक रहता नहीं। पीछे चाहे हजार कहें कि बाधा तो होती ही हैं,
ऐसा तो
सम्भव नहीं कि सदा हर हालत में कामनाएँ पूरी हों,
आदि-आदि। मगर वह बात रह जाती नहीं-वह मजा और स्वारस्य रह जाता नहीं।
और जब बाधाएँ अवश्यमेव आती ही हैं,
तब
उनके जिक्र की जरूरत ही क्या हैं?
गीता
के तीसरे अध्याय के अन्त में
'काम
एष क्रोध एष'
में तो
साफ ही काम और क्रोध को एक ही कहा भी हैं।
पाँचवीं
श्रेणी में मोह या सम्मोह आता हैं जो क्रोध से पैदा होता हैं। मोह तो
एक तरह का पर्दा हैं जो दिमाग पर,
विवेकशक्ति पर पड़ जाता हैं। जब वही पर्दा खूब जबर्दस्त और गाढ़ा हो तो
उसे सम्मोह कहते हैं। हमारी आँखों के सामने हजारों चीजें पड़ी हों और
बीच में पर्दा न हो तो हम सबको ठीक-ठीक देखते,
जिन्हें चाहते उन्हें चुन लेते,
उनके
बारे में कुछ दूसरा ख्याल करते और सोचते-विचारते हैं। मगर अगर बीच
में कोई पर्दा आ जाये तो यह सारी बात रुक जाती हैं। यही हालत दिमाग
की भी हैं। युगयुगान्तर की देखी,
सुनी
और जानी हुई बातें संस्कार के रूप में उसमें पड़ी रहती हैं। उनका एक
तरह का सूक्ष्म चित्र पड़ा रहता हैं। समय-समय पर दिमाग उन्हें देखता,
विचारता,
चुनता और उनसे
काम लेता रहता हैं। उन चीजों और उसके बीच कोई पर्दा नहीं होता। हाँ,
नींद,
नशा,
बीमारी
आदि के करते मोटा या महीन पर्दा कभी-कभी आ जाया करता हैं और ऐसा हो
जाता हैं कि वे ओझल हो गयीं। यही बात क्रोध के समय भी होती हैं। कहते
हैं कि क्रोध में आदमी अन्धा हो जाता हैं-उसे सूझता ही नहीं। इसका
यही मतलब हैं। क्रोध का पर्दा बड़ा खतरनाक होता हैं। वह बुरी तरह
भटकाता और गुमराह करता हैं। जिससे महान अनर्थ हो जाता हैं। यह बात
नींद वगैरह में नहीं होती हैं। क्रोध में तो इन्सान क्या से क्या कर
बैठता हैं। इसलिए उसे सम्मोह कहा हैं। इसीलिए गीता के तीसरे अध्याय
के अन्त के (36-43)
आठ
श्लोकों में इसी क्रोध को सभी पापों का मूल कारण,
महापाप,
आवरण,
कुम्भकर्ण जैसा पेटवाला,
असली शत्रु,
आग और
कभी पूरा न होनेवाला बताया हैं। उससे सुन्दर चित्रण हो सकता हैं
नहीं। क्रोध होते ही दिमाग में भादों की घोर अँधेरी छा जाती हैं।
''त्रिविधां
नरकस्येदं'' (16।21-22)
आदि दो
श्लोकों में काम,
क्रोध
और लोभ को नरक के द्वार तथा आत्मा के नाशक कह दिया हैं।
सम्मोह से
स्मृति का खात्मा हो जाता हैं और यही छठी बात हैं। घोर अँधियारी में
सूझने क्यों लगा?
अँधियारी का तो काम ही हैं कि किसी चीज का पता लगने न दे। स्मृति या
स्मरण के भ्रंश का अर्थ इतना ही हैं कि स्मृति हमेशा के लिए खत्म न
हो के तत्काल जाती रहती हैं। यह तो कही चुके हैं कि दिमाग में सारी
बातों के सूक्ष्म चित्र हैं। वह भौतिक या बाहरी कान,
आँख
आदि तो हैं नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव तो उन बातों का होता नहीं।
किन्तु वह स्मरण हो आती हैं। यही दिमाग का देखना हैं और क्रोध के
चलते यही हो पाता नहीं;
रुक
जाता हैं। जितनी बातें पहले देखी-सुनी,
पढ़ी-लिखी या जानी थीं एक की भी याद नहीं हो पाती। सब चौपट!
इसका परिणाम
यह होता हैं कि भले-बुरे,
कर्तव्य-अकर्तव्य,
आत्मा-अनात्मा आदि का विवेक हो पाता नहीं-यह विवेक-शक्ति ही कुण्ठित
हो जाती हैं और अपना काम कर पाती नहीं। यही सातवीं चीज होती हैं।
विवेक या विचार हैं क्या चीज यदि जानी-सुनी बातों का जोड़-बटोर और
मिलान नहीं हैं?
समय-समय पर सभी तरह की बातें हम जानते रहते हैं और उनका संस्कार
दिमाग में पड़ा रहता हैं। कभी कुछ जानते तो कभी कुछ। एक बार एक चीज
जानते;
तो दूसरी बार
दूसरी और कभी-कभी पहले की विरोधी। एक लम्बी बात का एक अंश आज,
एक कल,
दो
परसों इस तरह भी जानते रहते हैं। एक दिन जिसे सही जानते हैं,
दूसरे
दिन उसी को अंशत: या पूरा-पूरा गलत जानते हैं। ये सारी
जानकारियाँ-सारी बातें-फोटो की तख्ती पर के चित्र की तरह दिमाग में
पड़ी रहती हैं। दिमाग का यही काम हैं कि समय-समय पर इन्हें जोड़ बटोर
कर-इन्हें स्मरण करके-एकत्र करके-और काट-छाँट के एक नई बात,
नई चीज,
नया
निश्चय तैयार करे। इसे ही विवेक कहते हैं। विवेक का अर्थ हैं
काट-छाँट,
जोड़-बटोर करना,
चावल
को भूसे से जुदा करके राशि बनाना। मगर जब जानी-सुनी बातें याद ही
नहीं,
उनकी स्मृति
ही नहीं,
तो विवेक कैसे
होगा?
तब अक्ल और
बुद्धि कैसे होगी-समझ
क्योंकर होगी?
इस तरह
भौतिक पदार्थों का ही विवेक जब नहीं हो पाता,
तो फिर
आत्मा का विवेक और उसका तत्त्वज्ञान कैसे होगा?
वह तो
गहन विषय हैं। इसलिए उसके सम्बन्ध की बातों का जाना-सुना जाना तो और
भी लापता हो जायेगा,
उड़
जायेगा,
खत्म हो
जायेगा।
और जब बुद्धि
ही नहीं तो मनुष्य को चौपट ही समझिये। यही आठवीं और अन्तिम बात हैं।
अब बाकी रही क्या गया,
जब
चौपट ही हो गये?
पत्थर,
वृक्ष
और पशु-पक्षियों से मनुष्य में यही तो फर्क हैं कि यह बुद्धि रखता
हैं,
समझदार हैं-rational
being—हैं।
और भले-बुरे का विचार करता
हैं,
कर सकता
हैं।
मगर जब इसमें यही बात न रह गयी तो मनुष्य क्या खाक रहा?
तब तो चौपट
हो ही
गया।
अब सवाल यह
होता हैं कि तो आखिर किया क्या जाये?
अगर
किसी चीज का ख्याल न करें तो क्या पत्थर बन जायें?
यों तो
ख्याल करने पर पीछे देर से पत्थर बनने की नौबत आती हैं,
जैसा
अभी कहा हैं। बल्कि खामख्वाह पत्थर बन जाने की भी नौबत नहीं आती हैं।
हाँ,
मनुष्यता जरूर
चली जाती हैं। मगर यदि ख्याल करें ही न,
तब तो
सोलहों आना पत्थर बनी चुके। और अगर ऐसा नहीं करते तो शरीर-रक्षा एवं
जीवन-यात्र करते हुए मनुष्यता की भी रक्षा करने का कोई बीच का रास्ता
नजर आता नहीं। आखिर विवेकी के लिए भी तो शरीर,
इन्द्रियादि की रक्षा जरूरी हैं। नहीं तो विवेक-विचार वह करेगा क्या
खाक?
मगर इसके लिए
तो पदार्थों का ख्याल जरूरी हो जाता हैं। आखिर भूख लगने पर ही तो
खायेगा और प्यास लगने पर पानी पियेगा। मल-मूत्रदि का त्याग भी बिना
ख्याल के होगा नहीं। उधर ख्याल में आसक्ति का खतरा ही ठहरा। तो फिर
किया क्या जाये?
इसी का
उत्तर-इसी पहेली का समाधन-आगे के दो श्लोक इस तरह करते हैं-
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्।
आत्मवश्यैर्विधोयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥64॥
प्रसादे
सर्वदु:खानां हानिरस्योपजायेते।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि:
पर्यवतिष्ठते॥65॥
राग और द्वेष
से शून्य तथा अपने कब्जे में रहने वाली इन्द्रियों के द्वारा
(आवश्यक) विषयों को भोगने वाले पुरुष का तो मन अपने अधीन रहने के
कारण (चित्त की) प्रसन्नता (ही) प्राप्त होती हैं। प्रसन्नता होने पर
इस (मनुष्य) की सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि प्रसन्नचित्त
पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही सर्वथा स्थिर हो जाती हैं।
64।65।
यहाँ पर कई
बातें जानने योग्य हैं। पदार्थों के ख्याल या संसर्ग मात्र से ही कुछ
होता जाता नहीं। विरागी पुरुष भी तो आखिर खाता-पीता और जीवनयात्र
करता ही हैं। उसके दिमाग के सामने भी पदार्थ आते ही रहते हैं। मगर वह
तो चौपट होता नहीं?
क्यों?
इसीलिए
न,
कि पूर्व कथन
के अनुसार उसके भीतर पदार्थों के लिए रस नहीं हैं,
संग और
आसक्ति नहीं हैं,
राग-द्वेष नहीं हैं?
वह तो
पदार्थों से उदासीन रहता हैं। केवल अनिवार्य आवश्यकता से ही उनसे काम
लेता हैं। मलमूत्र त्याग का ही दृष्टान्त लें। हर आदमी के लिए यह
प्रतिदिन जरूरी बात हैं। मगर क्या कभी ऐसा भी देखा-सुना गया कि कोई
आदमी मल-मूत्र त्याग में आसक्ति रखता हो?
ऐसी तो
कभी होता नहीं। क्यों?
इसीलिए
न कि मजबूरन लोगों को यह काम करना ही पड़ता हैं। नहीं तो शरीर रहेगी न?
अनिवार्य आवश्यकता के अतिरिक्त इस काम में और कोई वजह होती ही नहीं।
इसीलिए उसमें फँसने का सवाल उठता ही नहीं। वैराग्ययुक्त विवेकी पुरुष
ठीक इसी तरह खानपान वगैरह भी करता हैं। उनकी नजर में मल-मूत्र त्याग
और खानपान आदि में जरा भी अन्तर नहीं हैं-दोनों ही शरीर-रक्षा के लिए
अनिवार्य हैं। उसे न तो मल-मूत्र में राग-द्वेष हैं,
आसक्ति
हैं,
चस्का हैं और
न खानपान आदि में ही। फिर वह फँसेगा क्यों?
बस,
यही
बात हमें करनी होगी यदि हम भी कल्याण चाहते हैं,
चौपट
होना नहीं चाहते और सभी अनर्थों से बचना चाहते हैं।
'रागद्वेषवियुक्तै:'
में जो
वियुक्त शब्द हैं वह यही बात बताता हैं कि हम इन बातों में जरा भी
चसकें न,
लिपटें न,
जैसा
कि मल-मूत्र त्याग में नहीं लिपटते।
पहले के
60वें
श्लोक में ''इन्द्रियाणि
प्रमाथीनि''
आदि
उत्तरार्ध्द में यह कहा गया हैं कि इन्द्रियाँ पुरुष को बेचैन कर
देती हैं,
मथ देती हैं
जैसे मथानी से दही मथा जाये और मन को जबर्दस्ती खींच ले जाती हैं।
मथने की बात हम 'व्यथयन्ति'
की
व्याख्या में बखूबी बता चुके हैं। उसका उल्टा यहाँ कह दिया हैं कि
'आत्मवश्यै:'-अर्थात्
इन्द्रियाँ अपने काबू में हो जाती हैं,
अपने
मन के अधीन रहती हैं। आत्मा का अर्थ स्वयं और मन दोनों ही हैं। जब
चस्का और राग-द्वेष नहीं हैं,
तो
इन्द्रियों को यह शक्ति होती ही नहीं कि मन को खींच सकें। क्योंकि
वही तो रस्सी हैं जिनके द्वारा उनके साथ मन जुटा हैं। इसीलिए जब
चाहती हैं उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। मगर वह रस्सी ही अब गयी हैं
टूट। फिर हो क्या?
मगर
मनीराम कौन से भले हैं?
यह
हजरत तो खुद इन्द्रियों की पीठ ठोंकते और ललकारते फिरते हैं कि
वाह-वाह,
खूब किया। ऐशी
दशा में यदि इन्द्रियाँ इनके हाथ आ गयीं तो इन्हें तो मजा ही हुआ। अब
पीठ ठोंकने में और भी आसानी जो होगी। इसलिए कह दिया हैं कि
'विधोयात्मा'।
असल में मनीराम यह काम जरूर करते। मगर वे तो खुद परेशान हैं। वे
आत्मा के सोलह आने कब्जे में जो हैं। इसीलिए कुछ कर नहीं सकते! कहाँ
तो 'आ
फँसे'
वाली हालत
हैं। असल में राग-द्वेष के खत्म होते ही सारी परिस्थिति ही उलट जाती
हैं। कहते हैं कि किसी ऊँटनी का बच्चा उसके साथ चलते-चलते जब थक गया
तो माँ से गिड़गिड़ा के बोला कि माँ,
जरा
ठहर जा। बहुत थक गया हूँ। थोड़ी दम तो मार लूँ। इस पर ऊँटनी ने उत्तर
दिया कि बेटे,
मैं भी
क्या कम थकी हूँ?
मैं भी
तो दम मारना चाहती हूँ। मगर मेरी नकेल दूसरे के हाथ जो हैं और वह
दाढ़ीजार रुकना नहीं चाहता। इसलिए बेबसी हैं। बस,
ठीक
यही हालत मन और इन्द्रियों की हैं। जब ये मन से पूछती हैं कि क्यों
भई,
हुक्म दो तो
जरा मजा लें,
तो
मनीराम चट कह बैठते हैं कि बोलो मत बहनो,
बड़ी
बेबसी हैं,
सारा
मजा किरकिरा हैं। वह और भी बिगड़ जायेगा।
इस तरह पहले
श्लोक के स्पष्टीकरण के बाद इसके तथा दूसरे के
'प्रसाद'
और सब
दु:खों की हानि की बात रह जाती हैं। दुनिया का नियम यही हैं कि कोई
भी अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा काम करने के बाद यदि मनस्तुष्टि या
चित्त की प्रसन्नता न हो तो वह काम बेकार माना जाता हैं और सारा
परिश्रम व्यर्थ ही समझा जाता हैं। विपरीत इसके अगर उसके बाद
प्रसन्नता हो गयी,
तबीअत
खुश हो गयी तो सब किया दिया सफल माना जाता हैं। इससे निष्कर्ष निकलता
हैं कि असली चीज भला-बुरा काम नहीं हैं,
किन्तु
उसके अन्त में होने वाली मनस्तुष्टि ही,
जिसे
यहाँ प्रसाद कहा हैं और
'प्रसन्नचेतस:'
में
प्रसन्नता भी कहा हैं। दोनों का अर्थ एक ही हैं।
बात यों हैं
कि वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार हृदय में या अन्त:करण में आत्मा का
लहलहाता प्रतिबिम्ब मानते हैं। जैसे साफ-सुथरे दर्पण मुख का
प्रतिबिम्ब पड़ता हैं और उसे देख के हम खुश या रंज होते हैं जैसा मुख
प्रतीत हो। ठीक उसी तरह सत्त्वप्रधान अन्त:करण का दर्पण भी चमकदार
हैं। उसी में आत्मा का प्रतिबिम्ब मानते हैं। आत्मा को आनन्द स्वरूप
भी मानते हैं। वह आनन्द का महान स्रोत हैं। इसीलिए आत्मा के
प्रतिबिम्ब का अर्थ हैं उसके आनन्दसागर का प्रतिबिम्ब। जो लोग उसका
अनुभव करते हैं वह आनन्द में मस्त रहते हैं-उसी में गोते लगाते रहते
हैं। वेदान्ती यह भी मानते हैं कि आनन्द या सुख तो केवल आत्मा में ही
हैं। केवल वही आनन्दरूप हैं। भौतिक पदार्थों में सुख का लेश भी हैं,
''यो
वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति''
(छान्दोग्य.
7।23।1)।
लेकिन जिस तरह
जल में पड़ा प्रतिबिम्ब तभी दीखता हैं जब जल निश्चल एवं निर्मल हो;
जरा भी
हिलता-डोलता न हो। वैसे ही आत्मानन्द का प्रतिबिम्ब तभी अनुभव में
आता हैं जब अन्त:करण निर्मल और निश्चल हो। आईना मैला और बराबर नाचता
हो तो प्रतिबिम्ब दिखेगा कैसे?
इसीलिए
योगी और आत्मदर्शी लोग बराबर ही चित्त की शान्ति और निर्मलता की
कोशिश करते हैं। गीता ने भी इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया हैं।
राग-द्वेष आदि ही चित्त की मैल हैं। उसकी चंचलता तो सभी को विदित
हैं। क्षण भर में दिल्ली से कलकत्ता और वहाँ से तीसरी जगह जा पहुँचता
हैं। कहीं भी टिकना तो वह जानता ही नहीं। बन्दर या पारे से भी ज्यादा
चंचल उसे कहा गया हैं। बिजली से भी ज्यादा तेज वह दौड़ता हैं।
अब रही विषय
सुख या भौतिक पदार्थों से मिलने वाले सुख की बात। वेदान्तियों का
इसमें कहना यही हैं कि जब मनुष्य को किसी चीज की सबसे ज्यादा चाट
होती हैं तो वह दिन-रात उसी का ख्याल करता रहता हैं। इस प्रकार उसका
मन एकाग्र हो जाता हैं। फलत: अन्त:करण की चंचलता दूर हो जाने के कारण
उसमें आत्मानन्द का लहलहाता प्रतिबिम्ब नजर आता हैं। मगर मन निश्चल
एवं एक ही जगह बँधा होने पर भी बाहर की उसी चीज में लगा हैं जिसकी
चाट या प्रचण्ड अभिलाषा हैं। इसीलिए उस आत्मानन्द को अनुभव कर नहीं
सकता,
उसे देख या
जान नहीं सकता। वह बाहर जो टँगा हैं। भीतर आ जो नहीं सकता। मगर ज्यों
ही वह चीज मिली कि चट भीतर लौटा और उस आत्मानन्द का अनुभव करके मस्त
हो जाता हैं। इस तरह उसे जिस आनन्द का अनुभव होता हैं वह तो
आत्मानन्द ही हैं। फिर भी अभिलषित पदार्थ के मिलने पर ही उसका अनुभव
होने के कारण ऐसा भ्रम हो जाता हैं,
ऐसा
माना जाने लगता हैं कि उस पदार्थ में ही आनन्द हैं। उस पदार्थ के ही
चलते मन- अन्त:करण-की एकाग्रता हुई हैं जरूर। इसीलिए आत्मानन्द का
अनुभव भी हुआ हैं। इसीलिए उस विषय को आनन्द के अनुभव का सहकारी कारण
भले ही माना जाये। मगर उसमें आनन्द तो हर्गिज नहीं हैं। ऐसा मानना तो
सरासर भ्रम हैं। आनन्द तो केवल भूमा में हैं-महान से भी महान पदार्थ
रूपी आत्मा में ही हैं।
यही कारण हैं
कि एक ही चीज से एक आदमी को आनन्द मिलता हैं और दूसरे को नहीं। यदि
आनन्द उस वस्तु का स्वभाव होता,
उस
वस्तु में ही रहता तो अग्नि की गर्मी की तरह सभी को समान रूप से ही
उसका अनुभव होता। परन्तु ऐसा होता नहीं। खूब भूखे आदमी को भरपेट
सत्तू या सूखी रोटी खिलाइये तो वह आनन्द-विह्नल हो उठता हैं। लेकिन
अमीर का तो वही चीजें देख के भी कष्ट होता हैं,
खाने
की तो बात ही जाने दीजिए। यदि भौतिक पदार्थ में ही आनन्द होता तो ऐसा
कदापि न होता। इसी तरह वही हलवा-पूड़ी भूखे को खिलाइये और पेटभरों को
भी। भूखे तो खा के आनन्द से लोटपोट हो जायेगे। मगर पेटभरे लोग आनन्द
मनाने या खुश होने के बदले उसमें हजार ऐब ही निकालेंगे कि पूड़ी जरा
नर्म सिंकी,
खर न
थी,
घी अच्छा न था,
सूजी
खराब थी,
कुछ अच्छी
गन्ध आती न थी,
मालूम
होता हैं चीनी खाँटी न थी,
घी
शुद्ध न था,
आदि-आदि। क्यों?
इसीलिए
न,
कि भूखे का मन और अन्त:करण उस अन्न की रट लगाये एकाग्र था,
निश्चल
था;
फलत: उसे पाते
ही उसने आत्मानन्द का उक्त रीति से पूर्ण अनुभव किया?
मगर
पेटभरों का मन तो एकाग्र था नहीं। क्योंकि हलवा-पूड़ी की रट थी नहीं।
उनका पेट जो भरा था। इसीलिए वह चीजें मिलने पर भी उनमें कोई फर्क न
हुआ। इसीलिए उनका मन आत्मानन्द का अनुभव कर न सका। वह तो बन्दर की
तरह पहले भी दौड़ता रहा और खाने के समय एवं उसके बाद भी। फिर
आत्मानुभव हो तो कैसे?
वह
आनन्द मिले तो कैसे?
देखा जाता हैं
कि सूखी हड्डी को कुत्ता चबाता हैं। उसमें कुछ रस तो होता नहीं। केवल
हड्डी की महक से कुत्तो को ख्याल होता हैं कि जिस तरह ताजी और रसीली
हड्डी में खून का रस मिलता हैं उसी तरह इसमें भी मिलेगा। इसीलिए खूब
जोर से उसे चबाता हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो और भी जोर लगाता हैं।
नतीजा यह होता हैं कि हड्डी की नोकों से उसके जबड़े छिल जाते हैं और
उनका खून हड्डी में टपक पड़ता हैं। कुत्ता उसी को चाट के खुश होता
हैं। फिर तो पहले से भी ज्यादा जोर लगाता हैं। फलत: और भी जख्म होते
हैं जो ज्यादा खून टपकाते हैं। यही बात देर तक चलती हैं जब तक वह थक
के छोड़ नहीं देता। कुत्ता अपने ही खून को मिथ्या ही हड़डी का समझ के
खुश होता हैं। क्योंकि अपने खून का स्वाद उसे उस हड़डी के ही बहाने
मिल पाता हैं। इसी से उसे भ्रम होता हैं कि हड़डी में ही खून हैं।
ठीक इसी तरह हरेक आदमी हमेशा मौका पड़ने पर अपने ही आत्मानन्द का
अनुभव करता हैं। मगर स्वतन्त्र रूप से ध्यान और समाधि के द्वारा वह
आनन्द लूटने का शऊर तो उसे होता नहीं। वह तो विषयों के बहाने ही उसे
कभी-कभी लूटता हैं,
उसका
अनुभव करता हैं। इसीलिए उसे भ्रम हो जाता हैं कि विषयों-भौतिक
पदार्थों-में ही सुख हैं। उसे अनुभव भी उस आत्मानन्द के एक तुच्छ कण
का ही हो पाता हैं क्योंकि जरा सी देर के बाद ही उसका मन फिर चंचल जो
हो जाता हैं। वह उसमें डूब तो सकता नहीं। इसीलिए वृहदारण्यक के चौथे
अध्याय में लिखा हैं कि इसी परमानन्द के एक छींटे से सारे संसार का
काम चलता हैं-''एषोऽस्य
परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रमुपजीवन्ति''
(4।5।32)।
इस लम्बे
विवेचन से यह साफ हो गया कि चित्त की प्रसन्नता ही असल चीज हैं। उसके
होते ही परमानन्द का अनुभव होने लगता हैं। फिर तो संसार के सारे कष्ट
भाग जाते हैं मन तो एक ही होता हैं न?
और जब
वही आत्मानन्द में डूब चुका तो दु:खों का अनुभव कौन करे?
''इक
मन रह्यो सो गयो स्याम संग कौन भजै जगदीस''?
और जब
अनुभव होता ही नहीं,
तो
दु:ख रही क्या चीज?
वह
अन्न-वस्त्रदि की तरह कोई स्थायी या ठोस चीज तो हैं नहीं?
वह एक
विलक्षण प्रकार की मानसिक वृत्ति ही तो हैं,
जिसका
अस्तित्व उसके अनुभव के साथ ही रहता हैं। अनुभव के बिना वह लापता
रहता हैं,
लापता हो जाता
हैं। इस तरह जब मन आत्मानन्द में डूबा हैं तो दु:ख रूपी उसकी वृत्ति
भी हो इसका मौका ही कहाँ रहा?
इसकी
फुर्सत ही कहाँ रही?
जब
आत्मज्ञानी या योगी राग-द्वेष में बँधाता नहीं तो उसके मन की
एकाग्रता हमेशा ही बनी रहती हैं। उसमें बाधा तो कभी पड़ती नहीं। वह
निरन्तर अविच्छिन्न रहती हैं। इसीलिए आत्मानन्द का अनुभव भी निरन्तर
अविच्छिन्न रहता हैं। मन वश में हैं यह तो
'विधोयात्मा'
से
स्पष्ट ही हैं। इसीलिए कह दिया हैं कि सभी तकलीफों का खात्मा हो जाता
हैं। न तो मानसपटल की गम्भीरता कभी भंग होती हैं और न यह बला आती
हैं। इसी अविच्छिन्न गम्भीरता का ही नाम प्रसाद हैं।
जिनने गौर से
'ध्यायतो
विषयान्'
आदि दो
श्लोकों को पढ़के उसी तरह बाद के
'रागद्वेषवियुक्तैस्तु'
आदि दो
श्लोकों को भी पढ़ा होगा उन्हें साफ पता लगा होगा कि पहले दो श्लोकों
में जो बात शुरू की गयी थी कि रागद्वेषादि के वशीभूत होने से कैसी
दुर्गति होती हैं,
उसी के
बीच में ही बादवाले दो श्लोकों के जरिये सिर्फ एक शंका को दूर किया
गया हैं जो उठ खड़ी हुई थी और जिसका स्वरूप हम अच्छी तरह बता चुके
हैं। वह शंका एकाएक उठ गयी और मौजूँ भी थी। इसीलिए अपनी बात पूरी न
करके पहले उसी का उत्तर देना जरूरी हो गया। तभी तो श्रोता आगे की उस
प्रधान विषय से सम्बन्ध रखने वाली बातें अच्छी तरह सुन सकेगा। इसीलिए
बादवाले श्लोकों के शुरूवाले शब्द के साथ ही
'तु'
जुटा
हुआ हैं। इसका अर्थ
'तो'
होता
हैं। यह वहीं आता हैं जहाँ बीच में ही कोई दूसरी या उलटी बात
प्रासंगिक रूप में खड़ी हो जाये और जिसका उत्तर देना जरूरी हो जाये।
ऐसी बात आगे भी गीता में
''यस्त्वात्मरतिरेव''
(3।17)
आदि
श्लोकों में आयी हैं। इसीलिए असली प्रसंग अभी पूरा नहीं हुआ हैं यह
तो मानना ही पड़ेगा।
जो लोग ऐसा
समझते हों कि वह प्रसंग तो पहले के उन दो ही श्लोकों में पूरा हो गया
उन्हें जरा भी सोचने पर अपनी भूल मालूम हो जायेगी। देखिये न?
उन
दोनों के अन्त में यही तो कहा जाता हैं-'बुद्धिनाशात्प्रणाश्यति'।
मगर क्या अर्थ हैं?
अगर
पत्थर में बुद्धि नहीं हैं तो क्या वह चौपट हो गया?
ऐसा
कौन मानता हैं?
विपरीत
इसके बुद्धि न होने से ही तो उसे तकलीफ-आराम किसी बात का अनुभव नहीं
होता। यह तो मानते ही हैं कि यह अनुभव ही तो संसार हैं,
आफत
हैं,
बला हैं,
बुरी
चीज हैं। आनन्द का अनुभव तो होता भी शायद ही हैं। होता तो हैं अधिकतर
कष्ट का ही। इसलिए इस दृष्टि से तो पत्थर अच्छा ही ठहरा । और आत्मा
तो सर्वत्र हैं,
सभी की
हैं यह कही चुके हैं। फिर पत्थर उससे जुदा कैसे माना जायेगा?
इसलिए
चौपट होने का मतलब क्या?
और क्या
पागलों में मस्ती नहीं होती?
उनकी
समझ चली गयी और वे सभी आफतों से अलग हो गये! मौज में विचरते फिरते
हैं! नंगे हैं तो भी फिक्र नहीं हैं! गालियाँ पड़ रही हैं या आशीर्वाद
मिल रहा हैं। मगर लापरवाह और बेगम हैं! फिर यह कैसे कहा जाये कि
बुद्धि या समझ के चले जाने से ही मनुष्य नष्ट हो जाता हैं
?
यह भी नहीं कि
पागल लोग फौरन मर जायें। वे तो बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं,
जैसे
दूसरे लोग। हाँ,
यह
जरूर होता हैं कि सभी रोग-बीमारियाँ लापता हो जाती हैं। लेकिन यह तो
मनमाँगा वरदान ही समझिये।
एक बात और भी
हैं। माना कि राग-द्वेष छोड़ के और उनके फन्दे में हर्गिज न पड़ के ही
शरीरोपयोगी पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मगर क्या इतने से ही सब
आफतें खत्म हो जायेगी?
जन्म-जन्मान्तर के संस्कार और राग-द्वेषों के बीज तो अन्त:करण में
पड़े ही रहते हैं। वह एकाएक तो चले जाते नहीं। इस शरीर में भी अभी-अभी
हमने आसक्ति छोड़ के पदार्थों का सेवन शुरू किया हैं। मगर इससे पहले
तो यह बात थी नहीं। तब तो आसक्ति थी ही। उसी के करते दिमाग में पहले
के पदार्थ बैठे हैं जो खामख्वाह उमड़ पड़ेंगे और दिक करेंगे। आखिर सपने
की तकलीफें ऐसी ही तो होती हैं। दिमाग में बीज रूप में पड़े पदार्थ ही
तो सपने में उभड़ के जाने कौन-कौन सी आफतें ढाते रहते हैं। राग-द्वेष
रहित हो के खानपान करने वाले के भी ये सपने कायम ही रहते हैं। वे
एकाएक तो मिट जाते नहीं। फिर क्या हो?
यह
गन्दगी धुले कैसे?
मिटे
कैसे?
किस साबुन से
अच्छी तरह रगड़ के धोई जाये?
यह तो
हजारों जन्मों की पुरानी मैल हैं न?
इसीलिए
इसे हटाने में बहुत ज्यादा मेहनत,
बार-बार की लगातार रगड़ दरकार होगी। सो क्या हैं यह तो मालूम हैं
नहीं।
और जो यह कह
दिया कि स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता हैं-'स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाश:',
इसके
क्या मानी हैं?
क्या
सचमुच ज्ञान रही नहीं जाता और आदमी पत्थर हो जाता हैं?
यह बात
तो ठीक नहीं। क्रोध के बाद भी आदमी तो आदमी ही रहता हैं। रोज ही यह
बात देखी जाती हैं। फिर पत्थर होने की कौन सी बात?
और अगर
यह नहीं हैं तो बुद्धि के नाश के मानी भी क्या हैं?
किस
क्रोधी की बुद्धि खत्म हो जाती हैं?
थोड़ी
देर तक खास ढंग का कोई पर्दा सा पड़ा रहता हैं। मगर पीछे तो पीछे,
उस समय
भी समझदारी के दूसरे काम तो वह करता ही रहता हैं। आखिर उस समय भी
उसके सभी काम पागलों जैसे ही होते नहीं। यह ठीक हैं कि वह कुछ काम उस
समय बेविचार के-विवेकशून्य-कर डालता हैं जिससे मुसीबतें बढ़ जाती हैं।
इसी तरह बढ़ती रहती हैं भी। मगर इसे बुद्धिनाश तो कभी नहीं कह सकते।
उसकी बेचैनी और परेशानी जरूर बढ़ जाती हैं,
इसमें
कोई शक नहीं हैं। इसके करते यह भी सम्भव हैं,
उसे
आराम न मिले। ऐसा ही प्राय: होता भी हैं। बेचैनी और परेशानी की आग बढ़
जाने पर चैन कहाँ?
आराम
कहाँ?
मगर वह चौपट
नहीं होता। उसे बुद्धि भी रहती ही हैं।
इस तरह की
अनेक बातों के रहते ही,
और
सुनने वाले के मन में इस प्रकार की शंकाओं के बनी रहने पर भी यह कह
देना कि मूल प्रसंग पहले दो श्लोकों में ही पूरा हो गया,
कोई
मानी नहीं रखता। इसीलिए आगे के श्लोक उसी बात को पकड़ के यही बातें
खुद पेश करते और इनसे बचने के उपाय सुझाते हैं। हमें यहीं पर यह जान
लेना होगा कि जो कुछ अभी कहा गया हैं अगले श्लोक उसे मानते हैं।
बुद्धिनाश का वही मतलब हैं जो अभी कहा गया हैं। उस समय विवेक से काम
लिया जा सकता नहीं। इस तरह बेचैनी और मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। और जो
आदमी मुसीबतों में घिरा हैं वह तो मरने से भी बदतर हैं। उससे तो मरा
कहीं अच्छा। अशान्त जीवन तो जहर ही समझिये,
चौपट
ही मानिए। आखिर शान्ति ही तो असल चीज हैं न?
आगे के
श्लोकों ने जन्मजन्मान्तर के पुराने संस्कारों और राग-द्वेष के बीजों
को जलाने के लिए-इस गहरी से गहरी गन्दगी को मिटाने के लिए-जिस नये
साबुन का नाम लिया हैं,
जिस
लगातार चिरकालीन रगड़ का आविष्कार किया हैं उसे भावना कहते हैं। यही
नाम उसे दिया भी हैं। जैसे रंग को गाढ़ा करके कपड़े पर चढ़ाने में कपड़े
को रह-रह के रंग में डुबोते और सुखाते हैं। सोने को भी रह-रह के गर्म
करके पानी में डुबाते और इस तरह उसे टंक बनाते हैं। मामूली लोहे को
भी बार-बार आँच दे के पीटते और पानी में डुबाते हैं ताकि इस्पात हो
जाये। ठीक यही बात रागद्वेषादि मैलों को धो बहाने के लिए भी की जाती
हैं,
करनी पड़ती
हैं। बार-बार सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करके मन को रोकते और
आत्मतत्त्व-में ही लगाते हैं। हर मौके पार सजग रह के यही करते हैं।
इसे ही पातंजल योग में ध्यान,
धारणा
और समाधि कहा हैं। इन तीनों को मिला के संयम नाम दिया हैं-'त्रयमेकत्र
संयम:' (3।4)
गीता
ने भी आगे 'संयमी'
(2।69)
में
यही कहा हैं। इनमें ध्यान नीचे दर्जे की चीज हैं। उसके बाद धारणा
आती हैं। ध्यान करते-करते मजबूती आने पर धारणा और उसकी मजबूती होने
पर समाधि का समय आता हैं। इन तीनों के पूरा होने पर-संयम की पूर्णता
हो जाने पर-अन्त:करण की,
बुद्धि
की सारी की सारी युग-युगान्तर की मैल जल-धुल जाती हैं। फिर तो वह
निर्मल हीरे की ही तरह धाप्-धाप् हो जाती हैं। इसके बाद अखण्ड
विज्ञान का व्यापक एवं सनातन-अचल-प्रकाश होता हैं। इसीलिए पतंजलि ने
भी कहा हैं-'तज्जयात्
प्रज्ञालोक:' (3।5)।
उस प्रचण्ड प्रकाश-उस द्वादश आदित्य-के सामने अज्ञान और अन्धकार का
पता कहाँ?
इसी संयम,
इसी
भावना के करते मन आत्मा के ही रंग में रंग जाता हैं-कभी भी ईधर-उधर
टस से मस नहीं होता। उसमें अब ऐसा करने की योग्यता एवं शक्ति ही नहीं
रह जाती हैं। इसीलिए निर्वात समुद्र के जल की तरह एकरस,
गम्भीर
और शान्त रहता हैं। उसकी यह निश्चलता,
निष्क्रियता,
शान्ति
अखण्ड हो जाती हैं। फलत: योगी उसमें लहलहाते आत्मानन्द का अनुभव
दिन-रात सोते-जागते करता ही रहता हैं। एक क्षण के लिए भी उसके सामने
से वह आनन्द-वह मजा-ओझल हो पाता नहीं,
हो
सकता नहीं। मगर जो यह नहीं कर सकता हैं;
जिसे
भावना का अवसर नहीं मिला वह हमेशा बेचैन और परेशान रहता हैं,
अत्यन्त अशान्त रहता हैं। फिर उसे सुख कहाँ?
उसे
सुख मयस्सर क्यों हो?
हमें यह भी
जान लेना होगा कि इस भावना के लिए विवेक की तो जरूरत हुई। वही तो
इसके मूल में हैं। जब तक हमें बखूबी आत्मतत्त्व का और रागद्वेषादि का
पता न चल जाये और यह न मालूम हो जाये कि इनमें कैसे फँसते हैं तब तक
हम मन को रँगेंगे कैसे?
तब तक
उसे सब आफतों से खींच के आत्मा या कर्म में ही लगायेंगे कैसे?
सभी
बातें जान लेने पर ही तो आगे कदम बढ़ायेंगे। इसीलिए भावना के पहले
बुद्धि या विवेक जरूरी हैं। रँगने की सारी प्रक्रिया अच्छी तरह जब तक
न जाने सुन्दर रंग चढ़ायेगा कैसे?
मगर यही
बुद्धि चौपट होती हैं जिस रीति से उसी का वर्णन पहले
'ध्यायतो
विषयान्'
में किया गया
हैं। इसलिए वहाँ कहे गये विषयों के ख्याल से लेकर स्मृति-विभ्रम तक
की सारी बातें,
जिनका
परिणाम बुद्धि नाश हैं,
एक ही
जगह मिला के योगभ्रष्टता कहते हैं। छठे अध्याय में जिस योगभ्रष्ट और
योगभ्रष्टता की बात कही गयी हैं वह भी कुछ इसी तरह की चीज हैं। उसमें
पातंजल योग भी भले ही आ जाये। मगर यह तो हुई,
यह बात
पक्की हैं। यदि हम गौर से उन सभी बातों को देखें जो इन दो श्लोकों
में लिखी हैं तो हमें मानना ही होगा कि जो लोग गीतोक्त योगी नहीं
होते हैं,
मुक्त नहीं
होते हैं,
किन्तु उस
स्थान से गिर पड़ते और पतित हो जाते हैं-च्युत और अयुक्त हो जाते हैं,
उन्हीं
में ये बातें अक्षरश: पाई जाती हैं। फलत: उन्हें बुद्धि होती ही
नहीं। फिर भावना कैसी?
भावना
के अभाव में शान्ति भी कहाँ?
और जब
शान्ति ही नहीं,
तो सुख
कैसा?
आनन्द कहाँ?
यही
बात आगे के 66वें
श्लोक में कहने के उपरान्त बादवाले दो श्लोकों में इसी का विवरण दे
के उपसंहार किया हैं।
नास्ति
बुद्धिरयुक्तस्य
न चायुक्तस्य भावना।
न
चाभावयत: शान्तिरशान्तस्य कुत: सुखम्॥66॥
अयुक्त को
बुद्धि ही नहीं होती। जिसे बुद्धि ही न हो उसे भावना भी नहीं होती।
जिसे भावना न हो उसे शान्ति नहीं मिलती। जिसे शान्ति ही नहीं उसे सुख
कहाँ?66।
यहाँ एक जरा
सी बात सोचने की हैं। श्लोक के देखने से पता चलता हैं कि यहाँ कोई
ऋंखला हैं जिसकी लड़ें एक के बाद दीगरे आयी हैं। यदि नीचे से ही शुरू
करें तो सुख के पहले शान्ति तथा उसके पहले भावना की तीन लड़ें मिल
जाती हैं। शुरू में भी योग के बाद बुद्धि के आने से योग और बुद्धि की
भी लड़ें जुटती हैं। मगर बीच में
'न
चाबुद्धस्य भावना'
कहने
के बजाये 'न
चायुक्तस्य भावना'
कह
दिया हैं,
जिससे बुद्धि
के साथ भावना की लड़ी जुट जाने से आगे भावना से शान्ति की जुटान आदि
को ले के पूरी ऋंखला तैयार हो जाने के बजाये टूट सी जाती हैं,
प्रसंग
विशृंखल हो जाता हैं। यह कुछ ठीक जँचता भी नहीं कि योग का बुद्धि से
और बुद्धि का ही भावना से सीधा सम्बन्ध जोड़ने के बजाये योग का ही
सीधा सम्बन्ध दोनों से जुटे। यह असम्भव सा भी लगता हैं। क्योंकि यदि
योग जुट चुका हैं बुद्धि के साथ,
तो फिर
भावना से कैसे जुटेगा?
और अगर
ऐसा मानें भी तो फिर शान्ति और सुख के साथ भी उसी को सीधे क्यों न
जोड़ा जाये?
इसीलिए
हमने दूसरे अयुक्त शब्द का अबुद्ध ही अर्थ किया हैं और कहा हैं कि
बिना बुद्धि के भावना होती ही नहीं। असल में,
जैसा
कि पहले ही कह चुके हैं,
योग
में भी बुद्धि ही वास्तविक चीज हैं। इसीलिए
'बुद्धियोगाद्धनंजय'
(2।49)
में
बुद्धि को ही योग कहा भी हैं। इसीलिए जान पड़ता हैं,
यहाँ
भी 'अबुद्धस्य'
की जगह
'अयुक्तस्य'
कह
दिया हैं। ताकि बुद्धि पर ही जोर दिया जा सके।
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते।
तदस्य
हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि॥67॥
क्योंकि
(विषयों में) रमने वाली इन्द्रियों के पीछे जब मन लग जाता-चल
जाता-हैं तो (अपने साथ ही) बुद्धि को भी (विवश करके) वैसे ही खींच
लेता हैं जैसे मझधार में पड़ी नाव को वायु (विवश करके ईधर-उधर खींचता
और अन्त में डुबो देता हैं)।67।
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश:।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥68।
इसीलिए हे
महाबाहो,
जिसकी सभी
इन्द्रियाँ (अपने-अपने सभी) विषयों से पूरी तरह खींच ली गयी हैं उसी
की बुद्धि स्थिर होती हैं।68।
इन दो श्लोकों
में दो बातें हैं,
जिन पर
दो शब्द कह देना हैं। जिस तरह हवा के झकोरे में पड़ी नाव विवश हो के
ईधर-उधर भटकती और अन्त में डूबती या छिन्न-भिन्न होती हैं;
फिर भी
नाववाले कुछ कर नहीं सकते। ठीक उसी तरह इन्द्रियों का साथी मन हो
जाने पर हालत होती हैं। बुद्धिरूपी नाव के लिए इन्द्रियों का वेग हवा
के झकोरे का काम करता हैं। उसकी सफलता के लिए जिस मझधार की जरूरत हैं
उसका काम वही मन पूरा कर देता हैं। मझधार न होने पर हवा के तेज से भी
तेज झोंके नाव का खाक नहीं बिगाड़ सकते। इन्द्रियाँ भी मनुष्य का कुछ
कर नहीं सकती हैं यदि उनका साथी मन न मिल जाये। मन के मिलने का अर्थ
ही हैं रागद्वेष-पूर्वक पदार्थों का भोगा जाना। फिर तो सब
ज्ञान-ध्यान खत्म। बुद्धि का भी होश फाख्ता ही समझिये। असल चीज यह
मनीराम ही हैं। यही जिधर चलते हैं उधर ही सब कुछ होता हैं। जब ये
इन्द्रियों की ओर चले तो बुद्धि पर भी वारंट जारी हुआ और जबर्दस्ती
बाँध-छान के उधर ही घसीटी गयी! और अगर ये हजरत बुद्धि की तरफ आ गये
तो इन्द्रियाँ बेकार सी हो गयीं। वे हाथ जोड़ें बुद्धि की ही मातहती
करती और हुक्म बजाती हैं। इन्हें तो खींचने की भी जरूरत नहीं होती।
खुद हाथ जोड़े हाजिर रहती हैं और बुद्धि के काम में मदद करती हैं। वह
तो अपना काम निर्बाधा करती ही रहती हैं।
इसलिए विषयों
से इन्द्रियों को बखूबी रोक रखने का यह मतलब हर्गिज नहीं हैं कि
खाना-पीना,
देखना-सुनना,
पढ़ना-लिखना सब कुछ बन्द हो जाये। तब तो आफत ही आ जायेगी और कोई भी
काम हो ही न सकेगा। आखिर भावना के लिए भी तो शरीरोपयोगी काम करना
जरूरी होता ही हैं। मर जाने से तो कुछ होगा नहीं। जबर्दस्ती करने में
तो मरने में भी फजीती होगी। श्लोक में
'निगृहीत'
शब्द
हैं। निग्रह कहते हैं दण्ड को। जिस तरह दणश्निडत आदमी,
बन्दी
या कैदी काम-धाम तो सब कुछ करता हैं;
मगर
उसकी आजादी जाती रहती हैं;
वह
तकुवे की तरह सीधा बन के शैतानियत छोड़ देता हैं। ठीक यही हालत
इन्द्रियों की होती हैं। ये भी कैदी की तरह हुक्म बजाती हैं,
सब कुछ
करती हैं,
और तकुआ बन
जाती हैं।
परन्तु यह बात
असम्भव जैसी मालूम होती हैं और साधारण आदमी के दिमाग में घुसती ही
नहीं। विषयों को जरूरत भर काम में इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा
लायेंगे भी और हमें कुछ पता भी न चलेगा कि इनमें क्या मजा हैं,
यह कुछ
अजीब बात हैं। जिन्हीं इन्द्रियों से विषयों को भोगेंगे,
उनका
अनुभव करेंगे वही तो उसी के साथ उनका मजा भी बताई देंगी। इसके लिए
उन्हें दूसरा काम,
दूसरा
यत्न तो करना होगा नहीं। यह काम एक ही साथ होगा। असल में भोग का अर्थ
ही हैं मजा लेना,
सुख-दु:ख का अनुभव करना। भोग इसी को कहते ही हैं-''सुखदु:खान्यतरसाक्षात्कारो
भोग:''।
फिर यह क्या बात कि मजा न आये;
हम
चसकें नहीं,
या मन
में ये बातें न आयें?
इसका उत्तर भी
सुन्दर हैं। जिसे फाँसी की सजा हो,
फाँसी
दी जाने वाली ही हो उसे आप चाहे सुन्दर से भी सुन्दर पदार्थ खिलाइये
और कोमल से भी कोमल शैया पर सुलाइये। मगर जरा पूछिये तो सही कि उसे
कुछ भी मजा आता हैं?
उसे तो
पता ही नहीं चलता कि वह क्या खा-पी रहा हैं और कहाँ सो रहा हैं। उसका
मन मौत में जा के अटक जो गया हैं। उसके सामने तो मौत बराबर खड़ी हैं।
जरा भी हटती नहीं। फिर मजा आये तो कैसे?
यहाँ
तो मौत आयी हुई हैं और हटती ही नहीं,
दूसरों
को जगह देती ही नहीं। इसी तरह नृत्यकला में कुशल नटी को खड़ा कीजिए और
उसकी कला की जाँच कीजिए तो देखिए क्या होता हैं। उसके सिर पर पानी से
भरा एक पात्र रख के बिना उसे हाथ से पकड़े नाचने को कहिये। वह बराबर
बाजे-गाजे के ताल-सुर में ही ठीक-ठीक नाचेगी,
जरा भी
फर्क न पड़ेगा। मगर उसका मन निरन्तर उस जलपूर्ण पात्र में ही लगा
होगा। नहीं तो जरा भी चूकते ही वह नीचे जा गिरेगा और नटी नृत्यकला की
परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जायेगी।
ठीक यही हालत
योगी,
समदर्शी और
आत्मतत्त्वज्ञ मस्तराम की भी समझिये। इनके मनीराम तो उधर ही टँगे
रहते हैं,
फँसे और लटके
रहते हैं। दूसरे काम की इन्हें फुर्सत हुई नहीं। फिर चस्का लगे तो
कैसे?
मजा आये तो
कैसे?
नटी के
ताल-सुरवाले नृत्य की तरह मस्तराम भी खाना-पीना सब कुछ करते ही हैं।
मगर मजा नहीं रहता,
रस
नहीं मिलता! उनके लिए सारी दुनिया जैसे अँधरे की चीज हो,
भादों
की घोर अँधियाली की बात हो। इसलिए जिन चीजों में दूसरों को मजा आता
हैं उनका उन्हें पता ही नहीं चलता। अँधियाली की चीजों का पता किसे
चले,
सिवाय उल्लू
के?
मगर जिस तरह मस्तराम लगे हैं,
जिधर
वे जगते हैं,
जिधर
उन्हें प्रखर प्रकाश और उजियाली हैं,
जहाँ
उनके लिए बिना लैम्प,
चाँद,
सूरज
और आग के ही खुद-ब-खुद अखण्ड प्रकाश हैं-'आत्मैवास्य
ज्योतिर्भवति', 'अत्रयं
पुरुष: स्वयंज्योतिर्भवति'
(वृहदा.
4।3।6-8),
वहाँ
बाकी लोगों के लिए काली अँधियाली हैं,
भादों
की रात हैं। फलत: वे लोग कुछ भी जान पाते नहीं। आखिर दोनों मजा
मारेंगे कैसे?
एक को
तो छोड़ना ही होगा। यही बात आगे का श्लोक कहता हैं।
''पश्यतो
मुनै:''
का अर्थ ही यह
हैं कि उसकी भीतरी आँखें बराबर खुली हैं-
या निशा
सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।
यस्यां
जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने:॥69।
सब लोगों के
लिए जो रात हैं उसमें संयमी-योगी-जागता हैं। (और) जिसमें लोग जागते
हैं निरन्तर भीतरी आँखें खुली रखने वाले उस मुनि-मननशील-के लिए वही
रात हैं।69।
इस तरह
पदार्थों के भोग की बात जो कही गयी हैं उसका निचोड़ कह देना जरूरी
हैं। क्योंकि सभी तो इतने गहरे पानी में उतर सकते नहीं कि इन
लम्बी-चौड़ी बातों को समझ सकें। साथ ही,
ऐसे
आदमी की क्या हालत रहती हैं जो औरों को भी साफ-साफ मालूम हो जाती हैं,
यह बता
देना भी जरूरी हैं। ताकि योगी भी अपने आपको लोकमत की तराजू पर बराबर
तौलता रहे। दूसरे लोग भी उसकी पहचान करके उससे फायदा उठा सकें,
कुछ
सीख सकें। इसीलिए नर्त्तकी या फाँसीवाले की अपेक्षा एक तीसरा
दृष्टान्त,
जो सब
दृष्टियों से अनुकूल हो,
पेश
करके 'कैसे
बैठता हैं'
प्रश्न
के उत्तर का और इस प्रसंग की सारी बातों का एक तरह का उपसंहार अगले
श्लोक में करते हैं। बचे-बचाये आखिरी प्रश्न
'कैसे
चलता हैं'
का उत्तर तो
उसके बादवाले श्लोक में दिया गया हैं।
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥70।
सभी तरफ से
निरन्तर पानी के आते रहने पर भी जिसका पानी जरा भी बढ़ता नजर नहीं आता
और ज्यों का त्यों बना रहता हैं-जिसमें जरा भी उफान नहीं आता,
ऐसे
समुद्र में घुस के उसी का रूप बन जाने वाले पानी की ही तरह सभी भौतिक
पदार्थ जिस (पुरुष) के पास आते हैं (और उसकी गम्भीरता में जरा भी
फर्क डाल नहीं सकते),
वही
शान्ति प्राप्त करता हैं,
न कि
पदार्थों के लिए हाय-हाय मचाने वाला।70।
इस श्लोक में
जो खूबी हैं वह यही कि इससे योगी और आत्मज्ञानी के बाहरी लक्षण का
पता लगने के साथ ही इसमें कही गयी बात बहुत मार्के की हैं। यहाँ
'समुद्रमाप:'
और
'यं
प्रविशन्ति'
में
द्वितीयान्त शब्द आये हैं
'समुद्रं'
तथा
'यं'।
हालाँकि-समुद्र में पानी जाता हैं,
इस
मानी में 'समुद्रे'
जैसी
सप्तमी विभक्ति चाहिए और
'यं'
की जगह
भी 'यस्मिन्'
चाहिए।
किन्तु वैसा कहने पर कुछ ऐसा मालूम होने लगता हैं कि चाहे जो हो,
फिर भी
पानी समुद्र में निराली ही चीज हैं। क्योंकि वह पानी के पात्र की तरह
आधार बन जाता हैं। पात्र में रहने वाले पानी की ही तरह वहाँ जाने
वाला भी उससे जुदा आध्य बनता हैं। मगर द्वितीय विभक्ति में यह बात
नहीं रह जाती हैं। उससे तो साफ ही मालूम होता हैं कि पानी समुद्र का
ही रूप बन गया-उसी में विलीन हो के तद्रूप बन गया। या यों कहिए कि
पानी अपने आप में ही जा मिला। इसी तरह पदार्थ भी जब योगी के पास
जायें तो ऐसा हो जाये कि अपने आपके ही पास आये हैं। क्योंकि आत्मा तो
सभी की हैं और योगी सभी की आत्मा बन चुका हैं,
वह
'सर्वभूतात्मभूतात्मा'
(5।7)
बन
चुका हैं। फिर अपने आपसे ही अपनी लड़ाई या अपने ही करते अपने में उफान
और बेचैनी कैसी?
वहाँ
तो भेद रही न गया। फिर बेचैनी का क्या सवाल?
वहाँ
तो मालूम पड़ता हैं,
न कोई
आया न गया! जैसी दशा पदार्थों के मिलने के पूर्व थी वैसी ही मिलने पर
और बाद में भी रह गयी! जरा भी फर्क नहीं आया!
विहाय
कामान्य: सर्वान् पुमांश्चरति नि:स्पृह:।
निर्ममो
निरहंकार: स शान्तिमधिगच्छति॥71॥
(इसलिए)
सभी पदार्थों को छोड़ के-उनकी जरा भी परवाह न करके-जो पुरुष नि:स्पृह
विचरता हैं और जिसमें माया-ममता-अहन्ता ममता-जरा भी नहीं होती,
वही
शान्ति प्राप्त करता हैं-उसी को शान्ति मिलती हैं।71।
अहन्ता और
ममता ही तो सारी खुराफातों की जड़ हैं। मैं और मेरा यही तो हैं अहन्ता
और ममता। अहम् और मैं,
मेरा
और मम एक ही अर्थ में आते हैं और यही हैं जहर जिससे सभी मरते हैं। यह
ख्याल ही हैं कालानाग जिसके डसते ही सभी मर जाते हैं। योगी में यही
नहीं होता। फिर पदार्थों की उसे क्या परवाह?
किसी
दण्डी महात्मा से जब एक ने,
जो बड़ा
मगरूर मालदार था,
पूछा
कि महाराज,
संन्यासी किसे कहते हैं?
तो
उन्होने चट उत्तर दिया कि तुमसे ले के ब्रह्मा तक को जो तृण के बराबर
भी न समझे वही संन्यासी हैं। यही लापरवाही और बेफिक्री मस्ती की असली
निशानी हैं। इसीलिए ऐसा आदमी मस्त हो के सर्वत्र विचरता हैं और
शान्ति उसके चरण चूमती रहती हैं। उसका तो मन जहीं जाता हैं वहीं
समाधि हैं-'यत्रयत्रमनोयाति
तत्रतत्रसमाधाय:'।
निर्मम के बारे में पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका हैं।
एषा
ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति॥72॥
हे पार्थ,
यही
ब्राह्मी स्थिति (कही जाती ) हैं। इसे हासिल कर लेने पर फिर मोह
नजदीक फटक सकता नहीं। अन्त समय में भी इस दशा में आ जाने वाला
(मनुष्य) निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता हैं।72।
यह श्लोक
आत्मविवेक और योग के समूचे निरूपण का और इसीलिए दूसरे अध्याय का भी
उपसंहार हैं। जिस मस्तीवाली हालत का वर्णन अभी-अभी किया हैं उसी का
नाम यहाँ ब्राह्मी स्थिति कहा गया हैं। चाहे उसे योगी की दशा कहिये,
स्थितप्रज्ञ और स्थिरबुद्धि की हालत कहिये,
युक्त
और मस्त की मौज कहिये,
साम्यावस्था या समदर्शन कहिये। सब एक ही बात हैं-एक ही चीज के अनेक
नाम हैं। इस मस्ती में आने पर प्रियतम,
सर्वप्रिय आत्मा या माशूक से सपने में भी जुदाई होती ही नहीं। फिर
मोह या भूलभुलैया कैसी?
इसीलिए
मस्तराम सदा मुक्त ही हैं। उसे कहीं आना-जाना हैं नहीं-न बैकुण्ठ,
न
ब्रह्मलोक। उसका तो शरीर ही उससे अलग होता हैं,
न कि
वह किसी से भी अलग हो सकता हैं। यह मस्ती यदि पहले से ही हो तो सोने
में सुगन्ध ही समझिये। नहीं तो शरीरान्त से पहले भी आ जाने पर
निर्वाण मुक्ति धारीधराई हैं। निर्वाण का अर्थ हैं जाने-आने से रहित।
उसकी तो आत्मा ब्रह्म रूप हुई। फिर आना-जाना कहाँ और कैसा?
इतिश्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रो
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगोनामद्वितीयोऽध्याय:॥2॥
श्रीमद्भगवद्गीता के रूप में (जो) उपनिषद रूपी ब्रह्मज्ञान प्रतिपादक
योगशास्त्र (हैं उस) में जो श्रीकृष्ण और अर्जुन का संवाद हैं। उसका
सांख्य-योग नामक दूसरा अध्याय यही हैं।
...अगला पृष्ठ
-
तीसरा अध्याय
(शीर्ष पर वापस)